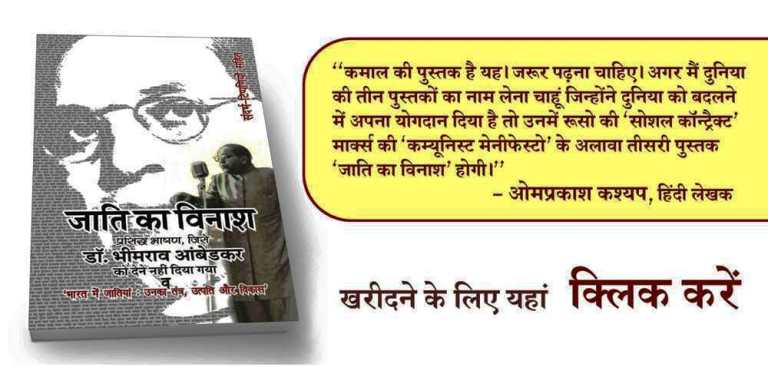महाराष्ट्रीय नवजागरण में निरंतरता
महाराष्ट्रीय नवजागरण में हमें एक ऐसी निरंतरता देखने को मिलती है जो भारत के और किसी प्रांत के नवजागरण में नहीं मिलती। ब्रिटिश शासन के तहत पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी मूल्यों से प्रेरित होकर भी महाराष्ट्रीय नवजागरण एक ओर अपने अतीत यानी तथाकथित मध्ययुग में हुए संतों भक्तों के आंदोलन से जुड़ा हुआ था, दूसरी ओर आगे उभरने वाले राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से भी कई अर्थों में जुड़ा। महाराष्ट्रीय नवजागरण का मराठी में एक नाम सुधारणा भी है। यानी धर्म और समाज का सुधार। महाराष्ट्र में 13वीं से 18वीं सदी तक चले संतों के आंदोलन को भी सुधारणा कहा जाता है। वह भी धर्म और समाज का ही आंदोलन था। इस तरह पेशवा शासन के उत्तरार्ध की अवधि में जबकि ब्राह्मणवाद बहुत मजबूत तथा जाति-प्रथा कठोर हो गई थी, इस अवधि को छोड़कर महाराष्ट्र में 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक सुधारणा का ही आंदोलन चलता रहा। 18वीं सदी तक यह संतों के नेतृत्व में चला तो 19वीं सदी में पश्चिमी शिक्षाप्राप्त मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में। यह निरंतरता सिर्फ इसके नाम की नहीं है। इसकी अंतर्वस्तु की भी है। इसे हम संतों के भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म की निरंतरता कह सकते हैं जिसके केंद्र में था जातिभेद का प्रश्न और महाराष्ट्रीय अस्मिता की चेतना। महाराष्ट्र में आगे उभरने वाली विभिन्न राष्ट्रवादी राजनीतिक धाराओं से महाराष्ट्रीय नवजागरण इस अर्थ में जुड़ा रहा कि जिन प्रश्नों और प्रवृत्तियों को लेकर 19वीं सदी का नवजागरण चल रहा था- जो प्रश्न और प्रवृत्तियां मूलतः आंदोलन की थीं- वे ही प्रश्न और प्रवृत्तियां 20वीं सदी की राजनीतिक धाराओं में भी अर्थपूर्ण बनी रहीं।
भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म के मूल्य बदले हुए राजनीतिक संदर्भों में भी प्रेरणादायक बने रहे। इसे तिलक और दूसरे मराठी राष्ट्रवादियों की राजनीति में देखा जा सकता है। सच पूछिये तो ये प्रवृत्तियां आज भी महाराष्ट्र से गायब नहीं हुई हैं। ऐसी निरंतरता हमें भारत के और किसी भी प्रांत में दिखायी नहीं देती। बंगाल में यह सिर्फ आंशिक रूप में मिलती हैं। वहां 19वीं सदी के आखिरी दशकों में उभरे राष्ट्रीय आंदोलन का ब्रह्मसमाज के नवजागरण से सजीव संबंध जरूर बना; लेकिन बंगाल के अतीत से; बंगाली संतों और भक्तों के आंदोलन से नवजागरण का कोई संबंध नहीं था। बंगाल में ब्रह्मसमाजियों ने सामान्य तौर पर सभी धर्मों और उनके महात्माओं के प्रति आदर प्रकट करते हुए वैष्णव धर्म और चैतन्य का नाम भी लिया है। लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। केशवचंद्र ने अपने जीवन के आखिरी सालों में रामकृष्ण परमहंस से आकर्षित होकर काली मां की रहस्यात्मक भक्ति की ओर जो थोड़ा रुझान प्रकट किया था, उसे साधारण ब्रह्मसमाजियों ने नवजगारण के मूल्यों से केशव के विचलन के रूप में ही देखा और इसके लिए केशव की आलोचना भी की गयी। बहुत बाद में बीसवीं सदी में जाकर रवींद्रनाथ ठाकुर बाउल गीतों से प्रभावित हुए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उभरी हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक भावनाओं के राजनीतिक संदर्भ में उन्हें बाउलों की मानववादी विचारधारा बहुत काम की चीज लगी। इन सबके बावजूद बंगला नवजागरण 15वीं, 16वीं सदी के बंगाली संतों-भक्तों के आंदोलन से उस अर्थ में कभी नहीं जुड़ा जिस अर्थ में महाराष्ट्रीय नवजागरण जुड़ा हुआ था। सच्चाई यह है कि 19वीं सदी में अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी शिक्षा और औपनिवेशिक शासन के प्रभाव में उभरा बंगाली शिक्षित वर्ग अपनी तथाकथित मध्ययुगीन विरासत से पूरी तरह से कटा हुआ नजर आता है। औपनिवेशिक शासन से पहले का समय उनके लिए अंधकारयुग और मुसलमानी अत्याचारों का युग ही रहा। यही बात हिन्दीभाषी अवध और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी दिखाई देती है जहां प्रांत के पश्चिमी हिस्सों में नवजागरण का नेतृत्व कर रहा आर्य समाज संतों-भक्तों की विचारधारा के सख्त खिलाफ था। सत्यार्थ प्रकाश में कबीर और नानक आदि संतों के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां मिलती हैं और तुलसी की रामचरितमानस को पाठ्यक्रम से प्रतिबंधित करने का सुझाव मिलता है। हालांकि हिन्दी भाषी प्रदेश में अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव बंगाल से आधा भी नहीं था, फिर भी ऐतिहासिक कारणों से क्या भारतेन्दु और क्या शिवप्रसाद, हिंदी के सभी बड़े लेखकों ने पूर्व औपनिवेशिक काल को मुसलमानों के अत्याचारों से भरे अंधकार युग के रूप में ही देखा। भक्ति आंदोलन से हिंदी नवजागरण का संबंध होने के एकाध संक्षिप्त और सतही दावों के बावजूद सवाल यह है कि भक्ति आंदोलन के जो केंद्रीय मुद्दे थे, जैसे दलितों में अपने मनुष्यत्व और आत्मगौरव की चेतना का विकास, ऊंच-नीच, जाति-पांति, छुआछूत, ब्राह्मणवाद की आलोचना, पुरोहिती, धार्मिक कर्मकांड इत्यादि के तीव्र विरोध की जो प्रखर अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में, खासकर कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य में हुई; उसका संबंध भारतेन्दु मंडल के लेखन से क्या और कितना रहा है?
बंगाल, महाराष्ट्र और हिन्दी भाषी प्रदेश की तुलना में गुजरात में स्थिति थोड़ी अलग दिखायी देती है। वहां 19वीं सदी के प्रखर सुधारक गोवर्धनराव त्रिपाठी ने 1894 में अपनी एक महत्वपूर्ण किताब ‘क्लासिकल पोएट्स आफ गुजरात एंड दियर इन्फ्लुएंस आन सोसायटी एंड मोरल’ में 15वीं से 18वीं सदी तक के गुजराती भक्ति काव्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। गोवर्धनराम ने 17वीं सदी के तीन गुजराती कवियों आखो, प्रेमानंद और सामल को सबसे ज्यादा महत्व दिया। जाति-पाति और सामाजिक हैसियत के बजाय भक्ति के आधार पर भक्तों के बीच समानता के विचार की प्रशंसा करते हुए गोवर्धनराम ने उपरोक्त तीनों कवियों में धार्मिक सामाजिक रुढ़ियों के खिलाफ मिलने वाले तत्वों को, खासकर पितृसत्तात्मक मूल्यों के खिलाफ सामल के स्त्री चरित्रों में अपने प्रेम के लिए मिलने वाले सामाजिक विद्रोह के भावों को, साफतौर पर आधुनिक मानते हुए सवाल पूछा है कि जिस आधुनिकता के लिए हम अंग्रेजी राज की तारीफ करते हैं, वही आधुनिकता क्या 17वीं सदी के इन भक्त कवियों में नहीं दिखायी देती? इस लिहाज से 19वीं सदी ज्यादा विकसित है या 17वीं सदी? भक्तिकाव्य के इस असाधारण मूल्यांकन के बावजूद गोवर्धनराम 19वीं सदी के गुजराती नवजागरण और 17वीं सदी के गुजराती भक्ति आंदोलन के बीच न तो किसी निरंतरता का दावा करते हैं और न कोई विशेष संबंध देखते हैं। इसके उल्टे उनकी शिकायत यह है कि 17वीं सदी के संत भक्तों से कोई प्रेरणा न लेकर 19वीं सदी के हिंदू सुधारक आधुनिक बनने के लिए अंग्रेजों की ओर देखते रहते हैं। इस तरह वे अपनी विरासत से अनजान और कटे हुए लगते हैं। गुजराती नवजागरण की इस स्थिति से ठीक उल्टी स्थिति है महाराष्ट्रीय नवजागरण की जहां नवजागरण के सभी नेता बहुत सचेत रूप से अपनी भक्तिकालीन विरासत से खुद को जोड़ते और उस पर अपना दावा जताते दिखायी देते हैं।
19वीं सदी के महाराष्ट्रीय सुधारकों ने अपने नवजागरण को संतों की जिस विरासत से जोड़ा, उसकी तीन विशेषतायें गौरतलब हैं- भागवतधर्म, महाराष्ट्रीय अस्मिता और महाराष्ट्रधर्म। यहां बहुत संक्षेप में इनकी चर्चा कर लेना जरूरी है।
महाराष्ट्र में 12वीं सदी में संत चक्रधर के महानुभाव संप्रदाय से शुरू हुआ भक्ति आंदोलन कुछ खास कारणों से आगे लोकप्रिय नहीं हो सका। लेकिन उनके बाद अपने वाले वरकरियों का भागवतधर्म बहुत प्रभावशाली और लोकप्रिय हुआ। वरकरियों की परंपरा नासिक के पास पंढरपुर में विठोबा या विट्ठल की भक्ति करने और हर साल इस जगह की यात्रा करने की परंपरा मूलतः पांचवीं सदी से चली आ रही थी। 13वीं सदी में नाथ संप्रदाय से आये ज्ञानदेव जब इससे जुड़ गये तो इस परंपरा का प्रभाव बहुत बढ़ गया। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ने संस्कृत के दार्शनिक ग्रंथ श्रीमद्भगवतगीता का मराठी में स्वतंत्र पद्यानुवाद करके जिस भावार्थदीपिका की रचना की, वह ज्ञानेश्वरी के नाम से मशहूर हुई और उसमें निरूपित भागवतधर्म महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का दूसरा नाम हो गया। एक रामदास को छोड़कर दूसरे सभी संतों ने- नामदेव, एकनाथ और तुकाराम वगैरह ने- इसी भागवतधर्म का प्रचार किया। वैदिक परंपराओं का आदर करने वाला यह भागवतधर्म में समाज में वर्णाश्रम के पालन को स्वीकार करता था, लेकिन धर्म और भक्ति के क्षेत्र में यह जाति-पांति को महत्व नहीं देता था। इसने सभी वर्णों और जातियों के लोगों को विट्ठल की भक्ति के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और समाज के निचले व्यक्ति में भी नैतिक आचरण और भक्ति भावना के जरिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का आत्मविश्वास जगाया। भागवतधर्म के प्रचारक संतों ने कहा कि धर्म और भक्ति के क्षेत्र में जाति, कुल, वंश और ओहदे का कोई महत्व नहीं; यहां तो हृदय की पवित्रता और भक्ति की उत्कटता ही एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व है। ईश्वर जात-पांति नहीं देखता, वह सिर्फ अपने भक्त की सच्चाई देखता है। वरकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वर और एकनाथ जैसे ब्राह्मण संत हुए तो नामदेव दर्जी, तुकाराम कुनबी, चोखामेला महार और गोरा कुम्हार भी हुए। ये सभी संत एक दूसरे का आदर करते थे। इनमें बहिणाबाई जैसी स्त्रियां और शेख मुहम्मद जैसे कुछ मुसलमान संत भी हुए। जाति-पांति और वर्ण की जगह धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति का यह नया महत्व प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए मराठी संत साहित्य के विद्वान गं.बा.सरदार ने इसे आध्यात्मिक मानववाद का नाम दिया। विट्ठल की भक्ति के अलावा वरकरी संतों ने मराठी भाषा के माध्यम से भी सभी महाराष्ट्रियों को एक करने का प्रयास किया। उन्होंने न सिर्फ अपना सारा साहित्य मराठी भाषा में लिखा, बल्कि अपनी भाषा के प्रति मराठी भाषियों के अंदर गर्व की भावना भी पैदा की। अपनी भाषा के प्रति यह गर्व महाराष्ट्र प्रदेश के प्रति गर्व से भी जुड़ा हुआ था। इस तरह संतों भक्तों के आंदोलन से सभी मराठी भाषियों में एक सांस्कृतिक समुदाय- एक जाति (नेशन) के रूप में खुद को पहचानने की चेतना विकसित हुई। महाराष्ट्रीय अस्मिता की यही चेतना आगे चलकर मराठा राज्य के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि बनी और शिवाजी इसके सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे।

संत रामदास ने वरकरी होते हुए भी अपने ग्रंथ ‘दासबोध’ में भागवतधर्म से अलग महाराष्ट्र धर्म का प्रचार किया। उन्होंने शिवाजी के पुत्र संभाजी को अपने पिता के कदमों के निशान पर चलने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखा- ‘सभी महाराष्ट्रियों को एक करो (पृ.78, राइज आफ मराठा पावर, रानाडे, यूनिवर्सिटी ऑफ बाम्बे, 1961) महाराष्ट्रधर्म से रामदास का ठीक-ठीक मतलब क्या था- इसके बारे में अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग व्याख्यायें हैं। इतना साफ है कि महाराष्ट धर्म सिर्फ हिंदू धर्म नहीं था। वह ऐसा धर्म था जिसका पालन मूलतः महाष्ट्रियों को करना था। रामदास भी भक्त थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ भागवतधर्म की आध्यात्मिक साधना को पर्याप्त नहीं माना और लोगों को अपने व्यवहारधर्म का निर्वाह करने पर जोर दिया। अपने सभी प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहा। रामदास ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और वर्णाश्रमधर्म के समर्थक थे। उन्होंने धनुर्धारी राम को अपना नायक बनाया और लोगों को शक्तिशाली बनने की शिक्षा दी। अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना राज्य कायम करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए जगह- जगह मठ कायम करने और ब्राह्मणों को संगठित करने पर जोर दिया। वरकरियों का भागवतधर्म जहां साधारण लोगों तथा दलित शूद्रों में भी लोकप्रिय हुआ, वहां रामदास का प्रभाव मुख्य रूप से सिर्फ ब्राह्मणों और समाज के छोटे से उच्चवर्ग पर ही पड़ा।

मराठी संतों के इस आंदोलन से, उनके भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म से 19वीं सदी के महाराष्ट्रीय नवजागरण का घनिष्ठ संबंध रहा है। पश्चिमी शिक्षा और यूरोपीय इनलाइटनमेंट के मूल्यों से प्रभावित होने के बावजूद महाराष्ट्रीय सुधारकों ने अपनी जातीय परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। ऐसा कोई मराठी सुधारक नहीं हुआ जिसने मराठी संतों के आंदोलन पर टिप्पणी न की हो, उसकी अपने ढंग से व्याख्या न की हो। अपने सुधार आंदोलन को उन्होंने संतों-भक्तों के आंदोलन का ही जारी रूप बतलाया। प्रार्थना समाज के सुधारकों ने अपने संगठन के धार्मिक सिद्धांतों का निरूपण करते हुए उसे हमेशा मराठी संतों की धार्मिक शिक्षाओं से जोड़ा। उदाहरण के लिए रानाडे संतों के उदार मूल्यों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने प्रार्थना समाज के आंदोलन को संतों के भागवतधर्म का ही एक रूप और उसकी विनम्र संतान बतलाया। (पृ.55, दी प्रार्थना समाज एंड इट्स क्रिटिक, जे.वी.नाइक, वेस्टर्न इंडिया: हिस्ट्रीयन सोसायटी एंड कल्चर में शामिल निबंध, प्रकाशक इतिहास शिक्षक महामंडल कोल्हापुर, 1997) खुद भागवतधर्म के आंदोलन को रानाडे ने यूरोप के रिफार्मेशन जैसा धर्म सुधार का महान आंदोलन बतलाया जबकि राजा राममोहन राय ने बंगाल के भक्ति आंदोलन का कभी कोई जिक्र नहीं किया और वे अपने ब्रह्मसमाज के आंदोलन को ही यूरोपीय रिफार्मेशन जैसा महसूस करते थे। प्रार्थना समाज के ही दूसरे सुधारक नेता आर.जी.भंडारकर ने ‘वैष्णवइज्म, शैविज्म एंड माइनर रिलिजियस सिस्टम’ नामक अपनी किताब में जिसे भारत के धार्मिक इतिहास के अध्ययन में एक उल्लेखनीय रचना माना जाता है- नामदेव और तुकाराम जैसे संतों के योगदान पर और उनकी केन्द्रीय शिक्षाओं पर लिखा। जो प्रार्थना समाज के अंदर उनके अपने मत को प्रतिबिंबित करता था। उन्होंने प्रार्थना समाज के धार्मिक सिद्धांतों का निरूपण करते हुए इन्हें विभिन्न धर्मों की उदार और विवेकशील परंपराओं के अलावा तुकाराम की शिक्षाओं से जोड़ा। (पृ.130, रामाकृष्ण गोपाल भंडारकर एंड दी एकेडमिक रेनेसां इन महाराष्ट्र, आर.एन.डांडेकर, राइटर्स, एडीटर्स एंड रिफार्मर्स, सं.एन.के.वागले, मनोहर, दिल्ली, 1999 में संकलित निबंध)
19वीं सदी में महाराष्ट्रीय नवजागरण के दौर में वरकरी संप्रदाय के कितने ही संतों की रचनायें फिर से प्रकाशित हुईं और उनके नये संस्करण प्रकाशित हुए। महाराष्ट्रीय नवजागरण के सबसे पहले प्रवर्तक बालशास्त्री जांभेकर ने- जिन्होंने दर्पण पत्रिका निकालकर मराठी पत्रकारिता की नींव डाली- 1845 में ज्ञानेश्वरी को फिर से प्रकाशित किया। इसी दौर में महाराष्ट्रीय नवजागरण के सबसे पहले संगठन परमहंस सभा के एक सदस्य तुकारामात्या पडवल ने तुकाराम के नाम से प्रचलित सभी रचनाओं को बहुत परिश्रम से जमा करके तुकाराम गाथा का संपादन प्रकाशन किया। भारत के और किसी भी प्रांत के नवजागरण में यह विशेषता नहीं दिखायी देती कि उसके सुधारकों ने अपने समय की जरूरतों को देखते हुए अपने संतों भक्तों की रचनाओं को फिर से संकलित, संपादित और प्रकाशित किया हो। इसी दौर में रामदास का ग्रंथ ‘दासबोध’ और महीपति द्वारा लिखी गयी मराठी संतों की जीवनियों का संकलन भी फिर से प्रकाशित हुआ।
महाराष्ट्रीय सुधारक धर्म, समाज और राजनीति के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। भागवतधर्म के उदार मूल्यों से उन्हें बल मिलता था। ये सुधारक उदार राष्ट्रवादी थे। लोगों की एकता किसी भी राष्ट्रवाद की पहली शर्त होती है। भागवतधर्म और मराठी भाषा के माध्यम से सभी महाराष्ट्रियों को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास वरकरी संतों ने किया था, उससे पैदा हुई महाराष्ट्रीय अस्मिता की चेतना 19वीं सदी के इन राष्ट्रवादियों के लिए बहुत मूल्यवान थी। ये सुधारक आधुनिकता के समर्थक थे। पश्चिमी शिक्षा और यूरोपीय इनलाइटनमेंट से उन्हें जो भी आधुनिक मूल्य मिले, उसका इन्होंने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। लेकिन देसी आधुनिकता का पहला और बुनियादी मूल्य जातिभेद का विरोध ही हो सकता था। यह मूल्य उन्हें संतों के भागवतधर्म से मिला। प्रार्थना समाज के ज्यादातर सुधारक ब्राह्मण परिवारों से आये थे। जातिप्रथा के विरोधी होने के बावजूद इसे खुलकर तोड़ने का साहस उनमें कम था। समाज में भी जातिप्रथा की कट्टर समर्थक ताकतें मौजूद थीं। इन परिस्थितियों में प्रार्थना समाज के इन सुधारकों ने जातिप्रथा को तोड़ना अपना लक्ष्य नहीं माना और उसके प्रति एक उदार रवैया अपनाया। इस प्रसंग में जातिभेद के प्रति भागवतधर्म का उदार दृष्टिकोण इन सुधारकों को बहुत आकर्षित करता था। महाराष्ट्र में पांच सौ सालों तक चले भक्ति आंदोलन में, रानाडे के मुताबिक, करीब पचास संत हुए जिनमें से आधे ब्राह्मण और आधे गैर ब्राह्मण थे। ज्ञानेश्वर और एकनाथ जैसे ब्राह्मण संतों ने जातिभेद के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए दलितों-शूद्रों के सामाजिक उत्पीड़न को सहानुभूति के साथ देखा था। महार जाति से आये दलित संत चोखामेला ने सामाजिक धार्मिक उत्पीड़न की व्यथा को एक भुक्तभोगी की मार्मिक अभिव्यक्ति दी, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति करते हुए उन्हें एक तीव्र असहनीय तनाव से भी होकर गुजरना पड़ता था। क्योंकि इन दलित संतों को अपने पहले के दासतापूर्ण संस्कारों और नयी मिली आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बीच चलने वाले द्वंद्व का सामना करना पड़ता था। इसलिए उनकी अभिव्यक्ति में एक संस्कारजन्य निरीहता और विनम्रता भी होती थी। जिसके कारण आंबेडकरवादी उन्हें आज भी पसंद नहीं करते। संतों की देसी आधुनिकता की सबसे प्रखर अभिव्यक्ति शूद्र संत तुकाराम में हुई। जातिप्रथा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता के दंभ के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक तुकाराम ही थे। यह तथ्य नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 19वीं सदी के मराठी सुधारकों पर, खासकर उन पर जो जातिभेद के साफ विरोधी थे, सबसे ज्यादा असर तुकाराम का ही पड़ा। तुकाराम पुणे के पास देहू गांव के थे और उनकी उपाधि मोरे थी। देहू और उसके आसपास बसे उनके वंशजों में से एक विद्वान सदानंद मोरे ने महाराष्ट्र के आधुनिक सुधारकों पर तुकाराम के प्रभाव का वर्णन करते हुए महत्वपूर्ण लेख लिखा है। (इम्पैक्ट आफ तुकाराम ऑन माडर्न महाराष्ट्र; वेस्टर्न इंडिया, हिस्ट्री एंड सोसायटी में शामिल निबंध, कोल्हापुर, 1997) इसमें मोरे ने लिखा है कि बालशास्त्री जांभेकर के एक अनुयायी डाडोबा पांडुरंग तरफड़कर ने- जो महाराष्ट्र के सबसे पहले प्रभावशाली सुधारक थे- प्रार्थना समाज से बहुत पहले बंबई और गुजरात में क्रमशः दो संस्थाओं परमहंस सभा और मानवधर्म सभा का गठन किया था। डाडोबा खुद एक वरकरी परिवार से आये थे और 1849 में स्थापित महाराष्ट्रीय नवजागरण की सबसे पहली संस्था परमहंस सभा का नाम परमहंस तुकाराम के एक अभंग से लिया गया था- परमहंस तारी जाने सहजा वरमा, तेथे याती कुला धर्मा नाहीं। तुकाराम ने उस परमहंस उस व्यक्ति को कहा था जो जातिभेद और पारिवारिक प्रथाओं के बंधनों से ऊपर उठ चुका हो। डाडोबा की इस संस्था में सिर्फ ऐसे ही लोग सदस्य बन सकते थे। जो जातिबंधनों को तोड़ने में विश्वास करते हों। कहने की जरूरत नहीं कि इस लिहाज से परमहंस सभा वास्तव में बाद में जाकर बनी प्रार्थना समाज से कहीं ज्यादा साहसी थी।

तुकाराम से डाडोबा इतने गहरे प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी कई कवितायें तुकाराम के अभंगों के ढर्रे पर लिखीं। संतों की परंपरा के बाद आधुनिक महाराष्ट्र में अभंग सबसे पहले नवजागरण के इन सुधारकों ने ही लिखे। परमहंस सभा के सदस्य बंगाल के डिरोजियोपंथियों की तरह जातिबंधन के झूठे संस्कारों को तोड़ने की भावना से प्रेरित होकर किसी दलित के हाथ की बनी रोटी या फिर पुर्तगाली नानबाई से खरीदी पावरोटी खाते थे। फर्क इतना ही था कि डिरोजियोपंथी यह काम खुले बाजार में करते थे। जबकि परमहंस सभा के अनुयायी इसे गुप्त रूप से आयोजित अपनी सभाओं में करते थे। बंगाली भद्रवर्गीय समाज में जब यह बात और इसी तरह की कुछ और बातें फैलीं तो डिरोजियोपंथियों के संबंध अपने परिवारों से तल्ख हो गये और कुछ एक को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र में जब इन गुप्त सभाओं की जानकारी सामने आयी और सभा के सदस्यों के नाम बाहर उजागर हो गये तो परमहंस सभा को ही तोड़ना पड़ गया। महाराष्ट्र की तुलना में बंगाल के डिरोजियोपंथियों में पुराने बंधनों के खिलाफ विद्रोह का भाव ज्यादा उग्र था और इसके लिए वहां गुंजाइश भी महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा थी। 1859 में भंग कर दी गयी परमहंस सभा के बिखर गये सदस्यों में से कुछ एक ने 1866 में बंबई पधारे केशवचंद्र सेन के व्याख्यानों से प्रेरित होकर फिर से अपना संगठन खड़ा किया। इस बार उसका नाम प्रार्थना समाज रखा गया जिसमें एलीफिंस्टन कॉलेज से निकले नये स्नातकों की संख्या काफी थी। लेकिन इस बार इसमें जातिप्रथा के बंधनों को तोड़ने का उत्साह कम था। उग्रता की जगह उदारता ने ले ली थी।
लेकिन प्रार्थना समाज पर भी वरकरी संतों में सबसे ज्यादा प्रभाव तुकाराम का ही था। प्रार्थना समाज के सुधारकों का प्रोफेसर अलेग्जेंडर ग्रांट के प्रति काफी आदरभाव था। ग्रांट प्रांत के शिक्षा विभाग के निदेशक थे और बंबई विश्वविद्यालय उन्हीं के कार्यकाल में खुला। अरस्तू के दर्शन के अनुयायी ग्रांट भी तुकाराम से प्रभावित थे। यह प्रभाव ऐसा था कि ‘तुकारामगाथा’ पहले से प्रकाशित होने के बावजूद ग्रांट ने तुकारामगाथा का एक ज्यादा सटीक और प्रामाणिक संस्करण सरकार की ओर से निकालने के लिए खुद गवर्नर को चिट्ठी लिखी। भारी सरकारी अनुदान से प्रार्थना समाज के दो सदस्यों विष्णु परशुराम पंडित और शंकर पांडुरंग द्वारा संपादित ‘तुकारामगाथा’ का आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित हुआ तो मराठी प्रकाशन के इतिहास में इसका स्थान उतना ही महत्वपूर्ण माना गया जितना 20वीं सदी में भंडारकर रिसर्च इंस्टिच्यूट से प्रकाशित महाभारत के प्रामाणिक संस्करण का। मोरे के मुताबिक प्रार्थना समाज के सुधारक जस्टिस रानाडे, आर.जी.भंडारकर, एन.जी.चंदावरकर और बी.ए.मोदक आदि तुकाराम से सिर्फ प्रेरणा ही नहीं लेते थे बल्कि अपने जीवन को भी उनके अभंगों के मुताबिक जीने की कोशिश करते थे। इन सुधारकों के लिए तुकाराम उनके मित्र, पथप्रदर्शक और दार्शनिक, तीनों थे। रानाडे और चंदावरकर ने तुकाराम के अभंगों पर कई व्याख्यान दिये। जबकि भंडारकर, मोदक और विट्ठल रामजी शिंदे तुकाराम के अभंगों पर कीर्तन किया करते थे। गौरतलब है कि ये सुधारक खुद को तुकाराम का आधुनिक अनुयायी और अपने धर्म को नवभागवतधर्म कहते थे। (पृ.120,मोरे) सबसे खास बात यह है कि इन सुधारकों ने अपने संतों को उन पश्चिमी विचारकों के मुकाबले खड़ा किया जिनका प्रभाव नवजागरण के दौर में हर जगह नजर आता था। उदाहरण के लिए रानाडे ने सुधारकों की नयी पीढ़ी, जिसके प्रतिनिधि गोपाल गणेश आगरकर थे, का मिल और स्पेंसर के पीछे भागना पसंद नहीं किया और उसके मुकाबले अरस्तू और तुकाराम का समन्वय करते हुए भागवतधर्म की अपने ढंग से व्याख्या की और नयी पीढ़ी के आनंदवादी जीवन दर्शन की जगह जीवन की सभी संभावनाओं के पूर्ण विकास का दर्शन पेश किया। (वही)
मोरे ने लिखा है कि इन मराठी सुधारकों ने तुकाराम के प्रभाव को महाराष्ट्र के बाहर दूसरे प्रदेशों में भी फैलाया। इन्हीं के जरिए तुकाराम का प्रभाव बंगाल में ब्रह्मसमाज तक पहुंचा। जहां सत्येन्द्रनाथ ठाकुर ने तुकाराम के अभंगों का बंगला में अनुवाद किया और उनकी जीवनी लिखी। एक दूसरे ब्रह्मसमाजी हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने तुकाराम के जीवन को लेकर नाटक लिखा। तुकाराम के अभंगों का अनुवाद गुजराती में भी हुआ और 20वीं सदी के सुधारक गांधीजी उनसे प्रभावित हुए। नवजागरण से होते हुए तुकाराम का प्रभाव आधुनिक मराठी साहित्य तक पहुंचा। 19वीं और 20वीं सदी के कई आधुनिक मराठी साहित्यकारों जैसे केशवसुत, बालकवि, गउकरी और बी.एस.मर्ढेकर पर तुकाराम का गहरा प्रभाव पड़ा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दिलीप चित्रे ने तुकाराम को आधुनिकता से जोड़ते हुए मराठी आलोचना में तुकाराम केंद्रित आलोचना सिद्धांतों की चर्चा की और तुकाराम की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्हें विश्व साहित्य का अंग बना दिया। (पृ.125, वही)

संतों के आंदोलन के प्रति सिर्फ प्रार्थना समाज के उदार ब्राह्मण सुधारक ही मुखातिब नहीं थे, उनके विरोधी एक ओर परंपरानिष्ठ ब्राह्मण और दूसरी ओर गैरब्राह्मण सुधारक भी उतने ही मुखातिब थे। संतों के आंदोलन और उनके भागवतधर्म की व्याख्या करना 19वीं सदी के महाराष्ट्र में उभरी हरेक विचारधारा के लिए जरूरी था कि क्योंकि उससे किसी न किसी रूप में जुड़कर ही वे महाराष्ट्रीय समाज में अपने लिए वैधता और प्रामाणिकता हासिल करते थे। संतों की परंपरा के प्रति उनका रवैया आलोचनात्मक भी था। वे अपने विरोधियों से होड़ करते हुए, उनकी व्याख्या को चुनौती देते हुए, संत आंदोलन की व्याख्या अपने ढंग से अपने पक्ष में करते थे। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में परंपरानिष्ठ ब्राह्मणों की धारा ने प्रार्थना समाज के उदार ब्राह्मणों की व्याख्या को नामंजूर करते हुए संत आंदोलन के एक दूसरे ही पक्ष को सामने लाकर उससे अपना संबंध जोड़ा। चिपलूणकर से शुरू हुई सुधारकों की पंरपरानिष्ठ ब्राह्मणों की परंपरा में विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े सबसे प्रबल और प्रतापी विद्वान हुए। उन्होंने प्रार्थना समाज के सुधारकों द्वारा ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम जैसे वरकरी संतों की प्रशंसा और भागवतधर्म के गुणगान को स्वीकार नहीं किया और इनकी जगह 17वीं सदी के संत स्वामी रामदास को आगे बढ़ाया। राजवाड़े ने रानाडे वगैरह का विरोध करते हुए वरकरी संतों पर जनता को दुर्बल, अकर्मण्य और भाग्यवादी बनाने का दोष लगाया। बाद में अपने मूल्यांकन में थोड़ा सुधार करते हुए उन्हें भी हिंदू धर्म की रक्षा करने का कुछ श्रेय दिया। लेकिन यह आरोप कायम रखा कि वरकारी संतों ने सब कुछ विठोबा पर छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गये। राजवाड़े ने वरकरी संतों को ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का महत्व घटाकर समाज में अराजकता फैलाने का दोषी ठहराते हुए उन्हें एकांगी बतलाया। वरकरी संतों की तुलना में रामदास को समाज के सभी अंगों पर ध्यान देने वाला, लोगों को कर्मठ, पुरुषार्थी बनाने और समाज की समुचित व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की मंत्रणा देने वाला बतलाया। वरकरी संतों से रामदास का फर्क दिखाते हुए राजवाड़े ने लिखा- ‘‘रामदास इतिहास तत्व निरूपण करने वाले प्रथम महाराष्ट्र ग्रंथकार हैं। एकनाथ, तुकाराम आदि साधु संत नीति तथा भक्ति की ओर उन्मुख थे। नीति तथा भक्ति के गीत गाने वाले साधु संतों ने भी महाराष्ट्र का अत्यंत हित किया है, इसमें संदेह नहीं परंतु राष्ट्रीय और राजनीतिक दिशा में विचार करने का महत्व उन्होंने नहीं जाना। रामदास और उनके पूर्ववर्ती संतों में सबसे बड़ा भेद यही है। पूर्ववर्ती साधु संत एकदेशीय थे, रामदास सार्वदेशिक संत थे। इसके अतिरिक्त एक अंतर यह भी है कि पहले के संतों ने ब्राह्मणों के दोष दिखलाने का मानो व्रत लिया था। उनकी रचनाओं एवं युक्तियों का परिणाम यह हुआ कि चातुर्वण्य घटित महाराष्ट्रीय समाज के नेता ब्राह्मणों का महत्व कम होने लगा। स्वजनों के दोषों को उजागर करना बुरा काम नहीं, पर दोष दिखाने वालों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व सही मार्ग दिखलाना और अपने आचरण द्वारा उसकी सत्यता सिद्ध करना होता है। इस उत्तरदायित्व के अज्ञान एवं दोषविष्करण से मनोभंग तथा मानभंग हुआ और समाज में अराजकता छा गयी, बिखराव चारों ओर दिखायी देने लगा। संतों की एकांतिकता का यही पर्यवसान था जिसका प्रतिकार रामदास की सार्वदेशिकता ने किया।’’ (पृ.291,राजवाड़े लेख संग्रह, सं. तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, साहित्य अकादमी, दिल्ली, 2000)
राजवाड़े ने लिखा है कि रामदास की विशेषता यह थी कि उन्होंने समाज में दोष तो दिखाया ही, साथ ही वर्णव्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्णों के प्रति करुणा का भाव रखते हुए उनके लिए भी सही मार्ग बतलाया। राजवाड़े वर्णव्यवस्था को समाज में संतुलन बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी समझते थे। उन्हें लगा कि यूरोप के विद्वान भी अपने समाज की समस्या का हल निकालने के लिए वर्णाश्रम धर्म की ओर झुक सकते हैं: ‘‘हजारों वर्षों का हमारा इतिहास चतुरर्वण्यबद्धता का साक्षी है। कहा नहीं जा सकता कि आगे कितनी सदियों तक चतुर्वण्य रहेगा। इसलिए चतुर्वण्य का अस्तित्व पूरी तरह स्वीकार कर देश के हितैषियों को दोष तथा उनके परिहार का मार्ग दिखलाना चाहिए। यूरोपीय समाज का असंतोष तथा ‘सोशलिष्टिक’ झुकाव देखते हुए यदि वहां के दूरदर्शी विद्वान विचार कर रहे हों कि उनके समाज को प्रायः चतुर्वण्य का आश्रम कभी न कभी लेना ही पड़ेगा तो हम अपने यहां की संतोषप्रवण संस्था को तोड़कर असंतुष्ट समाज की स्थिति की ओर उन्मुख हों, तो उससे देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसी महत्वपूर्ण पार्श्वभूमि पर रामदास ने अपने उपदेश का सूत्र प्रस्तुत किया।’’ (पृ.291, वही)

भागवतधर्म, वरकरी संतों और रामदास की भूमिका के बारे में प्रार्थना समाज के उदार ब्राह्मण सुधारकों और उनके विरोधी परंपरानिष्ठ ब्राह्मणों की परस्पर विरोधी व्याख्याओं और रवैये से अलग एक तीसरा रवैया गैरब्राह्मण सुधारकों का था। जिसके सबसे बड़े प्रतिनिधि जोतिराव गोविंदराव फुले थे। फुले प्रार्थना समाज के उदार सुधारकों के कड़े आलोचक और परंपरानिष्ठ ब्राह्मणों के विरोधी थे। उन्होंने संतों के आंदोलन की व्याख्या करते हुए और उससे अपना संबंध जोड़ते हुए उसके प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाया। दलितों–शूद्रों के प्रति वरकरी संप्रदाय के ब्राह्मण संतों की उदारता को फुले ने संदेह की नजरों से देखा। उनका संदेह इस बात को लेकर था कि वरकरी संतों ने भागवतधर्म के नाम पर असल में उस वैदिक धर्म को ही आदर दिया था, जो समाज में वर्णव्यवस्था को बनाये रखने का आग्रह करता है। फुले ने वरकारी के ब्राह्मण संतों द्वारा दलित शूद्रों को सिर्फ धर्म और भक्ति के क्षेत्र में स्थान देने (और बाकी समाज में वर्णाश्रमधर्म को जारी रखने) के प्रयत्न को इसके ऐतिहासिक संदर्भ में देखा तो उन्हें लगा कि इस उदारता के पीछे एक कारण इस्लाम है। फुले ने भागवतधर्म के आंदोलन में मुस्लिम विरोध को छुपा हुआ देखा और दलित शूद्रों के प्रति ब्राह्मण संतों की उदारता को उनकी धूर्तता बतलाया। इस ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि जब देश में मुसलमान आये और इस्लाम फैलने लगा, सिर्फ तभी इन ब्राह्मण साधुओं को दलित शूद्रों की याद क्यों आयी? उससे पहले कभी क्यों नहीं आयी? फुले ने लिखा है कि मुसलमानों को शासन कायम हो जाने के बाद- ‘‘उस समय बहुत ही चतुर मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि ब्राह्मण धूर्त संतों ने काल्पनिक भागवतग्रंथ के धोखेबाज अष्ट पहलू वाले कृष्ण ने कुतर्क से भरी गीता में पार्थ को जो उपदेश दिया था, उसी का विश्लेषण किया और उस उपदेश का समर्थन करने के लिए उन्होंने प्राकृत भाषा में विवेकसिंधु, ज्ञानेश्वरी, दासबोध आदि जैसे कई पाखंडी ग्रंथों की रचना की और सभी ग्रंथों की कारस्तानी के जाल में अनपढ़ शिवाजी जैसे महावीरों को फंसाकर उनको मुस्लिमों के पीछे लगने के लिए मजबूर किया। इसी की वजह से मुस्लिम लोगों को कभी महाधूर्त ब्राह्मणों के बारे में समझने सोचने का समय ही नहीं मिला। यदि ऐसा न कहा जाये तो मुस्लिम लोगों के इस देश में आने के संक्रातिकाल में धूर्त ब्राह्मण मुकुंदराज को शूद्रादि अतिशूद्रों पर दया क्यों आयी उसके लिए विवेकसिंधु नाम का ग्रंथ उसी समय क्यों लिखा? इसके पीछे… अनपढ़ शूद्रादि अतिशूद्रों के मुस्लिम हो जाने का डर था और तब धूर्त ब्राह्मणों के मतलबी धर्म की बेइज्जती होनी थी।’’ (पृ.137, फुले रचनावली, खंड-2, सं. एल.जी. मेश्राम, विमल कीर्ति, राधाकृष्ण, प्र. दिल्ली, 1996)
फुले के मुताबिक देश में मुस्लिम विरोधी भावनायें फैलाने में भी इन्हीं का हाथ था। इन ब्राह्मण संतों ने ‘अपने उन ग्रंथों के द्वारा किसानों के मन इतने गुमराह कर दिये कि वे कुरान और मुहम्मदी लोगों को नीच मानने लगे हैं, उनसे नफरत करने लगे हैं।’ (वही)
इस तरह फुले ने नवजागरण में संतों के आंदोलन को लेकर चल रहे विमर्श का पूरा परिप्रेक्ष्य ही बदल दिया और उदार ब्राह्मण सुधारकों के बड़प्पन का आधार ही खिसका दिया। शूद्र दलितों की सामाजिक स्थिति के हिसाब से फुले का यह विवेचन बिल्कुल स्वाभाविक और अनिवार्य था। क्योंकि तत्कालीन महाराष्ट्रीय समाज में व्यापक समाज का मुख्य अंतर्विरोध ब्राह्मणों द्वारा कायम वर्णाश्रमधर्म से था न कि मुसलमान शासकों से।

फुले ने जिस तरह प्रार्थना समाज के उदार ब्राह्मणों और उनके विरोधी परंपरानिष्ठ ब्राह्मणों के बीच कोई बुनियादी फर्क नहीं किया, उसी तरह उन्होंने इनके आदर्श ज्ञानेश्वर और रामदास के बीच भी कोई फर्क नहीं किया। फुले ने सबका नाम एक ही साथ लिया। फुले की नजरों में स्वामी रामदास ने शिवाजी के जरिए महाराष्ट्र में ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने और शिवाजी की सेना को मुसलमानों के खिलाफ लगाये रखने की कोशिश की थी ताकि ब्राह्मणों का राज पहले जैसा ही चलता रहे। परंपरानिष्ठ ब्राह्मणों के इस आदर्श संत के खिलाफ टिप्पणी करते हुए साफ लफ्जों में लिखा- ‘‘रामदास धूर्त आर्य ब्राह्मण था जिसने शूद्र राजा शिवाजी की, उनके अनपढ़ होने की वजह से, चापलूसी की।’’ (पृ.99, वहीं, खंड-2)
वास्तव में फुले ने किसी भी ब्राह्मण संत पर विश्वास नहीं किया और पांच सौ सालों तक चले संतों के आंदोलन में से जिस एक संत का श्रद्धा से नाम लिया, वह संत तुकाराम थे। जो मराठी भाषियों के बीच सबसे आदरणीय और लोकप्रिय थे। तुकाराम सचमुच मेहनतकश शूद्र दलितों के संत थे। उन्होंने बिल्कुल किसानों की भाषा में अभंग लिखे और उनके अभंगों की कई पंक्तियां आज भी महाराष्ट्रीय किसानों के बीच मुहावरों और कहावतों की तरह चलती हैं। फुले की नजर में तुकाराम एकमात्र ऐसे संत थे जो दलितों शूद्रों को ब्राह्मण धर्म के आध्यात्मिक और कर्मकांडी प्रपंचों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई संत शूद्रों के अनपढ़ राजा शिवाजी का सच्चा हितैषी था तो वह तुकाराम ही थे। फुले ने लिखा- तुकाराम नाम का एक साधु पुरुष किसान के घर में पैदा हुआ। वह किसानों को उनके जाल से मुक्त कर देगा, इस डर की वजह से भट्ट ब्राह्मणों के अटल वेदांती रामदास स्वामी ने महाधूर्त गंगाभट्ट के सहयोग से अनपढ़ शिवाजी को गुमराह करने का निश्चय किया। उन्होंने अज्ञानी शिवाजी और निर्विकार तुकाराम का स्नेह संबंध बढ़ने नहीं दिया।’’ (पृ.303,वही, खंड-2)

फुले के प्रसंग में तुकाराम का महत्व समझने के लिए एक बार फिर तुकारामात्या पडवल की चर्चा करना जरूरी है जो परमहंस सभा के सदस्य और फुले के मित्र थे। सदानंद मोरे ने एक हिंदू के नाम से पडवल की लिखी किताब जातिभेद विवेकसरा की चर्चा की है जिसने 19वीं सदी के महाराष्ट्रीय भद्रवर्ग में खलबली मचा दी थी। मोरे ने लिखा है कि इस किताब को खुद फुले पुणे में बेचा करते थे। इस किताब में जातिप्रथा की विस्तार से आलोचना करते हुए पडवल तुकाराम के दृष्टिकोण से काफी प्रभावित दिखते हैं। इस किताब में उन्होंने जातिप्रथा के खिलाफ कई उद्धरण बौद्ध लेखक अश्वघोष के संस्कृत ग्रंथ वज्रसूची के मराठी अनुवाद से दिये थे। ब्राह्मणों के वर्णाश्रमधर्म की तीखी आलोचना करने वाले इस ग्रंथ का संस्कृत से मराठी में अनुवाद खुद तुकाराम के आदेश पर उनकी ब्राह्मणी शिष्या बहिणाबाई ने किया था। तुकाराम की रचनाओं की खोज में पडवल जब तुकाराम के गांव देहू गये, तो उनके साथ की कुछ ऐसी कवितायें पहली बार शामिल की गयी थीं। जो ब्राह्मणों के आचार विचार की तीखी आलोचना करने के कारण वरकरी या किसी भी परंपरा में पहले शामिल नहीं की गयी थीं (पृ.117, मोरे)। गौरतलब है कि फुले के ज्यादातर अनुयायी बुनियादी तौर पर वरकरी पृष्ठभूमि वाले ही थे और वे उन्हीं इलाकों से थे, जहां तुकाराम का प्रभाव खासतौर पर था। मोरे का दावा है कि वरकरी संप्रदाय की आलोचना करते रहने पर भी फुले ने वरकरी द्वारा उठाये गये मुद्दों को ही आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसा दावा करते हुए मोरे उन मुद्दों पर वरकरियों से फुले की व्याख्या और दृष्टिकोण के भेद पर पूरा ध्यान नहीं देते। फिर भी भक्ति के क्षेत्र में वरकरी संतों का उदार और काफी हद तक जनवादी दृष्टिकोण फुले के दृष्टिकोण से हू ब हू मिलता नहीं, तो उसके करीब जरूर था। शायद इसी कारण फुले की भाषा में वरकरियों की शब्दावलियों और बिंब भरे मिलने की बात कही जाती है। मोरे ने लिखा है कि प्रार्थना समाज से असंतुष्ट होकर जब फुले ने सत्यशोधक समाज बना लिया, तो उसमें उनके एक सहयोगी कृष्णराव भालेकर एक वरकरी ही थे। जिन्होंने सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाने के लिए वरकरियों की डिंडी (अभंग गाते हुए पंढरपुर जाने वाले तीर्थयात्रियों के जुलूस की प्रथा) का इस्तेमाल किया। भालेकर के बेटे मुकुंदराव पाटिल भी, जिन्होंने सत्यशोधक समाज के पत्र ‘दीनमित्र’ का प्रकाशन किया, तुकाराम से गहरे प्रभावित थे और उनका यह मानना काफी दिलचस्प है कि सत्यशोधक समाज ही भागवतधर्म का असली अनुयायी है, न कि परंपरागत वरकरी। (पृ.118,वही)
19वीं सदी के महाराष्ट्रीय नवजागरण में संतों के आंदोलन से खुद को जोड़ने की होड़ में जैसे भागवतधर्म को लेकर इतना घमासान चलता दिखायी देता है, वैसा महाराष्ट्रधर्म को लेकर भी चला। संतों के आंदोलन में महाराष्ट्रधर्म शब्द का प्रयोग 17वीं सदी में समर्थ रामदास ने शिवाजी के पुत्र संभाजी (1680-1689) को लिखे एक पत्र में किया था। यह गौरतलब है कि रामदास ने संभाजी को हिंदू धर्म के पालन के लिए नहीं कहा, वैदिक, पौराणिक या सनातन धर्म की वृद्धि करने के लिए नहीं कहा। इन सब धर्मों से अलग यह महाराष्ट्रधर्म क्या है? यह प्रामाणिक रूप से स्पष्ट नहीं है। 19वीं सदी के महाराष्ट्र में प्रभावशाली तीनों धाराओं के प्रतिनिधि इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हुए इसका इस्तेमाल अपनी अपनी सामाजिक राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में करते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित न होने के बावजूद महाराष्ट्र के इतिहास में संतों के जमाने से लेकर आज तक की राजनीति में महाराष्ट्रधर्म की अवधारणा लगातार मौजूद रही है। इस पर सबसे ज्यादा विमर्श 19वीं सदी के नवजागरण में हुआ और महाराष्ट्रधर्म में राष्ट्रवादी राजनीति की कोई भी धारा इससे जुड़े बिना अपना अस्तित्व सार्थक नहीं कर सकती थी। राजेंद्र वोरा ने अपने एक लेख में दिखलाया है- हालांकि काफी सतही ढंग से- कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी आंदोलन की विभिन्न धाराओं के बीच चाहे जो भी मतभेद रहे हों, महाराष्ट्रधर्म पर उन सबकी सहमति ही है। (पृ.24, महाराष्ट्रधर्म एंड दी नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, राइटर्स, एडीटर्स एंड रिफार्मर्स में शामिल निबंध, सं.एन. के. वागले, मनोहर, दिल्ली, 1999) वोरा का विवेचन सतही इस अर्थ में है कि ऐसा करते हुए उन्होंने उनके बीच के सूक्ष्म और बुनियादी फर्क को भुला दिया है या उनका महत्व कम करके आंका। जैसे वोरा के विवेचन में रानाडे, तिलक और राजवाड़े के विचारों के बीच के फर्क को बहुत कम करके आंका गया है।
महाराष्ट्रधर्म अपने मूल रूप में धर्म (हिंदू धर्म) की रक्षा के लिए महाराष्ट्रियों के स्वाधीन राज्य (स्वराज्य) कायम करने और इससे संबंधित उनके राष्ट्रीय कर्तव्यों की अवधारणा प्रतीत होता है। यह अवधारणा पहली बार शिवाजी के द्वारा स्थापित मराठा राज्य में मूर्त हुई थी। 19वीं और 20वीं सदी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समुदाय अपनी विचारधारा के अनुसार इसकी व्याख्या करते हुए अक्सर इसे संकुचित, विस्तृत या विकृत करते रहे हैं। 19वीं सदी के नवजागरण और राष्ट्रवाद के प्रसंग में इस अवधारणा की पहली महत्वपूर्ण व्याख्या रानाडे ने अपनी किताब ‘राइज आफ मराठा पावर’ में की। इसमें संतों के आंदोलन का विवेचन करते हुए उन्होंने निष्कर्ष रूप में महाराष्ट्रधर्म की विशेषताओं को इन शब्दों में पेश किया- ‘इसने लोकभाषाओं में मूल्यवान साहित्य रचा। इसने पुरानी जातिप्रथा की कठोर संरचना में सुधार किया। इसने शूद्रों को आध्यात्मिक शक्ति और सामाजिक महत्व की उस हैसियत तक पहुंचाया जो करीब-करीब ब्राह्मणों के बराबर थी। इसने पारिवारिक संबंधों को पवित्रता प्रदान की और स्त्री की दशा में सुधार किया। इसने मराठी जाति (राष्ट्र) को ज्यादा मानवीय बनाया, साथ ही उन्हें सहिष्णुता के जरिये ज्यादा एकजुट किया। इसने मुसलमानों के साथ मेलजोल का रास्ता दिखलाया और कुछ हद तक ऐसा मेलजोल कायम भी कर लिया। इसने बहुदेववाद की बुराइयों को कम किया। इन सब तरीकों से इसने मराठा जाति को विचारों और कार्यों, दोनों स्तरों पर ऊंचा उठाया और विदेशी प्रभुत्व की जगह एक देशी सत्ता को फिर से कायम करने के लिए इसे इस तरह तैयार किया जैसा और किसी भी तत्कालीन भारतीय प्रदेश में नहीं दिखता है। यह सब महाराष्ट्रधर्म की मुख्य-मुख्य विशेषतायें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर रामदास ने शिवाजी के पुत्र को अपने पिता के चरणचिह्नों पर चलने को कहा था और खुद इस धर्म का प्रचार किया था। जो एक ही साथ सहिष्णु और सुदृढ़ है, आध्यात्मिक है और किसी दूसरे की निंदा भी नहीं करता है।’ (पृ.92, रानाडे, राइज आफ पावर बंबई विश्वविद्यालय, बंबई, 1961)
रानाडे ने ऊपर जो विवेचन किया है, वह महाराष्ट्र में उभरने वाले एक आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आदर्श रूप प्रतीत होता है। लेकिन इस विवेचन में एक गंभीर गड़बड़ी है। ऊपर की जिन बातों को उन्होंने ‘महाराष्ट्र धर्म की मुख्य विशेषतायें’ (प्रिंसिपल फीचर आफ दी रिलीजियन आफ महाराष्ट्र) बतलाया है, वास्तव में वे सबकी सब महाराष्ट्रधर्म की विशेषतायें नहीं हैं। दरअसल इस पूरे उद्धरण में रानाडे ने वरकरी संतों के भागवतधर्म और रामदास के महाराष्ट्रधर्म के बीच कोई फर्क न करते हुए उन दोनों की विशेषताओं को आपस में मिला दिया है। यही वजह है कि रानाडे की किताब ‘राइज आफ मराठा पावर’ के संपादकों ने किताब के इंट्रोडक्शन में रानाडे के इस विवेचन को तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं माना। (पृ.6)
रानाडे ने ऐसा घालमेल क्यों किया?
वरकरी संतों के उदार मूल्यों से रानाडे के उदार राष्ट्रवाद का एक सहज और स्वाभाविक संबंध था। रानाडे उसे किसी भी तरह छोड़ नहीं सकते थे। साथ ही वे रामदास द्वारा प्रतिष्ठित महाराष्ट्रधर्म की भी उपेक्षा नहीं कर सकते थे, जो कि मराठा राज्य और मराठा राष्ट्रवाद के मूलमंत्र जैसा था। रानाडे मानते थे कि महाराष्ट्रियों में राष्ट्रीय चेतना अंग्रेजीराज से बहुत पहले 17वीं सदी में पैदा हुई थी। मराठा स्वराज्य को जन्म देने वाली इस राष्ट्रीय चेतना की पृष्ठभूमि, रानाडे के मुताबिक, संतों के भागवतधर्म ने ही तैयार की थी। इस तरह रानाडे संतों के आंदोलन और मराठा स्वराज्य के बीच, भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म के बीच एक संबंध होने का दावा करते हैं। सभी महाराष्ट्रियों की तरह रानाडे भी शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा राज्य पर गर्व करते थे और दिल्ली के तख्त पर मराठों की सत्ता कायम होने की संभावना का उत्साहपूर्वक उल्लेख करते थे। इसलिए रानाडे इसे भी छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन महाराष्ट्रधर्म में सिर्फ इतना ही नहीं था। रामदास द्वारा निरूपित महाराष्ट्रधर्म में भक्ति के क्षेत्र में और बाकी समाज में भी वर्णाश्रमधर्म का कड़ाई से पालन करने और ब्राह्मणों के नेतृत्व में आस्था रखने का आग्रह भी प्रबल रूप से मौजूद था। जिसके साथ 17वीं सदी के शासकवर्गीय मराठा सरदारों ने एक हद तक समझौता कर लिया था। ऐसे प्रबल आग्रह से वरकरी संतों के भागवतधर्म की उदारता का मेल नहीं बैठता था। रामदास के महाराष्ट्रधर्म के पालन करने वाले को गौ और ब्राह्मण का प्रतिपालक होना भी अनिवार्य था। रानाडे उदार मूल्य महाराष्ट्रधर्म के इन पक्षों से टकराते थे। भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म के बीच इन अंतर्विरोधों का समाधान करना रानाडे जैसे उदार ब्राह्मण सुधारकों के लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा महाराष्ट्रधर्म के इन पक्षों को छोड़ देने और इन पर चुप्पी साध लेने के सिवा रानाडे के पास और कोई चारा नहीं था। गं.बा. सरदार ने इसे नोट किया है भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म के बीच के अंतर्विरोधों को रानाडे ने स्पष्ट नहीं किया। इसके बावजूद जब सरदार यह लिखते हैं कि रानाडे ने ‘भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म का सफलतापूर्वक सामंजस्य बैठाया’ (पृ.1, संत वांगमय…) तो यह संदेश होता है कि वह सामंजस्य सफल हुआ। खुद गं.बा. सरदार जैसे वामपंथी लेखक भी अपनी किताब में किसी जगह भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म के बीच विरोध बतलाते हैं तो दूसरी जगह उन्हें परस्पर पूरक या अविरोधी भी बतलाते हैं। यह अंतर्विरोध उनकी पूरी किताब में मौजूद है। रानाडे और गं.बं.सरदार के उदाहरण बतलाते हैं कि महाराष्ट्र में 19वीं सदी के उदार ब्राह्मण सुधारकों से लेकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध के वामपंथी ब्राह्मण लेखक तक पश्चिमी शिक्षा के जरिये आये पश्चिमी ढंग के राष्ट्रवाद को आत्मसात कर लेने के बावजूद अपनी परंपरागत प्रादेशिक राष्ट्रवाद की धारा से जुड़े रहना गर्व की बात समझते रहे हैं।
भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश करना- तथ्यों के विरुद्ध जाकर भी- उदार ब्राह्मण सुधारकों की मजबूरी थी या सचेत लक्ष्य चाहे जो कह लीजिए; लेकिन उनके विरोधी परंपरानिष्ठ ब्राह्मणों की न ऐसी कोई मजबूरी थी, न लक्ष्य। बिना किसी दुविधा के उन्होंने भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म को दो ध्रुवों की तरह पेश किया और सवाल खड़ा कर दिया कि भागवतधर्म या महाराष्ट्रधर्म? इस धारा के प्रखर प्रतिनिधि विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने महाराष्ट्रीय इतिहास के साधनों से संबंधित अपने ग्रंथ के चौथे खंड में रामदास के ‘दासबोध’ को सामने रखकर मराठों के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में महाराष्ट्रधर्म का विवेचन किया है, ‘राइज ऑफ मराठा पावर’ में किये गये रानाडे के विवेचन से उसका फर्क और विरोध बहुत साफ है। राजवाड़े ने उस ऐतिहासिक संदर्भ को पेश किया जिसमें रामदास ने महाराष्ट्रधर्म का प्रसार करने का आह्वान किया था- ‘महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश म्लेच्छ संस्कृति द्वारा ग्रस्त किया जा चुका था।’ इसी संदर्भ में बाकी बचे हुए महाराष्ट्र को लक्ष्य कर रामदास ने अपनी ओजस्वी वाणी में हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा में प्राण देने के लिए ललकारा कि ‘कुत्तों को मार भगाओ और स्वराज्य कायम करो।’ जाहिर है, जब रानाडे महाराष्ट्रधर्म की मुख्य-मुख्य विशेषताओं के प्रसंग में हिंदू मुसलमानों के मेलजोल का रास्ता स्थापित करने की बात कर रहे थे तो ऐसा वे 19वीं सदी के उदार राष्ट्रवाद की जरूरतों के मद्देनजर कर रहे थे, रामदास द्वारा निरूपित महाराष्ट्रधर्म से उसका दूर-दूर का भी संबंध नहीं था।
राजवाड़े ने दो टूक शब्दों में ‘हिंदू धर्म की स्थापना, गौ ब्राह्मण की रक्षा, स्वराज्य की स्थापना; मराठों का एकीकरण और नेतृत्व’ को ‘महाराष्ट्रधर्म के प्रमुख अंग’ बतलाया जो राजवाड़े के मुताबिक, शिवाजी और दूसरे मराठा शासकों को प्रेरित करके रहे। (पृ.206,राजवाड़े लेख संग्रह) 19वीं सदी की विभिन्न राष्ट्रवादी धाराओं की विशेषता यह है कि वे महाराष्ट्रधर्म को रामदास के निरूपण और शिवाजी के शासन तक सीमित न रखकर मराठा राज्य के पूरे विस्तार पर- मराठा राज्य के मराठा साम्राज्य में बदलने तक के पूरे इतिहास पर- लागू करते चले हैं जिसकी कल्पना शायद रामदास ने भी नहीं की होगी। यह विशेषता उग्र राष्ट्रवादी धारा में, जिसके प्रतिनिधित राजवाड़े थे, खासतौर पर दिखायी देती है। राजवाड़े महाराष्ट्रधर्म को एक बिल्कुल ठोस राजनीतिक एजेंडे की तरह पेश करते हैं और फिर उसे तारीखवार मराठा इतिहास पर लागू करते चलते हैं। उन्होंने तारीख देकर बतलाया कि ‘सन् 1720 ई. के लगभग महाराष्ट्र में महाराष्ट्रधर्म की पूर्णरूपेण स्थापना हुई’ क्योंकि इस समय तक ‘स्वराज्य की स्थापना’ हो गयी थी और गौ, ब्राह्मण तथा हिंदू धर्म की दीनता का सदा के लिए अंत हुआ।’ (पृ.208, वही) लेकिन तब तक महाराष्ट्रधर्म सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर ही लागू हुआ था, बाकी भारत के लोगों में अभी अपने धर्म की रक्षा और स्वराज्य कायम करने का सामर्थ्य नहीं हुआ था। लिहाजा उसके लिए मराठों को महाराष्ट्र से बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने ‘समस्त भारत को यवनों के चंगुल से मुक्त करके उसे अपने अधिकार में लाने तथा हिंदू धर्म एवं गौ, ब्राह्मण का प्रतिपालन करने का निश्चय किया।’ (पृ.209) मराठों ने महाराष्ट्र से बाहर जितने भी इलाके जीते और अपनी सत्ता कायम की, वह सब महाराष्ट्रधर्म का ही प्रचार प्रसार करना था। इसके लिए राजवाड़े सबूत देते हैं कि विभिन्न लड़ाइयों में पराजित शासकों से मराठों ने जो संधियां कीं, उन संधियों में बकायदे ‘धर्म, गौ, ब्राह्मण तथा स्वराज्य की संरक्षा से संबंधित अनुच्छेद हैं।’ इन्हीं लड़ाइयों और साम्राज्य के विस्तार के जरिए ‘सन् 1646 से 1796 तक’ महाराष्ट्रधर्म का प्रसार हो रहा था जिसमें भिन्न-भिन्न जातियां मराठों का नेतृत्व कर रही थीं। (पृ.206 वही)
राजवाड़े के मुताबिक मराठा स्वराज्य कायम करने से लेकर मराठा साम्राज्य के फैलने तक शिवाजी, राजाराम, शाहू और बालाजी विश्वनाथ इन चार महापुरुषों ने प्रयत्न किया। इस तरह हिंदू पद पादशाही अस्तित्व में आयी। राजवाड़े इस हिंदू पद पादशाही को ब्राह्मण पद पादशाही भी कहते हैं क्योंकि यह पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में आयी थी। ‘ब्राह्मण पद पादशाही वस्तुतः हिंदू पद पादशाही ही है।’ (पृ.206 वही) कुनबी मराठों को राजवाड़े रामदास द्वारा वर्णित क्षत्रिय वर्ण जैसा मान कर- ताकि रामदास द्वारा निरूपित महाराष्ट्रधर्म सही लागू हो सके- इस मराठा राज्यसत्ता को भोसले कुल पादशाही और भट्ट कुल पादशाही कहते हैं क्योंकि यह भोसले मराठों और भट्ट ब्राह्मण पेशवाओं, दोनों के नेतृत्व में चली। इस तरह पूरे भारत में हिंदू स्वराज्य और वर्णाश्रमधर्म कायम करने के लक्ष्य को केंद्र में रखकर राजवाड़े ने महाराष्ट्रधर्म की जो व्याख्या की है, तो उसकी वैसे कई विशेषतायें हैं, पर यहां उसकी दो विशेषतायें गौरतलब हैं। राजवाड़े इस बात को बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि रामदास ने उस सहिष्णु हिंदू धर्म की वकालत नहीं की जिसके गीत वरकरी संत गाते थे, बल्कि जयिष्णु हिंदू धर्म के गीत गाये। यानी इस हिंदू धर्म को मानने वाले योद्धा होंगे जो पूरे भारत को जीतने के लिए लड़ेंगे। दूसरी विशेषता यह है कि ऐसा हिंदू स्वराज्य कायम करने के लिए सिर्फ प्रतिरक्षा नहीं, बल्कि आक्रमण की रणनीति को अपनाना होगा। रामदास ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए सिर्फ प्राण नहीं देना है, बल्कि शत्रुओं के प्राण लेने हैं-
धर्म साठीं मरावें। मरोनी अवध्यांसी मारावें।।
मारितां मारितां ध्यावें। राज्य आपुले
(धर्म में मर जाना। पहले दूसरों को मारना। फिर मरना। लड़ते हुए अपना राज्य लेना)
इस तरह रामदास के महाराष्ट्रधर्म ने एक हमलावर हिंदू की छवि को आदर्श रूप में पेश किया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरू के दशकों में महाराष्ट्रीय इतिहास का विवेचन करते हुए राजवाड़े इसी हमलावर हिंदू छवि को आगे बढ़ाते हैं। तत्कालीन युवा मराठी पीढ़ी को यह छवि रानाडे के उदार राष्ट्रवाद की तुलना में कहीं ज्यादा आकर्षित करती है। वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु और वीर सावरकर इसी छवि को अपने मन में बसाकर राष्ट्रीय संग्राम में कूद पड़े थे। आगे चलकर सावरकर इसी विचारधारा के सिद्धांतकार बने। जिन्होंने हिंदू पद पादशाही और ‘सिक्स ग्लोरियस इपोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री’ नामक किताब लिखीं। इन किताबों में रामदास द्वारा निरूपित महाराष्ट्रधर्म का ही राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में प्रतिपादन किया गया है। मराठा इतिहास को हिंदू पद पादशाही का नाम देते हुए सावरकर ने उन्हीं बातों को दोहराया जिन्हें रामदास की व्याख्या करते हुए राजवाड़े ने कहा था; जैसे महाराष्ट्रीय सिर्फ अपने घर, जमीन या खेत के लिए नहीं लड़े थे। वे लड़े थे पूरे भारत में धर्म की स्थापना के लिए; कि मराठों का असली पथ प्रदर्शक सिद्धांत रक्षा नहीं, आगे बढ़कर हमला करना था। (पृ.409-15 सिक्स ग्लोरियस इपोच…,राजधानी ग्रंथागार, दिल्ली, 1971) इन विचारों को अमली रूप देने के लिए 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत नाम से एक संगठन भी खड़ा किया।

लेकिन महाराष्ट्र में विकसित हुए राष्ट्रीय आंदोलन के असली नेता फड़के या सावरकर नहीं, बाल गंगाधर तिलक थे। जिन्होंने कांग्रेस का नेता बनकर पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर अपनी छाप छोड़ी। तिलक भी रामदास के महाराष्ट्रधर्म से प्रेरित और प्रभावित थे। हालांकि वे उस हद तक कभी नहीं गये जिस हद तक राजवाड़े या सावरकर गये। उनकी तुलना में तिलक उदार थे। तिलक की इस अपेक्षाकृत उदारता के कई कारण थे। वे सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के नेता थे। उन्हें जन आंदोलन करना था। जिसमें सभी धर्मों और वर्णों की एकता जरूरी थी। इसलिए तिलक ने वर्णाश्रमधर्म में विश्वास करते हुए भी इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया और न ही मुस्लिमविरोध को हवा दी। अपने गीता रहस्य में उन्होंने वरकरी संतों के भागवतधर्म की तारीफ भी की कि इन संतों ने भक्ति के क्षेत्र में जाति पांति का भेद नहीं किया और धर्म का रास्ता सभी के लिए समान रूप से खोल दिया। तिलक पर महाराष्ट्रधर्म का प्रभाव कुछ बारीक और उदार ढंग से पड़ा।
तिलक के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार ग्रंथ गीता रहस्य है। महाराष्ट्र में गीता की व्याख्या करते हुए सिद्धांत निरूपण की परंपरा 13वीं सदी से चली आ रही थी। ज्ञानेश्वर, एकनाथ और रामदास, सबने अपने सिद्धांतों का निरूपण गीता की व्याख्या के जरिये ही किया। महाराष्ट्रीय संतों की इसी परंपरा में तिलक भी गीता की व्याख्या करते हैं और ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अपने राजनीतिक दर्शन के बुनियादी सिद्धांतों के लिए उससे समर्थन जुटाते हैं।
गीता रहस्य में तिलक ने सबसे पहले यह साफ कर दिया कि गीता में कर्म शब्द का मतलब सिर्फ कर्मकांड या श्रुतियों और स्मृतियों में बताये कर्मों से न होकर किसी भी तरह के काम से है। जाहिर है कि यह काम सामाजिक या राजनीतिक भी हो सकता है। फिर यह आलोचना की है कि अतीत में प्रचलित भागवतधर्म के कारण गीता के मूल संदेश के चार तत्वों ज्ञान, कर्म, भक्ति और वैराग्य में कर्म का स्थान गौण और भक्ति की प्रधानता होती गयी। इसी तरह आगे बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से इसके चार तत्वों में से एक वैराग्य या संन्यास ही सबसे प्रमुख तत्व बन गया। शताब्दियों तक इसे ही गीता का मूल संदेश समझा जाता रहा। इसलिए आज की नयी परिस्थितियों में गीता के मूल सत्य को फिर से उजागर करने की जरूरत है। तिलक के अनुसार गीता मनुष्य को ज्ञान, कर्म, वैराग्य और भक्ति के बीच सामंजस्य बैठाते हुए मूलतः उचित कर्म करने का उपदेश देती है जिसे कर्मयोगशास्त्र कहा जा सकता है। गीता रहस्य के ग्यारहवें और बारहवें अध्याय में तिलक ने समर्थ रामदास का हवाला देते हुए इस मूल प्रश्न को उठाया है कि जिस व्यक्ति ने इस संसार के सत्य को जान लिया है, उसे सांसारिक कर्म करने चाहिए कि नहीं? इसका उत्तर देते हुए तिलक ने लिखा है कि गीता कर्म पर जोर देती है। सिद्ध और ज्ञानी व्यक्ति भी अगर निष्काम भाव से कर्म करता है तो वे कर्म उसके बंधनों का कारण न बनकर लोक का कल्याण करेंगे। इसी प्रसंग में तिलक ने लोकसंग्रह शब्द का कई बार प्रयोग किया और कहा कि ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह की भावना से कर्म करता है। कौन सा कर्म उचित या अनुचित है, इस पर तिलक ने लिखा है कि गीता के मुताबिक कर्मों का औचित्य कर्ता के विवेक और उद्देश्य पर निर्भर करता है। नैतिकता सिर्फ कार्य के बाहरी स्वरूप में निहित नहीं होती, वह कर्ता के विवेक और उद्देश्य से तय होती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जिसका विवेक शुद्ध है, वह कभी अनुचित कार्य अथवा पाप कर्म कर ही नहीं सकता। (पृ.533, श्रीमदभागवत गीता रहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र, भाग एक, अनुवाद भालचंद्र सीताराम सुकठंकर, लो प्राइस पब्लिकेशन, दिल्ली, 2002) इतना ही नहीं, इस सर्वोच्च ज्ञान की आदर्श स्थिति को प्राप्त करने का इंतजार किये बिना, उसे पहले भी निःस्वार्थपूर्ण ढंग से सभी कार्य करने चाहिए, जिससे मनुष्य का विवेक शुद्धतर होता है और वह सर्वोच्च आदर्श तक पहुंच पाता है। तिलक ने यह भी लिखा कि जब तक समाज में अनीतिवान लोग हैं, तब तक नीतिवानों द्वारा उन्हे दंडित किये जाने की जरूरत बनी रहेगी। बुरे या अनीतिपूर्ण कार्य करने वालों की हत्या करने से भी अहिंसा का सिद्धांत उसी तरह खंडित नहीं होता जैसे बुराई करने वाले दंडित करने से सभी को आत्मवत समझने का संतों का सिद्धांत खंडित नहीं होता।(पृ.548, वही) रामदास को उद्धृत करते हुए तिलक लिखते हैं कि दुष्टों को दंड देने में कुछ भी अनुचित नहीं है और कोई दूसरों के साथ बुराई करता है तो उसके भी साथ बुराई करने में कुछ भी गलत नहीं है। (पृ.552,वही)
गीता की व्याख्या के जरिये और संतों के समर्थन से तिलक की ये सारी स्थापनायें निश्चय ही उनके उस राजनीतिक दर्शन का अंग थीं जिसके आधार पर वे भारत में वे ब्रिटिश शासन के अन्याय और दमन के खिलाफ एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उनकी स्थापनाओं का निहितार्थ राष्ट्रीय संग्राम में देशभक्ति से प्रेरित होकर, स्वराज्य के महान लक्ष्य के लिए, अपने प्राण देने और शत्रुओं के प्राण लेने वालों को नैतिक दार्शनिक समर्थन देना था। विदेशी सरकार के खिलाफ होने वाले संघर्ष को- हिंसक और प्रतिशोधपूर्ण होने पर भी- वैधता प्रदान करना था। तिलक की इन स्थापनाओं का संदर्भ 20वीं सदी में उभरा उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन जरूर था, लेकिन इन स्थापनाओं की जड़ें मराठी संतों के आंदोलन में थीं। इन सभी स्थापनाओं को महाराष्ट्रधर्म के आधार पर खड़ा किया जा सकता है, हालांकि तिलक खुद उतनी दूर तक नहीं जाते जहां तक जाने की महाराष्ट्रधर्म इजाजत या आदेश देता है। वास्तव में ये स्थापनायें रामदास के महाराष्ट्रधर्म से पहले के वरकरी संत एकनाथ में भी मिल जायेंगी। जैसे लोकसंग्रह की धारणा। मराठी भाषा में इसका पहला प्रयोग शायद एकनाथ ने ही अपने ग्रंथ एकनाथी भागवत में किया था-
उद्धवा तुझे जें आचरण। तोचि जनासि उपदेश जाण।
यालगीं वैराग्य भक्तिज्ञान। स्वधर्माचरणा सांडूं न को।।
त्रिभुवनामाजीं सर्वथा। उद्धवा मज नाहीं कर्तव्यता।
तोही भी लोकसंग्रहार्थ। होय वर्तला निजधर्माी।।
(पृ.95 पर उद्धृत, संतवाड़मयाची सामाजिक फलश्रुति, पांचवीं आवृत्ति, 24 लोकवांग्मय गृह, मुंबई) इसमें कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कोई भी कर्म करने की अनिवार्यता न होने पर मैं लोक के लिए कर्म करता हूं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के प्रति सच्चे रहकर लोक को प्रबुद्ध करना ही लोकसंग्रह है।
लगता है, सिर्फ काल की ही दृष्टि से नहीं, विचार की दृष्टि से भी एकनाथ संत ज्ञानेश्वर और रामदास के बीच में थे। इस सिलसिले में एकनाथ का खुद का ऐतिहासिक संदर्भ गौरतलब है। एकनाथ का ऐतिहासिक संदर्भ यह था कि उन्हीं के जीवनकाल में यानी 1533 से लेकर 1599 तक महाराष्ट्र में इस्लाम का और बहमनी सुल्तानों के शासन का दबाव महसूस होना शुरू हो गया था। इसका एक उदाहरण फारसी के चलन का बढ़ना था। गौरतलब है कि इसी ऐतिहासिक संदर्भ में तुलसीदास और मराठी में एकनाथ, दोनों समकालीन संतकवि राम के आदर्श की ओर मुड़े। क्योंकि राम की छवि प्रतिरोध करने वाले और दुष्ट शत्रुओं का संहार करने वाले नायक के रूप में थी। यह महज संयोग नहीं है कि तुलसीदास का विवेचन करते हुए हिंदी के सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने जिस एक शब्द का प्रयोग बार बार किया है, वह लोकसंग्रह ही है। इसके अलावा रामदास की तरह क्षात्रधर्म पर जोर देने वाले रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले आलोचक हैं जिन्होंने उस युग में उभरे संतों के साहित्य को मुसलमानी शासन की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा। गौरतलब यह भी है कि रामचंद्र शुक्ल ब्रिटिशविरोधी राजनीतिक आंदोलन में तिलक के समर्थक थे।
बहरहाल, गं.बा.सरदार ने लिखा कि रामदास के युग की कई विशेषतायें एकनाथ के समाज में अपने प्रारंभिक रूप में मिल जाती हैं। एकनाथ ने अपने साहित्य में ऐसी कई बातों पर ध्यान दिया है जिनसे रामदास का रास्ता आसान हो गया। जैसे व्यवहारधर्म पर जोर, राम को नायक बनाकर बुराई का प्रतिरोध करने पर जोर, समाज और लोक के प्रति जागरूकता, परंपरा का आदर और ब्राह्मण की प्रशंसा। ये सभी बातें जो एकनाथ में सौम्य रूप में आयी है, रामदास में काफी उग्र रूप में प्रकट होती है। तिलक के लोकसंग्रह का स्रोत एकनाथ तक जाता है। ज्ञानी और सिद्ध पुरुष को भी लोक के हित में कर्म करना चाहिए, यह विचार एकनाथ में स्पष्ट रूप से मिलता है। एकनाथ ने राम के आदर्श के माध्यम से दिखलाया कि सिद्ध पुरुष को भी आत्मा के आनंद में न डूब कर लोक के प्रति अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। (पृ.91, गं.बा.,सरदार संत पोएट्स आफ महाराष्ट्र: दियर इम्पैक्ट आन सोसायटी; ओरिएंट लांगमन, 1969) एकनाथ ने यह भी कहा कि शुद्ध हृदय और निःस्वार्थ भाव से किये गये सांसारिक कर्म भी अध्यात्म की कोटि में आते हैं। (पृ.92,वही) एकनाथ के इन सभी विचारों को रामदास ने अपने व्यवहारधर्म के रूप में आगे बढ़ाया। व्यवहारधर्म यानी परिवार, समाज और राज्य के प्रति हर व्यक्ति के कर्तव्य। जाहिर है कि तिलक के राजनीतिक दर्शन की जड़ें मराठी संतों के आंदोलन में थीं, खासकर एकनाथ और रामदास के साहित्य में।
तिलक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने महाराष्ट्रधर्म को विचारों के स्तर से आगे बढ़ाकर ठोस राजनीतिक आंदोलन का अंग बनाया जो रानाडे नहीं कर सके थे। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक का एक महत्वपूर्ण योगदान महाराष्ट्रधर्म के मूर्त प्रतीक शिवाजी को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ देना है। 1895 में उन्होंने केसरी में शिवाजी स्मारक कायम करने का आंदोलन चलाया और 1896 में शिवाजी महोत्सव का सिलसिला शुरू करके शिवाजी को महाराष्ट्र में आधुनिक आंदोलन का सबसे बड़ा प्रेरणापुरुष बना दिया। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए महाराष्ट्रियों को शिवाजी से कैसी प्रेरणा मिलती रही होगी, इसे वही लोग ठीक से समझ सकते हैं कि जिन्हें महाराष्ट्रियों के हृदय में बसे शिवाजी के और मराठा स्वराज्य के प्रति उनके गर्व का कुछ अंदाजा हो।
तिलक की तुलना में गांधीजी, जो गुजराती वैष्णव संतों से प्रभावित थे और इसलिए ज्ञानेश्वर जैसे उदार वरकरी संतों के मूल्यों के करीब थे- महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी राजनीति में कभी लोकप्रिय नहीं हो सके। तिलक जहां बुरे लोगों को दंडित करने के समर्थक थे, गांधीजी यह मानते ही नहीं थे कि हममें से किसी को भी यह अधिकार है कि हम दूसरों को दंड देने का फैसला करें। गांधीजी की अहिंसा का महाराष्ट्रधर्म में कोई स्थान नहीं था। तिलक के मित्र और अनुयायी जैसे एन.सी.केलकर ने गांधी के नेतृत्व का विरोध करते हुए महाराष्ट्र के अपने राष्ट्रवादी नेताओं को ज्यादा अहमियत देने और शिवाजी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाने पर जोर दिया। गांधी की हत्या भी आखिरकार सावरकर के एक अनुयायी नाथूराम गोडसे ने की। महाराष्ट्रधर्म की जड़ें महाराष्ट्रीय इतिहास और उसकी राजनीतिक परंपराओं में इतनी गहरी थीं कि महाराष्ट्रधर्म वहां महाराष्ट्रीय राष्ट्रवाद का दूसरा नाम हो चुका था। उसकी उपेक्षा करना महाराष्ट्र के गांधीवादियों के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए गांधी के युवा अनुयायी विनोबा भावे ने 1923 में जब अपना पहला मराठी पत्र निकाला तो उन्होंने उसका नाम महाराष्ट्रधर्म ही रखा।
महाराष्ट्रीय नवजागरण की तीसरी धारा- गैरब्राह्मण- ने अपना नाता महाराष्ट्रधर्म से कैसे जोड़ा?
चूंकि शिवाजी ने अपने शासन में ब्राह्मण पेशवा के अलावा महाराष्ट्र की दूसरी सभी जातियों- प्रभु कायस्थ, कुनबी, रामोशी, महार और मातंग के लोगों को भी शामिल किया था और शिवाजी खुद कुनबी थे जो चितपावन ब्राह्मणों की नजर में शूद्र थे- इसलिए महाराष्ट्र की सभी गैर ब्राह्मण जातियां भी शिवाजी के राज्य को अपना राज्य मानकर गर्व करती थीं। अक्सर यह वर्ग उसी अनुपात में होता जिस अनुपात में राज्य में उनकी जाति की हिस्सेदारी होती। जैसे कुनबी मराठे सरदारों और कायस्थ फौजी अफसरों को ब्राह्मणों के साथ राज्य में ऊंचे ओहदे मिले हुए थे; इसलिए शिवाजी के राज्य पर गर्व भी इन्हीं जातियों को सबसे ज्यादा था। दलितों और दूसरी पिछड़ी हुई शूद्र जातियों के ओहदे और गर्व, दोनों का स्थान इसके बाद था। इसी वजह से गैरब्राह्मण आंदोलन के अंदर भी थोड़ा फर्क था। फिर भी रेडिकल विचारधारा के तहत गोलबंद करने की कोशिश की। फुले ने रामदास द्वारा महाराष्ट्रधर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन महाराष्ट्रधर्म के मूर्त प्रतीक शिवाजी के राज्य को शूद्रों के राज्य के रूप में गर्व से याद करते हुए शिवाजी को कुनबी कूलभूषण कहा। फुले द्वारा शिवाजी को कुनबी कुलभूषण कहना बहुत अर्थपूर्ण था। ऐसा कहकर फुले ब्राह्मणों के द्वारा झूठी वंशावली तैयार करके शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करने के पाखंड को अमान्य करते हैं। फुले ने शिवाजी को वैसा अवतारी पुरुष भी नहीं माना जैसा तिलक आदि ब्राह्मण नेता मानते थे। इसके बजाय फुले ने शिवाजी को शूद्र कुनबियों में श्रेष्ठ रत्न मानते हुए उनके प्रति एक आत्मीय, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखा। फुले के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वे महाराष्ट्रधर्म के सबसे बड़े प्रतीक शिवाजी को ब्राह्मणों के चंगुल से कैसे छुड़ायें? इसके लिए फुले ने तीन महत्वपूर्ण स्थापनायें कीं। सबसे पहले उन्होंने 17वीं सदी के उस पूरे दृश्य से मुसलमान को अगर हटाया नहीं, तो उसे गौण जरूर कर दिया। मुसलमान को गौण कर देने का मतलब मुसलमानों की उस तथाकथित धर्मनाशी भूमिका को खारिज कर देना था जिसकी ब्राह्मण सबसे ज्यादा दुहाई देते थे। फुले का यह काम बहुत बुनियादी महत्व का था क्योंकि इससे उस युग का परिप्रेक्ष्य ही बदल जाता था। फुले ने एक तरह से उस युग के मुख्य अंतर्विरोध को ही बदल दिया। उन्होंने यह स्थापित किया कि उस समाज का मुख्य अंतर्विरोध मुसलमान और हिंदू के बीच नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था और व्यापक गैरब्राह्मण जनता (मुख्यतः दलित-पिछड़े शूद्र) के बीच था। वास्तव में तथ्य भी यही था। शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए मुट्ठीभर ब्राह्मण अपने और मुसलमानों के बीच के अंतिर्विरोध को पूरे समाज का मुख्य अंतर्विरोध बतला रहे थे जबकि लाखों- गैरब्राह्मण जातियों, खासकर दलित शूद्रों- के साथ अपने व्यापक अंतर्विरोध को छुपा रहे थे। इसके बाद फुले शिवाजी के मराठा राज्य के साथ ब्राह्मण वर्ग के इस बहुप्रचारित संबंध को खारिज करते हैं कि एक ब्राह्मण रामदास शिवाजी के गुरु थे और मराठा राज्य कायम करने का मुख्य श्रेय रामदास के उपदेशों का ही था- जैसाकि राजवाड़े ने भी लिख रखा है। फुले ने रामदास को शिवाजी का गुरू मानने से इंकार कर किया। वैसे भी यह एक विवादास्पद धारणा थी। ऐतिहासिक रूप से अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि रामदास शिवाजी के गुरु थे या सलाहकार। इससे आगे बढ़कर फुले ने रामदास और शिवाजी के दूसरे ब्राह्मण मंत्रियों के प्रचारित भूमिका को भी उलट दिया और उसकी जगह वास्तविकता का दूसरा पहलू पेश किया। फुले के मुताबिक ये ब्राह्मण वास्तव में गुरु नहीं, गुरुघंटाल थे, जिन्होंने शिवाजी का भला करने के बजाय बुरा किया। इन चालाक ब्राह्मणों ने शूद्र और अनपढ़ राजा शिवाजी के राज्य के सभी ऊंचे पदों पर बैठकर उस राज्य का इस्तेमाल ब्राह्मणों की सत्ता को और मजबूत करने में किया। इस तरह फुले 19वीं सदी के नवजागरण में मराठा राज्य को लेकर चल रहे उस पूरे विमर्श को उलट देते हैं जिस पर कट्टर और उदार, दोनों किस्म के ब्राह्मणों ने अपना कब्जा जमा रखा था। दलित शूद्रों के दृष्टिकोण से वे सत्य को इस रूप में पेश करते हैं कि एक रत्न शिवाजी के जरिये जिस महान मराठा राज्य को कायम किया था, उसे ब्राह्मणों ने अपनी धूर्तता से हड़प लिया।
इन तीनों धाराओं के बीच का परस्पर संघर्ष, खासकर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण का संघर्ष, 19वीं सदी के महाराष्ट्रीय नवजागरण की ऐसी विशेषता है जो भारत के किसी भी प्रांत के नवजागरण में दिखायी नहीं देती। बंगाल में हमें सुधारकों और परंपरावादियों के बीच संघर्ष ब्रह्मसमाज और धर्मसभा के संघर्ष के रूप में दिखायी देता है। लेकिन यह विरोध महाराष्ट्रीय नवजागरण में मिलने वाले विरोध से कुछ अलग ढंग का है। बंगाल में इस विरोध के न सिर्फ कई मुद्दे अलग थे- जैसे सतीप्रथा, और ब्रह्मविवाह विधान- बल्कि इसका जातिगत और वैचारिक आधार भी वैसा सुसंगत नहीं था जैसा महाराष्ट्र में था। बंगाल में नये सुधारों के पक्षधर और उनके विरोधी, दोनों खेमों में ब्राह्मण और गैरब्राह्मण, कई जातियों के लोग एक साथ शामिल थे जबकि महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मण एकमात्र मुख्य शक्ति थे- सुधारकों में भी, उनके विरोधी परंपरानिष्ठों में भी। महाराष्ट्र और बंगाल के बीच इससे भी महत्वपूर्ण फर्क इस संघर्ष में शामिल तीसरी धारा गैरब्राह्मण आंदोलन का था। बंगाल के नवजागरण में यह तीसरी धारा बहुत क्षीण रूप में मिलती है जबकि महाराष्ट्र में यह इतने प्रखर रूप में मौजूद थी कि अपने अकेले दम पर इसने सुधारकों और परंपराष्ठिों दोनों तरह के ब्राह्मणों से मोर्चा संभाल रखा था। अगर इन सबकी तुलना हम 19वीं सदी के हिंदी प्रदेश से करें तो दृश्य क्या उभरता है? वहां कोई तीसरी धारा तो दिखती ही नहीं, पहली और दूसरी धारा भी वहां किसे कहेंगे? रामविलास शर्मा के हिसाब से चलें और हिंदी नवजागरण की पहली धारा भारतेंदु मंडल के रूप में देखें तो वहां इसकी विरोधी धारा किसे कहेंगे? उनके बीच विरोध के मुद्दे क्या थे और उनका संघर्ष किस रूप में कहां होता है? रामविलास शर्मा के लेखन में ऐसी किसी दूसरी धारा की पहचान नहीं मिलती। सच्चाई यह है कि हिंदी प्रदेश के हिंदुओं के बीच हुए नवजागरण में मुख्य धारा आर्यसमाज की थी जो प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी जिलों- मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, सहारनपुर, रुड़की, शाहजहांपुर इत्यादि में काफी ताकतवर थी। उनसे विभिन्न मुद्दों पर जैसे- मूर्तिपूजा पर, सनातन धर्म और नियोग विधि या विधवा विवाह इत्यादि पर संघर्ष करने वाले हिंदी के लेखक, संपादक और पत्रकार बनारस, इलाहाबाद में प्रबल थे जहां उन्होंने आर्यसमाज के पैर जमने नहीं दिये। महाराष्ट्रीय नवजागरण में संघर्ष के कई मुद्दे ब्रह्मसमाज और आर्यसमाज जैसे ही थे, लेकिन भागवतधर्म और महाराष्ट्रधर्म, जातिभेद, वर्णव्यवस्था तथा मराठा राष्ट्रवाद और महाराष्ट्रीय अस्मिता जैसे मुद्दे न तो बंगाल के नवजागरण में थे और न हिन्दी प्रदेश में।
ब्राह्मण और गैरब्राह्मण धाराओं के बीच सिर्फ यह संघर्ष ही नहीं, इस संघर्ष की तीव्रता भी महाराष्ट्रीय नवजागरण की एक विशेषता है। फुले के नेतृत्व में महाराष्ट्रीय नवजागरण की गैर ब्राह्मण धारा ने ब्राह्मणों, सुधारकों और परंपरानिष्ठों से समाज, संस्कृति और इतिहास के हर मुद्दे पर लोहा लिया। गैरब्राह्मण धारा ने वहां ब्राह्मणों की हर बात को काटते हुए, उनका तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए अपनी स्वतंत्र स्थापनायें रखीं। अगर ब्राह्मण ज्ञानदेव को ज्ञानेश्वरी का रचयिता मानते हैं तो गैरब्राह्मणों ने कहा कि ज्ञानदेव कोई और थे और ज्ञानेश्वरी के रचनाकार ज्ञानेश्वर कोई और। ब्राह्मणों ने गर्व के साथ एक ब्राह्मण रामदास को शिवाजी का गुरु बतलाया। गैरब्राह्मणों ने इस दावे को बिल्कुल खारिज कर दिया, इस पर रत्ती भर विश्वास नहीं किया। कुछ एक ने तो इसके उल्टे रामदास को औरंगजेब का गुप्तचर भेदिया तक कहा। (पृ.79, मराठी संत कवियों की सामाजिक भूमिका, गणेश तुलसीराम अंबेडकर, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1980) शूद्र जाति से आये संत तुकाराम की मृत्यु को ब्राह्मण स्वाभाविक मानते हैं। गैरब्राह्मणों ने कहा कि तुकाराम की हत्या की गयी थी। (अमरावती के सुदामा सावरकर ने 1960 के दशक में तुकाराम: का खून की वैकुंठगमन नामक किताब लिखकर यह स्थापित करने की कोशिश की है तुकाराम का खून किया गया था। इसके लिए लेखक ने कई सबूत भी दिये।) मराठा राज्य के पतन का कारण ब्राह्मण मुख्यतः सैन्यशक्ति की कमजोरी को मानते हैं तो गैरब्राह्मणों की नजर में मराठा राज्य के पतन के असली जिम्मेदार खुद धूर्त ब्राह्मण थे।
ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण के बीच हर एक मुद्दे पर विरोध और तीखा विचारधारात्मक संघर्ष एक ऐसे नवजागरण का चरित्र सामने लाता है जो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन और ऐतिहासिक अनुभवों में काफी गहरे धंसा हुआ था। बंगाल और महाराष्ट्र के नवजागरण में यह बहुत बड़ा फर्क है। बंगाल का नवजागरण बंगाल के कुलीन और संपत्तिशाली वर्गों से आये धनी मानी लोगों का आंदोलन था जो मुख्यतः कलकत्ता महानगर में ही प्रभावशाली था। बंगाल की संस्कृति और इतिहास में इसकी जड़ें नहीं थीं और न ही स्थानीय इतिहास और संस्कृति इसके विमर्श के ज्वलंत मुद्दे थे। उदाहरण के लिए जब वे सतीप्रथा पर बहस करते हैं तब भी वे स्थानीय इतिहास में इसकी जड़ों की खोज इतना नहीं करते जितना सर्वमान्य हिंदूशास्त्रों में इससे संबंधित वचनों की खोज करते हैं। इसके विपरीत महाराष्ट्रीय नवजागरण के सुधारक धनी मानी परिवारों से नहीं बल्कि साधारण मध्यवर्गीय परिवारों से आये शिक्षित लोग थे और उनका नवजागरण सिर्फ बंबई नगरी तक सीमित नहीं था। महाराष्ट्र का इतिहास और उनकी संस्कृति इस नवजागरण में तीखी बहस के ज्वलंत मुद्दे थे। 19वीं सदी के महाराष्ट्रीय नवजागरण में इतिहास और संस्कृति, संतों के आंदोलन और मराठा राज्य को लेकर तीनों धाराओं के बीच जो तीखा वैचारिक संघर्ष चला, वह वास्तव में ब्रिटिश राज की बदली हुई परिस्थितियों में इन सामाजिक वर्गों के द्वारा अपने अपने वर्गहितों और सांस्कृतिक अस्मिता को प्रतिष्ठित करने की लड़ाई थी। दूसरे शब्दों में विभिन्न सामाजिक वर्ग या समुदाय अपने वर्गीय हितों और विचारधारा की लड़ाई महाराष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति के अखाड़े में लड़ रहे थे। रोजालिंद ओ हानलीन ने अपने एक निबंध में इसे अच्छी तरह दिखलाया है।
रोजालिंद ने इस ओर ध्यान खींचा है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठी भाषा में शिवाजी तथा मराठा इतिहास के दूसरे वीर नायकों पर साहित्य रचने की प्रबल लहर चल पड़ी थी। इसमें मुख्य विधा पंवाड़ों की यानी वीरगाथाओं की थी। शिवाजी पर पंवाड़े पहले से प्रचलित थे, लेकिन मौखिक रूप में थे। नये लिखित पंवाड़ों की मुख्य विशेषता यह थी कि इनमें शिवाजी और मराठा राज्य के इतिहास की व्याख्या करने के बहाने से विभिन्न सामाजिक वर्गों ने एक दूसरे को चुनौती देते हुए अपनी अपनी समुदायी अस्मिता को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। शिवाजी से संबंधित ऐसी तीन रचनाओं को लेकर रोजालिंद ने जो तुलनात्मक अध्ययन किया वह दिलचस्प है। इसमें पहला पंवाड़ा 1869 में जोतिबा फुले ने लिखा। इस पंवाड़े में शिवाजी के राज्य का रूपक आर्यपूर्व राजा बली के राज्य से बांध कर फुले ने शिवाजी और मराठा राज्य के पूरे इतिहास की गैरब्राह्मणी व्याख्या को बहुत प्रभावशाली ढंग से स्थापित करने की कोशिश की। आर्यों की वर्णाश्रम संस्कृति से पहले का राजा बली श्रम करने वाले शूद्र किसानों का प्रिय राजा था। फुले ने खेत को क्षेत्र और इसलिए खेती करने वालों को क्षत्रिय कहा जो इन शूद्रों को पहले से कहा जाता था। बली का राज्य हर तरह से धन धान्य से भरा हुआ था, उनकी प्रजा खुशहाल थी। तब उत्तर से आर्य ब्राह्मण वामन का रूप धारण करके आये जिन्होंने छल कपट से बली का राज्य हड़प लिया और खुद राजा बन बैठे। उनके राज्य में शूद्र क्षत्रियों (किसानों) का भयानक शोषण उत्पीड़न शुरू हुआ। वे गुलाम बना लिए गये और गरीबी की बुरी दशा में पहुंच गये।
प्राचीन राजा बली के राज्य को वामन रूप धारण करके हड़पने का इतिहास मानो शिवाजी और उनके मराठा राज्य के अपहरण के रूप में फिर से दोहराया गया। शिवाजी शूद्रों के राजा थे। शूद्र सैनिकों के बल पर उन्होंने शूद्रों के कल्याण के लिए जो राज्य खड़ा किया था, उसे पेशवा ब्राह्मणों ने हड़प लिया। शूद्रों की ताकत से खड़े हुए मराठा राज्य में शूद्र फिर से गुलामी की दशा में पहुंच गये। इस पंवाड़े में फुले ने ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित इस कहानी को खारिज कर दिया कि शिवाजी ने अपना राज्य गौ और ब्राह्मण के प्रतिपालन के लिए कायम किया था। फुले ने एक ओर मराठा राज्य के पतन और उसके बाद शूद्रों की बदहाली के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराया, दूसरी ओर बली और शिवाजी के राज्य को शूद्रों के ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास के रूप में पेश किया जिससे प्रेरणा लेकर वे फिर से खड़े होने और अपनी वर्तमान हालत को बदलने के लड़ाई लड़ सकते हैं।
1869 में जब यह पंवाड़ा प्रकाशित हुआ, तब इस पर उस समय के ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया कैसी थी? इस प्रसंग में रोजालिंद ने उस समय की एक साहित्यिक पत्रिका विविध अध्ययनी विस्तार का जिक्र किया है जिसमें फुले की किताब समीक्षा के लिए आयी थी। पत्रिका के चितपावन ब्राह्मण संपादक ने अपनी टिप्पणी में लिखा: ‘‘छत्रपति राजा शिवाजी पर पंवाड़े की एक प्रति हमारे पास आयी है। इसका लेखक कोई जोतिराव गोविंद राव फुले या कोई है। जब हमने पुस्तक को पढ़ा तो पाया कि इसे स्वीकार करना महान साहसी राजा शिवाजी की गरिमा और समस्त हिंदू जाति की गरिमा को नीचे गिराना होगा। हमारे पास लेखक का कोई पता नहीं है, इसलिए हम इसे वापस भेजने में भी असमर्थ है।’’ (पृ.20, मराठा हिस्ट्री एज पालिमिक्स: लो कास्ट आइडियोलाजी एंड पालिटिकल डिबेट इन लेट नाइनटींथ सेंचुरी वेस्टर्न इंडिया, माडर्न एशियन स्टडीज, 17, 1 (1983) ग्रेट ब्रिटेन)
शिवाजी के बारे में दूसरी रचना 1898 में प्रकाशित राजाराम शास्त्री भागवत की शिवाजी चरित्र है। भागवत सेंट जेवियर कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे और एक उदार ब्राह्मण सुधारक थे जो दलितों, शूद्रों की दशा सुधारने के लिए काम करते थे। शिवाजी चरित्र के अलावा उन्होंने महाराष्ट्रीय इतिहास पर दो किताबें और भी लिखी थीं- महाराष्ट्रधर्म (1895) और मराठया संबंधी चार उद्गार (1895)। रोजालिंद के मुताबिक भागवत ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि मराठा राज्य महाराष्ट्र के सभी जातियों के द्वारा मिलजुल कर कायम किया गया था। विभिन्न जातियों के बावजूद महाराष्ट्र की संस्कृति और धर्म सदा से एक रहा है उनका एक ही समुदाय है जिसे महाराष्ट्र मंडल कह सकते हैं। भागवत के मुताबिक महाराष्ट्रियों की यह एकता मराठी संतों के धार्मिक आंदोलन की देन थी। संतों ने सभी मराठी भाषियों को एक धर्म के सूत्र में बांध कर उनके अंदर एक महाराष्ट्रपन की भावना पैदा की। भागवत ने शिवाजी के ब्राह्मण सलाहकारों को भी काफी महत्व दिया।
शिवाजी से संबंधित तीसरी रचना ‘शिवाजी महाराज को दादोजी कोंडदेव’ की सलाह 1877 में छपी। इसके लेखक एकनाथ अन्नाजी जोशी एक परंपरानिष्ठ ब्राह्मण थे और इंदौर के एक अंग्रेजी स्कूल में सहायक हेडमास्टर थे। उनकी किताबों को दक्षिणा प्राइज फंड से पुरस्कार भी मिला था। अपनी रचनाओं में उन्होंने शिवाजी को पूरे भारत में प्रचलित हिंदू धर्म का रक्षक नेता बतलाया। फुले की सरल और किसानों के बीच प्रचलित मराठी के उल्टे जोशी की भाषा संस्कृतनिष्ठ थी और श्लोकों में लिखी गयी थी। जोशी के शिवाजी गौ, ब्राह्मण और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं। जोशी हिंदुओं के प्राचीन रामराज्य की चर्चा करते हैं और उसे स्वर्णयुग बताते हैं जिसे मुसलमान हमलावरों ने आकर बर्बाद कर दिया। शिवाजी ने उस राज्य को मुसलमानों के अत्याचारों से मुक्त कराया। गौरतलब है कि जोशी के रामराज्य का ब्राह्मण ही फुले के बली राज्य को हड़पता है और खुद राजा बली ब्राह्मणों के पुराण में एक दैत्य के रूप में चित्रित हैं। जोशी ने शिवाजी को क्षत्रिय दिखाया है, लेकिन फुले के किसान के अर्थ में नहीं बल्कि वर्णाश्रम धर्म के अर्थ में क्षत्रिय कहा है जो ब्राह्मणों की सलाह से राज्य चलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जोशी की रचना में ब्राह्मण दादोजी राजा शिवाजी को बड़े-बड़े जनसम्मेलन आयोजित करने, जनसभायें बुलाने और उन सभाओं, सम्मेलनों में सभी लोगों से विचार विमर्श करके उन्हें बड़ी कार्रवाइयों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की सलाह देते हैं जो निश्चित रूप से आधुनिक औपनिवेशिक काल की राजनीतिक विशेषता थी। (वही, रोजालिंद)
इस तरह 19वीं सदी के महाराष्ट्रीय नवजागरण में मौजूद उदार ब्राह्मण, कट्टर ब्राह्मण और गैरब्राह्मण- ये तीनों धारायें एक दूसरे के खिलाफ तीव्र विचारधारात्मक संघर्ष में उलझी हुई दिखायी देती हैं। यह संघर्ष वे महाराष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति के सवालों पर कर रही थीं। इन तीनों धाराओं से जुड़ी जातियों और सामाजिक, राजनीतिक समुदायों की अस्मिता की जड़ें महाराष्ट्रीय इतिहास में धंसी हुई थीं। ऐसा संघर्ष करते हुए दरअसल वे अपने वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक हितों और दावों की लड़ाई ही लड़ रहे थे। आज महाराष्ट्रीय समाज जिस भी रूप में है, उसमें विभिन्न जातियों और राजनीतिक समुदायों के बीच जो शक्ति समीकरण है, उसके पीछे संतों के आंदोलन, मराठा राज्य और महाराष्ट्रीय नवजागरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
वर्तमान के राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्ष में अतीत के नायकों का इस्तेमाल महाराष्ट्रीय समाज की ऐसी विशेष परंपरा रही है जो आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाती है। लोकतांत्रिक संवैधानिक महाराष्ट्रीय सरकार द्वारा हर साल मनाया जाने वाला राजा शिवाजी का जन्मदिन, बाल ठाकरे की शिवसेना और मराठी मानुस के नाम पर चलने वाली राजनीति, यह सब भी बदले हुए संदर्भों में किसी न किसी रूप में उसी ऐतिहासिक परंपरा के राजनीतिक इस्तेमाल से जुड़े रूप हैं।
मैं आभारी हूं महाराष्ट्रीय इतिहासकार प्रोफेसर राम बापट का जिनकी विद्वता, विनम्रता और मनुष्यता मुग्ध कर देने वाली है। 2009 में फरवरी में पुणे में उनके घर पर एक शाम उनके साथ हुई बातचीत से ही मुझे महाराष्ट्रीय नवजागरण को देखने समझने की दृष्टि प्राप्त हुई। उनके अलावा मैं शिमला में दो साल तक अपने पड़ोसी रहे मराठी के मशहूर कवि, आलोचक और उपन्यासकार भालचंद्र नेमाड़े जी का आभारी हूं जिनसे मैंने कई मराठी नामों और शब्दों का सही उच्चारण जाना, कई ऐतिहासिक तथ्यों का सही संदर्भ समझा और जिन्होंने मेरे लिए कुछ मराठी पुस्तकें उपलब्ध कराने के अलावा उनके कुछ अंशों का हिंदी अनुवाद भी कर दिया।
(यह लेख पूर्व में हिंदी पत्रिका तद्भव के अक्टूबर, 2016, अंक -26 में प्रकाशित हुई)
( कॉफी संपादन : नवल/सिद्धार्थ/इमामुद्दीन )
आलेख परिवर्द्धित : 22 मई, 2019 11:10 AM
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया