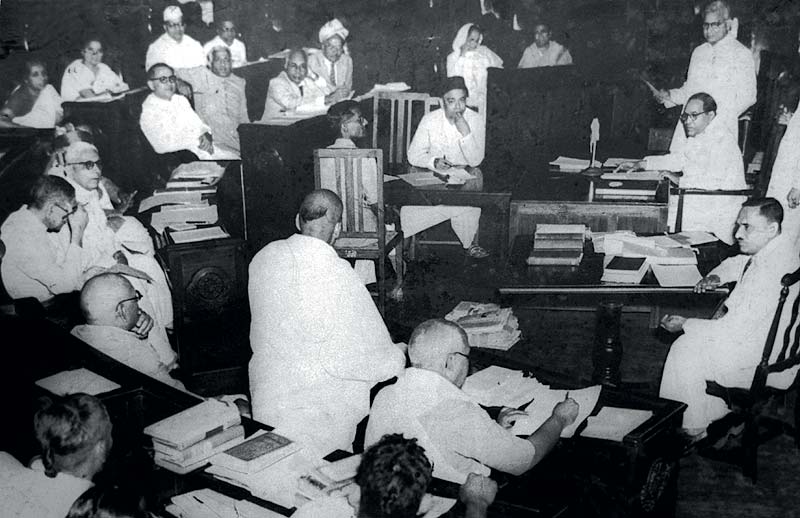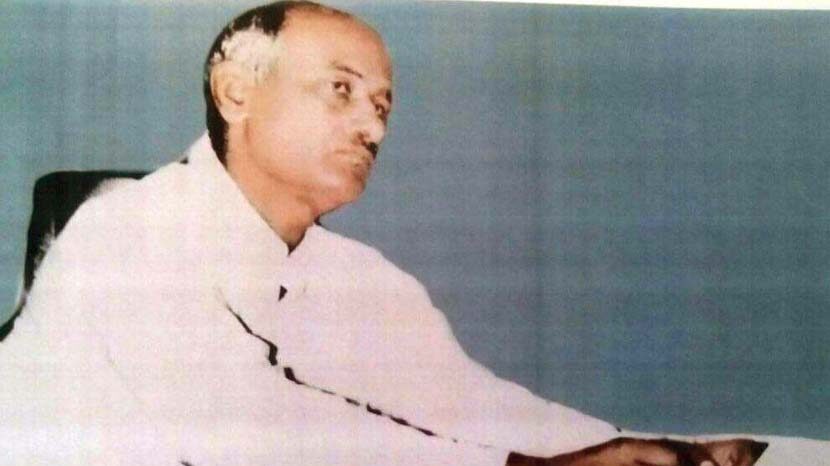पेरियार अपनी मान्यता का पालन करते हुए मृत्युपर्यंत जाति और हिंदू धर्म से उत्पन्न असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। ऐसा करते हुए उन्होंने लंबा, सार्थक, सक्रिय और सोद्देश्यपूर्ण जीवन जिया था। अपनी मृत्यु से ठीक दो वर्ष पूर्व अपनी स्थिति को साफ करते हुए उन्होंने लिखा था–
‘‘यद्यपि मैं पूरी तरह जाति को खत्म करने को समर्पित था; लेकिन जहां तक इस देश का संबंध है, उसका एकमात्र निहितार्थ था कि मैं ईश्वर, धर्म, शास्त्रों तथा ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए आन्दोलन करूं। जाति का समूल नाश तभी संभव है, जब इन चारों का नाश हो। यदि इनमें से कोई एक भी बचता है, तब जाति का आमूल उच्छेद असंभव होगा….। क्योंकि, जाति की इमारत इन्हीं चारों पर टिकी है….केवल आदमी को गुलाम और मूर्ख बनाने के बाद ही, जाति को समाज पर थोपा जा सकता था। (लोगों में) ज्ञान और स्वाधीनता के प्रति जागरूकता पैदा किए बिना जाति का कोई भी खात्मा नहीं कर सकता। ईश्वर, धर्म, शास्त्र और ब्राह्मण लोगों में गुलामी और अज्ञानता की वृद्धि के लिए बनाए गए हैं। वे जाति व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं।’ (पेरियार : 93वें जन्मदिवस पर प्रकाशित स्मारिका, 17 सितंबर 1971, अनीमुथू 1974 : 1974)।
इस तर्क के अन्य पाठांतर भी थे। 1930 और 1940 के दशक में पेरियार ने व्यक्ति को समानता और स्वाभिमान से भरपूर, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, तीन प्रकार के पूर्वाग्रहों, यथा- जाति, धर्म और राष्ट्र(वाद) का विरोध करने की सलाह दी थी। कुछ सीमा तक पेरियार ने इनमें चौथे और पांचवें पूर्वाग्रह को भी शामिल कर दिया था। जैसे कि भाषा तथा पूर्वनिर्धारित अवधारणाओं के माध्यम से स्त्री की अधीनस्थता को न्यायसंगत ठहराना। दैहिक शुचिता को अनिवार्य घोषित करना, जो स्त्रियों को नीरस दांपत्य से बांधे रखती है, उन्हें अपने मनोभावों को दबाने को प्रेरित करती तथा दैहिक सुख के अधिकार से वंचित रखती है।
संक्षेप में, पेरियार ने मानव-मस्तिष्क के जटिल एवं विवेकसम्मत गतिविधियों, चिंतनधाराओं, पसंदों का निर्धारण व्यक्ति और राज्य, सामाजिक और धार्मिक, यानी जीवन के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया था। वे मानते थे कि मानवमात्र इस तरह के प्रभावों को ग्रहण करने में सक्षम है। उनके लिए ‘स्वतंत्रता और ज्ञान के प्रति अभिरुचि’ व्यक्ति-विशेष के मनुष्यत्व को परिभाषित करती थी। वे चाहते थे कि लोग यदि इससे अनभिज्ञ हैं, तो उन्हें इससे परिचित कराया जाना चाहिए था। उनके अनुसार, सामाजिक न्याय और समानता के समग्र दर्शन को, मनुष्यत्व की प्राप्ति में बाधक सभी तरह के कारकों की बुद्धिसंगत आलोचना, समीक्षा द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इसका सामान्य अर्थ है, धर्म की प्रासंगिकता तथा उन सभी दावों एवं तर्कों के आगे प्रश्न-चिह्न लगाना, जो धर्म से प्रेरित हैं; तथा उनके (धार्मिक-सामाजिक अभिजात्य वर्गों) सांस्कृतिक, सामाजिक और शक्ति-संबंधी विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण ठहराते हैं। प्रकारांतर में पेरियार के लिए धर्म की आलोचना अपरिहार्य रूप से धर्म द्वारा पोषित-संवर्धित सामाजिक-सांस्कृतिक स्तरीकरण की आलोचना थी।
पेरियार द्वारा धर्म की आलोचना, विशेषरूप से हिंदू धर्म की आलोचना; उनके नास्तिक होने तक सीमित कर दी जाती है। जबकि, इसके व्यापक संदर्भ हैं। पहले पेरियार का निष्कर्ष था कि धर्म जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन को न्यायोचित ठहराता है; साथ ही वह जाति-आधारित भेदभाव को सांस्थानिक वैधता प्रदान करता है। इस मामले में सभी शास्त्र, इतिहास, पुराणादि पूर्णतः स्पष्ट हैं। उनका कहना था कि इन ग्रंथों को महज शूद्रों और पंचमों के जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं रचा गया था, अपितु उनकी रचना शूद्रों और पंचमों को उनकी तुच्छता का बोध कराने और उसे स्वीकारने के लिए की गई थी। (कुदी अरासु-कु.अ., 30 मार्च 1926)।
दूसरे, उन्होंने पाया था कि हिंदू धर्म सिवाय ब्राह्मण के किसी और को पढ़ने-लिखने की अनुमति नहीं देता। बाकी लोग किसी शिल्पकला को सीख सकते हैं अथवा अपने व्यापार में पारंगत हो सकते हैं; परंतु वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि उन्हें ईश्वर अथवा धार्मिक कार्य-कलाप को लेकर सवाल करने की अनुमति नहीं थी। वस्तुतः उन्हें मुक्त चिंतन और आसपास की दुनिया को जानने-समझने के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया था। (वही 92)।

तीसरे, हिंदू आस्था ब्राह्मण के योगदान, उसके कार्यक्षेत्र को अपरिमित मान लेती है; न केवल पुजारी के रूप में उसकी क्षमता को, अपितु धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी, जैसा कि उसने अपने लिए चुना हुआ है; मान्य ठहरा देती है। जैसे कि ब्राह्मणों के उस दावे पर भी जब वे मौलिक चिंतक और समाज के मार्गदर्शक होने का दावा करते हैं, सहज विश्वास कर लिया जाता है। (कुदी अरासु, 14 अप्रैल 1929, अनीमुथू, 255)। यह राष्ट्रवाद के लिए ब्राह्मण के समर्थन को रेखांकित करता है, अथवा नौकरशाह या शिक्षाविद् के रूप में जो भी ब्राह्मण स्त्री-पुरुष अपने लिए चुनना चाहें, उसे उनका विशेषाधिकार घोषित कर देता है। (कुदी अरासु, 19 मई 1929, अनीमुथू, 371-72)।
पेरियार द्वारा धर्म की आलोचना हिंदू धर्म तक सीमित नहीं थी। जब उनका ध्यान इस्लाम के वैश्विक भाईचारे के आदर्श की ओर दिलाया गया और कहा गया कि उन हिंदुओं जो धर्मांतरित होने की इच्छा रखते हैं; के लिए वह बेहतर विकल्प है। तो उन्होंने इस्लाम में स्त्रियों की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाया और उसकी आलोचना की। इस्लाम और उसमें व्याप्त लैंगिक भेदभाव पर वे जीवंत बहसें, आत्म-सम्मान आन्दोलन की पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित हुई थीं। (कुदी अरासु, 14 अक्टूबर 1928, 25 नवंबर 1928)।
ईसाई धर्म की संस्थाओं में जाति-आधारित विभाजन को स्वीकृति तथा चर्च और पादरी को, ईसाई धर्मावलंबी के जीवन से संबंधित अतिरेकपूर्ण अधिकार देने के कारण उनका दृष्टिकोण ईसाई धर्म के प्रति भी आलोचनात्मक था। (कुदी अरासु, 15 मार्च 1936)।
यह भी पढ़ें – बुद्धिवाद : पाखंड व अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग
पेरियार बौद्ध धर्म के पक्ष में थे। वे इतिहास में उसके क्रांतिकारी योगदान को स्वीकारते भी थे। लेकिन, किसी व्यक्ति के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसे लेकर वे निश्चित नहीं थे। इस प्रकार उन्हें बोध था कि उन जैसे व्यक्ति के लिए धर्मांतरण को तैयार होना बुद्धिमानी भरा काम हो, तब भी धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि, उसके पश्चात वे हिंदुत्व के लिए बाहरी व्यक्ति माने जाएंगे। तब उनके द्वारा हिंदुत्व की आलोचना अपना तेज खो बैठेगी। (वी.एम. सुबागुनराजन, 2018 : 360)।
पेरियार ने साफ कर दिया था कि वे उन विभिन्न विचार प्रणालियों तथा उनके अनुशीलन के विरुद्ध नहीं हैं, जो मनुष्यता को नैतिकता की राह दिखाती हैं। यही वह आधार था, जिससे उन्हें लगता था कि हिंदू धर्म अपने दायित्व का निर्वाह करने में विफल सिद्ध हुआ है। वह सार्वभौमिक नैतिकता यानी समधर्म, जो सर्वसाधारण के लिए न्याय और समानता का पर्याय है; के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था; अपितु ‘मनुधर्म’ यानी जन्म पर आधारित दंडविधान और विशेषाधिकारों का समर्थन करता था। 1945 के दौरान कानपुर में ‘आल इंडिया बैकवर्ड क्लास हिंदूज’ की सभा में भाषण देते हुए उन्होंने हिंदुओं से उनकी आस्था की सीमाओं तथा उसमें अंतर्निहित अन्याय को समझने की अपील करते हुए उनसे उसे मुक्त हो जाने का आग्रह किया था। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक पहचान से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। यह आसान है; क्योंकि उसका जन्म ही उसमें हुआ था।
कोई भी व्यक्ति विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों और उससे संबंधित आस्थाओं के दावे का परीक्षण कर, उनमें से इच्छानुरूप चयन कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह इस नतीजे पर पहुंचेगा कि वस्तुतः विवेकपूर्ण तर्क ही सभी विश्वासों का जन्मदाता है! दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यापक पहचान चाहता था, तो स्वयं को ‘हिंदू’ के रूप में देखने के बजाय ‘द्रवड़ियन’ कह सकता था। क्योंकि, सभी गैर-ब्राह्मण शूद्र आर्य के रूप में मान्य नहीं थे। इसके अलावा वह मानवतावादी राह चुनकर स्वयं को ‘जीवकारुण्य’ को समर्पित करने की सोच सकता था, जिसका आशय प्राणिमात्र के प्रति करुणाभाव दर्शाना है। सबसे मुख्य बात, जिसे विचार किया जाना चाहिए था; वह यह है कि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म में सुधार की उम्मीद नहीं कर सकता। जिन लोगों ने भी इस दिशा में प्रयास किए थे; उन्हें उनके विचारों के कारण भले ही मान-सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल हुई हो, किंतु उससे हिंदू धर्म की संरचना लगभग अपरिवर्तित ही रही। उन्होंने चेताया था कि पुराणों, महाकाव्यों तथा सामाजिक रीति-रिवाजों की प्रामाणिकता हेतु बुद्ध को भी उनमें शामिल कर लिया गया था। रामानुज जैसे सुधारवादियों ने यह काम हिंदू-आस्था को मजबूत करने के नाम पर किया था। (वी.एम. सुबगुनराजन : 257-263)।
पेरियार के लिए समस्या यह नहीं थी कि हिंदुत्व पुरातन के प्रति अतिरेकी आस्थाओं के अंबार तथा उनसे जुड़े आडंबरों से भरपूर है; या वह पूरी तरह अतार्किक है। आधुनिक युग में हिंदुत्व ने चतुराई पूर्वक राष्ट्रवाद का नया कलेवर प्राप्त कर लिया है। पेरियार का कहना था कि राष्ट्रवाद का दबदबा, उसका बढ़-चढ़कर प्रचार, आस्था की भाषा को नई जमीन देता था; जो काफी खतरनाक था। उनके लिए राष्ट्र के नाम पर जादुई आभामंडल तैयार किया जाता था, तथा राष्ट्रवाद पर इतने तीव्र और गर्वीले अंदाज में विचार किया जाता था कि उसकी आलोचना असंभव-प्रायः हो जाती थी। राष्ट्रवाद को उसकी स्वयं-सिद्ध शुभता किसी भी प्रकार के सवालों से परे बहुमूल्य आदर्श के रूप में परिभाषित करने में राष्ट्रवादी ब्राह्मणों की मुख्य भूमिका थी। दूसरी ओर वे सामाजिक दुनिया, जो उनके लिए कृत्रिम भारतीय राष्ट्र का निर्माण करती थी; के आगे भी प्रश्नचिह्न लगाने को तैयार नहीं होते। हालांकि, उन्होंने स्वराज को दमनकारी विदेशी शासन से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया था; लेकिन वे उसके सामाजिक सरोकारों पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे। न ही वे पुराने उत्पीड़क सामाजिक रीति-रिवाजों, जाति, लैंगिक और वर्गीय भेदभाव से मुक्ति को लेकर कोई सवाल उठाते थे। (रिवोल्ट 27 मार्च, 1927; वी. गीता और एस.वी. राजदुरै, 2008 : 34)।
ऐसे समझौतावादी राष्ट्रवाद के विरुद्ध अपने आजीवन संघर्ष के दौरान पेरियार आलोचना की एक साथ दो धाराओं का अनुगमन करते हैं। पहली, सीमित राष्ट्रवादी एजेंडा के विरुद्ध; दूसरी, हिंदू धर्म के विरुद्ध। पहली धारा का समापन स्वयंभू द्रविड़ राष्ट्र की मांग रूप में होता है; जिसमें उन्होंने सभी गैरब्राह्मणों को उसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि, पेरियार कभी-कभी द्रविड़ राष्ट्र की कल्पना को भारतीय राष्ट्र की मांग से मिला देते हैं; जिसके बारे में उनका मानना था कि वह बलपूर्वक घुस आए आर्यों से सुरक्षित है। सच तो यह है कि वे इस मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं देते; सिवाय ब्राह्मण-बनिया गठजोड़ से बने सत्ताकेंद्र की ओर ध्यानाकर्षित करने के। उनके लिए ‘द्रविड़ियन’ का आशय, जैसा कि वे बहुधा लिखते थे; एक बहुमूल्य भाषिक प्रतीक था। एक आदर्श रचना, जो धर्म और जाति के बंधनों से सर्वथा मुक्त, कल्पनालोक की रूपरेखा गढ़ती थी। उन्होंने उसे जातीय अथवा संस्कृति विशेष के प्रभाव से मुक्त रखा था। (कुदी अरासु, 25 जून 1944)।

आलोचना की दूसरी लाइन भी पहली से संबद्ध थी। पेरियार का आग्रह था कि द्रविड़ कार्यकर्ताओं को उन हिंदू विश्वासों का विरोध करना चाहिए, जो मनुष्यता के साथ हील-हवाला करते हैं, तथा अल्पसंख्यक सवर्णों को प्राप्त जन्माधारित शक्तियों एवं अधिकारों को वैध ठहराते हैं। इस अल्पसंख्यक समूह में सम्मिलित ‘आर्य’ यानी ब्राह्मण को बाहरी माना गया, जो महज जातीय अथवा नस्लीय अर्थों में नहीं था। ब्राह्मणों ने एक शक्तिशाली सामाजिक समूह का गठन किया था, तमाम चुनौतियों के बीच वे अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक वर्चस्व की सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित थे। इसलिए वे ऐसा कोई काम करने के लिए इच्छुक नहीं थे, जो सर्वकल्याणकारी हो; जिससे जनसाधारण का हित भी समाहित हो। यही आधार उन्हें बाहरी सिद्ध करता है। उनका धर्म भी मूलतः आरोपण था। वह केवल उन्हीं के हितों की रक्षा तथा बाकी लोगों के सापेक्ष श्रेष्ठत्व के उनके दावे की पुष्टि करता है। (कुदी अरासु, 26 अगस्त, 1928 अनीमुथू, 249)।
पेरियार के लिए हिंदुत्व के विरोध में संघर्ष अपरिहार्य भी था। उन्होंने द्रविड़ बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वे प्रचलित सामाजिक वास्तविकताओं की तर्कसंगत आलोचनाओं को आगे बढ़ाएँ। उनका अभिप्राय था– हिंदूवादी विश्वासों के आगे प्रश्नचिह्न लगाना; उन पर सवाल खड़े करना। पेरियार जानते थे कि हिंदुत्व की आलोचना को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, कदाचित पर्याप्त न हो। इस उद्देश्य के लिए ‘द्रविड़यार कड़गम’ पहले ही स्थापित हो चुका था; तथापि केवल राजनीतिक प्रयासों द्वारा जातिविहीन समाज की स्थापना की सफलता संद्धिग्ध थी। पेरियार के लिए राजनीति, निरंतर परिवर्तनशील घटनाओं और परिस्थितियों के बीच यहीं और अभी कुछ करने जैसा था। दूसरी बात यह थी कि राजनीतिक परिवर्तन, जिनमें राजनीतिक नियमों में बदलाव भी शामिल थे; के लिए आवश्यक नहीं था कि वे सामाजिक स्थितियों में भी परिवर्तनकारी सिद्ध हों। वस्तुतः अधिकांश राजनीतिक नियमों की प्रवृत्ति, प्रचलित सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने के बजाय उन्हें समायोजित करने की होती थी। यदि वे चुनौती देती भी थीं, ऐसा उन्होंने किया भी, तो उनका प्रभावक्षेत्र बहुत सीमित होता था। इस कारण आवश्यक था कि राजनीतिक बदलाव अथवा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के बारे में सोचने के साथ-साथ, व्यक्ति रूढ़िग्रस्त समाज को विचारशील समाज में ढालने पर ध्यान दे।
सामाजिक सक्रियता पर जोर देने का आशय यह नहीं था कि पेरियार राजनीति के सर्वथा विरोधी थे। वे राज्य की शक्ति तथा पहुंच से पूरी तरह परिचित थे। इसलिए वे आजीवन सामाजिक न्याय को लक्ष्य मानकर काम करने वाली सरकारों के समर्थक बने रहे। पेरियार राजनीति के विरोधी भी नहीं थे, मगर वे ऐसी राजनीति का समर्थन करते थे, जो सामाजिक न्याय को अपना लक्ष्य और उद्दिष्ट मानती हो। उन्होंने के. कामराज की कांग्रेस सरकार का समर्थन किया था; क्योंकि वे महसूस करते थे कि कामराज सरकार ने अपेक्षित, त्वरित आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के साथ-साथ आरक्षण को भी महत्त्व दिया था। साथ ही उन्होंने अंतनिर्हित जातीय लाभों के लिए भी संघर्ष किया था। पेरियार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी राजनीति के आजीवन विरोधी रहे। बावजूद इसके वे नेहरू की समाजवादी राजनीति में संभावनाएं देखते थे। उन्हें लगता था कि उससे गैर-ब्राह्मण और दलित लाभान्वित हो सकते थे। (वी.एम. सुबगनराजन : 345-350)।
पेरियार इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि राजसत्ता, यदि वह सामाजिक न्याय के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर न हो तो किस तरह आसानी से वर्चस्वकारी शक्तियों की तरफदारी करने लगती है। द्रविड़यार कड़गम इस मामले पर विशेष संवेदनशील था कि किस प्रकार क्षेत्रीय सरकार, विशेषरूप से उसके अधिकारीगण; वर्चस्वकारी जातियों से तालमेल बनाकर उनके वर्गीय हितों की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए 1960 के दशक से ही कड़गम, जिसके मुखिया उन दिनों पेरियार थे; ने मांग की थी कि दलितों को स्थानीय निकायों, विशेष रूप से पुलिस, थाना, राजस्व विभाग में अनिवार्यतः भर्ती किया जाना चाहिए। क्योंकि, ये क्षेत्र स्थानीय जातियों और राजनीतिक शक्ति के प्रमुख केंद्र बने थे। उन्होंने यह मांग भी की थी कि दलितों को गांव के बीच में, ब्राह्मणों या सवर्णों के पड़ोस में, जिनसे उन्हें दूर रखा गया था; उन्हें घर बनाने के लिए जमीनें दी जानी चाहिए। (वी.एम. सुबगनराजन : 361-362)।
फिर भी पेरियार के लिए राजनीति मात्र अवांतकर कथा के समान थी। मूल कहानी जाति और धर्म पर केंद्रित थी; इन दोनों की उन्होंने अनथक स्थाई और लगातार आलोचना की थी।
पेरियार के लिए हिंदू धर्म और उसकी जाति-व्यवस्था के बीच स्वयं-सिद्ध संबंध था; ठीक ऐसे ही जातिवाद विरोधी सक्रियता भी पीढ़ियों से मौजूद रही है। उनके अनुसार, हिंदू धर्म भेदभावपूर्ण जातीय स्तरीकरण के सिवाय कुछ नहीं है। जाति ही इसका मूल सिद्धांत इसकी असली जीवनधारा है। इसके ग्रंथ सामाजिक भेदभाव और ऊंच-नीच का समर्थन करते हैं। इसकी प्रथाओं ने अमानवीय और बर्बर रीति-रिवाजों को स्वीकृति दी है। वे सब मिलकर सामाजिक ऊंच-नीच और भेदभाव का समर्थन करते आए हैं। सामाजिक रीति-रिवाजों और धर्मशास्त्रों की व्याख्या पर उसके पुजारियों का एकाधिकार बना हुआ है। उसके माध्यम से वे जाति के आधार पर बंटे समाज के आध्यात्मिक मामलों के स्वार्थपूर्ण प्रबंधक तथा उनके एकमात्र अधिकारी बने हुए हैं।
यह भी पढ़ें : पेरियार के इंकलाबी बोल : जाति का उन्मूलन
पेरियार के लिए जाति और धर्म का अंतःसंबंध बहु-व्यापी है। यह ज्ञान और ज्ञानार्जन के समस्त साम्राज्य, श्रम और शिल्पकर्म की दुनिया में दुनियादारी और यहां तक कि आंतरिक संबंधों के बीच भी अनेकानेक रूपों और स्तरों पर लागू होता है।
जहां तक ज्ञान और ज्ञानार्जन का संबंध है; वे सभी ब्राह्मणों के विशेषाधिकार में शामिल थे तथा उनके शास्त्रों, पुराणों एवं स्मृतियों के पठन-पाठन सहित उनकी विवेचना करने के ईर्ष्यापूर्ण एकाधिकार द्वारा निर्देशित थे। बाकी लोगों को उन्होंने इससे वंचित किया हुआ था। पेरियार का तर्क था कि उन सभी को, जिनके जीवन ब्राह्मणों के बनाए नियमों के अनुशासित होते थे; उन्हें इन नियमों या इनके निर्माताओं की अच्छाई या बुराई को चुनौती देने का न तो अधिकार था; न उनमें वैसी क्षमता थी। (कु.अ., 15 अगस्त, 1926; अनीमुथू, 11)।
आधुनिक युग में चीजें बदल चुकी थीं। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था; तथापि बहुत कम लोग धर्म और धार्मिक रीति-रिवाजों को लेकर प्रश्न उठाने का साहस जुटा पाते थे। साथ ही, जैसा पहले था; हिंदू धर्म आज भी मनुष्य ने क्या खाया है? कैसा पहना हुआ है? यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर उसके व्यवहार, सामाजिक संबंधों–संक्षेप में उसके सदाचरण और दुराचरण, मानवीय उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। (कु. अ., 9 नवंबर, 1946; अनीमुथू, 1197-98)।
पेरियार ने लिखा था कि हिंदू विश्वास जाति-भेद को जिंदा रखने, असमानता को स्वीकार्य बनाने में सहायक थे। वे सुनिश्चित करते थे और जातीय विधान एवं धार्मिक संरचनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को दंडित किया जाए। उन्होंने छूआछूत को कायम रखा तथा उसकी उपस्थिति को न्याय-संगत ठहराया था। (वही)।
पेरियार के अनुसार, इस तंत्र की असफलता के साथ ही इसके आस्था-संबंधी मामलों में अड़चन इसलिए पैदा हुई, क्योंकि आध्यात्मिक मामलों में ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता को एकाएक चुनौती मिली थी। इस चुनौती को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें की जानी अत्यावश्यक थीं। पहला, धर्म के संबंध में ब्राह्मण की प्रभुसत्ता को समझना; यह जानना कि उनका सारा ज्ञान वस्तुतः अतार्किक है और अधिकांश उन्हीं के द्वारा फैलाया गया था। उन्हें विश्वास था कि अध्यात्म और परंपरा-संबंधी मामलों की असलियत को केवल तर्क के सहारे समझा जा सकता है। जनेऊ पर लिखे अपने एक निबंध में पेरियार ने ब्राह्मणों के ज्ञानानुराग का उपहास उड़ाया था। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार एक धागा ब्राह्मण की संतान को उसके वास्तविक चरित्र और आचरण से परे संपूर्ण प्रतिष्ठा और अथाह शक्तियां प्रदान करता था। यही कारण है कि ब्राह्मण संतान अभाव और विपन्नता में जन्म लें, तो भी न तो उसका जनेऊ धारण का अधिकार बाधित होता था, न ही उस धागे से जुड़े विश्वास में कोई कमी आती थी। जबकि, दूसरे समुदाय की संतान, वह चाहे जितनी स्वच्छ, पवित्र और देखने में आकर्षक क्यों न हो; उसे जनेऊ धारण करने के अधिकार तथा उसके आधार पर प्राप्त मान-सम्मान से वंचित कर दिया जाता था। दूसरे, कोई ब्राह्मण जनेऊ धारण करे या न करे, उससे जुड़ी परंपराओं के नियमानुसार पालन में सफल रहे या असफल; वह उन सभी सामाजिक पद-प्रतिष्ठा से गौरवान्वित हो सकता है, जो उसे जनेऊ के आधार पर प्राप्त हैं। दूसरी ओर यदि कोई गैर-ब्राह्मण अपने ज्ञान और पवित्र कर्मों के आधार पर जनेऊ धारण करना चाहता है, तो उसे उसको धारण करने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। (कु.अ., 27 दिसंबर, 1925)।
विचारणीय यह है कि ज्ञान और बुद्धिमानी के प्रति ब्राह्मण का दावा न तो उसकी योग्यता पर निर्भर है, न ज्ञान के प्रति उसकी उत्सुकता से। बजाय इसके ये दावे महज जन्म के संयोग तथा उन विशेषाधिकारों से संबंधित हैं; जो इसके साथ स्वाभाविक रूप से चले आते हैं।
ज्ञान और योग्यता के ब्राह्मणवादी दावे के बरक्स पेरियार तर्क की दावेदारी करते हैं। उनके अनुसार सभी मानवीय प्राणी बौद्धिक चिंतन में सक्षम थे और सभी मामलों में, चाहे वे धार्मिक हो, सामाजिक हों अथवा राजनीतिक–उपलब्ध प्रमाणों के विश्लेषण; सभी में तर्क करने, समझने तथा उपयुक्त निष्कर्ष तक पहुंचने की योग्यता थी और अपनी निर्णय क्षमता का इस्तेमाल करते थे। पेरियार ने खुद भी धर्म और राजनीति पर अपने क्रांतिकारी विचारों को तर्कसंगत ढंग प्रस्तुत किया था। इसके बावजूद अपने अनुयायियों से उनका आग्रह था कि उनके विचारों का भली-भांति परीक्षण किए बगैर उन्हें स्वीकार न करें। वे अकसर कहा करते थे कि आने वाले दशकों में उनके विचार पुरातनपंथी, यहां तक कि निरर्थक सिद्ध हो सकते हैं। यही उनका तर्क-आधारित, मुक्त चिंतन एवं परीक्षण द्वारा ज्ञानार्जन का रास्ता था। गैर-ब्राह्मण और दलित उस ज्ञान-पद्धति को अपनाकर लाभान्वित हो सकते हैं तथा अच्छे और न्यायसंगत समाज की रचना में उसका सदुपयोग कर सकते हैं।
पेरियार समझाते हैं कि अतीत में ब्राह्मणों की वर्णाधारित ज्ञानार्जन प्रणाली किस प्रकार श्रम का जाति-आधारित विभाजन करती थी। यह दो तरह से काम करती थी। जाति का स्तर समाज में समृद्धि-अनुपात भी तय करता था। मालदार और विशिष्ट वर्ग में शामिल थे– पुरोहित, अधिकारी, वकील, दुकानदार, पूंजीपति, जमींदार और मिरासीदार। ‘उच्च कुल’ में जन्म के आधार पर उन्हें धन-संपदा और प्रतिष्ठा अर्जित करने का अधिकार था। बाकी लोग उसी तर्क के आधार पर, श्रम के लिए ढकेल दिए जाते थे। (कु.अ., 6 सितंबर 1931, अनीमुथू, 1640)।
विशिष्ट वर्ग अपनी सुख-समृद्धि और संपन्नता को न्याय-संगत मानता था। क्योंकि, पवित्र धर्मशास्त्रों की व्यवस्था थी कि ‘शूद्र को संपत्ति अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि किसी शूद्र के पास संपत्ति है; तो ब्राह्मणों को पूरा-पूरा अधिकार है कि वे उसे बलपूर्वक छीन लें।’ पेरियार ने संकेत किया था कि इस तरह के सुविधाजनक विचार आधुनिककाल में भी महत्त्वपूर्ण और कारगर हैं। गांधी ने वर्णाश्रम धर्म को चतुराईपूर्वक नए सिरे से स्थापित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि गांव के गरीब आदमी को ‘मुंबई के बनिए जितना धन जमा करने की इच्छा’ नहीं करनी चाहिए। बजाय इसके ‘वह श्रद्धापूर्वक अपना काम करेगा; गाय चराएगा; जूते गांठेगा।’ (कु.अ., 13 सितंबर, 1931 अनीमुथू, 1640-43)।
दूसरे, हिंदू धर्म ने खास लोगों के लिए खास श्रम का प्रावधान किया था। इस रूप में कि वे केवल वही काम कर सकते हैं; कुछ और नहीं। इस प्रणाली को उन्होंने स्मृतियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं तथा राजाओं की दमनकारी ताकत के भरोसे लागू किया था। ब्राह्मणों के समर्थन पर यह वर्ग हजारों वर्षों से अपनी अधिसत्ता को भोगता आया है। (कु.अ., 14 अप्रैल, 1929 अनीमुथू, 255)।
तदनुसार कोई मजदूर किसी काम को करना चाहे या नहीं; उस पर वह कार्य थोप दिया जाता था। आशय यह नहीं है कि मजदूर थोपे गए काम को लाभदायक या रचनात्मक मानने से इनकार करते थे। इसलिए कि आधुनिक युग में भी मजदूर वर्ग की विकास या प्रगति संबंधी चेतना, उनके आर्थिक स्तर द्वारा निर्धारित नहीं होती; न ही समाजार्थिक शोषण के प्रति उनकी उनकी समझ द्वारा तय की जाती है; अपतिु सामाजिक स्तर पर इस घोषणा द्वारा तय होती है कि वे इस या उस वर्ण से संबंध रखते हैं। इस तरह यदि कोई बुनकर या लोहार अपना ब्राह्मणीकरण करना चाहता है; तो दूसरा कोई शिल्पकार उसे रोककर, स्वयं ‘ऋषि-पद’ को प्राप्त करना चाहेगा। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म की संरचना ही ऐसी है कि इसमें मजदूर ‘वेतन श्रमिक’ के बजाय ‘जातीय श्रमिक’ बने रहना चाहते हैं। जाति के संदर्भ में सर्वहारा चेतना का निर्माण जाति-व्यवस्था और धार्मिक अनुराग, जो उसे संरक्षित करते हैं; को चुनौती दिए बगैर संभव नहीं है। (विदुथलाई, 16 फरवरी 1940; अनीमुथू, 1748-50)।
पुनश्चः पेरियार के अनुसार, वर्णधर्म के आधार पर गठित समाज में श्रम का न तो अंतनिर्हित मूल्य होता था, न उसकी गरिमा। यदि यह जीवित रहने के आवश्यक हो, तब भी इसे प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जाता था। और भी बुरा तब होता है, जब विशेषाधिकार संपन्न वर्ग खुद काम करने से इनकार कर, दूसरों के श्रम पर जीने पर जोर देने लगता है। उसकी देखा-देखी श्रमिक वर्ग भी मानवीय श्रम से कतराने लगता था; उनके बीच उसके सामाजिक औचित्य को बिना जाने-समझे ब्राह्मण, अपने अध्ययन-मनन का निरंतर दावा करते हुए; खुद को मानसिक श्रम का एकमात्र अधिकारी बनाने लगता है। (कु.अ., 14 जून, 1931; अनीमुथू, 1658-60)।
पेरियार का तर्क था कि जब तक धार्मिक मान्यताओं को, जो जाति-आधारित श्रम-विभाजन को न्यायोचित ठहराती हैं; चुनौती नहीं दी जाती–तब तक असमानता और भेदभाव बने रहेंगे। श्रमिक संगठनों की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष हो सकता है। पेरियार के अनुसार यह केवल मार्क्स, ऐंगल्स और लेनिन के लिखे को रट लेने, अथवा यह कहने से नहीं होगा कि ये पूर्वज्ञात सत्य की परिणतियां थीं। समाजविज्ञानियों को इसे विशिष्ट सामाजिक सत्य, भारतीय समाज की विशेषताओं के रूप में समझना होगा, जिसे मार्क्स अथवा लेनिन से पूरी तरह जानने की अपेक्षा नहीं की जा सकती–
‘‘क्या मार्क्स इस देश के ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई प्रभुसत्ता से परिचित था? क्या वह जानता था कि अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वे किस तरह षड्यंत्र रचते हैं? क्या वह जानता होगा कि इस देश के मूल निवासियों को, जन्म से ही शूद्र, गुलाम माता-पिताओं की संतान माना गया है? कि इस देश में ऐसी धार्मिक और शास्त्रोक्त विद्या है, जो इसे वैध ठहराती है? मार्क्स ने पूंजीवाद और उसके वर्चस्व के बारे में कहा है, बताया है कि धर्म किस प्रकार विशिष्ट संदर्भों और वास्तविकताओं में पूंजीवाद शोषण को न्यायोचित ठहराता है। यह उम्मीद करना कि मार्क्स हमारे हालात से परिचित था; न तो उचित है, न ही न्यायपूर्ण।’’(विदुथलाई, 20 सिंतबर, 1952; अनीमुथू: 1746)।
मार्क्स के विपरीत पेरियार का कथन तर्कसंगत है कि जाति-आधारित श्रम की समाप्ति हो; ताकि हम श्रमिक के जीवन के बारे में नए सपने देख सकें–
‘‘यहां तक जातीय विभाजन को पेशागत विभाजन में बदल दिया था, तब भी इस तरह के विभाजन को क्यों होना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति सुबह को बढ़ई, दोपहर बाद व्यापारी और रात को अध्यापक नहीं हो सकता; और इसके साथ-साथ क्यों ऐसे समय में, जब किसी व्यक्ति का दमन हो रहा हो; दूसरे आदमी की मदद के लिए आगे नहीं आ सकता।’’(कु.अ., 11 जनवरी, 1931)
पेरियार के अनुसार, जाति और धर्म आधारभूत आर्थिक ढांचे को मनचाहा रूप देने के अलावा सामाजिक संबंधों पर भी गहरा असर डालते हैं। किसी व्यक्ति के लिए, यहां तक कि दलित और शूद्रों के लिए भी; आत्मसम्मान का अभाव असमान और अपमानजनक सामाजिक संबंधों का कारण बन सकता है। ध्यातव्य है कि पेरियार ने जातीय उत्पीड़न के शिकार लोगों से आग्रह किया था कि वे देखें कि वे स्वयं महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जाति-व्यवस्था के अस्तित्व के लिए स्त्री की अधीनता, उसके चाल-चलन पर सवाल खड़े करना आवश्यक था। पत्नीत्व, मातृत्व और योनि-शुचिता के अतिरेकी महिमा-मंडन द्वारा जाति-केंद्रित समाज में स्त्री का अस्तित्व महज प्रजननीय प्राणी में सिमट चुका था। उसके माध्यम से ही वह अपने अस्तित्व को बचाए हुए था। (कु.अ., 8 फरवरी, 1931)।
पेरियार जानते थे कि जाति-व्यवस्था बंधुत्व-भावना के लिए काम नहीं करती। असल में वह आपसी संदेह और नफरत को बढ़ाती है। हिंदू आस्था और ब्राह्मणों का आधिपत्यपूर्ण आचरण, दलितों एवं शूद्रों को कई तरीकों से प्रभावित करता है। छूआछूत अपने आपमें विशिष्ट स्थिति थी। समग्र जातीय संदर्भों और तर्कों को समझते हुए, उसका सामना सीधे-सीधे किया जाना था। दूसरे केवल छूआछूत को समाप्त करना पर्याप्त नहीं था, अपितु वर्ण-धर्म नामक पूरी संस्था को मिट जाना चाहिए था। शूद्रत्व का मामला थोड़ा अलग था। हालांकि, शूद्र भी एक सीमा तक ही ‘स्पृश्य’ थे। ब्राह्मण की निगाह में उन्हें भी हीन और ओछा माना जाता था। लेकिन, जैसा पेरियार लिखते हैं– ‘शूद्र अपनी अस्थिर, अनिश्चित, अमानवीय परिस्थिति को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। इस कारण एक ओर तो उन्हें ब्राह्मणों का पिछलग्गू बनते हुए देखा गया। दूसरी ओर खुद को दलितों से अलग दिखाते हुए।’ दलितों के प्रति शूद्रों के विद्वेष पर चर्चा करते हुए पेरियार लिखते हैं–
‘‘गैर-ब्राह्मणों के बीच भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जो जातिभेद को अपनाए हुए हैं। लेकिन, यदि आप चाहते हैं कि उच्च जातियां आपको अपने बराबर समझें, तो आपको उन जातियों को जो आपसे निचले क्रम पर हैं; अपने बराबर मानना पड़ेगा। कभी-कभी मुझे लगता है कि हम जो जातीय उत्पीड़न करते हैं, वह ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले जातीय उत्पीड़न से अधिक है। नट्टुकोट्टई चेटियार (तमिलनाडु की व्यापारी जाति), जिनके पास अपार धन-संपदा है; वे उसे वेदों के अध्ययन-अध्यापन पर खर्च करना चाहते हैं। यह ठीक ऐसा ही है, जैसे कोई अपनी छुट्टियां आजीवन भिक्षावृत्ति सीखने में अकारथ करे। वे न केवल ब्राह्मणों को खिलाते-पिलाते हैं, अपितु वेदाध्ययन के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। यदि वे अपने धन का सदुपयोग कुछ आदि-द्रविड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए करते, तो वे किशोरावस्था से ही कुली का काम करने को विवश न होते।’’ (कु.अ., 9 दिसंबर 1928, अनीमुथू, 332)।
अन्य अवसर पर पेरियार आवेश में लिखते हैं–
‘‘जब हम आदि-द्रविड़ों की बात करते हैं, तो बात समझ में आती हैं कि उससे ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। लेकिन, यह मेरी समझ से बिलकुल परे है कि गैर-ब्राह्मण भी उससे हतोत्साहित हो जाएंगे। यदि आप वास्तव में खुद को शूद्र समझे जाने पर अपमानित महसूस करते हैं, तब क्या आप उस समय क्षण-भर के लिए भी असहज महसूस करते, जब हम कहते हैं कि अछूत-भाव को भी पूरी तरह नष्ट हो जाना चाहिए।’’ (कु.अ., 11 अक्टूबर 1931, अनीमुथू, 60)।
पेरियार ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों की ‘जातीय-उन्नयन’ की इच्छा को भी निरर्थक माना है। उनके अनुसार–
‘‘प्रत्येक जाति-वर्ग अपनी श्रेष्ठता संबंधी दावों की खोजकर उन्हें प्रस्तुत कर सकता है। परंतु, वे सभी प्रमाण केवल इस दावे की पुष्टि करेंगे कि बाकी सभी जातियां उन लोगों से, जो स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं; हीन हैं।’’ (कु.अ., 30 नवंबर, 1930, अनीमुथू, 1599)।
सामाजिक अनुकरण की प्रवृत्ति का सामना करने के लिए पेरियार समझाते हैं कि शूद्रों को शिक्षा द्वारा, ब्राह्मण पुजारियों एवं ब्राह्मणवादी परंपराओं का बहिष्कार करके तथा स्त्री को शिक्षा एवं समानता का अधिकार देते हुए अपना आधुनिकीकरण करना चाहिए। यह जानते हुए कि शूद्र दक्ष शिल्पकार रह चुके हैं; पेरियार ने उन्हें विज्ञान के लाभों को प्राप्त कर तकनीकि दक्षता में सुधार के लिए भी प्रोत्साहित किया था।’’ (वी.एम. सुबुगनराजन : 119-121)।
1940 के दशक से ही पेरियार उनसे हिंदुत्व के परित्याग का अनुरोध करते आ रहे थे। यह बताते हुए कि भारत बहुत जल्दी स्वतंत्र हो जाएगा, तब उस पर ब्राह्मणों और बनियों का राज होगा। ऐसे में हिंदुत्व के परित्याग एवं धर्मनिरपेक्ष ‘द्रविड़यन’ पहचान के लिए उन्हें अभी से अपना आत्मसम्मान सुरक्षित रखकर अपनी स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करना चाहिए।
दलितों के लिए पेरियार के भाषण भिन्न थे। उन्होंने दलितों से कहा था कि परस्पर एकजुट रहें, स्थानीय जातिवादी राजनीतिक शक्ति और सत्ताओं को चुनौती दें तथा गांधीवादी संस्थानों का दृढ़तापूर्वक परित्याग कर दें। उन्होंने दलितों से अनुरोध किया था कि वे हिंदुत्व से बाहर आएं। यदि आवश्यक हो तो कोई और धर्म जो न्यायपूर्ण लगता हो और उनके समानता और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता हो, उसे अपनाएं। इसके साथ-साथ पेरियार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि शूद्र स्वयं को श्रेष्ठतर समझ सकते हैं। मगर, असलियत में वे बिलकुल नहीं है। क्योंकि, जाति-आधारित समाज उन्हें सम्माननीय मानने से इनकार करता है। ब्राह्मण धर्मशास्त्र और स्मृतियां शूद्र को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती हैं, जो ‘‘दास, वेश्या अथवा रखैल की औलाद हो; जन्मजात दास हो अथवा दास के रूप में बड़ा हुआ हो।’’ (कु.अ., 16 जून 1929, अनीमुथू, 57)।
शूद्र-दलित अंतर्संबंधों को पेरियार तथा उनके आन्दोलन ने कितनी दक्षता से संभाला था। इसका सटीक उदाहरण कल्लर समुदाय (जिन्हें आज पिछड़ी जाति का दर्जा दिया गया है) द्वारा दलितों पर लगाए गए प्रतिबंध थे; जिन्हें आज कुख्यात देवकोट्टई आदेशों के नाम से जाना जाता है। इस मामले को पेरियार ने क्षेत्र में आयोजित पहले आत्मसम्मान सम्मेलन में उठाया था। सम्मेलन की अध्यक्षता भलीभांति समृद्ध व्यापारी वर्ग, चेट्टियार समुदाय के वरिष्ठ-जनों ने की थी। उस सम्मेलन में हिंसा तथा उसके जिम्मेदार शूद्र समुदाय के लोगों की निंदा का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। सम्मेलन में उस दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। खास बात यह है कि उस सम्मेलन में उन शूद्रों की प्रशंसा की गई थी, जिन्होंने दलितों पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया था। उस सम्मेलन में जो भाषण हुए उनमें दलितों के बराबरी के अधिकार का समर्थन किया गया था। (वी.एम. सुबागराजन : 193)।
स्पष्ट है कि ‘जाति का विनाश’ शूद्रों और दलितों से अलग-अलग अपेक्षाएं रखता था। पेरियार को ‘आत्म-सम्मान समुदाय’ बनाने की मांग अभी करनी ही थी; उसमें द्रविड़यन बिरादरी की घोषणा भी शामिल थी; जो उन्हें साहचर्य की नई संस्कृति के तहत परस्पर निकट लाने वाली थी। इस लक्ष्य को जड़ हिंदू विश्वासों, रीति-रिवाजों के सतर्क खंडन तथा जीवन के नए रास्तों का चयन के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। उसमें अंतर्जातीय विवाहों, स्त्री को सहयात्री मानने, कार्यक्षेत्र, परिवार या अंतरंग संबंधों के मामले में उन्हें उनकी मर्जी के अनुसार जीवन जीने में मदद करना भी सम्मिलित था।
दलितों एवं पिछड़े वर्गों में भाईचारा कायम करना और उसे बनाए रखना आसान न था। क्योंकि, उसके मूल में भौतिक संबंधों, यथा– शक्ति, संपदा, श्रम आदि से जुड़े अनेकानेक अवरोधक थे। दूसरे, शूद्र अपने आधुनिकीकरण को लेकर पेरियार के आह्वान को तो गंभीरता से लेते थे, परंतु उनकी आपसी भाईचारे की अपील के प्रति उतने गंभीर नहीं थे। विभिन्न शूद्र जातियों के काफी लोग, कभी-कभी भारी संख्या में; छूआछूत विरोधी संघर्ष में सबसे आगे थे। वे अंतर्जातीय विवाहों, विशेषरूप से शूद्रों और दलितों के बीच; का समर्थन भी करते थे। बावजूद इसके शूद्र जातियों का एक उल्लेखनीय हिस्सा ऐसा भी था, जो ब्राह्मणवाद की आलोचना का दिल से समर्थन तो करता था; मगर दलितों के साथ संपूर्ण एकता के आह्वान को अनसुना कर देता था।
पेरियार के स्त्री-पुरुष दोनों को बराबर का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी हर समय, समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि, इस पर कायम रहना कठिनतम आदर्श था। तथापि, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऐसे स्त्री-पुरुष भी बहुतायत में थे, जो आपसी सम्मान, समानता और साझा राजनीतिक विश्वासों के आधार पर अलग तरह के पारिवारिक और अंतरग जीवन जीने के लिए संकल्परत थे।
पेरियार ने हिंदुत्व की सिर्फ आलोचना नहीं की थी। इसके साथ-साथ उन्होंने एक श्रेष्ठ और न्यायपूर्ण समाज के अपने और अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं के प्रगतिगामी सपने को निरंतर प्रचारित किया था। 1910 के दशक के अंतिम तथा 1920 के शुरुआती वर्षों में, जब पेरियार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे; उनके लिए श्रेष्ठ समाज का अर्थ ऐसे समाज से था, जिसे सृजनात्मक कार्यक्रमों के आधार पर बनाया जा सके। वे गांधी की ओर उनके त्रिसूत्रीय कार्यक्रमों, यथा– छूआछूत उन्मूलन, संयम एवं सहिष्णुता तथा खादी के कारण आकर्षित हुए थे। आगे चलकर कांग्रेस के एक वर्ग तथाकथित स्वराजियों के असहयोग आन्दोलन से किनारा करने तथा विधायिकाओं में प्रवेश करने की मांग का गांधी ने समर्थन किया, तो उनका कांग्रेस से एकाएक मोहभंग हो गया। उन्हें लगा कि उपर्युक्त तीन महत्त्वपूर्ण कारण, जो उनकी दृष्टि में गैर-ब्राह्मणों और दलितों के जीवन के लिए विशेष आशाजनक थे; के साथ समझौता किया गया है। गांधी के प्रति उनकी मायूसी बढ़ती ही गई। आगे चलकर जब गांधी द्वारा उतने ही उत्साह से वर्णधर्म की सुरक्षा तथा छूआछूत के खात्मे के लिए प्रतिबद्धता का दावा किया गया; पेरियार ने लिखा था–
‘‘यदि वर्ण-व्यवस्था अस्तित्व में नहीं होती, तो अस्पृश्यता भी, जो उसकी देह का प्राणतत्त्व है; जीवित नहीं रह पाएगी।’’ इसलिए, ‘यदि हम महात्मा के अस्पृश्यता उन्मूलन के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, तो हम दोबारा अस्पृश्यता, जिसे हम समाप्त करने के प्रयास में लगे हैं; के गहरे गर्त में जा पड़ेंगे।’’ (कु.अ., 7 अगस्त, 1927 अनीमुथू, 1976-77)।
गांधी से मोहभंग ने पेरियार को जाति और अस्पृश्यता से टकराव तथा श्रेष्ठ समाज हेतु अपने सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उससे पहले कांग्रेस में रहते हुए ही उन्होंने साफ कर दिया था कि स्वराज की मांग को उन लोगों के अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए, जिन्हें शिक्षा और सरकार में उनकी न्यायोचित सहभागिता से अभी तक वंचित रखा गया है। इसके साथ-साथ उसमें तथाकथित अस्पृश्यों की जरूरतें भी शामिल होनी चाहिए–
‘‘हम (अस्पृश्यों को) वे अधिकार देने से भी इनकार करते हैं, जो कुत्तों और सूअरों को आसानी से प्राप्त हैं। क्या स्वराज हमारे संदर्भ में अनिवार्य है? जनता से ही पूछना चाहिए कि उसके लिए महत्त्वपूर्ण क्या है? स्वराज या अस्पृश्यों की प्रगति तथा उनके लिए आत्मसम्मान भरे जीवन की उपलब्धता।’’ (कु.अ., 31 जनवरी, 1926, अनीमुथू, 450)।
उन्हें इस बात से हैरानी थी कि जिस समाज में आत्मसम्मान का अभाव हो, वहां स्वराज का क्या अर्थ हो सकता है–
‘‘तिलक का दावा है कि स्वराज उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। चूंकि, वर्णव्यवस्था के अनुसार वे ब्राह्मण हैं और ऐसे मनुष्य मानते हैं कि बाकी लोग उनसे हीन हैं; यह भावना ही अपने आप में उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए, इस अर्थ में तिलक को ‘स्वराज’ शब्द का उपयोग करने के लिए बाध्य किया गया था; जो इस उद्देश्य हेतु निरर्थक, परिणामों की दृष्टि से भ्रांतिपूर्ण, अपने जन्मसिद्ध अधिकार के लिए राजनीति से अपनाया हुआ है। मगर हम दूसरों को भरमाकर जीवित रहने के अभ्यस्त नहीं हैं। बजाय इसके हम मनुष्यता को उसके वास्तविक अर्थों में खोजने के इच्छुक हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ‘आत्मसम्मान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।’ हमें यह मानना होगा कि स्वराज तभी संभव है, जब पर्याप्त आत्मसम्मान हो; अन्यथा यह अपने आप में संद्धिग्ध मसला है।’’ (कु.अ., 9 जनवरी 1927, अनीमुथू, 3-4)।
‘आत्म-सम्मान’ की सैद्धांतिकी का खूब प्रचार-प्रसार किया गया; और आने वाले दशकों में यह प्रमाणित हो गया कि यह स्वराज की राजनीति के साथ-साथ धर्माडंबरों और धर्मादेशों के भी विरुद्ध है; जो इस प्रकार की राजनीति का संरक्षण करते हैं। इसके अंतर्गत एक ओर तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों की न केवल आलोचना की गई, बल्कि बेहतर जीवन और उसकी संभावनाओं की वैकल्पिक रूपरेखा भी तैयार की गई। पेरियार के नेतृत्व में जैसे ही आत्मसम्मान आन्दोलन की जमीन तैयार हुई, इसके सदस्य, स्त्री-पुरुष दोनों नए मानवादर्शों, रूपांतरित मानव-संबंधों पर बातचीत करने लगे थे। निजी और घरेलू संबंधों को लेकर भी उदारतापूर्ण ढंग से पुनर्विचार की मांग उठने लगी थी।
दूसरी ओर, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादियों को भी नहीं बख्शा गया था। राष्ट्रवाद, जैसा ऊपर कहा गया है; की आलोचना नए और पक्के धर्म के रूप में की गई। जिसके शिखर पर महात्मा गांधी के रूप में एक भद्र राजनीतिक तानाशाह विराजमान है; जिनकी प्रेरक वाणी इस धर्म को जादुई आभामंडल प्रदान करती है–
‘‘उनका धार्मिक बाना, ईश्वर संबंधी व्याख्यान, सत्य का अनवरत संदर्भ, अहिंसा, सत्याग्रह, हृदय-शुद्धि, आत्मशक्ति, उपवास एक ओर तथा उनके शिष्यों एवं अन्य राष्ट्रवादियों, पत्रकारों, जो राजनीति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर उन्हें एक साधु, क्राइस्ट, पैगंबर, मसीहा, महात्मा….तथा विष्णु का सच्चा अवतार…दूसरी ओर….साथ में धनाढ्य और पढ़े-लिखे लोगों द्वारा गांधी नाम का अवसरानुकूल उपयोग, सब मिलकर गांधी को राजनीतिक तानाशाह बना चुके थे।’’ (23 जुलाई, 1933; अनीमुथू, 389-90)।
पेरियार गांधीवादी प्रतिरोध के सबसे उत्कृष्ट माने गए रास्ते ‘सत्याग्रह’ के भी आलोचक थे। उनका तर्क था कि इसने समाज के दबंगों की सत्य को खास संदर्भों में समझने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए, वह नैतिक रूप से संद्धिग्ध और अनेकार्थी है। दूसरे, सत्याग्रह ऐसे वातावरण में काम नहीं कर पाएगा, जहां सामाजिक न्याय का अभाव हो। वह भूमिहीन दलितों को जमीन दिलवाने में मदद नहीं कर पाएगा, न ही वह उस धन में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकेगा है, जो मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं में सुरक्षित है; न ही सत्याग्रह जमींदारों, व्यापारियों और राजाओं के विरुद्ध काम करने में सक्षम होगा, जो कामगारों को अपने स्वार्थ के अनुरूप जकड़े रहते हैं और बदले में महज उतना ही देते हैं, जिससे वह श्रम के लिए जीवित रह सकें। (कु.अ., 6 सिंतबर, 1931)।
गांधीवादी धर्मनिष्ठता के मुकाबले, विशेषरूप में सत्याग्रह और राष्ट्रवाद के सापेक्ष; पेरियार ने आत्म-सम्मान का दर्शन प्रस्तुत किया था; जिसकी नींव आपसी संवाद, प्रोत्साहन और तर्क पर रखी गई थी। पेरियार ने लिखा है कि अनिवर्चनीय, अव्यक्त सत्य बोलने-करने के दावे के विरोध में, आत्म-सम्मानी व्यक्ति लोगों की राय बलपूर्वक राय बदलने के बजाय उन्हें इस दिशा में मात्र प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने इस कस्बे से उस कस्बे, इस गांव से उस गांव तक की यात्राएं की थीं। वहां वे लोगों की बैठक करने, उनसे सुनने, यदि सहमत हों तो उन शब्दों को आत्मसात करने की अपील करते थे। उन्होंने अवसर या संदर्भ के अनुरूप अपने विचारों को बदलने या व्याख्या करने की कोशिश नहीं की थी। पेरियार का जनता से संवाद करने का यह तरीका, कांग्रेस के राजनीतिक अभियान और जनसभाओं को संबोधित करने से अलग था। कांग्रेस की रुचि अपने शक्ति प्रदर्शन तथा लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में थी। वह सीधे-सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति अनादर और उत्तेजना से भरपूर थी। कांग्रेसी नेताओं जनता को शिक्षित करने के बजाय मामले को लेकर उसकी भावनाओं और संवेदनाओं को भड़काते रहते थे। (वही)।
1930 के दशक में पेरियार तथा आत्मसम्मान आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने अपने दर्शन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की थी; जिसमें उन्होंने अपने स्वयं को समाजवादी आदर्शों तथा सशक्त एवं तर्कसंगत नास्तिकता से जोड़ा था। उनके द्वारा कांग्रेसी राष्ट्रवाद के सशक्त और सार्थक विरोध ने, विशेषरूप से गांधी के निरंतर चलने वाले अनशनों और बाद में पूना समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जनमानस में क्रांतिकारी त्वरा के साथ अपनी जगह बनाई थी। यह उस समय भी उपयोगी सिद्ध हुई, जब उन्होंने भारत में साम्यवादी आन्दोलन की विस्तृत समीक्षा की थी; जिसमें उन्होंने जाति के विनाश तथा उसे अपनी राजनीति का केंद्रीय विषय बनाने के प्रति साम्यवादियों की अरुचि की आलोचना की थी। (कु.अ., 25 मार्च 1944, अनीमुथू, 1711-13)।
इस बीच पेरियार हिंदुत्व की आलोचना करते रहे। 1940 के दशक में जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी थी; वह लोगों का ध्यान तेजी से अपनी ओर खींचने में सफल रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री (1937 के चुनावों के बाद जब उन्हें मद्रास प्रांत का प्रधानमंत्री चुना गया था) के नाते, कांग्रेस जब हिंदुस्तान की विविध संस्कृति को मानने वाली जनता पर ‘हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान’ अथवा ‘हिंदुस्तान का विचार’ के रूप में एकल भाषा और संस्कृति तथा ब्राह्मण-बनिया नेतृत्व को थोपने की कोशिश कर रही थी; उसके विरोध में पेरियार और उनके साथियों को कांग्रेस और उसके नेताओं पर जमकर हमला करने का अवसर दिया। पेरियार द्वारा हिंदी विरोध के पीछे मुख्य कारण था कि वह संस्कृत से सीधे जुड़ी थी। इसलिए उसे पौराणिक मूल्य की संवाहक माना गया। (कु.अ., 22 अगस्त 1937)। हालांकि, जैसा ऊपर बताया गया है; पेरियार ने उसका कोई जातीय अथवा सांस्कृतिक कारण नहीं बताया था। यद्यपि, वह उन दिनों वह सांस्कृतिकरण को प्रश्रय देती थी। पेरियार के लिए हिंदी का प्रश्न चुनौतीपूर्ण था। मुख्यतः इसलिए, कि वे सोचते थे कि हिंदी को थोपना प्रकारातंर में हिंदू राष्ट्रवाद को प्रश्रय दे सकता है।
द्रविड़ राष्ट्र की मांग इसी संदर्भ में उभरी थी। परंतु, जैसा ऊपर कहा गया है; उसके पीछे सांस्कृतिक अथवा जातीय आग्रह कम, आदर्शोन्मुखी चेतना अधिक थी। इसमें एक ऐसा समाज, जिसके बारे में पेरियार ने 1940 के दशक में अपने वक्तव्यों में बार-बार स्पष्ट किया था, कि वह पूरी तरह जाति मुक्त होगा; जिसमें हिंदुवादी आदर्श लोगों की संचेतना और दिलो-दिमाग को नियंत्रित नहीं करेंगे। पुनश्चः, ऐसा समाज, जो समाज समाजवादी एवं सहकारिता के आदर्शों के अनुसार परिचालित होगा।
द्रविड़ राष्ट्र के संदर्भ में पेरियार ने गैर-ब्राह्मणों तथा दलितों से हिंदुत्व से बाहर आने को कहा, उनकी यह मांग भारत की आजादी के बाद भी बनी रही। पेरियार का कहना था कि भारतीय विधिक और संवैधानिक तंत्र दोषपूर्ण सिद्ध होगा। क्योंकि, उसमें जाति-उन्मूलन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यद्यपि, संविधान घोषणा करता है कि अस्पृश्यता को खत्म किया जाएगा; तथापि उनका स्पष्ट मत था कि संविधान असल में मौजूदा जाति-आधारित तंत्र का संरक्षण करता है। मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय, जिसने तत्कालीन सरकार के आरक्षण संबंधी निर्णय को खारिज कर दिया था तथा उच्चतम न्यायालय ने जिसका समर्थन किया था; ने पेरियार को सरकार से यह मांग करने का अवसर दिया था कि वह सकारात्मक कार्यवाही के साथ आगे आए। 1950 के बाद से निरंतर व्यापक विरोध के फलस्वरूप पहला संविधान संशोधन संभव हो पाया था। (अनीमुथू, 2009, 148-9)।
भारत सरकार, विशेष रूप से ब्राह्मण बहुल नौकरशाही की कार्यशैली, संविधान के साथ कैसा वर्ताब करती है; पेरियार की इस पर निरंतर नजर थी। नौकरशाही में व्याप्त कुनबापरस्ती के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शनों की अनवरत शृंखला के बाद द्रविड़यार कड़गम ने एक मुहिम की शुरुआत की थी–1957 में उसने संविधान की उन धाराओं को आग के हवाले करने का निश्चय किया था, जो वर्तमान जाति-व्यवस्था का संरक्षण करती तथा ब्राह्मण नौकरशाही को अजेय बनाती हैं। (वही, 256-157)।
1960 के दशक में भी कड़गम द्वारा जाति, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का विरोध जारी रहा। यह तब था, जब तमिलनाडु में कड़गम, कांग्रेस के साथ सरकार में सहयोगी बनी थी। (ऊपर देखें)।
पेरियार की अंतिम और औचित्यपूर्ण लड़ाई गैर-ब्राह्मणों एवं दलितों के आगमिक मंदिर का पुजारी बनने के अधिकार को लेकर थी; परंपरागत रूप से ब्राह्मण ही उसके शीर्ष पुजारी बनते आए थे। 1970 में, जब तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सरकार थी; प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने हिंदू धार्मिक और धमार्थ बंदोबस्त अधिनियम– तमिलनाडु, 1971 का अधिनियम-2, में संशोधन करते हुए, 10000 से अधिक मंदिरों में अर्चकों (पुजारियों) की वंशानुगत नियुक्ति के नियम को समाप्त कर दिया था। फलस्वरूप, सभी जातियों के पात्र व्यक्तियों को पुजारी बनने का रास्ता साफ हुआ था। पेरियार की दृष्टि में ऐसे कानून को तत्क्षण अमल में लाने की आवश्यकता थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन यह समझाने में लगा दिया था कि धार्मिक पूजा-पाठ आदि पर ब्राह्मणों का समय-सिद्ध अधिकार उन्हें विशिष्ट पहचान और अधिकार उपलब्ध कराता है। तमिलनाडु सरकार के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की बेंच ने माना कि पुजारी की नियुक्ति का मामला धर्मनिरपेक्ष अनिवार्यताओं से बाहर आता है। इस प्रक्रिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। इसके बावजूद बेंच ने भविष्य में सभी जातियों से पुजारियों की नियुक्ति के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। न्यायालय का मत था कि यदि इस तरह की नियुक्तियां, यदि वे मान ली जाती हैं तो आगमिक आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन होंगी; जो प्रस्तावित पुजारी के लिए अनिवार्य आचरण के संबंध में बहुत कठोर हैं। दूसरे, यदि इस प्रकार के आदेशों की जानबूझकर उपेक्षा की गई, तो वह हिंदू उपासक के धार्मिक विश्वास में सीधा हस्तक्षेप होगा। बेंच का मानना था कि हिंदू उपासक के लिए मूर्ति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण और पवित्र वस्तु है। धर्मनिष्ट हिंदू सिवाय पारंपरिक पुजारी के किसी और को मूर्ति छूने की अनुमति नहीं दे सकता। इस बारे में उसकी आस्था एकदम स्पष्ट है। पुनश्चः–
‘‘कोई राज्यादेश किसी आगम द्वारा अनाधिकृत आर्चक के स्पर्श से अपवित्र या अशुद्ध माना जाता है, तो वह धार्मिक आस्था और हिंदू उपासक के पूजा-विधान में बड़ा हस्तेक्षप होगा। अतः प्रथम दृष्टया यह संशोधन संविधान की धारा 25(1) के अंतर्गत अमान्य है।’’ (ए.आई.आर. 1972: 1592-93)।
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह के विचारों ने ही पेरियार को नाराज किया था। साथ ही उनके इस विचार की पुष्टि भी की कि भारतीय राष्ट्र को उन लोगों के हितों की रक्षा में दिलचस्पी नहीं थी, जिन्हें हिंदू धर्म में सामान्य मनुष्य की गरिमा से सिर्फ इसलिए वंचित रखा गया था, क्योंकि वे ब्राह्मण नहीं थे। ऐसे सांस्थानिक तर्कों द्वारा घेरा जाना पेरियार के लिए विशेष कष्टप्रद थे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संकेत मिलता था कि आगे हर राह अवरुद्ध है। अपने फैसले के अंत विद्वान जजों ने आखिर में पांडुरंग वामन काणे का ब्रह्मपुराण से संदर्भ उद्धृत किया था, जिसमें कहा गया है कि ‘जब कोई मूर्ति….किसी जानवर जैसे कि गधा द्वारा स्पर्श की जाती है….अथवा बाहरी जातियों (गैर-ब्राह्मणों) द्वारा अशुद्ध कर दी जाती है; ईश्वर उसमें रहना छोड़ देता है।’ दूसरे, बेंच ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि वे संविधान की धारा 25 और 26 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध हैं–
‘‘इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त सुरक्षा किसी सिद्धांत अथवा आस्था, विश्वास तक सीमित नहीं हैं। इनमें वे कर्तव्य भी आते हैं, जो धार्मिक कार्यकलाप या उनका हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए, इनमें परंपराओं तथा उनके अनुपालन, उत्सवों, पूजा-पद्धतियों, जो धर्म का आंतरिक हिस्सा हैं; की गारंटी भी शामिल है….। ऐसे सभी मसले, जो धर्म अथवा धार्मिक प्रक्रिया का आवश्यक अंग हैं; अदालतों द्वारा उनके फैसले– धर्म-विशेष की सैद्धांतिकी और उन सभी पूजा-पद्धतियों, जिन्हें कोई समुदाय अपने धर्म का अनिवार्य हिस्सा मानता है; के तत्वावधान में किए जाएंगे।’’ (ए.आई.आर., 1972: 1593)।
इन परिस्थितियों में पेरियार ने अलग तमिलनाडु का नारा उछाला, जो जैसा ऊपर बताया गया है; ऐसा राज्य होगा, जिसमें राजनीति और नस्लीय मामलों को न्यूनतम जगह मिलेगी….इसके विपरीत उसमें वर्ण-धर्म के विनाश तथा समानता एवं न्याय की स्थापना के लिए अधिकाधिक संभावनाएं होंगी।
वह 1972 का वर्ष था। एक वर्ष पहले ही पेरियार ने जीवन के 90 वर्ष पूरे किए थे। फिर भी वे संघर्ष के लिए तैयार थे; जैसा कि उन्होंने लिखा भी था– ‘जाति के विरुद्ध लड़ाई आसान नहीं है, न ही यह बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है।’ अपनी उपलब्धियों को लेकर वे बहुत ही विनम्र थे, मगर भविष्य में किए जाने कार्यों को लेकर सचेत। कुल मिलाकर जाति का विनाश ऐसा कार्य है, जिसके लिए परम-मानवीय प्रयासों की आवश्यकता है। जैसा कि अपने जीवन के अंतिम दशक में उन्होंने कई बार दोहराया था कि यह ‘पहाड़ उलटने जैसा है’, आगे लिखा– ‘बालों की लट से!’ उस समय भी पेरियार न तो क्षुब्ध थे; न हताश। जीवन के अंतिम वर्षों में वे खुद को ऐसे वृक्ष के रूप में देख रहे थे, जो अपनी सभी पत्तियों को बिखरा चुका है। उनके पास खोने के लिए कुछ और नहीं था; और इस बीच हर चीज थी, जिसे जाति के विरुद्ध बोलकर, आत्मसम्मान और समधर्म के समर्थन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था।
(अंग्रेजी से अनुवाद- ओमप्रकाश कश्यप, कॉपी संपादन : सिद्धार्थ )
संदर्भ :
पुस्तकें
- वी. अनीमुथू, संपा. ई.वी. रामास्वामी सिथानायकल (पेरियार के विचार), 3 खंडों में, सिंथानायलार पाथीप्पगम, त्रिचनापोली, 1974, (सीमित संस्करण के रूप में 2009 में कई खंडों में पुनर्प्रकाशित)।
- वी. गीता और एस.वी. राजदुरै, संपा. रिवोल्ट : ए रेडीकल वीकली फ्राम कोलोनियल मद्रास, पेरियार द्रवीदार कड़गम पब्लिकेशन, चेन्नई, 2008 (उसके बाद से ‘पेरियार द्रवीदार कड़गम’ बदलकर ‘द्रवीदार विदुथालाई कड़गम’ हो चुका है।)
- वी.एम. सुबगनराजन, संपा. नमक्कू एन इंधा, इझी निलाई? जाति मानादुगल्लीलम जाति ओझिप्पु मानादुगल्लीलम पेरियार (हम अपमानित स्थिति में क्यों हैं? जाति और जाति उन्मूलन सभाओं में पेरियार के भाषण, कायल काविन, चेन्नई 2018)।
अन्य स्रोत
- कुदी अरासु (कु.अ.); विदुथालाई (Vi); रिवोल्ट: आत्मसम्मान आन्दोलन और द्रवीदार कड़गम का प्रकाशन।
- ए.आई.आर.– आल इंडिया रिपोर्टर (डाटाबेस ऑफ जजमेंट्स)
टिप्पणी
क. पेरियार के लेखन संबंधी सभी अनुवाद वी. गीता और एस.वी. राजदुरै द्वारा।
ख. गैर-ब्राह्मण और आत्मसम्मान आन्दोलन, 1926-1938 के विस्तृत इतिहास के लिए देखें : वी. गीता और एस. वी. राजदुरै की पुस्तक– ‘टूवार्ड्स ए नान-ब्राह्मिन मिलेनियम : फ्रॉम ज्योति थास टू पेरियार’, साम्या (1998), 2008।
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया