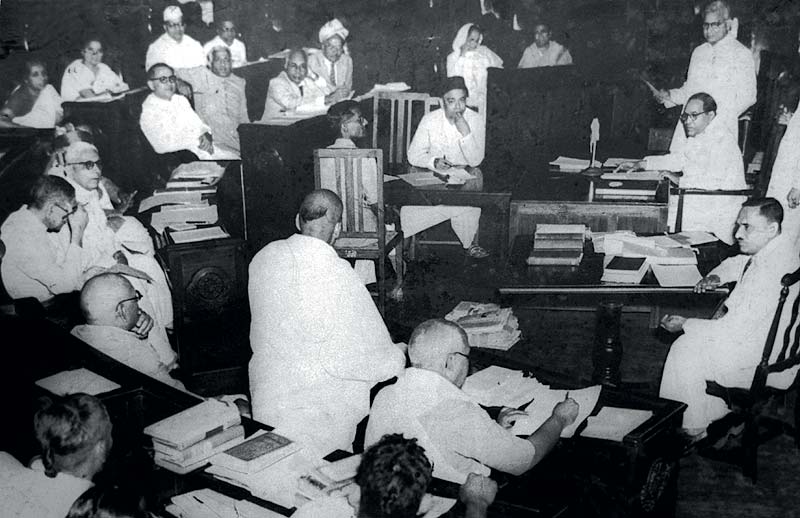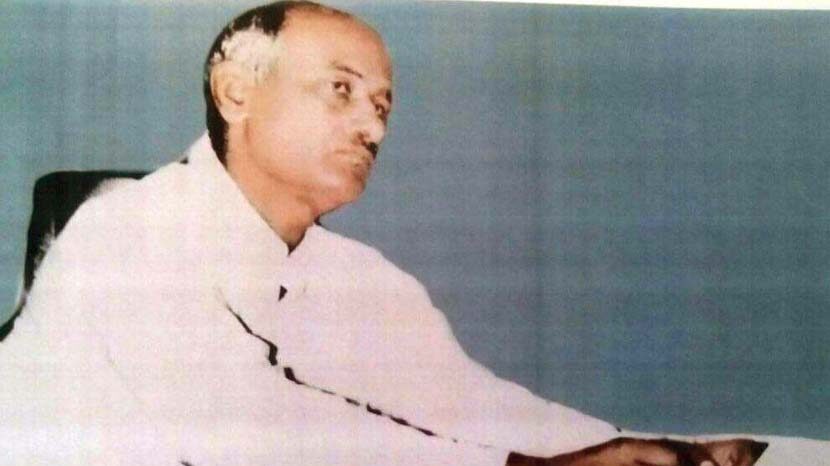ऋग्वेद में इंद्र को दुर्ग-भंजक बताते हुए उसका महिमा-मंडन किया गया है। वहां एकाधिक स्थानों पर आया है कि इंद्र ने शंबर नामक असुर के सौ दुर्गों का नाश किया था (1/130, 2/14)। जब तक ये ग्रंथ केवल “ब्राह्मणों” के घरों और आश्रमों की शोभा बने हुए थे और अशिक्षा के अंधकार में डूबे जन सामान्य के लिए उन्हें पढ़ने, उनपर स्वतंत्रता-पूर्वक चिंतन-मनन करने, यहां तक कि सुनने पर भी प्रतिबंध था, तब तक ब्राह्मण जैसा कहते-थोपते थे, वही उन्हें स्वीकार करना पड़ता था। कई बार उनका मौन भी शक्तिशाली के वर्चस्व को वैध ठहराने का काम करता था। जनता की मौन स्वीकृति के आधार पर ही जाति प्रथा को जगह मिली, जो कालांतर में अपनी विकृतियों के साथ फलते-फूलते हिंदू समाज का कलंक बन चुकी है।
समय के साथ हिंदू धर्म को लगातार मिल रही चुनौतियों के बीच, नए ज्ञान की रोशनी में उनके नए संदर्भ खोजे जाने लगे थे। वर्ष 1855 में “गुलामगिरी” के माध्यम से जोतीराव फुले ने उन मिथकों को निशाना बनाया था, जो ब्राह्मणवाद को संरक्षण प्रदान करते थे। वेदादि ग्रंथों से संदर्भ लेते हुए उन्होंने बताया कि अनार्य संस्कृति न केवल आर्य-संस्कृति से कहीं अधिक समृद्ध, अपितु न्याय और समानता की पोषक-संरक्षक भी थी। ब्राह्मणों ने निहित स्वार्थ के लिए वर्ण-व्यवस्था का सिद्धांत गढ़ा। उसके माध्यम से वे भारत के मूल निवासी अनार्यों को अनेकानेक जातियों में बांटकर स्वयं शासक बन बैठे।
दक्षिण भारत के दार्शनिक-विचारक पेरियार की लड़ाई भी इसी सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के विरुद्ध थी। उनके द्वारा स्थापित “आत्मसम्मान आंदोलन” का उद्देश्य था- दबी-कुचली, शूद्र-अतिशूद्र जातियों को उनके गौरवशाली अतीत से पहचाना कराना। आर्य-श्रेष्ठता के मिथकीय चंगुल से बाहर निकालकर उनमें सम्मानजनक जीवन जीने की ललक पैदा करना। उस आत्मविश्वास को वापस लौटाना जिसे वे शताब्दियों की सांस्कृतिक दासता के कारण गंवा चुकी थीं।
सिंधु सभ्यता के अंत और ब्राह्मण धर्म का उदय
प्रसंगवश बता देना उचित होगा कि सिंधु सभ्यता (3300—1750 ईस्वी पूर्व), वैदिक सभ्यता से काफी पुरानी सभ्यता है।[1] लगभग 1500 ईस्वी पूर्व तक, आर्यों के भारत आने से पहले ही वह सभ्यता लगभग नष्ट हो चुकी थी। वह अपनी समकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक उन्नत और विकासशील सभ्यता थी। खासतौर पर अपनी विशिष्ट नगर-रचना को लेकर। आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया तो उनका सामना सिंधु सभ्यता के ध्वंसाशेषों से हुआ।[2] लगभग नौ लाख वर्ग किलोमीटर में फैली, अपने समय की सर्वोत्कृष्ट सभ्यता के ध्वंसाशेषों को देखकर, कदाचित उनके मन में नागरिक बसावट के प्रति अनजान भय पैठ गया था। इसलिए अपने प्रवास के लिए उन्होंने वन-प्रांतर को वरीयता दी; तथा मन में पैठे भय के कारण प्राकृतिक शक्तियों को पूजना आरंभ कर दिया। यह डर इतना बड़ा था कि सिंधुवासियों के गणित और ज्यामिति संबंधी ज्ञान का उपयोग वे वर्षों-बरस तक यज्ञ-वेदिकाएं बनाने पर खर्च करते रहे। देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय के अनुसार सिंधु सभ्यता के विकास-स्तर को प्राप्त करने में उन्हें लगभग 1000 वर्ष का समय लगा था।[3]

भारतीय भू-भाग में अपने पैर जमाने के लिए आर्यों को यहां के प्राचीन निवासियों से संघर्ष करना पड़ा था। उसमें जीत आर्यों की हुई थी। पराजित अनार्य भारत में यहां-वहां बिखर गए। उनका एक हिस्सा दक्षिण की ओर पलायन कर गया, जिसने वहां द्रविड़ सभ्यता की नींव रखी।[4] हिंदुओं के दोनों प्रमुख महाकाव्यों की रचना, उस राजनीतिक विजय को, सांस्कृतिक विजय का रूप देने के लिए की गई थी। “रामायण” दक्षिण भारत पर आर्य-संस्कृति की विजय की कीर्ति-गाथा है, जबकि “महाभारत” की रचना सिंधु सभ्यता के पराभव के काफी समय बाद पनपे आर्य-अनार्य राज्यों को एकल धर्म-संस्कृति के दायरे में लाने के लिए की गई थी। महाभारत का मूल कथासूत्र भले ही पुराना रहा हो, मगर जिस रूप में वह हमें आज प्राप्त होती है, वह बमुश्किल 2000 वर्ष पुरानी रचना है, जब छोटे राज्य अपनी प्रासंगिकता खो चुके थे और बाहरी ताकतों का जवाब देने के लिए बड़े राज्यों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। बौद्ध धर्म के पराभवकाल में पुष्यमित्र शुंग का भारत ऐसे धर्म के नाम पर एकजुट होना चाहता था जिसकी नींव, राज्यों के बीच स्पर्धा, अविश्वास, धार्मिक संकीर्णता और सामाजिक-सांस्कृतिक असमानता पर टिकी थी।
पेरियार की द्रविड़ अस्मिता
जातिवाद और ब्राह्मण वर्चस्व जैसी चुनौतियां पेरियार के सामने भी थीं। मगर उनकी परिस्थितियां अलग थीं। ब्राह्मणवादी वर्चस्व से बाहर आने के लिए उन्होंने “द्रविड़ अस्मिता” को हथियार बनाया था। अपने उद्देश्य में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। “आत्मसम्मान आंदोलन” न केवल तमिलनाडु, अपितु पूरे दक्षिण भारत में सामाजिक-राजनीतिक क्रांति का संवाहक सिद्ध हुआ। इसका कारण है कि जिस उद्देश्य को लेकर पेरियार ने संघर्ष की शुरुआत की थी, उसके प्रति प्रच्छन्न चेतना द्रविड़ समाज में शताब्दियों पहले से मौजूद थी। अपने संघर्ष, समर्पण और मौलिक तर्कों द्वारा पेरियार ने उसे केवल उभारने का काम किया था। “आत्मसम्मान आंदोलन” की चर्चा करने से पहले तमिल समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर विचार करना समीचीन होगा।
“आत्मसम्मान आन्दोलन” की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
रामायण की भांति ऋग्वेद आदि ग्रंथ भी आर्य-अनार्य द्वंद्व की पुष्टि करते हैं। इस तरह राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पराजयों का कलंक पूरे दक्षिण भारत के माथे पर लगा था। मुट्ठी-भर ब्राह्मण जो स्वयं को आर्यों का उत्तराधिकारी मानते थे, वहां सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक परिक्षेत्र पर छाए हुए थे। उनके पास अकूत सुख-संपदा और विशेषाधिकार थे। तमिलनाडु में ब्राह्मणों की आबादी बामुश्किल तीन प्रतिशत थी। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ये तीन प्रतिशत ब्राह्मण प्रदेश की 70 प्रतिशत सरकारी नौकरियों पर काबिज थे। राज्य के 90 प्रतिशत संसाधनों पर सवर्णों का अधिकार था, जिनकी ब्राह्मणों को मिलाकर कुल संख्या, प्रदेश की कुल आबादी का मात्र 10-12 प्रतिशत थी।

“जस्टिस पार्टी” के नॉन ब्राह्मण मेनिफेस्टो 1916 के अनुसार मैसूर प्रांत में सिविल सेवा की खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में, उससे पिछले 20 वर्षों के दौरान ब्राह्मण 85 प्रतिशत पदों पर अपना कब्ज़ा जमाने में कामयाब रहे थे। उसी अवधि के दौरान मद्रास में, सहायक इंजीनियर की परीक्षाओं में 17 ब्राह्मण, 4 गैर-ब्राह्मण थे। लेखा विभाग की प्रतियोगी परीक्षाओं का भी यही हाल था। मद्रास में ही 140 में से 77 ब्राह्मण तथा 33 गैर-ब्राह्मण हिंदू थे। गैर-ब्राह्मण हिंदुओं में मुस्लिम, ईसाई, सिख, आदि शामिल थे। न्याय सेवाओं का भी यही हाल था। 1913 में मद्रास में 128 जिला मुन्शिफों में से 93 ब्राह्मण और 25 गैर-ब्राह्मण थे, जिनमें मुसलमान, ईसाई, यूरोपीय नागरिक आदि थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा खोले गए स्कूलों की आलोचना करने वाले, उन्हें भारत के ईसाईकरण की साजिश का हिस्सा बताने वाले ब्राह्मण, चार्टर अधिनियम 1833 और 1853 द्वारा सरकारी नियुक्तियों में भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों के बाद, अंग्रेजी स्कूलों में छाने लगे थे। 1917 में मद्रास विश्वविद्यालय के कुल पंजीकृत 650 स्नातकों में से 452 ब्राह्मण, मात्र 12 गैर-ब्राह्मण तथा 74 अन्य समुदायों के थे।
सच यह भी है कि दक्षिण भारत पर आर्यों की सांस्कृतिक विजय को लेकर उनके उत्तराधिकारियों के चाहे जो दावे हों, मगर वहां के समाज का बहुसंख्यक हिस्सा उससे सहमत न था। विपन्नता और जातीय दबावों के बीच भी वह अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं को बचाए हुए था। इसके प्रमाण तमिल साहित्य और संस्कृति में खोजे जा सकते हैं। तमिल भाषा संस्कृत जितनी ही पुरानी है। दक्षिण में दोनों भाषाओं के बीच करीब-करीब बराबर का लेन-देन रहा है। ए. एल. बाशम के अनुसार तमिल पर संस्कृत का सबसे पुराना प्रभाव संघम् साहित्य (200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक) में देखने को मिलता है। उससे पता चलता है कि 200 ईस्वी पूर्व तक दक्षिण भारत उत्तर भारत के सांस्कृतिक प्रभाव से मुक्त थे। सांस्कृतिक विजय-गाथा के रूप में, महाकाव्यों की पुनर्रचना यानी जिस रूप में वे आज प्राप्त हैं, उसके बाद हुई थी।
“एट्टुथोगई” (संघम् साहित्य के आठ प्रमुख काव्य-ग्रंथ) की भाषा, संस्कृत से उधार लिए गए ढेर सारे शब्दों का स्पष्ट प्रमाण है। तमिलों द्वारा आर्य संस्कृति से मेल-जोल के ये प्राचीनतम स्रोत हैं।’[5] दूसरे शब्दों में रामायण जैसे ग्रंथ भले ही उत्तर की दक्षिण पर सांस्कृतिक-राजनीतिक विजय का बखान करते हों, वहां की भाषा एवं संस्कृति पर ईसा पूर्व 200 वर्ष से पहले तक उत्तर भारतीय संस्कृति का कोई प्रभाव न था। वहां समृद्ध आर्येत्तर संस्कृति फल-फूल रही थी। रामायणादि ग्रंथों की रचना उसी को अपने प्रभाव में लेने की चेष्ठा का परिणाम थी।
तमिल और संस्कृत में लेन–देन
तमिल और संस्कृत के बीच भाषायी लेन-देन का सिलसिला ईसा पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी से आरंभ होता है। उस समय तक बौद्ध और जैन दर्शन दक्षिण में अपने पैर जमाने लगे थे। इसके बावजूद, भाषायी लेन-देन से अलग, तमिल सभ्यता और संस्कृति अपने मूल चरित्र को बचाए हुए थी। सुप्रसिद्ध बंगाली भाषाविद् सुनीति कुमार चटर्जी इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं— “तमिल के संदर्भ में इंडो-आर्यन उत्प्रेरण ठीक वैसा ही था, जैसा कि दूसरी अनार्य भाषा-बोलियों पर। यद्यपि तमिल ने इंडो-आर्यन (संस्कृत एवं प्राकृत) शब्दों को स्वीकार किया था, तथापि तमिल में साहित्य का जैसा विकास हुआ वह उसका अपना, निश्चित रूप से दक्षिणी द्रविड़ियन मूल का था।”[6] चटर्जी के अनुसार वर्तमान तमिलों के पूर्वज उर्वर मस्तिष्क वाले, द्रविड़ भाषा-भाषी लोग थे, जिनकी साहित्य में गहरी रुचि थी।[7] दक्षिण तमिल से कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो ब्राह्मी लिपि के काफी बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। उनकी भाषा को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। चटर्जी के अनुसार उन अभिलेखों में तमिलनाडु में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की पुरालिपियां हैं, जिनमें अंशतः तमिल, अंशतः इंडो-आर्यन (प्राकृत) अथवा मिली-जुली भाषा का इस्तेमाल किया गया है।
यह भी पढ़ें : पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन : द्रविड़ अस्मिता का उद्घोष
तमिल में साहित्य परिषदों का इतिहास भी बहुत पुराना है। उनके लिए संघम् शब्द बौद्ध धर्म के “संघ” से लिया गया है। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि तमिल तक संस्कृत और प्राकृत शब्द पहुंचाने वाले, आर्य साम्राज्यवादी न होकर, जैन और बौद्ध श्रमण थे। उन्होंने वहां समाज के एक हिस्से को प्रभावित भी किया। बावजूद इसके वे दक्षिण भारतीय संस्कृति के मूल चरित्र में आमूल बदलाव करने में असमर्थ रहे। सिवाय वहां के ब्राह्मणों और उच्च जातियों के जिनकी जनसंख्या दस-बारह प्रतिशत है, वे आर्य-विजय के सिद्धांत को शायद ही कभी स्वीकार कर पाए। के.एम. पनिक्कर इसे और भी स्पष्ट कर देते हैं। उनके अनुसार — “तमिलनाडु का इतिहास….उत्तर भारत की घटनाओं से प्रभावित नहीं था। आरंभ से ही उसका इतिहास प्रायद्धिपीय घटनाक्रमों द्वारा नियंत्रित था, और उसपर समुद्री जन-जीवन का प्रभाव था।”[8]
इस तरह आर्यों की द्रविड़ों पर राजनीतिक विजय का सच चाहे जो भी रहा हो, तमिलनाडु सहित समस्त दक्षिण भारत पर, उनकी सांस्कृतिक विजय, वास्तविकता से ज्यादा मिथक है। इसलिए वहां ब्राह्मणवाद के विरोध के स्वर उत्तर भारत के सापेक्ष कहीं अधिक पुराने और प्रखर हैं।
आर्य विरोधी संघम् साहित्य
दक्षिण भारत में “मुरुगन” एक बड़ा देवता है, जो “स्कंद” (कार्तिकेय) के लिए आया है। संघम् साहित्य में भी इस देवता का गुणगान है। “स्कंद” को शिव का पुत्र बताया गया है, जो अनार्य देवता और महादेव हैं। उनकी उपस्थिति सिंधु सभ्यता में भी देखी गई है। “वे कर्म-संस्कृति के संरक्षक और संपूर्ण न्याय-प्रदाता हैं। न्याय से उनका आशय है, प्राणि-मात्र के प्रति प्यार….उनके गुण, उनका रूपाकार, उनका ज्ञान, उनके कर्म यहां तक कि उनके हाथ-पैर आदि सब प्रेम और प्रीति से भरपूर हैं।”[9] तमिलनाडु में सिद्ध परंपरा भी बहुत पुरानी है। इसका उदय बौद्ध धर्म के पराभव के पश्चात हुआ था। कुछ विद्वान उनके इतिहास को ईसा पूर्व छह सौ वर्ष पहले तक ले जाते हैं। शैव परंपरा के प्रति आस्थावान, सिद्ध चरित्र की निर्मलता और मनुष्यता को सर्वोपरि मानते थे। वे पूजा-पाठ, जातिवाद यहां तक कि ब्राह्मणवाद का भी विरोध करते थे। 18 सिद्धों में से एक सिद्ध थे, शिवा वाक्कियार। 10वीं शताब्दी से पहले उनका जन्म हुआ था। शिवा वाक्कियार की एक कविता है—
ओ पुजारी! तब और अब, तुमने मछली नहीं खाई
लेकिन जिस पानी को तुम पीते और नहाते हो,
क्या उसमें मछलियां नहीं थीं?
ओ पुजारी! तब और अब तुमने हरिण नहीं खाया
क्या तुम्हारी छाती पर चमकता जनेऊ हरिणचर्म का नहीं है?[10]
एक और बड़े सिद्ध कवि हैं, नाम है पेतिनत्तार। मूर्तिपूजा पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा है—
मेरा परमात्मा छेनी से तराशा हुआ नहीं है
न उसे इमली से घिस-रगड़कर चमकाया गया है
कांसे की मूर्ति की तरह
मैं इन सबकी पूजा नहीं कर सकता….[11]
संघम युग के एक संत कवि हैं, पेत्रिहारियार। उनका समय 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक है। पेत्रिहारियार अतीतमोह से ग्रस्त कवि हैं। तमिल भूमि का प्राचीन गौरव, जब समाज एक था, जातिगत बंटवारे से दूर सभी लोग मिल-जुलकर रहते थे — उनकी कल्पना में बसता है। उनकी कई कविताएं अतीत-गायन जैसी हैं, जिनमें आमजन की पीड़ा समायी हुई है। इस कारण पेत्रिहारियार तथा उनकी परंपरा के कवियों को “जनकवि” भी कहा गया है। एक कविता में पेत्रिहारियार ने जन्म के आधार पर समाज को बांटने वाले प्रवृत्ति की आलोचना की थी—
जब हम होंगे महान भाईचारे के साथ
जिसे जाति का आतंक मिटा नहीं सकेगा
जो मौजूद था इस समाज में बहुत पहले से
उन दिनों जब सभी मनुष्य एक थे
वे दिन जो अब बीत चुके हैं।[12]
चार्ल्स रीयरसन के अनुसार तमिल लोकचेतना में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब वर्ण-व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार लिया गया हो, उसकी आलोचना न की गई हो। उसमें ब्राह्मणों की सर्वोच्चता और वर्ण-व्यवस्था के प्रति सदैव विद्रोह भाव था। यह विद्रोह-चेतना पुराने गौरव को याद करती हुई, उनके आधार पर स्वतःप्रमाणित थी। उसमें संघम् काल (ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का समय) को आदर्श युग की तरह देखा गया था।”[13] जाहिर है कि ईसा पूर्व दूसरी या तीसरी शताब्दी तक तमिल समाज का वर्ण-व्यवस्था के आधार पर बंटवारा नहीं हो पाया था। इसलिए उत्तर की दक्षिण पर सांस्कृतिक विजय जिसका दावा रामायण और दूसरे संस्कृत ग्रंथ करते हैं, से वहां का समाज पूरी तरह मुक्त था।
“आत्मसम्मान आंदोलन” के माध्यम से पेरियार का उद्देश्य तमिल के प्राचीन गौरव को वापस लाना था। चूंकि सिद्ध कविताएं लोकगीतों तथा दूसरे सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से समाज में पहले से ही चेतना मौजूद थीं, इसलिए पेरियार के आंदोलन का काम लोगों की स्मृति को खंगालकर उस परंपरा से जोड़ना भर था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मकसद में वे कामयाब भी हुए थे।
(संपादन: गोल्डी/नवल)
[1] (जोनाथन एम. केनोयर एंड रिचर्ड्स एच. मीडो : दि रावी फेस : ए न्यू कल्चरल मेनिफेस्टशन एट हड़प्पा, साउथ एशियन आर्कोलॉजी-1997, खंड-1)
[2] जोनाथन एम. केनोयर, कल्चर्स एंड सोसाइटीज ऑफ़ दि इंडस ट्रेडिशन, https://www.harappa.com/content/cultures-and-societies-indus-tradition)
[3] (देवीप्रसाद चटृोपाध्याय, हिस्ट्री आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी इन एन्शीएंट इंडिया, 1986, फिरमा केएलएम प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, पृष्ठ 109)
[4] (राधाकुमुद मुखर्जी, हिंदू सभ्यता, हिंदी अनु. वासुदेवशरण अग्रवाल, राजकमल प्रकाशन, 1975, पृष्ठ 57)
[5] ए.एल. बाशम, सम रिफ्लेक्शंस आन द्रवड़ियंस एंड आर्यंस, बुलेटिन आफ ट्रेडीशनल कल्चर्स, यूनीवर्सिटी आफ मद्रास, मद्रास, 1963 पृष्ठ-226, रीजनलिज्म एंड रिलीजन: तमिल रेनेसांस एंड पोपुलर हिंदुइज्म, दि क्रिश्चन इंस्टीट्यूट फार दि स्टडी आफ रिलीजंस एंड सोसाइटीज, बंगलौर, में चार्ल्स रीयरसन द्वारा उद्धृत, पृष्ठ 32।
[6] सुनीति कुमार चटर्जी, लेंग्वेजिज एंड लिटरेचर आफ माडर्न इंडिया, बंगाल पब्लिशर्स, 1963, पृष्ठ 306 लिंक : http://dspace।wbpublibnet।gov।in:8080/xmlui/bitstream/handle/10689/12259/Chapter2_253-332p।pdf?sequence=9&isAllowed=y
[7] उपर्युक्त।
[8] के. एम. पन्निकर, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियाज हिस्ट्री, भारतीय विद्याभवन, मुंबई, पृष्ठ-27, ‘रीजनलिज्म एंड रिलीजन’ में चार्ल्स रीयरसन, पृष्ठ 26 द्वारा उद्धृत।
[9] बेशाम, दि वंडर देट वाज इंडिया, रूपा एंड कंपनी, 15 बंकिम चटर्जी मार्ग, कोलकाता, पृष्ठ 336।
[10] ‘रीजनलिज्म एंड रिलीजन’ में चार्ल्स रीयरसन, द्वारा उद्धृत, पृष्ठ 42
[11] उपर्युक्त
[12] उपर्युक्त, पृष्ठ-52
[13] उपर्युक्त, पृष्ठ-52