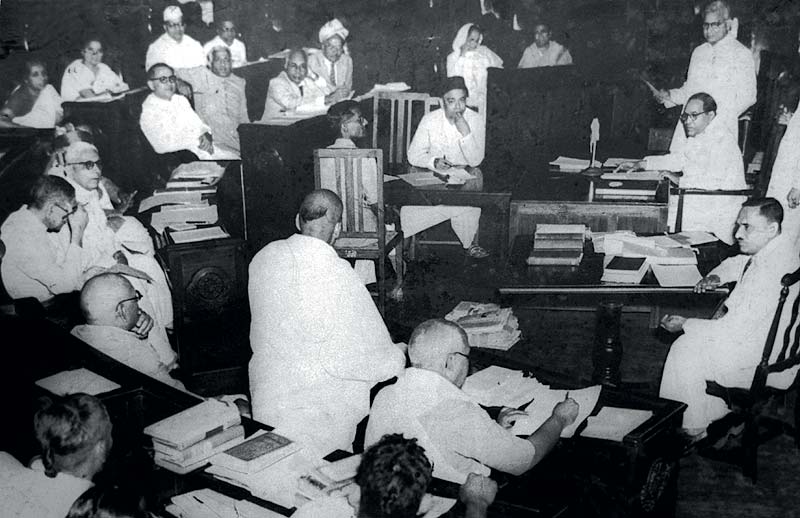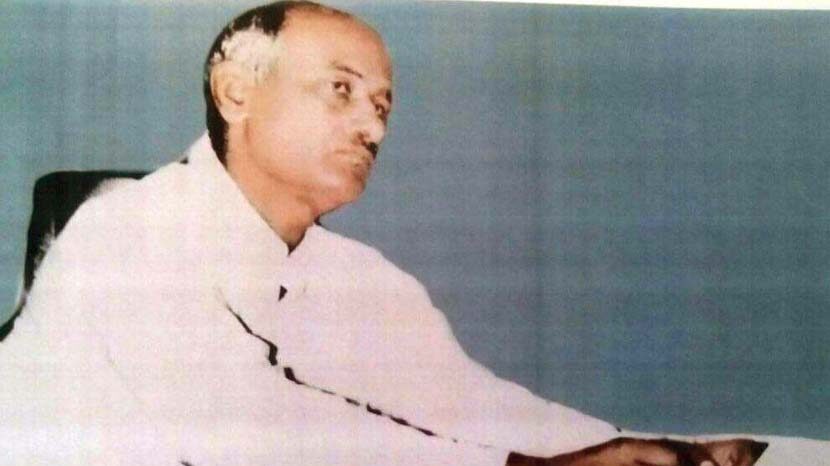मानव सभ्यता सदियों से जंगलों पर निर्भर रही है। बीसवीं सदी के प्रारंभ में सिन्धु घाटी में खुदाई में मिली सीलों और रंगे हुए मिट्टी के पात्रों में पीपल और बबूल के पेड़ों के प्रतीकात्मक चित्रण से यह संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता (5000-4000 ई.पू.) में भी इमारतों के लिए लकड़ियां आदि तमाम वनोपजों का प्रयोग होता था। गुप्तकाल (200-600 ई.) का वनों से संबंधित विवरण, मौर्य काल से मेल खाता है। वहीं मुग़लकाल (1526-1707) में इमारती लकड़ी और खेती के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों का सफाया किया गया। ब्रिटिश शासन आने के बाद, सरकार और आदिवासियों में सीधा टकराव शुरू हुआ और वन इसका एक प्रमुख कारण थे।
भारत की वन सम्पदा
अठारहवीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि भारत के वनों में अकूत संपदा छिपी हुई है और इसलिए उन्होंने वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी। वे या तो सीधे अथवा ज़मींदारों और साहूकारों के ज़रिए जंगलों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। इसका एक कारण यह था कि उन्हें न केवल भारत वरन् इंग्लैंड में भी मकान बनाने और अन्य कामों के लिए इमारती लकड़ी की ज़रुरत थी। उन्होंने ज़मींदारी प्रथा को मज़बूत किया और उसके ढांचे में इस तरह के परिवर्तन किये ताकि वे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर वन क्षेत्रों पर कब्ज़ा जमा सकें। जाहिर तौर पर इसका खामियाजा स्थानीय रहवासियों को भुगतना पड़ा। अंग्रेजों ने ऐसे इलाकों में घुसपैठ करनी शुरू कर दी जो आदिवासियों के वास स्थल थे और इस कारण उनके बीच टकराव शुरू हुआ।
भारत में आदिवासी विद्रोहों के पहले 100 सालों (1760 के दशक से लेकर 1860 के दशक तक) में वन कानून नहीं थे और इस दौरान जंगलों से इमारती लकड़ी और अन्य संसाधनों का अनियंत्रित दोहन हुआ। भारत में रेल सेवा शुरू करने का निर्णय 1832 में लिया गया और इसके लिए मद्रास को चुना गया। रेलों की आवाजाही के लिए जो पटरियां बिछाई जानी थीं उनके स्लीपर इमारती लकड़ी से बनने थे। इसके अलावा, इंजनों और डिब्बों के निर्माण में भी लकड़ी का इस्तेमाल होना था। सन् 1837 में भारत की पहली रेल सेवा – जिसे रेड हिल रेलवे का नाम दिया गया – शुरू हुई। यह एक मालगाड़ी थी, जिसे भाप का रोटरी इंजन खींचता था. यह गाड़ी मद्रास में रेड हिल्स और चिंताद्रिपेट ब्रिज के बीच चलती थी।
सन् 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता से दिल्ली तक रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया, परन्तु यह योजना अमल में नहीं लाई जा सकी। देश की पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच चली और बाद में, कलकत्ता और मद्रास में भी रेलगाड़ियां चलने लगीं। रेलवे के निर्माण के इस दौर में, इमारती लकड़ी की मांग बहुत बढ़ गई। यही नहीं, भारत की इमारती लकड़ी पानी के जहाजों के निर्माण के लिए भी मुफीद थी। भारतीय इमारती लकड़ी से बने मज़बूत जहाजों की मदद से ही इंग्लैंड, नेपोलियन के साथ अपने युद्ध (1803-15) में विजय प्राप्त कर सका।
शुरुआत में अंग्रेज़ इमारती लकड़ी की अपनी ज़रुरत बर्मा के जंगलों से पूरी करते थे। सन् 1826 में वे तेनास्सेरिम पर कब्ज़े के बाद से मौल्में में इमारती लकड़ी का व्यापार करने लगे। बाद में, इमारती लकड़ी के लालच में ही उन्होंने पेगू प्रान्त पर कब्ज़ा किया। परन्तु समय के साथ, उन्होंने भारत के जंगलों का दोहन शुरू कर दिया।
भारत में वन कानूनों का उद्भव और विकास
सन् 1850 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों ने तेजी से भारत के उन वन क्षेत्रों में घुसपैठ करनी शुरू कर दी, जहां आदिवासी रहते थे। रेलवे के विस्तार के लिए इमारती लकड़ी की ज़रूरत बढ़ती जा रही थी। सन् 1855 के संथाल विद्रोह के मद्देनजर, 1856 में गवर्नर जनरल लार्ड डलहौज़ी ने एक स्थाई वन नीति बनाने पर जोर दिया ताकि इमारती लकड़ी के लिए वनों का दोहन करने में आ रही दिक्कतें दूर हो सकें। सन् 1857 के गदर से उपजी अस्थिरता पर काबू पाने के बाद, 1860 में अंग्रेजों के आदिवासियों द्वारा स्थानान्तरी कृषि किये जाने को प्रतिबंधित कर दिया और 1864 में इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की।
सन् 1855 में भारत के पहले वन कानून – इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1855 – के जरिए अंग्रेजों ने देश के संपूर्ण वन क्षेत्र पर अपने अधिपत्य की घोषणा कर दी। सन् 1876 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और नये संशोधनों के साथ फॉरेस्ट एक्ट, 1878 लागू किया गया। इसके अंतर्गत, वनों के सामुदायिक उपयोग की सदियों पुरानी परिपाटी पर कई तरह की रोकें लगा दी गयीं और सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह सार्वजनिक उपयोग के लिए वनों का अधिग्रहण कर सकती है। इस अधिनियम के ज़रिए एक ओर वनों पर राज्य का लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया तो दूसरी ओर यह संदेश दिया गया कि ग्रामीणों द्वारा वनोपज का उपयोग उनका ‘अधिकार’ नहीं, बल्कि एक ‘सुविधा’ है जिसे ब्रिटिश सरकार कभी भी वापस ले सकती है।
वहीं सन् 1894 में अपनी वन नीति के आधार पर अंग्रेजों ने वनों को चार श्रेणियों में विभाजित किया : अ) वे वन, जिनका आवश्यक रूप से संरक्षण किया जाना है। ब) वे वन, जिनका इमारती लकड़ी के लिए व्यावसायिक दोहन किया जा सकता है। स) लघु वन और ड) चारागाह। सन् 1878 के अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करते हुए, इस नीति के अंतर्गत कुछ सुरक्षा उपायों के साथ वन भूमि पर खेती की इज़ाज़त दी जा सकती थी। इस नीति का यह प्रावधान वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और अन्य देशज व्यक्तियों के लिए राहत का एकमात्र सबब था कि आरक्षित वनों के बाहरी क्षेत्र का ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु, कुल मिलाकर, इस नीति का सार यही था कि राज्य के हितों को जनता के हितों पर प्राथमिकता मिलेगी।
सन् 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सन 1878 में वनों के दोहन के लिए बनाई गई नीति के अनुरूप था। इसका लक्ष्य अंग्रेजों की इमारती लकड़ी की ज़रुरत को पूरा करना था और इसमें वनों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं थे। इसके अंतर्गत, वनों को राज्य की संपत्ति घोषित कर, इमारती लकड़ी के दोहन का रास्ता साफ़ कर दिया गया और पारंपरिक वनाधिकारों और वन प्रबंधन प्रणालियों को दरकिनार कर दिया गया। इस अधिनियम में वनों की कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई थी। वनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था – आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन। आमजनों का आरक्षित वनों में प्रवेश गैर-क़ानूनी घोषित कर दिया गया और स्थानान्तरी कृषि पर और कड़े प्रतिबन्ध लगा दिए गए। हां, इसमें वनों को अनारक्षित करने का प्रावधान ज़रूर था।
ब्रिटिश भारत में आदिवासी और देशज लोगों के विद्रोह
वन नीति और वनों का प्रबंधन, लम्बे समय से बहस, विवाद और टकराव का विषय रहे हैं. अंग्रेजों द्वारा 19वीं सदी में वन विभाग की स्थापना करने और वनों से सम्बंधित कानून बनाने के समय से ही दो महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज़ किया गया. पहला, आदिवासियों और अन्य देशज समुदायों द्वारा वनों के संरक्षण और उनके धारणीय उपयोग के लिए सदियों पुरानी सुस्थापित पारंपरिक प्रणालियाँ और वनों की पर्यावर्णीय, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका।
वन विभाग की स्थापना से पहले, अर्थात 1864 से पूर्व, जो प्रमुख विद्रोह हुए उन्हें केवल किसानों का अंग्रेजों या ज़मींदारों या साहूकारों के विरुद्ध करों से जुड़े मुद्दों को लेकर विद्रोह नहीं कहा जा सकता। उन्हें हमें बाहरी शक्तियों द्वारा आदिवासियों के वासस्थलों, जो मुख्यतः जंगल और पहाड़ थे, में जबरदस्ती घुसने के प्रयासों के संदर्भ में समझना होगा। इन विद्रोहों और आंदोलनों के इतिहास और पृष्ठभूमि के गहराई से अध्ययन से हमें यह पता लगेगा कि सिर्फ भूमि और जंगलों के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को नज़रअंदाज़ करते हुए लोगों को इन संसाधनों के स्वामित्व से वंचित करना इनका कारण नहीं थे। इनके पीछे था वह अघोषित सांस्कृतिक युद्ध जिसमें एक ओर थे आदिवासी तो दूसरी ओर गैर-आदिवासी निहित स्वार्थी तत्त्व, जिन्हें सरकार का समर्थन और सहयोग हासिल था.

इन विद्रोहों में प्रमुख थे, तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह (1770-85), हल्बा डोंगर (हल्बा), बस्तर (1774-79), महादेव कोली, महाराष्ट्र (1784-85), तमर, छोटानागपुर (1781; 1894-95), पंचेट एस्टेट सेल (1798), कुरुचि, वायनाड (1812), सिंघ्पो, आसाम (1825; 28; 43; 47), कोल विद्रोह (हो और मुंडा सहित) (1832), खोंड, ओडिशा (1850), संथाल, छोटानागपुर (1855), सोनाखान, छत्तीसगढ़ (1856-57), भील, गुजरात (1857-58), अंडमानीज़, अंडमान (1859), लुशाई, त्रिपुरा (1860), सिंतेंग, जैंतिया हिल्स (1860-62), जुआंग, ओडिशा (1861) और कोय, आंध्रप्रदेश (1862)।
चार मुर्मू भाईयों, सिदो, कान्हु, चंद और भैरव के नेतृत्व में हूल विद्रोह पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुआ था। यद्यपि ऐसे कहा जाता है कि इस विद्रोह का कारण महाजनों और ज़मींदारों की ज्यादतियां थीं, परन्तु शायद आदिवासियों को यह भी महसूस हो रहा होगा कि उनकी ज़मीनों और जंगलों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। सन् 1857 का सोनाखान विद्रोह, इसी वर्ष हुए एक और बहुचर्चित विद्रोह से कुछ समय पहले हुआ था। इसका नेतृत्व आदिवासी राजा नारायण सिंह ने किया था और इस विद्रोह के मुद्दे भी सन् 1855 के संथाल विद्रोह से मिलते-जुलते थे। सोनाखान एक वनीय इलाका है और इसके पास बरनावापारा में घने जंगल हैं। सन् 1852 में बम्बई और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले कोल और अन्य वन-आधारित समुदायों में बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने को लेकर भारी गुस्सा था, परन्तु वह विद्रोह में नहीं बदल सका।
सन् 1864 के बाद से, ब्रिटिश भारत में केन्द्रीयकृत राजनैतिक-प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो गई और इसके साथ ही, वनों और वनवासियों के बीच विभाजक रेखा खींच दी गई। औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर अपने स्वामित्व को क़ानूनी जामा पहना दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि वनों में रहने वाले समुदाय गैरकानूनी कब्जाधारी हैं और उन्होंने सरकार की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। अंग्रेज़ अधिकारियों. ज़मींदारों, जागीरदारों आदि को छोड़ कर अन्यों के शिकार करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।
इस दौर में अनेक आदिवासी विद्रोह हुए। जब भी आदिवासियों के जीवन में बेजा हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, जब भी उन्हें उनकी भूमि या जंगलों से बेदखल करने के प्रयास हुए, जब भी उनकी पारंपरिक संस्कृति, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, नागरिक अधिकारों या न्याय व्यवस्था का उल्लंघन या तिरस्कार किया गया, उन्होंने इसका तीव्र, त्वरित और आक्रामक प्रतिरोध किया। इस दौर में हुए देशज लोगों के विद्रोहों में शामिल थे धनबाद में संथालों का विद्रोह (1869-70), उत्तरपूर्व में नागाओं का (1879), तम्मनडोरा के नेतृत्व में ओडिशा के मलकानगिरी में कोयायों का (1880), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनेलियों का (1883), छोटानागपुर में मुंडाओं का (1889), लुशाईयों का (1892), बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं का (1895), बस्तर के आदिवासियों का (भूमकाल विद्रोह और गुंडा धुर के नेतृत्व में एक अन्य विद्रोह, 1910-11), गोविन्द गुरूके नेतृत्व में संप सभा और गुजरात व राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ियों में भीलों का (1913-16), मणिपुर में कुकियों का (1917-19), रम्पा में कोयायों का (1922), उत्तरपूर्व में नागाओं का (1932), तेलंगाना के आदिलाबाद में गोंड और कोलम जनजातियों का (1941) और लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में कोरापुट, ओडिशा में आदिवासियों का विद्रोह (1942).
वन कानून और जन प्रतिरोध
देश के स्वाधीन होने के बाद, सन् 1952 में, भारत सरकार ने अपनी वन नीति बनाई जिसके अंतर्गत वनों को राष्ट्रीय सम्पदा माना गया और ‘राष्ट्रहित’ को सामुदायिक हितों पर प्राथमिकता दी गई। यह साफ़ कर दिया गया कि स्थानीय प्राथमिकताएं व हित और स्थानीय समुदायों के दावे, व्यापक राष्ट्रीय हितों के अधीन होंगे। सन् 1952 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत चिन्हित वन क्षेत्रों को केवल वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित कर दिया गया और उनमें मनुष्यों के रहवास और प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। सभी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसी अधिनियम के प्रावधानों से शासित होते हैं।
सन् 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह अनुशंसा की कि “औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए लकड़ी का उत्पादन वनों का मूल प्रयोजन होना चाहिए” और व्यक्तियों व समुदायों की आवश्यकताएं, औद्योगिक आवश्यकताओं के अधीन होनी चाहिए। उसी वर्ष, संविधान संशोधन (42वां संशोधन) के जरिए वन को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया और इस प्रकार, वनों के प्रबंधन में केंद्र सरकार की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया गया।
सन् 1980 में वनों की कटाई पर रोक लगाने और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसके लिए, अधिनियम के अंतर्गत, निम्न उपाय किए गए (अ) वनों के गैर-वानिकी उपयोग पर प्रतिबन्ध (ब) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत जिन वनों को आरक्षित घोषित किया गया है उन्हें अनारक्षित करने पर रोक (स) वन भूमि को व्यक्तियों या गैर-सरकारी संस्थाओं, निगमों आदि को लीज पर दिए जाने पर रोक और (ड) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने पर प्रतिबन्धञ मूलतः यह अधिनियम वन भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय लेने के अधिकार को राज्य सरकारों से वापस लेकर, केंद्र के हाथों में सौंपता है।
सन् 1947 से लेकर 1986 तक, केंद्र सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश का तेजी से औद्योगिक विकास हुआ, विशेषकर खनन के क्षेत्र में। औद्योगिक और खनन परियोजनों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों को साफ़ किया गया। इसके चार चरण थे: सिलेक्टिव फेल्लिंग (1947-60) क्लियर फेल्लिंग एंड मोनोकल्चर प्लांटेशन्स (1960-75), फार्म फॉरेस्ट्री (1975-85) और इम्पोर्ट एंड कैप्टिव प्लांटेशन (1985 के बाद से)। परन्तु वनों को राज्य की संपत्ति मानने की नीति जारी रही और आदिवासियों को वन और वन भूमि पर उनका अधिकार वापस नहीं दिया गया। इस कारण, आदिवासी इलाकों में वन से जुड़े मसलों पर कई प्रजातान्त्रिक आन्दोलन और संघर्ष हुए। इनके पीछे जो मुद्दे थे वे थे : अ) बाहरी लोगों द्वारा शोषण, ब) आर्थिक वंचना, स) राजनैतिक भेदभाव और ड) सामाजिक-सांस्कृतिक स्वायत्तता।

इन संघर्षों के चलते, सन् 1988 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, वह स्वाधीनता के पश्चात 1952 में बनाई गई नीति से कई मामलों में बहुत भिन्न थी – विशेषकर वन प्रबंधन के सन्दर्भ में। चूँकि वह केवल एक नीति थी इसलिए कानून की तरह उसे लागू करना आवश्यक नहीं था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 ने विशाल उद्योगों के विरुद्ध चल रहे जन आंदोलनों में आशा की एक किरण जगाई, परन्तु यह आशा जल्दी ही समाप्त हो गई। यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा के लिए क़ानूनी ढ़ांचे के निर्माण की मांग और उसके लिए चल रहे संघर्षों के मद्देनज़र बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत किसी भी औद्योगिक परियोजना को लागू करने से पहले उसके पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक-आर्थिक लाभ-हानि का आंकलन करना और जन सुनवाई आयोजित करना आवश्यक बना दिया गया। पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 के अंतर्गत, औद्योगिक परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए ग्राम सभा से चर्चा करना और उसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक बना दिया गया है। परन्तु इन सभी प्रावधानों का कुछ ही समय तक ठीक से पालन हुआ। पिछले एक दशक के दौरान, जन सुनवाईंयां महज औपचारिकता भर रह गईं हैं जिनकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार रहती है। जिन मामलों में स्थानीय रहवासी इस आशय के पर्याप्त प्रमाण जुटा भी लेते हैं कि वे वनों पर निर्भर हैं और वनों को काटने से क्षेत्र के पर्यावरण को हानि होगी, तब भी उनकी आपत्तियों और दावों को दरकिनार कर दिया जाता है। उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली जातीं हैं और उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है। पेसा और वन अधिकार अधिनियम के बावजूद पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं।
आदिवासी आज भी अपने उन नैसर्गिक अधिकारों को पाने के लिए संघर्षरत हैं, जो उनसे छीन लिए गए हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के पारित होने के बाद ऐसी आशा जगी थी कि सदियों से आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर कुछ लगाम लगेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिकार देने में कई विभागों और मंत्रालयों और अनेक कानूनों की भूमिका रहती है। इस अधिनियम में वन अधिकारों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: 1) व्यक्तिगत भू अधिकार व 2) सामुदायिक भू अधिकार – अ) आदिवासियों के लिए व ब) अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए। परन्तु ये अधिकार पाने की राह में कई विभाग और कानून रोड़ा बनते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत, किसी भी विकास परियोजना या औद्योगिक गतिविधि के लिए किसी भी बाह्य एजेंसी के लिए ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति लेना ज़रूरी है।
विकास, औद्योगिक और खनन परियोजनाएं, पारंपरिक रूप से वनों पर निर्भर समुदायों के जीवन और जीवनयापन से सम्बंधित कई चुनौतियां उपस्थित करतीं हैं। हाल में, केंद्र सरकार ने चार राज्यों में स्थित 41 कोयला ब्लाकों की नीलामी करने की घोषणा की है। इनमें से दस ब्लाक मध्यप्रदेश में हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखण्ड में नौ-नौ ब्लाक हैं तथा तीन ब्लाक महाराष्ट्र में हैं। इनमें से कई ब्लाक ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ आदिवासी व अन्य देशज समुदाय निवासरत हैं और वहां के वनों पर निर्भर हैं। उनका पुनर्वास या तो संभव ही नहीं है या उसके लिए कोई योजना नहीं है। जाहिर है, यह निर्णय उनके जीवन के लिए खतरनाक है।
कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि वन अधिकारों के खतरे में पड़ने का मूल कारण यह है कि न तो औपनिवेशिक काल में और ना ही स्वाधीन भारत में, वनवासियों के पारंपरिक वासस्थलों और वनों पर उनकी निर्भरता को मान्यता नहीं दी गई. इसके कारण, आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के साथ सदियों से अन्याय होता चला आ रहा है। और यह तब जब कि वे वनों के पारिस्थितिकी तंत्र का अविभाज्य हिस्सा हैं और वनों के बचे रहने में उनकी अनिवार्य भूमिका है।
(अनुवाद: अमरीश हरदेनिया, संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया