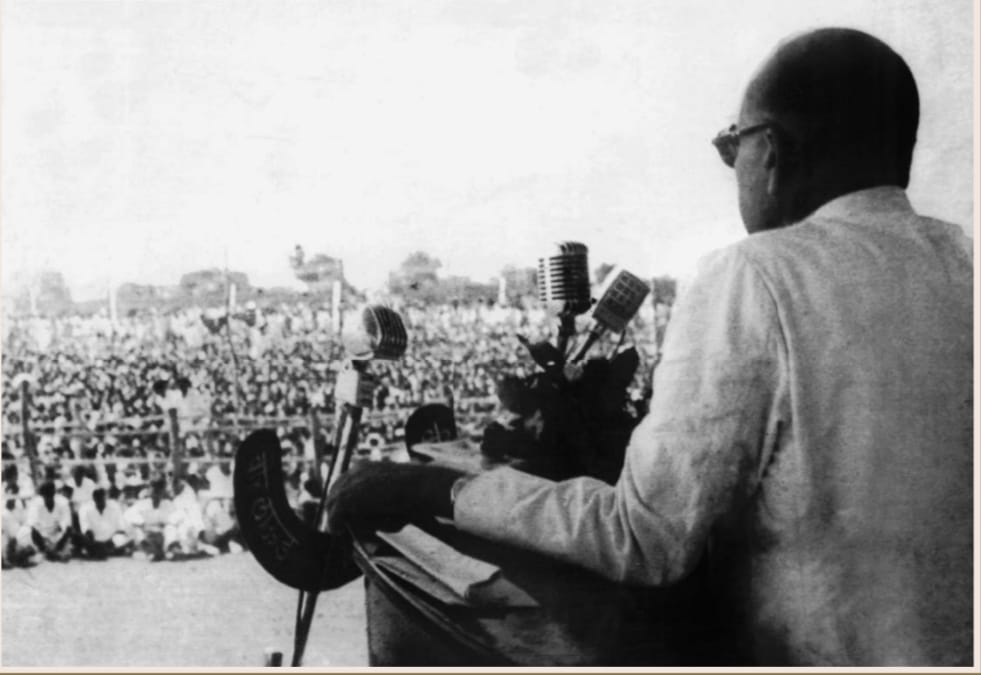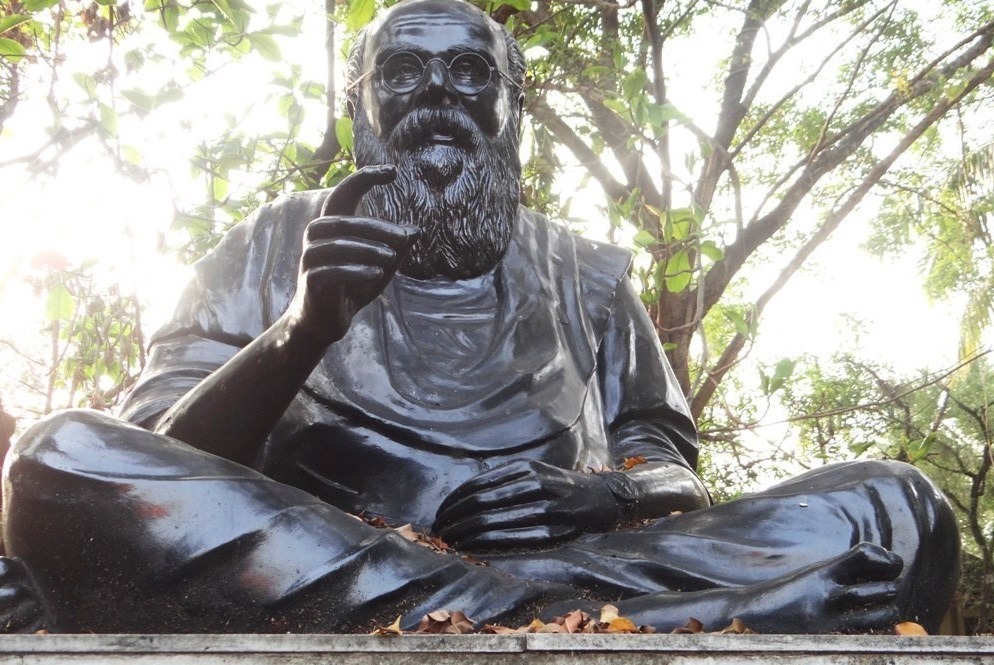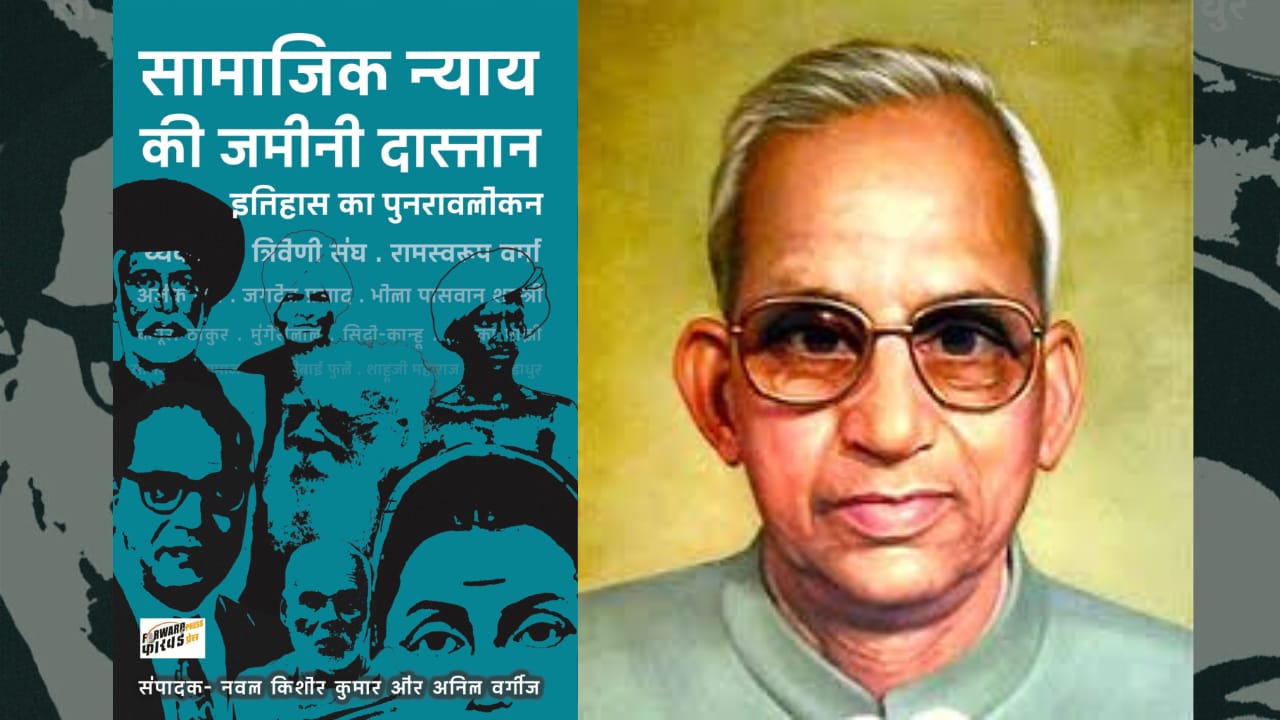असुर भारत का एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है। असुर जनसंख्या का घनत्व मुख्यतः झारखण्ड, मध्य प्रदेश और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल, ओडि़शा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है। झारखंड में असुर मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार जिलों में निवास करते हैं। ये वहीं असुर आदिम आदिवासी समुदाय है जिसने दुनिया को लोहा गलाने का ज्ञान दिया। इसी ज्ञान से कालांतर में स्टील बना और इंसानी समाज ने विकास के नए युग में छलांग लगाई। असुर मूर्तिपूजा नहीं करते हैं। इनका जीवन-दर्शन प्रकृति आधारित होता है। असुर जनजाति के तीन उपवर्ग हैं- बीर असुर, विरजिया असुर एवं अगरिया असुर।

बीर असुर
सामान्य तौर पर बीर असुरों को असुर जनजाति कहा जाता है। लोग सिर्फ इसी समुदाय को ही असुर जनजाति समझते हैं, जबकि बीर असुर के अलावा विरजिया और अगरिया असुर भी असुर जनजाति से हैं। बीर शब्द असुरी और मुंडारी भाषा में ‘जंगल’ से संबंधित है, जिसका अर्थ है ‘शक्तिशाली जंगल वासी’। बीर असुर में 12 गोत्र होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षी एवं अनाज के नाम पर है। जैसे -’’‘अइंद’ (मछली), ‘टोप्पो’ (चिडिय़ा), ‘दारोठे’ (मेढक का डिंभकीट), ‘खुसार’ (उल्लू), ‘केरकिटिया’ (केरकिटिया), ‘महतो रोठे’ (दादुर-बड़ा मेढ़क), ‘सिन्दुरिया रोठे’ (जमीन पर रहने वाली मेढ़क जिसके पीठ पर लकीर होते हैं) ‘छोटे अइंद’ (छोटी मछली), ‘छोटे टोप्पो’ (छोटी चिडि़या), ‘छोटे केरकिटिया’ (एक प्रकार का चिडिया), ‘कोयबरवा’ (जंगली जानवर जिसके मुख पर काला धाग होता है) होते हैं। बीर असुर विजातीय विवाह करते हैं। जिस वस्तु या प्राणी विशेष से गोत्र के नाम दिए जाते हैं, उनसे वह समूह दूरी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका उल्लंघन किये जाने पर वे दुर्भाग्यशाली हो जायेंगे। इस समुदाय में कुल/गोत्र के बाद परिवार सबसे महत्वपूर्ण सामजिक इकाई है।”[1] बीर उपजाति के विभिन्न नाम हैं, जैसे सोल्का, युथरा, कोल इत्यादि। बीर असुर समुदाय की मुख्य भाषा असुरी है, जो मुंडारी भाषा वर्ग से संबंध रखती है। इसके अलावा ये सादरी, नागपुरी और हिंदी भाषा भी बोलते हैं।
असुर जनजाति में पारम्परिक शिक्षा हेतु युवागृह की परम्परा थी जिसे ‘गिति ओड़ा’ कहा जाता था। जो आधुनिकता के संपर्क से अभी समाप्त हो चुकी है। इनमें युवा होने की आयु 10-12 वर्ष मानी जाती थी। आईएएस अधिकारी डॉ. मनीष रंजन के अनुसार, “गिति ओड़ा मुख्यतः नौनिहालों के विविध विकास के केंद्र हैं। यहां इन्हें अपनी मान्यताओं, पूर्वजों और लोककथाओं का ज्ञान मिलता है। आखेट पद्धति भी सिखाई जाती है और सामूहिक कार्यों में भागीदारी का पाठ पढ़ाया जाता है। मानसिक और कलात्मक विकास के लिए नृत्य, संगीत और प्रश्नात्मक पहेलियों की शिक्षा मिलती है तथा जीवन में आवश्यक कार्यों के प्रति रूझान पैदा कर इन्हें अनुशासन एवं श्रम का महत्व बताया जाता है। यहां पुश्तैनी व्यवसायों की शिक्षा भी मिलती है और साथ ही अनुशासनहीनता या गलत कार्यों के लिए दंडित भी किया जाता है। युवागृहों में लड़के-लड़कियों की सदस्यता विवाह के पश्चात समाप्त हो जाती है।”[2] गिति ओड़ा की परंपरा साठ के दशक में खत्म हो गई।
बीर असुर के बारे में साहित्य की एकमात्र प्रकाशित एवं सुषमा असुर और वंदना टेटे द्वारा संपादित पुस्तक ‘असुर सिरिंग’ (कविता संग्रह, 2010) है। इसमें असुर पारंपरिक लोकगीतों के साथ कुछ नये गीत शामिल हैं। यह रांची से प्रकाशित है। 1
1991 की जनगणना के अनुसार बीर असुर की जनसंख्या पूरे भारत में 10,712 है, जबकि झारखण्ड में इनकी संख्या 7,783 है। (स्रोत – विकीपेडिया)
विरजिया असुर
विरजिया एक अलग आदिम जनजाति के रूप में अधिसूचित है। यह मुख्यतः झारखण्ड में ही निवास करते हैं। विरजिया असुर भी लौह उत्पादन करते थे, लेकिन 1950 में बने लौह संरक्षण कानून ने इनसे लौह उत्पादन के कारोबार को छीन लिया। “इनके बारे में कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश से आकर यहां बसे हैं। इनकी दो शाखाएं तेलिया और सिंदुरिया है। इनकी अपनी भाषा बिरजिया है। इनमें बहुविवाह प्रचलित है। विरजिया असुर का पेशा और पर्व बीर असुर से काफी मिलता-जुलता है।”[3] अभी विरजिया जनजाति पत्ता तोड़ने, दोना और पत्तल बनाने का काम करती है। यह जनजाति विलुप्ति के कगार पर है। “विरजिया जनजाति के लोग खुद को रावण और महिषासुर का वंशज मानते हैं, इसलिए रावण दहन भी नहीं करते। दशहरा के दिन ये लोग रावण और महिषासुर की पूजा करते हैं।”[4]

2001 की जनगणना के अनुसार विरजिया असुर जनजाति की जनसंख्या 5356 है।[5]
अगरिया असुर
अगरिया असुर जनजाति मुख्यत: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पायी जाती है। इनमें से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास पाये जाने वाले अगरिया लोग अंग्रेजी राज के समय लोहे के खनन एवं उसे पिघलाकर धातु बनाने का काम किया करते थे। अगरिया जनजाति के कुछ लोग आगरा और मथुरा जिले में भी निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल और मंडला जिलों के अगारिया समुदाय आज भी लोहा गलाने का कार्य करते हैं। इन्हें गोंडों का लोहार कहा जाता है। ये लोग अगरिया भाषा के साथ-साथ हिन्दी और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। “अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता ‘लोहासुर’ है, जिनका निवास धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। ये लोग अपने देवता को काली मुर्गी का भेंट चढ़ाते हैं। इस जनजाति के लोग मार्गशीर्ष महीने में दशहरे के दिन तथा फाल्गुन महीने में लोहा गलाने में प्रयुक्त यंत्रों की पूजा करते हैं। इनका भोजन मोटे अनाज और सभी प्रकार का मांस है। अगरिया सूअर का माँस विशेष चाव से खाते हैं। इनमें गुदने गुदवाने का भी रिवाज है। विवाह में वधु शुल्क का प्रचलन है। समाज में विधवा विवाह की स्वीकृति है। अगरिया लोग उड़द की दाल को पवित्र मानते हैं और विवाह में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है।”[6]

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी अगरिया जनजाति निवास करती है। ख्यात मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने अगरिया असुर के जीवन-दर्शन पर ही ‘अगरिया’ किताब लिखी है। श्री एल्विन कहते हैं, “अगरिया और असुर उसी आदिवासी समूह के वंशज हैं जिनका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में असुरों के रूप किया जाता है।”[7] वे कहते हैं कि, “अगरिया (असुर), जो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं, कुल मिलाकर एक ही आदिवासी हैं जो एक शाखा और अन्य आदिवासियों की शाखाओं का समूह ही हैं। यहां तक कि उनकी एक ही पौराणिकता है, वे एक ही आदि देवता को मानते हैं और उनके टोने-टोटके भी एक से हैं।”[8]

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के महरौनी तहसील में अगौड़ी, अगौरी, आगरा गांवों के नाम अगरिया जनजाति के नाम पर ही रखे गए हैं।[9] उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश के केवल सोनभद्र जिले में अगरिया समुदाय को जनजाति का दर्जा हासिल है व शेष उत्तरप्रदेश में उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। वहीं मध्यप्रदेश में भी उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। आबादी के हिसाब से देखें तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगरिया जनजाति की पूरे भारत में जनसंख्या 72,000 है।[10]
ध्यातव्य है कि गुजरात के कच्छ में भी ‘अगरिया’ नाम से एक जनजातीय समूह पाया जाता है, जो नमक बनाने का काम करता है। गुजरात के अगरिया जनजाति का असुर समुदाय से किसी प्रकार के संबंध के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं।
[1] असुर : जीवन से मरण तक, सुरेश जगन्नाथम, फारवर्ड प्रेस(मासिक), नई दिल्ली, अप्रैल 2016, पृष्ठ – 57-62
[2] डॉ. मनीष रंजन, झारखण्ड सामान्य ज्ञान(2016), प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
[3] डॉ. मनीष रंजन, झारखण्ड सामान्य ज्ञान(2016), प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
[4] http://hindi.eenaduindia.com/States/East/JharKhand/RanchiCity/2016/10/11122801/worships-raavana-on-vijyadashmi-in-ranchi.vpf
[5] http://pib.nic.in/archieve/others/2008/Dec/r2008121914.pdf
[6]http://bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%85%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%E
[7] वेरियर एल्विन, अगरिया (2007), अनुवाद-प्रकाश परिहार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
[8] वेरियर एल्विन, अगरिया (2007), अनुवाद-प्रकाश परिहार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
[9] डॉ. राकेश नारायण द्विवेदी, स्थान-नाम समय के साक्षी (ललितपुर के संबंध में), 2012, जानकी प्रकाशन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश
[10] https://www.ethnologue.com/language/agi
महिषासुर से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ‘महिषासुर: एक जननायक’ शीर्षक किताब देखें। ‘द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन, वर्धा/दिल्ली। मोबाइल : 9968527911. ऑनलाइन आर्डर करने के लिए यहाँ जाएँ: अमेजन, और फ्लिपकार्ट। इस किताब के अंग्रेजी संस्करण भी Amazon,और Flipkart पर उपलब्ध हैं।