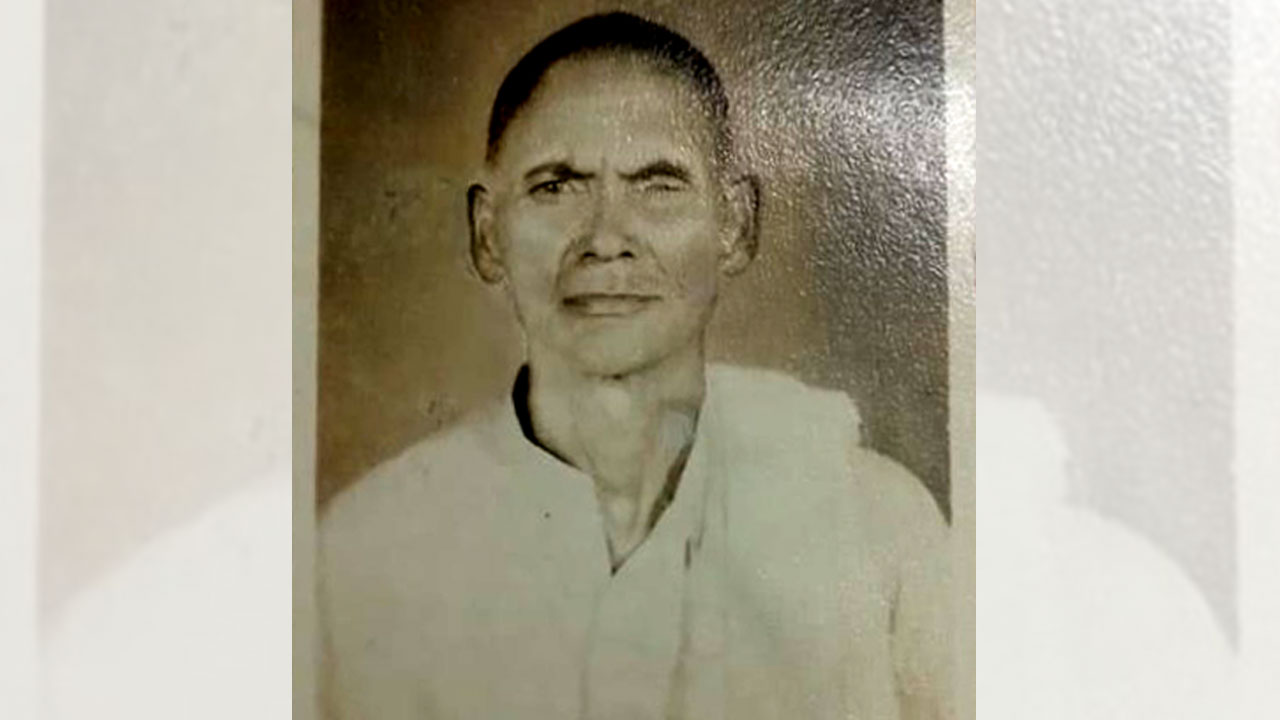संपूर्ण हिंदू वांङ्मय में आदिवासियों को दस्यु, दास, राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर, वानर आदि शब्दों से संबोधित किया गया है, जो मायावी शक्तियों से संपन्न धरती, आकाश और पाताल में विचरण करने वाले प्राणी हैं, और जो हमेशा सज्जन मनुष्यों और देवताओं को परेशान करते हैं। गौरतलब है कि हिंदू वर्ण-व्यवस्था में उन्हें शामिल नहीं किया गया है और उन्हें अनार्य माना गया है। हिंदू वर्ण-व्यवस्था की चार श्रेणियां हैं– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके काम भी विभाजित हैं। जैसे कि ब्राह्मण शास्त्रों के पठन-पाठन का कार्य करता है। क्षत्रिय, वह जो शस्त्र धारण करता है और शासन करता है। वैश्य, वह जो व्यापार करता है। और शूद्र, वह जो हाथ से किए जाने वाले सारे काम करता है। इस व्यवस्था को प्रचलित भाषा में ‘मनुवाद’ कहते हैं।
कहा जाता है कि इसकी शुरुआत श्रम विभाजन से हुई और प्रारंभिक दौर में इन श्रेणियों में इतनी जड़ता भी नहीं थी। यानि, अपनी क्षमता और अध्यवसाय से शूद्र भी ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता था। लेकिन रामायण काल तक यह व्यवस्था जड़ रूप ले चुकी थी। एक शूद्र ने जब सशरीर तप कर स्वर्ग जाने का प्रयास किया तो राम ने उसका सर कलम कर दिया। यह कथा शंबूक वध के रूप में विख्यात है और वाल्मिकी रामायण में वर्णित है।
अनार्य ही रहे आदिवासी
खैर, अभी हम यहां बस इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं कि आदिवासी इस वर्ण-व्यवस्था के हिस्सा नहीं रहे। इसकी दो ही वजहें हो सकती हैं। एक तो वे इस व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा, मनुवादियों ने उन्हें इस योग्य नहीं पाया। हमारी समझ तो यही है कि उनका वश चलता तो वे उन्हें दलित संवर्ग में तो शामिल कर ही लेते, लेकिन आदिवासियों ने उनकी दासता कभी स्वीकार नहीं की। वे निरंतर अपनी अस्मिता और अलग पहचान के लिए संघर्ष करते रहे। शायद कभी वे मैदानी क्षेत्र के वाशिंदे थे, लेकिन निरंतर संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना ठिकाना दुर्गम पर्वतीय और झाड़-झंकाड़ से भरे इलाकों को बनाया।
एक धारणा यह भी है कि पहाड़ और मैदानी क्षेत्र की संस्कृति में प्रारंभ से अलगाव रहा है। आदिवासी प्रारंभ से ही प्रकृति के साहचर्य में पर्वतीय क्षेत्र और जंगलों में निवास करते रहे हैं, जहां उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से जंगल को साफ कर खेती योग्य जमीन बनाया। उन्होंने मैदानी क्षेत्र में प्रवेश की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन जब भी उनके इलाके में प्रवेश कर उनके जल, जंगल, जमीन को छीनने की कोशिश हुई, इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। अंग्रेजों के जमाने में यह संघर्ष तीव्र रूप में दिखा। सिदो और कान्हू का ‘हूल’ और बिरसा का ‘उलगुलान’ उसी संघर्ष की अभिव्यक्ति है। इस संघर्ष की मूल भावना थी– ‘अबुआ दिसुम, अबुआ राज’। यानि, ‘अपने देश में अपना राज’।
अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों का यह संघर्ष 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से शुरू हो गया था, जबकि भारत की आजादी के संघर्ष में यह भावना यानि, पूर्ण स्वराज्य की मांग करीबन सौ वर्ष बाद 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ से शुरू हुई। मुख्यधारा के इतिहासकारों ने कभी भी उस आदिवासी संघर्ष के महत्व को अपने इतिहास में जगह नहीं दी। हालांकि, उन संघर्षों को अपने बेहतर और आधुनिक हथियारों के बल पर अंग्रेजों ने कुचल तो दिया, लेकिन उन्हीं संघर्षों और आदिवासियों की शहादत के कारण उन्होंने आदिवासियों के लिए विशेष भूमि कानून बनाए। पांचवीं व छठी अनुसूची की परिकल्पना भारतीय संविधान में शामिल हुई।
‘सरना और सनातन एक’ होने का नारा अब क्यों?
सवाल उठता है कि जिन अनार्य आदिवासियों के साथ आर्यों का इतिहास के लंबे दौर में लगातार संघर्ष होता रहा, जो आर्यों की वर्ण-व्यवस्था में शामिल नहीं रहे, उन्हीं आदिवासियों को कट्टर हिंदूवादी संगठन अब हिंदू बनाने या कहने के लिए लालायित क्यों हैं? ‘सरना और सनातन एक’ होने का नारा क्यों लगाया जा रहा है?
डॉ. आंबेडकर जैसे महामानव भी आदिवासियों को असभ्य और जंगली तो मानते थे, लेकिन उन्हें हिंदू ही बताते थे और उन्हें इस बात का गहरा क्षोभ था कि हिंदुओं ने उन असभ्य भाइयों को सभ्य बनाने का काम क्यों नहीं किया? इसकी एकमात्र वजह यह कि संसदीय प्रणाली बहुमत के आधार पर चलती है और आदिवासी आबादी चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके गर्भनाल से जुड़ी भाजपा पुरजोर स्वर में ‘सरना’ और ‘सनातन’ के एक होने का प्रचार करती रहती है। आदिवासी शब्द को संविधान में रखने से परहेज किया गया और उन्हें अलग धार्मिक कोड देने के लिए वे तैयार नहीं हैं।
आदिवासी और गैर-आदिवासी संस्कृति का फर्क
रंग, रूप और भाषा के आधर पर एक नस्ल के लोगों की पहचान और दूसरे से उसके फर्क को रेखांकित करने की कोशिश होती रही है, लेकिन जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण के अंतर को जब तक नहीं समझा जाए, तब तक आदिवासी और गैर-आदिवासी समाज के फर्क को हम नहीं समझ सकते। समाज विज्ञान ने संसार की सभी जातियों को रंग के आधार पर मुख्यतः तीन नस्लों में बांटा है। पहली नस्ल गोरों की है, जिसे हम काकेसियन कहते हैं। दूसरी नस्ल मंगोलो की है, जिनका रंग हल्का पीला होता है। तीसरी नस्ल काले लोगों की है। अन्य रंग इन्हीं रंगों के मेल से बने हैं। लेकिन सिर्फ रंग के आधार पर पहचान करने की बात हो तो द्रविड़ों और आदिवासियों के रंग में एक तरह से समानता है, फिर भी दोनों की संस्कृतियों में बहुत फर्क है।
इसी तरह रूप के आधार पर विभाजन किया जाए तो अपने देश में चार प्रकार के लोग मिलते हैं। एक तरह के लोगों का कद छोटा, रंग काला, नाक चौड़ा और बाल घुंघराले होते हैं। ये संभवतः जनजातीय समुदाय के लोग हैं और जिन्होंने अपना ठिकाना जंगलों में बना रखा है।

इतिहासकारों के मतानुसार ये द्रविड़ों और आर्यों के पहले से यहां आकर बसे थे। एक दूसरे किस्म के लोग वे हैं जिनका कद छोटा, रंग काला, सिर के बाल घने और नाक खड़ी और चौड़ी होती है। रंग और कद-काठी में ये आदिवासियों के समान दिखते हैं, लेकिन वे आदिवासियों से भिन्न हैं और विंध्याचल के नीचे सारे दक्षिण भारत में फैले हुए हैं। ये द्रविड़ जाति के लोग हैं जो आर्यों के पहले इस देश में आए थे और नगर-सभ्यता की नींव इन्हीं लोगों ने डाली थी। तीसरी जाति के लोग आर्य हैं, जिनका रंग गोरा या गेहुंआ होता है, कद-काठी लंबी और नाक नुकीली होती है। लेकिन इस देश की उष्ण जलवायु और अन्य जातियों के वैवाहिक मिश्रण से उनका रूप रंग भी आज बहुत बदल गया है।
रंग-रूप के लिहाज से चौथे लोग वे हैं जो बर्मा, असम, भूटान, नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर बंगाल और कश्मीर के उत्तरी किनारे पर पाए जाते हैं। इनका रंग पीला, आकृति चिपटी और नाक पसरी हुई होती है। ये मंगोल जाति के लोग हैं।
भाषा के लिहाज से भी मनुष्य समुदाय का वर्गीकरण किया गया है। डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी का कहना है कि भारतीय जनता की रचना जिन लोगों को लेकर हुई है, वे मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। आस्ट्रिक अर्थात आग्नेय, द्रविड़ और इंडो-यूरोपीय। झारखंड में इंडो-यूरोपीय समूह की भाषाएं सदानी[1] में बदल गई हैं। वहीं द्रविड़ ग्रुप की भाषाओं से मिलती-जुलती हैं कुडुख व उरांव और आस्ट्रिक ग्रुप में संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया को रखा गया है। इस प्रकार भाषायी दृष्टि से झारखंड के आदिवासी आस्ट्रिक भाषा समूह के सदस्य हैं।
कौन इस देश में पहले आया और कौन बाद में, इसको लेकर भी थोड़ा विवाद है। सामान्यतः यह माना जाता है कि सबसे पहले नीग्रो समुदाय के लोग यहां आए। उनके बाद आग्नेय जाति के लोग, फिर द्रविड़ और सबसे बाद में आर्य जाति के लोग। लेकिन इस बात को लेकर थोड़ा विवाद है कि द्रविड़ पहले आये या आदिवासी। आस्ट्रिक भाषा भाषी उरांवों की भाषा द्रविड़ भाषा के करीबी मानी जाती है, इसको लेकर एक मत यह भी है कि आदिवासी जातियां द्रविड़ों की ही संतान हैं। लेकिन यह एक अपुष्ट धारणा है।
अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि जब आर्य इस देश में आए तो आग्नेय जाति के लोग सिंधु की तराई में विद्यमान थे।
कई ऐसी परंपराएं आज भी वर्तमान में हैं, जिनसे पता चलता है कि आग्नेय जाति के इन आदिवासियों का कभी इस देश पर प्रभुत्व रहा था। मारवाड़ के राजा राज्याभिषेक के समय किसी भील के अंगूठे से रक्त लेकर उसका तिलक लगाते थे। क्योंझर, जो झारखंड के बगल के राज्य ओडिशा में पड़ता है, के राजा का राजतिलक भी प्रजा जनजाति के किसी सदस्य द्वारा होता था। इसी तरह की परंपरा जयपुर, राजस्थान में भी पाई जाती थी।
आदिवासियों को वनवासी कहने का निहितार्थ
इन वर्गीकरणों और विभाजनों के बाद हजारों वर्षों तक साथ रहने की वजह से एक मिली-जुली संस्कृति बनी है, लेकिन इस मिली-जुली संस्कृति से आदिवासी संस्कृति का मेल नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों ने भारत में जातियों और संस्कृतियों का जो समन्वय किया, उसी से हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति का निर्माण हुआ। बाद में जो भी आए, उन्होंने इस हिंदू संस्कृति को स्वीकार किया और उसमें समाहित हो गए, चाहे वे मंगोल हो, यूनानी, यूची, शक, अभीर, हूण और तुर्क हों। लेकिन यह सर्वमान्य तथ्य है कि आग्नेय परिवार के आदिवासियों ने उस हिंदू धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। यह अलग बात कि हिंदू समाज के लोग और खुद को हिंदू धर्म का पैरोकार मानने वाले संघ परिवार के लोग आदिवासियों को, जिन्हें हाल तक वे वनवासी कहते थे, हिंदू साबित करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदू समाज में वनवासियों की हैसियत क्या है, उसे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कुछ कहानियों और मिथकों से समझा जा सकता है।
मसलन, हनुमान को वनवासियों का पूर्वज बताते हुए उसे राम का परम सेवक होने का दर्जा दिया गया है। है वह सेवक ही। सूर्यवंशी आर्यपुत्र राम के चरणों में बैठने और वक्त बे वक्त उन्हें कंधे पर लाद कर घूमने वाला सेवक। महाभारत की कथा के अनुसार एक आदिवासी युवक एकलव्य ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखनी चाही तो उन्होंने सिखाने से इंकार कर दिया। अपने कौशल और लगन से जब उसने धनुर्विद्या सीख ली तो कहीं वह उनके शिष्य अर्जुन से प्रतिस्पर्धा न करने लगे, इसलिए द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में उससे अंगूठा ही मांग लिया। आज भी तथाकथित विकास के नाम पर आदिवासी समाज से कुर्बानी मांगी जाती है और अपनी बलि देने से इंकार करने पर उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। ठीक वैसे जैसे ओडिशा के कलिंगनगर और झारखंड के तपकरा में हुआ। कलिंगनगर में वे अपनी जमीन पर टाटा कंपनी का कारखाना बनने का विरोध कर रहे थे, जहां पुलिस फायरिंग में बारह आदिवासी मारे गए। इसी तरह झारखंड राज्य गठन होने के बाद कोयलकारो परियोजना का विरोध करने वाले आदिवासियों पर तपकरा में पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें सात आदिवासी और एक मुसलमान मारा गया।
आदिवासियों का जीवन और धर्म-दर्शन
दरअसल रंग-रूप और भाषा की खाई को तो पाटी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें पाटना मुश्किल होता है। मसलन, जीवन के बारे में हमारा दृष्टिकोण, प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते आदि। आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के जीवन दृष्टि के फर्क को हम कुछ ठोस उदाहरणों से समझ सकते हैं।
ईश्वर की कल्पना किसी न किसी रूप में सभी धर्मावलंबी करते हैं। गैर-आदिवासी समाज ईश्वर की कल्पना सगुण रूप में अलौकिक गुणों से संपन्न पुरूष के रूप में करता है। राम, कृष्ण या विष्णु आदि अलौकिक शक्तियों से संपन्न पुरूष हैं। ईश्वर का निर्गुण रूप भी मानवीय गुणों से ही संपन्न है। जबकि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। वे पहाड़, जंगल, जंगल के किसी वृक्ष मात्र को पूजते हैं। किसी आदिवासी गांव में मंदिर नहीं होता। उनके देवता जंगल, पहाड़ों में निवास करते हैं और उनका पूजा स्थल भी वहीं होता है।
पूरी हिंदू सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म पर टिकी हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके चार भाग हैं। हिंदू धर्मावलंबी और विद्वान इस व्यवस्था को उचित ठहराते हुए यह सफाई देते हैं कि यह मूल रूप में जड़ व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि दलित घर में जन्म लेने वाला हर आदमी दलित और अछूत ही माना जाता है। आदिवासियों में यह वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था नहीं है।
आदिवासी समाज श्रम आधारित समाज है और गैर-आदिवासी समाज दूसरे के श्रम के शोषण पर टिका समाज है। खुद रिक्शा खींचकर जीवनयापन करना श्रम आधारित समाज की रचना करता है। जब कोई दो, चार या दस रिक्शा दूसरे से खिंचवा कर पैसे कमाता है तो कहा जाएगा कि वह दूसरे के श्रम के शोषण पर टिका है। गैर-आदिवासी समाज का भी एक बड़ा हिस्सा कृषि व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन वहां जमीन का मालिक वैसा व्यक्ति भी हो सकता है जो खुद खेती नहीं करता हो। पूरे उत्तर भारत में कृषि व्यवस्था दिहाड़ी मजदूरों पर टिकी हुई है। आदिवासी समाज में ऐसी कल्पना ही नहीं की जा सकती।
पूरी गैर-आदिवासी व्यवस्था अतिरिक्त उत्पादन और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांतों पर टिका है। विकास के लिए जरूरी है अतिरिक्त उत्पादन और मुनाफा। कुछ लोगों के श्रम से उनकी जरूरत से अधिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन हुआ तभी मानव जाति के विकास का रास्ता खुला। कुछ लोग अन्य कार्यों में लगे जिससे विभिन्न पेशों और सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। अब कुछ लोग पठन-पाठन का कार्य कर सकते थे, शोध का कार्य कर सकते थे। कुछ लोगों ने लड़ने-भिड़ने में ही महारत हासिल की। कुछ लोग नृत्य और गीत में ही प्रवीण हुए। कुछ लोग सिर्फ दलाली करके जी सकते हैं। इस व्यवस्था की विडंबना यह हुई कि इसमें शारीरिक श्रम की कीमत सबसे कम आंकी गई और इसलिए श्रम करने वाले को निकृष्ट माना गया। खेत में काम करने वाला, चमड़े का सामान बनाने वाला, कपड़े बुनने वाला – ये सभी निम्न हैं और आर्थिक दृष्टि से भी सबसे अधिक विपन्न हैं।
सरप्लस इकोनॉमी में विश्वास नहीं रखते हैं आदिवासी
आदिवासी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अतिरिक्त उत्पादन और अतिरिक्त मूल्य/मुनाफा के सिद्धांत का पूरी तरह निषेध करता है। वह उतना ही उत्पादन करता है जितने की उसे जरूरत है। वह कल की चिंता नहीं करता और इसलिए प्रकृति का उतना ही दोहन करता है, जिससे उसका नुकसान न हो। परिवार के सदस्य अपने हाथ से खेती करते हैं। कुछ ऐसे काम जो अपने बलबूते नहीं हो सकता, मसलन रोपनी का काम, तो इस काम में एक-दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन यह कल्पना करना कि कोई अपनी पूरी जमीन बटाई पर दे रखी हो, इस समाज में हाल तक कठिन था। और चूंकि अतिरिक्त उत्पादन की गुंजाइश नहीं, इसलिए सभी को श्रम करना है। कोई पाहन, पुरोहित हो सकता है, लेकिन इस वजह से उसे मुफ्त में खाने का अवसर नहीं मिल जाता।
हालांकि गैर-आदिवासी समाज में सभी में थोड़ी बहुत वणिक बुद्धि होती है। यानी जोड़-तोड़, हिसाब-किताब करना। कल की चिंता और उसके लिए संचय करना। इसलिए गैर-आदिवासी समाज का कोई भी सदस्य ‘धंधा’ कर सकता है। यह अलग बात है कि कोई ज्यादा प्रवीण होता है कोई कम। लेकिन आदिवासी समाज का संपन्न से संपन्न व्यक्ति ‘धंधा’ नहीं कर सकता। संपन्न होने के बावजूद महाजनी नही कर सकता।
सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के इस अंतर का प्रतिफलन कलाओं के क्षेत्र में भी हुआ है। गैर-आदिवासी समाज में रंगमंच होता है और दर्शक दीर्घा / प्रेक्षागृह, कलाकार और दर्शक। लेकिन आदिवासी समाज में इस तरह का विभाजन नहीं है। पीड़ा और उल्लास के क्षणों की भी सामूहिक अभिव्यक्ति होती है जिसमें सभी भागीदार होते हैं। फसल कटने के बाद चांदनी रात में नाचते वक्त आदिवासी समाज का हर औरत-मर्द कलाकार बन जाता है। दूसरी तरफ यदि कोई अच्छी बांसुरी बजाता है तो वह उसका अतिरिक्त गुण तो है लेकिन इस वजह से उसे इस बात की छूट नहीं कि वह अपने खेत में काम न करे।
ये कुछ आदिवासी और गैर-आदिवासी समाज तथा उनकी संस्कृति में अंतर करने वाली बातें हैं। इन्हें और भी सूत्रबद्ध करने की जरूरत है ताकि यह समझा जा सके कि गैर-आदिवासी समाज का पिछड़ा, दलित तबका या कोई भी अन्य व्यक्ति आदिवासी समाज में पहुंच कर उत्पीड़क कैसे बन जाता है? आदिवासी इतनी आसानी से ठगे क्यों जाते हैं?
पुनश्च
आश्चर्य तो यह होता है कि इन सबके बावजूद आदिवासी आज तक अपना अलग अस्तित्व बनाये रखने में कामयाब कैसे है। वह शायद इसलिए कि वे अपनी जमीन और अपनी संस्कृति से अभिन्न रूप से जुड़े हैं और लगातार अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष भी करते रहे हैं। यह भी गौरतलब है कि सिर्फ वाचिक रूप में रहने के बावजूद आदिवासी भाषाएं हजारों वर्षों से नदी की अविरल धार की तरह बहती आई हैं और जीवित हैं। जबकि इस बीच गैर-आदिवासी समाज की अनेकानेक भाषाएं समय के साथ विलुप्त हो गईं या अपना रूप-रंग बदल लिया। सामंतों और अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत थी जो सिमट कर रह गई है। उसकी जगह अंग्रेजी उनकी भाषा बन गई है। इतने सांस्कृतिक और धार्मिक अंतर के बावजूद ‘सरना और सनातन एक है’ की बात कैसे कही जा सकती है। आरएसएस द्वारा यह बार-बार दुहराना कि ‘सरना’ और ‘सनातन’ एक हैं, का निहितार्थ बस इतना कि आदिवासी धर्म और संस्कृति का विलोपन हो जाये और वे हिंदू धर्म में समाहित हो जाएं।
[1] झारखंड के आदिवासी इलाकों में रहने वाले गैर-आदिवासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली एक क्षेत्रीय बोली
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in