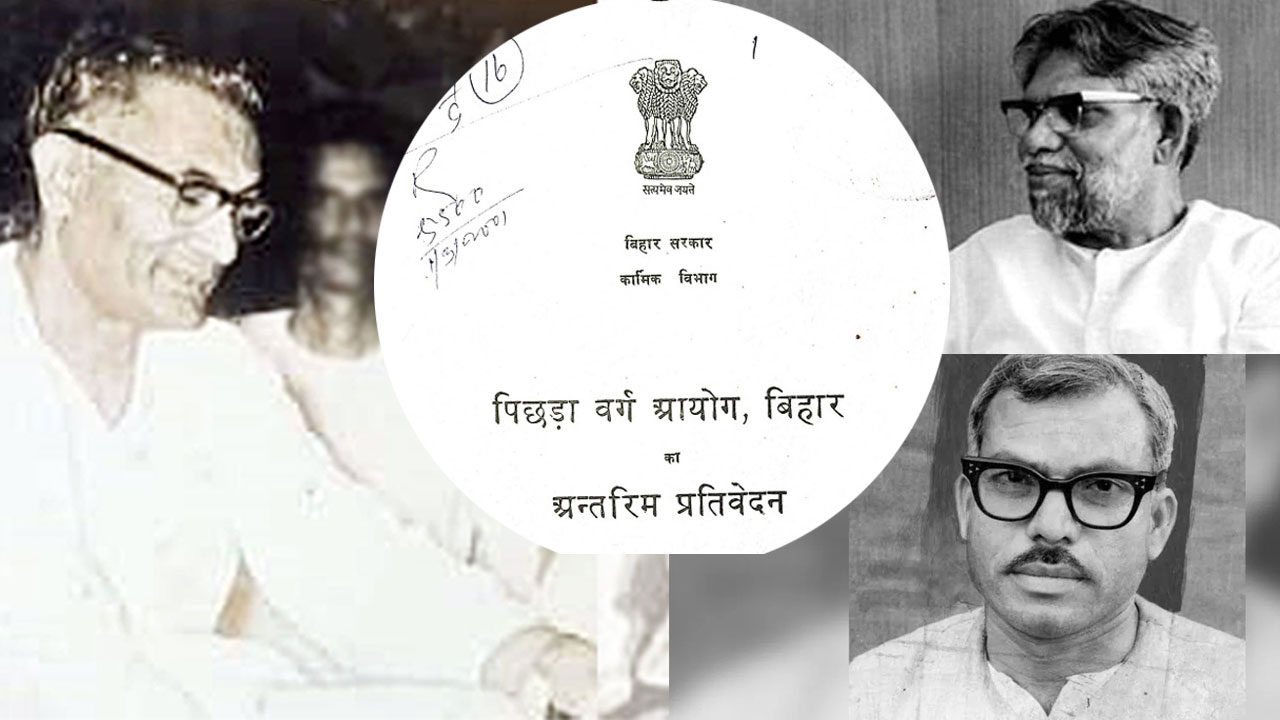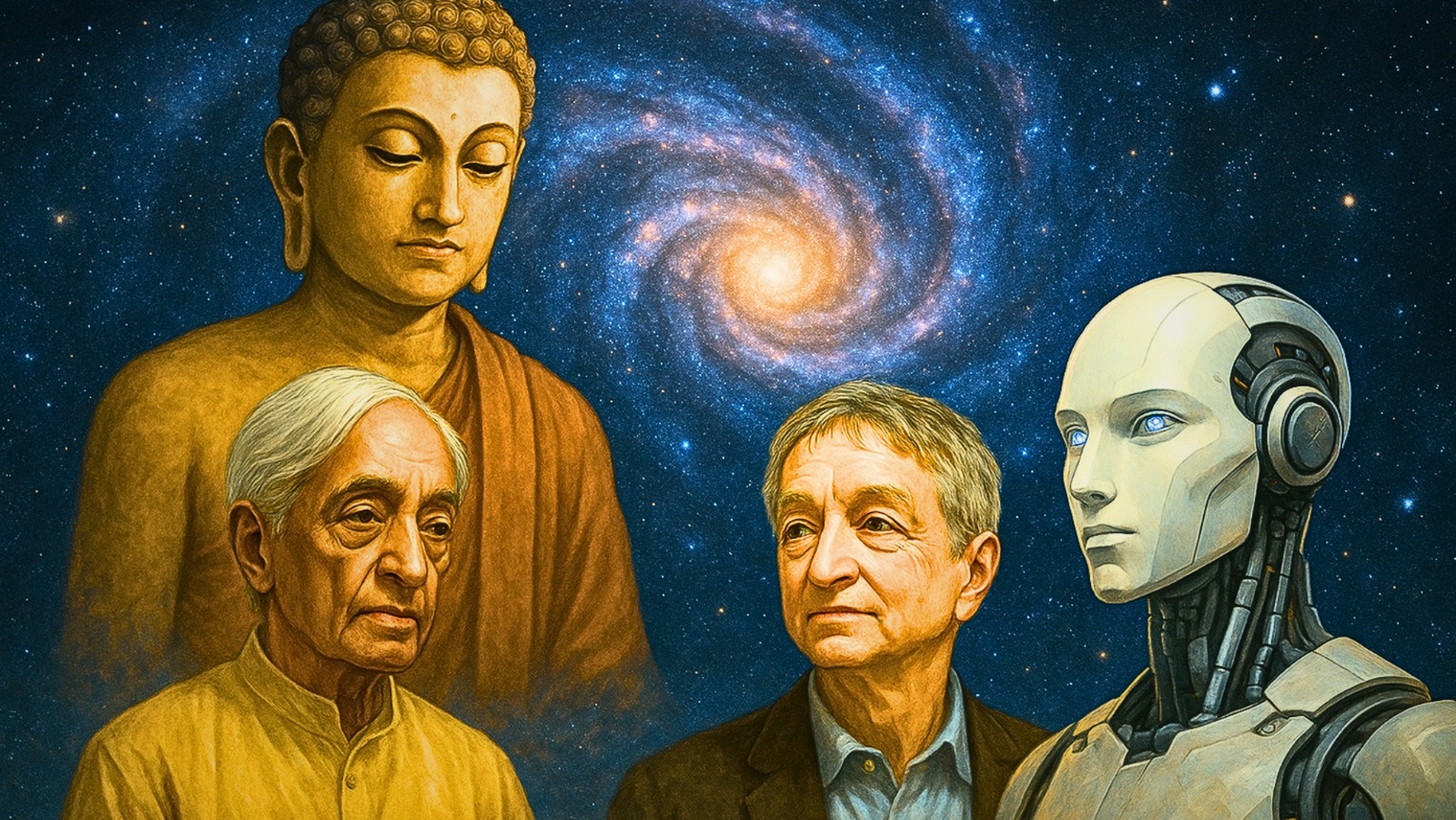औपनिवेशिक काल में भारत में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के उदय के साथ ही सभी जातियों के लिए शिक्षा उनमें प्रवेश पाने की राह बन गई। उच्च जातियों का शिक्षा पर पहले से ही एकाधिकार था और इसलिए इन संस्थाओं में भी उनका वर्चस्व कायम हो गया। दलितों के लिए शिक्षा सामाजिक उन्नति के द्वार खोलने वाली कुंजी थी। फुले ने शिक्षा को ‘तृतीय रत्न’ बताया था और आंबेडकर ने अपने लोगों को ‘शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो’ का नारा दिया था। (रेगे, 2010)
औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली ने दलितों के एक छोटे से तबके को सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ने का अवसर दिया। इस सामाजिक गतिशीलता के चलते वे राज्य के विभिन्न अवयवों में अपने लिए न्यायसंगत स्थान मांगने लगे। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासन में भी दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों को शिक्षा और प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों ने ऊंची जातियों को ज्यादा तवज्जो दी और हमेशा यह ख्याल रखा कि उन्हें किसी प्रकार से चोट न पहुंचे। उन्होंने जाति के प्रश्न को नज़रअंदाज़ किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष फुले के अविस्मरणीय भाषण – जिसकी चर्चा इस लेख में आगे की गई है – इस बात को साबित करता है।
हाशिए के लोगों की शिक्षा की मांग
औपनिवेशिक काल में दलित और शासक वर्ग शिक्षा को अलग-अलग तरीकों से देखते-समझते थे। दलितों के लिए शिक्षा समाज में एक सम्मानित स्थान पाने और निम्न दर्जे के कामों से मुक्ति पाने का साधन थी। औपनिवेशिक सरकार के लिए शिक्षा का उद्देश्य था– मजदूरों, गृहणियों और किसानों के रूप में दलितों को उत्पादक, अनुशासित और उनके प्रति वफादार बनाए रखना। (कुमार, 2019) रूपा विश्वनाथ का तर्क है कि मिशनरियां समतावाद के आदर्श से प्रेरित नहीं थीं। वे केवल धार्मिक नजरिए से जाति के गुण-दोष की समीक्षा करती थीं। उन्हें जाति के ढांचे की सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक समालोचना में कोई रूचि नहीं थी। वे तो केवल कठोर और क्रूर ‘प्राच्य दासता’ को अपेक्षाकृत थोड़ी नर्म और थोड़ी उदार गुलामी से प्रतिस्थापित करना चाहती थीं। (वही) औपनिवेशिकतावाद के व्यापक ढांचे के अंदर मिशनरियों में परस्पर वैचारिक विरोधाभास भी थे। एक ओर वे ज्ञानोदय और उदारवादी मूल्यों की बात करती थीं तो दूसरी ओर वे यह भी मानती थीं कि ऊंची जातियां एक श्रेष्ठ और सभ्य नस्ल हैं और हाशियाकृत श्रमिक जातियों के उत्पादन अधिशेष पर कब्जा करने के लिए उच्च जातियों के साथ गठबंधन भी किया। अमेरिकन मेथोडिस्ट अपिस्केपल चर्च (एमईसी) के अभिलेखों को ध्यान से पढ़ने से यह जाहिर होता है कि चर्च ने स्कूल क्यों खोले। उसने स्कूल इसलिए खोले ताकि जो दलित ईसाई धर्म अपना रहे थे, उनका उपयोग मिशनरी की प्रशिक्षित कर्मिंयों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा सके और इसके चलते ऐसे काम उनके हाथ आ गए, जो सम्मानजनक थे और जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती। (वही) लेकिन इसके बावजूद दलितों के संबंध में मिशनरियों में पूर्वाग्रह कायम रहे और वे उन्हें केवल मजदूर के रूप में देखती रहीं। दलितों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण 1850 के दशक से शुरू हुआ। उस समय की शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता की दृष्टि से बहुस्तरीय थी। नतीजा यह कि बहुत कम संख्या में नव ईसाइयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकी। इससे भारत का ईसाई समुदाय, शिक्षा, रहवास के क्षेत्र और पेशे की दृष्टि से अत्यंत असमान बन गया।
एक बहु-प्रचारित प्राच्य नैरेटिव हमें बताता है कि औपनिवेशिक सरकार की नीतियों और ईसाई मिशनरियों के प्रयासों से दलितों का एक तबका शिक्षा हासिल कर सका। इस प्रक्रिया में दलितों की थोड़ी-सी भी भूमिका थी, ऐसा हमें नहीं बताया जाता। शिक्षा हासिल करने के लिए उनके स्वयं के प्रयासों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दलितों को यह एहसास था कि उनकी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के चलते अगर उन्हें अपना सामाजिक दर्जा बेहतर बनाना है तो शिक्षा हासिल करना ही उनके सामने एकमात्र रास्ता है। (नंबीसन, 1996) फिलिप कॉन्सटेबल का तर्क है कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक परिवर्तनों के मुख्य वाहक औपनिवेशिक अधिकारी नहीं, बल्कि अछूत हिंदुओं और अछूत ईसाइयों की पहली शिक्षित पीढ़ी थी। अरूण कुमार इस तर्क के समर्थन में प्राथमिक आंकड़े उपलब्ध करवाते हुए बताते हैं कि किस प्रकार मुरादाबाद शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले मज़हबी सिक्खों ने 1859 में शिक्षा और रोजगार दिए जाने की मांग की और किस तरह बदायूं के भंगियों ने मिशनरियों से संपर्क किया। जैसे-जैसे दलितों में शिक्षा की मांग जोर पकड़ने लगी वैसे-वैसे दकियानूसी तत्वों को यह डर सताने लगा कि दलितों पर उनका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। मेथोडिस्ट अपिस्केपल चर्च के उपदेशक ज़हूर-उल-हक़ लिखते हैं कि आज के उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हसनापुरा गांव के चमार जुलाहे मिशनरी स्कूलों के जरिए खुद को और अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए लालायित थे। ज़हूर-उल-हक़ ने यह संभावना व्यक्त की कि पड़ोसी जिलों के चमार बड़ी संख्या में ईसाई धर्म अपना सकते हैं। और यह ऐसी एकमात्र घटना नहीं थी। इन सबसे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि दलितों को यह समझ में आ गया था कि सामाजिक गतिशीलता और आत्मसम्मान हासिल करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इसलिए वे शिक्षा हासिल करने के लिए एक नए धर्म का वरण करने के लिए भी तैयार थे। अरूण कुमार का कहना है कि दलितों के सामूहिक धर्मपरिवर्तन के डर के चलते ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसके झंडे तले ज़मींदारों और स्थानीय व्यापारियों ने दलितों को बुनियादी शिक्षा देनी शुरू की। इसका उद्देश्य दलितों का उत्थान करना नहीं, बल्कि दलितों पर ईसाई धर्म और इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। वे लोग यह भी चाहते थे कि दलित उनके अधीन बने रहें।

शिक्षा के प्रति ब्रिटिश प्रशासन के दृष्टिकोण को अक्सर अंग्रेजों की नैतिकता से जोड़ा जाता है। लेकिन हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि अंग्रेजों को प्रशासन चलाने में उनकी सहायता करने के लिए भारतीयों की ज़रूरत थी। अंग्रेजों द्वारा शिक्षा पर जोर दिए जाने के बाद भी केवल मुट्ठीभर भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा हासिल हो सकी और उनके अधीन काम करने वाले भारतीयों में से अधिकांश अकुशल श्रमिक ही बने रहे। भारत में ब्रिटिश शासन की एक अन्य विशेषता यह थी कि यद्यपि उसने उत्पादन के अधिशेष पर कब्जा करने के लिए एक नए राज्य तंत्र का निर्माण किया मगर साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि शोषण और अधिशेष को हड़पने की पारंपरिक प्रणाली – अर्थात जाति व्यवस्था – बनी रहे। उन्होंने अधिशेष पर कब्जा करने के लिए ऊंची जातियों के साथ साठगांठ की। अंग्रेजों का एक तबका इस गठजोड़ का औचित्य सिद्ध करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगा कि ब्राह्मण एक ‘शुद्ध नस्ल’ है। इस सोच ने इतनी मज़बूत जड़ें पकड़ लीं कि गवर्नर माउंट स्टूअर्ट एलफिंस्टन जैसे औपनिवेशिक सत्ता के कुछ अधिकारी सरकार को चेताने लगे कि अछूतों को शिक्षा से जोड़ने से शेष आबादी में शिक्षा की स्वीकार्यता बाधित होगी। इसके विपरीत, ब्राह्मणों को पश्चिमी शिक्षा के झंडाबरदार के रूप में देखा जाता था और अंग्रेजों ने इस समुदाय पर विशेष ध्यान दिया। एक और तथ्य यह है कि अंग्रेजों के आने के पहले सदियों से ऊंची जातियों की पारंपरिक शिक्षा तक बेहतर पहुंच थी और वे सामाजिक ढांचे के शीर्ष पर थे। पारंपरिक शिक्षा का उद्देश्य वर्ण-व्यवस्था को कायम रखना था। और इस प्रणाली में विद्यार्थियों को उनके वर्ण या जाति के अनुरूप कौशल सिखाए जाते थे। अंग्रेजों ने शिक्षा के रास्ते जिस विचारधारा को भारत में फैलाया वह प्राच्यवाद ही थी। अलबत्ता, इस कड़वी गोली पर उदारवादी मूल्यों की मीठी परत चढ़ा दी गई थी। अंग्रेजों को नए कौशलों से लैस श्रम बल की आवश्यकता थी। मगर इस मामले में जाति उनकी राह में बाधक थी क्योंकि वह श्रमिकों को नए कौशल हासिल करने से रोकती थी। इन विरोधाभासों ने अंग्रेजों के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को आकार दिया।
गीता बी. नंबीसन बताती हैं कि हालांकि कहने को अंग्रेजों की नीति यह थी कि – किसी लड़के को सरकारी कॉलेज या स्कूल में जाति के कारण दाखिला देने से इंकार नहीं किया जाएगा – लेकिन व्यवहार में यह नीति लागू नहीं की जाती थी। (नंबीसन, 2020) ऊंची जातियां नहीं चाहती थीं कि उनके बच्चे अछूतों के साथ उठे-बैठें। इस मामले में बंबई सरकार शुरुआत में कुछ असमंजस में रही। फिर, 1859 में उसने साफ कर दिया कि अध्यापकों के लिए निम्न जातियों के विद्यार्थियों को दाखिला देना आवश्यक नहीं होगा, अगर ऐसी संभावना हो कि उसके कारण अन्य विद्यार्थी स्कूल का बहिष्कार करेंगे। मगर यह भी सही है कि सरकार ने अछूतों के लिए विशेष स्कूल खोले और कुछ निजी मिशनरी स्कूलों को उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुदान भी दिया। जैसा कि विकास गुप्ता लिखते हैं, “सरकार के पास कानूनी ताकत भी थी और खजाने पर भी उसका नियंत्रण था। मगर फिर भी उसने शिक्षा के इस क्रांतिकारी सिद्धांत को लागू करने का समुचित प्रयास नहीं किया कि सभी विद्यार्थियों को एक-समान स्कूलों में एक-सी शिक्षा मिलनी चाहिए।” (गुप्ता व अन्य, 2021) जिला शिक्षा बोर्ड प्रगतिशीलता का मुखौटा भी पहने रहना चाहते थे मगर उच्च जातियों के हिंदुओं को नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बड़ी चतुराई से अछूत बच्चों के लिए बरामदों में बैठने की अलग व्यवस्था कर दी।
शिक्षा आयोग के समक्ष फुले का अविस्मरणीय संबोधन
जैसा कि हमने देखा दलितों को शिक्षा तक पहुंच बदली हुई परिस्थितियों के कारण मिल सकी। मगर इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि दलितों ने शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ स्वयं संपर्क-संबंध स्थापित किए, खुद पहल की।
फुले शूद्र थे। वे अछूत नहीं थे। अगर वे आज जीवित होते तो दलित नहीं, बल्कि ओबीसी कहलाते। मगर उन्होंने शूद्र-अतिशूद्रों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अछूतों या दलितों के लिए अति-शूद्र शब्द का प्रयोग शुरू किया। इसका उद्देश्य था निम्नतम वर्ण शूद्र और अवर्ण अछूतों को उन पर लादी गई ब्राह्मणवादी वंचनाओं के खिलाफ एक करना। यह महत्वपूर्ण है कि फुले ने ही उनके बाद आने वाली पीढ़ियों की दलितों की मुक्ति हेतु संघर्ष करने की राह बनाई।
महात्मा फुले माली जाति के थे। इस जाति के लोग भूस्वामी और किसान थे और उन्हें समाज में सम्मानीय दर्जा हासिल था। शुरुआत में जोतीराव फुले एक पारंपरिक स्कूल में पढ़े। किशोरवय में प्रवेश होते ही सावित्रीबाई से उनका विवाह कर दिया गया। बाद में उन्हें स्कॉटिश मिशन के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिला दिलवाया गया, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सन् 1847 में पूरी की। (त्सुरेनेव एवं म्हासकर, 2021) लड़की होने के कारण सावित्रीबाई इतनी भाग्यशाली नहीं थीं। मगर जोतिबा फुले उस समय व्याप्त लैंगिक अन्याय को समझते थे और इसलिए उन्होंने सावित्रीबाई को घर में पढ़ाया। फिर फुले और सावित्रीबाई वंचित वर्गों को शिक्षित करने के मिशन में जुट गए। उनका ज़ोर विशेषकर दलितों और महिलाओं को शिक्षित करने पर था। लड़कियों के अपने तीन स्कूलों के लिए जोतीराव फुले ‘दक्षिणा कोष’ से मदद हासिल करने में सफल रहे। ‘दक्षिणा कोष’ की स्थापना पेशवाओं द्वारा ब्राह्मणवादी ग्रंथों का अध्ययन-अध्यापन प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। शुरुआत में औपनिवेशिक शासकों ने भी पंरपरा का पालन करते हुए इस कोष का उपयोग ब्राह्मणवादी संस्कृत के ज्ञान के प्रसार के लिए किया। मगर बाद में हुए विरोध, जिसमें फुले सबसे आगे थे, के चलते उन्हें इस कोष को सभी के लिए खोलना पड़ा।
हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष अपने अविस्मरणीय संबोधन में फुले ने इस बात पर जोर दिया कि औपनिवेशिक सरकार को अपनी शिक्षा नीति का फोकस ब्राह्मणों को शिक्षा प्रदान करने से हटाकर शूद्र-अतिशूद्रों की शिक्षा पर केंद्रित करना होगा। दूसरे शब्दों में, उन्हें पारंपरिक दमनकर्ताओं को शिक्षित करने की बजाए पारंपरिक दमितों को शिक्षित करना होगा। फुले ने तर्क दिया कि “उच्च और धनी वर्गों का सरकारी खजाने भरने में न के बराबर योगदान होता है।” (फुले, 1884) फुले ने आयोग से पूछा कि क्या ब्राह्मणों ने कभी उस शिक्षा, जो उन्हें अंग्रेजों से हासिल होती है, को निम्न वर्गों को हस्तांतरित किया? “या फिर वे अपने ज्ञान को एक व्यक्तिगत उपहार मानकर अपने तक सीमित रखे रहे क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि गंवार और अज्ञानी लोगों के संपर्क में आने से उनका ज्ञान कलुषित हो जाएगा?” (वही) फुले ने यह भी दिखाया कि राज्य की नीति और शिक्षा प्रदान करने के तरीके किस तरह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि अध्यापक अलग-अलग जातियों के बच्चों के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यापकों की नियुक्ति में बहुलता होनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए जो अध्यापन को सत्य की खोज की कवायद के रूप में देखते हैं। फुले जो कह रहे थे, वह यह था कि नियुक्त किए जाने वाले अधिकांश अध्यापक ब्राह्मण होते हैं, जो अपने आपको उच्च समझते हैं और अपनी जातिगत शुद्धता की धारणा से आसक्त रहते हैं। ऐसे में वे अन्य जातियों के विद्यार्थियों के साथ घुल-मिल नहीं पाते। फुले ने यह मांग भी की कि स्कूलों में मराठी पढ़ाने के लिए मोडी व बालबोध लिपियों का इस्तेमाल किया जाए। उनका तर्क था कि भाषा अक्सर वंचित वर्गों के शिक्षा से दूर हो जाने का कारण बन जाती है। फुले ने सरकार से अपील की कि वह विद्यमान स्कूलों में जाति आधारित भेदभाव को ध्यान में रखते हुए अछूतों के लिए और स्कूल खोले और श्रमजीवी जातियों को वजीफे दे ताकि वे स्कूलों में दाखिला लेकर पढ़ाई करने के प्रति प्रवृत्त हों। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। (वही)
फुले का संघर्ष और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई पर उसका प्रभाव
भारतीय स्वाधीनता संग्राम को औपनिवेशिक अंग्रेजों और भारतीयों के बीच संघर्ष के रूप में परिभाषित किया जाता है। मगर इस संघर्ष के यह स्वरूप ग्रहण करने के पहले और इस संघर्ष के समानांतर भी एक दूसरा संघर्ष चलता रहा। यह संघर्ष दमितों और औपनिवेशिक प्रणाली के बीच था। पारंपारिक जाति-व्यवस्था औपनिवेशिक ढांचे का भाग बना दी गई थी। फुले के जीवन और कार्यों से पता चलता है कि जब तक जातिवाद, ज़मींदारी प्रथा और अन्य वर्चस्ववादी प्रणालियों के खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष नहीं किया जाता है तब तक पूर्ण स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती।
फुले ने शिक्षा का इस्तेमाल सामाजिक और आर्थिक अन्याय के प्रतिरोध के लिए किया। शिक्षा के मुद्दे ने दमितों में एकता स्थापित की और शिक्षा ने उनकी चेतना को आकार दिया। शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की मांग एक ऐसा हथौड़ा साबित हुई जिसने अंग्रेजों और उच्च जातियों के गठजोड़ को छिन्न-भिन्न कर दिया। शिक्षा के जरिए फुले ने आमजनों को जातिगत, लैंगिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ गोलबंद किया।
संदर्भ :
अल्थुसेयेर, लुई, ‘आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजीकल स्टेट एपरेटसेस’, लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर एस्सेज़ से, न्यूयार्क : मंथली रिव्यु प्रेस, 1971
देशपांडे, जी.पी., संपादक, सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ़ जोतीराव फुले, नई दिल्ली : लेफ्टवर्ड बुक्स, 2002
गुप्ता, विकास, रमा कान्त अग्निहोत्री एवं मिनाति पांडा, एजुकेशन एंड इनइक्वलिटी: हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी ट्रेजेकटरीज, हैदराबाद : ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2021
कुमार, अरुण, “द ‘अनटचेबिल स्कूल’: अमेरिकन मिशनरीज, हिन्दू सोशल रिफॉर्मर्स एंड दि एजुकेशनल ड्रीम्स ऑफ़ लेबरिंग दलित्स इन कोलोनियल नार्थ इंडिया”, साउथ एशिया : जर्नल ऑफ़ साउथ एशियाई स्टडीज 42, अंक 5 (2019): 823-844, https://doi.org/10.1080/00856401.2019.1653162.
नंबीसन, गीता बी, “कास्ट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ़ दि अर्ली ‘पब्लिक’ इन स्कूलिंग : दलित स्ट्रगल फॉर एन इक्विटेबल एजुकेशन”, कंटेम्पररी एजुकेशन डायलाग 17, अंक 2 (2020): 126-154, https://doi.org/10.1177/0973184920946966.
ऑम्वेट, गेल, “द रेलेवेंस ऑफ़ महात्मा फुले इन टुडेज वर्ल्ड: व्हाई द ‘अदर महात्मा’ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन गांधी”. कंटेम्पररी वोइस ऑफ़ दलित 4, अंक 1 (2011): 7-18, https://doi.org/10.1177/0974354520110102.
फुले, जोतीराव, “मेमोरियल एड्रेस्ड टू द एजुकेशन कमीशन”, राउंड टेबल इंडिया, 20 जून 2012, मूल अभिलेख: एजुकेशन कमीशन, बॉम्बे, खंड दो (कलकत्ता: सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ़ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, 1884), 140-145, 3 सितंबर 2024 को देखें https://www.roundtableindia.co.in/memorial-addressed-to-the-education-commission/
रेगे, शर्मीला, “एजुकेशन एज़ ‘तृतीय रत्न’: टूवर्ड्स फुले-आंबेडकराइट फेमिनिस्ट पीडेगोजी प्रैक्टिस”, इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली 45, अंक 44/45 (अक्टूबर 30 – नवंबर 12, 2010): 88-98, https://www.jstor.org/stable/20787534.
त्सुरेनेव, जना व सुमीत म्हासकर, “वेक अप फॉर एजुकेशन: कोलोनिअलिज्म, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बिगिनिंग्स ऑफ़ दि एंटी-कास्ट मूवमेंट इन इंडिया”, पीडेगोजीका हिस्टोरिका 59, अंक 4 (2021): 630-648, https://doi.org/10.1080/00309230.2021.1920986.
(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in