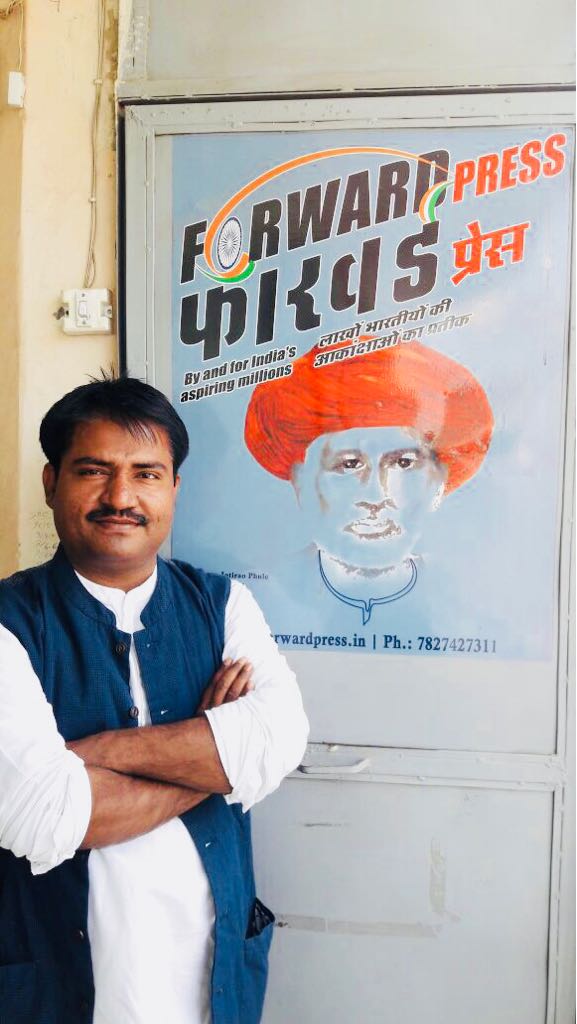23 दिसंबर, 1971 बिहार के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए वह ऐतिहासिक तारीख है जब राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। उस समय सूबे में भोला पासवान शास्त्री कांग्रेसी सरकार के मुखिया थे। इस आयोग के अध्यक्ष थे मुंगेरीलाल। इस आयोग ने 23 जनवरी, 1976 को अपना तीसरा प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया। इस आयोग ने सरकार के अधीन विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए अलग-अलग आरक्षण के कोटे का सुझाव दिया। यह इस तरह था कि ग्रुप ‘ए’ में 25 प्रतिशत, ग्रुप ‘बी’ में 33.13 प्रतिशत, ग्रुप ‘सी’ व ग्रुप ‘डी’ में 40-40 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग के सदस्यों को मिले। ऐसा संभवत: इसलिए किया गया ताकि पिछड़े वर्ग के सदस्य केवल ग्रुप ‘सी’ और ग्रुप ‘डी’ की नौकरियों तक सीमित न रह जाएं तथा ग्रुप ‘ए’ और ग्रुप ‘बी’ की नौकरियों में भी उनका समुचित प्रतिनिधित्व हो।
आयोग की इसी अनुशंसा को बाद में कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में संशोधित रूप में लागू किया। इसके तहत सभी श्रेणी की नौकरियों में अति पिछड़ी जातियों को 12 प्रतिशत, पिछड़ी जातियों को 8 प्रतिशत, महिलाओं को 3 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके बावजूद ऊंची जातियों द्वारा बवाल काटा गया और कर्पूरी ठाकुर के लिए सार्वजनिक तौर पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। आरक्षण को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए। यहां तक कहा गया कि यह मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं।
जबकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आरक्षण के संबंध में उल्लेखित किया कि “सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े और अनपढ़ लोगों के हित में प्रावधान किया जाना चाहिए भले ही उससे उन्नत नागरिकों के अधिकार पर कुछ आघात क्यों न पहुंचता हो। स्पष्टत: यह प्रावधान उचित समझा गया कि जनतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सभी नागरिक उन्नत हों और कोई पिछड़ा न रहे ताकि समान मौका सबों को मिल सके और यदि इस अच्छे एवं निष्कलंक विचार के प्रतिपादन के लिए कुछ अंश तक उन्नत वर्गों के हितों की गारंटी पर हस्तक्षेप होता है तो यह अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस महान देश की उन्नति के लिए उन विशाल समुदायों को आगे बढ़ाना है जो आजतक पिछड़े हैं और शोषित होते रहे हैं।” (पिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार सरकार, तृतीय प्रतिवेदन, पृष्ठ 16)
जब इस रिपोर्ट को लागू किया जा रहा था तब पिछड़े वर्ग की पहचान के सवाल पर भी सवाल उठाए गए। यहां तक कि आयोग के ही एक सदस्य यमुना प्रसाद सिंह ने यह सवाल उठाया और आय के आधार पर पिछड़ापन निर्धारित करने की बात कही। लेकिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ शब्दों में लिखा कि “सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा कौन है, इसे निर्धारित करने के लिए हर समय यह याद रखना पड़ेगा कि हमारे समाज के शिकंजे क्या हैं। बिना समाज का निरूपण किये इस प्रश्न का सही हल हो नहीं सकता। यदि समाज में समानता रहती या यदि इसके द्वारा कोई शोषण नहीं होता रहता तो ऐसे उपबंधों की आवश्यकता ही नहीं रहती। हमारे समाज में वर्ग हैं, जिन्हें वर्ण रूप में जाना जा सकता है। जातियां हैं, जो इन्हीं वर्णों में विभाजित हैं। समाज के सभी वर्णों का अस्तित्व हमारे धर्म के द्वारा प्रतिपादित हैं, जिनमें उनके कर्म और गुण का उल्लेख है और उनके द्वारा कार्य तथा अधिकार प्रतिपादित होते हैं। बहुत से धर्मावलंबी इस देश में हैं, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था उन समुदायों के द्वारा मान्य हैं, जो भारत में असंख्य हैं और जिनका उत्थान या पतन इस देश का उत्थान या पतन है। यह कहना कि इन समुदायों ने अपने आपको कार्य के निष्पादन के हेतु जातियों और वर्णों में विभाजित कर लिया है, भ्रामक है और असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश है। यह तो धर्म और अध्यात्म के द्वारा प्रतिपादित है और ये संस्कार गिराने वाले हैं। हिंदू धर्म भी मनुस्मृति पर ही आधारित है। इसलिए ऐसे समाज के उत्थान के लिए उन जातियों का उत्थान करना आवश्यक है, जिन्हें शूद्र की उपाधि देकर युग-युग से शोषण किया जा रहा है। आयोग के विचार में इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और इस प्रश्न का हल ढूंढ़ने के लिए इस सच्चाई को हर समय सामने रखना पड़ेगा और इस तरह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को ढूंढ़ने के लिए आय की बात उठा देना भ्रमित कर देना है। इसके लिए तो जाति को आधार मानना ही पड़ेगा।” (वही)
खैर, मुंगेरीलाल की अध्यक्षता वाले इस पिछड़ा वर्ग आयोग को केवल आरक्षण के सवाल तक सीमित करके देखा जाता रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इस आयोग ने पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों, जिनमें मुख्य रूप से अति पिछड़ी जातियों के लोगों के चौमुखी विकास के लिए अपने सुझाव दिये। आयोग की निगाह में छोटे किसान भी थे, जिनके लिए आयोग ने लिखा कि “व्यक्तिगत रूप से अन्य पिछड़ी जाति के गरीब किसानों को कृषि सुधार के लिए 1000 रुपए तक अनुदान देने की व्यवस्था की जाय। हल, बैल, खेती के औजार तथा उन्नत किस्म के बीज आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाय। अगर अनुदान ग्रहीता कुछ काम करके दिखाएं तो उन्हें नाममात्र के ब्याज पर जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था की जाए।” (वही, 44)
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जातियों के हितों को ध्यान में रखकर कहा कि “अत्यंत पिछड़ी जाति के सदस्यों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए यह भी आवश्यक है कि उन्हें दुधारू पशु – गाय अथवा भैंस – सरकार की ओर से दी जाय। इस सुविधा का दुरुपयोग न हो सके, इसके लिए यह उचित होगा कि अभ्यर्थियों को ये पशु प्रखंड विकास समिति की बैठकों या पंचायतों की बैठकों में जन-साधारण के सामने दी जाय। उन्हें मुर्गी, बकरी इत्यादि पालने के लिये एवं मत्स्य उत्पादन के लिए भी अनुदान दिया जाय। (वही, पृष्ठ 45)

इसके अलावा आयोग ने कई जातियों का उल्लेख करते हुए उनके पारंपरिक पेशों और दुश्वारियों का जिक्र किया। साथ ही आयोग ने उनकी स्थिति में सुधार के लिए सुझाव भी दिये। मसलन, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल मल्लाह जाति का उल्लेख करते हुए आयोग ने लिखा कि “मल्लाह समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पंचवर्षीय योजनांतर्गत सरकार द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समितियां एवं नाव यातायात सहयोग समितियां निबंधित की गई हैं। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ मछलीवाला जल कर और मखानावाला जल कर की बंदोबस्त करने के लिए तथा नाव यातायात सहयोग समितियों के साथ घाट बंदोबस्त करने के लिए सरकारी आदेश जिन परिपत्रों के द्वारा निर्गत किया गया है, उन परिपत्रों को बिहार भूमि सुधार अधिनियम में अंकित नहीं किया गया है। अत: इन परिपत्रों को कानूनीरूप नहीं देने के कारण न्यायालयों में इन परिषदों की मान्यता नहीं होती है। आयोग को बताया गया है कि फलत: जल कर, मखाना कर एवं घाट की बंदोबस्ती प्राप्त करने में उक्त समितियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।” (वही, 46)
लोहारों के बारे में आयोग के मुताबिक, “इस जाति के लोग आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। इनके पास जमीन का अभाव है। इनका मुख्य पेशा लोहे के विभिन्न औजारों को बनाना है। आयोग यह सिफारिश करता है कि इस जाति के लोगों को अपने पारंपरिक रोजगार को समुन्नत बनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, मशीनरी और वित्तीय सहायता दी जाए।” (वही)
नाई जाति के बारे में आयोग ने लिखा कि “इस जाति के पारंपरिक पेशे की अनिवार्यता सभी के लिए है। शहरों में आज सैलून खोले जा रहे हैं, जिनमें दाढ़ी हजामत बनाने का काम तो इस जाति के लोग करते हैं, सैलून का मालिक प्राय: दूसरा होता है। नतीजा यह होता है कि नाई समाज के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए शहरों आदि में नाई समाज के लोग अपना सैलून खुद खोल सकें, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता व कर्ज आदि उपलब्ध कराए।” (वही, पृष्ठ 47)
कुम्हारों के विषय में आयोग ने विस्तार से लिखा कि “भारतीय सभ्यता और समाज में इस जाति की अहम भूमिका रही है। ये विभिन्न बर्तन, गृह निर्माण के लिए विशेष किस्म की ईंटें आदि बनाते हैं। इसी से इनका किसी तरह जीवन निर्वाह होता है। इस प्रगतिशील और वैज्ञानिक युग में इस राज्य के अधिकांश घर इनके द्वारा बनाए गए खप्पड़ों से छाए हैं। जमींदारी उन्मूलन के पहले इन्हें मिट्टी, बालू या कच्ची मिट्टी के बर्तनों को पकाने आदि में कोई कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन अब गांवों में चप्पा-चप्पा जमीन पर खेती होने या सभी जमीन स्थानीय प्रखंड या जिला पंचायत के अंतर्गत आ जाने के बाद इन जातियों को बड़ी कठिनाई होती है। सरकार से सिफारिश है कि सरकारी जमीन से इन्हें मिट्टी, बालू आदि बगैर सार्वजनिक हित को हानि पहुंचाए लेते रहने का अधिकार होना चाहिए। समय-समय पर इस कला में निपुण और दक्ष कलाकारों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन देना चाहिए। चूंकि अपने कामों के लिए आए दिन ये कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, इसलिए उन्हें कम ब्याज पर सरकारी ऋण देने का प्रबंध किया जाय। साथ ही अनुदान की भी व्यवस्था की जाए।” (वही)
इसी तरह गरेड़िया जाति के बारे में आयोग ने लिखा कि “इस जाति का मुख्य पेशा भेड़ पालना एवं कंबल बनाना है। इनकी शिकायत है कि भेड़ पालने के लिए चारागाह की कोई व्यवस्था नहीं है। दिनों-दिन परती जमीन आबाद होती जा रही है। उनका सुझाव है कि सरकार को चाहिए कि वन विभाग के अधिकारी द्वारा चारागाह की व्यवस्था कराए ताकि भेड़ पालने में लोगों को सुविधा हो। भेड़ों की नस्ल-सुधार के लिए विदेश से उन्नत नस्ल के भेड़ मंगाकर भेड़ पालनेवालों को दिया जाए। भेड़ों को कई तरह की संक्रामक बीमारियां होती हैं, जिनसे अधिकांश की मृत्यु कुछ ही दिनों में हो जाती है। इसके लिए भी सरकार को चाहिए कि भेड़ पालनेवालों को चिकित्सकीय प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि ये स्वयं भेड़ों का इलाज कर सकें। भेड़ों से ऊन निकाल कर उनका कंबल आदि का निर्माण इस जाति के लोगों का मुख्य पेशा है। आयोग सिफारिश करता है कि ये अपनी पारंपरिक कला का विकास कर सकें और दुशाला व कालीन तैयार कर सकें, इसके लिए सरकार इन्हें प्रशिक्षण दिलाए, ताकि ये बढ़िया माल और अन्य उत्पादन तैयार कर सकें और और अपनी आर्थिक दशा सुधार सकें। आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य में भेड़-ऊन विकास बोर्ड का गठन हो।” (वही, पृष्ठ 47-48)
आयोग ने सोनार जाति के बारे में लिखा कि “सोनार (स्वर्णकार) पिछड़े वर्ग में प्रतिष्ठित जाति मानी जाती है। सोना, चांदी, तांबा आदि का गरीब से लेकर अमीर तक के लिए मामूली मूल्य से लेकर बहुमूल्य गहना और जेवर बनाने का कार्य प्राय: ये किया करते हैं। इन सब धातुओं की खरीद-बिक्री ही इनका मुख्य पेशा है। यह जाति किसी-न-किसी रूप में अपने हुनर के माध्यम से समाज की सेवा करती है और अपना जीविका उपार्जन करती है। प्राचीन काल से आज तक राजा, महाराजा, बादशाह, नवाब तथा गरीब से गरीब की झोपड़ी तक में ये अपनी कारीगरी के माध्यम से अपनी सेवा देते आ रहे हैं। आज भी पुराने राजा, महाराजाओं, नवाबों के खजाने से जो कुछ भारत सरकार को प्राप्त हुआ है, उनमें इस जाति के सर्वोत्तम कारीगरी के रूप में जेवर आदि देखे जा सकते हैं। इस जाति ने विभिन्न संप्रदायों के महापुरुषों, देवी-देवताओं आदि की धातु की मूर्ति बनाकर भारतीय प्राचीन और अर्वाचीन सभ्यता को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज भी इसका ज्वलंत उदाहरण भिन्न-भिन्न देश के अजायब घरों में, मंदिरों, मठों या दर्शनीय स्थानों में देखे जा सकते हैं। इन सब के होते हुए भी इस जाति के अधिकांश लोगों की आर्थिक, समाजिक और शैक्षणिक स्थिति दयनीय है। इनमें से एक्के-दुक्के ही सुखी-संपन्न हैं। अधिकारी अपनी कारीगरी को बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। जब से गोल्ड कंट्रोल एक्ट इस देश में लागू हुआ है और शुद्ध सोना के गहने पर पाबंदी लग गई है तब से देश को तो जरूर लाभ हुआ है, पर सोनारी पेशे में लगे लाखों कारीगरों का जीवन कष्टमय हो गया है। इस स्थिति को समझकर सरकार ने इन विस्थापित सोनार कारीगरों को सहायता पहुंचाने के लिए, इनके बच्चों को छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा देना प्रारंभ किया था और साथ ही कुछ छोटे-मोटे धंधा भी देने का निश्चय किया था। इस पर भी इनकी हालत सोचनीय और दयनीय है। इसलिए इनके प्राचीन और अर्वाचीन सेवाओं को देखते हुए और इनकी सरकारी नौकरी या दूसरे रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए।” (वही, पृष्ठ 48-49)
मुंगेरीलाल आयोग की दृष्टि खेतिहर मजदूरों के ऊपर भी पड़ी। रिपोर्ट में लिखा गया कि “इनके लिए आयोग यह भी सुझाव देना चाहता है कि ग्रामीण खेतिहर मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन व समाधान के लिए एक परिषद का गठन किया जाए। इस परिषद में आदिवासी कल्याण शोध संस्थान के एक पदाधिकारी भी रखे जाएं जो इस संबंध में आवश्यक शोध करें।” (वही, पृष्ठ 49) जाहिर तौर पर आयोग के सदस्य इस बात से वाकिफ थे कि खेतिहर मजदूरों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के अलावा अनुसूचित जनजातियों के लोग भी शामिल होते हैं।
इतना ही नहीं, सभी गरीबों के पास रोजगार हो, आयोग ने लिखा कि “आयोग की यह भी जोरदार सिफारिश है कि नियोजन गारंटी स्कीम जिसका उल्लेख प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तावना में किया गया है चालू की जाए, जिससे कि अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को इस स्कीम से लाभ मिल सके।” (वही)
जिस आयोग की अनुशंसाओं को ऊंची जातियों के द्वारा हसीन सपने कहकर उपहास उड़ाया गया, उसकी संवेदनशीलता का उदाहरण यह है कि उसकी दृष्टि में रिक्शा चलानेवाले भी थे। आयोग ने लिखा– “रिक्शा चलाने के धंधे में अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य लगे रहते हैं। बड़े शहरों में जो व्यक्ति इस धंधे में रहते हैं वे दूर-दूर के गांवों से आते हैं। इसके लिए शहरों में किराए के मकान लेकर रहना असंभव है। इनके आवास की समस्या विकट रूप की है। इनकी कठिनाई का अनुमान सहज में किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कारगर कदम उठाए। आयोग का सुझाव है कि बड़े-बड़े शहरो में इनके लिए दो-तीन मंजिला मकान का निर्माण किया जाए्, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक-एक कमरा की व्यवस्था रहे। मकान में कैंटीन का भी प्रबंध किया जाए। नाममात्र का किराया लेकर रिक्शा चलानेवाले व्यक्ति को उसमें रहने की अनुमति दी जाए।”
बहरहाल, वास्तविकता यही है कि मुंगेरीलाल आयोग के अन्य अनुशंसाओं पर न तो विस्तार से चर्चा की गई है और न ही आज तक उनके ऊपर अमल किया गया है।
(संपादन : राजन/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in