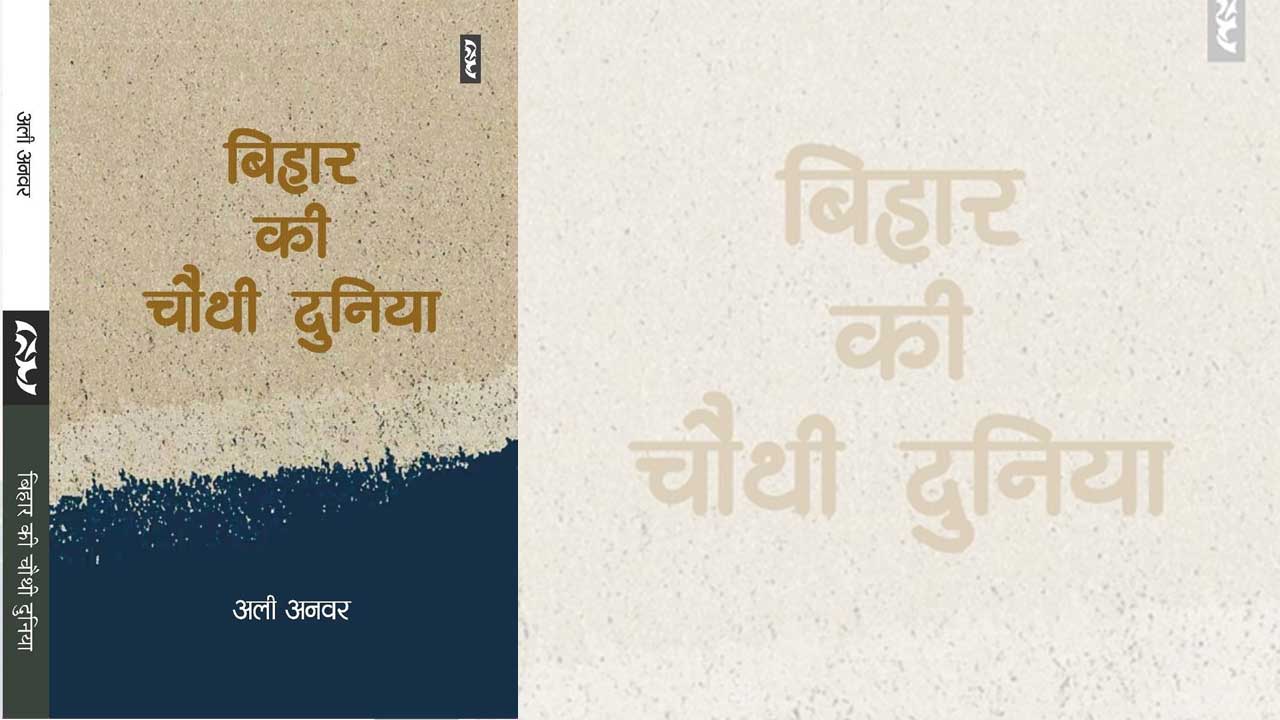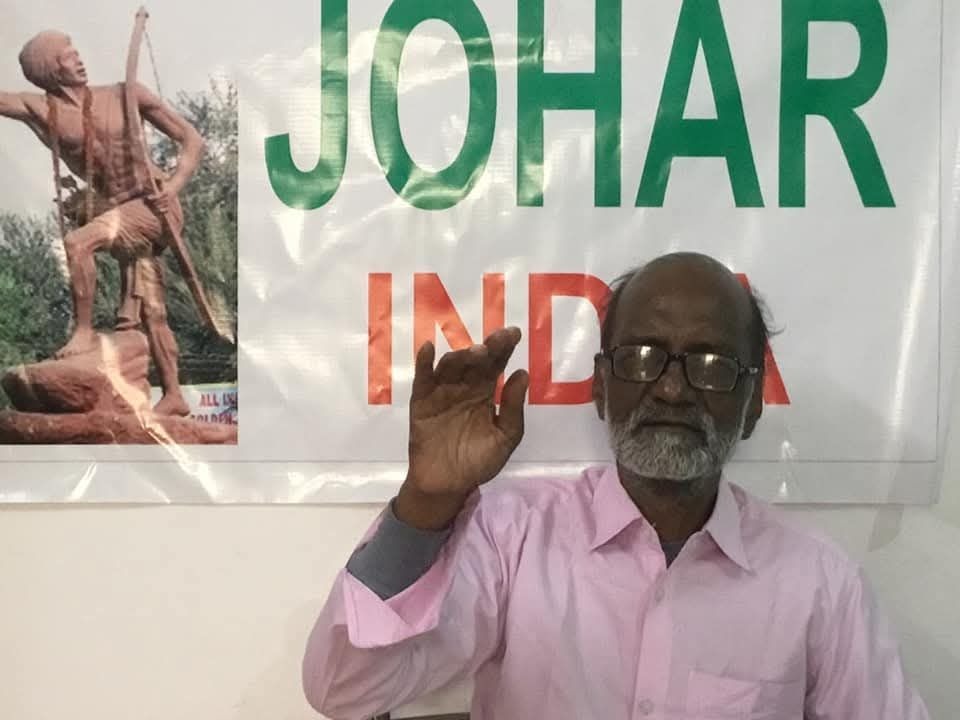संसदीय चुनाव सत्ता पर नियंत्रण का औजार है। यह उस सत्ता को भी बनाए रखने का जरिया है जो सदियों से समाज की सत्ता पर काबिज है। यह उस सत्ता को भी नियंत्रित करने का जरिया है जिसकी शक्ल संविधान की किताब और लोकतांत्रिक विचार के चेहरे से मिलती-जुलती है।
बिहार के चुनाव नतीजों को किस नजरिये से विश्लेषण करें? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक नजरिया संसदीय चुनाव की प्रक्रिया, संविधान की भावना और संसदीय परिपाटी है। दूसरा नजरिया संविधान पूर्व की सामाजिक, राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के तंत्र और तौर तरीके हैं। तीसरा नजरिया दोनों को गड्डमड्ड करके सत्ता के पूरे तंत्र की चुनाव में भूमिका की पड़ताल हो सकती है।
संसदीय तंत्र और तौर तरीकों का उल्लंघन
बिहार में बीस वर्षों से सरकार चलाने वाले एनडीए गठबंधन को 2010 की तरह 243 में दो सौ से ज्यादा सीटें 2025 में भी हासिल हुई हैं। सरकार चलाने वाले दलों ने अपने कार्यक्रमों व नीतियों से किस तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं कि गठबंधन को पिछले चुनाव के मुकाबले वोट में दस प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा हो गया है? यह संसदीय प्रक्रिया का सहज प्रश्न है। संसदीय संस्कृति में यह देखा गया है कि लंबे समय तक सरकार में रहने वाली पार्टियों की लोकप्रियता घटती जाती है, जिसका फायदा विपक्ष को मिलता है। लेकिन बिहार के चुनाव नतीजों को इस कसौटी पर देखना पुराने समय की भाषा है। चुनाव नतीजों को यह देखने का पुराना नजरिया है कि चुनाव पूर्व सभाओं में लोगों की भीड़ किस तरह जमा होती है और वह किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही है।
वोटो से हार-जीत के नहीं, पूरे चुनावी तौर-तरीकों को बदलने के नतीजे
यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ते हैं और न ही मतदाताओं को स्वतंत्र एवं बिना किसी दबाव में मतदान करने के अधिकार की भावना नतीजों में शामिल होती है। चुनाव पूरा सत्ता तंत्र लड़ता है और मतदाताओं का बहुमत हिस्सा अच्छे या बुरे गवर्नेंस के फैसले के साथ मतदान नहीं करता है। वह किसी-न-किसी तरह की घेराबंदी के दबाव में उम्मीदवार के लिए मतदान करता है।
बिहार में चुनावी तौर तरीकों के तंत्र को देखने की शुरुआत चुनाव आयोग के मतदाता सूची के गहन परीक्षण से की जा सकती है। चुनाव की तिथि की पूर्वसंध्या में आयोग ने गहन परीक्षण का कार्यक्रम लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में शुद्धिकरण के नाम पर पुराने मतदाताओं को एक बड़ी संख्या में बाहर करना था। संविधान लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं की कतार को लंबा करने की भावना से खड़ा किया गया है। दरअसल, मतदाताओं को बाहर करना नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने का इरादा इसमें छिपा दिखता है। चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां मतदाताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को ले जाती हैं। लेकिन आयोग के इस फैसले से दो काम हुए।
पहला तो विपक्षी पार्टियों के लिए मतदाता सूची ही मुद्दा बन गया। सत्ता के लिए लाइन में खड़ी पार्टियों को संभवत: यह भनक नहीं लगी कि मतदाता सूची के प्रकाशित होते ही मतदाता सूची चुनाव के लिए मुद्दे के रूप में खड़ा नहीं हो सकता लेकिन तब तक वे मतदान के दरवाजे तक पहुंच चुके होंगे। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों की तलाश, स्थानीय स्तर पर आपस की उठापटक के तार को समझने और पोस्टर में हाथ जोड़कर खड़े होने के लिए भी वक्त की किल्लत होगी।
दूसरा, आयोग के फैसले के बाद विपक्ष के माने जाने वाले मतदाताओं में असुरक्षा की भावना घर कर सकती है। असुरक्षा की भावना अधिकार की चेतना को कमजोर कर देती है जबकि वह चेतना संसदीय चुनाव में विपक्ष के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है।
इसके अलावा नई आर्थिक नीतियों के आने के साथ देशभर में खड़ा किया गया स्वयं सहायता समूहाें के पूरे तंत्र की भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में सुनिश्चित कर दी गई। यह बिल्कुल नया प्रयोग है। आर्थिक निर्भरता किसी भी कमजोर आर्थिक वर्ग के समूह के लिए किसी विपरीत फैसले के लिए बेहद चुनौती पूर्ण होती है। इस वर्ग में अनिश्चय का असुरक्षा बोध होता है। इस वर्ग पर पहरेदारी की उस दौर में कल्पना की जा सकती है जबकि पन्ना प्रमुख का एक सांगठनिक ढांचा तैयार किया गया है। पन्ना प्रमुख सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की देन है। भाजपा मतदाता सूची के शुद्धिकरण को 1990 के दौर से चिह्नित कर उसके अनुरूप एक ढांचा खड़ा करने के लिए सक्रिय रही है। एक एक मतदाता पर नजर, उसके नतीजों को चुनाव से पहले ही स्पष्ट कर देती है। दूसरी तरफ संसदीय संस्कृति में सभाओं और सड़कों पर भीड़ की स्थिति से नतीजे देखे जाने के भोथरे औजार को विश्लेषक इस्तेमाल करते है। क्या बिहार में जिस तरह के नतीजे आए, वे छत्तीसगढ़ में नहीं थे? पिछले कितने चुनावों से वे तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसका अध्ययन भी संभवत: बिहार के नतीजों के बाद किए जाए।
संक्षेप में कहा जाए कि राजनीतिक दलों के बीच बराबरी के स्तर पर मतदान के दिन बीत गए है। गहरी असमान स्थितियों में चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच असमानता है और उम्मीदवारों एवं मतदाताओं के बीच गहरी असमानता है। दूसरा संविधान में बराबरी लाने के लिए प्राप्त अधिकार वाले मतदाता की कतार की जगह धर्म का भक्त, धार्मिक सशक्तिकरण को महसूस करने वाला प्रतिनिधि, पांच किलो राशन को दान-पुण्य मानने वाला गरीब और सामाजिक स्तर पर उत्पीड़न से क्षुब्ध खड़े लोगों की कतार है, जो कि गड़ेरिये से ज्यादा कसाई पर भरोसा करने लगता है। इस तरह की कतार को लंबी कर देने के क्या नतीजे निकल सकते हैं? अच्छी और बुरी सरकार का भेद करने की भाषा ही उसे अपरिचित लगती है।

बिहार में तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं की सहमति थी कि मतदान के लिए लगने वाली लंबी कतार में लालच के साथ लोलुपता की संस्कृति का दबाव बनाया जाए। खाते इसीलिए खुलवाए गए ताकि ऐन मौके पर अधिकार खरीदे जा सके। दस-दस हजार रुपए चुनाव की पूर्वसंध्या पर भेजे गए। पहले के चुनावों में हम यह सुना करते थे कि शहर का कोई रईसजादा शहर के सबसे बुरी हालात में रहने वाली आबादी के बीच नगरपालिका में वार्ड का नुमांइदा चुने जाने के लिए मतदान की पूर्व रात शराब की टंकी खोल देता था और नोटों की गड्डियां बिखेर देता था। अब बिहार जैसे राज्य का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह के बुरे हालात में खड़ा कर दिया गया है। बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा है लेकिन अमीरी और अमीरों की नीति वाली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनी जाती है।
चुनावी तौर तरीकों का तंत्र और भी गहरा है। लेकिन उसके उल्लेख करने का अवकाश यहां नहीं है। लिहाजा दूसरे पहलू पर बातचीत कर सकते हैं।
क्या विपक्ष यह मानकर चल रहा था कि उसे तो किसी भी हालत में सत्ता के खिलाफ नाराजगी और गुस्से का लाभ मिलेगा? यह पुरानी किस्म की समझ है। नई राजनीतिक संस्कृति में यह जरूरी नहीं। बिहार में तो 2025 में सरकार विरोध भावनाओं के लिए 1990 से 2005 के शासनकाल का सत्ताधारी खेमे ने इस्तेमाल किया। लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासनकाल को सनातनी भाषा में ‘जंगल राज’ के रूप में प्रचारित किया गया और वह लालू-राबड़ी के बेटे तेजस्वी की राजनीति पर लाद दिया गया।
विपक्ष के सामने यह संकट दिखता है कि वह किस तरह से विपक्ष दिखे। वह संसदीय विपक्ष दिखना चाहता है या फिर सत्ता भर के लिए विपक्ष दिखना चाहता है। वह उसी तरह की संस्कृति का पोषक है जो कि संगठन के अभाव में सत्ता से बदलाव का सपना दिखाता है। इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है।
पहली बात तो विपक्ष क्या उन चुनावी तौर-तरीकों के तंत्र को संवैधानिक लोकतंत्र के लिए चुनौती मान रहा है?
बिहार में मोटेतौर पर राजनीतिक दलों की मतदान करने वालों के बीच क्या स्थिति थी? यहां जानबूझकर मतदाता का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्हें मतदान करने वाले ‘लोग’ के रूप में संबोधित किया गया है। संविधान पूर्व की पुरानी सत्ता और संविधान के बाद की नई सत्ता की भूमिका को समझने के लिए यह अंतर जरूरी है। मतदान करने वालों के बीच जातीय स्तर पर एक विभाजन है। एक तरफ भाजपा है, जिसके साथ समाज का वह हिस्सा पूरी ताकत से लगा है जो कि वर्चस्ववादी माना जाता है और सवर्ण के रूप में संबोधित किया जाता है। लेकिन उसकी संख्या मतदान की जो प्रणाली है, उसमें बहुमत पाने तक नहीं है। वह हिंदुत्व में अपनी गति देखता है। भारतीय समाज में वर्चस्ववाद का हथियार जाति कलह को कायम रखना है। संसदीय राजनीति में वर्चस्ववाद उस कलह को वोट में तब्दील करने की रणनीति अख्तियार करता है। बिहार में भाजपा सत्ता की राजनीति का वैचारिक नेतृत्व करती है। सत्ता के लिए उसे अपने आधार में जो जोड़ना है वह उन जातियों के श्रमिकों का विशाल समूह का हिस्सा है, जो इतिहास में वर्चस्ववाद के विरोध में खड़ी रही है।
संवैधानिक भाषा में इन समूहों को हम अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान करते हैं। इनके लिए पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी सामान्य शब्द हैं। इनके बीच एक-दूसरे के विरुद्ध रोजमर्रे के विवाद और बहस हैं। लेकिन ऐतिहासिक और वैचारिक विरोध वर्चस्वाद से रहा है। यह संसदीय चुनाव का जादूई पहलू है कि तात्कालिक शिकायतों का तात्कालिक समाधान करने का एक कामयाब भ्रम खड़ा करता है। पिछड़ों की दो मजबूत जातियों में एक-दूसरे के खिलाफ की भावनाओं में एक को अपने पक्ष में करना, इसी तरह दलितों की कोई मजबूत या संख्या में अधिक लाचारी के हालात वाली जाति को शामिल करना चुनावी कामयाबी का एक खुला मंत्र है।
कुल मिलाकर देखें तो सत्ताधारी दलों के पास अपने पक्ष में जोड़ने के लिए मतदाता सूची के परीक्षण से लेकर आर्थिक स्रोत और जातिगत भावनाओं का बहाव और धार्मिकता को लेकर आक्रमकता थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष था जो एक ही सामाजिक आधार के बीच आपस में ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने की प्रतिस्पर्धा कर रहा था। सामाजिक न्याय की वैचारिकी का पोस्टर उसने बनाया, लेकिन जातीय गणित उसका औजार बना रहा। बैनर राष्ट्रीय जनता दल का था, लेकिन चुनाव तेजस्वी यादव लड़ और लड़वा रहे थे। कांग्रेस अपना आधार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि उसके पास कोई अपना आधार नहीं है। राहुल गांधी के प्रति एक आकर्षण है। वामपंथी तभी मजबूत दिखते हैं जब विपक्ष की पार्टियां मजबूती हासिल कर लेती है। इंडिया गठबंधन में सत्ताधारी दलों को सत्ता से हटाने के प्रतिबद्ध होने का तालमेल ही नहीं दिखा और न ही भीड़ को मतदान केंद्रों तक जोड़े रखने और एक-एक वोट के लिए प्रेरित करने वाला कोई सूत्र ही देखा गया। केवल तेजस्वी का ब्रांड चुनाव मैदान में चमकता दिखा। सत्ताधारी दल जिन्हें अपने साथ जिन भी कारणों से जोड़ रहे थे उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन किन रास्तों से?
मसलन, पक्की नौकरी का वादा और दस हजार रुपए के बदले तीस हजार रुपए का वादा। बिहार में क्या केवल आर्थिक बेहतरी के आश्वासन पर चुनाव लडा जा सकता है? उस राजनीतिक संस्कृति के बीच जिसमें कहीं भी दूर-दूर तक आश्वासान को पूरा करने के चिह्न नहीं दिखते हैं। बिहार के चुनाव नतीजे बताते है कि महागठबंधन तो 37 प्रतिशत मत पाकर अपनी पुरानी स्थिति को बनाए रखा है। यानी उसकी कोई हार नहीं हुई है लेकिन सत्ताधारी दलों ने जीत हासिल की है, क्योंकि उसके पूरे तंत्र ने मतदान में दस प्रतिशत से ज्यादा वोट जोड़ लिये।
अतीत के चुनाव का यह अनुभव बताता है कि मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता है तो उसे सत्ताधारी दल के विरुद्ध नाराजगी का संकेत माना जाता है। लेकिन नई खबर है कि सत्ता ने पुराने मतदाताओं को वंचित करने, नए मतदाताओं को जोड़ने के तौर-तरीकों का एक तंत्र विकसित कर लिया है। नई संसदीय संस्कृति को विचारधारा की संस्कृति से ही चुनौती दी जा सकती है।
बहरहाल, बिहार में चुनाव के दौरान व्यवहारगत ऐसा और भी कुछ देखा गया, जिसपर बातचीत उपरोक्त के साथ की जानी चाहिए थी। दरअसल चुनावों के नतीजे कई सतहों पर खड़े होते हैं। सभी सतहों पर बातचीत एक छोटी-सी टिप्पणी या विश्लेषण में संभव नहीं है। खासतौर से यह माना जाता है कि समाज में पढ़ने और सुनने का धैर्य बहुत नीचे स्तर पर पहुंच गया है। धैर्य एक राजनीतिक औजार है। लिहाजा कुछ अन्य बातें फिर कभी।
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in