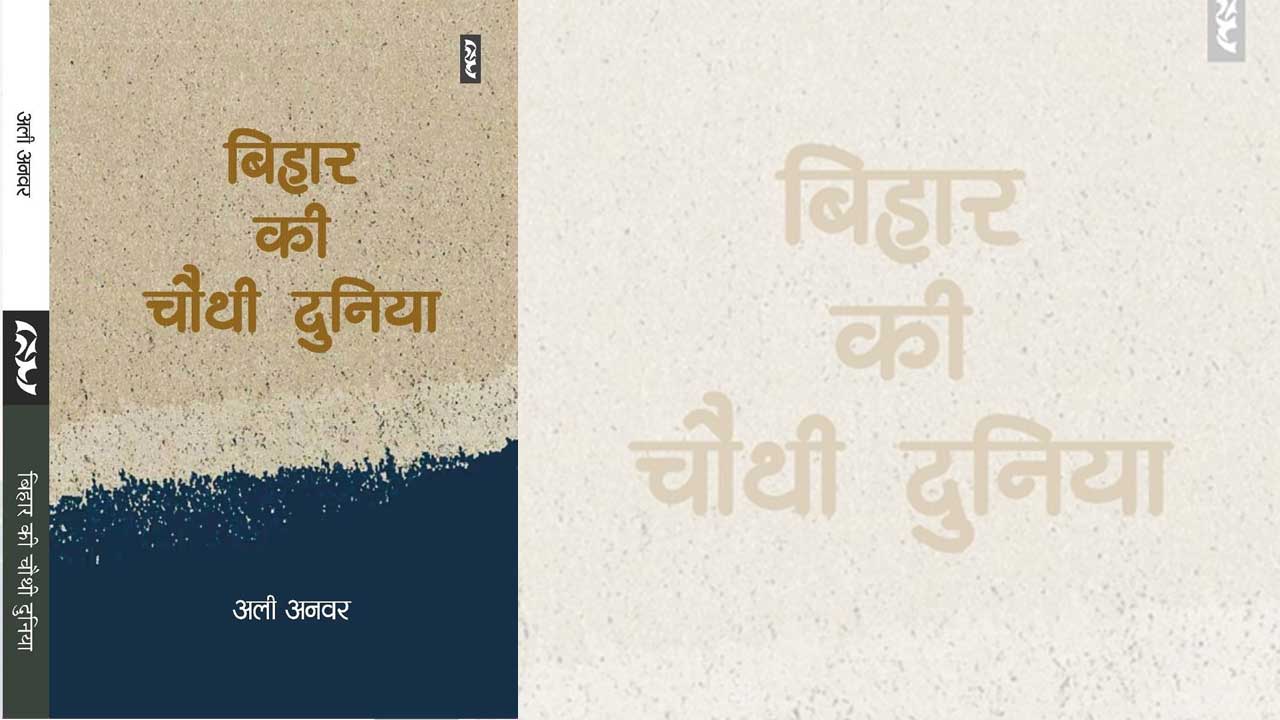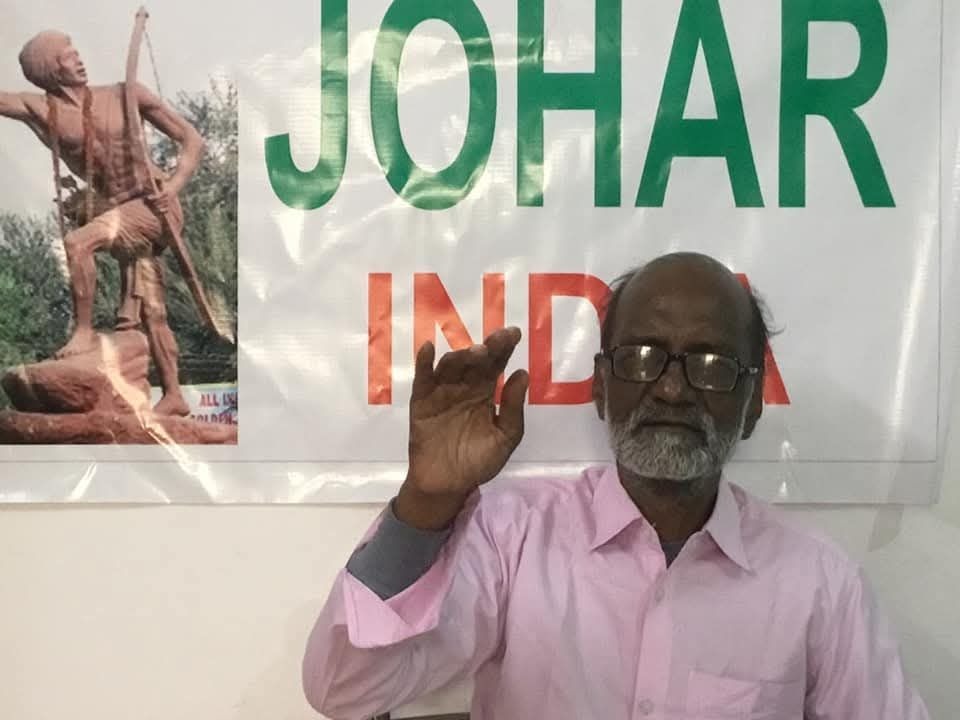बिहार में विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। बीस वर्षों से सत्ता पर काबिज दलों जनता दल यूनाईटेड (जदयू) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ मतदाताओं के बड़े हिस्से में नाराजगी देखी जा रही है। सत्ताधारी दल उस नाराजगी को कम से कम करने की कोशिश में तरह-तरह से लगी हुई है। सरकार के फैसलों के जरिए भी और दलों के स्तर पर तरह-तरह के प्रचार के जरिए। इन कोशिशों में एक महत्वपूर्ण बात यह दिखती है कि भविष्य में राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी व गठबंधन की सरकार बन सकती है। यह जदयू और भाजपा द्वारा किए जा रहे एक प्रचार से समझा जा सकता है। प्रचार यह कि तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी के नेतृत्व में बीस साल पहले जो सरकार थी वह किस तरह से काम करती थी। यह शैली दिल्ली में भी है। यहां दिल्ली में भाजपा के नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पिता, नानी, परनाना नेहरू के शासन को सत्ताधारी दल चुनिंदा पहलूओं को लेकर लगातार निंदा प्रचार करते हैं क्योंकि कांग्रेस के बतौर नेता राहुल गांधी सत्ताधारी दलों को चुनौती दे रहे हैं। यानी सत्ता विरोधी लहरों से निपटने के लिए नए नेतृत्वों के खिलाफ ‘परिवार’ के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।
सत्ता और सरकार का अर्थ
संसदीय चुनाव जब आते हैं तो यह आंकने की कोशिश की जाती है कि सत्ता विरोधी लहर कितनी है। यदि लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे है तो सत्ता का मतलब केंद्र सरकार से होता है। जब विधानसभा के लिए राज्यों में चुनाव होते हैं तो सत्ता का अर्थ राज्य की सरकार से होता है।
इसमें पहली बात तो यह स्पष्ट होनी चाहिए कि सत्ता का अर्थ सरकार नहीं होता है। यहां सत्ता का अर्थ सरकार को चलाने वाली पार्टी या पार्टियों से होता है। इसीलिए चुनाव में विपक्षी पार्टियां अपने विरोधियों के खिलाफ यह शिकायत करते हैं कि वे सत्ता को दुरुस्त तरीके से नहीं चला रहे हैं। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाते हैं। मतदाता भी सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियों के फैसले के आधार पर अपना समर्थन व विरोध जाहिर करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में यह माना जाता है कि जो भी पार्टी पांच साल या उससे ज्यादा समय तक के लिए सरकार में रहती है, उसके खिलाफ लोगों के बीच एक स्वभाविक विरोध या नाराजगी खड़ी हो जाती है। राजनीति शास्त्र में इसे मतदाताओं के सत्ता विरोधी रुख के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन यह गुजरे जमाने का चुनावी सिद्धांत है कि सरकार को चलाने वाली पार्टी के विरुद्ध में लोगों के बीच एक स्वभाविक नाराजगी उत्पन्न हो जाती है। पिछले कुछ चुनावों से यह स्पष्ट है कि सरकार चलाने वाली पार्टी से नाराजगी के आधार पर चुनाव को जीत लेने की उम्मीद विरोधी पार्टियों के काम नहीं आती है।
सत्ताधारी कैसे विरोध के रुख को कम करते हैं?
सत्ताधारी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के कारण लोगों के बीच नाराजगी या प्रतिक्रिया को तो देखती है लेकिन वह नाराजगी को कैसे भी कम-से-कम करके चुनाव में जीत हासिल कर लेती है। चुनावी रणनीति नाम का एक पेशेवर क्षेत्र चुनाव मैदान के लिए उभरा है। किसी राज्य या केंद्र के लिए होने वाले चुनाव में सरकार के कामकाज के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार नहीं होती है, बल्कि लोकसभा या विधानसभा की प्रत्येक सीटों की सामाजिक संरचना के हिसाब से चुनावी रणनीति तैयार होती है। इसीलिए केंद्र में या राज्य में सरकार चलाने वाली पार्टियों के खिलाफ उसकी योजनाओं या कामकाज के तौर-तरीको के मद्देनजर की गई अपील पूरे देश व राज्य में सामान स्तर पर कारगर नहीं हो पाती है। विरोधी पार्टियों को भी अब प्रत्येक सीट के आधार पर चुनावी रणनीति बनानी होती है। चुनावी रणनीति के लिए सर्वेक्षण का एक नया क्षेत्र भी जुड़ा है।
यह समझने की जरूरत है
इसी चुनावी रणनीति में यहां हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच सत्ता के विरोध के क्या-क्या मायने होते हैं। मसलन सत्ता पर काबिज दल या दलों के खिलाफ सत्ता की लहर हो सकती है, लेकिन सत्ता पर काबिज पार्टियां या पार्टी उस विरोध के प्रभाव को दूसरी तरफ मोड़ देने के लिए एक नए तरह के विरोध को हवा देती है। जैसे बिहार में चुनाव होने वाले है। वहां सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ एक माहौल दिख रहा है। नीतीश कुमार बीस वर्षों से सरकार के मुखिया बने हुए हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टियां इस प्रचार पर जोर दे रही हैं कि बिहार में उनके विरोध में बनने वाली सरकार कैसी हो सकती है। यानी विपक्ष एक सत्ता संरचना के विरुद्ध अपनी एक सत्ता संरचना के साथ चुनाव मैदान में उतरता है और सत्ताधारी दल विपक्ष की सत्ता संरचना के विरुद्ध एक लहर तैयार करने की कोशिश करता है। बिहार में जैसे सत्ताधारी दल द्वारा जंगल राज आने की एक आशंका का प्रचार किया जाता है। बीस वर्ष पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। उसका नेतृत्व लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने किया। उस पार्टी को जंगल राज के आरोप के साथ सत्ता से बाहर करने में सफलता विरोधी पार्टियों को मिली थी। लेकिन उस समय के प्रचार को आज भी इसलिए दोहराने में फायदा दिख रहा है क्योंकि इस बार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव विरोधी पार्टी के गठबंधन इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी की हार की स्थिति में वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार है।

विरोधी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की रणनीति
विरोध में खड़ी पार्टियों को भी चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के सिद्धांत में शामिल कर लिया गया है। हरिय़ाणा के चुनाव में यह प्रवृति देखी गई। सत्ताधारी पार्टी विरोधी रुख मतदाताओं में तीव्र था लेकिन इस तीव्रता को इस प्रचार के साथ कमजोर किया गया कि विरोधी पार्टियों की सरकार कैसी हो सकती हैं।
स्थानीय प्रतिनिधि की सत्ता बनाम सत्ताधारी दल
इस तरह सत्ता की कई सतहें मतदाताओं के बीच मौजूद होती हैं। मतदाता किस सत्ता से ज्यादा त्रस्त हैं, यह चुनावी रणनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। मसलन लोकसभा या विधान सभा के चुनाव में स्थानीय प्रतिनिधि के खिलाफ मतदाताओं का रुख भी है और सरकार चलाने वाली पार्टी के खिलाफ भी है। यदि प्रतिनिधि और सरकार चलाने वाली पार्टी एक है तो वह सत्ता विरोधी लहर की सबसे ज्यादा शिकार हो सकती है। लेकिन जहां स्थानीय प्रतिनिधि सरकार चलाने वाली पार्टी के विरोध वाली पार्टी का है तो मतदाताओं के सामने यह चुनाव करना एक चुनौतीपूर्ण होता है कि वह सत्ता विरोधी लहर में किसे अपने निशाने पर लें। इसीलिए यह देखा जाता है कि चुनावी रणनीति में सत्ताधारी पार्टियां अपने जीते हुए प्रतिनिधियों के बदले नए चेहरे क्षेत्र विशेष में उतार देती हैं। यह रणनीति सत्ता विरोधी लहर को कम कर देती है।
मतदाताओं के बीच कोई संगठित रणनीति नहीं हो सकती है जबकि पार्टियों के पास जितने ज्यादा संसाधान होते हैं, उसके हिसाब से उसकी चुनावी रणनीति प्रभावकारी मानी जाती है। पार्टियों को नामांकन दाखिल करने से लेकर मतदान तक मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का जुगाड़ करना होता है। यह जुगाड़ कामयाब मानी जाती है कि पांच वर्षों के अनुभव के आधार पर मतदाताओं के बीच जो राय बनती है वह मजबूती से खड़ी रहने के बजाय हवाहवाई हो जाए।
दरअसल संसदीय चुनावों में मतदाताओं के बीच राजनीतिक प्रशिक्षण का संकट गहरा होता जा रहा है। चुनावी रणनीतियां एक राजनीतिक हथियार की तरह धारदार हो गई हैं तो दूसरी तरफ मतदाताओं के लिए चुनावों के अर्थ महज आर्थिक लाभ व भावनाओं की तुष्टीकरण की सीमाओं में सिमट जाना रह गया है। इसका एक उदाहरण यह है कि लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय स्तर के चुनावों का स्वर एक जैसा हो गया है। संविधान की इन संस्थाओं के कामकाज और इनके प्रतिनिधियों की मुख्य जिम्मेदारियों को लेकर बुरी तरह से घालमेल कर दिया है।
लोकतंत्र के लिए राजनीति का पीछे जाना
किसी समय में विपक्ष अपनी किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। यह देखना दिलचस्प है। नई आर्थिक नीतियों के आने से पहले चुनाव सुधार पर विमर्श के दौरान पैसे के प्रभाव, सत्ता के दुरुपयोग, आचार संहिता आदि पहलू महत्वपूर्ण होते थे। नई आर्थिक नीतियों ने सत्ता द्वारा मतदाताओं के बदत्तर होते हालात में आर्थिक दान की पेशकश का रास्ता साफ किया है। यानी चुनाव होने से पहले घंटे तक सत्ता मतदाताओं को आर्थिक दान या सहायता देने के ऐलान करती है। यहां तक कि बैंक खाते में हजारों रुपए जमा करवा देती है। ऐसी स्थिति में पहले विपक्ष की भाषा यह होती थी कि चुनाव के लिए सत्ताधारी दल सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन नई आर्थिक नीतियों के बाद का विपक्ष एक नई भाषा के साथ तैयार हुआ है। विपक्ष अब यह कहता है कि सत्ताधारी दल द्वारा दी जा रही राशि मतदाता ले सकते हैं लेकिन वोट उन्हें यानी विपक्ष की पार्टी को देना चाहिए। इस तरह संसदीय लोकतंत्र में एक पैरोडी तैयार होती है। सत्तधारी दल कहता है कि पैसे लो, वोट दो। विपक्ष कहता है वोट उसे दो और पैसे भी ले लो। इस तरह चुनाव में पैसे की संस्कृति पूरी संसदीय व्यवस्था के लिए स्वीकृति पाती है। चुनाव के संदर्भ में ही नहीं बल्कि हर स्तर पर यह संस्कृति स्वीकार्य कराने की प्रवृति संसदीय पार्टियों में दिखती है। मसलन पुलिस गोलीकांड पहले होते थे तो विपक्ष गोलीकांड की जांच और पुलिस वालों को सजा देने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग के साथ आंदोलन करता था। अब गोलीकांड के बाद सत्ताधारी दल मुआवजा देने पीड़ितों के पास पहुंच जाता है। सत्ताधारी दल की तरह विपक्ष भी मुआवजे के साथ पीड़ितों के पास पहुंच जाता है। गोलीकांड आम हो गया है। राज्य व्यवस्था का हिंसक और आक्रामक होने के पहलू पर विचार करने का पक्ष गायब हो गया। मीडिया में एक खबर बनने की अहमियत भी गोलीकांडों में नहीं रह गई। विपक्ष के आंदोलन की बात तो इतिहास में कैद हो गया है। गोलीकांड के बाद सत्ताधारी पार्टी के चुनाव नतीजों पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है।
सत्ता विरोधी लहर का सिद्धांत सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों पर लागू होने लगा है। संसदीय राजनीति एक नए दौर से गुजर रही है। मतदाताओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की संस्कृति से ही संसदीय राजनीति को लोकतांत्रिक बनाए रखा जा सकता है।
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in