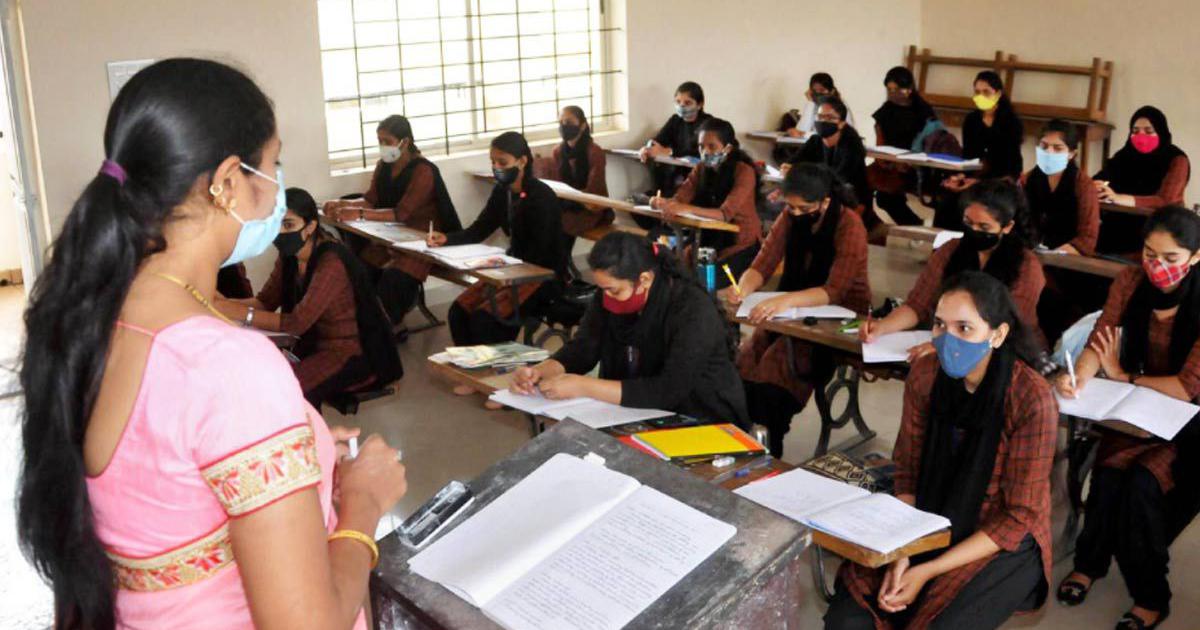बहु-वैकल्पिक प्रश्नों (एमसीक्यू) के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के लिए कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाओं की घोषणा जिस रूप में सामने आयी है,उसमें पहली ही नज़र में सिर्फ़ एक और नौकरशाही हस्तक्षेप, बीमार मानसिकता, और उच्च शिक्षा नीति को लेकर जल्दबाज़ी दिखती है। जो कुछ हो रहा है,उसे लेकर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उच्च शिक्षा दो तरह के जबरदस्त और कहीं ज़्यादा व्यापक बदलाव से गुज़र रही है। पहला बदलाव तो सरकारी विश्वविद्यालय प्रणाली का विध्वंस है और इसकी जगह निजी विश्वविद्यालयों को लाए जाने की योजना है,जो विश्वविद्यालयों को मुनाफ़ा कमाने वाले संगठनों के रूप में चलाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। हालांकि, यह प्रक्रिया नरेंद्र मोदी के शासन में आने से पहले से ही चल रही है।
दूसरा बदलाव हिंदुत्व की विचारधारा और हर नियम और मानदंड के अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तरफ़ से ठोक बजाकर और उनकी विचारधाराओं के रंग में जांचे-परखे शिक्षकों से तो भरा ही जा रहा है, बल्कि विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से जेएनयू में छात्र संगठन के वैचारिक रंग को नियंत्रित करने की कोशिश भी की जा रही है। यही वह संदर्भ है, जिसमें जेएनयू के लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि बहु-वैकल्पिक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्नों से अधिक ‘निष्पक्ष’ हैं, और यह कि ऑनलाइन परीक्षायें सुगम तथा ज़्यादा सुरक्षित हैं और इनमें किसी भी तरह के पूर्वाग्रह तथा छेड़छाड़ की कम आशंका है। हालांकि, ये दावे अपनी ज़मीनी सच्चाई से बहुत दूर हैं।

क्या एमसीक्यू वाक़ई निबंधात्मक प्रश्नों से अधिक ‘वस्तुनिष्ठ’ हैं?
ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में हो रहे इस बदलाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ़ से जो बयान आए हैं, वे छात्रों के चयन में ‘पूर्वाग्रह’ को ख़त्म करने का हवाला देते हैं। इस प्रकार के आरोपों में दो तरह की ग़लतबयानी हैं। सबसे पहले तो किसी और की तरह जेएनयू संकाय की सियासी राय पूरे राजनीतिक विस्तार में फैली हुई हैं। किसी भी मामले में, सभी विवेकशील शिक्षकों (जेएनयू और हर जगह) के लिए शिक्षण का लक्ष्य छात्रों को गंभीर रूप से सोचने-विचारने के लिए तैयार करना है, यहां तक कि हम जो भी सिखाते हैं, उसे लेकर भी आलोचनात्मक रूप से उन्हें तैयार करना है।
उदाहरण के लिए, जेएनयू प्रवेश परीक्षा के दो सामान्य प्रश्नों पर विचार करें :
“भाषायी बहुलता भारत की एक समस्या है या उसकी विशिष्टता है?”
और
“क्या वंचित समूहों के लिए सकारात्मक प्रयास समानता के सिद्धांत के विपरीत है ? अपने जवाब के लिए कारण दें। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सकारात्मक कार्रवाई नीति के साथ भारत में आरक्षण की नीति की तुलना करें।”
बहुजन विमर्श को विस्तार देतीं फारवर्ड प्रेस की पुस्तकें
क्लोज्ड एमसीक्यू तो और अधिक विचारधारात्मक हो सकते हैं, क्योंकि छात्रों को चार विकल्पों में से एक को चुनना है; वे पांचवें विकल्प पर विचार कर ही नहीं सकते हैं। हाल ही में यूजीसी नेट परीक्षाओं में आए ऐसे दो प्रश्नों पर विचार करें। जनवरी 2017 में, निम्नलिखित प्रश्न रखे गये थे:
प्र.47. नीचे दो तर्कवाक्य (ए और बी) दिए गए हैं। उन दोनों तर्कवाक्यों से चार निष्कर्ष (i), (ii), (iii) और (iv) निकाले गए हैं। उस कूट का चयन करें जो तर्कवाक्यों से (एकल अथवा संयुक्त रूप से) मान्य निष्कर्षों को दर्शाता है।
तर्क वाक्य :
(ए) अस्पृश्यता एक अभिशाप है। ।
(बी) सभी गर्म बरतन अस्पृश्य हैं ।
निष्कर्ष :
(i) सभी गर्म बरतन अभिशाप हैं ।
(ii) कुछ अस्पृश्य चीजें गर्म बरतन हैं ।
(iii) सभी अभिशाप अस्पृश्यता हैं ।
(iv) कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है ।
कोड
(1) (i) और (ii)
(3) (i) और iv)
(2) (ii) और (i)
(4) (i) और (iv)
इस सवाल से जो कुछ धारणा बनती है, आइये उस पर विचार करते हैं। अस्पृश्यता एक ‘अभिशाप’ (एक ऐसा शब्द,जो दैवी या अलौकिक हस्तक्षेप को इंगित करता है) है, यह किसी ऐसी घटना को इंगित नहीं करता है, जिसे जानबूझकर उत्पीड़न और बहिष्कार के सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक संरचनाओं के माध्यम से बनाए रखा गया हो; यह कि इस शब्द के अलग-अलग संदर्भों में ‘अस्पृश्यता’ को समान समझा जा सकता है- गर्म बरतनों को छूकर उंगलियां जल जायेंगी; कुछ लोग अन्य लोगों के स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार,यह सवाल राजनीतिक निहितार्थों से पूरी तरह अटा पड़ा है।

दूसरा उदाहरण, जुलाई 2018 में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा से है :
प्र. नीचे दो कथन दिये गये हैं। पहला,अभिकथन ए के रूप में वर्गीकृत है और दूसरा,कारण आर के रूप में वर्गीकृत है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें।
अभिकथन (ए) : शीत युद्ध और विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने राज्य के भीतर संयुक्त राष्ट्र की अधिक सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित किया।
कारण (आर): राज्यों के राष्ट्रीय हित के रूप में अपने-अपने प्राथमिक हित हैं।
कोड :
- ‘ए’ और ‘आर’ दोनों सत्य हैं और ‘आर’, ‘ए’ की सही व्याख्या है
- ‘ए’ और ‘आर’ दोनों सत्य हैं,लेकिन ‘आर’, ‘ए’ की सही व्याख्या नहीं है
- ‘ए’ सत्य है, लेकिन ‘आर’ असत्य है
- ‘आर’ सत्य है, लेकिन ‘ए’ असत्य है।
यहां यूजीसी के अनुसार, 1-’सही’ विकल्प है। अब, A और R दोनों अत्यधिक विवादास्पद हैं, और यह कहना कि दोनों ही ‘सही’ है, बहुत ही हास्यास्पद भी है। वे तो तथ्य ही नहीं हैं; दोनों ऐसे कथन हैं,जिनसे वैचारिक और सैद्धांतिक धारणायें सामने आती हैं, जो सम्बन्धित विषय की परिधि में अत्यंत विवादास्पद हैं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में क्यों गिरावट आयी ? क्या राज्य तर्कसंगत व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं ? क्या राज्यों के पास आंतरिक रूप से एक ही तरह के ‘राष्ट्रीय हित’ हैं? पिछले दो प्रश्नों के जवाब अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के यथार्थवादी अवधारणा से ‘हां’ में दिये जायेंगे, लेकिन इस विचार वालों की भी पर्याप्त आलोचनायें होती हैं। यदि ‘ए’ और ‘आर’ को प्रश्न के रूप में रखा गया होता, तो इनमें इन मुद्दों के इर्द-गिर्द बहस का विस्तार और आगे जाता। लेकिन, इसके बजाए कि एक छात्र के पास इस सहमति के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि ‘ए और ‘आर’ दोनों ‘सही’ हैं और ‘ए’, ‘आर’ का अनुसरण करता है। तब क्या होगा,जब कोई विचारशील छात्र अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सिद्धांत में यथार्थवाद की आलोचना करता है और विकल्प 3 चुनता है ? जो यथार्थवाद को स्वीकार करता है,वह विकल्प 2 का भी चुनाव कर सकता है, जो एक तरह से व्यवहार्य विकल्प प्रतीत होता है। मुद्दा यही है कि ये सभी राय विवादास्पद हैं, सही और ग़लत जवाब का मामला नहीं है।
यह भी पढ़ें : कोर्ट की फटकार के बाद एमफिल, पीएचडी के दाखिले में ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की अड़चनें खत्म
ऑनलाइन एमसीक्यू और मानवीय त्रुटि
इसके अलावा, एक संभावना यह भी है कि मानवीय त्रुटि के कारण एमसीक्यू परीक्षा ही ग़लत उत्तर कुंजी वाली हो। 2015 में, फ़ारसी के एक भी उम्मीदवार ने यूजीसी नेट परीक्षा पास नहीं की, क्योंकि प्रश्नपत्र के 125 प्रश्नों में से 94 के जवाब ग़लत थे।
अब,नई प्रवेश परीक्षाओं की चार और परेशान कर देने वाली विशेषताएं यहां दी गयी हैं। ये परीक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रही हैं। सिर्फ़ जेएनयू के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए इसका निहितार्थ है। शेष तीन परेशान करने वाली विशेषताएं जेएनयू को लेकर ज़्यादा ख़ास हैं।
दूसरी ख़ास बात कि जेएनयू प्रशासन को इस बात की ज़रूरत है कि परीक्षा आयोजित करने से पहले उत्तर कुंजी प्रदान की जाए। तीसरी बात कि प्रश्नों को जेएनयू संकाय सदस्यों द्वारा ही नहीं,बल्कि ‘जेएनयू संकाय के अलावा देश भर के विशेषज्ञों द्वारा’ तैयार एक प्रश्न बैंक से चुना जायेगा।’ चौथी बात कि यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे जेएनयू की ‘डिप्राइवेशन प्वाइंट सिस्टम’ (वंचितों के लिए विशेष प्वाइंट प्रणाली) लागू की जाएगी, और सामाजिक न्याय को लेकर इसके क्या मायने होंगे। आइए इसपर एक-एक करके विचार करते हैं।
हम दो अपेक्षाकृत छोटे (हालांकि नितांत समस्याग्रस्त) मुद्दों से शुरुआत करते हैं, इसके बाद एक और ज़्यादा गंभीर समस्या पर आगे बढ़ेंगे।

तकनीकी रूप से अनुचित और भेदभावपूर्ण
जेएनयू में सेवा देने वालों के लिए निविदा जारी की गयी थी। बोलियां लगाने की प्रक्रिया 19 सितंबर 2018 से शुरू की गयी थीं, और चयनित कंपनी को दिसंबर 2018 में जेएनयू प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंप दिया जाएगा। यह जल्दबाज़ी है और तय है कि परिणाम में बड़े पैमाने पर ख़ामियां होंगी। पूरे भारत में प्रत्येक परीक्षा स्थलों को जोड़ने के लिए परीक्षण करना होगा, कई परीक्षणों से गुज़रना होगा, और इसके विफल होने की स्थिति में आकस्मिक योजना बनानी होगी और उसका भी परीक्षण करना होगा। इस तरह की छोटी अवधि में इस जटिल प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जा सकता है?
यह भी पढ़ें : लिखित परीक्षा के बहाने जेएनयू से बाहर किए जाएंगे बहुजन!
पिछले साल ही भारत के विभिन्न हिस्सों में कई ऑनलाइन परीक्षणों में गंभीर समस्याएं आयी थीं। सर्वर नीचे चले गए थे, और विश्वविद्यालय की वेबसाइट में “तकनीकी समस्याएं” थीं; लखनऊ के 15 अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में आयोजित आम कानून प्रवेश परीक्षा में परीक्षा पत्र नहीं खुल पाया था, इसका परिणाम यह हुआ था कि उम्मीदवारों के पास प्रश्नों का उत्तर देने का समय कम पड़ गया था। इससे पहले 2012 में भी मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में सौ से अधिक बार हैकिंग करने के प्रयास हुए थे, इसी तरह की स्थिति से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी, चिकित्सा और दंत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए) का भी सामना हुआ था। उल्लेखनीय है कि एक बार फिर एक लिखित परीक्षा के रूप में वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली एनईईटी परीक्षा की जगह अब छमाही ऑनलाइन परीक्षा होने लगी है।
इस बदलाव को लेकर एक चिंता यह भी है कि कंप्यूटर-आधारित परीक्षा, ग्रामीण इलाकों के उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह और तक़लीफ़देह हो सकती है।
हालांकि आईआईजी जेईई को एमसीक्यू संचालित ऑनलाइन के साथ आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के सफल उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा रहा है, लेकिन यह एक भ्रामक प्रचार है। उपर्युक्त उदाहरणों को देखते हुए, जिसमें हजारों छात्रों के भविष्य खतरे में होंगे, यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली असंतुलित है और ऐसी तकनीकी ख़ामियों से भरी हुई है, जिनका समाधान नहीं हो पाया है। नीट प्रयोग का पलटा जाना एक ज़रूरी उदाहरण है, जिसका अध्ययन जेएनयू को गंभीरता से करनी चाहिए।
ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा : यह कौन सी व्यूह रचना है और इसका लाभ किसे मिलता है?
इस बात का कोई सबूत नहीं है,जो यह दावा कर सके कि ऑनलाइन परीक्षा पेन और पेपर वाली परीक्षाओं के मुक़ाबले सस्ता है। आईआईएम कैट परीक्षा आयोजित करने का अनुबंध 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। लगभग 2 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर हम एक डॉलर को 70 रुपये के बराबर मान लें, तो लागत प्रति छात्र 14 हजार रुपए होगी। जेएनयू की लागत (1 लाख उम्मीदवारों के लिए) इससे कम हो सकती है, लेकिन अब भी एक सरकारी विश्वविद्यालय के लिए यह एक बड़ी राशि है।
जहां तक संचालन व्यवस्था का सवाल है, तो इसके साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है, इसके बारे में अधिकांश लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि निविदा पाने वाली कंपनी को पूरे देश में चिह्नित की गयी। ऐसी छोटी-छोटी कंपनियों को प्रवेश परीक्षा के देशव्यापी संचालन के लिए आउटसोर्स करना होगा, जो सही मायने में परीक्षाओं को आयोजित करेंगी। ये कंपनियां गैर-पर्यवेक्षण योग्य संस्थाएं होंगी। शामिल उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए स्पष्ट है कि एक बार में प्रत्येक उम्मीदवार को कंप्यूटर टर्मिनल प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रत्येक केंद्र में बैचों में परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रत्येक वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्नों के कई सेटों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एमसीक्यू प्रारूप में प्रश्नों को दोहराया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक 100 उम्मीदवारों के लिए प्रश्नों के कम से कम पांच सेट होने चाहिये, यह मानते हुए कि प्रत्येक बैच में लगभग 20 उम्मीदवार हैं। परीक्षा केंद्रों की संख्या के बीच एक समन्वय भी स्थापित करना होगा, ताकि प्रत्येक केन्द्र के पास इतनी न्यूनतम सुविधायें तो हों कि उस केन्द्र पर परीक्षा आयोजित कराई जा सके।
इसके अलावा, इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न अगला साल दोहराया नहीं जा सकता है – यह सब इसलिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही जवाब है। दूसरी ओर, निबंधात्मक प्रश्नों को बीतते समय के साथ फिर से दोहराया जा सकता है, क्योंकि यहां कोई भी सही उत्तर नहीं होता है, और इसमें तर्क-वितर्क बहुत मायने रखते हैं। इसलिए, जहां प्रश्नों के बड़े बैंकों का निर्माण किया जाना है, वहां इतनी बड़ी संख्या में सृजित प्रश्नों की गुणवत्ता क्या होगी ? दिलचस्प बात है कि जेएनयू अधिकारियों ने जेएनयू संकाय से केवल दो ही सेट सवालों के लिए कहा है। शेष प्रश्न कौन-कौन निर्धारित करेंगे ?
यह भी पढ़ें : जेएनयू को विश्वविद्यालय से स्कूल बनाने की तैयारी
देशभर के विश्वविद्यालयों में व्यापक लागत-कटौती की गयी है, लेकिन इसके साथ ही साथ बॉयोमीट्रिक मशीनों और ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में भारी निवेश किया गया है। ऐसे में, ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए भुगतान करने के लिए विश्वविद्यालयों से की जाने वाली लागत कटौती कहां हैं? कोई शक नहीं कि जेएनयू में हो रही लागत-कटौती से पुस्तकालय प्रभावित हो रहा है। जेएनयू के संकाय सदस्यों ने अगले साल होने वाली लाइब्रेरी समितियों की बैठकों से सीखा है, और हम लाइब्रेरी के लिए बड़े पैमाने पर बजट कटौती की तरफ़ देख रहे हैं,जो जेस्टोर और म्यूज़ जैसे ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच बनाए बिना हमें छोड़ देगा। इसलिए, ऐसा नहीं है कि सभी ऑनलाइन समाधानों को प्राथमिकता दी जा रही है।
असली सवाल तो यही है कि सभी प्रवेश परीक्षाओं को ऑनलाइन में बदले जाने पर ज़बरदस्त जोर देने के पीछे की ताक़तें कौन हैं? ऑनलाइन परीक्षाओं (और बॉयोमीट्रिक उपस्थिति जैसे अन्य बड़े ख़र्च वाले तकनीकी सुधार) के लिए एक मजब़ूत पिच बनाने में रुचि रखने वाले “हितधारक” वास्तव में हैं कौन। हमारे सिस्टम में संस्थानों को इस विनाशकारी, प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले तकनीकी रूप से संचालित प्रारूप में और शायद आख़िरकार सभी परीक्षाओं में धकेलने वाला इस तरह का मौद्रिक लोभ का विस्तार क्यों हो रहा है?
इस सिलसिले में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुभव से सीखा जा सकता है। ब्रिटेन का विशाल प्रकाशन पियर्सन के पास वास्तव में ऑनलाइन कक्षाओं और छात्र डेटा सिस्टम के परीक्षण से लेकर शिक्षा के सभी पहलुओं पर एकाधिकार है। पॉलिटिको द्वारा की गयी एक जांच में पाया गया कि :
“पियर्सन, करदाताओं के डॉलर से करोड़ों डॉलर बनाने में सफल है, वह फ़्लोरिडा से टेक्सास के राज्यों तक में प्रतिस्पर्धी बोलियों के बिना व्यवस्थित सौदों से छात्र के ट्यूशन में कटौती करती है। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि पियर्सन का अनुबंध विशिष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों को निर्धारित करता है- लेकिन जब वे उन मानकों को पूरा करने में विफल रहती है, तो कंपनी को दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसे लेकर कुछ बाधाओं के साथ उच्च शिक्षा क्षेत्र में ये अनुबंध, पियर्सन को छात्र से सम्बन्धित डेटा तक व्यापक पहुंच प्रदान करते हैं।”
हालांकि,अंततः जैसा कि न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के एक शिक्षा इतिहासकार जॉनाथन ज़िमर्मन ने का कहना है: “जिन लोगों को हमने चुना है, उन्होंने एक परिदृश्य बनाया है और इसी परिदृश्य ने पियर्सन को मालामल कर दिया है।” यह पूछने की बिल्कुल ज़रूरत है कि भारत में शिक्षा सॉफ्टवेयर व्यवसाय में कौन से बड़े खिलाड़ी हैं और निर्णय निर्माताओं को किस प्रकार से लाभ पहुंचाये जा रहे हैं?
अब जेएनयू से सम्बन्धित ख़ास मामले मसलन अग्रिम रूप से उत्तर कुंजी देने में समस्यायें
प्रशासन ने शुरू में यह नहीं बताया था कि परीक्षा आयोजित होने से पहले उत्तर कुंजी की आवश्यकता क्यों है। जब यह मामला छात्रों के संगठन द्वारा प्रसारित एक प्रेस नोट में आया, तो प्रशासन की तरफ़ से मीडिया को दी गयी सार्वजनिक प्रतिक्रिया यह थी कि उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त होने के समय अपना स्कोर पता होना चाहिए (जेएनयू 2018)। यह एक ताजा मामला है, जिसे प्रशासन द्वारा पहले नहीं उठाया गया था, और यह स्पष्ट नहीं है कि यदि छात्र योग्यता सूची में आ गये हों या अंतत: चुन लिए गए हों, तो छात्रों द्वारा किसी प्रश्न का सही जवाब पता चल जाने से उनके कौन से उद्देश्य पूरे होने हैं। प्रश्नपत्र सेट करने वालों की उपस्थिति में परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी को सामने लाने का नियम है। हालांकि, जेएनयू प्रशासन ने शुरू में इस बात पर ज़ोर दिया था कि परीक्षा आयोजित होने से पहले पेन ड्राइव में उत्तर कुंजी की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रश्न पत्रों को सही करने के लिए ख़ुद को दो सप्ताह भी दे दिया। इन दोनों आवश्यकताओं ने जेएनयू संकाय को संदेहास्पद बना दिया।
प्रश्न सेट करने के लिए बाहरी विशेषज्ञ
प्रशिक्षित शिक्षाविदों के पास अपने क्षेत्रों की विशिष्ट कौशल होता है, और किसी भी विषय का कोई भी पूरा विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। जेएनयू के विभिन्न केंद्रों में उनके अपने शैक्षणिक केन्द्रबिन्दु और क्षेत्र हैं, जिनके वे विशेषज्ञ होते हैं, और प्रवेश परीक्षाओं में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए। जेएनयू के अधिकांश केंद्र बहु-विषयक होते हैं, और प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम में उनके अनेक विषय घटक होते हैं। नतीजतन, एक साथ एक से अधिक विषयों के साथ परिचित होने के लिए भी प्रश्न तैयार किए जाते हैं।
कोई भी प्रवेश परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा या यहां तक कि स्नातक रिकॉर्ड्स परीक्षा (जीआरई) जैसे मानकीकृत परीक्षाओं से अपने लक्ष्यों में मौलिक रूप से भिन्न होते हैं, जो उम्मीदवार के ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन करती है। हालांकि, किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। फिर वह संकाय, जो उस पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ा रहे होते हैं, किसी भी विशेषज्ञता का दावा कैसे कर सकते हैं? अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेएनयू के बाहर के विशेषज्ञ कौन हैं,जो प्रश्न निर्धारित करेंगे, उन्हें कैसे चुना जायेगा, और किसके द्वारा चुना जायेगा?
प्रवेश नीति और सामाजिक न्याय का परिप्रेक्ष्य
2017-18 के सत्र में एडमिशन के बाद, जेएनयू की प्रगतिशील नामांकन नीति को मौजूदा कुलपति ने तबाह कर दिया है। 2017-18 के एडमिशन में विश्वविद्यालय की रिसर्च डिग्री के लिए सीटों में 83% कटौती कर दी गयी थी, और आख़िरी नामांकन से पता चला कि इन पाठ्यक्रमों के लिए केवल 159 छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया था और 131 सीटें ख़ाली रह गयीं थीं। सवाल है कि जेएनयू 2017-18 में अपनी सीटों को क्यों नहीं भर सका था और जेएनयू रिसर्च डिग्री पाठ्यक्रम में सामाजिक न्याय घटक इतना कमज़ोर क्यों हुआ है, इसका कारण वह नीति है, जो इस परीक्षा को लेकर होने वाली मौखिक परीक्षा तक पहुंचने के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत का अर्हता अंक निर्धारित करती है। कोई भी अन्य संस्था किसी भी विषय में रिसर्च परीक्षाओं के लिए इस उच्च योग्यता प्रतिशत को निर्धारित नहीं करती है। ज़्यादातर संस्थायें किसी भी पाठ्यक्रम के लिए इतना उच्च अंक निर्धारित नहीं करती हैं। जेएनयू संकाय को अधिकारियों द्वारा पहली बार मौखिक रूप से सूचित किया गया था कि प्रत्येक स्तर पर स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध-पाठ्यक्रमों में समान रूप से ऑनलाइन परीक्षण योग्यता के रूप में 50 प्रतिशत के इस प्रतिशत को अपनाया जायेगा, लेकिन जारी किये गये दो अलग-अलग दिशा-निर्देशों में से किसी में इस बात का उल्लेख नहीं हैं कि होने जा रही किसी भी परीक्षा के लिये क्वालीफाइंग अंक क्या होगा। इससे वे सभी छात्र प्रभावित होंगे, जो पहली बार इस प्रारूप का सामना करने जा रहे हैं या जिनके पास इस फॉर्मेट को समझने का न तो समय है या न ही साधन है; कोई शक नहीं कि यह प्रारूप पहली बार परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जेएनयू प्रवेश परीक्षा अब तक शिक्षकों को सर्वोत्तम क्षमता वाले छात्रों का चयन करने में सक्षम बनाती रही है, क्योंकि इससे न्यूनतम प्राप्ति के वैसा उचित मानदंड अपनाया जाता रहा है, जो छात्र के नियंत्रण से बाहर के कारकों से बिल्कुल प्रभावित नहीं था।
यह भी पढ़ें : कोर्ट की फटकार के बाद एमफिल, पीएचडी के दाखिले में ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की अड़चनें खत्म
आशंका इस बात को लेकर है कि जेएनयू अधिनियम की आवश्यकताओं की सेवा में बनाये गये जेएनयू के इस अनूठे नवाचार को अब सभी बोर्डो में समाप्त किया जा रहा है। इसी प्रकार, आरक्षित श्रेणियों को लिखित परीक्षाओं में पास अंकों में मिलने वाली अनिवार्य छूट को लेकर किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है।
कुल मिलाकर, जेएनयू की प्रवेश नीति में किये जा रहे परिवर्तनों को लेकर जेएनयू संकाय की चिंता यही है कि इसके पीछे जेएनयू के चरित्र और उसके पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल देने का इरादा है, और इसे इस तरह अंजाम दिया जा रहा है ताकि मुनाफ़ाखोरी और भेदभाव को बढ़ावा मिले। अलग से इससे भ्रष्टाचार पैदा होने की संभावना है, ख़ास तौर पर इस कारण से क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से जेएनयू संकाय के हाथों से बाहर कर दिया गया है।
जेएनयू के इतिहास में पहली बार, पूरी प्रवेश नीति एकेडमिक काउंसिल के नियंत्रण से बाहर कर दी गई है। सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की निगरानी के लिए जेएनयू प्रशासन द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित समिति में कुलपति द्वारा चुने गए कुछ जेएनयू संकाय (संस्थाओं में कोई प्रतिनिधित्व नहीं) और आईआईटी दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ संकाय शामिल हैं।
अंत में, जैसा कि पहले बताया गया है, यह प्रश्न सिर्फ़ जेएनयू या किसी विशेष विश्वविद्यालय का ही नहीं है। सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा में रुचि रखने वाले प्रत्येक भारतीयों को इस ऑनलाइन परीक्षाओं की तरफ़ बड़े पैमाने पर धकियाए जाने को लेकर सवाल पूछना चाहिए। क्या छात्रों को इससे फ़ायदा होगा? और आख़िरकार इससे किसको लाभ होने वाला है?
(कॉपी संपादन : एफपी डेस्क, अनुवाद : उपेन्द्र चौधरी )
(यह आलेख मूल रूप से 20 अक्टूबर 2018 के इकनॉमिक्स एंड पालिटिकल वीकली खंड-53, के अंक-42 में एक ही शीर्षक के साथ प्रकाशित एक लेख का संक्षिप्त संस्करण है। पूरा लेख पढ़ने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जाया जा सकता है- https://www.epw.in/journal/2018/42 )
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें