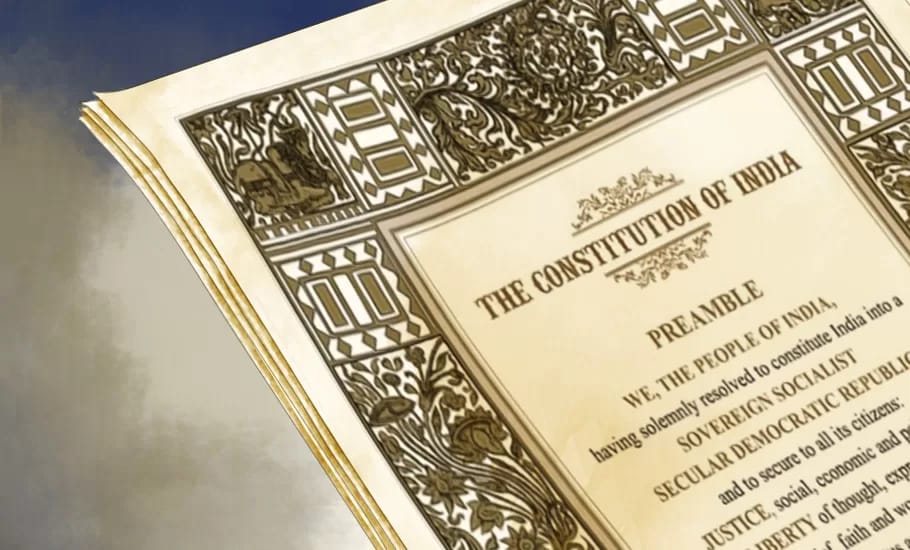सिएटल सिटी, अमेरिका का एक ऐसा शहर, जहां जातिगत भेदभाव को कानून के दायरे में लाया गया है। गत 21 फरवरी, 2023 को हुए सिएटल परिषद की बैठक में 6-1 से यह प्रस्ताव पारित किया गया। परिषद के सदस्य थे– लिसा हर्बोल्ड, टामी मोरालेस, क्षमा सावंत, अलेक्स पेडर्सन, देबोरा जौरेज़, डान स्ट्रॉस,अंद्रेव लेविस, टेरेसा मस्क्वेडा और सारा नेल्सन थे। प्रस्ताव के विरोध में केवल (सारा नेल्सन का) एक वोट असहमति का रहा। सिएटल परिषद के इस फैसले से वहां रहनेवाले भारतीय दलित-बहुजनोंको जातिगत भेदभाव के अत्याचार पर कानून का संरक्षण मिलेगा।
हालांकि अमेरिका में जातिगत भेदभाव को लेकर उठाया गया यह पहला कदम नहीं है। इसके पहले पिछले तीन वर्षों में, अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए हैं। मसलन, दिसंबर 2019 में, बोस्टन के पास ब्रैंडिस विश्वविद्यालय पहला अमेरिकन कॉलेज बना, जिसने अपनी गैर-भेदभाव नीति में जाति को शामिल किया है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम, कोल्बी कॉलेज, ब्राउन यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ कड़े उपाय अपनाए हैं। यहां तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी 2021 में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानूनी निति अपनाई।
सनद रहे कि अमेरिका भारतीयों की पहली पसंद रहा है। अभी हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में उन 135 देशों की सूची उपलब्ध कराई, जिनकी नागरिकता भारतीयों ने हासिल की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका (78,284) की नागरिकता लेने वालों की रही। दूसरे नंबर पर आस्ट्रेलिया रहा जहां 23,533 भारतीयों ने नागरिकता ली।
वर्ष 2010 में अमेरिका में जनगणना के अनुसार 3.5 मिलियन से अधिक दक्षिण एशिआइ लोग रहते थे । साउथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर समूह के रिपोर्ट अनुसार, अमेरिका में लगभग 5.4 मिलियन दक्षिण एशियाई लोग रहते हैं। इनमें सबसे अधिक भारतीय हैं।
सवाल है कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में जातिवाद कौन कर रहा है? भारत में ब्रिटीश काल के समय से सवर्ण जातियों के लोग यूरोप और अमेरिका में जाकर बसे। उसके बाद भी गंतव्य का यह सिलसिला जारी रहा है। लेकिन वहां जाने के बाद भी वे अपने साथ अपना वर्चस्ववाद साथ लेते गए। भारत के आजादी के कुछ सालो बाद ओबीसी, दलित एंव आदिवासी समुदाय के शिक्षित लोग भी नौकरी और शिक्षा के लिए यूरोप और अमेरिका जाने लगे। इसके बाद वहां जातिवादी भेदभाव की खबरें आनी शुरू हुईं।

वहीं भारत की बात करें तो यहां जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई। वर्णव्यवस्था द्वारा जबरदस्ती थोपे गए व्यवसाय प्रणाली सदियों से मुस्लिम और ब्रिटिश शासन के तहत विकसित हुई है। हालांकि भारतीय संविधान में जातिवाद के खिलाफ 1948 में ही कानून बना दिया गया। लेकिन इसके बावजूद यह भेदभाव जारी है।
अमेरिका में जातिगत भेदभाव रहने की जगहों, शिक्षा और नौकरी आदि के क्षेत्र में सामने आ रहा है। जातिगत भेदभाव के कारण बहुजन समाज के लोग अपनी जाति छिपाकर रहते हैं। वहीं ब्राह्मण वर्ग के लोग छाती ठोककर अपनी जाति को उजागर करके गौरव महसूस करते हैं।
परिषद् के प्रस्ताव के लिए 200 से अधिक सगठनों ने अपनी सक्रियता दिखाई। प्रस्ताव के समर्थन में परिषद को चार हजार से अधिक ईमेल प्राप्त हुए थे। सिएटल परिषद के भारतीय अमेरिकी सदस्य क्षमा सावंत ने जातिगत भेदभाव को कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव पेश किया था। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य व भारतीय मूल की प्रमिला जयमाला ने प्रस्ताव का स्वागत किया। सिएटल निवासी योगेश माने कहते हैँ कि “मैं भावुक हूं, क्योंकि यह पहली बार है जब इस तरह का कानून दक्षिण एशिया के बाहर दुनिया में कहीं भी पारित किया गया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है।” ओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया स्थित इक्वैलिटी लैब्स के कार्यकारी निदेशक थेनमोझी सौंदरराजन ने कहा कि इस निर्णय से हमने एक सांस्कृतिक युद्ध जीतलिया है। जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कानूनों की सख्त जरुरत थी।
बहरहाल, सिएटल परिषद के प्रस्ताव के विरोध में सवर्ण हिंदू समाज विरोध कर रहा था। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने प्रस्ताव का विरोध किया था। यह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुडा है। लिसा हर्बोल्ड ने विरोधियों के इस तर्क को ख़ारिज किया कि, यह कानून हिंदुओं को अलग करता है। उन्होंने कहा कि यहां की छोटी आबादी इस भेदभाव को महसूस कर रही है। इसीलिए यह तर्क महत्वपूर्ण नहीं है। सिएटल के इस अध्यादेश का संदेश साफ़ है। उसने भारत के जातिवादी भेदभाव को दुनिया के सामने उजागर कर दियाऔर दुनिया के अन्य देशों को “जाति” को वंशवादी भेदभाव में अंतर्भूत कर कानून के दायरे में लाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन भारत के वर्चस्ववादी कौम के लोग, जो मनुवादी व्यवस्था पर गर्व करते हैं, क्या वे इससे सबक सीखेंगे? यह एक बड़ा सवाल है।
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in