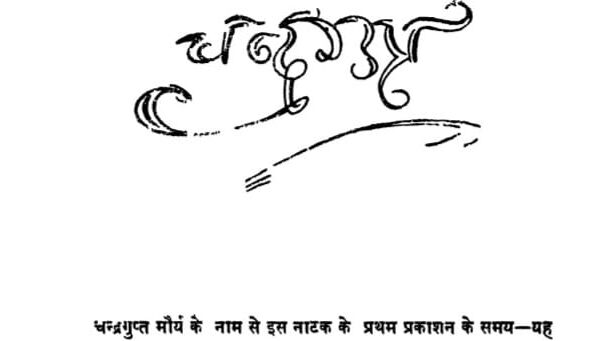हिंदुत्ववादी भाजपा 2014 से केंद्र में सत्तासीन है। मगर एक अर्थ में वह कभी भी सत्ता से बाहर रही ही नहीं। सन् 1925 में स्थापित उसकी मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भारत के सामाजिक-आध्यात्मिक ढांचे के कई हिस्सों पर मज़बूत पकड़ रही है। मुसलमानों और ईसाइयों पर धौंस जमाना इस हिंदुत्ववादी ताकत के एजेंडे का एक भाग भर है। शूद्रों और उनके अकूत बाहुबल पर इस ताकत का लंबे समय से नियंत्रण रहा है, हालांकि दलितों और आदिवासियों के बारे में यह बात उस हद तक सही नहीं है।
असल में ब्राह्मणवादियों का काम सन् 2014 में भाजपा के पहली बार संसद में अपने बल पर बहुमत हासिल करने के बाद शुरू नहीं हुआ और ना ही वह 1925 में आरएसएस के गठन के बाद से शुरू हुआ। यह काम तो ऋग्वेद, रामायण और महाभारत (गीता जिसका एक भाग माना गया है) एवं सनातन धर्म के अन्य ग्रंथों की रचना के साथ ही शुरू हो गया था।
इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है और वह यह कि हिंदू धर्म में शूद्रों की क्या भूमिका है? हिंदुओं के पवित्र और आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं कि शूद्र चौथा वर्ण है। मगर हिंदू देवों में एक भी शूद्र नहीं है। पौराणिक हिंदू देव या तो ब्राह्मण हैं (जैसे ब्रह्मा व परशुराम) या क्षत्रिय (जैसे विष्णु और राम)।[1]
शरीर और चेतना
भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमारे समाज का जो तबका देश में सामाजिक-आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता था और जो भारत को एक नए प्रकार की सभ्यता वाला देश बना सकता था, वह तबका था शूद्र। सन् 1931 की जनगणना के अनुसार वे देश की कुल आबादी का 52 प्रतिशत थे और इन दिनों वे जातिगत जनगणना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
मगर शूद्रों को यह मौका ही नहीं दिया गया कि वे अपनी रोज़ाना की जिंदगी और अपने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर ब्राह्मणवाद की मज़बूत पकड़ को ढीला या समाप्त कर सकें। सुनियोजित ढंग से शूद्रों की आत्मा को उनके शरीर से विलग कर दिया गया। शरीर से खेतों में काम कराया जाने लगा। शरीर का उपयोग सड़कों और गलियों में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों, से लड़ने-भिड़ने के लिए किया जाने लगा। दूसरी ओर आत्मा को जागने नहीं दिया गया। उन्हें ज्ञान से कोसों दूर रखा गया। आरएसएस और हिंदू महासभा ने उनके अधीन संगठनों में काम करने वाले सभी जातियों के लोगों को पुरोहिताई में प्रशिक्षित करने का कोई प्रबंध नहीं किया। उन्होंने ऐसे मंदिर नहीं बनाए, जिनमें प्रतिष्ठापित देवों की जाति अज्ञात हो। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए लंबा अभियान चलाया। मगर राम के बारे में सब जानते हैं कि वे क्षत्रिय थे। इस मंदिर में उन्होंने ब्राह्मणों को पुजारी बनाया। उन्होंने कभी पोचम्मा[2] का मंदिर बनवाने की बात नहीं की, क्योंकि पोचम्मा की जाति के बारे में हम कुछ नहीं जानते। शूद्रों को यह समझ में नहीं आया कि वे राम मंदिर या दूसरे वैष्णव मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं बन सकते।
किसी शूद्र, दलित और आदिवासी को राम मंदिर में पुजारी बनने का हक नहीं है। यह हक केवल ब्राह्मणों को है। शूद्रों, दलितों और आदिवासियों को गुणहीन और अयोग्य हिंदू माना जाता है। गुण और योग्यता की यह भाषा द्विज बुद्धिजीवियों ने विकसित की है। अगर आप किसी समुदाय को पुरोहित बनने ही नहीं देंगे, अगर आप उसे आध्यात्मिक दर्शन का ज्ञान हासिल ही नहीं करने देंगे तो उस समुदाय का पिछड़ जाना अवश्यंभावी है। आरएसएस और भाजपा चाहते हैं कि शूद्र हाशिए पर बने रहें, क्योंकि तभी वे ब्राह्मणों और अन्य सवर्णों की हिंदू समुदाय के नियंता बने रहने में मदद कर सकेंगे।
आरएसएस व आध्यात्मिक बराबरी
आरएसएस ने कभी भी हिंदू धर्म में समानता पर बहस नहीं छेड़ी। अगर मंदिर, अध्यात्म के संस्थागत स्वरूप की आत्मा है तो वह विद्यालय जहां मंदिर का संचालन करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, निश्चित रूप से आत्माओं का निर्माता है। मगर आरएसएस अपने संगठनों में काम करने वाले शूद्रों, आदिवासियों और दलितों को इस आत्मा का हिस्सा नहीं बनने देता। वह उन्हें हिंदू धर्म के ढांचे में सिर्फ एक शरीर बने रहने देना चाहता है। शरीर यानी केवल एक भौतिक वस्तु। यद्यपि सभी जातियों के लोग उन्हीं देवों की आराधना करते हैं जिनमें आरएसएस की आस्था है, मगर फिर भी वह जाति से परे आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ब्राह्मण को उच्च सांस्कृतिक दर्जा दिया गया है। वह प्रधानमंत्री बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकता है, मंदिर का पुजारी बन सकता है, फिल्म का हीरो बन सकता है, खिलाड़ी बन सकता है और आरएसएस का मुखिया भी बन सकता है। अगर वह चाहे तो खेती भी कर सकता है और पशुओं को चरा भी सकता है।
जो शूद्र, दलित और आदिवासी हिंदुत्व नेटवर्क का हिस्सा हैं, वे अपने आध्यात्मिक हाशियाकरण को चुपचाप झेलते रहते हैं। वे हिंदू हैं, मगर उन्हें ईश्वर से संवाद करने का अधिकार नहीं है। उन्हें पुजारी बनने का अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म में ईश्वर से संवाद महत्वपूर्ण होता है और अगर इसकी अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे संबंधित व्यक्तियों में एक अलगाव का भाव पैदा होता है। वे सबसे और स्वयं से भी दूर हो जाते हैं। धर्मों का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि वे एक समेकित आध्यात्मिक जीवन के जन्मदाता होते हैं। शूद्र, दलित और आदिवासी तबकों को आरएसएस ने हिंदू बताया और उन्हें हिंदुओं के हित में काम करने के लिए प्रेरित भी किया। मगर साथ ही उन्हें अलग-थलग और अशिक्षित बनाए रखा गया और उनका इस्तेमाल ब्राह्मणवाद ने केवल अनाज पैदा करने वाले गुलामों की तरह किया। स्वाधीन भारत में उनके शिक्षा हासिल करने पर कोई रोक नहीं है, मगर संघ व भाजपा के मुस्लिम-विरोधी एजेंडे के नशे में वे इतने गाफिल हैं कि उनमें तार्किकता और विवेक जागृत ही नहीं हो पा रहा है।

क्या नए पाठ्यक्रमों में शूद्रों के लिए कोई जगह है?
हिंदुत्ववादी ताकतों ने शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों पर अपनी पवित्र पुस्तकों पर आधारित पाठ्यक्रम थोप दिया है। उनकी इन पुस्तकों में शूद्र, दलित और आदिवासी तबकों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। उनकी पुस्तकों में ऋषि, देवी-देवता, नायक और नायिकाएं सभी मुख्यतः ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। रामायण और महाभारत भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर केंद्रित हैं। तब आखिर क्यों शूद्र, दलित और आदिवासी समुदायों को इन ग्रंथों को अपना मानना चाहिए? क्या शूद्रों को यह मान लेना चाहिए कि जब ये पुस्तकें लिखी गईं थीं उस समय भारत में केवल दो ही जातियां थीं? क्या शूद्र, जो आज के भारत की आबादी का 52 फीसदी हैं, उस समय थे ही नहीं? क्या प्राचीन भारत में शूद्र जैसा कोई वर्ण था ही नहीं? उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी? खाद्यान्न का उत्पादन कौन करता था? ऐसा माना जाता है कि कृषि उत्पादन के अधिशेष से ही प्रशासन और सेना का खर्च चलता था और इसी से शासक वर्ग ऐश-ओ-आराम की जिंदगी जीता था।
जब राजा क्षत्रिय थे और अधिकांश ऋषि ब्राह्मण थे, तब निश्चय ही शूद्र और वैश्य उत्पादन और व्यवसाय करते रहे होंगे। हिंदू धर्म की पहली पुस्तक ऋग्वेद उन्हें यही करने की आज्ञा देती है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई पुस्तकें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वर्चस्व और प्रभुत्व की बात करती हैं और उसे उचित ठहराती हैं। कुछ हिंदुत्ववादी विचारक इन दिनों कहने लगे हैं कि जाति का निर्माण अंग्रेज औपनिवेशिक शासकों ने किया था। क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और ढेर सारे पुराण – जो अनवरत वर्ण व जाति की बात करते हैं – अंग्रेजों ने लिखे थे?
क्या प्राचीन काल में ऐसा एक भी शूद्र या वैश्य महिला या पुरुष नहीं हुआ, जिसे दैवीय दर्जा प्राप्त हो? क्या इन वर्गों के आम लोगों में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था, जिसने कोई उल्लेखनीय काम किया हो? फिर क्या कारण है कि ये प्राचीन पुस्तकें इन तबकों के बारे में कुछ नहीं कहतीं? जब क्षत्रिय राजा कोसल या कुरुक्षेत्र से अपने विशाल साम्राज्यों में रामराज्य या धर्मराज्य पर आधारित शासन चलाते थे, तब अनाज कौन पैदा करता था और मवेशियों को कौन पालता था? क्या ये अत्यंत समृद्ध राज्य बिना किसी उत्पादक कार्य के अस्तित्व में बने रहे? अगर शूद्र धरती से और पशुओं से भोजन उत्पन्न नहीं कर रहे थे तो ये साम्राज्य कैसे जिंदा थे? क्या कारण है कि रामायण और महाभारत से उन बहुसंख्यक लोगों को गायब कर दिया गया, जो भारत के लोगों के अस्तित्व में बने रहने में सबसे अहम् भूमिका निभाते थे? इतनी बड़ी संख्या में लोग देवी-देवताओं के दार्शनिक संबल के बिना भला कैसे जीवित रहते थे? अगर आध्यात्मिकता मानव जीवन का केंद्रीय तत्व है तो वे आध्यात्मिक दर्शन के बिना कैसे जीते थे? अगर उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा निर्मित तंत्र द्वारा नियंत्रण में नहीं रखा जाता था तो आखिर वे इतने दमित क्यों थे?
धर्म हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया है और वही उन्हें अस्तित्व में बनाए रखता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में शूद्रों का स्थान कहां है? धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी द्विज बुद्धिजीवी, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद और समाजवाद की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मगर इस विषय पर बात करना नहीं चाहते। वे एक मिथ्या दुनिया में जीते हैं, जिसका आम लोगों की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं होता।
वे कहते हैं कि धर्म हर व्यक्ति का निजी मसला है। मगर आरएसएस व भाजपा यह नहीं मानते। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी सारी गतिविधियां धर्म की धुरी के आसपास घूमती हैं और वे मुसलमानों को दुश्मन के रूप में पेश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते।
शूद्रों ने प्राचीनकाल में ब्राह्मणों के इस हुक्म को स्वीकार किया कि उन्हें हाशियाकृत और दमित बने रहना है। क्या वे अब भी उसे स्वीकार करते हैं? अगर वे इन प्रश्नों पर अब भी विचार नहीं करेंगे तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी।
संघ की विचारधारा में किसान
आरएसएस व भाजपा का शूद्र किसानों के प्रति क्या नज़रिया है, इसे समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाकर कांग्रेस और आरएसएस के इतिहास को खंगालना होगा। सन् 2021 में 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो हुआ, उससे इसे समझना आसान होगा। उस दिन तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने भाजपा सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे चार किसानों पर अपनी जीप चढ़ा दी। वे चारों गाड़ी के नीचे आकर मारे गए।
हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भाजपा के हर नेता की कथनी, करनी और सोच आरएसएस के प्रशिक्षण पर आधारित होती है। अजय मिश्रा और उनके पुत्र उसी संघ से निकले हैं। न तो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने और ना ही महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने इन हत्याओं की निंदा की। इस घटनाक्रम से यह प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर आरएसएस भारत के उत्पादक वर्ग के लोगों को कैसे देखता है? उसे यह पता है कि किसानों और कारीगरों में से अधिकांश शूद्र या दलित हैं। ऐसे में यह शंका पैदा होती है कि क्या इस संगठन के हाथों में मानवाधिकार, लोकतंत्र और भारत का संविधान सुरक्षित हैं?
आइये हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस – जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और जिसने हमारे देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा – और आरएसएस के बीच तुलना किसानों और अन्य उत्पादक वर्गों के प्रति दोनों के रवैये के आधार पर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की स्थापना भारतीय और स्कॉटिश स्वतंत्रता प्रेमियों ने मिलकर 1885 में की थी। कांग्रेस के संस्थापकों में दादाभाई नैरोजी, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम और दिनशा इडलजी वाचा इसके संस्थापकों में से थे। दादाभाई नौरोजी एवं दिनशा वाचा दोनों पारसी थे और ह्यूम स्कॉटिश स्वतंत्रतावादी थे। शुरुआत में कांग्रेस में कोई ब्राह्मण या बनिया नेता नहीं था। फ़िरोज़शाह मेहता नामक एक और पारसी नेता व वकील भी कांग्रेस के लिए काम करते थे।
उस समय देश में ऐसे कई ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ और खत्री वकील थे, जो इंग्लैंड में पढ़े थे। अंग्रेजी जानने वाले अधिकांश द्विज औपनिवेशिक सरकार में तब से अधिकारियों के रूप में काम करते आ रहे थे जब प्रशासन की भाषा फारसी हुआ करती थी और यह सिलसिला 1835 में अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बना देने के बाद भी जारी रहा।[3] शुरुआत में द्विज कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनका करियर ख़राब हो जाएगा। हां, पार्टी के मजबूत हो जाने के बाद वे उसमें शामिल हुए और उसके नेता बने।

अंग्रेजी भाषा शूद्र किसानों की पहुंच से दूर बनी रही। सन् 1827 में जन्मे महात्मा जोतीराव फुले पहले ऐसे शूद्र किसान थे, जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान था। मगर वे भी केवल सातवीं कक्षा तक पढ़े थे। अधिकांश शूद्र या तो किसान थे या कारीगर। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने से कभी गुरेज नहीं किया। सन् 1885 के पहले भी भारत के कई इलाकों में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए लगान के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया था। इनमें से बारडोली और चंपारण में हुए विद्रोह सबसे जानेमाने हैं।
वल्लभभाई पटेल, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस की सदस्यता ली, उन शुरुआती शूद्र किसानों में से एक थे, जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण की और वकील बने।[4] यद्यपि अन्य शूद्रों ने 1909 के आसपास दक्षिण भारत, विशेषकर मद्रास प्रांत, में शूद्र (गैर-ब्राह्मण) आंदोलन चलाए, मगर अखिल भारतीय पहचान वाले पहले शूद्र नेता पटेल ही थे।
उन्होंने कांग्रेस और महात्मा गांधी को सिखाया कि किसानों को कैसे लामबंद किया जाता है। वे एक अच्छे वकील थे, उनकी खासी प्रैक्टिस थी और उन्होंने गुजरात में खेडा और बारडोली सहित कई किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। सिर्फ वे ही गांवों और वहां के किसानों में पार्टी की अच्छी पैठ बना पाए। वे एक ऐसे बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते थे, जो उन वर्गों की लड़ाई लड़ते थे, जिनसे वे स्वयं आते थे। यद्यपि पार्टी के अंदर वे दक्षिणपंथी धारा लेकर आगे बढ़े। केवल 1931 में ही वे कांग्रेस के अध्यक्ष बन सके। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पहले किसान अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद अपने भाषण में उन्होंने कहा– “आपने एक मामूली किसान को वह उच्चतम पद दिया है, जिस तक पहुंचने की उम्मीद हर भारतीय करता है।”[5]
इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं– “सन् 1931 तक कांग्रेस का गठन हुए चार दशक बीत चुके थे। लेकिन इस लंबी अवधि में उसने इसके पहले तक किसान परिवार में जन्मे किसी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नहीं चुना था – और यह महात्मा गांधी के इस दावे और आह्वान के बावज़ूद था कि भारत अपने गांवों में रहता है।”[6]
आरएसएस की स्थापना सन् 1925 में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने की थी। इस संगठन में किसी भी स्तर के किसी भी पद पर मुसलमान तो छोड़िए, कोई पारसी, सिक्ख या बौद्ध भी नहीं था। संघ की विचारधारा को स्पष्ट करने वाले किसी भी दस्तावेज में किसानों के बारे में कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा गया था और उसने पटेल के नेतृत्व वाले किसी किसान आंदोलन में भागीदारी नहीं की। स्वाधीनता के बाद भी उसने कभी किसानों का कोई आंदोलन या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया। यह सचमुच एक पहेली है कि इसके बावजूद शूद्र – जो काम-धंधे के स्तर पर मुख्यतः किसान और शिल्पकार हैं – संघ द्वारा राममंदिर का मसला उछालते ही उसकी गोद में क्यों आ बैठे?
“एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक प्राचीन विरासत” का नारा देने वाले आरएसएस ने अपने 99 साल के इतिहास में किसी किसान को अपना मुखिया नहीं बनाया। लगता है कि संघ की निगाहों में किसान न तो राष्ट्र का हिस्सा हैं और ना ही उसकी प्राचीन विरासत का भाग हैं। यह है आरएसएस और कांग्रेस के बीच का फर्क। कांग्रेस ने अपने लंबे इतिहास में कई किसान संघर्षों का नेतृत्व किया और उनमें भागीदारी की।
किसानों के आंदोलनों – और वह भी ऐसे मुद्दों जो उनके लिए जीने-मरने का प्रश्न थे – को दक्षिणपंथी देशद्रोह मानते हैं। मानो हिंदुस्तान उन मुट्ठी भर हिंदुत्ववादी द्विजों का है, जिन्हें किसानी से कोई मतलब नहीं है। शायद खेती उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा नहीं है। उनका राष्ट्रवाद मंदिरों तक सीमित है, जिनके मुखिया किसान पुत्र नहीं हो सकते। उनका राष्ट्रवाद उन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से उपजा है, जो खेती और शूद्रों व दलितों की बात तक नहीं करते।
आशीष मिश्रा को यह हिम्मत किसने दी कि वे देश के अन्नदाताओं को सड़कों पर भटकते आवारा कुत्तों के मानिंद अपनी गाड़ी से कुचल सकते हैं? यह हिम्मत उन्हें आरएसएस की इसी विरासत ने दी – उस विरासत ने, जो जातिवादी और वर्चस्ववादी संस्कृति पर आधारित है और जो अहंकारी व्यवहार का समर्थन करती है। आरएसएस को किसानों और खेती से ज़रा भी अनुराग नहीं है। मगर फिर भी वह किसानों के समर्थन से देश पर राज कर रहा है। यह एक अजीबोगरीब विरोधाभास है।
शूद्र और शिक्षा
शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार अंग्रेजों द्वारा देश में अंग्रेजी स्कूल खोले जाने के बाद ही मिला। ब्राह्मणों ने शूद्रों को कभी शिक्षा हासिल करने की अनुमति नहीं दी। वह इसलिए क्योंकि अगर उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाता तो उन्हें आध्यात्मिक, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अधिकार भी देने पड़ते। ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा को उच्च दर्जा दिया, उसे देवभाषा घोषित कर दिया और शूद्रों को संस्कृत विद्यालयों में प्रवेश पर सख्त पाबंदियां लगा दीं। अगर प्राचीन काल से शूद्र पढ़े-लिखे होते तो वे अपने बारे में लिखते। वे यह लिखते कि वे देश को किस रूप में देखते हैं। वे देश में और वैश्विक, अध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपने लिए जगह बना पाते।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सभी हिंदू देवी-देवता या तो ब्राह्मण हैं या फिर क्षत्रिय। जब ब्राह्मणों ने यह नीति बनाई कि यदि कोई शूद्र असाधारण वीरता का प्रदर्शन करता है तो उसे क्षत्रिय का दर्जा देकर राजा बनने की इजाजत दी जा सकती है, तब भी ऐसे राज्यों में ब्राह्मणवादी पौराणिक देवी-देवताओं को सबसे उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठापित किया गया। भले ही राजा कोई शूद्र हो, मगर उसके राज्य में भी शूद्र किसान और कारीगर मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। शूद्रों का आध्यात्मिक जीवन, कृषि से जुड़े देवों तक सीमित था। बाद में मुसलमानों के शासन और भक्ति आंदोलन के चलते उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने की इजाजत मिल गई। ब्राह्मण व क्षत्रिय द्वारा मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति शूद्रों को देने के पीछे मुख्यतः उनका यह डर था कि कहीं शूद्र समुदायों के लोग इस्लाम न अपना लें। मगर दलितों के मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध फिर भी जारी रहा।
ईश्वर और श्रम
ईश्वर ने यह नियत किया है कि सभी मनुष्यों को श्रम करना चाहिए और अपने पसीने की कमाई से जीवनयापन करना चाहिए। मनुष्यों के श्रम से ही फल, खाद्यान्न, सब्जियां और मांस मानव जीवन का हिस्सा बने हैं। ईश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वह खेतों में काम न करे और केवल एक कमरे में बैठकर किताबें पढ़ता रहे या मंत्रों का जाप करता रहे। बाइबिल की ‘उत्पत्ति’ में बताया गया है कि ईश्वर ने 6 दिनों तक मेहनत करके इस दुनिया को बनाया और फिर सातवें दिन आराम किया।
यह कहानी काल्पनिक हो सकती है। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि खुदा और उसके बंदों दोनों को काम करना चाहिए। भारतीय ब्राह्मणवाद में श्रमजीवी ईश्वर की कोई परिकल्पना ही नहीं है। यह कथा कि 6 दिनों तक काम करने के बाद सातवें दिन ईश्वर ने आराम किया, हमें यह बताती है कि और काम करने के लिए ताजादम होना ही आराम का एकमात्र उद्धेश्य है। यह विचार कि ईश्वर स्वयं श्रम करता है, सभी लोगों को यह प्रेरणा देता है कि वे भी मेहनत से अपनी रोजी-रोटी कमाएं। ब्राह्मणवाद उत्पादक श्रम से जुड़े हुए किसी भी सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता। कोई ब्राह्मणवादी पुस्तक हमें यह नहीं बताती कि आखिर बिना उत्पादन के कोई समाज कैसे जिंदा बना रह सकता है।
शूद्रों और दलितों को बिना आराम किए सातों दिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मगर ब्राह्मणों को कोई काम नहीं करना होता। वे सातों दिन आराम करते हुए केवल खाने-पीने का मजा ले सकते हैं। बीच-बीच में किसी न किसी देवी-देवता के नाम पर दावतें भी होती रहती हैं। इस तरह की आध्यात्मिकता मनुष्यों की दुनिया को खत्म कर देगी। चाहे कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो या बौद्ध, उसे यह विश्वास होना चाहिए कि जीवन में श्रम करना आवश्यक है। हिंदुओं की आध्यात्मिक-सांस्कृतिक दुनिया में शूद्रों और दलितों को इसलिए निम्न दर्जा दिया गया है, क्योंकि केवल वे ही वह काम – अर्थात श्रम – करते थे, जिसके लिए ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। वे खेतों में काम करते थे, मवेशी चराते थे, बर्तन और कालीन बनाते थे, फल इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे, चमड़े का काम करते थे और उत्पादक कामों के लिए जरूरी औजार बनाते थे। और यह सब वे बिना आराम किए करते थे।
दुनिया में कहीं भी स्पर्श से प्रदूषण की संकल्पना नहीं है। पवित्रता औैर प्रदूषण जैसी परिकल्पनाओं के लिए किसी आध्यात्मिक प्रणाली में जगह नहीं है। मगर ये ब्राह्मणवादी आस्था का हिस्सा हैं। भारत के द्विजों ने जो किया वह सर्वव्यापी ईश्वर कभी नहीं चाह सकता। ब्राह्मणवादी मूल्य, अन्य धर्मों के मूल्यों से एकदम अलग हैं। हम अन्य मनुष्यों से प्रेम करें या न करें इसका संबंध केवल ब्राह्मणों की पवित्रता और अपवित्रता की परिकल्पनाओं से नहीं है। दूसरों से प्रेम करना – चाहे वे हमारे पड़ोसी हों या हमसे बहुत दूर रहने वाले लोग – मानवता को बचाए रखने और उसकी भलाई और कल्याण के लिए आवश्यक है। चाहे आपका धर्म कोई भी हो – हिंदू, ईसाई, इस्लाम या बौद्ध – हम सबको श्रम करना चाहिए और मानवीय मूल्यों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। आरएसएस की धार्मिक और राष्ट्रवादी विचारधारा उन लोगों से घृणा करने पर आधारित है जो भोजन का उत्पादन करते हैं। यह विचारधारा द्विजवाद से अतिशय प्रेम करती है। भारत अगर इस विचारधारा पर चलेगा तो वह एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकेगा।
शूद्र दर्शन और दलितों की मुक्ति
शूद्रों को अपने दर्शन को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि वे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने न केवल अपने श्रम वरन् अपने आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक दर्शन से इस राष्ट्र का निर्माण किया है।
उनका दर्शन ब्राह्मणवादी पुस्तकों के ढांचे से बाहर है। जब तक शूद्र अपने आपको ब्राह्मणवाद की बेड़ियों से मुक्त नहीं कर लेते तब तक जातिगत भेदभाव और अछूत प्रथा जैसी बीमारियों से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। आंबेडकर जब ‘जाति के विनाश’ की बात करते हैं तो वे केवल दलितों की बात नहीं करते। जाति का विनाश केवल दलितों का एजेंडा नहीं है। भविष्य में भारत की शिक्षा प्रणाली को शूद्र दर्शन से जोड़ना होगा तभी भारत दुनिया का एक मजबूत और कार्यकुशल देश बन सकेगा।
पहचान और मुक्ति दो भिन्न धारणाएं हैं। मुक्ति के लिए पहचान का निर्माण अपरिहार्य है। मगर केवल पहचान के निर्माण से मुक्ति हासिल नहीं होगी। आरएसएस के प्रभाव से मुक्त दलित चिंतक तर्क देते हैं कि उन्हें बौद्ध धर्म के रूप में एक स्वतंत्र अध्यात्मिक प्रणाली उपलब्ध है, इसलिए उन्हें ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व की खिलाफत करने की ज़रूरत नहीं है। बौद्ध धर्म के रूप में एक स्वतंत्र आध्यत्मिक प्रणाली दलितों को आंबेडकर की भेंट है और उसे नवायन बौद्ध धर्म कहा जाता है। मगर बौद्ध धर्म और विशेषकर नवयान बौद्ध धर्म को हिंदुओं द्वारा ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के हिस्से के बतौर देखा और माना जाता है। यह इस तथ्य के बावजूद कि वह वैदिक हिंदू आध्यात्मिक प्रणाली और उसके मूल्यों के खिलाफ है। इसी कारण आंबेडकर ने उसे अपनाया था। बौद्ध धर्म के हिंदू धर्म का भाग होने के बारे में आरएसएस के ब्राह्मणवादी प्रचार के अलावा एक कांग्रेसी ब्राह्मण जयराम रमेश की हालिया पुस्तक ‘द लाइट ऑफ़ एशिया : द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा’, जो एडविन अर्नाल्ड की रचना ‘द लाइट ऑफ़ एशिया’ पर आधारित है, बताती है कि किस तरह इस अंग्रेज़ औपनिवेशिक कवि ने अश्वघोष के ‘बुद्धचरित’ के तर्ज पर, बुद्ध को एक हिंदू देव बताया है।[7] यह वह एकमात्र कारण था जिसके चलते इस कविता ने महात्मा गांधी, विवेकानंद और अन्यों को प्रभावित किया।
बहुत लंबे समय तक धर्मनिरपेक्षता पर देशव्यापी विमर्श के चलते हिंदू धर्म में आध्यात्मिक असमानता को नज़रअंदाज़ किया जाता रहा। धर्मनिरपेक्षता पर विमर्श पर भी द्विज अध्येताओं, राजनेताओं और अन्य द्विजवादी तंत्रों का कब्जा था। उन्होंने कभी आध्यात्मिक प्रणाली और उत्पादन के परस्पर रिश्तों के संबंध में कोई सार्थक विमर्श होने ही नहीं दिया। कोई धर्म और कोई राष्ट्र ऐसे सामाजिक समूहों को स्वीकार नहीं कर सकता है, जो न तो शारीरिक श्रम करते हों और ना ही भोजन के उत्पादन में उनकी कोई साझेदारी हो। उलटे वे केवल संपत्ति इकट्ठा करते रहें। और वह भी झूठे और अनैतिक आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर – जैसे यह कि खाद्यान्न उत्पादन में भागीदारी प्रदूषित करती है और यह भी कि लोग गैर-बराबर होते हैं और कुछ को तो छुआ ही नहीं जा सकता। ब्राह्मणों का बहुसंख्यक भारतीयों पर नियंत्रण था और वे उन्हें गुलाम या अर्द्ध-गुलाम मानते थे। हांलाकि आरएसएस-भाजपा यह नहीं कर सकते, मगर चूंकि वे हिंदुत्ववादी धार्मिक एजेंडा को लागू करने के घोषित उद्देश्य से सत्ता में हैं, इसलिए यह बात पूरे दमखम से कही जानी चाहिए कि हिंदू भारत में जो अन्याय सदियों से जारी थे, वह अब और जारी नहीं रह सकते।
जाति और अछूत प्रथा जैसी समस्याओं की जड़ धर्म में है और धर्म से ही उनका स्थायी समाधान हो सकता है।
बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक
धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी और वामपंथी बुद्धिजीवी में से अधिकांश द्विज पृष्ठभूमि से हैं। उन्होंने हिंदुत्व के लिए एक भ्रामक शब्द गढ़ा है – बहुसंख्यकवाद। यह अवधारणा भारत के मुसलमानों और ईसाइयों – जो इस समय एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं – को भी पसंद आ रही है। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों की अल्पसंख्यक बतौर स्थिति का वैश्विक महत्व है, क्योंकि भारत को 1947 में हिंदू-मुसलमान के आधार पर ही विभाजित किया गया था, जिसके बाद लाखों लोग अपने घर-बार छोड़ने को मजबूर हुए थे और भयावह दंगों में अनगिनत जाने गईं थीं। ऐसे में अगर धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी और वामपंथी लेखक पीड़ित अल्पसंख्यकों के साथ खड़े दिखते हैं तो उन पर पूरी दुनिया की निगाह जाती है।
मगर समस्या यह है कि बहुसंख्यकवाद पर विमर्श से जाति-आधारित असमानता और शोषण जैसी समस्याओं का हल नहीं होता, क्योंकि यह विमर्श जाति और अछूत प्रथा जैसी समस्याओं पर बात ही नहीं करता। ऋग्वेद के लेखनकाल से शुरू हुए धार्मिक विमर्श और आचरण में हमेशा से द्विजों का बोलबाला रहा है। संस्कृत साहित्य और धर्म पर उन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया था। यह वर्चस्व आज भी कायम है और हिंदुत्ववादियों के सत्ता में आने के कारण उसकी पकड़ और मजबूत हुई है। मुसलमानों के आने के पहले भारत पर ब्राह्मणवाद का संपूर्ण कब्जा था और जाति और अछूत प्रथा ने संस्थागत स्वरूप ले लिया था। मध्यकाल में मुसलमानों के शासन के दौरान भी मुस्लिम राजाओं और ज़मीदारों ने शूद्र, दलित और आदिवासी समुदायों को कोई राहत नहीं दी। मुस्लिम अध्येताओं और शायरों ने जाति और अछूत प्रथा जैसी बर्बर व्यवस्थाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा। भारत के इतिहास से हमें यह कहीं पता नहीं चलता कि मुसलमानों ने फारसी या उर्दू भाषा के स्कूलों में गैर-द्विजों को भर्ती करने का कोई प्रयास किया हो। कहने की जरूरत नहीं कि अशिक्षित और अज्ञानी सामाजिक समूह कभी अन्याय के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। शूद्र, दलित और आदिवासी तबकों में वह बौद्धिक शक्ति ही नहीं थी, जिसके चलते वे राष्ट्रीय और वैश्विक विमर्श में अपना हिस्सा मांग सकते थे। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में शूद्र, दलित और आदिवासी समुदायों से कोई राजनीतिक नेता, समाज सुधारक या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं निकला। मगर जब किसी समुदाय के अधिकांश सदस्य अशिक्षित हों और केवल खेती, कारीगरी और पशुपालन का काम करते हों तो वह समुदाय सुधार या परिवर्तन के आह्वान पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। उस समय ईसाई धर्म जैसी कोई धार्मिक संस्था भी नहीं थी। ईसाई धर्म ने इन समुदायों को हर हफ्ते के अंत में मिलने-जुलने का अवसर प्रदान किया, जिससे आधुनिक काल में इन वर्गों में साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना जागी। हिंदू धर्म में सामूहिक रूप से साहित्यिक, सामाजिक या सांस्कृतिक ज्ञान पाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। स्वभाविक तौर पर शूद्र वही करते रहे जो ब्राह्मण पुरोहित उनसे कहते थे। आधुनिक काल में केवल एक ऐसा शूद्र आंदोलन हुआ, जिससे व्यापक सामाजिक परिवर्तन आया। वह आंदोलन था पेरियार रामासामी नायकर का आंदोलन। मगर वह केवल मद्रास प्रांत और उसके भी तमिल क्षेत्र तक सीमित था। पेरियार ने नास्तिकतावाद से उपजने वाली समस्याओं का हल भी निकाला। यह इसलिए आवश्यक था, क्योंकि नास्तिकतावादियों को कोई ऐसे लिखित ग्रंथ उपलब्ध नहीं रहते, जिन्हें पढ़कर वे कुछ सीख-जान सकें।
ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भी शूद्र, दलित और आदिवासी तबकों पर द्विजों का नियंत्रण समाप्त नहीं हुआ। संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाएं बौद्धिक, सामाजिक और प्रशासनिक विमर्श का माध्यम थीं। इन तीनों पर द्विजों का नियंत्रण था। द्विज जातियों का अंग्रेजी पर एकाधिकार है। इससे हमें यह समझ में आता है कि उन्हें एक वैश्विक भाषा सिखाकर औपनिवेशिक शासन ने उन्हें कितना लाभ पहुंचाया है। विदेशों में शिक्षा प्राप्त अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वालों, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वालों और दुनियाभर में काम करने वाले भारतीयों में द्विजों की भारी संख्या से यह साफ है। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद जब उस दौर में देश को हुई क्षति की भरपाई की बात आई तब उस विमर्श में भी जाति का विरोध और शूद्रों, दलितों और आदिवासियों की स्थिति में बेहतरी लाने जैसे मुद्दे शामिल नहीं थे। उलटे आधुनिकतावादी एवं उत्तर-आधुनिकतावादी विमर्श ने भारतीय समाज में व्याप्त आंतरिक वर्चस्ववाद और द्विजों द्वारा उत्पादक शूद्र, दलित और आदिवासी तबकों के शोषण पर पर्दा ही डाला।
संदर्भ :
[1] हिंदू धर्म ग्रंथ ‘महाभारत’ में कृष्ण को यदुवंशी कहा गया है। हालांकि ग्रंथों में वर्णित उनके कृत्य ब्राह्मण व क्षत्रिय के हितार्थ हैं।
[2] आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गांवों में कृषक समुदायों द्वारा पूजी जानेवाली एक लोक देवी। बरगद के पेड़ के नीचे इनकी प्रतिमा रखी जाती है। इनकी पूजा के लिए हल्दी और नीम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस लोक देवी को मांस (चिकेन व मटन) भी अर्पित किया जाता है।
[3] कोचर. आर., (2020), इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, 1715-1835: हाफ कास्ट, मिशनरी एंड सेक्युलर स्टेजेस, रूटलेज इंडिया
[4] इनके बारे में विस्तार से चर्चा आठवें अध्याय में है।
[5] द टेलीग्राफ, 7 फरवरी, 2022 https://www.telegraphindia.com/opinion/vallabhbhai-patel-and-the-peasantry/cid/1833926
[6] रामचंद्र गुहा (10 अक्टूबर, 2021), रामचंद्र गुहाः वॉट टूडेज़ फार्म प्रोटेस्ट्स शेयर विथ वल्लभभाई पटेल्स बारडोली सत्याग्रह, द स्क्रॉल डॉट इन, https://scroll.in/article/1007334/ramachandra-guha-what-todays-farm-protests-share-with-vallabhbhai-patels-bardoli-satyagraha
[7] जयराम रमेश (2021), द लाईट ऑफ एशिया–ए पोयम देट डिफाइन्ड बुद्धा, पेंगुइन
(यह आलेख प्रो. कांचा आइलैय्या शेपर्ड द्वारा लिखित किताब ‘द शूद्रा रिबेलियन’ में संकलित पहले अध्याय ‘दी शूद्राज इन हिंदुत्व : लिविंग विदाउट अ सोल’ का हिंदी अनुवाद है, जिसे हम लेखक व प्रकाशक की अनुमति से प्रकाशित कर रहे हैं)
(अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : राजन/नवल/अनिल)