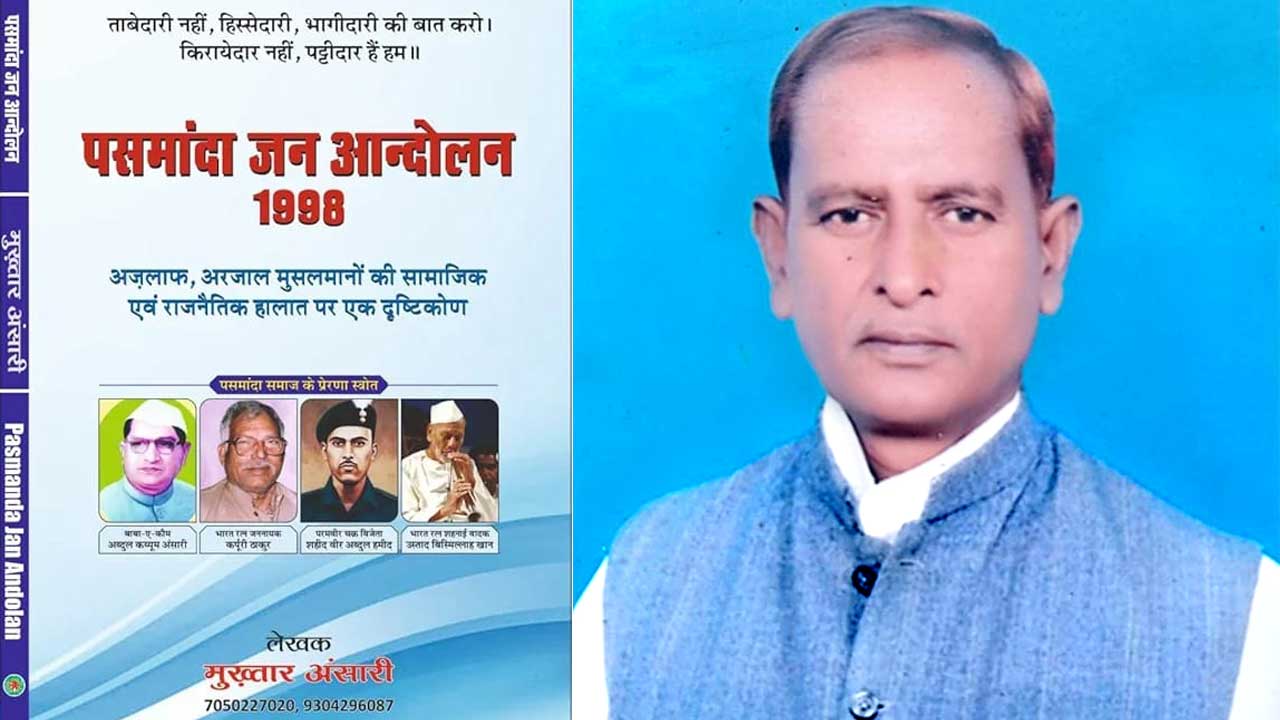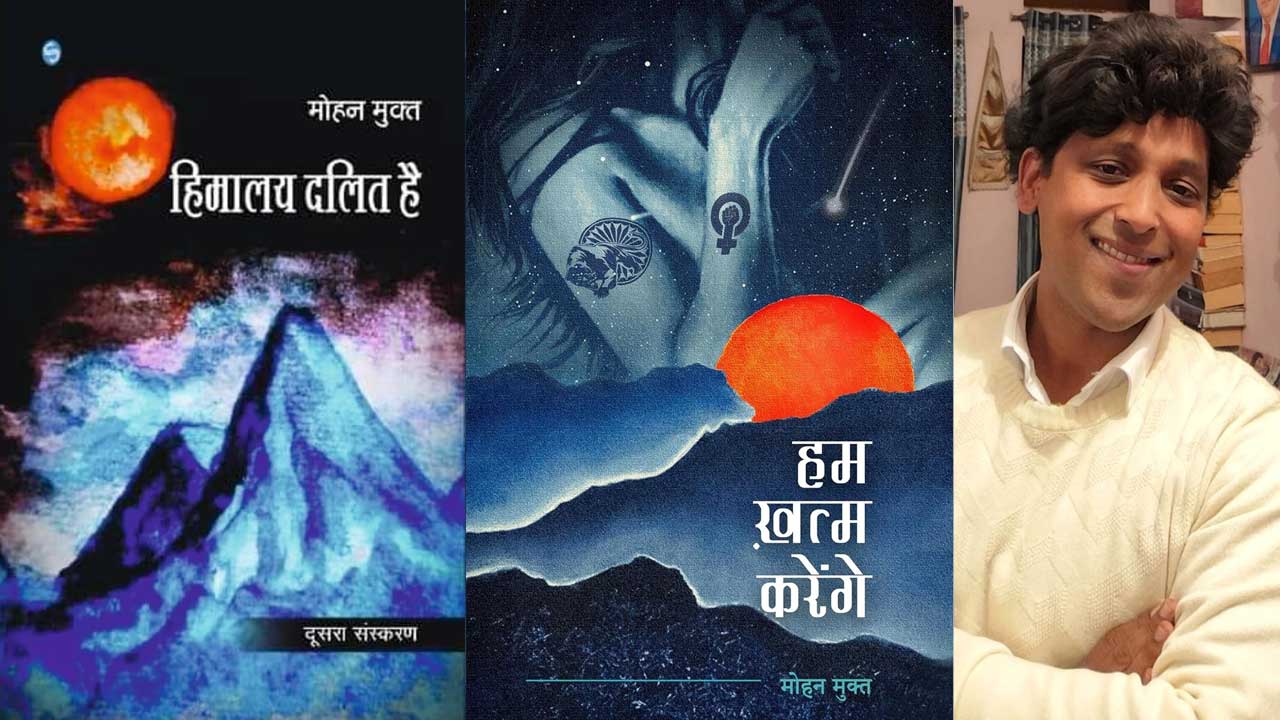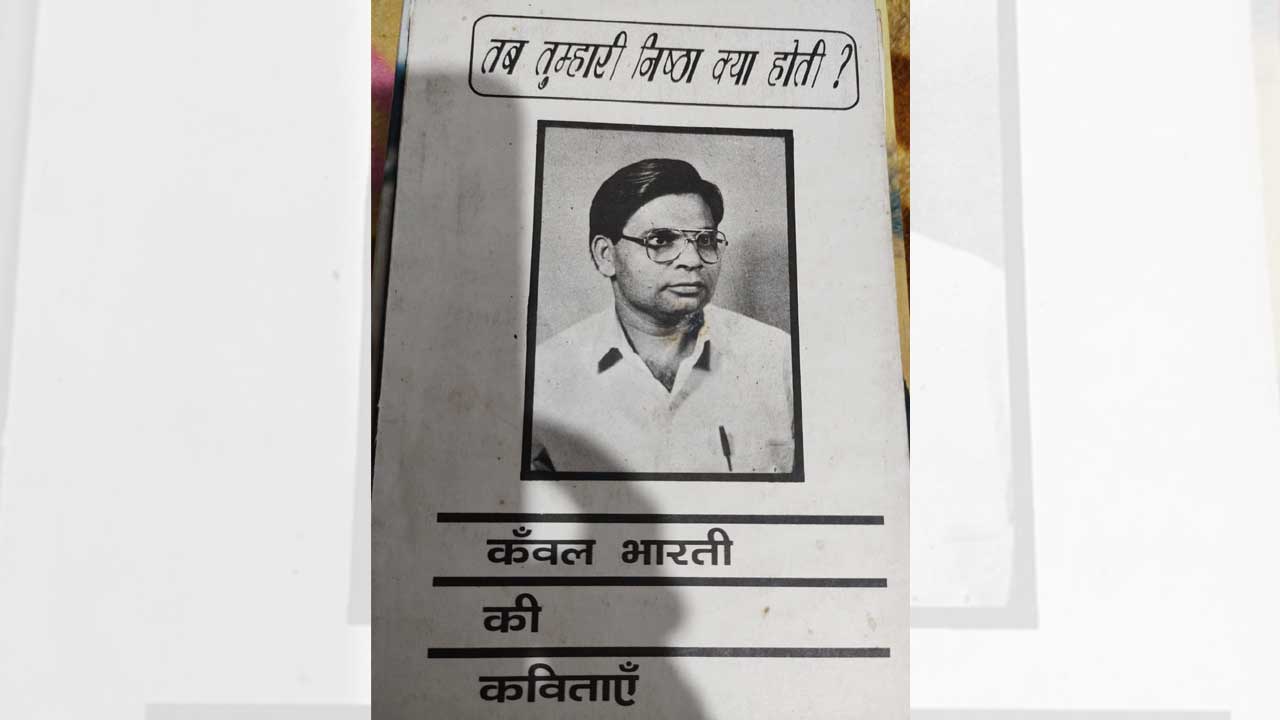पहले भाग से आगे
जयशंकर प्रसाद को पुनरुत्थानवादी लेखक माना गया है। उन्होंने कालखंड विशेष से संबंधित ‘अजातशत्रु’, ‘चंद्रगुप्त’ और ‘स्कंदगुप्त’ आदि अनेक नाटक लिखे, लेकिन अशोक को छोड़ दिया था। साफ है कि अशोक उनकी हिंदु पुनरुत्थानवादी नीति का हिस्सा नहीं था। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना व्यर्थ है कि उन्होंने शताब्दियों पहले विस्मृति-गर्त में समा चुके आजीवक दर्शन को चर्चा में लाने के लिए तत्संबंधी प्रसंग को ‘चंद्रगुप्त’ का हिस्सा बनाया होगा। गोकुलनाथ के ‘अमृतोदय’, नारायण भट्ट के ‘वेणीसंहार’ और कृष्ण मिश्र के ‘प्रबोधचंद्रोदय’ आदि अनेक नाटकों में आजीवकों (नास्तिकों) की सीधी या प्रतीकात्मक उपस्थिति है। सभी में नाटककारों की दृष्टि उसे वैदिक धर्मों की तुलना में हेय सिद्ध करने की रही है। ‘युगीन परंपरा’ के अनुरूप प्रसाद की रचनाओं में भी आजीवकों के साथ वैसा ही सुलूक हुआ है। लेकिन संस्कृत नाटककारों/लेखकों ने सीधे नाम लेने के बजाय मायामोह, महामोह, पाषंड, चार्वाक, नास्तिक, बार्हस्पत्य आदि प्रतीकों का प्रहसननुमा उपयोग किया था। वहीं जयशंकर प्रसाद उसके प्रतिनिधित्व के लिए सीधे आजीवक भिक्षुओं को कथानक का हिस्सा बना लेते हैं; और बीसवीं शताब्दी में हिंदी पाठकों को याद दिला देते हैं कि भारत में एक समय आजीवक नाम की भी श्रमण परंपरा थी।
कदाचित उन्हें लगा था कि ऐसा करना नाटक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को वास्तविकता के करीब ले जाएगा। वे गलत भी नहीं थे। ‘चंद्रगुप्त’ नाटक का बड़ा हिस्सा नंद के शासन में घटता है, जब आजीवक राज्य का प्रमुख धर्म था, इस कारण इसे अन्यथा भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में नाटक से इन दृश्यों का हटाया जाना कई प्रश्न छोड़ जाता है। खासतौर पर यह देखते हुए कि पहले तथा दूसरे संस्करण के बीच मात्र एक वर्ष का अंतर है।[1]
जहां तक जयशंकर प्रसाद का सवाल है, उन्हें इन तीन दृश्यों में आए पात्रों ‘आजीवक’, ‘धनदत्त’, ‘मणिमाला’ तथा ‘चंदन’ से बहुत अनुराग रहा होगा। ये चारों पात्र अपने उसी विशिष्ट चरित्र के साथ उनके अधूरे उपन्यास ‘इरावती’ के कथानक का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। अधूरा होने के कारण यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि उपन्यास यदि लेखक के जीवनकाल में पूरा हो गया होता तो उसकी वर्तमान सामग्री ठीक उसी रूप में रहती, जिस रूप में वह फिलहाल प्राप्त है, लेकिन इससे उनके द्वारा, आजीवक दर्शन के बारे में जानने के लिए जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के गहन अध्ययन की पुष्टि हो जाती है।
‘इरावती’ की विषयवस्तु उस दौर की है जब मौर्य शासन कमजोर हाथों में था। उसका पुराना वैभव समाप्त हो रहा था। जिस कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने लंबा युद्ध लड़ा था, वहां का शासक खारवेल सिर उठा रहा था, और कमजोर शासक के चलते मगध की जनता के मन में यवन आक्रमण का भय समाया हुआ था। वास्तविक सत्ता सेनापति पुष्यमित्र शुंग के हाथों में थी। ब्राह्मण आश्रमों को छोड़कर सत्ता के इर्द-गिर्द संगठित होकर शक्ति बढ़ाने में लगे थे। आजीवक, जैन, बौद्ध जैसे श्रमण परंपरा के प्रमुख दर्शनों को तीखी आलोचना से गुजरना पड़ रहा था। उपन्यास में आए ‘कुकुरवृत्ति’, पाखंड (पाषंड), ‘नियतिवादी’ जैसे शब्द तत्कालीन समाज में श्रमण दर्शनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का एहसास कराते हैं।

उपन्यास की कथानायिका इरावती देवदासी है। देव-मंदिर की नृत्यांगना। एक बार उसका संपर्क बौद्ध भिक्षु से होता है। उसके प्रभाव में वह मंदिर छोड़, भिक्षु संघ में बिना दीक्षा-उपसंपदा के रहने लगती है। वहां वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। एक बार एक शैव साधु वहां आता है। इरावती उससे संवाद करने लगती है। वह शैव-साधक के आनंदवाद के दर्शन से असहमत थी, फिर भी भिक्षु संघ की ओर से उसपर, ‘अपरिचित पाखंड की पापमति से प्रभावित’ होने के आरोप लगाकर प्रायश्चित करने को कहा जाता है। इरावती प्रायश्चित करने के बजाय संघ से प्रस्थान कर जाती है।[2] यहां भिक्षु के मुंह से, दूसरे भिक्षु के लिए ‘पाखंड’ संबोधन से चौंकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज विभिन्न धर्मों में स्पर्धा चलती है, उन दिनों भी चलती थी। बुद्ध ने बाकी सभी धर्मों को ‘मिथ्यादृष्टि’ कहा है। यही उनके धर्म के बारे में दूसरे मतावलंबियों का विचार था।
कथ्य की समानता
‘इरावती’ का धनदत्त ‘चंद्रगुप्त’ के धनदत्त जितना ही धनाढ्य था। ‘चंद्रगुप्त’ के धनदत्त के तीन भूगर्भ सोने से भरे हैं, ‘इरावती’ के धनदत्त के पास भी ठीक उतनी ही संपदा है। ‘चंद्रगुप्त’ के धनदत्त का ‘आजीवक भिक्षु’ विश्वासी मित्र था, ‘इरावती’ के धनदत्त की भी आजीवक से मैत्री थी। ‘चंद्रगुप्त’ में धनदत्त की पत्नी मणिमाला कुछ समय के लिए गायब होकर आजीवक की मदद से लौट आती है। ‘इरावती’ में भी ठीक यही घटनाक्रम है। ‘चंद्रगुप्त’ का आजीवक बात-बात पर नियतिवाद का हवाला देता था, ‘इरावती’ का आजीवक भी नियतिवाद की रट लगाए रहता है– ‘मनुष्य कुछ कर नही सकता’, ‘मैं तो नियतिवादी हूं, जब सोना होगा सो जाऊंगा’, ‘आगे जाने नियति। लाखों योनियों में भ्रमण कराते-कराते जैसे यहां तक ले आई है वैसे और भी जहां जाना होगा’। ऐसे कथन ईसापूर्व पहली-दूसरी शताब्दी में, मक्खलि गोसाल के प्रभाव की याद दिला देते हैं। यह स्वाभाविक था, क्योंकि श्रावस्ती से उजड़ने के बाद आजीवकों ने पाटलिपुत्र के दक्षिण में लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित बराबर पहाड़ी समूह को अपना ठिकाना बनाया था। जहां अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ मौर्य ने उनके लिए संगमरमर की छह गुफाएं बनवाकर दी थीं।
लगता है कि जयशंकर प्रसाद ने ‘चंद्रगुप्त’ के तीन दृश्यों में जो उपकथा सृजित की थी, उनके हटाए जाने का उन्हें मलाल था। इसलिए ‘इरावती’ में उसे नए सिरे से विस्तार देने की कोशिश की गई है। उपन्यास पूरा नहीं हो पाता। कहा जाता है कि ‘इरावती’ का लेखन कामायनी (1936) के बाद शुरू किया था। अगले ही वर्ष उनका देहांत हो जाता है। साफ है कि धनदत्त की उपकथा को वे लंबे समय तक मानस में सुरक्षित रखे हुए थे। ‘इरावती’ में वे भारत की श्रमण परंपरा के विभिन्न अपररूपों को सामने लाने की कोशिश करते हैं।
तरह-तरह के श्रमण
‘हर्षचरित’ में राज्यश्री की खोज में निकला हर्ष विभिन्न मतावलंबी श्रमणों तथा साधुओं से मिलता है। ऐसे ही इरावती की खोज में निकला अग्निमित्र बौद्धों, शैव-साधुओं, पुनर्जन्मवादियों, जटिलकों, निर्ग्रंथों तथा आजीवकों के संपर्क में आता है। इनमें ज्यादा स्पेस आजीवक को मिला है। ‘तपस्वी! तीर्थक! बड़ी-बड़ी जटा! त्यागी!’ जैसे शब्दों से जयशंकर प्रसाद आजीवक श्रमण-तीर्थंकर का मानो पूरा बिंब खड़ा कर देते हैं।[3] हालांकि यह सब वे उपन्यास के कथानक की ऐतिहासिकता को प्रामाणिक बनाने के लिए करते हैं, न कि आजीवक दर्शन से किसी भी प्रकार की सहानुभूति के चलते। यथा–
इतने में एक आजीवक उसी स्थान पर आकर चंदन से पूछने लगा– ‘धर्मशाला कितनी दूर है, उपासक?’
धनदत्त कुढ़ रहा था। उसने कहा– ‘धर्मशाला पूछते हैं आप? समूचा मगध धर्मशाला ही तो है। जहां चाहिए रहिए। पूछना क्या है, यही सुन कर तो सुदूर यवन-देश से बहुत-से अतिथि आ गए हैं।’
‘मैं आपकी बात समझ नही सका।’
‘आश्चर्य। इतनी छोटी-सी बात और इस दार्शनिक मस्तिष्क में नही आई।’
‘नही भी आ सकती है। होगी वैसी बात ही, मुझे तो धर्मशाला चाहिए, न होगा तो इसी सामने वाले चैत्य-वृक्ष के नीचे पड़ा रहूंगा।’
‘पड़े रहिए। मैं पूछता हूं कि मगध ही ऐसा अभागा देश है क्या, जहां दरिद्र दार्शनिक उत्पन्न होते हैं? जिसे कपड़ा नहीं मिला, उसने सोच लिया कि माता के गर्भ से क्या कपडे़ पहन कर आये थे। बस एक सिद्धांत बन गया, नंगे घूमने लगे। कभी धोखे से कोई मच्छर भी उन्हीं की श्वांसों से खिंचकर चला गया, बस प्राणि-हिंसा हो गई। मुंह पर कपड़े बांधकर चलने लगे। गड़ गया कांटा। ढोंग बनाया कि चीटिंयां दबती हैं। फिर तो हाथ में झाड़ू वाले दार्शनिक! सिर नही घुटा– जटाधारी अस्वस्थ हुए, पानी गरम करके पीने लगे; और ये सब सिद्धांत बन गए! वाह रे मगध!’[4]
उपर्युक्त कथन में श्रमण परंपरा के प्रति कटाक्ष देखा जा सकता है। आजीवक श्रमणों को जटिलक (जटाधारी) भी कहा गया है। जीव-हत्या न हो इस कारण वे गर्म जल का सेवन करते थे। मुंह पर पट्टी बांधकर चलने वाले श्रमणों से लेखक का आशय जैन-मुनियों से है। उनके लिए निर्ग्रंथ शब्द भी उपन्यास में आया है। नंगे घूमने वाले दार्शनिक आजीवक और जैन थे। धनदत्त का आक्रोश अपनी पत्नी से बिछुड़ जाने की परिणति था। उसे बताया गया था कि उसकी पत्नी मणिमाला किसी आजीवक के साथ चली गई है। कुछ अंतराल के बाद मणिमाला आजीवक के साथ ही लौट आती है–
‘मैंने सुना था कि तू एक आजीवक के साथ कहीं चली गई!’
‘चली गई नहीं, चली आई कहिए। वह आजीवक भी साथ है, उन्हीं की रक्षा में तो मैं जीवित रह सकी।’ उसने गाड़ी [बैलगाड़ी] की ओर देख कर पुकारा, ‘आइए आर्य।’ गाड़ी से उतर कर एक आजीवक साधु आया। उसे देखते ही पहले आजीवक ने चिल्ला कर कहा–
‘अरे मैं यह क्या देखता हूं? मेरे गुरुदेव।’
‘धनदत्त मैंने तुम्हारा कुछ लिया नहीं, यह सब लो। मैं अपनी नियति का भोग भोगने आगे बढ़ता हूं। आओ वत्स!’[5]
मणिमाला के आजीवक के साथ लौटने के प्रसंग का उल्लेख चंद्रगुप्त नाटक में भी है। वहां आजीवक नंद के सिपाहियों द्वारा मणिमाला और धनदत्त की संपत्ति लूटे जाने से बचाता है।[6]
आजीवक विरोधी माहौल
आजीवकों को जो स्वतंत्रता नंद के समय में थी, पुष्यमित्र के समय नहीं थी। बौद्ध मतावलंबियों तथा आजीवकों के लिए वह प्रतिकूल समय था। कौटिल्य पूरी श्रमण परंपरा का आलोचक था। यह कहकर कि आमजन के बीच पैठ रखने वाले आजीवकादि श्रमण, दुश्मन देश के जासूस हो सकते हैं, उसने आजीवक, बौद्ध आदि श्रमणों को घर पर आमंत्रित कर भोज कराने पर, 100 पण का जुर्माना लगाए जाने की अनुशंसा ‘अर्थशास्त्र’ में की थी।[7] यह पूरी तरह आजीवक, जैन, बौद्ध आदि श्रमण परंपरा के दर्शनों को कमजोर करने की नीति का हिस्सा था। जो गुप्तचर आजीवक, जैन आदि श्रमणों के वेश में जासूसी कर सकते थे, वे ब्राह्मण वेश में भी जासूसी करने जा सकते थे। अजातशत्रु का मंत्री वस्सकार ब्राह्मण वेश में ही वैशाली में जासूसी करने गया था। जुर्माने की गंभीरता का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि ‘अर्थशास्त्र’ के अनुसार उस समय शिल्पकार वर्ग को, जिनके बीच आजीवकों का बड़ा समर्थन था, राज्य की सेवा के लिए मात्र 48 पण वार्षिक वेतन मिलता था।
मगध में उस समय आजीवकों को लेकर वही विधान लागू था। ब्राह्मण पुष्यमित्र को आजीवकों के सफाये के लिए लगातार उकसा रहे थे। उन्हें रास्ते का कांटा बताया जा रहा था– “सेनापति! पाखंड छद्यमवेशियों से तुम्हारी राजपुरी भर गई है … यदि तुम इन कंटकों का उपाय न करोगे तो विनाश में संदेह नहीं।”[8]
उसके बाद महानायक अग्निमित्र के आदेश पर आजीवकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका पिता सेनापति पुष्यमित्र आजीवकादि श्रमणों को भिक्षा देने पर पाबंदी लगा देता है। राज्य के दबाव में धनदत्त जैसा आजीवकोपासक भी उससे किनारा करने लगता है–
‘वह कुकुरव्रती दार्शनिक तो हटता ही नहीं। उसी तरह गेंडुरी मारे दोनों केहुनियों के बल कुत्ते की तरह पड़ा है।’
‘पड़ा रहने दो।’ अन्यमनस्क भाव से धनदत्त ने कहा।
‘किंतु सेनापति की आज्ञा क्या भूल गए? ऐसे बेकार पाखंडियों को अन्न देने के लिए उन्होंने वर्जित किया है।’ चंदन ने कहा।
‘हां, उनका उद्देश्य है कि भोजन न पाने से ये सब स्वयं नगर के बाहर हो जाएंगे।’[9]
जैन ग्रंथों में आजीवकों की विचित्र साधनाशैलियों की चर्चा की है। उन्हीं में से एक था भिक्षान्न को हथेली पर लेकर, बिना हाथ लगाए बिना सीधे मुंह से खाना। उनमें कुछ ऐसे थे जो भिक्षान्न को जमीन पर रखवा लेते, फिर सीधे मुंह से उठाकर खाते थे। पहले वालों को हाथ-चट्टा या हथेली चट्टा तथा दूसरी श्रेणी के श्रमण कुकुरव्रती कहे जाते थे। उपन्यास में बौद्धविहार को कुक्कुटाराम नाम दिया गया है। जबकि कुक्कुटाराम, कुक्कुटनगर आदि का संबंध बौद्ध धर्म से ज्यादा आजीवकों से था।
जिस दौर में प्रसाद ने इन कृतियों की रचना की, वह भी सांस्कृतिक-राजनीतिक उथल-पुथल का था। आजादी की लड़ाई अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आड़ में जातिवादी ताकतें सत्ता शिखरों को कब्ज़ा लेना चाहती थीं। तत्कालीन लेखकों और बुद्धिजीवियों के बड़े वर्ग का उन्हें समर्थन था। उनकी सारी कोशिश ब्राह्मणधर्म की पुनर्वापसी थी। ब्राह्मणवाद तथा उससे उपकृत शक्तियां, बुद्धि और छल-बल द्वारा विदेशी शासकों के दौर में हुए नुकसान की भरपाई में लगी थीं। ऐसे में जातिवाद विरोधी, युद्ध विरोधी, वेद तथा याज्ञिक कर्मकांडों के विरोधी, पाप-पुण्य-तीरथ-दान के धुर-विरोधी आजीवक दर्शन को, जिसे शताब्दियों पहले यत्नपूर्वक, तरह-तरह के लांछनों के साथ विमर्श से गायब कर दिया गया था दुबारा विमर्श के केंद्र में लाना, वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देने जैसा था। शायद इसीलिए ‘चंद्रगुप्त’ के लेखक की इच्छा/अनिच्छा से उसे, नाटक के प्रकाशित हो जाने के बावजूद उससे हटाया/हटवाया गया। यह लेखक का उस उपकथा तथा उसके पात्रों से मोह था, जिसने उसे अप्रकाशित उपन्यास के हिस्से के रूप सुरक्षित रखा।
[1] चंद्रगुप्त मौर्य, shorturl.at/3E8Ma
[2] जयशंकर प्रसाद, इरावती [1967 : 57-59], भारती भंडार, इलाहाबाद, https://www.hindwi.org/ebooks/irawati-ebooks
[3] जयशंकर प्रसाद, इरावती [1967 : 57-59]
[4] जयशंकर प्रसाद, इरावती [1967 : 70]
[5] जयशंकर प्रसाद, इरावती [1967 : 74]
[6] चंद्रगुप्त, तृतीय अंक, दृश्य छह, प्रसाद वाङ्मय, पृष्ठ 608
[7] शाक्याजीवकानदीन्वृषलप्रव्रजितान्देवपितृकार्येषु भोजयतः शत्यो दण्डः— अर्थशास्त्र 3।20।20
[8] जयशंकर प्रसाद, इरावती [1967 : 75]
[9] जयशंकर प्रसाद, इरावती [1967 : 85]
(समाप्त)
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in