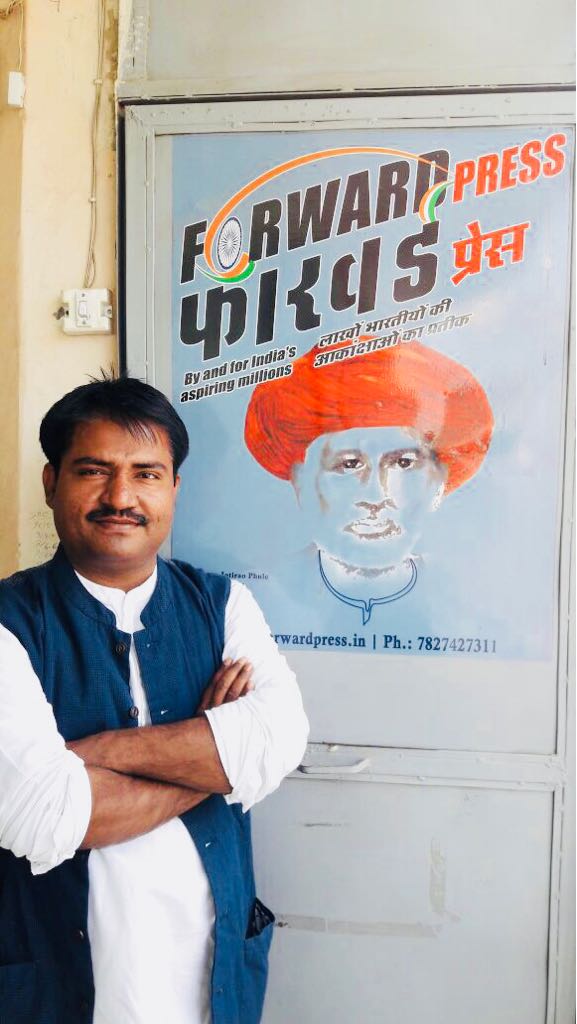दिल्ली के सियासी गलियारे से लेकर झुग्गी-झोपड़ियों तक हिम्मत सिंह नजर आते हैं। गले में गमछा और कंधे में एक झोला उनकी पहचान है। झोले में अनेक लोगों के आवेदन और कई पत्र-पत्रिकाएं। सार्वजनिक जीवन में लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करते हुए उन्हें अब तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है। वे बहुजन सवालों को लेकर मुखर रहे हैं। उनके संघर्ष और विचारधारा आदि को लेकर नवल किशोर कुमार ने उनसे बातचीत की। इस बातचीत को पठनीय बनाने के लिए आंशिक तौर पर संपादित किया गया है।
कृपया अपनी परिवारिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में बताएं।
मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे-से गांव कोड़रा से हूं। वहां एक गरीब किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी थोड़े पढ़े-लिखे थे और आसाम में नौकरी करते थे। इसी वजह से हम लोगों की पढ़ाई-लिखाई हो पाई थी।
आप किस जाति से हैं?
हम तो चौहान हैं वहां के। लोग हमें नोनिया भी बोलते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों के यहां जो पूरा अंतरविरोध होता था, वह जातिगत दबंगई के कारण था। उसे प्रभुत्व बनाने की सामंती मानसिकता ही प्रभुत्व कहिए। वहां के जमींदार राजपूत और भूमिहार आदि यही सब हुआ करते थे। और अधिकांश लोग बटाई पर उनका खेत लेकर खेती-बाड़ी करते थे। हमारे यहां सुविधा थोड़ी सी यह थी कि हमारा अपना भी थोड़ा-सा खेत था। उससे खाने भर अनाज वगैरह हो जाता था। चूंकि पिताजी नौकरी भी करते थे।
आपके पिताजी आसाम में सरकारी नौकरी करते थे?
नहीं, सरकारी नौकरी नहीं करते थे। वहां एक मारवाड़ी थे। मेरे पिता उनके यहां मुनीम थे। लोग उन्हें बड़े बाबू कहते थे। वे आजीवन वहीं रहे। गुजरने से कुछ साल पहले वे वापस आए। यह तो हो गई मेरे घर की कहानी। बचपन में हमारे यहां सीपीआई के कुछ लोग आते थे। हमारे चाचाजी गांव में ही रहते थे।
कृपया हमें पहले यह बताएं कि आपकी पढ़ाई-लिखाई कहां हुई?
मेरी पढ़ाई-लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीएमपी डिग्री कॉलेज में हुई। मैंने 1991 में बीएससी (बायोलॉजी) किया था। इसके पहले बारहवीं तक अपने गांव के पास ही पढ़ाई की। उन दिनों डाक्टर वगैरह बनने की बात सोचा करता था।
यदि मैं अनुमान गलत नहीं लगा रहा हूं तो आपका जन्म 1960-65 के बीच में हुआ होगा?
मेरा जन्म 4 मई, 1968 को हुआ। लेकिन दस्तावेजों में मेरी जन्मतिथि है– 10 जुलाई, 1969।
आप बता रहे थे कि प्राइमरी की पढ़ाई गांव की स्कूल में हुई।
हां, प्राइमरी स्कूल गांव से करीब 3-4 किलाेमीटर दूर थ। बारहवीं की पढ़ाई के लिए 6-7 किलोमीटर दूर पैदल जाना होता था। गांव में उस समय कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। बरसात के दिनों में जब बारिश होती थी तब प्राइमरी स्कूल जाना लगभग दो महीने के लिए बंद ही हो जाता था। चारों तरफ पानी भर जाता था।
बिहार से आपका संबंध कैसे बना?
हां, मैं यही बता रहा था। बिहार कनेक्शन में पार्टी वाला ही मामला है। पार्टी के कारण ही भोजपुर और पटना के आस-पास इलाकों में आना-जाना और लोगों से मिलना-जुलना शुरू हुआ।
यह कब प्रारंभ हुआ?
सन् 1993-94 में मैं भाकपा माले का पूर्णकालिक सदस्य बन गया था। मेरा कार्यक्षेत्र ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में था। जैसे गाजीपुर, चंदौली, बनारस, बक्सर और भभुआ आदि। वहां के किसानों के आंदोलन में हमारी सक्रियता रहती थी।
वामपंथ के पीछे प्राथमिक वजह क्या थी?
प्राथमिक वजह तो यही थी कि कमाने वाले खाएंगे और लूटने वाले जाएंगे। यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। वजह यह कि समाज में भयंकर डिस्क्रेमिनेशन था। शोषण और उत्पीड़न का दौर था। मन में सवाल उठता था कि आखिर इसकी वजह क्या है। कई बार लगता था कि शायद भगवान ने किया होगा। फिर जब आध्यात्मिक विचारधारा वालों के पास जाता था तो लगता था कि नहीं, भगवान ने सबको बराबर बनाया है। समझ नहीं आता था कि आखिर मामला क्या है। कभी लगा कि शायद हमारे लोग उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, इस कारण ऐसा होता होगा। लेकिन देखा कि हमारे पढ़े-लिखे लोगों के साथ भी वही डिस्क्रेमिनेशन होता था। राजनीतिक दलों का रवैया भी हमारे लोगों के प्रति वैसा ही था। हमलोग जिस गांव में रहते थे, वहां कोई राजनीतिक दल था ही नहीं। ले-देकर सीपीआई के कुछ लोग आते थे। वो भी जब सोवियत रूस विघटित हो गया तो वे बेचारे भी कहां गायब हो गए, पता नहीं। लेकिन उससे अच्छा यह हुआ कि कुछ किताबें वे पढ़ाते थे। बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थीं, लेकिन इतना जरूर समझ में आता था कि वे मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरों के अधिकार की बात करते हैं। बाकी और कोई करता ही नहीं था। इस कारण भी लाल झंडा के प्रति थोड़ा एक आकर्षण था। लेकिन तब उसके प्रति कोई ऐसा आकर्षण नहीं था कि हम वैचारिक रूप से जुड़ते। पार्टियां कैसे काम करती हैं, इसकी तब समझ नहीं थी। लेकिन जो एक सामाजिक ताना-बाना था, उसमें वो बातें प्रभावित करती थीं।

क्या आपके गांव में किसी एक जाति का वर्चस्व था और उसके खिलाफ आपके मन में कोई आक्रोश था जिसके कारण आप वामपंथ से जुड़े?
हां, बहुत वर्चस्व था। और हमारे अंदर आक्रोश भी बहुत था। मुझे याद है कि उस समय गांव में हम लोग बच्चों को इकट्ठा करते थे, पढ़ाते थे। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत उधर से आब्जेक्शन होता था, उसका हम लोग कैसे जवाब दें, इसकी तैयारी कराते थे।
आब्जेक्शन अपरकास्ट की तरफ से होता था?
हां, अपरकास्ट मतलब जमींदार। मुझे यह लगता था कि तीन-चार सौ साल पहले ये लोग आए होंगे। उनकी रैयत थी, तो हमारे लोग भी रैयती रहे होंगे। आजादी के बाद भी सामंती प्रवृत्ति और दबंगई जैसी तमाम मानसिकताएं बनी रहीं।
कोई ऐसी घटना, जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे?
बहुत सारी घटनाएं हैं। ऊंची जातियों के यहां का बच्चा भी हमारे लोगों को ‘रे’ और ‘तू’ ही कहता था। यदि किसी ने जरा-सा भी विरोध किया तब वे लोग बंदूक, लाठी और बल्लम आदि लेकर घर पर चढ़ जाते थे और पीट-पाट कर चले जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनका विरोध करे।
आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई?
नहीं, मेरे साथ नहीं हुई। लेकिन मेरे गांव में हमारे लोगों के साथ ऐसा होता था। मेरे चाचाजी सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर बन गए थे। उन्होंने विरोध करना शुरू किए। एक-दो लोग और थे उन्हीं के उम्र के। चाचा और कुछ अन्य लोग थोड़ा-थोड़ा विरोध करने लगे। थोड़ी ऊंची जाति वालों की भी हेकड़ी कम हुई। हालांकि कई बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ।
आपके चाचाजी पर?
हां, फिर इधर से भी जवाब दिया गया। फिर पुलिस में मुकदमा आदि भी हुआ। चूंकि मेरे चाचा जी सरकारी कर्मचारी बन चुके थे, इसलिए पुलिस अधिकारियों को भी उनके प्रति थोड़ी सिम्पैथी थी। लेकिन तब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन सबकी वजह क्या है। क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? यह समझ में तब आया जब पढ़ाई की, स्नातक करने के बाद जब पार्टी से जुड़ा।
पहला जुड़ाव किस संगठन से हुआ?
सबसे पहला तो मैंने पहले ही बताया कि सीपीआई से जुड़ाव हुआ। हमारे गांव में सीपीआई के एक कार्यकर्ता या लीडर आते थे। वे हमलोगों को कुछ-कुछ बताते थे। हमारे चाचाजी को बताते थे तो हमलोग वहीं बैठे रहते थे। तो थोड़ी बहुत बातें तो समझ में आई थीं। बाद में जब इलाहाबाद गया तो कोशिश करता रहा कि कोई ऐसा संगठन मिल जाए, जिससे जुड़ा जए। लेकिन फाइनली आइसा, जो कि सीपीआई (एमएल) का छात्र संगठन है, से जुड़ाव हुआ।
कब और कहां जुड़े आप?
सन् 1992 के अंत में इलाहाबाद में ही जुड़ाव हुआ। मुझे याद है कि 6 दिसंबर, 1992 को जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, तब 4 या 5 दिसंबर को मैंने सदस्यता ली थी। 7 दिसंबर को ही हम करीब ढ़ाई-तीन सौ छात्रों ने तख्ती लेकर कचहरी तक मार्च निकाला और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का पुतला फूंके। तब हमें लग रहा था कि इन्होंने ही पूरा षड्यंत्र किया। इसके अगले ही दिन पुलिस ने हम दस-बारह लोगों को गिरफ्तार करके नैनी जेल में डाल दिया था। बाकी सब तितर-बितर हो गए थे। तो जेल का जो डर मन में था, वह आरंभ में ही जाता रहा। मैंने देखा कि हमलोगों से ज्यादा लोग वहां जेल में हैं। यह अहसास हुआ कि जेलें किसी को सजा देने या सुधारने के लिए जगह नहीं हैं। यह इसलिए है कि कैसे शोषितों-वंचितों को उनके अधिकार से महरूम कर दिया जाए। मैंने तो यह भी देखा कि वहां कई सारे लोग थे जो बाहर जाना ही नहीं चाह रहे थे। जिस अपराध की सजा 4 महीने, 6 महीने या साल भर है, लोग बीस-बीस साल से वहीं पड़े हुए हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। कोई कहता कि आपको रिहा करा देते हैं, आप चले जाइए तब वे कहते थे कि जाएंगे कहां। यहां मन लगा रहता है। सब लोग आते-जाते रहते हैं। जेलों के बारे में यह बातें समझ में आईं।
आप तब कितने दिन में जेल से बाहर निकले?
हमलोग तो चार-पांच दिन में ही बाहर आ गए थे। ऐसे ही आ गए थे। हमसे कहा गया कि जमानत हो गई है। जेल के ही किसी कर्मचारी ने हमारी जमानत कराई थी। हम लोग नैनी जेल से बाहर निकले। तो एक गणेश टैंपू मिला। पैसा-वैसा भी नहीं था। किसी तरह टेंपू चालक ने हम लोगों को इलाहाबाद छोड़ा। वहां से हम अपने-अपने कमरे में पहुंचे।
तब क्या आप हॉस्टल में रहते थे?
नहीं, चूंकि हमारा ग्रेजुएशन 1991 में हो चुका था। हॉस्टल से लेना-देना नहीं था। पहले लगता था कि डाक्टर वगैरह बनेंगे। लेकिन फिर लगा कि डाक्टर वगैरह बनकर क्या करेंगे। अब जो करना है समाज के लिए करना है। जिस समाज से आए हैं, उनके बदलाव की बात करनी है। फिर वहां से होल्टाइमर बना।
आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय सीपीआई (एमएल) के महासचिव विनोद मिश्र थे। क्या कभी उनका सान्निध्य मिला?
सान्निध्य क्या, वे जनरल सेक्रेटरी थे और जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, वैसे ही बात होती थी। एक बार मैं बीमार भी पड़ा था। उस समय दिल्ली में पार्टी की बड़ी रैली थी। मुझे टायफाइड हो गया था। उस समय डाक्टर ने बाहर निकलने से साफ मना कर दिया था कि आप बेडरेस्ट पर रहिए। आपकी हालत खराब है। तो विनोद मिश्र जहां रहते थे, वहीं मुझे भी रखा गया कि यहां थोड़ी शांति है। वहीं खाना-पीना आ जाता था। उस समय कामरेड विनोद मिश्र बीच-बीच में आते रहते थे और हालचाल के बारे में पूछते रहते थे। उनसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। मैं कार्यकर्ता और वे लीडर थे। कार्यकर्ता और लीडरशिप के बीच अलग-अलग चीजें होती हैं।
कहा जाता है कि विनोद मिश्र अपने कार्यकर्ताओं से बहुत मिलजुल कर रहते थे।
हां, वे मिलते तो थे। सब लोग साथ बैठते थे और चाय पीते थे। सब बातचीत करते थे। लेकिन मेरे मन में यह बात रहती थी कि वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं।
पार्टी में एक अनुशासन बनाकर रखा जाता था?
अनुशासन बनाया नहीं जाता था। नेता के प्रति स्वाभाविक रूप से जो एक सम्मान होता है, बस वही मामला था। कोई कहता नहीं है। पार्टी में सेंट्रल कमेटी है, पोलित ब्यूरो है। बॉडी लैंग्वेज ऐसा बन जाता है। कोई बनाता नहीं है।
1990 के दशक में बिहार में नरसंहार हो रहे थे, उस समय पार्टी की भूमिका कैसी थी?
देखिए दो-तीन चीजें थीं। उसी दशक में बथानी टोला, लक्ष्मणपुर-बाथे और कई जगहों पर नरसंहार हुए। उसी समय आप यह भी देखें कि वह दौर नई आर्थिक नीति का था। दुनिया भर की चीजें हो रही थीं। और साथ ही साथ तमाम जो आंदोलन चल रहे थे, खासकर समाज के निचले तबके में जो जागृति हो रही थी, उसे दबाने के लिए प्रतिगामी ताकतें काम कर रही थीं। स्वाभाविक रूप से भाकपा माले वहां गरीब-गुरबा के चैंपियन के रूप में आया। मतलब कुछ भी होता था तो यह मान लिया जाता था कि माले का गढ़ है, इसलिए वहां हमला हुआ। या फिर यह कि माले वाले हैं, इसलिए हुआ। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे एक चीज और लग रहा था कि 1960 के दशक में जिस तरह प्रतिरोध का एक तरह का आंदोलन चला था, वह धीरे-धीरे दूसरा स्वरूप अख्तियार कर रहा था। पार्टी चुनावी मोड में आ गई थी। जिस जनता को आपने पहले आत्मरक्षा के लिए तैयार किया था, उसको कहा गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। उसी का खामियाजा सबसे ज्यादा अगर किसी ने भुगता तो वह वही समाज था, जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी और वे स्वयं इस लड़ाई में शामिल थे। आप बाद में देखिए कि कैसे वामपंथी पार्टियों का आधार खिसक गया या कहिए कि खत्म हो गया। उस पर हम अलग से बातचीत करेंगे, लेकिन कोई कुछ भी कहे, माले गरीब-गुरबों का चैम्पियन तो था ही। माना जाता था कि वहां पर तमाम शोषितों, दलितों-वंचितों की वह एक सशक्त आवाज है।
आप उस क्षेत्र में कब तक रहे?
मुझे तो 1994 में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। कहा गया कि आपको दिल्ली जाना है, और वहां जाकर काम करना है। मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो मानता था कि पार्टी कहीं भी भेज देगी, जंगल में भी खड़ा कर देगी तो वहां जाएंगे और काम करेंगे। एक क्रांति का जुनून था। वह अभी भी है, लेकिन थोड़ा रूप बदल गया है। बाद में यह भी कहा गया कि वापस जाना है, लेकिन यहां दिल्ली में साथियों ने कहा कि अभी यहीं पर रूकिए। यहां पर तमाम तरह के काम हैं। मेरे पास ड्राइंग करने, कंप्यूटर आदि का स्किल था। पोस्टर और बैनर आदि तमाम चीजों की यहां ज्यादा जरूरत थी। वे सात-आठ साल भयंकर एक्टिविज्म का दौर था। कभी एक दिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरे दिन कहीं और। हम छात्र संगठन में काम कर रहे थे। मजदूरों के बीच जाकर काम कर रहे थे। झुग्गियों में जा रहे थे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित कर रहे थे। बस एक जुनून था कि चीजों को बदल देना है।
आपको कब लगा कि राह बदल लेनी चाहिए?
दो-तीन चीजें थीं। मेरा मानना है कि कई बार आप बड़ी मासूमियत से नेताओं से या लीडरशिप से सवाल करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि उनसे कोई आपका दुराग्रह है। तो कुछ-कुछ सवाल मैंने भी करना शुरू किया। जैसे बहुत सारे लीडर सुबह आ जाते थे और बैठे रहते थे पार्टी ऑफिस में। दुनिया भर की बहस, कहानियां और किस्से सुनाते थे। फिर शाम को चले जाते थे। चाय-सिगरेट सब चलता रहता था। तो एक बार मैंने कहा कि यहां बैठने से ज्यादा अच्छा होता कि हमलोग मजदूरों के बीच जाते। इससे कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत होने लगी। और फिर मुझे कहा गया कि आप नोएडा चले जाइए, मजदूरों के बीच में काम करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहां गया तो उन मजदूरों का होकर ही रह गया। उनकी झुग्गी-झोपड़ियों में सुबह से शाम तक उठना-बैठना, खाना-पीना और सोना। जैसे वे लोग रहते थे वैसे ही मैंने भी रहना शुरू कर दिया। हालांकि इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे टीबी भी हो गया। दोष उन मजदूरों का नहीं था, मेरी लापरवाही थी। क्योंकि उनके कारण टीबी होता तो सबको हो जाता।
फिर बाद में 2001 में जब मेरी शादी हुई तब पार्टी के नेताओं के व्यवहार में बदलाव होना शुरू हुआ। मेरी जीवनसंगिनी भी पार्टी की सक्रिय सदस्य थी।
आपने अंतरजातीय विवाह किया?
हां, शादी तो अंतरजातीय ही थी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्टी में तो कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। नेताओं के व्यवहार में बदलाव के पीछे मामला वह नहीं था। लोगों ने सोचा कि पहले होलटाइमर थे तो कुछ नहीं लेते थे लेकिन अब इनको भी कुछ देना पड़ जाएगा। फिर धीरे-धीरे कहा गया कि आप अपना स्वयं देख लीजिए।
फिर तो लगा कि कहां तो सोचे थे कि क्रांति करेंगे। थोड़ी-सी तकलीफ तो हुई, लेकिन मैंने खुद से कहा कि छोड़ो यह सब चलता है। लेकिन बाद में धीरे-धीरे उन लोगों ने इग्नोर करना शुरू किया। 2004-05 आते-आते कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम कहां हो, मीटिंग में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो…। और मैं भी उनसे दूर होने लगा था।
लेकिन एक बात जिसने इस पूरी प्रक्रिया में मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वह यह था कि हमने अपनों के अरमानों को खारिज किया। मैं क्रांति का सपना देखकर या लक्ष्य लेकर चला था। होलटाइमर बना। मां-बाप ने कितने अरमानों से पढ़ाया था कि बड़ा होकर यह बनेगा, वह बनेगा, उन सबको धत्ता बता कर पार्टी से जुड़ा था। लेकिन यहां आइडियोलॉजी का सवाल था। वही आइडियोलॉजी, जिसके लिए हम मर-मिटने के लिए भी तैयार थे, उसका नेतृत्व गलत लोगों के हाथ में था। उनके लिए हमारे सवाल महत्वपूर्ण नहीं थे।
इन बातों ने परेशान किया। डिप्रेशन में जाने के बजाए मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। उन तमाम किताबों को पढ़ा, जिनको वे लोग बहुत बड़ा जटिल और जाने क्या-क्या बताकर पेश करते थे। जब पढ़ना शुरू किया तब हमने कहा कि मार्क्स तो हमारी भाषा में और हमारे लिए बात कर रहे हैं। और वे कहते थे कि यह कोई जटिल थियरी है, जो हमलोगों को समझ में ही नहीं आएगी। हमें यही बताया जाता था।
इसके अलावा एक बात और हुई। एक साथी थे कमल कुमार नियोगी। वे अभी भी हैं। उनके साथ जब बैठता तब सुबह से रात हो जाती थी। हम विचार विमर्श करते थे। वे भी इसी तरह से उपेक्षित थे। हालांकि वे बड़े लेवल पर पहुंचे थे। ट्रेड यूनियन के अच्छे नेता थे। उन्होंने एक दिन कहा कि कार्ल मार्क्स की जो सबसे बुनियादी किताब है, वह है– ‘जर्मन दर्शन’। इसमें उन्होंने पूरी दुनिया में ‘मोड ऑफ प्रोडक्शन’ के बारे में लिखा है। मतलब श्रम और उत्पादन प्रक्रिया में किस तरह का संबंध है। मार्क्स हमें उसमें बताते हैं कि कौन श्रम करता है और कौन नियंत्रित करता है। यह पूरी दुनिया में अलग-अलग है। उन्होंने कहा कि भारत और इजिप्ट में जो ‘मोड ऑफ प्रोडक्शन’ है, वह जाति आधारित है। इसे न केवल राज्य ने बल्कि वहां के धर्म ने भी मान्यता दे रखी है। मैं तो पहली बार ऐसा सुना। इसके बारे में पहले किसी नेता ने यह नहीं बताया था। वे तो कहते थे कि नहीं-नहीं, मार्क्स का यहां की जाति-व्यवस्था से कुछ लेना-देना ही नहीं है। सवाल है कि जब लेना-देना नहीं है तो 1848-49 में मार्क्स कैसे लिख रहे थे? वे कैसे रियलाइज कर रहे थे कि यहां भारत में जो शोषण की पूरी पद्धति है वह जाति के आधार पर है। अब यहां से मेरी नई यात्रा शुरू हुई।
मतलब यह कि भारत के वामपंथियों ने यह बात छिपाकर रखी कि मार्क्स जाति-व्यवस्था से परिचित थे और वे इसे समाज की प्रगति में बड़ा बाधक मानते थे?
हां, मुझे रियलाइज हुआ कि हमें भारत में रूस की क्रांति, और वहां के बड़े क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ाई जाती थीं। फ्रांस और इंग्लैंड के तमाम बड़े-बड़े लेखकों की किताबे पढ़ाई जाती थीं। भारत के बारे में हमको कुछ मिलता ही नहीं था। देवी प्रसाद चटोपध्याय की किताब थी– ‘भारतीय दर्शन में क्या जीवित है क्या मृत’। यह बहुत तार्किक किताब है। या राहुल सांकृत्यायन की कुछ किताबें थी। मसलन, ‘वोल्गा से गंगा’ बहुत रोमांचक ढंग से लिखी हुई। लेकिन कुल मिलाकर यह कि जो जाति-व्यवस्था है, इसके बारे में सब गोलमोल कर जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे ‘गुलामगिरी’ किताब मिली। मैंने सोचा कि यह तो ठीक वही दौर है जब मार्क्स ‘जर्मन दर्शन’ लिख रहे थे और फुले ‘गुलामगिरी’ लिख रहे थे। और दोनों किताबों में असल दुश्मन और असल दोस्त की पहचान की गई है। वे दर्शन से लेकर अर्थशास्त्र तक बात करते हैं।
लगा कि मैं तो हवा में था। मैं सचमुच में हवा में ही था। मैं जाति छुपाता था ताकि कोई नीच न समझे। लेकिन हम तो श्रमजीवी समाज हैं भाई। हमारे बल पर ही तो समाज चल रहा है। और हम क्यों अपने आपको छुपाके चलें? एक नई यात्रा यहां से शुरू हुई।
आप नक्सलबाड़ी आंदोलन को देखिए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। साठ के दशक में खासकर भोजपुर में जो कुछ हुआ वह दौर केवल नक्सलबाड़ी का नहीं था। वहां तमाम बड़े-बड़े चिंतक अपने-अपने ढंग से पहले से काम कर रहे थे। जगदीश मास्टर, रामेश्वर अहीर और रामनरेश राम नक्सलबाड़ी की वजह से भोजपुर में आंदोलन नहीं कर रहे थे। वे पहले से ही आंदोलन कर रहे थे। आपको बताऊं कि आरा में तब इन लोगों ने डॉ. आंबेडकर की जयंती पर बड़ा जुलूस निकाला था और चमारिस्तान बनाने की बात कही थी।
दूसरी बात, आप यह देखें कि सामान्य तौर पर हमें जातिगत संघर्ष के बजाय वर्ग-संघर्ष के बारे में बताया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, या ठाकुर या राजपूत, इनको भी लोग जाति बोल देते हैं। लेकिन वे जाति नहीं, वर्ण हैं। दूबे, त्रिपाठी आदि उनकी उपजातियां होंगी। लेकिन हैं तो वे वर्ण ही। जातियां तो केवल और केवल श्रमजीवियों के लिए बनाई गई हैं। श्रम के आधार पर शोषण और उत्पीड़न करने के लिए। भाई, लोहे का काम करने वाला लोहार हुआ। आप देखें कि पूरी दुनिया में आयरन स्मिथ (लोहे का काम करनेवाले) हैं। लेकिन यहां क्या सिस्टम बना दिया गया कि बढ़ई लोहार से भेदभाव करेगा, यादव बढ़ई और लोहार से भेदभाव करेगा। यह जो पूरा विभाजन है, यही ब्राह्मणवाद है। यह विभाजन ही ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा हथियार है। और इसको तोड़े बगैर या इससे थोड़ा-सा भी आप समझौता करेंगे तो लोकतंत्र या फिर समाज में समानता लाने की बात आपके दिमाग से हट जाएगी और आप वहीं गच्चा खा जाएंगे। और यह लगातार हुआ है। यही दिक्कत रही है कम्युनिस्ट पार्टियों में। आप सीपीआई को देख लीजिए। एमएन राय जैसे भद्रलोक जाते हैं, लेनिन से मिलने। ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में 1925 में बनती है। कौन लोग हैं बनाने वाले और वहां से आकर सबके सब नेता बन जाते हैं।
अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1928 में पहली कांग्रेस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सिंगारवेलु चेट्टियार ने की थी। वे दलित थे।
वे थे और नंबूदरीपाद आदि सब थे। बहुत सारे लोग थे। जिनको लगेगा कि मार्क्सवाद तो हमारी मुक्ति का रास्ता है, वे सब थे। इसलिए तो हम भी पार्टी में आए थे। अब किसी के लिए हो सकता है कि रोमांटिसिज्म हो। सिगरेट का धुंआ छोड़ते हुए एक दूसरी दुनिया की बात करना, जिसे उनका यूटोपिया कह सकते हैं। इसमें अजीब-सा प्लेजर वाला भाव होता है। फिर लात मार कर निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता।
एक छोटी-सी कहानी है। बंगाल की है। एक सच्ची घटना है। तीन भाई थे। एक व्यापारी था, एक कांग्रेसी था और एक कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट वाला अपने नौकर को साथी कहता और बराबरी का सम्मान देता था। वह बेचारा नौकर भी उसको बड़े सम्मान के साथ कामरेड कहता था। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग ये करेंगे, वह करेंगे आदि बात कहता था। एक दिन तीनों भाई बैठे खा रहे थे खाना एक टेबल पर। वह नौकर भी खा रहा था। इस बीच तीनों भाइयों में कुछ कहासुनी हो गई। नौकर ने हस्तक्षेप किया। तब कम्युनिस्ट भाई ने उसे तमाचा जड़ दिया और कहा कि यह हम भाइयों के बीच का मामला है, तू कहां से बीच में घुस गया।
तो यह है पूरी कहानी। यहां जिसके खिलाफ लड़ना था वही हमारा झंडा थामे हुए था। जो दूसरी धाराएं हैं, जैसे कि समाजवादी धारा है, बहुजन समाज पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, उसको ये लोग जातिवादी बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ का जितना बड़ा प्रभाव था, वह कहां गायब हो गया, कैसे गायब हो गया।
मूल बात यह है कि हमारी अपनी लड़ाई को जातिवादी कहकर खारिज कर दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या है? यहां वामपंथी पार्टियों का जो लीडरशिप है, वह तो वही है, जिसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है। राय साहब, फालाना साहब, ढिकना साहब।
हमारे यहां एक नेता थे। सीपीआई के मलिकार कॉमरेड नाम था। उनकी बहुत बड़ी-बड़ी मिल्कियत थी। वे अपने हरवाहे और चरवाहे सभी को कामरेड कहते थे। सीपीआई में इसलिए थे कि उसके जरिए रूस वगैरह में जाने के लिए ठीक-ठाक खर्चा मिलता था। बाकी उनके हलवाहे, चरवाहे, मलिकार कॉमरेड बोलते थे।
आप देखिए कि जमीनी यथार्थ को नकारने का खामियाजा सीपीआई को भी भुगतना पड़ा। यदि बुनियादी चरित्र आप नहीं समझेंगे, डायलेटिक्स को नहीं समझेंगे तो आप भले उसको नकार दीजिए, नकारने से हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी पीठ थपथपाई जाए। लेकिन बुनियादी जो डायलेटिक्स है, समाज में यह कैसे काम करता है और पूंजीवाद कैसे काम करता है, कैसे वह आपको अपने से ही अलग कर देता है, समाज को प्रकृति से अलग करता है। इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है।
फिलहाल आप वर्तमान में किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं?
देखिए, मैंने तो 2016 में बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। उस समय बड़ी आलोचना हुई कि आप मार्क्सवाद में जातिवाद क्यों घुसा रहे हैं। मैंने कहा कि अभी जातिवाद हुआ नहीं है। अब सचमुच में जातिवादी बनना है। यहां की कम्युनिस्ट पार्टियों को या किसी को बिना जातिवादी बने कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। जाति का संबंध श्रमिकों से है। बाकी तो सभी वर्ण हैं। हम तो चाह रहे हैं कि बड़ी जातिवादी गोलबंदी हो। तभी आप ब्राह्मणवादी कवच को तोड़ पाएंगे। मार्क्स ने कहा था कि सर्वहारा का जो आंदोलन है, मुक्ति का आंदोलन है, वह केवल अपने को ही मुक्त नहीं करता है, शोषकों को भी मुक्त करता है। उन्होंने कहा कि सर्वहारा का आंदोलन होगा, क्रांति होगी। अपनी मुक्ति के साथ-साथ तमाम जो दूसरी उत्पीड़ित समुदाय हैं या सभ्यताएं हैं, सबको मुक्ति मिलेगी। असल में इस तरह का जातिवाद हम करना चाहते हैं। उसका हमारे पास एक वर्गीय दृष्टिकोण है। हो सकता है कि हजार जातियों में बंटे हैं, हजार तरह के पेशे में हैं लोग, हजार तरीके के क्षेत्रों में लोग हैं, हजार तरह के उपजातियों में लोग बंटे हुए हैं। लेकिन हैं तो सब श्रमजीवी ही, जिनके बल पर दुनिया चल रही है। तो अब भारत में यदि क्रांति होगी तो पहला काम होगा जिसे कहते हैं बहुजन जनवादी क्रांति, जिसकी हम बात कर रहे हैं।
हम लोगों ने बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी 2016 में। फिर हमने रिसर्च किया तो पता चला कि बीस साल पहले आंध्र प्रदेश में लोगों ने बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी बना रखी थी। इसका मतलब यह है कि इस तरह से लोग सोच रहे हैं कि असल में कम्युनिस्ट पार्टी किसकी है और किसके नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी होगी। कायदे से कहा जाता है न कि मजदूरों की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी? यहां का मजदूर तो यहां की जातियां हैं।
आप देखिए यह पूरा आंदोलन नेतृत्वहीन नहीं रहा है। जैसे कि पेरियार ललई सिंह रहे। उन्होंने पेरियार के मार्ग पर चलते हुए लड़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन आप इसको मार्क्सवादी परिभाषा में देखेंगे तो यह भी वर्ग-संघर्ष का एक नया रूप है, नए तरीके का रूप है। वह कितना सफल हुआ, उस पर हम अलग से विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यह है यही।
आप देखिए कि जाति जनगणना की बात हो रही है। इसका मतलब है कि जो अभी तक इनविजिबल है उसे विजिबल बना दिया जाए। जैसे ही विजिबल बनेगा वह अपनी दावेदारी पेश करेगा। लेकिन उसको खत्म करने के लिए सांप्रदायिक और धार्मिक चालें चली जा रही हैं। मैं राहुल गांधी का नाम लूंगा। उनको यह रियलाइज हो गया कि इस तरह की फोर्सेज, जो सब कुछ हड़प जाना चाह रही हैं, को कोई यदि रोक सकता है तो यहां की जातियां मतलब वर्ग श्रमजीवी वर्ग ही रोक सकता है। पूरी ऊंची जातियां मोटा-मोटी भाजपा और आरएसएस के साथ लामबंद हैं। दो-चार प्रतिशत को हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं गया होगा। लेकिन अब उसके खिलाफ यदि लड़ाई होगी तो एंटी ब्राह्मनिकल जो ये फोर्सेज हैं, ये ही लड़ेंगीं।
हम लोगों ने वहां से काम करना शुरू किया है। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ-कुछ जगहों पर हम प्रैक्टिस करें। साधन-संसाधन की अपनी कमी है। कुछ लोग तैयार हुए हैं। बिहार वगैरह में हमलोग कुछ कमेटियां बनाना प्रारंभ किए हैं बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले। वहां सीधे-सीधे हम यह नहीं कह रहे हैं कि बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी बनाइए। हम कह रहे हैं कि बहुजन सांस्कृतिक संगठन बनाइए या पहले से बना बनाया है तो उसको नए सिरे से रिवाइव करिए। उनके छात्रों का संगठन बनाइए या उनके मजदूरों का संगठन बनाइए। उनके वकीलों का, उनके डॉक्टरों का या जो भी जिस लेवल पर है, उस लेवल पर करिए। लेकिन बुनियाद में बहुजन सर्वहारा है, वही हमारा कोर होगा, जो अंतिम क्षण तक लड़ेगा।
(संपादन : समीक्षा/राजन/अनिल)