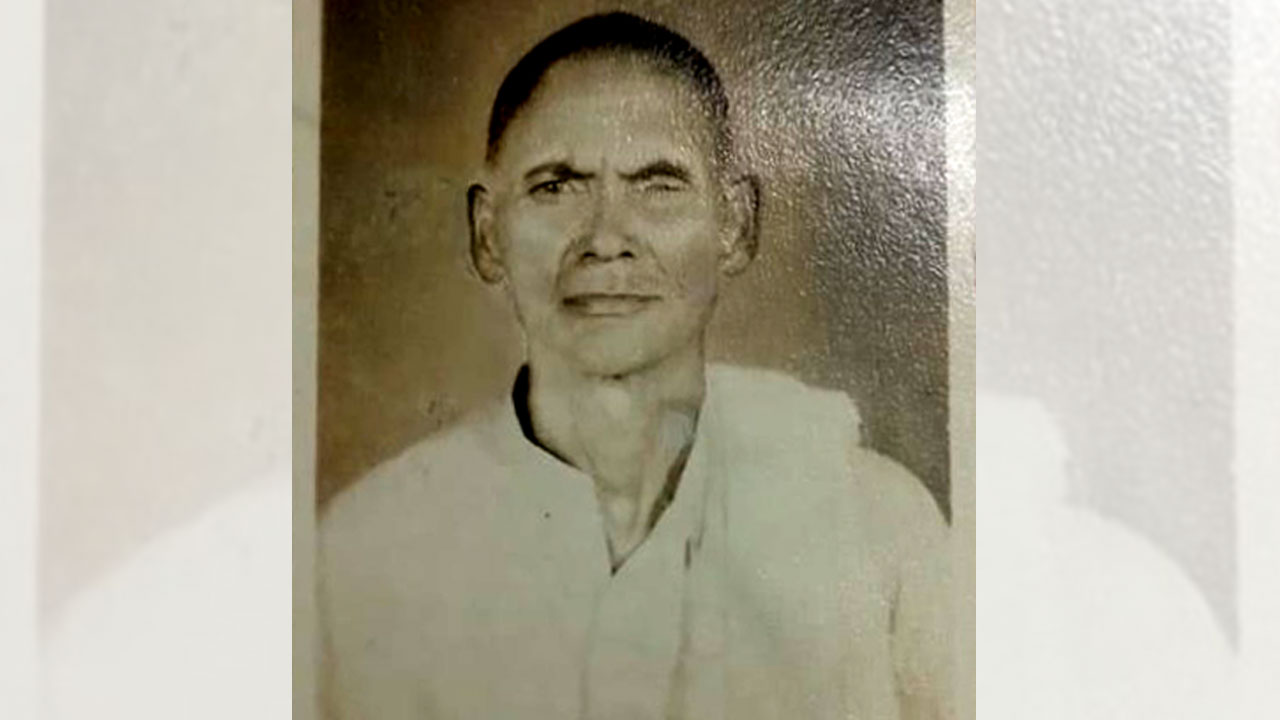बीते करीब 50 दिनों से दिल्ली को घेरकर डटे हुए किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। वही सरकार का भी अपने कृषि कानूनों को लेकर अड़ियल रूख कायम है। इसके बावजूद किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस आंदोलन में छोटे सीमांत किसान और खेतिहर भूमिहीन मजदूरों की अपेक्षित भागीदारी नहीं हैं। जबकि कृषि कार्य करनेवालों में इनकी संख्या सबसे अधिक है और इनमें सबसे अधिक आबादी दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों की है।
बताते चलें कि भारत में बहुत बड़ी आबादी कम जोत वाले किसानों की है जिनके पास आधा एकड़ से लेकर दो एकड़ तक जमीन है। इनसे भी अधिक संख्या बटाईदार किसानों की है जो बटाई के आधार पर या फिर जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं। ये किसान हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। चूंकि बटाईदार किसानों के पंजीकरण का कानून नहीं है, इसलिए सरकार के पास इनका आंकड़ा नहीं है। जिनके नाम पर जमीन है या फिर जमीन का पट्टा है, वे भले ही वह किसान न हो, लेकिन सरकार की नजर में वे किसान माने जाते हैं।
पहले तीनों कानूनों पर चर्चा कर लें। पहला कानून है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020। इसके बारे में सरकारी दावा है कि यह कानून किसान को अपनी उपज मंडियों से बाहर सीधे बाज़ार में बिना दूसरे राज्यों को टैक्स चुकाए बेचने का अधिकार देता है। सरकार के हिसाब से यह उसका क्रांतिकारी कदम है। लेकिन किसान कह रहे है कि यह मंडियों को ख़त्म करने का प्रयास है और किसानों को बाज़ार के हवाले करने की साजिश है।

दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध अधिनियम 2020। इसके मुताबिक किसान संविदा आधारित खेती कर सकेंगे और उसकी अपने स्तर पर मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इससे एक बात तो तय है कि छोटी जोत वाले किसान इस व्यवस्था में पिसकर रह जाएंगे। उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा।
तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। यह कानून उत्पादन, भंडारण के अलावा दलहन, तिलहन और प्याज की बिक्री को युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों के अलावा नियंत्रण से मुक्त करने की बात कहता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह जमाखोरी बढ़ाने वाला कानून है। किसान भी यही मानते हैं कि यह जमाखोरी को कानूनी संरक्षण देने का सरकारी प्रयास है।
यह बड़ी विडंबना है कि सरकार ने किसानों के लिए तीन कानून बनाए हैं और उसका दावा है कि इन कानूनों से किसानों की आय बढ़ जाएगी और खेती लाभदायक पेशा बन जाएगी। लेकिन इस कानून में भूमिहीन किसानों के लिए कुछ नहीं है। उलटे इस कानून में सरकारी गोदामों के समानांतर प्राइवेट कंपनियों को असीमित भंडराण की छूट दी गई है। लिहाजा इसका असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी पड़ेगा। वर्तमान में इसी व्यवस्था के जरिए बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहनेवालों को राशन की आपूर्ति की जाती है। दरअसल इस कानून को यह मानकर बनाया गया है कि सभी किसानों के पास भूमि हैं। चाहे आप एमएसपी की बात करें या उर्वरक में छूट देने की। सभी सुविधाएं भूमि वाले किसानों के लिए है। छोटे किसानों को तो एमएसपी का लाभ मिलता ही नहीं है। इसकी एक वजह तो यह कि उनकी उपज ही बहुत कम होती है और दूसरी यह कि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वे अपनी फसल को संजोकर रख सकें या सरकारी मंडी तक ले जा सकें। इस कारण वे बिचौलियों व स्थानीय व्यापारियों के हाथों औने-पौने दाम पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हो जाते हैं।
यह भी पढ़ें – दिल्ली में किसानों का डेरा : श्रमजीवी सिक्ख-शूद्र बनाम ब्राह्मणवादी परजीवी
इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा किसान आंदोलन के केंद्र में भारत सरकार द्वारा बनाए गए तीन कानून हैं और किसानों को यह डर है कि इसके कारण जमीन पर उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन इनके आंदोलन के मुद्दों में वे किसान शामिल क्यों नहीं हैं, जिनके पास जोत कम है या फिर जो भूमिहीन हैं? एक तरफ सरकारें इन्हें किसान नहीं मानतीं तो दूसरी ओर बड़े किसान संगठनों के लिए भी ये किसान नहीं हैं। अधिकतर लोग जिनके पास जोत ज्यादा है, खुद खेती नहीं करते। वे अपने खेत को अधिया, रेगहा, बटाई के रूप में गरीब भूमिहीनों को दे देते हैं। फिर वे अपनी मेहनत और पैसे के बल पर फसलें उगाते हैं और उत्पादन का बड़ा हिस्सा कभी अनाज के रूप में तो कभी नकद के रूप में जमीन के मालिकों को देते हैं।
दस्तावेजीकरण नहीं होने के कारण सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग, कितनी भूमि अधिया, बटाई पर लेते हैं? इसका भी एक खास कारण है सभी जमीन मालिक अपनी भूमि को गुपचुप तरीके से बटाई पर देते हैं। इसकी किसी प्रकार से कोई लिखा-पढ़ी करने से डरते हैं। इसका कारण यह है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि यदि वे लिखित समझौता करने के बाद जमीन को बटाई पर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि उनकी जमीन कोई और बो रहा है। फिर तीन साल तक जमीन बोना सिद्ध करके बटाईदार अपने नाम पर जमीन करा लेंगे।
बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं कि यदि बहुजन किसानों के सवालों को भी आन्दोलन में शामिल किया जाता तो वे भी इसमें भागीदारी करते और आंदोलन का स्वरूप और व्यापक होता।
(संपादन : नवल/अनिल/अमरीश)
(अलेख परिवर्द्धित : 15 जनवरी, 2021 02:37 PM)