उत्तर भारत के मीडिया पर दलित-बहुजन तबकों की ओर से लगातार यह आरोप लगते रहे हैं कि यहां उनकी बात नहीं सुनी जाती। बड़े मीडिया घरानों के पत्रकार इस कदर जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त होते हैं कि वे आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर हुए जुल्म की खबरों का मजाक उड़ाते हैं। ये स्थिति प्रिंट और इलेक्ट्रानिक दोनों माध्यमों में समान रूप से देखी जा सकती है। उदाहरणस्वरूप, देश में दलित-बहुजन तबके की महिलाओं के साथ रोजाना सैकड़ों बलात्कार और जबरदस्ती की घटनाएं होती हैं लेकिन इन खबरों को कहां दबा दिया जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन वहीं यदि किसी सवर्ण और कुलीन महिला के साथ जबरदस्ती की जाती है तो मीडिया आसमान को सर पर उठा लेता है। क्या यहां भारतीय मीडिया का अंतर्विरोध साफ-साफ नहीं दिख जाता? आइए, जानते हैं, इसके बाबत अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अशोक चौधरी से क्या कहा।

उदितराज
राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन जस्टिस पार्टी
यह बात एकदम सही है। मीडिया में दलितों की खबरों को जगह ही नहीं मिलती है। मीडिया ने ‘आप’ को मोदी के बराबर जगह दे रखा है जबकि दलित समाज के लिए उसके पास जगह नहीं है। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखना होगा। सामाजिक न्याय को लेकर मीडिया का रवैया बहुत खराब है। दलितों को अपनी बात रखने के लिए मीडिया हाउस की जरूरत तो है ही।

संजय पासवान
पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा एससी मोर्चा
सबसे पहले तो हमें अपने समाज में ही बराबरी लाना होगा। ऐसा नहीं है कि दलित-बहुजन ने अपना मीडिया हाउस खोलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इसीलिए इसी मीडिया में समन्वय बनाकर जगह बनानी होगी। सामाजिक न्याय को सबसे पहले नीचे से सुधारना होगा तभी हम ऊपर की जातियों से न्याय के लिए लड़ सकते हैं।

रवीश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी
मीडिया में दलितों की बात नहीं सुनी जाती है ऐसा नहीं है। मीडिया उसको कवर करता है, अनुपात में असमानता हो सकती है। चंद्रभान प्रसाद का लेख ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ में छपता है। हिन्दी के भी कुछ अखबार दलित आवाज को जगह देते हैं। मगर यह कवरेज घटना प्रधान है। इसका भाव सीमित होता है। जैसे दलितों का घर जल गया, उसको कवर करेगा, मगर आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर जमा लाखों लोगों की बात नहीं करेगा। जैसे औरतों के साथ उत्पीडऩ के मामले में पुरुष मानसिकता की धुलाई होती है वैसे मीडिया सवर्ण मानसिकता को टारगेट नहीं करता। उसे दलित और पिछड़े ही जातिवादी नजर आते हैं। राजनीति में जिस जातिवाद की आजकल आलोचना होती है, मीडिया उसका मतलब दलित-पिछड़ों की राजनीति बताता है, सवर्ण मानसिकता को नहीं। इसलिए दलित चिंतन को जगह देते हुए भी वह पूर्वाग्रहों को नहीं छोड़ता। इस मामले में मैं मीडिया से कोई उम्मीद नहीं करता। उसके पास इन मसलों पर सोचने-लिखने के लिए लोग नहीं हैं, और हैं भी तो उनकी कोई औकात नहीं है ।

प्रेमपाल शर्मा
वरिष्ठ कहानीकार, विचारक
सबसे पहले मैं इस आरोप से विक्षुब्ध हूं। शायद यह सब कुछ हमने आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से सीखा है। इस देश का मीडिया और उसका बुद्धिजीवी तबका भी छाया युद्ध लड़ रहा है। शिक्षाविद् कृष्ण कुमार के शब्दों में कहूं तो इस देश का पढ़ा-लिखा नागरिक ज्यादा सांप्रदायिक, धर्मांध, जातिवादी है, बजाय गरीब अनपढ़ों के, क्योंकि उन्होंने इन आरोपों को गढऩे-मढऩे के लिए तथ्य इकट्ठे नहीं किए हैं। मीडिया में काम करने वाले तो समाज के सबसे समझदार बुद्धिजीवी होते हैं, उन्हें तो सबसे पहले ऐसे विभाजन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समाज के दलित-पिछड़े और सबसे ऊपर गरीब को आगे लाने के लिए विशेष प्रयास, विशेष रियायतों की जरूरत है। यदि मीडिया भी दलित, बहुजन, ब्राह्मण, सिया, सुन्नी, बिहारी, हरियाणवी, गुजराती के खाने में बंटा तो इस देश का कोई भविष्य नहीं है और न ही मीडिया का भविष्य है। इस प्रसंग में ‘इंडिया टुडे’ के ताजा अंक (11 दिसंबर, 2013) में तहलका प्रकरण पर तसलीमा नसरीन की टिप्पणी गौर करने लायक है-‘राजनेताओं या कट्टपंथियों के पथभ्रष्ट होने से देश का नुकसान उतना नहीं होता जितना बुद्धिजीवियों के पथभ्रष्ट होने से होता है।’ मीडिया के बुद्धिजीवी जातिवाद से दूर नहीं हुए तो खुदा ही मालिक है।
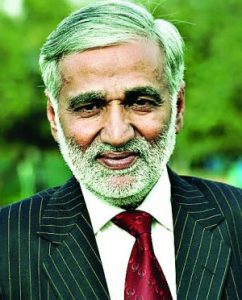
उर्मिलेश
वरिष्ठ पत्रकार
सिर्फ दलित-पिछड़ों की ही नहीं बल्कि किसी भी उत्पीडि़त समुदाय और समाजों की खबरों की मुख्यधारा की मीडिया में उपेक्षा होती है। यह कोई नई बात नहीं है। यह सिलसिला बहुत पुराना है। लेकिन भारत में आर्थिक सुधारों के बाद एक उम्मीद बंधी थी कि शायद भारत का मीडिया पुरानी सामंती सोच वाली संरचना और पिछड़ों के विवादों से बाहर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कथित आर्थिक झंडाबरदारों के साथ सामंती सोच वाली संरचना का गठबंधन-सा हो गया। मीडिया के कारपोरेटीकृत माहौल में दलित-पिछड़ों के साथ हाशिए पर खड़े जितने भी समाज और समुदाय हैं वो सभी उपेक्षा के शिकार हैं। अब तो गांवों, छोटे शहरोंं, कस्बों की खबरें गायब हो रही हैं। ऐसे माहौल में सिर्फ वैकल्पिक मीडिया एक जरिया बनता है जो सूचना और विचार के पूरे तंत्र पर एकाधिकारवादियों के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है।

अविनाश दास
संपादक, मोहल्ला लाइव
भारतीय मीडिया के बारे में प्रचारित धारणा भले ही निरपेक्ष, लोकतांत्रिक संस्था के रूप में हों, लेकिन सच यही है कि इसकी पूरी संरचना भारतीय समाज की अपनी विसंगतियों से अलग नहीं है। इसलिए अगर दलित-बहुजन भारतीय मीडिया पर उनकी बात अनसुनी करने का आरोप लगाते हैं, तो वह अकारण नहीं है। दूसरी बात, मीडिया अब पूरी तरह से कारोबारी संस्था हो चुका है। टर्न-ओवर की चिंता उसकी प्राथमिकता है, न कि खबरों की विश्वसनीयता। अभी के हालात में वहां सामाजिक सुधार की कोई भी प्रक्रिया मुश्किल है। ऊंचे पदों पर ऊंची जाति का कब्जा है और गलती से कोई बहुजन नेतृत्व वहां जाता भी है, तो उन्हीं के हितपोषण की अतिरिक्त कोशिश करता हुआ दिखता है। सिर्फ पूंजी का दबाव ही वहां काम कर सकता है। लिहाजा समृद्ध दलित-बहुजनों के लिए तो वहां एकाध गुंजाइश निकलते हुए तो हम देखते हैं, पर उसे सामान्य न्याय के रूप में नहीं देख सकते। दलित-बहुजन को अपने मीडिया-विकल्प पर इसलिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि देश को देखने के उनके नजरिए के प्रसार की आज बहुत सख्त जरूरत है। जब दलित-बहुजन की वैकल्पिक राजनीति के लिए देश में जगह बन सकती है, तो उनके वैकल्पिक मीडिया का भी स्वागत किया जाएगा। हां, ऐसे मीडिया का ढांचा अगर कॉरपोरेट की जगह कॉपरेटिव होगा, तो वह समग्रता में भारत के मुख्यधारा के मीडिया के विकल्प की तरह भी खड़ा हो पाएगा।
(फारवर्ड प्रेस के जनवरी, 2014 अंक में प्रकाशित )
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in





