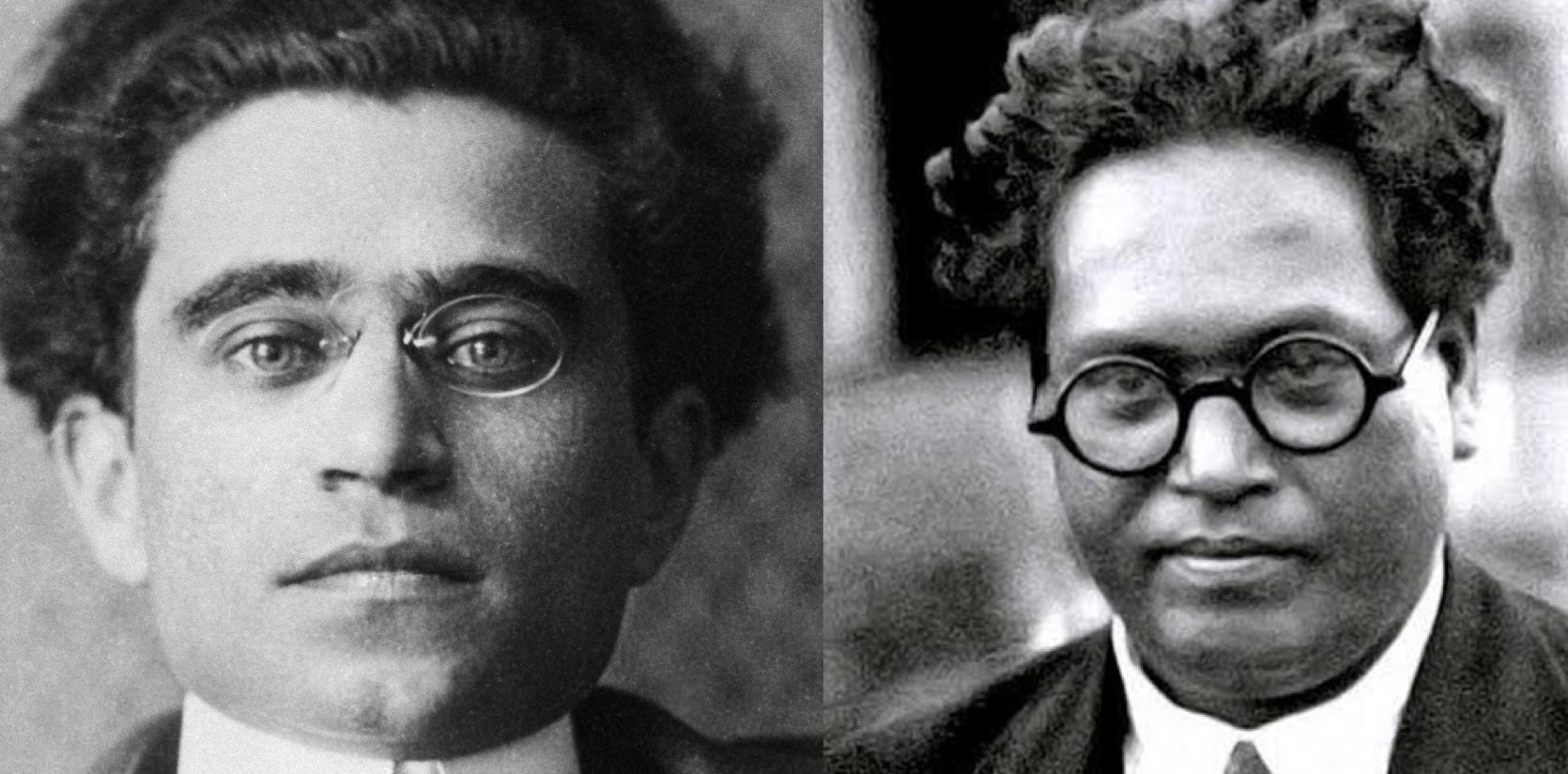इंग्लैंड से पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद जब युवा आंबेडकर भारत पहुंचे तो जाति-आधारित भारतीय समाज ने उन्हें यह याद दिलाने में तनिक भी देरी नहीं की कि वे अछूत हैं. बाबासाहेब ने स्वयं अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुआ लिखा कि बडौदा में न तो कोई हिन्दू और ना ही मुसलमान उन्हें “किराये पर मकान देने को तैयार था“. इसके लगभग एक सदी बाद, पिछले सितम्बर में, बिहार के मधुबनी जिले में स्थित एक मंदिर को, तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की यात्रा के बाद, धोया गया.
ये दोनों घटनाएँ उस भेदभाव और यंत्रणा का छोटा-सा उदाहरण मात्र हैं, जिनका सामना सामान्य दलित अपने दैनिक जीवन में निरंतर करते हैं. अगर मुख्यमंत्री जैसे शक्तिशाली दलित को ‘अपवित्र’ माना जा सकता है तो साधारण दलित की बिसात ही क्या है.
इसके बावजूद, कई प्रतिष्ठित भारतीय समाजशास्त्री, अछूत प्रथा व जाति के अभिशाप की गंभीरता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. उलटे, वे जाति की संस्था में कथित ‘गतिशीलता’ और ‘परिवर्तनीयता’ पर जोर देते हुए परोक्ष रूप से यह कहते हैं कि जातिवाद केवल एक “अफवाह“ है और अछूत प्रथा अब प्रासंगिक नहीं रह गयी है.
उदाहरणार्थ, जानेमाने समाजशास्त्री आंद्रे बेटिल्ले का दावा है कि शुद्धता-अशुद्धता से सम्बंधित कठोर नियम, जैसे एक साथ बैठ कर भोजन न करना, काफी हद तक शिथिल हो गए हैं (द हिन्दू, २१ फरवरी, २०१२). यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उनके ये विचार, उनके गुरु एमएन श्रीनिवास की याद दिलाते हैं. श्रीनिवास, जो कि भारतीय समाजशास्त्र के पितामह माने जाते हैं, ने अपने एक शोधपत्र (“एन ओबिचुअरी ऑफ़ कास्ट एज अ सिस्टम””, जो बाद में “इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली””, १ फरवरी, २००३ में प्रकाशित हुआ), में उन्होनें स्थिति का अति-सामान्यीकरण करते हुए यह घोषित कर दिया कि जाति प्रथा या तो मर चुकी है या मृत्यु शैय्या पर है. ““मुझे पूरा विश्वास है कि यह (जाति) व्यवस्था, जो दो हज़ार सालों से चली आ रही है, समाप्त होने की कगार पर है””, उन्होंने लिखा.

क्या जाति प्रथा सचमुच समाप्त होने की कगार पर है? तथ्य तो ऐसा नहीं कहते. पिछले दो दशकों में देश में हुए कई सर्वेक्षणों, मैदानी अध्ययनों और सैद्धांतिक कृतियों से यह साफ़ है कि अछूत प्रथा – किसी पुरानी आदत की तरह – आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी. परन्तु जहाँ अछूत प्रथा ख़त्म नहीं हुयी है वहीं यह भी सही है कि आधारभूत ढांचे, शिक्षा व स्वस्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकार के हस्तेक्षप के कारण इसके प्रचलन में निश्चित रूप से कमी आयी है. जैसा कि अतिफ रब्बानी ने फारवर्ड प्रेस के मार्च २०१५ अंक में अपने लेख (“छूट नहीं रहा छुआछूत”) में लिखा है, भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस-२) के अनुसार, हर चार में से एक भारतीय छुआछूत में विश्वास करता है और देश का कोई धर्म, जाति, जनजाति या क्षेत्र इस सामाजिक बुराई से मुक्त नहीं है. यह सर्वेक्षण नेशनल काउंसिल ऑफ़ एप्लाइड इकनोमिक रिसर्च और अमरीका के मेरीलैंड विश्वविद्यालय ने किया था.
इसके पूर्व, सुखदेव थोरात ने अपने सर्वेक्षण “दलितस इन इंडिया”, २००९ में पाया कि उच्च शिक्षित व आर्थिक दृष्टी से संपन्न भारतीय भी अछूत प्रथा से उपजे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं. उन्होंने विस्तार से बताया कि सार्वजनिक जीवन में दलितों को किस हद तक छुआछूत का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार उनके साथ सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के मामले में भेदभाव किया जाता है. इसके अतिरिक्त, उन पर जाति-आधारित अत्याचार तो होते ही हैं. उदाहरणार्थ, “भारतीय गांव जाति-आधारित टोलों में बंटे रहते हैं और एक जाति के लोगों के घर आसपास होते हैं” (पृष्ठ १३४). इसी प्रकार, “ग्रामीण क्षेत्रों में ४८ प्रतिशत दलितों की पीने के पानी के स्त्रोतों तक पहुँच नहीं थी और ३५ प्रतिशत के साथ गाँव की दुकानों में भेदभाव होता था” (पृष्ठ १३६).
ग्रामीण इलाकों में अछूत प्रथा की अपने संयुक्त अध्ययन (अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया, २००६) में जाने-माने अध्येता घनश्याम शाह, सुखदेव थोरात, सतीश देशपांडे, अमिता बाविस्कर व हर्षमंदर ने पाया कि अछूत प्रथा कतई समाप्त नहीं हुयी है. डेढ़ साल (२००१-०२) चले इस अध्ययन में ११ राज्यों के ५६५ गांवों का सर्वेक्षण किया गया. अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि “अछूत प्रथा जीवित है, यद्यपि उसके स्वरुप बदल गया है और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों व देश के विभिन्न इलाकों में उसका प्रचलन अलग-अलग रूपों में है” (पृष्ठ ४८)
इसी तरह, प्रसिद्द राजनीतिशास्त्री गोपाल गुरु अपने लेख “दलित मिडिल क्लास हेंग्स इन एयर” (इम्तियाज़ अहमद व हेलमुट रेफेल्ड द्वारा सम्पादित “मिडिल क्लास वेल्लूज़ इन इंडिया एंड वेस्टर्न यूरोप”, २००१) में उच्च जातियों के मध्यमवर्गीय लोगों द्वारा अपने आर्थिक वर्ग के दलित सदस्यों के साथ किये जाने वाले भेदभाव की चर्चा की है. वे लिखते हैं कि मध्यमवर्गीय दलितों को अक्सर जातिगत अपशब्द सुनने पड़ते हैं. इसलिए दलितों व द्विज हिन्दुओं के पारस्परिक सम्बन्ध तनावपूर्ण रहते हैं. अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर गुरु लिखते हैं कि पुणे में मध्यमवर्गीय दलितों को उच्च मध्यमवर्गीय रहवासी इलाकों में मकान नहीं लेने दिया जाता था.
यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले भारतीय दलितों को भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है. इंग्लॅण्ड में रह रहे प्रवासी दलित भारतीयों का आरोप है कि उच्च जातियों के हिन्दू उनके साथ स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों व सामाजिक जीवन में भेदभाव करते हैं.
एक दलित संगठन की रपट के अनुसार, “इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि इंग्लॅण्ड में जातिगत भेदभाव कई रूपों में विद्यमान है. दलितों के साथ रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्तुओं व सेवाओं के प्रदाय, राजनीति और हिन्दू मंदिरों में प्रवेश के मामलों में भेदभाव किया जाता है”. अछूत प्रथा के भारत से विदेशों में निर्यात की प्रक्रिया को समझाते हुए जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में कार्यरत समाजशास्त्री विवेक कुमार (के एल शर्मा व रेणुका सिंह द्वारा सम्पादित “ड्यूल आइडेंटिटी”, २०१३ में “द न्यू दलित डायस्पोरा: ए सोशिओलोजिकल एनालिसिस”) लिखते हैं कि जाति में जकड़े समाज, जिसमें रिश्तों का आधार जाति होती है, में जन्मे भारतीय जब विदेश जाते हैं तो वे अपने साथ अपने जातिगत मूल्य भी ले जाते हैं. कुमार आगे लिखते हैं कि चूँकि एक जाति के लोग नौकरी, ऋण, जीवनसाथी आदि पाने में एक-दूसरे की सहायता करते हैं, इसलिए जाति, सामाजिक संव्यवहार का महत्वपूर्ण तत्त्व बन जाती है.
कुल मिलाकर, सुदूर गांवों से लेकर महानगरों तक, अछूत प्रथा जीवित है. नस्लवाद की तरह, अछूत प्रथा, जिसे दशकों पहले गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था, आज भी खुले और दबे-छुपे दोनों रूपों में अस्तित्व में बनी हुयी है.
फारवर्ड प्रेस के अप्रैल, 2015 अंक में प्रकाशित