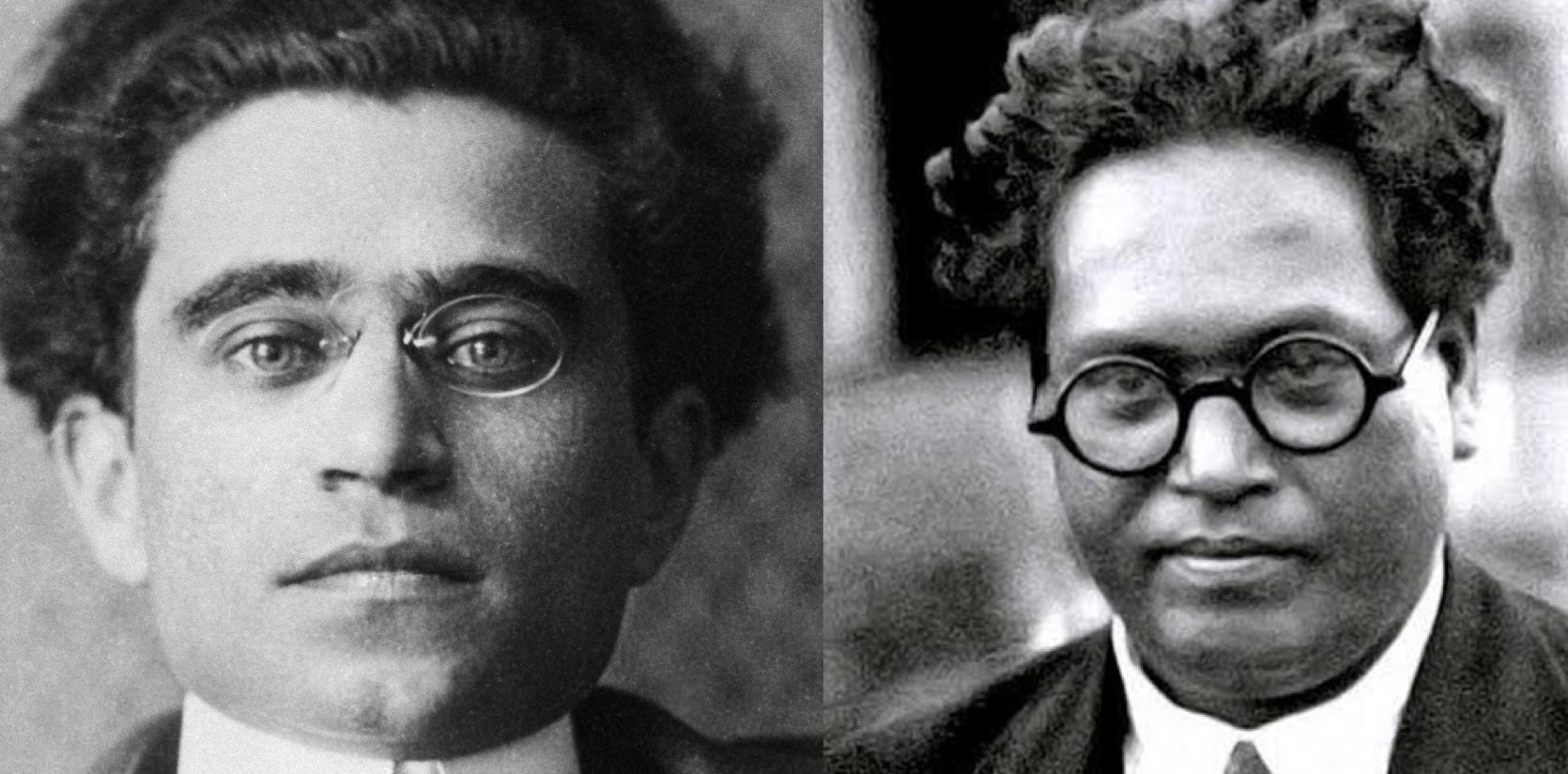मंदिरों को समर्पित देवदासियों का महिमामंडन, भले ही ईश्वर की सेविका के रूप में किया जाता रहा हो, परंतु असल में वे वेश्याएं हुआ करतीं थीं। देश के कई भागों में हिंदू मंदिरों में देवदासियां थीं और उन्हें मंदिरों का अभिन्न अंग माना जाता था। वे, दरअसल, इसलिए रखी जातीं थीं ताकि वे मंदिरों के पंडे-पुजारियों और उन रईसों, जो वहां तीर्थयात्रा के बहाने आते थे, की शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकें। ये महिलाएं लोगों को मंदिरों की ओर आकर्षित करतीं थीं और मंदिरों की लोकप्रियता बढ़ाती थीं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर और यहां तक कि तमिलनाडु के मंदिरों में भी देवदासियां होती थीं।
मार्च में एक अखबार में प्रकाशित रपट में कहा गया है कि देश की आखिरी देवदासी शशिमणि, जो कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुईं थीं, की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही, इस शर्मनाक प्रथा का अंत हो गया है। फ्रेंकोइस बर्नियर (1620-1688) एक फ्रांसीसी चिकित्सक व यात्री थे। मुगल भारत की यात्रा का उनका विवरण, उस समय के इतिहास के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जाता है। वे शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र शहजादा दाराशिकोह के व्यक्तिगत चिकित्सक थे और दाराशिकोह की मौत के बाद, वे औरंगजेब के दरबार से लगभग एक दशक तक जुड़े रहे। उन्होंने पुरी की यात्रा की थी। बर्नियर के अनुसार, हर साल पुरी में रथयात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ का विवाह एक नई युवती से किया जाता था। विवाह की पहली रात, मंदिर का कोई एक पुजारी उसके साथ संभोग करता था।

मार्च 1912 में बंगाल की विधान परिषद में छोटा नागपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकृष्ण सहाय ने ”बच्चियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को समर्पित करने की प्रथा’’ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, ”बड़े होने के बाद वे अनैतिक जीवन जीती हैं’’। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह इस ”अनैतिक प्रथा का उन्मूलन’’ करने के लिए हस्तक्षेप करे (बंगाल विधान परिषद की कार्यवाही खंड 34)। औपनिवेशिक सरकार ने अपनी नीति के अनुरूप, परिषद को बताया कि वह ”हिंदू समाज द्वारा पुरी की व्यवस्था से जुड़ी बुराईयों का उन्मूलन करने के किसी भी संगठित प्रयास का अनुमोदन करेगी और उसे अपना समर्थन देगी।’’
ब्रिटिश शासकों ने ”धर्म से जुड़े मसलों में सुधार के लिए कोई स्वस्फूर्त प्रयास’’ करने से साफ इंकार कर दिया। ”द न्यूयार्क ट्रिब्यून’’ के 8 अगस्त, 1853 के अंक में छपे अपने लेख में कार्ल माक्र्स ने भारत की ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ”वह ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि वह उड़ीसा और बंगाल के मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों और जगन्नाथ मंदिर में चलने वाले हत्या और वेश्यावृत्ति के व्यापार से धन कमाना चाहती है’’ (माक्र्स एंड एंजिल्स, सिलेक्टिड वक्र्स, खंड 1)। यह कोई झूठा आरोप नहीं था बल्कि तथ्यों पर आधारित झिड़की थी। इसके 74 साल बाद, सन् 1927 में, मोहनदास करमचंद गांधी ने यही बात कही: ”मुझे यह कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे देश के कई मंदिर वेश्यालयों से अलग नहीं हैं’’ (‘यंग इंडिया’ 6 अक्टूबर 1927)। ‘द हिंदू’ अखबार ने 15 सितंबर 1927 को गांधीजी को उद्धृत करते हुए लिखा, ”उनको देवदासियां कहकर हम धर्म के पवित्र नाम पर ईश्वर अपमान करते हैं और अपनी इन बहनों का अपनी वासना पूर्ति के लिए उपयोग कर हम दोगुना अपराध करते हैं…।’’
मंदिरों में पल रही इन विकृतियों को उजागर करने वाले केवल कार्ल माक्र्स ही नहीं थे। 19वीं सदी में हुगली (अब पश्चिम बंगाल) के तारकेश्वर मंदिर के आसपास ढेर सारे वेश्यालय थे। इस अत्यंत समृद्ध तीर्थस्थल के महंत माधवचंद्र गिरी, अपने गुंडों का इस्तेमाल कर सीधी-साधी महिलाओं को अगवा करने, बहलाने-फुसलाने और उनकी खरीद-फरोख्त करने के लिए कुख्यात थे। ”ये महिलाएं अपने परिवारों के पास वापस नहीं जा सकती थीं और उनके पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता था कि वे तारकेश्वर के आसपास स्थित वेश्यालयों में अपना जीवन बिताएं। सन 1873 में अखबार, पुरी और तारकेश्वर मंदिरों के पंडों के कुत्सित कारनामों के विवरण से भरे रहते थे…तारकेश्वर, महिलाओं के गैरकानूनी व्यवसाय का केन्द्र था’’, तनिका सरकार, ”हिंदू वाईफ, हिंदू नेशन : कम्युनिटी, रिलीजन एंड कल्चरल नेशनलिज्म’’ में लिखती हैं। सन् 1871 की जनगणना के अनुसार, हुगली जिले में असम, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के सभी जिलों से ज्यादा संख्या में वेश्याएं थीं। केवल 24 परगना जिले में वेश्याओं की संख्या हुगली से ज्यादा थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के धनी जमींदार, पुरी आते रहते थे और उनके इरादे कतई पवित्र नहीं होते थे। कई जमींदार दो-तीन महिनों तक पुरी में रहते थे और उनकी यात्रा पर लाखों रूपये खर्च होते थे। इस खर्च की वसूली के लिए वे गैरकानूनी चुंगी या अबवाव (जैसे हतभरा महाप्रसाद व बारून्निस्नान) लगाते थे। ये बातें उड़ीसा के बालासोर जिले के कलेक्टर जॉन बीम्स ने बंगाल सरकार को 1871 में भेजी अपनी एक रिपोर्ट में कही।
सिफलिस का सड़ांध मारता दलदल
अपनी पुस्तक ”अनहैपी इंडिया’’ (1927) में स्वाधीनता संग्राम के साहसी योद्धा लाला लाजपतराय ने यह पता लगाने का काफी श्रमसाध्य प्रयास किया है कि आखिर सिफलिस भारत कैसे पहुंचा। यह रोग इस क्षेत्र में नहीं उपजा था। चिकित्सा के तत्कालीन जानेमाने अध्येता डॉ. अवान ब्लोच को उद्धृत करते हुए लाला लिखते हैं, ”सिफलिस, कोलंबस के नाविकों के जरिये 1494 व 1495 में स्पेन पहुंचा। इसे वे लोग मध्य अमरीका, विशेषकर हैती द्वीप समूह, से स्पेन लाए थे। स्पेन से यह चाल्र्स सप्तम की सेना के साथ इटली पहुंच गया, जहां इसने महामारी का रूप ग्रहण कर लिया। बाद में इस सेना को तोड़ दिया गया और सैनिक इस रोग को अपने साथ यूरोप के अन्य देशों में ले गये। इसे पुर्तगाली सुदूरपूर्व – भारत, चीन और जापान – में लाए।’’ अपनी मौलिक कृति ”द द्रविडिय़न एलिमेंट इन इंडियन कल्चर’’ में गिल्बर्ट स्लेटर बताते हैं कि किस प्रकार मद्रास से 300 किलोमीटर दूर स्थित कुंभकोणम नगर के देवदासियों से भरे 12 महान मंदिरों के पुजारियों ने अपनी पत्नियों को सिफलिस से ग्रस्त कर दिया था।
इससे साफ होता है कि इस रोग के मुख्य ‘सरंक्षक’ उच्च जाति के श्रेष्ठीवर्ग के सदस्य थे, जिनकी मंदिरों तक पहुंच थी। आज भी नीची जातियों के लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
परन्तु अंग्रेजों को मंदिरों की वेश्याओं का भोग करने का मौका कैसे मिला? सेरामपोर के विलियम वार्ड नामक एक मिशनरी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास के इस लगभग अल्पज्ञात पक्ष पर प्रकाश डाला है। ‘हिस्ट्री, लिटरेचर एंड माइथोलॉजी ऑफ द हिंदूज खंड 2’ में वे लिखते हैं, ‘कांजीवरम में एक टूटा-फूटा शिव मंदिर था, जिसे ठीक करवाने की कोई फिक्र नहीं कर रहा था। एक अँगरेज अधिकारी ने (ईस्ट इंडिया) कंपनी को मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने के लिए राजी कर लिया एवं खुद भी इस हेतु धनराशि दान की’। इससे निश्चित रूप से कंपनी को मंदिर के कर्ताधर्ताओं की कृतज्ञता और कंपनी के अधिकारियों को मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच हासिल हो गई होगी। प्रारंभ में, कंपनी के अधिकारी अपनी पत्नियों को अपने साथ भारत नहीं लाते थे और मंदिरों की देवदासियों से अपनी शारीरिक भूख मिटाते थे। मंदिरों के पुजारी और ब्रिटिश अधिकारी दोनों देवदासियों से सम्भोग करते थे और इस तरह, पंडे-पुजारियों ने अपनी पत्नियों को सिफलिस का रोगी बना दिया।
सन 1803 में, कम्पनी द्वारा उड़ीसा पर कब्जा करने के बाद, जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने उसका प्रबंधन अंग्रेजों को सौंप दिया। इस हस्तांतरण की शर्तों के अनुसार, मंदिरों के पुजारियों व देवदासियों सहित सभी कर्मचारियों को कंपनी, मंदिर के कोष से वेतन देती थी। यह सिलसिला सन 1841 तक चला, जब कम्पनी ने मंदिर के प्रबंधन से अपने हाथ खींच लिए। पुरी आने वाले तीर्थयात्रियों से रुपये 2 से रुपये 10 प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क वसूला जाता था। एक बांग्ला पत्रिका (ब्रिजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, ‘सम्बाद्पत्रे सेकालेर कथा’ अंक 2) ने 1831 में खुलासा किया कि 17 सालों में, राजस्व अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों से 9,92,050 रुपये (अर्थात रू 58,355 प्रति वर्ष) वसूले। सन 1997 में 16 दिसंबर को, शशिमोनी और पारसमोनी नामक दो देवदासियों (जिन्हें उडिय़ा में महारी कहा जाता है) ने ‘ओडीसी विजऩ एंड मूवमेंट सेंटर’ के तत्वावधान में कलकत्ता में सार्वजनिक रूप से नृत्य प्रदर्शन किया। एक मीडिया रिपोर्ट (बैजयंती रे, ‘ब्राइड्स ऑफ द लार्ड’, द एशियन ऐज, कलकत्ता) में उन्हें यह कहते हुए उद्धत किया गया कि ‘हमारा जन्म उच्च वर्गीय कायस्थ परिवारों में हुआ था और हमें महारियों ने उनकी तरह बनाने के लिए गोद ले लिया था। ‘
दक्षिण भारत की योगिनियाँ
ईश्वर के नाम पर शोषण का अंतहीन सिलसिला जारी है। दक्षिण भारत के राज्यों में, अनुसूचित जातियों की युवा स्त्रियाँ, वर्चस्वशाली समुदाय के सदस्यों की वेश्या के रूप में सेवा करती हैं। सन 2007 में ‘एंटी-स्लेवरी इंटरनेशनल’ ने कर्मकांडी सेक्स गुलामी या जबरिया धार्मिक ‘विवाह’ पर एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन से यह सामने आया कि 93 प्रतिशत देवदासियां और योगिनियाँ अनुसूचित जातियों से और सात प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से थीं। जाहिर है कि यह कुप्रथा उन अनेक तरीकों में से एक है, जिनका इस्तेमाल वर्चस्वशाली जातियां अपना सामाजिक रुतबा और आर्थिक प्राधान्य बनाये रखने के लिए करती हैं। जो लड़कियां देवदासी या योगिनी बनती हैं, वे विवाह नहीं कर सकतीं और समाज उन्हें नीची निगाहों से देखता है। योगिनियों के बच्चों का जीवन नरक हो जाता है क्योंकि कोई उनका पिता होना स्वीकार नहीं करना चाहता।
भारत में भेदभाव, सामाजिक यथार्थ का हिस्सा है। उससे श्रेष्ठी और शासक वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता। योगिनी प्रथा को समाप्त करने से ईश्वर का प्रकोप लोगों पर होगा, यह भय दिखाकर शक्तिशाली, वर्चस्ववादी जातियों के निहित स्वार्थी तत्व इस कुत्सित परंपरा को जीवित रखने का प्रयास कर सकते हैं।
फारवर्ड प्रेस के नवंबर 2015 अंक में प्रकाशित