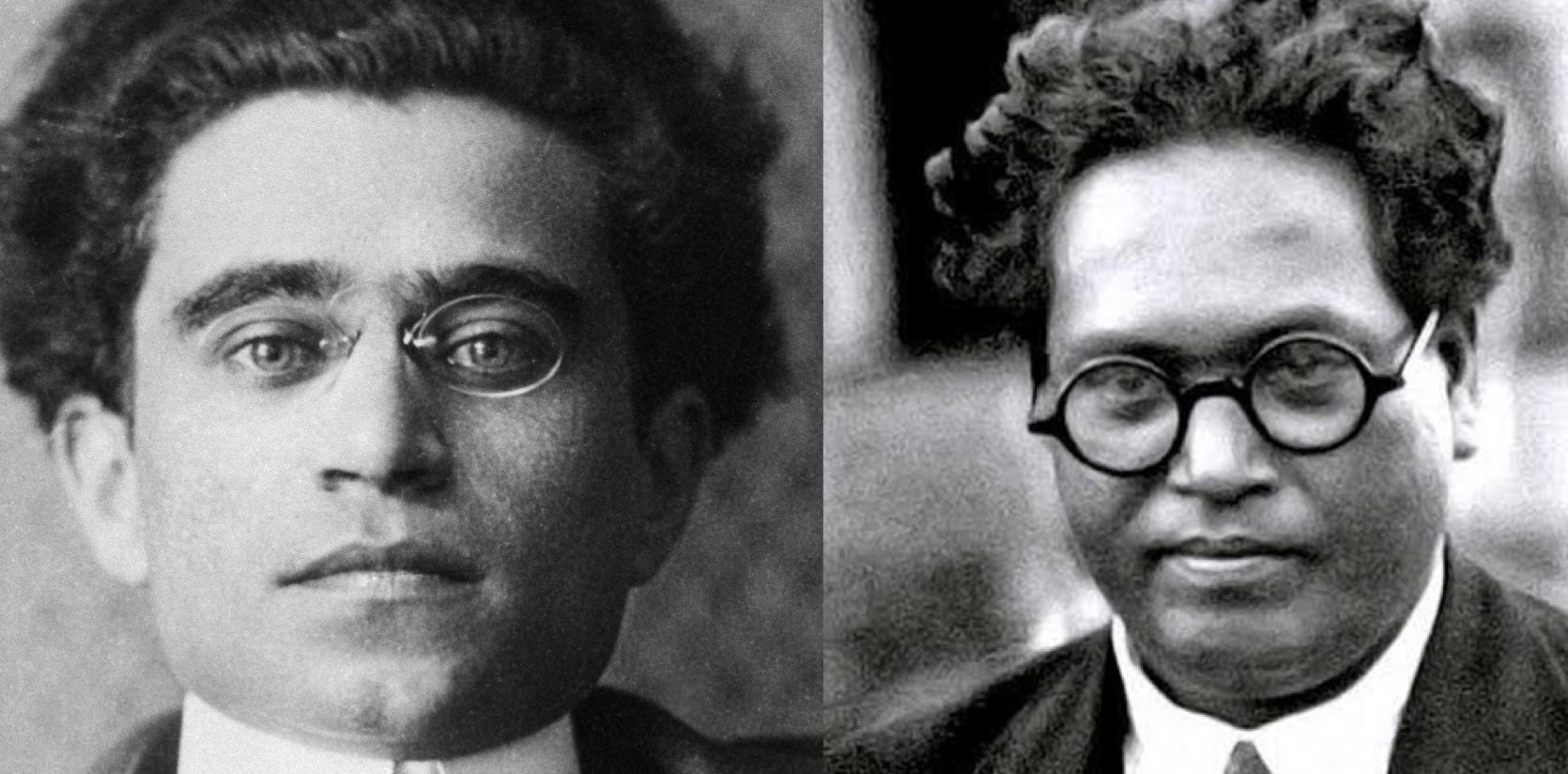इसी मार्च की बात है। दो युवा कार्यालय में आए। उनमें से एक जेएनयू से पढ़कर सरकारी नौकरी में था, दूसरा वहीं से एमफिल कर रहा था। चौकाने वाली बात थी कि उनके हाथ में ‘फारवर्ड प्रेस’ का ताजा अंक था। उन दिनों संसद में जेएनयू का मामला गर्माया हुआ था। मानव संसाधन मंत्री संसद में ‘महिषासुर शहादत’ वाला पर्चा लहरा चुकी थीं और अपने बेहद नाटकीय भाषण के कारण चर्चा में थीं। ऐसे में कोई युवा ‘फारवर्ड प्रेस’ का अंक हाथ में लिए घूमे तो बात चौकाने वाली ही थी। बातचीत के दौरान उनमें से एक ने बताया कि वह ‘सस्पेंड’ चल रहा है। क्या उसके निलंबन का संबंध जेएनयू की हाल की घटना से है मैं जानना चाहता था, परंतु एकाएक पूछना उचित नहीं समझा। पत्रिका कहां से मिली सवाल पर एक ने हंसकर बताया कि बाहर कोई बांट रहा है। बाद में उसने स्वीकार किया कि पत्रिका में आती है और वहां उसकी 1500 प्रतियों की खपत है। मुझे इस आंकड़े की हकीकत का अंदाजा नहीं।यदि यह सच है तो किसी भी पत्रिका के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। ऐसा विश्वविद्यालय जो देश के उच्चतम शिक्षा संस्थानों में आता हो, जिसकी प्रतिष्ठा वहां के खुले, लोकतांत्रिक परिवेश के कारण हो, वहां एक पत्रिका के 1500 अंकों की खपत, उस पत्रिका की विश्वनीयता और जरूरत दोनों को स्थापित करती है।
इसी मार्च की बात है। दो युवा कार्यालय में आए। उनमें से एक जेएनयू से पढ़कर सरकारी नौकरी में था, दूसरा वहीं से एमफिल कर रहा था। चौकाने वाली बात थी कि उनके हाथ में ‘फारवर्ड प्रेस’ का ताजा अंक था। उन दिनों संसद में जेएनयू का मामला गर्माया हुआ था। मानव संसाधन मंत्री संसद में ‘महिषासुर शहादत’ वाला पर्चा लहरा चुकी थीं और अपने बेहद नाटकीय भाषण के कारण चर्चा में थीं। ऐसे में कोई युवा ‘फारवर्ड प्रेस’ का अंक हाथ में लिए घूमे तो बात चौकाने वाली ही थी। बातचीत के दौरान उनमें से एक ने बताया कि वह ‘सस्पेंड’ चल रहा है। क्या उसके निलंबन का संबंध जेएनयू की हाल की घटना से है मैं जानना चाहता था, परंतु एकाएक पूछना उचित नहीं समझा। पत्रिका कहां से मिली सवाल पर एक ने हंसकर बताया कि बाहर कोई बांट रहा है। बाद में उसने स्वीकार किया कि पत्रिका में आती है और वहां उसकी 1500 प्रतियों की खपत है। मुझे इस आंकड़े की हकीकत का अंदाजा नहीं।यदि यह सच है तो किसी भी पत्रिका के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। ऐसा विश्वविद्यालय जो देश के उच्चतम शिक्षा संस्थानों में आता हो, जिसकी प्रतिष्ठा वहां के खुले, लोकतांत्रिक परिवेश के कारण हो, वहां एक पत्रिका के 1500 अंकों की खपत, उस पत्रिका की विश्वनीयता और जरूरत दोनों को स्थापित करती है।
बहरहाल, ‘फारवर्ड प्रेस’ की आठ वर्ष लंबी यात्रा में मेरा परिचय उससे काफी बाद में हुआ। कुछ वर्ष पहले साहित्य अकादमी में कार्यरत देवेंद्र कुमार देवेश ने एक लेख को वहां भेजने की सलाह दी थी। उन दिनों साध थी कि कोई पत्रिका हो, जो वर्णव्यवस्था के सताए वर्गों की एकता एवं सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना के लिए काम करे। दलित साहित्य लंबे समय से इस क्षेत्र में था। उसका नारा भी ‘सामाजिक न्याय’ और ‘बराबरी’ का था। लेकिन दलित साहित्य कुल मिलाकर वह उन्हीं वर्गों की आवाज बना था, जो सामाजिक स्तर पर सबसे निचले पायदान पर ढकेले हुए थे।जिन्होंने अस्पृश्यता का दंश सहस्राब्दियों तक झेला था।उसके अलावा ‘आदिवासी साहित्य’ भी आंदोलन का रूप ले रहा था।
इस मामले में पिछड़े वर्ग सचमुच पिछड़े हुए थे। ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, मंडल, रामस्वरूप वर्मा जैसे विचारक, लेखक आंदोलनकर्मी पिछड़े वर्गों से आए थे। लेकिन सिवाय राजनीतिक रूप में संगठित होने तथा चुनावों में जाति के आधार पर वोट देने के उन्होंने उनसे कुछ नहीं सीखा। उनका प्रयास जाति के आधार पर जोड़-तोड़ से सत्ता में भागीदारी करना था। एकाध को छोड़कर ऐसा कोई नेता न था जो सांस्कृतिक वर्चस्ववाद को समझता और उसे चुनौती देने में सक्षम हो। यह ‘बीच’ का होने की मानसिकता भी थी, जिसके कारण वे अपने वास्तविक सहयोगी का चयन करने में असफल सिद्ध हुए थे। आजादी के कुछ दशक पहले जब उसमें सामाजिक चेतना के अंकुर फूटने शुरू हुए तो उन्होंने अपने से निचले वर्गों को, जो उसी की तरह वर्णव्यवस्था का शिकार रहे थे, गले लगाने की बजाए कांग्रेस जैसे अगड़े दलों की शरण में जाना उचित समझा।
1948 में ‘त्रिवेणी संघ’ के कांग्रेस समर्थित ‘बैकवर्ड क्लास फेडरेशन’ में विलय को इसकी शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। तब मुझे टामस पेन का कथन कि अल्पसंख्यक अभिजन, स्वार्थ की खातिर बहुसंख्यक जनसमाज को बांटे रखता है—अकसर याद आता था। पेन ने अभिजन और गैर अभिजन समूहों के बीच अंतरण की बात स्वीकारी है। लेकिन जाति आधारित विभाजन में अंतरण की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। चाहे-अनचाहे अभिजन मानसिकता के शिकार दलित बुद्धिजीवी भी थे। वह मनुवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों में एका करने की बजाए, दलितों में ही अभिजन समूह को उभारकर कहीं न कहीं अभिजन राजनीति को ही बढ़ावा दे रहे थे।
 यह ठीक है कि दलितों की पीड़ा अलग थी। सामाजिक भेदभाव का जो दंश उन्होंने झेला वैसा पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों को नहीं झेलना पड़ा था। यह भी ठीक है कि दलितों के उत्पीड़न में कहीं न कहीं पिछड़ी जातियों का भी हाथ रहा था। किंतु दलित लेखक यह नहीं समझ पा रहे थे कि हजारों वर्ष की वर्ण-व्यवस्था ने पिछड़ों की मानसिकता को अभिजन हितों की ढाल बना दिया है। अधिकांश पिछड़ी जातियां कर्मकार वर्ग से थीं, जो सामंती अर्थव्यवस्था के चलते किसी न किसी रूप में अगड़ों पर निर्भर थी। इसलिए कभी अगड़ों के भक्तिभाव के चलते, तो कभी आजीविका के अवसरों के कम हो जाने की संभावना के चलते वे विप्र जातियों से सहयोग करती हुई नजर आती थी।
यह ठीक है कि दलितों की पीड़ा अलग थी। सामाजिक भेदभाव का जो दंश उन्होंने झेला वैसा पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों को नहीं झेलना पड़ा था। यह भी ठीक है कि दलितों के उत्पीड़न में कहीं न कहीं पिछड़ी जातियों का भी हाथ रहा था। किंतु दलित लेखक यह नहीं समझ पा रहे थे कि हजारों वर्ष की वर्ण-व्यवस्था ने पिछड़ों की मानसिकता को अभिजन हितों की ढाल बना दिया है। अधिकांश पिछड़ी जातियां कर्मकार वर्ग से थीं, जो सामंती अर्थव्यवस्था के चलते किसी न किसी रूप में अगड़ों पर निर्भर थी। इसलिए कभी अगड़ों के भक्तिभाव के चलते, तो कभी आजीविका के अवसरों के कम हो जाने की संभावना के चलते वे विप्र जातियों से सहयोग करती हुई नजर आती थी।
ब्राजील के शिक्षा-शास्त्री पाब्लो फ्रेरा का कथन कि उत्पीड़ित वर्ग आमूल परिवर्तन की बजाए अपनी मुक्ति उत्पीड़क की भूमिका में आने में देखता है—पूरे बहुजन समाज पर सटीक बैठता है। ऐसे में दलित लेखक यदि यह सोचकर कलम चलाते कि जिस मनुवादी व्यवस्था का शिकार वे हैं, उस मनुवादी व्यवस्था के शिकार पिछड़े भी रहे हैं, इसलिए जातीय वर्चस्ववाद के विरुद्ध असली लड़ाई उस व्यवस्था के शिकार रहे सभी वर्गों को एकजुट करके ही लड़ी जा सकती है।
ऐसे में ‘फारवर्ड प्रेस’ द्वारा बहुजन साहित्य और बहुजन संस्कृति के प्रतीकों के साथ आना, एक बड़े क्रांतिकारी आंदोलन की पहल-कदमी करने जैसा प्रयास था। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पत्रिका अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है अथवा जो वह कहना चाहती है, उसे समाज के संबंधित वर्गों तक पहुंचाने में सफल रही है। किसी भी बड़े आंदोलन के लिए आठ वर्ष का समय बड़ी लक्ष्य की भूमिका जितना होता है। इसलिए फारवर्ड प्रेस की सात वर्ष लंबी यात्रा को में केवल बड़े संकल्प की भूमिका के रूप में ही देखता हूं। सीमित संसाधनों से, कुछ लेखकों के जुनून के बूते निकल रही पत्रिका, अपने परिवर्तित रूप में भी सामाजिक न्याय का सपना देखने वालों के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के समान है।
(फारवर्ड प्रेस के जून, 2016 अंक में प्रकाशित )