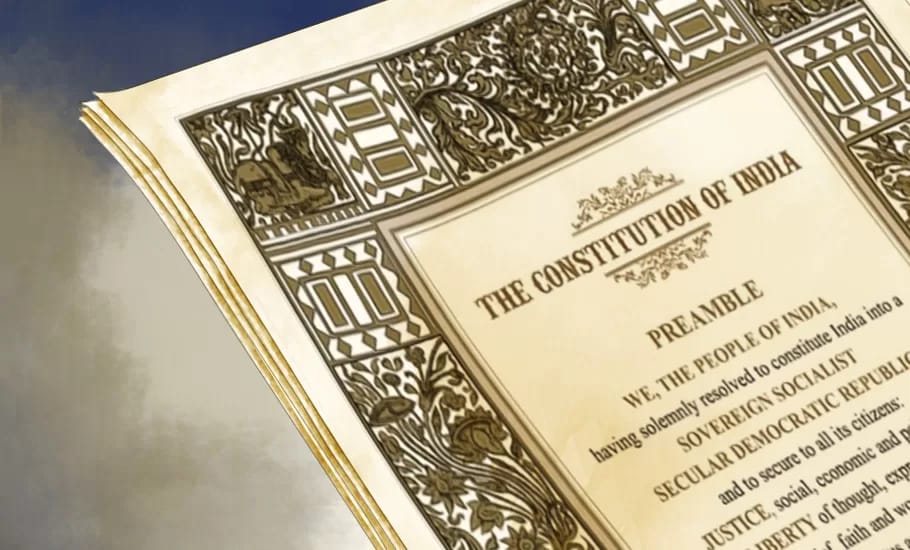इस निर्णय ने, विधिवेत्ताओं ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी जस्टिस कर्णन के साथ हुए व्यवहार को चर्चा का विषय बना दिया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वे अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं और लगातार यह कहते आये हैं कि उनकी जाति के कारण उनके साथ भेदभाव हो रहा है। परन्तु इस निर्णय पर दलित समुदाय की क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया जायज नहीं है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के जस्टिस कर्णन के आचरण को देखें तो हमें यह अहसास होगा कि उनके साथ जो कुछ हुआ, वह अपरिहार्य था।
जस्टिस कर्णन ने जो किया और कहा, उस पर मीडिया में बहुत कुछ प्रकाशित हुआ है। हाल में, पूरे घटनाक्रम पर एक विस्तृत रपट “इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली[1] में प्रकाशित हुई। परन्तु यहाँ हम केवल जस्टिस कर्णन के न्यायिक दुराचरण की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगें।
स्थानांतरण पर नाटक
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 12 फरवरी, 2016 को, जस्टिस कर्णन को मद्रास उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। कर्णन ने इस आदेश के अमल पर स्वयं ही रोक लगा दी। यह प्राकृतिक न्याय के इस सर्वमान्य सिद्धांत के विरुद्ध था कि “कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता”। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से अपने स्थानांतरण आदेश पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा।[2] जस्टिस कर्णन का यह कृत्य, गंभीर अनुशासनहीनता और न्यायिक दुराचरण है, जो कि संविधान के अंतर्गत किसी न्यायाधीश के महाभियोग का आधार हो सकता है।[3]
इसके पश्चात, मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह जस्टिस कर्णन को उनके ही स्थानांतरण के विरूद्ध आदेश जारी करने से रोकने के लिए निरोधक आदेश जारी करे। तत्पश्चात, 15 फरवरी 2016 को उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस कर्णन के स्थगन आदेश को रद्द करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय को यह आदेश दिया कि वह जस्टिस कर्णन को कोई काम न सौंपे। उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस कर्णन द्वारा 12 फरवरी के बाद जारी सभी आदेशों के अमल पर पूर्ण रोक लगा दी परंतु उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दायर की गई याचिका का विरोध करने की इजाजत दे दी[4]। इस आदेश के बाद, जस्टिस कर्णन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर से मिले और उनसे अपने आचरण के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगी। अपने क्षमायाचना पत्र में उन्होंने अपने आचरण के लिए ‘‘मानसिक कुंठाओं के कारण, मानसिक संतुलन खो देने” को दोषी ठहराया। उन्होंने लिखा कि वे मद्रास हाईकोर्ट में उनके साथ किए जा रहे जातिगत भेदभाव के कारण कुंठाग्रस्त थे।[5] उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने स्थानांतरण को भी स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान के अनुसार, अगर कोई न्यायाधीश स्वयं यह स्वीकार कर ले कि वह मानसिक रूप से असंतुलित है तो यह उसके महाभियोग का आधार बन सकता है। परंतु चूंकि यह केवल एक मौके पर मानसिक संतुलन खो देने का मामला था, इसलिए शायद वह महाभियोग का आधार नहीं बन सकता था। परंतु निश्चित तौर पर यह दुराचरण तो था ही। इसके बावजूद, उच्चतम न्यायालय ने उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की और उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार संभालने की अनुमति दे दी।
अवमानना का प्रकरण क्यों?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए किसी को दंडित करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति कर्णन ने ऐसा क्या किया था कि वे अवमानना के दोषी बन गए? कर्णन के विरूद्ध अवमानना का प्रकरण, उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लिया। यह तब हुआ जब कर्णन ने प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिखकर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के 20 न्यायाधीशों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कदाचरण के गंभीर आरोप लगाए और वह भी बिना किसी प्रमाण के। अवमानना प्रकरण पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के सात वरिष्ठतम जजों की एक पीठ गठित की गई।
उत्तरप्रदेश राज्य विरूद्ध श्यामसुंदर लाल[6] प्रकरण (1954) में अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ‘‘प्रधानमंत्री को भेजा गया कोई पत्र, जो जनसामान्य या उसके किसी हिस्से में प्रसारण के लिए नहीं है, लोगों के दिमाग में किसी न्यायाधीश की निष्पक्षता, योग्यता और सत्यनिष्ठा के संबंध में आशंकाएं उत्पन्न नहीं कर सकता”। परंतु जस्टिस कर्णन द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को उन्होंने स्वयं ही सार्वजनिक कर दिया और इस प्रकार यह पत्र आमजनों में न्यायाधीशों की छवि को कलंकित करने वाला बन गया। श्री बरदकांता मिश्रा विरूद्ध रजिस्ट्रार, उड़ीसा उच्च न्यायालय[7] (1974) में अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा :
‘‘न्यायाधीश और न्यायालयों के कई तरह के कार्य होते हैं। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से, कार्य के महत्व की दृष्टि से और विधिशास्त्र की दृष्टि से, जो कार्य समुदाय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और जिस कार्य को सार्वजनिक निंदा से बचाया जाना आवश्यक है, वह है न्यायिक कार्य। किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत आचरण या उसके प्रशासनिक निर्णयों की कटु निंदा से अपरोक्ष रूप से उसकी छवि खराब हो सकती है और लोगों का न्यायपालिका में विश्वास कमजोर हो सकता है। परंतु इसके साथ ही, हमें यह याद रखना चाहिए कि इस तरह की आलोचना की अनुमति देने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तो होगी ही, वरन इस तरह की सद्भावी आलोचना, चाहे वह कुछ बढ़ा-चढ़ाकर ही क्यों न की गई हो, का सामना करने से लोगों का विश्वास न्यायपालिका में बढ़ेगा। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्याय को कमरे में बंद रखने की आवश्यकता नहीं है।”
उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर थे, विशेषकर इसलिए क्योंकि आरोप लगाना वाला उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश था। परन्तु बिना किसी सबूत के इस तरह के आरोप लगाने से न्यायपालिका कलंकित होती है और आम लोगों की निगाहों में उसकी छवि गिरती है।
प्रश्न यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय को जस्टिस कर्णन के विरूद्ध अवमानना का नोटिस जारी करने का अधिकार था। इस सिलसिले में उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ[8] प्रकरण (1998) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का हवाला दिया जा सकता है। इस निर्णय में संविधान पीठ ने कहा :
‘‘न्यायालय की अवमानना एक विशेष क्षेत्राधिकार है, जिसका इस्तेमाल यदाकदा और अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब किसी कार्य से न्याय करने में बाधा आए या जो न्याय की राह में बाधक बन रहा हो या जिससे न्यायिक संस्थाओं में लोगों की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब विचाराधीन कार्य से विधि की प्रतिष्ठा या अदालतों की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अवमानना के क्षेत्राधिकार का उद्देश्य अदालतों की गरिमा को बनाए रखना है। यह एक असामान्य क्षेत्राधिकार है, जिसमें न्यायालय ही जूरी, न्यायाधीश और जल्लाद तीनों होता है और ऐसा इसलिए, क्योंकि अवमानना का प्रकरण सुनते समय अदालत दो प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों के दावों पर निर्णय नहीं कर रही होती। इस क्षेत्राधिकार का उपयोग किसी व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए नहीं किया जाता बल्कि न्याय व्यवस्था को कलंक से बचाने के लिए किया जाता है। यह जनहित में है कि अदालतों के अधिकारों को खतरे में न डाला जाए और न्याय करने की प्रक्रिया में कोई अनुचित हस्तक्षेप न हो।”
जस्टिस कर्णन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी
जस्टिस कर्णन को कई बार नोटिस और समन जारी कर सात जजों के बेंच के समक्ष उपस्थित होकर उनके द्वारा वर्तमान और पूर्व न्यायाधीशों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।[9] वे उनके विरूद्ध जमानती वारंट जारी होने के बाद ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। जस्टिस कर्णन और मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली खंडपीठ के बीच वार्तालाप, जो दिनांक 25 मार्च, 2016 के एक पत्र से सामने आया, के अनुसार जस्टिस कर्णन न केवल बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार थे वरन् वे उन 20 न्यायाधीशों, जिनके विरूद्ध उन्होंने पहले आरोप लगाए थे, के संबंध में अपनी शिकायत को वापिस लेने के लिए भी राजी थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस कर्णन द्वारा कोई ठोस उत्तर न दिए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने उन्हें शपथपत्र द्वारा अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा।[10] परंतु जस्टिस कर्णन ने न तो लिखित उत्तर प्रस्तुत किया और ना ही वे अगली सुनवाई में उपस्थित हुए।
बेहतर तो यह होता कि जस्टिस कर्णन उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही को चुनौती देते और उस पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाते। अगर उनके पास उनके आरोपों को प्रथम दृष्टया साबित करने के लिए भी सामग्री होती, तो उनकी चुनौती स्वीकार्य हो जाती और वे उच्च न्यायपालिका में भारी भ्रष्टाचार को उजागर करते। यहां यह महत्वपूर्ण है कि जस्टिस कर्णन के पास जो एकमात्र बचाव था, वह न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 13(ब) के अंतर्गत उनके आरोपों की सत्यता को प्रमाणित करना था। चूंकि वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने उनके विरूद्ध की जा रही अवमानना की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी इसलिए अदालत ने यह मान लिया कि उनके आरोप दुर्भावनापूर्ण थे और उनका उद्देश्य न्यायालय को बदनाम करना था। इससे भी खराब बात यह थी कि उन्होंने सात जजों की पीठ के खिलाफ समानांतर कार्यवाही शुरू कर दी। यह इस तथ्य के बावजूद कि उच्चतम न्यायालय ने उनके द्वारा किसी भी प्रकार के न्यायिक या प्रशासनिक कार्य किए जाने पर स्पष्ट रोक लगाई थी। वैसे भी, उनके द्वारा की गई कार्यवाही इसलिए वैध नहीं थी क्योंकि वह इस मूलभूत नियम का उल्लंघन करती थी कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रकरण में न्यायाधीश नहीं हो सकता। इसके बाद, जस्टिस कर्णन ने बेतुके और विचित्र आदेशों की झड़ी लगा दी, जिनमें सात जजों से रूपये 14 करोड़ के मुआवजे की मांग, उनके विरूद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करना और एयरपोर्ट एथारिटी ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर इन न्यायाधीशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। अपने अंतिम आदेश दिनांक 8 मई, 2017 को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के आठ न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास और रूपये एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें यह सजा ‘‘अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और संशोधित अधिनियम 2015 के अधीन अपराध कारित करने के लिए सुनाई गई[11]। इस आखिरी आदेश ने जस्टिस कर्णन की नियति तय कर दी।[12]
फरवरी 2017 के बाद और उसके पहले भी, जस्टिस कर्णन द्वारा पारित बेतुके आदेश, निश्चित तौर पर न्यायालय की अवमानना हैं। वे उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा घोर अनुशासनहीनता के उदाहरण हैं और आमजनों की निगाह में न्यायपालिका की छवि को गिराने वाले हैं।
क्या उच्चतम न्यायालय ने जल्दबाजी की?
जहाँ जस्टिस कर्णन के कृत्य और कथन, निश्चित तौर पर न्यायालय की अवमानना करने वाले थे, वहीं, क्या अदालत ने उन्हें छह माह के कारावास की सजा सुनाकर, और वह भी उन्हें सुने बगैर, ठीक किया? इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश में प्रक्रियात्मक कमियां नज़र आती हैं।
सबसे पहले, उनके विरुद्ध कोई आरोप तय नहीं किये गए। दूसरे, उन्हें दोषसिद्ध घोषित करने के बाद, अदालत को सजा के प्रश्न पर जस्टिस कर्णन को सुनना था, जो कि नहीं किया गया। यह दिलचस्प है कि जिस दिन जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी ठहराया गया, उसी दिन उच्चतम न्यायालय की एक दूसरी खंडपीठ ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को भी इसी आरोप में दोषी पाया परन्तु अदालत ने माल्या को सजा के प्रश्न पर अपना पक्ष रखने का मौका देने की पेशकश की। यह कहा जा सकता कि जहाँ माल्या इस समय इंग्लैंड में हैं और प्रत्यार्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं और इसलिए वे अपना बचाव नहीं कर सकते थे। वही जस्टिस कर्णन के लिए किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना बचाव करने का अवसर उपलब्ध था। परन्तु उन्होंने उच्चतम न्यायालय की जिस तरह से अवहेलना की और न्यायिक अनुशासन और उचित व्यवहार सम्बन्धी सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ाईं, शायद इस कारण अदालत ने यह आदेश दिया कि उनकी सजा को तुरंत क्रियान्वित किया जाए।
क्या सजा बहुत कड़ी है?
श्री बरदकांता मिश्र विरुद्ध रजिस्ट्रार, उड़ीसा उच्च न्यायालय[13] प्रकरण (1974) में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को न्यायालय की अवमानना के लिए कारावास की सजा सुनायी थी। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने कारावास के स्थान पर दोषी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा, “उनके आधिकारिक जीवन की संध्या में, अगर उन्हें कारावास के स्थान पर कोई और सजा दी जाती है तब भी न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं और आमजनों को यह भरोसा होता है कि अगर कोई जज भी कसूरवार होगा, जैसा कि इस मामले में अवमानना करने वाला है, तो उसे भी बख्शा नहीं जायेगा”। न्यायालय ने यह भी कहा कि “अगर कम सजा के काम चल जाये तो अधिक सजा देने का कोई तुक नहीं है”। न्यायालय के कहा कि अगर दोषी जुर्माना नहीं चुकाएगा तो उसे तीन महीने का कारावास भुगतना होगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ[14] प्रकरण (1998) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या किसी वकील को अदालत की अवमानना के लिए दी जाने वाली सजा में, किसी निर्धारित अवधि के लिए उसका लाइसेंस निलंबित करना शामिल हो सकता है। दोषी वकील को अवमानना के लिए सजा, संविधान के अनुच्छेद 129 सहपठित अनुच्छेद 142 के तहत दी गयी थी और लाइसेंस के निलंबन से वह अदालतों में पैरवी नहीं कर पाता। संविधान पीठ ने कहा कि सजा बतौर किसी वकील के पैरवी करने के अधिकार को निलंबित करने और उसका नाम शासकीय वकीलों की सूची में से हटाने का प्रावधान, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में है और यह दंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा तभी आरोपित किया जा सकता है, जब किसी का अपराध उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाये गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने हुए साबित हो जाये। पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायलय को राज्य के अन्य अंगों या किसी वैधानिक संस्था की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है।
इस प्रकार, अवमानना के पहले प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की कारावास के सजा को जुर्माने में बदल दिया, और दूसरे प्रकरण में, यह सबंधित विधिक संस्था पर छोड़ दिया कि वह वकील का पैरवी करने का लाइसेंस निलंबित करना चाहती है या नहीं। परन्तु इन दोनों मामलों और जस्टिस कर्णन के प्रकरण में मूलभूत अंतर हैं। जस्टिस कर्णन के मामले में उच्च न्यायलय के एक वर्तमान न्यायाधीश ने, अन्य न्यायधीशों के विरुद्ध, मिथ्या और अपमानजनक आरोप लगाये और न्यायिक अनुशासन को दरकिनार करते हुए, अनेक आदेश जारी किये, जिनसे निश्चित तौर पर न्यायिक प्रक्रिया की “प्रतिष्ठा और गरिमा” को चोट पहुंची। जस्टिस कर्णन के कार्यों से आम लोगों की निगाहों में न्यायपालिका का सम्मान गिरा और ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 माह की अधिकतम सजा सुनाये जाने को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत के सामने और क्या विकल्प थे?
जस्टिस कर्णन का मामला उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा अदालत की अवमानना का पहला (और हम आशा करते हैं आखिरी) मामला था। शायद उच्चतम न्यायालय को जस्टिस कर्णन के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उच्च न्यायपालिका के किसी सदस्य द्वारा इस तरह की अनुशासनहीनता से निपटने के लिए कोई कानून या प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह के पथभ्रष्ट न्यायाधीशों को सही रास्ते पर लाने का कोई तंत्र है ही नहीं। उच्चतम न्यायालय ने सी. रविचंद्रन अय्यर विरुद्ध जस्टिस ए. एम. भट्टाचार्जी[15] प्रकरण (1995) में अपने निर्णय में कहा कि न्यायपालिका द्वारा आत्म-नियमन ही सबसे बेहतर उपाय है। निर्णय की अंतिम पंक्तियाँ हैं :
“हमें ऐसा लगता है कि न्यायपालिका द्वारा आत्म-नियमन ही एकमात्र वह तरीका है, जिसे अपनाया जा सकता है। अगर उच्च न्यायलय का कोई असहयोगी न्यायाधीश/ मुख्य न्यायाधीश ऐसा कोई अनुचित व्यवहार करे, जो उसके उच्च पद की गरिमा के अनुरूप न हो, परन्तु जो सिद्ध दुराचरण की श्रेणी में नहीं आता हो, तब ऐसे न्यायाधीश को केवल आंतरिक आत्म-नियमन से अनुशासित किया जा सकता है। यह आंतरिक प्रक्रिया, संविधान में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रावधान के अभाव की पूर्ति कर सकती है और उसका हितकर प्रभाव पड़ेगा”।
जस्टिस कर्णन का प्रकरण, सिद्ध दुराचरण की श्रेणी में आ सकता है और इस आधार पर उन पर महाभियोग चलाया जा सकता था। परन्तु इसकी प्रक्रिया लम्बी है और यह केवल संसद कर सकती है। इन परिस्थितियों में शायद उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगा होगा कि आतंरिक जांच से काम नहीं चलेगा क्योंकि उससे लोगों की न्यायपालिका में आस्था पुनर्स्थापित नहीं होगी। अतः उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर जस्टिस कर्णन को अवमानना का दोषी ठहराया। यह चाहे सबसे बेहतर विकल्प न भी रहा हो परन्तु गैर-क़ानूनी तो कतई नहीं था।
निष्कर्ष
यद्यपि जस्टिस कर्णन को दी गयी कड़ी सजा और उनकी बर्खास्तगी पर बहस की जा सकती है परन्तु उनसे किसी प्रकार की सहानुभूति रखना मुश्किल है। किसी भी वर्तमान न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने शब्दों को बोलने से पहले तोले। जस्टिस कर्णन को किसी भी तरह अपने कृत्यों को उचित नहीं ठहरा सकते। बल्कि उन पर तो महाभियोग की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। शायद यह रास्ता इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वे जून में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और महाभियोग की लम्बी प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती थी। कुछ लोगों, जिनमें केके वेणुगोपाल शामिल थे, का कहना था कि बेहतर तो यह होता कि कर्णन को अकेला छोड़ दिया जाता। परन्तु उच्चतम न्यायालय इससे सहमत नहीं था और उसने हमारे न्यायिक इतिहास के एक अप्रिय अध्याय को अपने ढ़ंग से बंद करना उचित समझा। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि ऐसे दिन भारतीय न्यायपालिका को फिर कभी नहीं देखने पड़ेंगे।
[1] http://www.epw.in/journal/2017/18/web-exclusives/curious-case-justice-karnan.html
[2] उपरोक्त
[3] देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 298
[4] http://www.epw.in/journal/2017/18/web-exclusives/curious-case-justice-karnan.html
[5] http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/justice-cs-karnan-apologises-for-staying-transfer/articleshow/51114164.cms
[6] AIR 1954 All 308
[7] (1974) 1 SCC 374
[8] AIR 1998 SC 1895
[9] http://www.livelaw.in/contempt-justice-karnan-fails-appear-sc-gives-another-chance/
[10] http://www.livelaw.in/justice-karnan-vs-cji-led-bench-gripping-courtroom-exchange/
[11] http://www.livelaw.in/justice-karnan-convicts-cji-seven-judges-scst-act-orders-5yrs-imprisonment-read-order/
[12] https://barandbench.com/justice-cs-karnan-ignominious-end-arvind-datar/
[13] (1974) 1 SCC 374
[14] AIR 1998 SC 1895
[15] (1995) 5 SCC 457
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। डॉ. आम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व व कृतित्व पर केंद्रित पुस्तक फारवर्ड प्रेस बुक्स से शीघ्र प्रकाश्य है। अपनी प्रति की अग्रिम बुकिंग के लिए फारवर्ड प्रेस बुक्स के वितरक द मार्जिनालाज्ड प्रकाशन, इग्नू रोड, दिल्ल से संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911फारवर्ड प्रेस बुक्स से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं । ईमेल : info@forwardmagazine.in