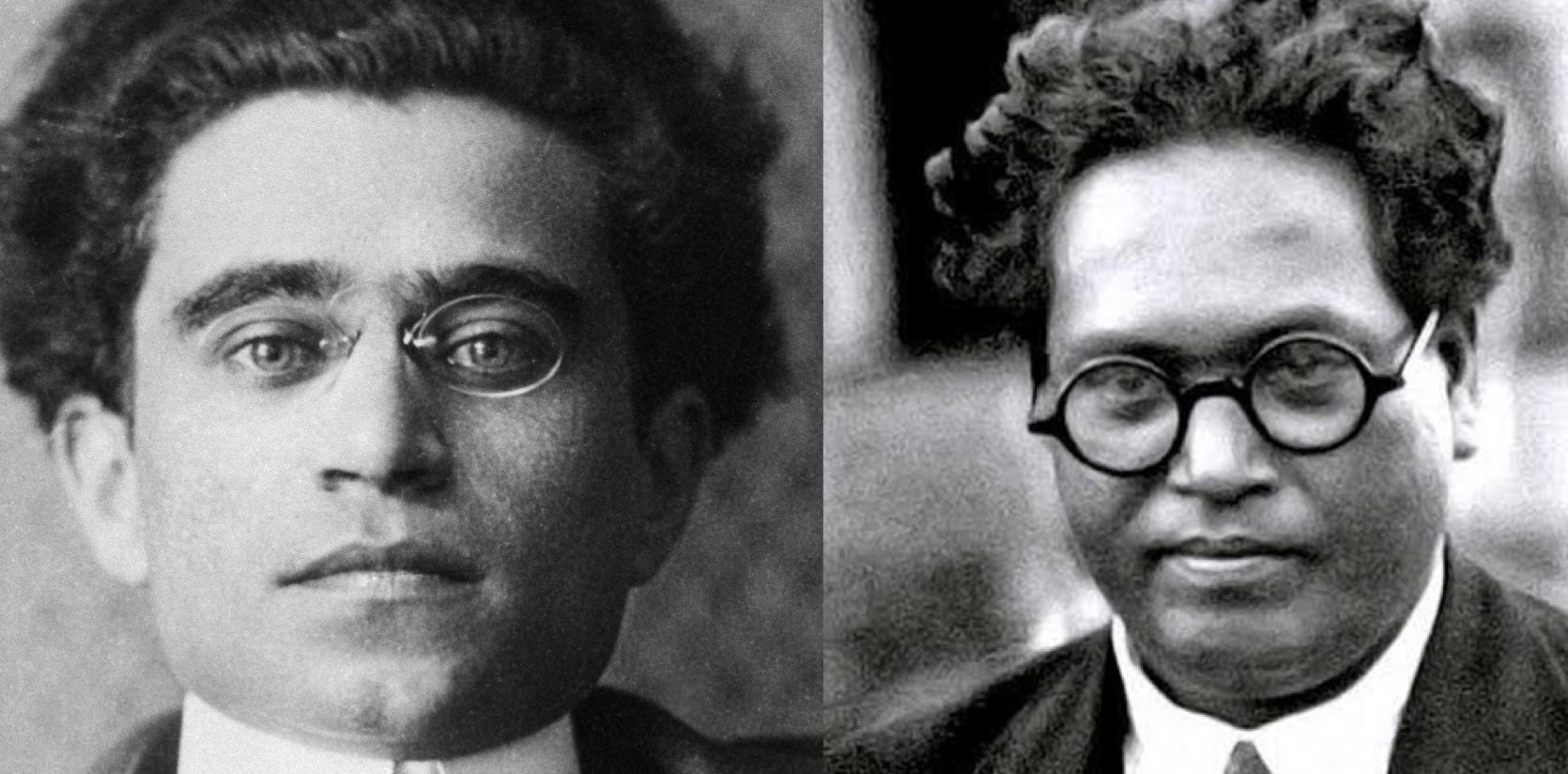सहारनपुर के शब्बीरपुर घटना क्यों घटी, इसका कारण जानने के लिए आपको इन इलाकों में दलितों के प्रति जातीय शोषण के चरम को देखना होगा। अन्याय के विरुद्ध गुस्सा बहुत देर तक नहीं रुक सकता। जबसे दलित लोग जातीय उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे हैं, सवर्ण जातियों में वर्चस्व टूटने का भय पैदा हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा के झज्झर, बग्गा, गोहाना से लेकर मिर्चपुर जैसी घटनाएँ क्यों घटीं इसे समझने में रामजी यादव की यह रिपोर्ट मददगार होगी, जिसमें उन्होंने एक दशक पहले की घटनाओं का जिक्र किया है। – संपादक
एक दशक पहले मैं दिल्ली की एक संस्था भारतीय दलित अध्ययन संस्थान के इकाई के रूप में डाक्यूमेंटरी बनाने के लिए पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में गया था। मेरा शोध केन्द्रित इलाका उत्तर प्रदेश का शामली, सहारनपुर और मुज़फ़्फरनगर था। संयोग से दलित कथाकार ओमप्रकाश वाल्मीकि का भी घर मुज़फ़्फरनगर के बारला गाँव में पड़ता है। वाल्मिकी ने जिस तरह अपनी आत्मकथा ‘जूठन’ में मुज़फ़्फरनगर की सामाजिक संरचना का चित्र उकेरा है, वह बहुत भयानक है। गूर्जर बहुल इलाके में विभिन्न दलित जातियों और उप जातियों की समाजिक स्थिति कमोबेश समान है। हमें लगा हम जूठन एक बार फिर देख रहे हैं। दलित जातियों में जाटव, चमार, बल्हार और वाल्मीकि, जिनका सीधा संबंध गूर्जरों से है, क्योंकि वे खेत के मालिक है, जबकि दलित भूमिहीन। इस संबंध में जाहिर है शोषक-शोषित का अखिल भारतीय और वैश्विक संबंध विकसित किया गया है लेकिन इसकी सबसे भयानक बात अपनी जातियों के कारण दलितों की बेगार करने की स्थिति और खेतिहर जातियों के द्वारा मनमाना तय की गई मजदूरी लेने की बाध्यता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी ने मजदूरी न करने या न्यूनतम मजदूरी मांगने और न मिलने पर गाँव छोड़कर शहर जाने का निश्चय किया तो उसका घर जलाना, मारना-पीटना और महिलाओं के साथ बलात्कार करना आम बात है। इसकी सुनवाई कहीं नहीं है। रिपोर्टें दर्ज ही नहीं की जाती।
‘जूठन’ वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी हरियाणा के उन लोगों की स्थितियों पर एक तब्सरा मात्र है जो इन गाँवों के बीच जाति का अपमान भोगने को अभिशप्त हैं। क्योंकि जब हमने कैमरा खोला तो कई ऐसी कहानियाँ सामने आने लगीं जिन्हें हम बीते जमाने की बातें समझते थे लेकिन वे अभी भी घटित हो रही थीं।
 आज़ादी के साठ साल बीत जाने के बाद भी वहां क्या स्थिति है इसे वृतचित्र में शामिल व्यथा-कथा से जाना जा सकता है। पुरुष कह रहे हैं कि आज़ादी के साठ साल बाद भी सबसे ताकतवर जाति गूर्जर है। उनके दबदबे में हम जी रहें है और कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करता। एक लड़की ने बताया, “स्कूल में गूर्जर लड़के-लडकियां जबरदस्ती हमको पीछे बैठने पर मजबूर करते हुए कहते हैं कि चमार को पीछे बैठना चाहिए।” एक अन्य लड़की ने बताया, “गूर्जर लोग खेतों की ओर निकलने पर हमसे छेड़खानी करते हैं, भद्दे इशारे करते हैं और गालियाँ देते हैं। अगर वे हमारे सामने की ओर से आ रहे होते हैं तो हमको खेतों में उतरने को मजबूर कर देते हैं ताकि वे हमसे छू न जायें। हर गाँव में गूर्जर खेतों के मालिक है, थाना-पुलिस-कचहरी में पैसा खर्च कर सकते हैं तो हमारे साथ हुए हर अन्याय की बात दबा दी जाती है।”
आज़ादी के साठ साल बीत जाने के बाद भी वहां क्या स्थिति है इसे वृतचित्र में शामिल व्यथा-कथा से जाना जा सकता है। पुरुष कह रहे हैं कि आज़ादी के साठ साल बाद भी सबसे ताकतवर जाति गूर्जर है। उनके दबदबे में हम जी रहें है और कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करता। एक लड़की ने बताया, “स्कूल में गूर्जर लड़के-लडकियां जबरदस्ती हमको पीछे बैठने पर मजबूर करते हुए कहते हैं कि चमार को पीछे बैठना चाहिए।” एक अन्य लड़की ने बताया, “गूर्जर लोग खेतों की ओर निकलने पर हमसे छेड़खानी करते हैं, भद्दे इशारे करते हैं और गालियाँ देते हैं। अगर वे हमारे सामने की ओर से आ रहे होते हैं तो हमको खेतों में उतरने को मजबूर कर देते हैं ताकि वे हमसे छू न जायें। हर गाँव में गूर्जर खेतों के मालिक है, थाना-पुलिस-कचहरी में पैसा खर्च कर सकते हैं तो हमारे साथ हुए हर अन्याय की बात दबा दी जाती है।”
इन खबरों की विश्वसनीयता जांचने के लिए मैं कुछ देर वहां रुका। मेरे सामने कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जिससे लगा कि दलित जो कह रहें है वह झूठ नहीं है। हमने देखा कि साधन-सम्पन्न गुर्जरों के उस गाँव में कैमरा खुलने से एक हौल पड़ गई है। दलित बस्ती के सैकड़ों लोग कैमरे के आसपास इकट्ठा हैं और यदा-कदा कुछ गुर्जर युवा मोटर साइकिल से गाँव और खेतों के बीच चक्कर काट रहे थे। उनका ध्यान कैमरा और टीम पर था। हमारे साथ गए सूरज बड़त्या ने कहा हमें चल देना चाहिये। एक आखिरी दृश्य के रूप में हमने एक दलित बच्चे से पूछा कि वे कहाँ खेलते हैं। उनमें से एक ने कहा, “स्कूल में हम खेलने जाते हैं तो मास्टर छड़ी से पीटकर पूरे विद्यालय की सफाई करवाते हैं और जब हम गाँव में खेलने जाते हैं तो गुर्जर हमको भगा देते हैं। हम कभी-कभी दलित बस्ती के छोटे से मैदान में खेलते हैं।” उन्होंने कबड्डी में हमें अपना कौशल दिखाया। सभी बच्चों ने अपनी चप्पलों को बीच में रखकर दो पाले बनाये और खेलने लगे। खेल अपने चरम पर जाता कि तभी दो गुर्जर युवा पास से गुजरे और उनकी आँखों में पता नहीं क्या था कि खेलते हुए बच्चों ने देखते-देखते अपनी चप्पलें उठाईं और फुर्र हो गए।
जब हम ये सब कर रहे थे तब मायावती की सत्ता उत्तर प्रदेश में चार बार आ चुकी थी और पांचवीं बार भी 2007 में भी आई। दलितों ने कहा, “इन सबसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा विधायक एक दबंग आदमी है। जब वह थाने जाता है तो हाथ से नहीं लात से दरवाजा खोलता है। दरोगा उसको कुर्सी से उठकर सलाम करके अदब से बैठने को कहता है। हम जब भी उसके यहाँ कोई अर्जी लेकर जाते हैं तो वह आश्वासन जरुर देता है लेकिन कुछ होता नहीं। बहनजी के सत्ता में आने से हमें बस इतना फायदा हुआ कि हम ये सोचकर रोमांचित होते हैं कि हमारी जाति की महिला मुख्यमंत्री है।” कुछ लड़कियां मायावती की प्रशंसक थीं और प्रशानिक सेवा, शिक्षा तथा डॉक्टरी पेशे में जाने का सपना देख रही थीं। सभी ने एक बात सामान्य तौर पर स्वीकार की कि हाँ, जय भीम हमारी बहुत बड़ी ताकत है।
इससे पहले कि हम सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचनाओं और उनके अंतर्विरोधों की ओर देखें हमें ऐसे ही कुछ अनुभवों के लिए हरियाणा के पूर्वी-उत्तरी जिलों में भी गए। पहले हम पानीपत जिले के तीन गाँवों में गए। एक गाँव तगाओं यानी त्यागियों, दूसरा जाटों और तीसरा गुर्जरों का था। सभी गाँव में सामान्य बात यह थी कि दलित सभी जगहों पर खेतिहर मजदूर के रूप में थे। कुछेक सरकारी नौकरियों में थे लेकिन उनकी संख्या उँगलियों पर गिनने लायक थी। एक गाँव में जब हमने कुछेक घरों में शूटिंग शुरू की, जो त्यागियों के वर्चस्व वाला गाँव था। महिलाओं ने बताया कि यह जो सामने तालाब है वहां सारे त्यागी स्त्री-पुरुष दिशा-मैदान करते हैं लेकिन जब दलित वहां जाते हैं तो वे गाली-गलौच करते हुए मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। त्यागियों का तर्क था कि इससे तालाब अपवित्र हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि सारे गाँव की गन्दगी का मुहाना दलितों की बस्तियों की ओर था और कई बार इसका विरोध करने पर दलितों की पिटाई भी हो चुकी थी। यहां भी स्कूल में बच्चों को दूर बैठने को मजबूर किया जाता है। दलितों के मन में दबे आक्रोश का अंदाजा हमने इस बात से लगाया कि कक्षा चार में पढ़ने वाले दो बच्चों ने कहा, “सन्नी देओल की फ़िल्में अच्छी लगती हैं क्योंकि वह बिना किसी से दबे बहुत अच्छी फाइटिंग करता है।” एक लड़के ने ड्राइवर बनने का सपना हमसे साझा किया।
 दूसरा गाँव जाट बहुल था और यहाँ महिलाओं ने खेतों में काम करना बंद कर दिया था क्योंकि जाट उनके साथ प्रायः बद्तमीजी करते थे। अमूमन पुरुष ही उनका काम करते थे। स्कूलों में दलित लड़कियों के साथ छेड़खानी की बात हर उस लड़की ने स्वीकार की जिससे हमने बातचीत की। इसलिए प्रायः वहां दलित लड़कियों में ड्राप आउट का प्रतिशत अधिक था।
दूसरा गाँव जाट बहुल था और यहाँ महिलाओं ने खेतों में काम करना बंद कर दिया था क्योंकि जाट उनके साथ प्रायः बद्तमीजी करते थे। अमूमन पुरुष ही उनका काम करते थे। स्कूलों में दलित लड़कियों के साथ छेड़खानी की बात हर उस लड़की ने स्वीकार की जिससे हमने बातचीत की। इसलिए प्रायः वहां दलित लड़कियों में ड्राप आउट का प्रतिशत अधिक था।
आखिरी में हम पानीपत के ही नारायणा गाँव में गए जो गुजरों के वर्चस्व वाला गाँव है। यहाँ हमने दो चीजों को मार्क किया। गाँव में एक ही ट्रांसफार्मर से बिजली आती है लेकिन शाम होते ही दलित बस्ती की ओर जाने वाली बिजली काट दी जाती है जिससे दलित बच्चों की पढाई पर बुरा असर पड़ता है। हारकर दलितों ने अपने लिए अलग ट्रांसफार्मर के लिए बिजली विभाग में दौड़ लगानी शुरू की लेकिन आठ साल की मशक्कत के बावजूद सन् 2006 तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा था। दूसरा मामला था गाँव में श्मशान का। गुर्जरों की जमीनें गाँव के हर कोने में थीं लेकिन श्मशान उन्होंने उस कोने पर बनाया जहाँ से दलित बस्ती शुरू होती है। इसे लेकर कई बार पंचायत हुई लेकिन मामला यहाँ आकर लटक जाता कि श्मशान हमारे खेत में है। हम जहाँ चाहेंगे वहां बनायेंगे।
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in