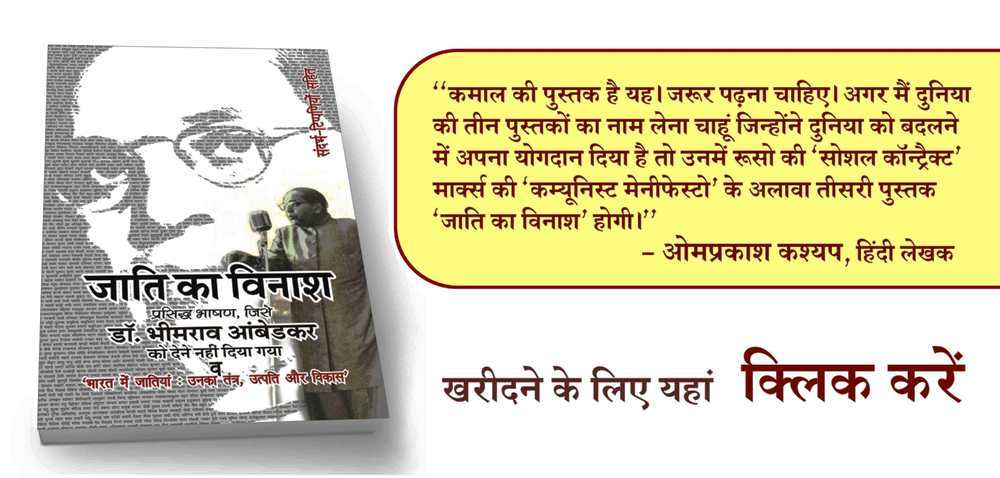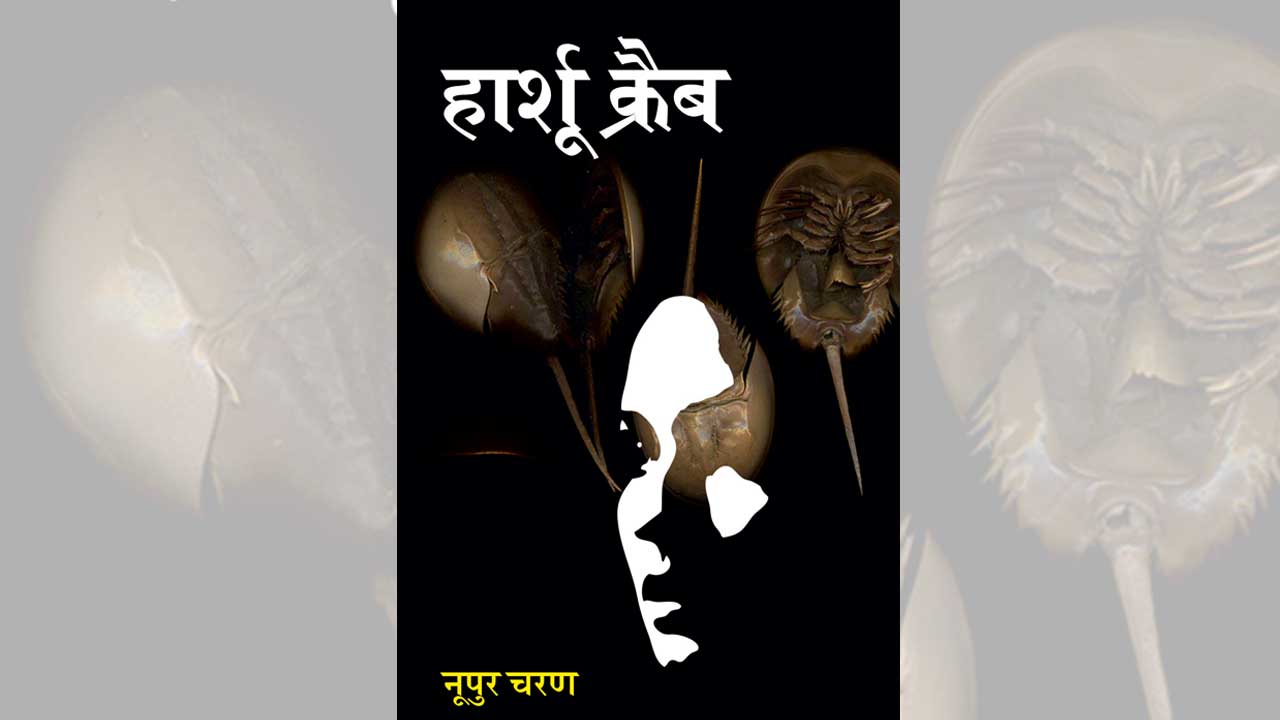भारतीय समाज पर राजनीतिक प्रभाव प्रारंभ से ही रहा है। वर्तमान दौर में हर जगह राजनीति की खाई बनी हुई है। परिवार, पड़ोस, विद्यालय, विश्वविद्यालय ऐसी कोई भी संस्था या स्थान नहीं जहाँ राजनीति ने अपनी पैठ स्थापित न की हो| इन सभी स्थानों पर राजनीति के छोटे से लेकर बड़े रूप के दर्शन हो ही जाते हैं अर्थात् हर जगह सत्ता का ही बोलबाला है, सत्ता की ही जय-जयकार है। आज की सत्ता जनतंत्र के लिए नहीं वरन अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु काम करती है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सत्ता सदैव छीनती आई है। सत्ता में परिवर्तन के साथ साथ समाज प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है। सत्ता ने हर प्रकार से समाज के निम्न, दलित एवं दमित वर्ग का ही शोषण किया है जो पहले से ही गरीबी की चक्की में पिसता चला आ रहा है।
संख्या में सबसे अधिक होने के कारण इस वर्ग के लिए रोजगार सबसे अधिक जरूरी है लेकिन सत्ता में बैठे लोग अपने पद का दुरूपयोग कर न सिर्फ इन्हें रोजगार से वंचित करते हैं अपितु इनकी मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) के लिए भी इन्हें यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं। सत्ता का यह दिखावा सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही सामने आता है। इतनी बड़ी संख्या को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना किसी सोची समझी राजनीतिक साजिश से कम नहीं। मन्नू भंडारी के उपन्यासों में समाज के लगभग सभी पहलू मुखरित हुए हैं किन्तु उनके ‘महाभोज’ में विशेष तौर पर राजनीतिक उथल पुथल के कारण निम्न वर्ग की पीड़ा सामने आती है।

सन् 1979 में लिखा गया मन्नू भंडारी का यह पहला राजनीतिक उपन्यास है। जिस समय स्त्रियों के लिए घर की देहरी लांघना मुश्किल था ऐसे समय में मन्नू भंडारी द्वारा ‘महाभोज’ लिखना किसी क्रांति से कम नहीं था। मन्नू भंडारी ने राजनीति के क्षेत्र में जिस स्याही से लिखा उसके निशान समकालीन लेखिकाओं के लेखन में भी दिखलाई पड़ते हैं। अब स्त्री सिर्फ घर-गृहस्थी तक ही सीमित होकर नहीं लिख रही अपितु उनका क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका है। समकालीन समय में मन्नू भंडारी के अतिरिक्त चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा आदि प्रसिद्ध लेखिकाएं भी हैं जिन्होंने राजनीतिक विषयों पर बड़ी गंभीरता से अपना लेखन कार्य किया है।
उपन्यास की शुरुआत बिसेसर की हत्या से होती है। बिसेसर उर्फ़ बिसू सरोहा गाँव का दलित युवा था। शोषित, पीड़ित, दमित एवं वंचितों को न्याय दिलाना ही उसके जीवन का ध्येय था। बिसू की प्रसिद्धि इसलिए भी थी क्योंकि उसने हरिजन बस्ती में आग लगाकर लोगों को जिंदा जला देने वाले अपराधियों को सजा दिलाने का भी दृढ़ संकल्प लिया था। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ संकल्पी बिसेसर को भ्रष्ट लोकतांत्रिक प्रणाली का शिकार होना पड़ता है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें ऊपर से देखने पर सब स्याह और सफेद है लेकिन भीतर गहराई में ढेरों इंसानरूपी खूनी गिद्ध ताक में बैठे हुए हैं जो कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। उपन्यास की शुरूआती पंक्ति में ही लेखिका ने ऐसे इंसानरूपी गिद्धों की ओर हमारा ध्यान खींचा है- “लावारिस लाश को गिद्ध नोंच-नोंचकर खा जाते हैं।”[1]
यहाँ पर लावारिस लाश का गिद्धों द्वारा नोंच-नोंचकर खाना भ्रष्ट नेताओं के द्वारा बिसेसर की हत्या करना है।
बिसेसर की हत्या सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी वरन उस लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या थी जिसमें ‘शिक्षा’ व ‘समानता’ जैसे अधिकारों को शामिल करने की आदर्श बातें की जाती रही है क्योंकि किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए इन दोनों (शिक्षा और समानता) का होना बेहद जरूरी माना गया है। यदि हम शिक्षा पर बात करें तो किसी भी समाज या जाति के उत्थान के लिए शिक्षा महत्त्वपूर्ण कारक मानी गयी है। शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाने में अक्षम होता है अर्थात् शिक्षा ही वह बूटी है जिसके लेप से अज्ञानतारूपी कोढ़ दूर होता है और हम ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। शिक्षा प्रदत्त ज्ञान ही हमारे भीतर ‘समानता’ और ‘असमानता’ आदि व्यवहार को निर्मित करता है लेकिन जब यही शिक्षा असमानता की दृष्टि से मृत्यु का कारण बनती है तो समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ‘महाभोज’ का बिसू बिसेसर पढ़ा लिखा युवक था। जब वह शहर से गाँव आता है तब सभी दलित भाइयों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाता है। वह एक स्कूल भी खोलता है, साथ ही घर-घर जाकर सभी को पढ़ाता भी है। डॉ. आंबेडकर के सिद्धांत (शिक्षित बनो, संघठित रहो और संघर्ष करो) को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए बिसू दलितोत्थान के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसका यही आन्दोलनकारी रूप सरोहा गाँव के समस्त दलित समाज के लिए प्रेरणादायक है। लेकिन गाँव की कुछ शोषक शक्तियों के आगे बिसेसर का शिक्षित होना उतना ही बड़ा अभिशाप बनकर सामने आता है जितना कि उसका दलित होना।

अपने इस उपन्यास के माध्यम से मन्नू भंडारी ने ऐसी कुत्सित एवं कुंठित राजनीति को उजागर किया है जिसमें चारों तरफ सत्ता (सिंहासन) को हथियाने की होड़ मची हुई है। सत्ता हासिल करने की यह आपसी होड़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है वरन समाज को भी बड़ी मात्रा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान वर्षों से बैठे भूखे नेता गरीबों को झूठे आश्वासन देते फिरते हैं। उनसे बड़े-बड़े वायदे कर उन्हीं के कन्धों पर अपनी राजनीतिक बंदूकें चलाते हैं। इतना ही नहीं अपनी स्वार्थसिद्धि के चलते ये भ्रष्ट नेता गरीबों एवं निचली जातियों को ही वोट बैंक के रूप चुनते हैं। उनकी यहीं धोखेबाजी प्रवृति गरीबों को ओर अधिक गरीब बनाती है। ऐसी ही जालसाजी प्रवृति का प्रतीक है सुकुल बाबू। जो पिछले चुनावों में हारने के बाद राजनीति से संन्यास लेने का वायदा कर चुके थे- “वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद सुकुल बाबू ने बाक़ायदा ऐलान कर दिया था कि वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही वे फिर लपक लिए। क्या करते, पद से उतरने के तुरंत बाद उन्होंने यह महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है।”[2]
भ्रष्ट नेताओं द्वारा फैलाई गयी भ्रष्ट राजनीति के इस दुरंगेपन को लेकर रजनी गुप्त लिखती है – “नेताओं की खोखली नारेबाजी, कुत्सित इरादे और दमघोंटू साजिशों की अंतहीन सच्चाइयों को पूरी बेबाकी से चीरते ‘महाभोज’ की प्रासंगिकता आज भी बहुत जरूरी हस्तक्षेप है जो चमकते-चिकने चेहरों को समझने के लिए सार्थक बयान करते हुए आमजन की विवशता और उनकी असहाय स्थितियों का जीवंत दस्तावेज बन जाता है।”[3]
बहुजन विमर्श को विस्तार देतीं फारवर्ड प्रेस की पुस्तकें
उपन्यास में अभिव्यक्त वोट की इस राजनीति में दलितों के साथ जो अमानवीय अत्याचार होते हैं वे इस बात को पूर्णत: सिद्ध करते हैं कि शक्तिशाली हमेशा अपने से दुर्बल पर काबिज होकर अपनी श्रेष्ठता के प्रतिमान गढ़ता आया है। तथा कमजोर अपने इसी दुर्बलता के कारण भय के माहौल में जीवन जीता रहा है। इसी भय को लेकर नमिता सिंह लिखती है – “महाभोज के दलित और अभावग्रस्त लोग आज भी आतंक के साये में जी रहे हैं। वे मनुष्य नहीं, केवल वोटर हैं। उचित मजदूरी का सवाल तो अलग रहा, यदि वे बाहुबलियों के कहने से वोट नहीं देते तो उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित ही नहीं किया जाता उनके घर भी जला दिए जाते हैं। इतना आतंक कि कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। पुलिस भी पीड़ितों का ही उत्पीड़न करती है।”[4]
चुनाव के समय बिसू की हत्या से मिले मौके को दोनों नेता (सुकुल बाबू और दा साहब) अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते क्योंकि बिसू की मौत उनके लिए किसी सफलता की सीढ़ी से कम नहीं। दोनों नेता बिसू की हत्या के मामले पर अपनी हमदर्दी जताकर समस्त दलित वर्ग के वोट को अपनी-अपनी झोली में डालने पर उतारू हैं। बिसू का मित्र बिंदा जिसके ऊपर बिसू की हत्या का सबसे गहरा आघात पहुँचा है, वह इन नेताओं की ढोंगी प्रवृति को भलीभांति जानता है तथा भाषण के बीच में ही उठकर चीख-चीखकर बोलता है- “कहाँ रखा है पद-वद! भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएँगे कि हम सब तापते ही रह जाएँगे। यह बिसू की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी।”[5]
बिसू का प्रतिरोधी स्वर बाद में बिंदा में साफ दिखलाई पड़ता है। बिंदा का संघर्ष इस भ्रष्ट सत्ता के साथ-साथ उसकी पैरवी करने वाली क़ानूनी व्यवस्था के खिलाफ भी है, जो गरीब जनता की फरियाद को हमेशा अनसुनी करके अपनी मनमानी करती आई है। पुलिस प्रशासक सक्सेना जब बिंदा से बिसू की मौत का प्रमाण मांगता हैं और पुलिस की मदद करने के लिए उसे कहता है तब वह बड़े ही विरोधी स्वर में सक्सेना को जवाब देता है – “कुछ नहीं करेगी यहाँ की पुलिस… कभी कुछ नहीं करेगी। करना होता तो पहले ही नहीं करती?…कानून और पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं! केवल गरीबों को पकड़ने के लिए?”
यह भी पढ़ें – बहुजन साहित्य : परिभाषा और पहचान
लेखिका ने यहाँ बिंदा के माध्यम से आज की मौजूदा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किये हैं। न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक ऐसी कोई भी संस्था नहीं जिसमें मिलावट न हो। यही कारण है कि आज हर जगह अन्याय, अत्याचार की ही तस्वीरें दिखलाई पड़ रही है जो कि भविष्य के लिए किसी अंधकार से कम न होगी। ‘महाभोज’ की प्रसंशा करते हुए उपन्यास के प्रसिद्ध मर्मज्ञ मधुरेश ‘हिन्दी उपन्यास का विकास’ में लिखते हैं – “मन्नू भंडारी का ‘महाभोज’ अंतर्वस्तु के विस्तार का एक विस्मयकारी और अभूतपूर्व उदाहरण है। महिला-लेखक और लेखन की परम्परागत छवि को वह एक झटके से ध्वस्त करता है। भारतीय राजनीति के अमानवीय चरित्र पर इससे तीखी टिप्पणी मुश्किल है। कमलेश्वर के ‘काली आँधी’ के साथ रखकर इस अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। भारतीय समाज में, राजनीतिक जीवन में घुसपैठ करती मूल्यविहीनता और तिकड़म को ‘महाभोज’ गहरी सलंग्नता के साथ उद्घाटित करता है। आज राजनीतिक व्यक्ति समाज और साहित्य का सबसे बड़ा खलनायक है। दा-साहब के दोहरे व्यक्तित्व को, उनके अंदर के शैतान और ऊपर के सत-रूप को, मन्नू भण्डारी ने आश्चर्यजनक विश्वसनीयता से साधा है। बिसेसर, बिंदा और हीरा उस दलित वर्ग के प्रतिनिधि पात्र’ हैं जिनके शव पर राजनीति के गिद्ध जीम रहे हैं।”[6]

धर्म की राजनीति का भी मन्नू भंडारी ने ‘महाभोज’ में बड़ी ही बेबाकी से पर्दाफाश किया है। आज धर्म को आधार बनाकर राजनीति करने वाले नेताओं एवं साधुजनों की कमी नहीं है। गली-कूचों से लेकर मंदिरों तथा बड़े-बड़े भव्य समारोह में आसानी से ऐसे सिद्धस्थ नेताओं के दर्शन होना आम बात है। ये सिद्धस्थ नेता धार्मिक मुखौटा पहनकर जनता के बीच हर दिन गंदी राजनीति का न सिर्फ खेल खेलते हैं अपितु उन्हें (जनता) भरमाकर सहयोग प्राप्त करने में सिद्धस्त होते हैं। धर्म के इस विशाल बाजार में हर रोज अमानवीयता के तराजू पर मानवीयता को तोला जाता है। ‘महाभोज’ के दा साहब इसी धर्म का मुखौटा पहनकर अपनी घिनौनी राजनीति को अंजाम देते हैं। वे न सिर्फ लोगों में गीता जैसे धार्मिक ग्रन्थ के उपदेश देते हैं बल्कि सभी के घरों में गीता की एक-एक प्रति भी बंटवाते हैं। उनका इस कदर गीता प्रेमी होना धार्मिक राजनीति को ही मुख्य रूप से प्रचारित-प्रसारित करना होता है। एक तरफ दा साहब गीता के माध्यम से धार्मिक आदर्शों पर चलने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ बिसू के मित्र बिंदा की गिरफ्तारी का जो षडयंत्र रचते हैं उससे उनका पाखंडी व्यक्तित्व सामने आता है।
प्रस्तुत उद्धरण द्वारा दा साहब की धर्म की इस राजनीति को लेखिका ने स्पष्ट रूप से उजागर किया है- “मेरे लिए राजनीति धर्मनीति से कम नहीं। इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गाँठ बाँध लो- निष्ठा से अपना कर्त्तव्य किये जाओ, बस। फल पर दृष्टि ही मत रखो।’ फिर एक क्षण ठहरकर पूछा, ‘पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो। चित्त को बड़ी शांति मिलती है।”[7]
आज राजनीति को धर्मनीति से जोड़ने वाले नेताओं की तादाद बहुत अधिक बढ़ गयी है। आए दिन समाचारों में साम्प्रदायिक दंगे, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं विषय बनी हुई है। जिसका महाभोज के बिंदा और सक्सेना की भांति घातक परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ रहा है।
यह भी पढ़ें : हिंदी साहित्येतिहास का बहुजन पक्ष
अतः यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि मन्नू भंडारी का ‘महाभोज’ उपन्यास अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। ‘महाभोज’ अर्थात् बड़ा भोज, बड़ा आयोजन। जिसमें खाने के लिए बड़े-बड़े लोग आमंत्रित किये जाते हों। किन्तु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने विशेष को न लेकर व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। ‘महाभोज’ में मन्नू भंडारी ने राजनीति के न सिर्फ एक रूप को दर्शाया है अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीजों को भी उजागर किया है जो सहज नहीं है।
पुस्तक : महाभोज
लेखक : मन्नू भंडारी
प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन
मूल्य : 275 रुपए
अमेजन से खरीदने के लिए यहां क्लिक करें
(कॉपी संपादन : एफपी डेस्क)
[1] भंडारी, मन्नू, ‘महाभोज’, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-1979, पृष्ठ-7
[2] वहीं, पृष्ठ संख्या-9
[3] सं- भारद्वाज, प्रेम, ‘पाखी’, जनवरी 2016, अंक-4, वर्ष-8, पृष्ठ संख्या-99
[4] सिंह कुँवर पाल, बिसारिया अजय, ‘हिन्दी उपन्यास जनवादी परम्परा’, नवचेतन प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2004, पृष्ठ संख्या-175
[5] भंडारी, मन्नू, ‘महाभोज’, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-1979, पृष्ठ-16
[6] मधुरेश, ‘हिन्दी उपन्यास का विकास’, लोकभारती प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2011, पृष्ठ सं-201
[7] भंडारी, मन्नू, ‘महाभोज’, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-1979, पृष्ठ-23
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। हमारी किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति, सामाज व राजनीति की व्यापक समस्याओं के सूक्ष्म पहलुओं को गहराई से उजागर करती हैं। पुस्तक-सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें