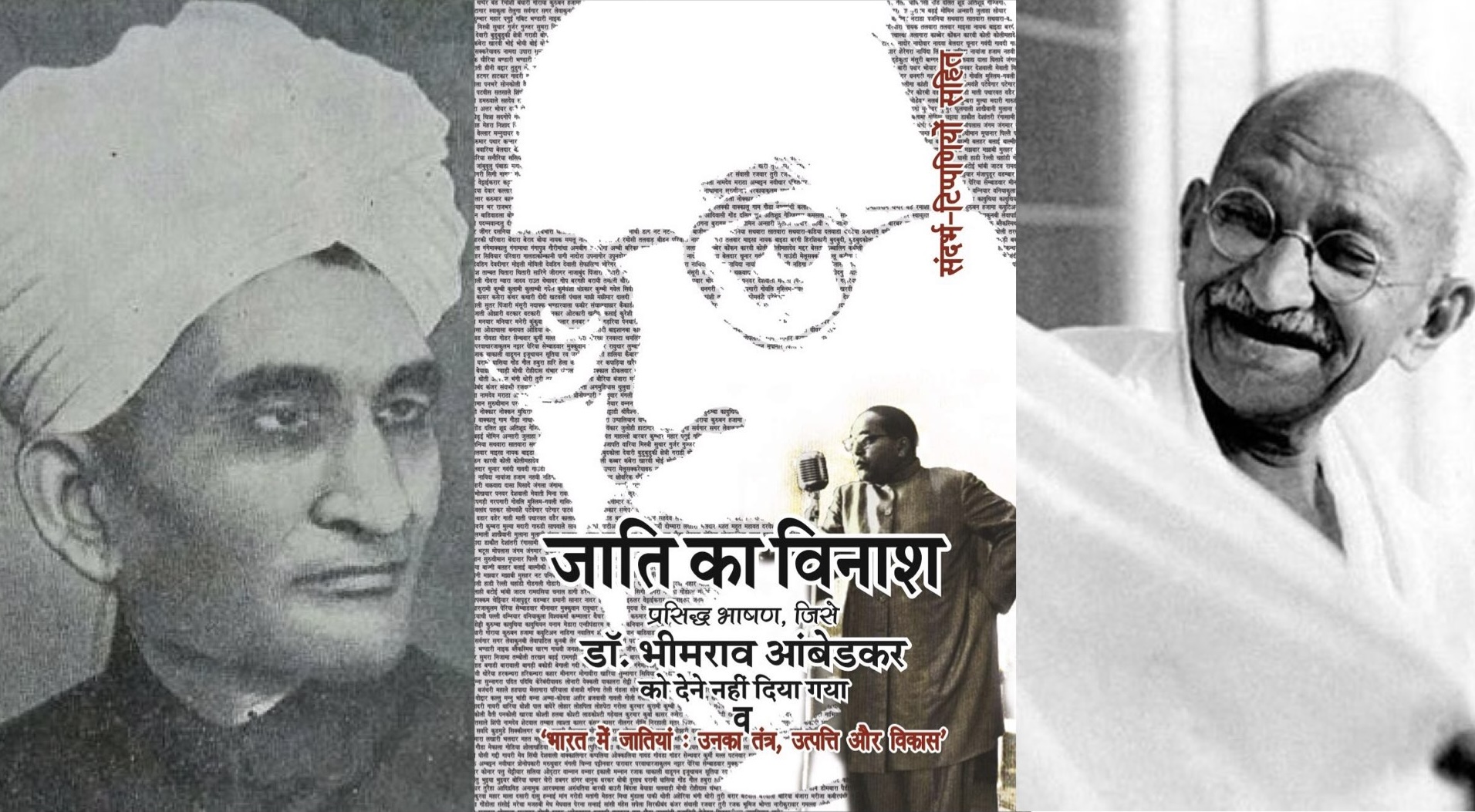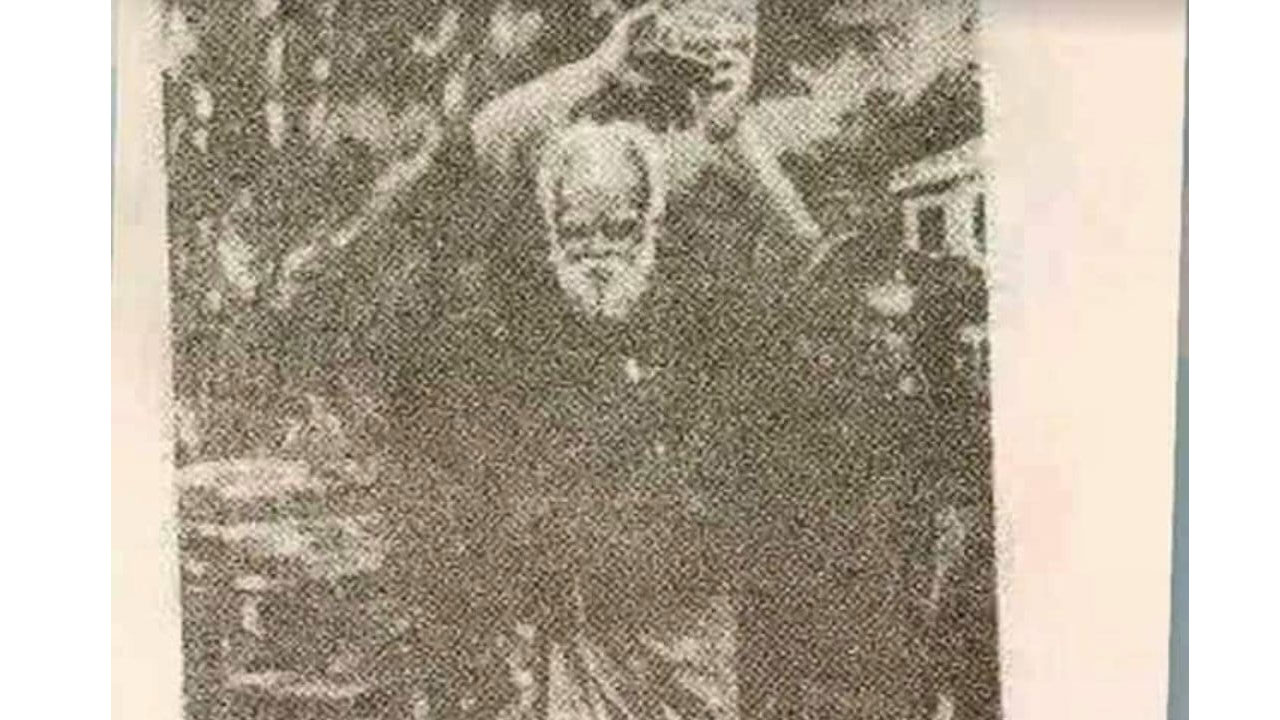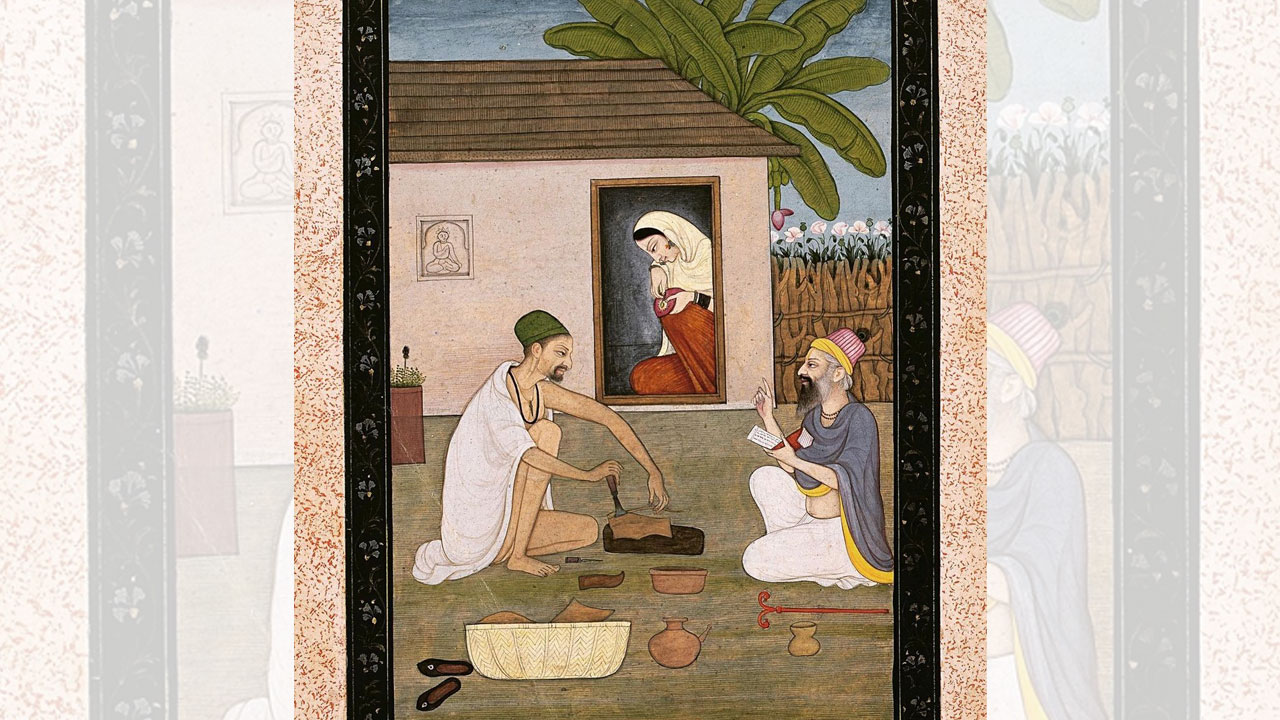झारखंड की राजधानी रांची से लोहरदग्गा तक चलने वाली रेलगाड़ी ‘गड्डी लोहरदग्गा’ अब नहीं चलती। यह ट्रेन 1907 में पहली बार चली थी। तब से लेकर 2004 तक यह गाड़ी चलती रही, न जाने कितने आदिवासियों को उनके गंतव्य तक छोड़ती रही। रांची से लोहरदग्गा के बीच के तमाम गांवों में इसे लेकर सैकड़ों किस्से–कहानियां लोगों के बीच कही-सुनी जाती रही हैं। परंतु, जिस तरह हर चीज को बड़ा बनाया जा रहा है, उसी तरह से छोटी पटरियों (नैरो गेज) को भी बड़ी पटरियों (ब्रॉड गेज) में बदला जा रहा है। इससे कई परंपरागत चीजें, जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, नष्ट हो जाती हैं। रेल पथ को चौड़ा करने के क्रम में छोटी पटरियों से गुजरने वाली यह ट्रेन अब बंद हो चुकी है। अगर रांची और लोहरदग्गा की यात्रा की जाय, तो ज्ञात होगा कि बड़ी पटरी बिछाने के पीछे लोगों को यातायात की सुविधा देने की नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की ढुलाई को आसान बनाने की भावना काम कर रही थी। इन पटरियों पर जो गाड़ियां दौड़ती हैं, उनसे यात्रा करना आदिवासियों के लिए अब पहले की तरह सामान्य नहीं रहा। ये गाड़ियां छोटे स्टेशनों, जहां आदिवासियों की बस्तियां हैं, पर नहीं रूकतीं।
नैरो गेज की पटरियों पर लोहरदग्गा जाने वाली रेलगाड़ी को किस्सा गाड़ी कहना ही उचित लगता है। हालांकि अब इसके बंद होने से किस्से-कहानियों का सिलसिला भी थम गया है। सरकार चाहे माने या न माने लेकिन आदिवासियों के लिए यह सवारी गाड़ी चलते-फिरते इतिहास की तरह थी। तीन-चार डब्बों वाली इस सवारी गाड़ी में जितने श्रम गीत गाए गए और रचे गए, उतने शायद ही किसी ट्रेन में गाए-रचे गए हों। इस ट्रेन से आदिवासियत का जुड़ाव है। आदिवासियों के लिए इसका महत्व विरासत की तरह है।
लोहरदग्गा जानेवाली गाड़ी में अंतिम यात्रा और प्रेम व विछोह के गीत
रेलगाड़ी के बंद होने के कुछ दिन पहले पद्मश्री रामदयाल मुंडा (23 अगस्त, 1939 – 30 सितंबर, 2011), पद्मश्री मधु मंसुरी हंसमुख, अश्विनी कुमार पंकज और बिजू टोप्पो जैसे आदिवासी लेखक, चिंतक और संस्कृति कर्मी इसमें सवार हुए थे। सभी सौ साल पुरानी ट्रेन के बंद होने की सूचना से बहुत दुखी थे। आदिवासियों का लगाव होता ही ऐसा है कि माटी-पानी से लेकर पेड़-पौधों तक को बचाने के लिए जान तक देने से नहीं चूकते। इस यात्रा में मधु मंसुरी हंसमुख ने “चांदो रे” गीत को गाया था। गीत की कुछ पंक्तियॉ हैं –
चांदो रे
चांदो रे, चांदो रे
चांदो रे, चांदो रे
तो कोड़ामय जाबे चांदो
हमार प्रेम तोरी।
दुनिया में प्रेम और समर्पण के अमर गीत बहुत ही सरल शब्दों में लिखे मिलते हैं। यही कारण है कि समूह गीत सबसे अधिक औरतों और आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। इन गीतों की सरलता के कारण ही ये गीत जनगीत का रूप अख्तियार करते हुए लाखों कंठ से एक साथ फूटते हैं। इस तरह के गीतों में प्रेम, समर्पण के साथ श्रम की रवानी भी हिली-मिली होती है। अब इसी गीत को देखें। यह नागपुरी भाषा का गीत है, जिसमें एक आदिवासी लड़की, जिसका नाम उसके प्रेमी ने चांद रखा है, को समझाते हुए उसका प्रेमी कहता है – चांद, तुम्हारे लिए मुझे परदेस जाना होगा। कमाई करके आऊंगा, तो घर अन्न और धन से भर जाएगा। तुम चांद की तरह घर, आंगन, पहाड़, और नदी को रौशन करोगी। परदेस में धूल-आंधी के बीच जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें याद करूंगा और तुम सोना की तरह चमकते हुए मेरे पास आओगी। सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगीं। आंधी-तूफान थम जाएंगे। चांद तुम हर समय मेरे साथ रहना।
चलती रेलगाड़ी में पद्मश्री मधु मंसुर को इस गीत में कई कंठों का साथ मिला। गीत के साथ-साथ कई लोगों ने अपने प्रेम और विछोह के किस्से सुनाए। हम जानते हैं कि दूसरे देश और शहर में कमाने सब जाते हैं, मगर अपने प्रेम को भुलाकर शहरी-परदेसी औरत के प्रेम में पड़ने की कथाएं आदिवासियों में नहीं मिलतीं, जबकि उत्तरप्रदेश और बिहार में ऐसे तमाम गीत और इस तरह की तमाम कथाएं मिल जाती हैं, जिसमें विदेश कमाने गया प्रेमी अथवा पति किसी और स्त्री को अपना लेता है।
किस्सा-कहानियों वाली लोहरदग्गा रेलगाड़ी की स्मृति को सहेजने के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया मगर आदिवासी फिल्मकार मेघनाथ और बिजू टोप्पो ने इस गाड़ी की अंतिम यात्रा पर डाक्युमेंट्री बनाकर उसे अमर कर दिया। छवियों में ही सही, मगर संरक्षित कर दिया। आदिवासियों के साथ जो जुड़ा, उससे उन्होंने टूटकर प्रेम किया। फिर चाहे गड़्डी लोहरदग्गा हो या पेड़-पालो और जन-जनावर! मरने-मिटने के कथाएं हर आदिवासी समुदाय में मिल जाएंगी। अब गौरा देवी को ही लीजिए।
जब गाती हुई गौरा देवी पेड़ों से लिपट गईं
26 मार्च, 1974 की तारीख को कौन भूल सकता है, जब 26 सहेलियों के साथ उत्तराखंड की गौरा देवी (1925 – 4 जुलाई, 1991) पेड़ों को बाहों में भरकर खड़ी हो गईं। उनकी सहेलियों में सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चांदी प्रसाद भट्ट और विरुक्षा देवी शामिल थीं। चमोली की पहाड़ी आदिवासी औरतों के सामने ठेकेदारों और पेड़ माफियाओं की एक न चली। रूतबा, रुपया और कारतूस जैसी दमनात्मक और हिंसाकारी शक्तियां औरतों की समूहगान और हौसलों के सामने ठहर न सकीं। आदिवासी औरतों ने गीत गाते हुए अहिंसात्मक तरीके से उपनिवेशीवादी भावनाओं और शक्तियों को पराजित कर दिया। यह गीत गाते हुए औरतें पेड़ों से लिपट जाती थीं –
माटू हमरू
पानी हमरू
हमरा ही छॉव ई बाऊं भी
पितरों ना लागी बॉऊ,
हमुनाहीं त बचाऊं भी
अर्थात माटी हमारी है/पानी हमारा है/पेड़ हमारे हैं/उनकी छाया हमारी है/यह पूर्वजों की थाती है/इसे हमें ही बचाना होगा।

पेड़ों को अंकवार में भरती हुई आदिवासी महिलाएं बहुत मुखर थीं। उनके तर्कों से प्रशासन निरूत्तर हो गया था। गौरा देवी कहती थीं – “भाई, ये पेड़ नहीं, हमारे जीने का आधार हैं। ये नहीं रहेंगे तो, गांव भी नहीं रह पाएंगे। पेड़ हिमालय की चट्टानों को संभाले हुए हैं।”
गौरा देवी का कथन 17 जून, 2013 को सच हो गया जब भूस्खलन से उत्तराखंड तबाह हो गया। तब लोगों को पता चला कि पहाड़ की अनपढ़ आदिवासी औरतें कितनी दूरदर्शी थीं। पेड़ों की रक्षा में उनसे चिपकी औरतें अक्सर कहा करती थीं – “पेड़ों की जड़ें हाथ हैं, जिनसे वे धरती को संभाले रहते हैं। वे भारी बरसात और बर्फ के पिघलने से आई बाढ़ से हमें बचाते हैं। ये पेड़ नहीं, हमारे पहुरूवे हैं। हमारे भाई बिरन (वीर भाई) हैं, जो इन्हें काटेगा, उसे पहले हमें काटना होगा। हमारे भाईयों ने बहनों की बहुत रक्षा की। अब भाईयों को बचाने की बारी बहनों की है। इसलिए टांगी का पहला वार हमारे शरीर पर करो। हमारा और हमारे भाई का धड़ एक साथ धरती पर गिरना चाहिए।”
इन औरतों को विचलित करने के लिए खूब प्रयास हुए। मगर वे टस से मस नही हुईं। आखिर में प्रकृति विनाशक शक्तियों को पीछे हटना पड़ा।
‘चिपको आंदोलन’ परिवर्तनकारी आंदोलन था। इसने भारत के तमाम पर्यावरण स्नेही आंदोलनों के लिए रास्ता खोल दिया, जिसे भारत के साथ-साथ दुनिया में भी बहुत आदर से देखा गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में इसे बहुत सराहा गया और कहा गया कि “यह आंदोलन सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से एक परिवर्तनकारी आंदोलन था, जिसने अहिंसात्मक आंदोलन चलाते हुए बाजार की ताकतों और लालफीताशाही के दुष्चक्र को पराजित करके वन संपदा को नष्ट होने से बचा लिया।” इस आंदोलन की सफलता ने पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बल दिया। कई पर्यावरण स्नेही संगठनों ने जल संपदा संरक्षण की दिशा में बेहतरीन काम किया और रूखी-सूखी धरती को जलमय बनाकर पूरे क्षेत्र को हरा-भरा बना दिया। कई गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वन और वन जीवन संरक्षण की दिशा में अच्छा काम किया जाने लगा। इतना ही नहीं, प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति रक्षा में हुए जनांदोलनों के अध्ययन की शुरूआत भी इस आंदोलन के बाद हुई। कई अध्येता तीसरी दुनिया की दलित और आदिवासी औरतों के जन-गीतों के अध्ययन की ओर अग्रसर हुए हैं। इरीन डंकेलमैन और जॉन डेविडसन इसी तरह के अध्येता हैं, जिन्होंने तीसरी दुनिया की औरतों के संघर्षों और यातनाओं का अध्ययन किया है। उनकी पुस्तक ‘वुमन एंड एनवायरनमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड – अलायंस फॉर द फ़्यूचर’ इसी तरह की एक दस्तावेज है, जिसमें औरतों द्वारा चलाए जा रहे तमाम पर्यावरणीय आंदोलनों की भूमिका को जांचा-परखा गया है। यह पुस्तक सोमालिया के शरणार्थी शिविरों में रहते हुए अपनी पीड़ा से मुक्ति के लिए संघर्षरत औरतों को समर्पित है। सोमालिया के राहत शिविरों में रहने वाली औरतों के जनगीत को इस किताब में जगह दिया गया है। वह गीत इस प्रकार है –
हम अपनी पीड़ा के गीत को गाना चाहती हैं
हम अपनी परेशानियों को बताना चाहती हैं
हमारा जीवन एक बुरा सपना है, जिसे कोई नहीं समझ सकता
मगर देखना एक दिन हमारी कोशिशें रंग लाएंगी….
इसी तरह के जनगीत चिपको आंदोलन की महिलाएं ने भी गाए थे। औरतों की पीड़ा सभी जगह एक-सी है, इसीलिए उनके गीत भी एक-से हुआ करते हैं। इन शरणार्थी औरतों में अधिकांश महिलाएं आदिवासी समुदाय से आती हैं। चिपको आंदोलन और सोमालिया की बेघर, बलत्कृत आदिवासी औरतों की एक ही आत्म पुकार है – धरती और संसाधनों की लूट से मुक्ति!
सोमालिया की औरतों का दर्द यातनाओं का दस्तावेज बनकर इस पुस्तक में नुमाया हुआ है। इन औरतों की समस्या से दुनियां की बड़ी शक्तियां मुंह मोड़ चुकी हैं। थोड़ा बहुत काम संयुक्त राष्ट्र संघ के राहत पैकेजों के माध्यम से कभी– कभार हो जाता है।
बहरहाल, आज भी जंगलों, पहाड़ों और नदियों को मिटाया जा रहा है। जिस तरह से गाड़ी लोहरदग्गा की स्मृति को संजोने के लिए आदिवासी कलाकारों ने डाक्युमेंट्री बनाई वैसी ही कोशिश सोमालिया, आरे कॉलोनी (मुंबई), छत्तीसगढ़, हिमांचल प्रदेश और झारखंड के आदिवासी करते आ रहे हैं।
(संपादन : नवल/अमरीश)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया