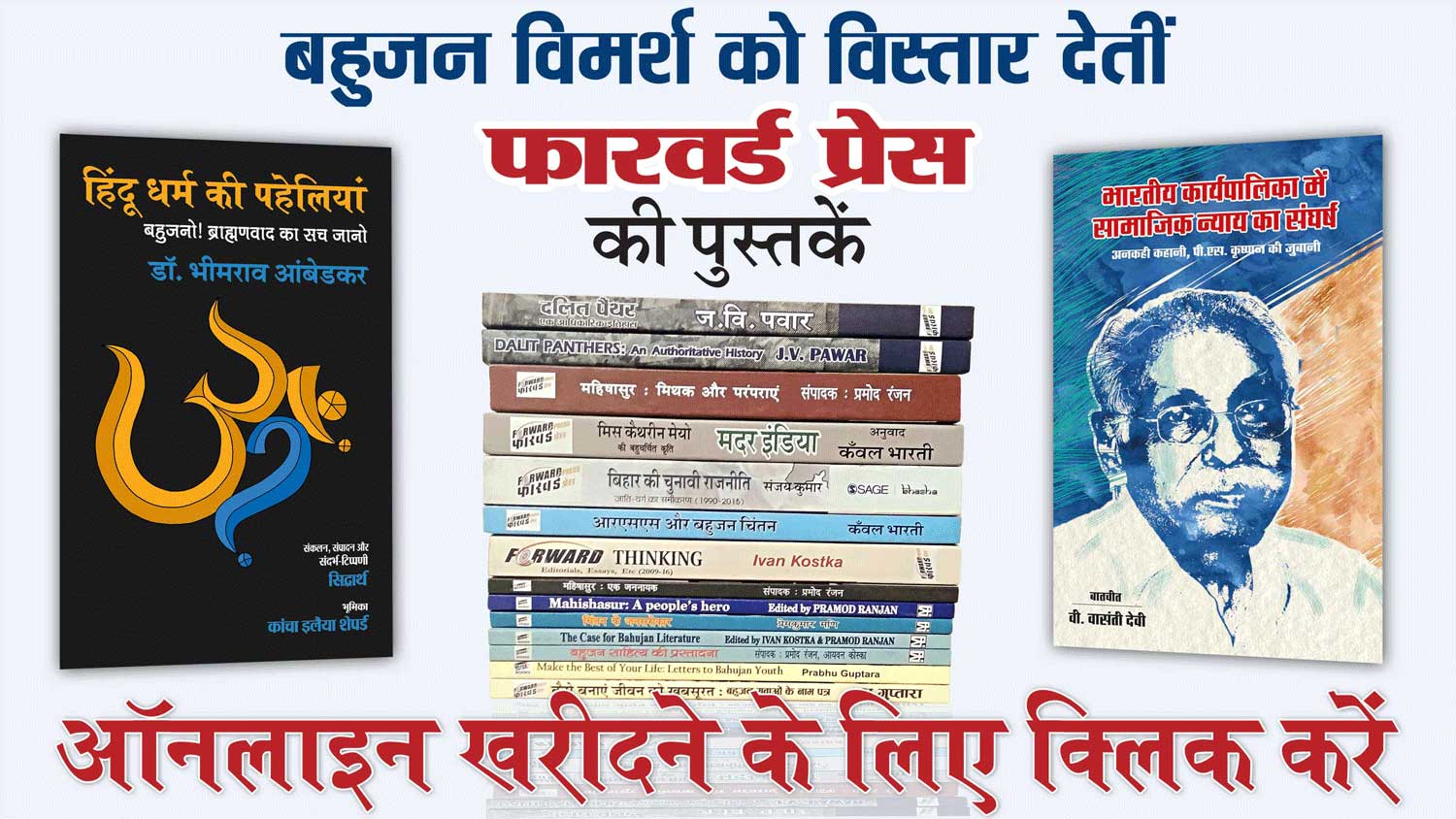महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन (25 दिसंबर 1927) से पहले तक डॉ. आंबेडकर को यह धुंधली सी उम्मीद थी कि हिंदू धर्म में परिवर्तन और सुधार करके हिंदू धर्म के भीतर दलितों को समता का हक दिलाया जा सकता है और हिंदू धर्म को एक समता मूलक धर्म बनाया जा सकता है। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने महाड़ के चवदार तालाब में दलितों के पानी पीने के अधिकार को स्थापित करने के लिए सत्याग्रहियों के साथ तालाब में 20 मार्च, 1927 को पानी पीया था, जिसके बाद सवर्णों ने दलितों के साथ मारपीट की और चावदार तालाब का शुद्धिकरण किया, क्योंकि उनके अनुसार आंबेडकर सहित अन्य अस्पृश्य दलितों के पानी पीने से तालाब अपवित्र हो गया था।
आंबेडकर चावदार तालाब में पानी पीने नहीं गए थे, बल्कि इस तथ्य को साबित करने गए थे कि हिंदू होने के चलते दलितों का भी अन्य हिंदुओं की तरह समान हक है, जिस तालाब में अन्य हिंदू पानी पी सकते हैं, यहां तक की गैर-हिंदू और जानवर तक पानी पी सकते हैं, उस तालाब में हिंदू समाज के हिस्से के रूप में आखिर दलित क्यों पानी नहीं पी सकते हैं। चावदार तालाब में पानी पीने अधिकार के लिए संघर्ष को डॉ. आंबेडकर ने धर्मसंग्राम की संज्ञा दी।
इस संदर्भ में डॉ. आंबेडकर ने ‘बहिष्कृत भारत’ के संपादकीय में लिखा कि ‘अस्पृश्य लोग पानी पीने के लिए चावदार तालाब पर गए, इसलिए मार-पीट हुई, ऐसा कहने पर मारपीट की घटना का सही स्वरूप उजागर नहीं होता, मारपीट की घटना का वास्तविक स्वरूप एकदम अलग है, अत: उसे दंगा कहने के बजाय धर्मसंग्राम (धर्मयुद्ध) कहना ज्यादा उचित होगा, ऐसा हमारा विचार है। हिंदू समाज के घटक, हिंदू धर्म का अनुयायी होने के नाते अन्य हिंदू जातियों की भांति हम भी समान योग्यता के अधिकारी हैं, प्रश्न यह है कि हमें भी समान अधिकार है अथवा नहीं? ( ‘बहिष्कृत भारत’ में प्रकाशित बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के संपादकीय, सम्यक प्रकाशन, पृ. 22)
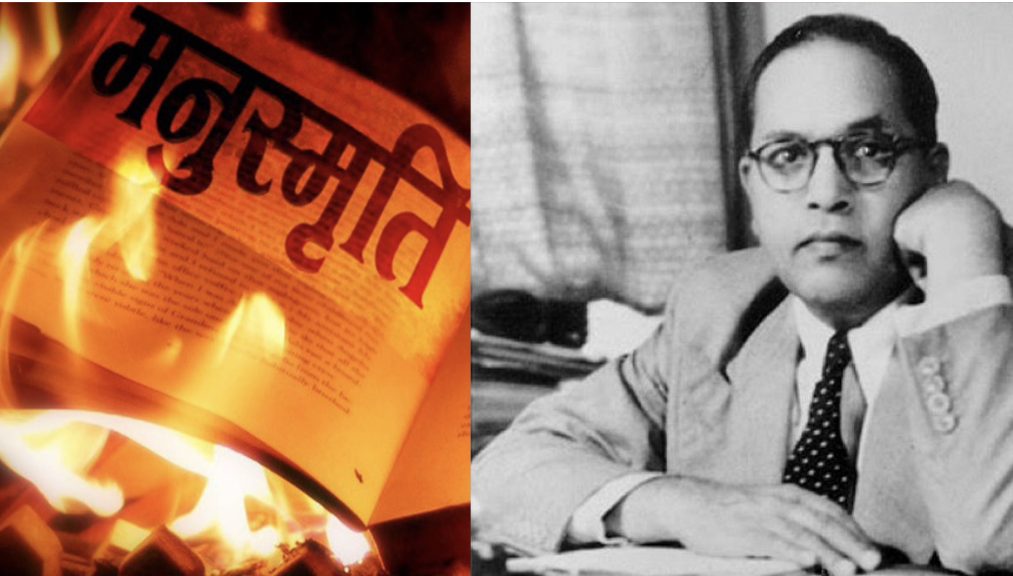
दरअसल, प्रश्न पानी पीने का नहीं था, प्रश्न यह था कि हिंदू कहे जाने के नाते अस्पृश्यों (दलितों) को हिंदुओं के समान अधिकार प्राप्त है या नहीं? यही तय करने का प्रश्न चावदार तालाब में पानी पीने के प्रकरण का आधार था। सवर्णों द्वारा दलितों के पानी पीने के अधिकार का विरोध, दलितों के साथ हिंसा और उनके पानी पीने के बाद तालाब को शुद्ध करने की घटना ने यह साबित कर दिया कि वे दलितों को समान अधिकार देने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है, भले ही वह उन्हें सिद्धांत रूप में हिंदू धर्म का हिस्सा मानते रहे हों।
महाड़ धर्मयुद्ध के चरित्र का विश्लेषण करते हुए डॉ. आंबेडकर लिखते हैं कि ‘महाड़ धर्मयुद्ध में दोनों पक्षों के लोग धार्मिक दृष्टि से एक ही धर्म यानी हिंदू धर्म के हैं। ऐसा होने पर भी कुछ धर्मबंधुओं ने अपने ही दूसरे धर्म बंधुओं को, तुम सामाजिक दृष्टि से नीच हो, तुम्हारे स्पर्श से हमार अध:पतन होगा, यह प्रमाणित करने के लिए इस तरह के हुडदंग किए।” (बहिष्कृत भारत में प्रकाशित बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के संपादकीय, सम्यक प्रकाशन, पृ. 23)
इस संदर्भ में हिंदू धर्म के दार्शनिक पाखंड को उजागर करते हुए डॉ. आंबेडकर ने हिंदू धर्म की तुलना ईसाई और मुस्लिम धर्म से करते हुए लिखा कि ‘इतना होने पर भी सामाजिक समता ईसाई और मुस्लिम राष्ट्रों में दिखाई देती है, किंतु हिंदू समाज में इसका कोई चिह्न दिखाई नहीं पड़ता। वह (समता) स्थापित होने के प्रयत्न होने पर उल्टे हिंदू धर्मी लोग ही रुकावट पैदा करते हैं। … आचरण की दृष्टि से वे (दलित) असमान ही नहीं, अपवित्र भी हैं।’ (वही) इसी संदर्भ में धर्म और मनुष्य के रिश्ते पर भी अपना विचार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धर्म के लिए है। दरअसल वे इस निष्कर्ष तक पहुंचते प्रतीत होते हैं कि जो धर्म हमारा खयाल रखेगा उस धर्म के लिए हम अपने प्राण न्योछावर करेंगे, जो धर्म (हिंदू धर्म) हमारी परवाह नहीं करता, उसकी परवाह हम क्यों करें?
दलितों (अस्पृश्यों) के प्रति हिंदू धर्म के असल रवैए से परिचित होने के बाद भी ही आंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति के दहन का कार्यक्रम रखा, जो शूद्रों को अपवित्र और दोयम दर्जे का ठहराती है और उन्हें हिंदू कहते हुए भी सभी अधिकारों से वंचित रखती है। मनुस्मृति के दहन को एक ऐतिहासिक घटना कहते हुए डॉ. आंबेडकर के जीवनीकार धनंजय कीर लिखते हैं कि 25 दिसंबर 1927 की दिन एक अत्यन्त स्मरणीय दिन कहा जाएगा।
महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन के करीब दो वर्ष बाद 2 मार्च 1930 को डॉ. आंबेडकर ने मंदिर प्रवेश सत्याग्रह भी चलाया, जिसमें नासिक मंदिर (कालाराम मंदिर) प्रवेश सत्याग्रह सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन इसका भी सवर्ण हिंदुओं ने तीखा विरोध किया और सत्याग्रहियों के साथ हिंसा की। पानी पीने के अधिकार के लिए सत्याग्रह के नतीजे के बाद मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए आखिर आंबेडकर ने क्यों सत्याग्रह किया? इसका उत्तर उन्होंने स्वयं दिया है– ‘मैंने मंदिर-प्रवेश संबंधी आंदोलन इसलिए शुरू नहीं किया कि मैं चाहता था कि पददलित वर्ग के लोग मूर्तिपूजक बने …अथवा मैं मानता था कि मंदिर प्रवेश का अधिकार मिल जाने से वे बराबरी प्राप्त कर लेंगे तथा हिंदू समाज के अभिन्न अंग बन जाएंगे …. (लेकिन) मुझे लगा कि यह पददलित वर्ग के लोगों को ऊर्जावान बनाने का तथा उन्हें उनकी स्थिति से वाकिफ़ कराने का सर्वोत्तम तरीका है। (उद्धृत, गेल ओमवेट, ‘आंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर’, पेंगुइन बुक्स, पृ.54)
महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के फलाफल के बाद आंबेडकर इस तथ्य से पूरी तरह मुतमईन हो गए कि हिंदू धर्म असमानता की बुनियाद पर खड़ा है और दलितों को इसमें समानता का हक प्राप्त नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में सुधार और दलितों को हिंदू धर्म में समान हक दिलाने के अपने प्रयासों (1920 से 1930 के बीच) के संबंध में स्वयं उन्होंने लिखा कि ‘लंबे समय तक मैं स्वयं यही मानता रहा कि हम हिंदू समाज को उसकी विकृतियों से मुक्त करा सकते हैं और डिप्रेस्ड क्लास (दलितों) को बराबरी की शर्तों पर उसमें समाहित कर सकते हैं। महाड़ में चावदार तालाब सत्याग्रह और नासिक मंदिर (कालाराम मंदिर) प्रवेश सत्याग्रह, दोनों इसी उद्देश्य से प्रेरित थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने मनुस्मृति दहन किया और सामूहिक जनेऊ धारण अनुष्ठानों का आयोजन किया था। खैर, अनुभव की बदौलत अब मेरे पास कहीं बेहतर समझ है। आज मुझे इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि हिंदुओं के बीच रहते हुए डिप्रेस्ड क्लासेज़ को बराबरी का दर्जा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू धर्म खड़ा ही असमानता की बुनियाद पर है। अब हमें हिंदू समाज का हिस्सा बने रहने की कोई चाह नहीं है।’ (उद्धृत, क्रिस्टोफ़ जैफरलो, भीमराव आंबेडकर, एक जीवनी, राजकमल प्रकाशन, पृ. 45)
महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह की असफलता के बाद आंबेडकर का हिंदू धर्म से इस कदर मोहभंग हुआ कि उन्होंने 12 अक्टूबर 1935 को येओल में दलित वर्ग के सम्मेलन में एक संकल्प रखा। संकल्प में उन्होंने वहां उपस्थित दसियों हजार उत्साही कार्यकर्ताओं के समक्ष धर्मपरिवर्तन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ‘मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं और अस्पृश्यता की मार झेलता रहा हूं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं।’ (उद्धृत, गेल ओमवेट, आंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर, पेंगुइन बुक्स, पृ.57) अपने इस संकल्प को उन्होंने ‘जाति का विनाश’ में दोहराया। अंतिम तौर पर उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म का औपचारिक तौर पर भी परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करते समय आंबेडकर और उनके अनुयायियों द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाएं इस बात का सबूत हैं कि आंबेडकर का हिंदू धर्म से किस कदर मोहभंग हुआ था।
(lसंपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया