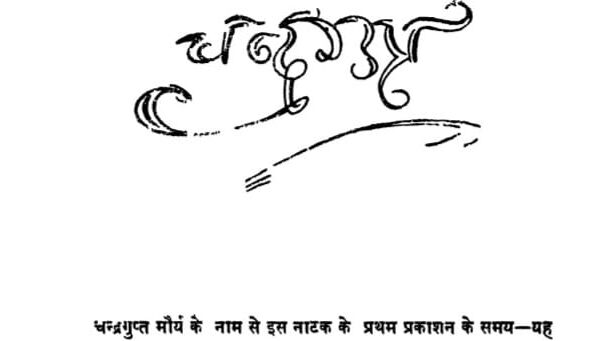हिंदी पट्टी के एक अहम प्रदेश बिहार में आज भी वामपंथ की उल्लेखनीय उपस्थिति है। इसके केंद्र में भाकपा-माले (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी लेनिनवादी) है। बिहार विधानसभा में अभी इसके 12 विधायक हैं। मौजूदा दौर में भाकपा-माले विपक्षी एकता के बिहार मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। इसकी यह स्थिति तब है जब मंडल उभार में बिहार-यूपी जैसे राज्यों में परंपरागत वामपंथ की जमीन खिसक गयी। केवल भाकपा-माले एक हद तक अपने जमीन को बचा पाने में कामयाब रही है। खासकर वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के हिस्सेदार के बतौर 19 सीटों पर चुनाव लड़कर भाकपा माले ने संसदीय इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि 12 सीटें हासिल की है। लेकिन उसका यह हासिल बिहार में उसके द्वारा कोई नयी जमीन तोड़ने और उल्लेखनीय विस्तार की अभिव्यक्ति नहीं है।
भाकपा-माले परंपरागत वामपंथ से अलग किस्म की पार्टी रही है। बिहार में सबसे हाशिए के समाज के ईज्जत-सम्मान, जमीन व मजदूरी जैसे सवालों पर लड़ते हुए यह पार्टी आगे बढ़ी है। जमीनी स्तर पर सवर्ण दबदबे के खिलाफ सबसे हाशिए के आत्मसम्मान व दावेदारी को बुलंद किया है, लेकिन जीवन के तमाम क्षेत्रों में सवर्ण वर्चस्व को तोड़ने के लिए सामाजिक न्याय के जरूरी प्रश्नों को राजनीतिक लड़ाई का एजेंडा बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ी।
अब हाल के दिनों में सामाजिक न्याय के प्रश्नों को लेकर भाकपा-माले मुखर हो रही है। इस बार पटना के गांधी मैदान में आयोजित अपने 11वां महाधिवेशन में इसके संकेत भी सामने आए। इस मौके पर ‘लोकतंत्र बचाओ-देश बचाओ’ रैली में जिन दस राजनीतिक प्रस्तावों को सहमति दी गई, उनमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रद्द करने तथा दलितों-पिछड़ो के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की मांग भी शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ सामाजिक न्याय की राजनीतिक पार्टियों के साथ अन्य वामपंथी पार्टियां ने भी खुलकर स्टैंड नहीं लिया है, जबकि भाकपा-माले के विरोध का स्वर लगातार सामने आ रहा है। अतिशयोक्ति नहीं कि 2020 के बाद से इस वामपंथी दल में एक तब्दीली दीख रही है। खासकर सामाजिक न्याय के परंपरागत मुद्देों यथा आरक्षण, जातिवार जनगणना आदि। हालांकि अपनी पहचान के अनुरूप वह इन मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं उतर रही है और न ही सामाजिक न्याय के व्यापक एजेंडा को राजनीतिक मुहिम के एजेंडा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हुए दीख रही है।
भाकपा-माले के सामाजिक न्याय पर बदलते रूख के साथ इस मसले पर गौर किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि भाकपा-माले के ढ़ांचे व सांगठनिक जीवन में सामाजिक न्याय किस हद तक अभिव्यक्त होता है। लंबे समय से परंपरागत वामपंथी पार्टियों के नेतृत्व में सवर्णों के वर्चस्व होने का सवाल उठता आ रहा है। इस मसले पर परंपरागत वामपंथी पार्टियों से भाकपा-माले किस हद तक अलग है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। सामाजिक न्याय के नजरिए से भाकपा-माले के सांगठनिक ढ़ांचे पर गौर करने से पहले यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टियों और अन्य संसदीय राजनीतिक पार्टियों के बीच फर्क होता है। कम्युनिस्ट पार्टियों में पार्टी संगठन प्रधान होता है। नेतृत्वकारी निकाय में राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव और राज्य व निचले निकायों में सचिव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे ज्यादा प्राधिकार रखते हैं। जनसंगठनों के नेतृत्वकारी निकायों में भी महासचिव और सचिव जैसे पदों का प्राधिकार ही ज्यादा होता है। कम्युनिस्ट पार्टियां अन्य संसदीय पार्टियों के पैटर्न पर नहीं चलती हैं। यहां विधायक-सांसद और जनसंगठनों की भूमिका पार्टी संगठन के मातहत होती है।
पटना में आयोजित हालिया महाधिवेशन से दीपंकर भट्टाचार्य लगातार पांचवीं बार महासचिव चुने गये हैं। साथ ही महाधिवेशन से पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्वकारी निकाय केन्द्रीय कमिटी भी गठित हुई है।
बताते चलें कि 18 दिसंबर, 1998 को विनोद मिश्र की मृत्यु के बाद से दीपंकर भट्टाचार्य लगातार महासचिव के पद पर आसीन हैं। आज तक भाकपा-माले का महासचिव कोई गैर सवर्ण नहीं हुआ है। महाधिवेशन खत्म होने के अगले दिन संवाददाताओं के लिए जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 77 सदस्यीय केंद्रीय कमिटी बनी है, जिसमें 13 नए सदस्य शामिल किए गये हैं। इस कमिटी में 5 नई महिला सदस्यों – फरहद बानू, मंजू प्रकाश, इंद्राणी दत्त, श्वेता राज और मैत्रेयी कृष्णन के शामिल किए जाने के साथ ही महिलाओं का औसत बढ़कर करीब 16 प्रतिशत हो गया है। प्रेस विज्ञप्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी का जिक्र जरूरी समझा गया है। इसके जरिए लैंगिक न्याय के प्रति चिंता व प्रतिबद्धता जाहिर की गयी है।
दूसरी तरफ एससी,एसटी व ओबीसी की हिस्सेदारी का कोई जिक्र नहीं है। आखिर उत्पीड़ित पहचानों की हिस्सेदारी का जिक्र नहीं करना क्या साबित करता है? इससे भाकपा-माले द्वारा जाति के प्रश्न को स्वीकारने और सामाजिक न्याय के प्रति गंभीरता पर ही सवाल खड़ा होता है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय कमिटी में शामिल किये गये नये लोगों में सत्यदेव राम, कुमार परवेज, संदीप सौरभ, नवीन कुमार, प्रकाश कुमार, नीरज कुमार, इंद्रेश मैखुरी व कैलाश पांडे शामिल हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नई केंद्रीय कमिटी में शामिल 8 नये पुरुष सदस्यों में 5 सवर्ण हैं। बिहार से शामिल 6 पुरुष व महिला सदस्यों में 2 सवर्ण, 2 पिछड़े और 2 दलित हैं। गौरतलब है कि बिहार से पिछली केंद्रीय कमिटी में 17 सदस्य थे, जिसमें 6 सवर्ण थे। वहीं पोलिट ब्यूरो में बिहार से 4 सदस्य थे, जिसमें सवर्णों की हिस्सेदारी आधी थी। इस महाधिवेशन से चुनी गयी केंद्रीय कमेटी द्वारा पोलिट ब्यूरो का चुनाव बाद में होना है।
ऐसे तो बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को सवर्णों, खासकर भूमिहारों के वर्चस्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी कही जाती रही है, लेकिन भाकपा-माले का सच भी ज्यादा जुदा नहीं है। बिहार में जहां पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है, वहां भी पार्टी के राज्य सचिव लगातार सवर्ण जाति से ही बनते आ रहे हैं और उसमें भी अधिकांश समय तक भूमिहार जाति के ही रहे हैं। वर्तमान राज्य सचिव कुणाल भी इसी जाति के हैं।
पूर्व विधायक व मध्य बिहार में नक्सलवाड़ी आंदोलन के सूत्रधारों में से एक रहे रामनरेश राम अपवाद रहे, जो भूमिगत आंदोलन के दौर में अत्यंत ही थोड़े समय के लिए राज्य सचिव बनाए गए थे।
इस सच्चाई पर नजर डालना जरूरी है कि सीपीआई के सामाजिक आधार में सवर्णों, खासतौर पर भूमिहारों के टोले-मोहल्ले भी शामिल रहे हैं, इसलिए नेतृत्व में सवर्णों के पहुंचने का आधार भी है। जबकि, कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच खासकर भाकपा-माले तो दक्षिण टोले यानी हाशिए के छोर से ही खड़ा हुआ है। इसका सामाजिक आधार तो विशुद्ध रूप से दलितों-पिछड़ों का ही रहा है, फिर भी नेतृत्व में सवर्णों का वर्चस्व होना सवाल खड़े करता है। दिलचस्प यह भी कि जमीन पर संघर्षों की अगुआई दलित-पिछड़े कार्यकर्ता-नेता ही करते हैं। जबकि पार्टी ढ़ांचे में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर उसकी हिस्सेदारी व हैसियत के मामले में स्थिति उलट जाती है। नेतृत्वकारी निकायों में सवर्णों का अनुपात बढ़ता जाता है। पार्टी स्थापना काल से आज तक शीर्ष नेतृत्व के मामले में सवर्ण विशेषाधिकार कायम है। भारतीय समाज के वर्ण-जाति व्यवस्था के ढ़ांचे के साथ इस वामपंथी पार्टी के ढ़ांचे की शानदार संगति बनती है।
हालांकि हाल के वर्षों में राज्य से लेकर केंद्रीय कमिटी तक के नेतृत्वकारी निकायों की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है, लेकिन आज भी गैर सवर्ण नेताओं की नेतृत्व में निर्णायक भूमिका नहीं है। बिहार से लेकर दिल्ली के मुख्यालय पर सवर्ण समूह का ही नियंत्रण है। यहां तक कि संघर्ष के मैदान से इतर पार्टी गतिविधियों में मंच से लेकर प्रेस कांफ्रेंस तक में भी नेतृत्व का गैर सवर्ण हिस्सा हाशिए पर ही नजर आता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि भाकपा-माले के सांगठनिक जीवन में बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम का बंटवारा भी वर्ण-जाति के अनुरूप ही दिखता है। पार्टी का बौद्धिक काम सवर्णों के हिस्से है। पार्टी के मुखपत्रों– ‘लिबरेशन’ व ‘लोकयुद्ध’ से लेकर अन्य पत्रिकाएं यथा ‘समकालीन जनमत’, ‘श्रमिक सॉलिडैरिटी’, ‘आधी जमीन’ का संपादन सवर्णों के जिम्मे ही है।
पिछले चुनावों में भी भाकपा-माले का टिकट पाने और जीतने वालों में खासतौर पर दलित-पिछड़े समुदाय के ही रहे हैं। जमीनी संघर्ष व जन आंदोलन का मोर्चा और जननेताओं के बतौर भूमिका स्वाभाविक तौर पर उनके लिए ही आरक्षित रही है। इसलिए चुनाव में उम्मीदवार होना अप्रत्याशित नहीं है।
जनसंगठनों पर गौर कीजिए तो वहां भी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में निर्णायक पदों पर कमोबेश सवर्णों की मौजूदगी बनी हुई है। हालांकि भाकपा-माले ने पार्टी दस्तावेज में जाति उन्मूलन को क्रांतिकारी लक्ष्य के बतौर स्वीकार किया है। लेकिन जिस स्थिति को समाज में बदलना है, उसे पार्टी जीवन में बनाये रखना और सवाल ही नहीं मानना बड़ा सवाल खड़ा करता है। जाति वर्चस्व को जीवन के हर क्षेत्र में तोड़ना है तो फिर पार्टी के ढ़ांचे में भी खत्म होना ही चाहिए। वैसे भी पांचवीं बार दीपंकर भट्टाचार्य को भाकपा-माले का महासचिव चुना जाना पार्टी विकास के गतिरोध और पार्टी पर सवर्ण नियंत्रण का प्रतीक ही बनाता है। आश्चर्य नहीं कि सवर्ण वर्चस्ववाद मंडल-बहुजन उभार में परंपरागत वामपंथी पार्टियों के हाशिए पर जाने और भाकपा-माले की अग्रगति के ठहर जाने की वजह है।
[लेखक रिंकु यादव 2005 से लेकर 2008 तक भाकपा-माले के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के प्रदेश अध्यक्ष व 2012 से लेकर 2015 तक पार्टी की राज्य कमिटी के सदस्य रहे। वर्ष 2015 के अंत में इन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी]
(संपादन : नवल/अनिल)