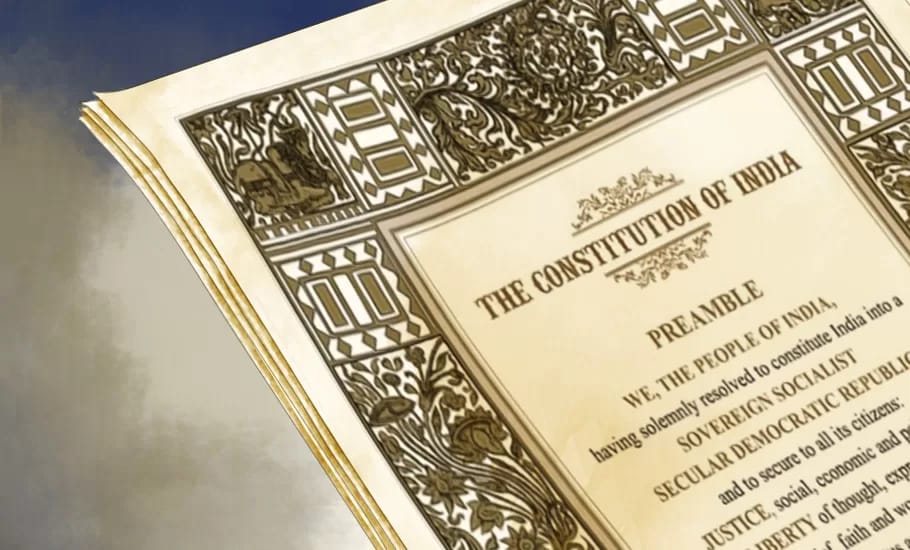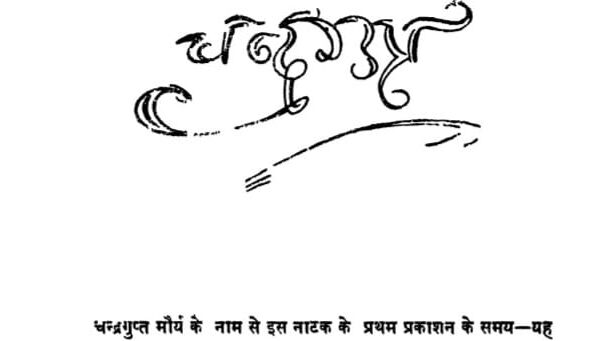उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बहरामपुर मोहल्ले में राप्ती नदी के किनारे बाले मियां का मैदान है। यह ऐतिहासिक मैदान स्वाधीनता आंदोलन का भी गवाह रहा है। उस दौर में यहां पर जवाहरलाल नेहरू और गांधी तक ने जनसभा को संबोधित किया था। इसका वर्णन ‘गोरखपुर गजेटियर’ में भी मिलता है। इसी बाले मियां के मैदान में हर वर्ष मई महीने में मेला लगता है। इसके साथ-साथ बहराइच जिले में भी यह मेला लगता है। इस वर्ष यह मेला 14 मई से शुरू होकर एक माह तक चलेगा।
इस मेले की शुरुआत बाले मियां के एक काल्पनिक विवाह से होती है, जिसमें होली के त्योहार के दो हफ्ते बाद उनकी लगन रखी जाती है। उसके ढाई महीने बाद बाले मियां के विवाह की रस्म होती है। उस दिन शाम को 6 बजे से ही आकर्षक झांकियों के साथ बारात का सिलसिला शुरू होता है। लोग पलंग-पीढ़ी लेकर नाचते-गाते दरगाह क्षेत्र में आते हैं। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे सिर पर छोटी-छोटी पलंग लेकर चलते हैं, जिसे पलंग-पीढ़ी कहते हैं। यह सिलसिला रात भर चलता है, जिसे देखने के लिए हज़ारों लोग उमड़ पड़ते हैं।
सिर पर पलंग-पीढ़ी लेकर आए लोगों का स्वागत आस्ताने (दरगाह) में जायरीनों द्वारा किया जाता है। लोग यहां पर जियारत करके अपने-अपने हिसाब से नज़राने या अकीदत पेश करते हैं। दोनों स्थानों पर एक माह तक चलने वाले इस मेले में लाखों लोग भाग लेते हैं। लोग इस दौरान मनौतियां भी मानते हैं और पूरी होने पर दरगाह में चादर चढ़ाते हैं।
बाले मियां के विवाह के बारे में गोरखपुर विश्वविद्यालय में सूफ़ी मत के जानकार बी. एन. चतुर्वेदी बताते हैं कि यह विवाह एक तरह से इंसान के खुदा से मिलने की एक रस्म है। सूफ़ी मत में अनेक जगह ऐसा देखा गया है। कबीर के सबद में भी ये बातें बार-बार आती हैं। संभव है कि कबीरपंथ और बाले मियां संबंधी विमर्श में साम्यता हो, इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है।
बाले मियां का मूल मेला बहराइच जिले में है, जहां इनका मूल मज़ार है। ऐसा बताया जाता है कि बाद में उसी मज़ार की एक ईंट लाकर गोरखपुर में स्थापित की गई और यहां भी मेले की शुरुआत की गई। वैसे तो इस मेले को लोग हज़ारों साल पुराना बतलाते हैं, लेकिन बहराइच के मज़ार की प्राचीनता को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यह मेला करीब 400-500 साल पुराना अवश्य रहा होगा।
इस मेले की ख़ासियत यह है कि इसमें मूलतः दलित-पिछड़े, आदिवासी समाज व पसमांदा मुस्लिम समाज के लोग ही अधिक शिरकत करते हैं।

बाले मियां को ही गाजी मियां के नाम से जाना जाता है। सवाल है कि गाज़ी मियां या बाले मियां कौन थे और यह मेला क्यों लगता है? इस संबंध में अनेक किंवदंतियां लोकगाथाओं के रूप में मौज़ूद हैं।
माना जाता है कि हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी या गाज़ी मियां (1014-1034) महमूद गज़नवी के भांजे थे तथा उनकी सेना के मुखिया भी थे। माना जाता है कि ग्यारहवीं शताब्दी की शुरुआत में वे महमूद गज़नवी के साथ एक आक्रमण के दौरान में भारत आए। कहा जाता है कि वे एक बार बहराइच के जंगलों में शिकार खेलने के लिए आए थे, तब स्थानीय लोगों ने उनसे संपर्क किया और उनसे गुज़ारिश की कि वे उनके मुक्तिदाता के रूप में काम करें।
यह वही दौर था जब राजा सुहेलदेव राज कर रहे थे। लोकगाथाओं के मुताबिक, सुहेलदेव निरंकुश व अत्याचारी राजा था, जिससे जनता बहुत परेशान रहती थी। जब सुहेलदेव ने बाले मियां के बारे में सुना, तो उसने उनके ऊपर हमला किया तथा समूची सेना सहित बाले मियां को मार डाला। इस लड़ाई में सुहेलदेव भी मारा गया।
हालांकि गज़नवी के इतिहास में इस युद्ध कहीं वर्णन नहीं मिलता है। गाज़ी मियां की शोहरत इस वज़ह से फैली कि जब उनका मज़ार बना, तब उसमें जादुई शक्तियां सामने आयीं। स्थानीय आबादी यही मानती है कि हिंदू-मुस्लिम दोनों ही वहां प्रार्थना करके लाभान्वित होते हैं। बारहवीं शताब्दी तक सालार मसूद बाले मियां के रूप में एक संत के तौर पर प्रतिष्ठित हो गए थे और बहराइच में उनका दरग़ाह एक तीर्थस्थल बन गया था।
हालांकि गज़नवी के साथ उनका संबंध केवल बाद के स्रोतों में दिखाई देता है। उनकी जीवनी का मुख्य स्रोत सत्रहवीं शताब्दी की ऐतिहासिक कल्पित कथा ‘मिरात-ए-मसूदी’ है। इस संबंध में उर्दू की लेखिका क़ुर्रतुल ऐन हैदर अपने चर्चित उपन्यास ‘आग का दरिया’ में लिखती हैं– “किस तरह मूर्तिभंजक माने जाने वाले सेनापति मसूद गाज़ी पिछली दो शताब्दियों में बाले मियां के रूप में कोसल देश के निवासियों के लिए एक और देवता बन चुके थे। उनके मज़ार पर घी के चिराग़ जलाए जाते थे, उनके झंडे उठाए जाते थे और हर साल धूमधाम से उनकी बारात निकाली जाती थी।”
इसी के समानांतर बाले मियां को लेकर एक दूसरा विमर्श भी विद्यमान है। विशेष रूप से नब्बे के दशक में हिंदुत्व की राजनीति के उभार के बाद, जिसे सांप्रदायिक तत्वों ने सचेत तौर पर निर्मित तथा प्रचारित किया है। वे राजा सुहेलदेव की बात इस रूप में करता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की और विदेशी आक्रमणकारी मसूद से हिंदुओं को बचाया। हम आसानी से देख सकते हैं कि सुहेलदेव के मिथक को लेकर सांप्रदायिक युद्ध वाली स्मृतियों के निर्माण के दो मक़सद हैं। एक– पासियों का ब्राह्मणीकरण और दूसरा– इस्लाम के ख़िलाफ़ हिंदू इतिहास को अपनी सुविधा के हिसाब से निर्मित एवं विस्तारित करना, ताकि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो सके।
जबकि बाले मियां की शोहरत का प्रतिवाद करने के लिए आरएसएस व उसके सहयोगी संगठनों ने सुहेलदेव के नाम पर समानांतर मेलों के आयोजन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शुरू किया। अब सुहेलदेव की याद में कई कार्यक्रम किए जाते हैं। मसलन, कलश-यात्रा निकाली जाती है, यज्ञ किया जाता है, कुश्ती और रामकथा का आयोजन किया जाता है।
अब यह सब सियासत में बदल चुका है। वर्ष 2002 में ओमप्रकाश राजभर के नेतृत्व में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया गया। 2017 में इस पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और पूर्वांचल के इलाके में उल्लेखनीय सफलता भी हासिल कीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गाज़ीपुर जाकर राजा सुहेलदेव की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया था और उनके नाम पर ट्रेन भी चलाई गई थी।
सालार मसूद ऊर्फ बाले मिया को एक क्रूर व्यक्ति के तौर पर पेश करने के अलावा आरएसएस इस बात पर लगातार जोर देता है कि यह दरगाह कभी बालार्क ऋषि का आश्रम था। उनका कहना है कि “इस आश्रम और सूर्यकुंड को सालार ने तबाह कर दिया था।” ऐसे हिंदू, जो साझी संस्कृति और विरासत में यकीन रखते हैं, उन्हें हीन दिखाने के लिए संघ का यह भी दावा होता है कि हिंदू धर्म और राष्ट्र के मुक्तिदाता को हिंदुओं ने ही भुला दिया और उन्हें किसी विदेशी आक्रांता के काल्पनिक क़ब्र पर जाने एवं वहां प्रार्थना करने से कोई गुरेज नहीं है।
यहां इस बात को रेखांकित किया जाना जरूरी है कि माहौल को विषाक्त करने की संघ और आनुषंगिक संगठनों की तमाम कोशिशों के बावज़ूद इस मसले को लेकर स्थानीय लोगों में मौज़ूद आख्यान इसके बिल्कुल विपरीत है और इस आख्यान के मुताबिक सुहेलदेव खलनायक हैं और बाले मियां नायक। जरूरत इस बात की है कि पासी समाज के लोग आरएसएस की मंशा को समझें और पूर्वांचल की धरती पर आपसी प्रेम व भाईचारा बनाए रखें।
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in