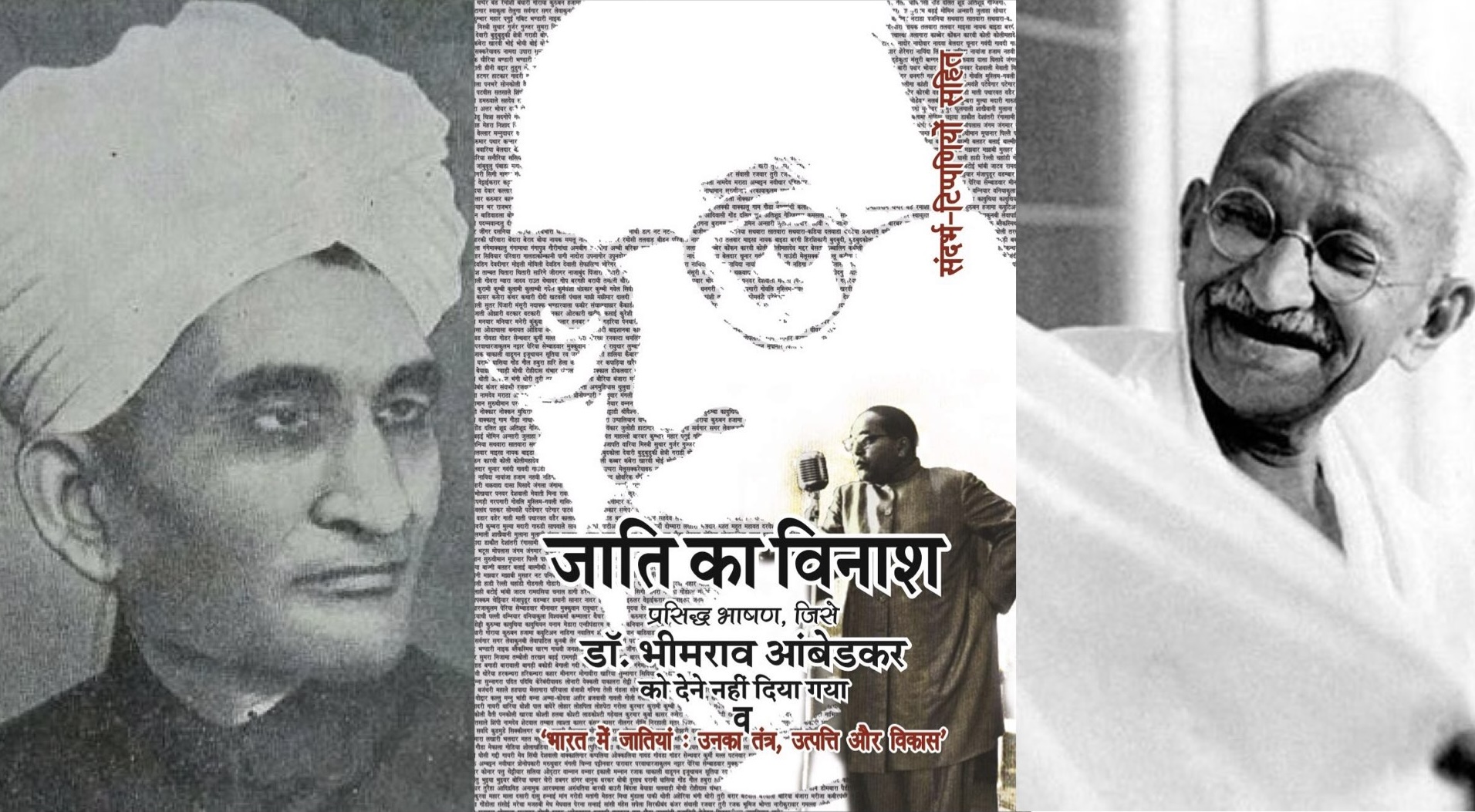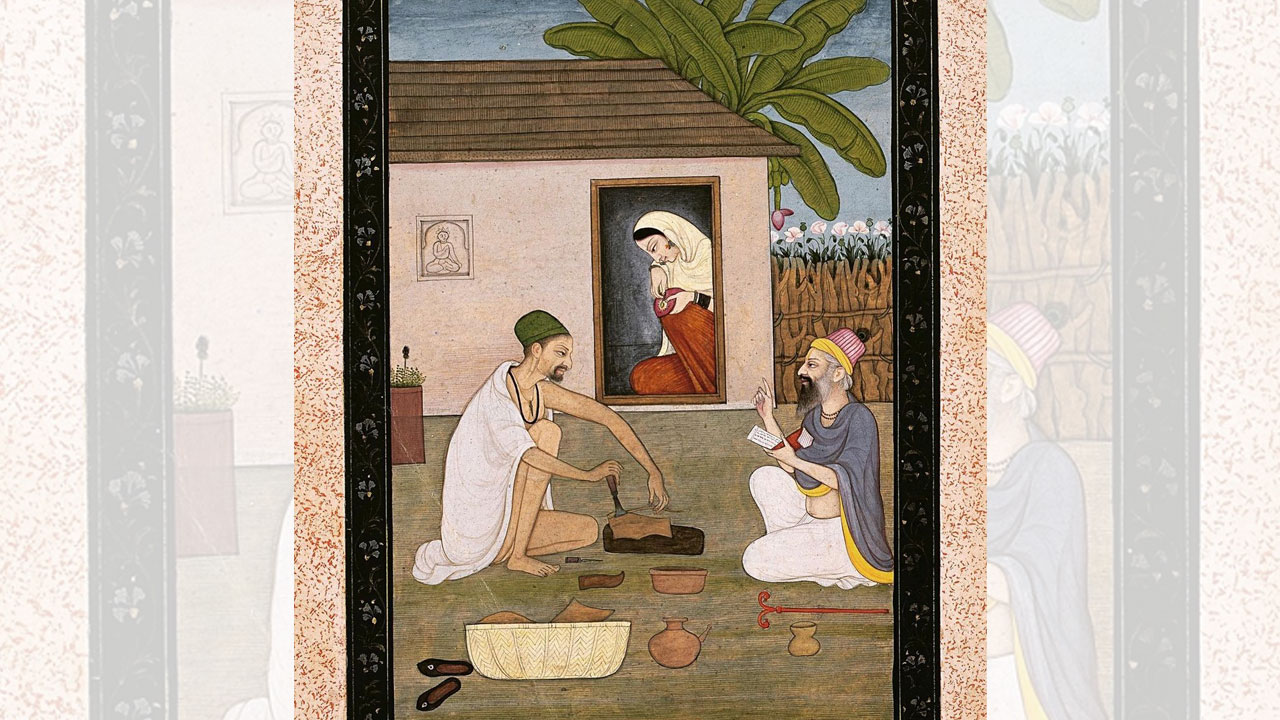सत्यशोधक समाज की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ (24 सितंबर, 1873) पर विशेष
महाराष्ट्र के पुणे को अहमदनगर से जोड़ने वाले राजमार्ग पर पुणे से लगभग 180 किलोमीटर दूर, अहमदनगर जिले के नेवासा तालुका में एक छोटा-सा गांव है– तारावाड़ी। यह दूरस्थ गांव कई मायनों में ख़ास है। पिछली सदी के शुरुआती दशकों में यह गांव देश को एक नई राह दिखाने वाले जोतीराव फुले के आंदोलन का गढ़ था। सत्यशोधक समाज ब्राह्मणों की प्रभुता का मुकाबला करते हुए हाशिए पर पड़े समूहों के उन्नयन के प्रति प्रतिबद्ध था। फुले के स्वयं के शब्दों में, ये समूह थे– स्त्री, शूद्र और अतिशूद्र। अतिशूद्र अर्थात अछूत।
तारावाड़ी की समृद्ध विरासत और इस तथ्य के बावजूद कि बचपन में मैंने कई छुट्टियां इस गांव से करीब 100 किलोमीटर से भी कम दूर अपने दादा के घर पर बिताईं। मैं तारावाड़ी पहली बार तब गया जब मैंने अपने शोध प्रबंध पर काम शुरू किया। इस गांव की मेरी पहली यात्रा अगस्त, 2021 में हुई। चश्मा लगाए और साफ़-सुथरी धोती पहने एक वयोवृद्ध सज्जन ने बड़ी उमंग से मेरा स्वागत किया। बयासी साल के उत्तमराव पाटील, ‘दीनमित्रकार मुकुंदराव पाटील अभिलेखागार एवं शोध केंद्र’ के एकमात्र कार्यवाहक हैं। मैं भारतीय भाषाओं में गैर-ब्राह्मण मुद्रित प्रकाशनों से संबंधित सामग्री इकठ्ठा करने वहां पहुंचा था।
मुकुंदराव पाटील, उत्तमराव के दादा थे। मुकुंदराव भारत के पहले ग्रामीण समाचार पत्र के संस्थापक और प्रमुख कर्ताधर्ता थे। इस अख़बार का नाम था– ‘दीनमित्र’। अर्थात दबे-कुचलों का दोस्त। मुकुंदराव ने 1910 में इस अख़बार का प्रकाशन शुरू किया था और 1967 में अपनी मृत्यु तक वे इसे निकालते रहे।
केंद्र के मुख्य कक्ष में मुकुंदराव के चित्र लगे हैं। साथ में, कुछ वरली पेंटिंग हैं और सत्यशोधक आंदोलन के सदस्यों के फ्रेम किये हुए फोटो भी। दो छोटे कमरों में मेरे जैसे शोधार्थी के लिए एक बड़ा खजाना है। यहां बीसवीं सदी की शुरुआत की किताबों, पत्रों, पुस्तिकाओं और पर्चों को बहुत सावधानी से संभाल कर रखा गया है। पतली से पतली पुस्तिका को भी प्लास्टिक के फोल्डरों में रख कर उसके ऊपर स्पष्ट लेबिल लगाए गए हैं। मुख पृष्ठ पर बड़े, काले अक्षरों में शीर्षक लिखे हैं।
उत्तमराव ने मुझे यह सब दिखाते हुए यह भी बताया कि किस प्रकार दूरदराज के गांवों में सत्यशोधक बैठकों में जाकर उन्होंने प्रदर्शित सामग्रियों को जमा किया है। वे उत्साह और उमंग से लबरेज और आपका स्वागत करने को आतुर दिखते हैं और केंद्र भी आपका स्वागत करता प्रतीत होता है। वहां सब कुछ आपकी पहुंच में है। यह बड़े शहरों के प्रतिष्ठित शोधकेंद्रों के औपचारिक और नियमों से बंधे वातावरण से एकदम अलग है। एक कोने में टेबल-कुर्सी, लैंप और फोटोकॉपी करने की मशीन है और दस्तावेजों को देखने-पढ़ने पर कोई रोक-टोक नहीं है। विद्यार्थी फटने की कगार पर पहुंच चुके नाजुक से नाजुक दस्तावेज को भी देख सकते हैं।

उत्तमराव एक कीमती विरासत के संरक्षक हैं। यह विरासत उस काल की है जब भारत के श्रेष्ठी वर्ग ने स्वाधीनता के बारे में अपनी सोच को अभिव्यक्त करने के लिए मुद्रित प्रकाशनों का उपयोग शुरू किया था। लेकिन स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में देश में एकमत नहीं था। मुकुंदराव पाटील और फुले जैसे लोग एक अलग तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था– हाशिए पर रखे गए समुदायों की निरक्षरता और निर्धनता की बेड़ियों से आज़ादी।
यही कारण है कि वे अक्सर अपने-आप को राजनीतिक स्वतंत्रता के पैरोकारों के विरुद्ध खड़ा पाते थे। राजनीतिक स्वतंत्रता के हामी वर्ग के लिए अंग्रेज़ दुश्मन थे। लेकिन सत्यशोधकों का नजरिया अलग था। वे जानते थे कि हाशिए पर रखे गए समुदायों के लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाले भारतीय नहीं, अंग्रेज़ थे।[1]
पाटील के लिए ऐसे राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं था, जिसमें समाज की अंतरात्मा, अछूत प्रथा और मानवाधिकारों के दमन से प्रदूषित हो।
यही कारण है कि ‘दीनमित्र’ ने देश के सच को लोगों के सामने रखा और मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलन के आख्यान को चुनौती दी। इसके लिए उसने एक अनूठा तरीका अपनाया। उसने स्थानीय भाषा में ऐसी पत्रकारिता की, जो घोषित रूप में, ताल ठोंक कर एक विशिष्ट सोच की समर्थक थी, और इस अर्थ में शहरों की तथाकथित निष्पक्ष और तथ्य-आधरित पत्रकारिता की विरोधाभासी थी।
पाटील उन आखिरी सत्यशोधकों में से एक थे, जिनके लिए धार्मिक और सामाजिक मसले, राजनीतिक मसलों से ज्यादा अहम थे। उनका समाचार पत्र उस काल के राष्ट्रवादी प्रकाशनों की समालोचना करता था। इनमें शामिल थे– बालगंगाधर तिलक के प्रसिद्ध समाचार पत्र ‘केसरी’ और ‘मराठा’, जो होमरूल और गणेशोत्सव जैसे सामुदायिक आयोजनों के बारे में लेखन को प्राथमिकता देते थे।
बी.आर. आंबेडकर द्वारा हिंदू धर्मग्रंथों और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों की गहन समालोचना के दो दशक पहले, पाटील ने लिखा था कि ब्राह्मण पुरोहित वर्ग “हिंदू धर्म का पहले नंबर का दुश्मन है।” वे स्वयं एक गैर-ब्राह्मण हिंदू थे और अपने पिता, जो फुले के निकट सहयोगी थे[2], की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे।
उनका ‘दीनमित्र’ एक ऐसे दौर में हाशियाकरण के सबसे अधिक शिकार वर्ग का कामरेड था, जब जोर-ज़बरदस्ती से लागू अछूत प्रथा के चलते, अछूत सामाजिक परिदृश्य से लगभग अदृश्य थे। ‘दीनमित्र’ और अन्यत्र प्रकाशनों में अपने लेखन के ज़रिए उन्होंने – राष्ट्र कैसा हो सकता है और उसे कैसा होना चाहिए – इस बारे में समाज पर हावी परंपरावादी और प्रभुत्वशाली सोच को चुनौती दी।
शुरुआत
मुकुदंराव के पिता कृष्णराव भालेकर की फुले से पहली मुलाकात 1868 में हुई थी। भालेकर उस समय 18 वर्ष के थे और पहले से ही “पाखंडी ब्राह्मणों द्वारा सीधे-साधे और निरक्षर लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाने” के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते आ रहे थे।
उस समय, ब्राह्मणों द्वारा संचालित अनेक प्रकाशन अस्तित्व में आ चुके थे। उनमें से एक था– मासिक ‘निबंधमाला’, जिसके संचालक प्रभावशाली मराठी पद्य लेखक विष्णुशास्त्री चिपलूणकर थे। चिपलूणकर अपने प्रकाशनों में अक्सर फुले का मज़ाक बनाते थे। एक बार उन्होंने फुले को “मानवता का लबादा ओढ़े घटिया कलमघसीट” बताया था।[3]
फुले के ब्राह्मणवाद-विरोधी लेखन और वैदिक परंपराओं की फुले की समालोचना पर निशाना साधते हुए वे अक्सर फुले की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का मखौल बनाते थे और उन्हें ‘शूद्र जगद्गुरु’ और ‘शूद्र धर्मसंस्थापक’ बताते थे।[4]
भालेकर देख रहे थे कि ब्राह्मण, मुद्रित प्रकाशनों के ज़रिए अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और अपने विचारों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। पूना पुस्तकालय में ब्राह्मणों द्वारा संचालित ‘लोककल्याणएच्छु’ और ‘ज्ञानचक्षु’ जैसे समाचार पत्रों को पढ़ते हुए उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि वे अपना स्वयं का समाचार पत्र निकालेंगे। उन्होंने सन् 1877 में, तिलक द्वारा ‘केसरी’ और ‘मराठा’ के प्रकाशन के चार साल पहले, ‘दीनबंधु’ का प्रकाशन प्रारंभ किया।
सत्यशोधक आंदोलन के पहले समाचार पत्र ‘दीनबंधु’ की शुरुआत बहुत साधारण थी। उसके केवल 13 वार्षिक ग्राहक थे। सन् 1880 तक वार्षिक ग्राहकों की संख्या बढ़कर 320 हो गयी थी। समाचार पत्र के एक अंक की कीमत चार आना हुआ करती थी।[5]
‘दीनबंधु’ का प्रकाशन पूना से होता था और उसे बंबई के समृद्ध गैर-ब्राह्मणों का सहयोग मिलता था। दो तेलुगू भाषियों, बालाजी कलेवार और राम्या वेंकाया ऐय्यावरु ने भालेकर के विचारों से प्रभावित होकर उन्हें 1,200 रुपए में एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद कर दी।
यह एक नई शुरुआत थी। इसके पहले तक केवल उच्च जातियों के लोगों को अपना अख़बार शुरू करने के लिए सामाजिक और आर्थिक पूंजी उपलब्ध हो पाती थी। जातिगत मसलों के प्रति संवेदनशील प्रकाशनों ने सत्यशोधक लेखकों, संपादकों, कवियों और उपन्यासकारों की एक पूरी पीढ़ी को जन्म दिया। सन् 1873 और 1930 के बीच, सत्यशोधक आंदोलन के सिद्धांतों के प्रति समर्पित करीब 60 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें से अधिकांश की नींव 1920 के दशक में रखी गई।
आने वाले वर्षों में पश्चिमी भारत देश का पहला ऐसा हिस्सा बना, जहां जाति-विरोधी लेखन शुरू हुआ। इसके बाद पंडिथार इयोथी थास्सर, नारायण गुरु और भीमा भोई ने क्रमशः तमिलनाडु, केरल और ओडिशा में इसी विषय पर लेखन शुरू किया।
आंदोलन और समाचार पत्र को बचाए रखने के लिए भालेकर ने अपने भांजे, अपनी बहन काशीबाई के लड़के, गणपतराव को अपने बाद समाचार पत्र की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार करना शुरू किया। दोनों मिलकर पूना के मंगलवार और बुधवार पेठ इलाकों में सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करते थे, जिनमें वे ब्राह्मणों द्वारा बहुजन समाज के दमन पर अपने विचार लोगों के सामने रखते थे।
सन् 1888 में गणपतराव ने अपनी स्वयं की पत्रिका शुरू की, जिसका नाम ‘दीनमित्र’ था। लेकिन यह पहला ‘दीनमित्र’ पांच साल बाद ही बंद हो गया, क्योंकि गणपतराव मात्र 27 वर्ष की वय में कालकवलित हो गए। भालेकर ने अपनी व्यथित और दुखी बहन को उनके पुत्र मुकुंदराव को गोद लेने के लिए राजी कर लिया। नेवासा, अहमदनगर के पाटील परिवार, जिसने मुकुंदराव को गोद लिया, ने उन्हें उनका नया उपनाम दिया– पाटील।
‘दीनबंधू’ आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। भालेकर का एक अन्य प्रकाशन ‘शेतकार्यांची कैवरी’ अर्थात ‘किसानों का रक्षक’ भी था और वह भी आर्थिक संकट में था। इस दौरान, भालेकर एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहे। वे किसी ऐसी नौकरी की तलाश में थे, जिसकी मदद से वे अपने विचारों के प्रसार के काम को जारी रख सकें। यह भी एक कारण था, जिसके चलते युवा मुकुंदराव अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके। आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों ने भालेकर को तोड़ दिया और 1910 में वे लकवाग्रस्त हो गए और इस दुनिया से चले गए। ऐसा बताया जाता है कि भालेकर जब मृत्यु शैय्या पर थे तब उन्होंने अपने पुत्र को यह कसम दिलवाई कि वह कम से कम 12 साल तक समाचार पत्र का प्रकाशन जारी रखेगा।
मुकुंदराव, जिन्होंने केवल दूसरी कक्षा तक शिक्षा हासिल की थी, अपने पिता से किए वायदे को पूरा करना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह अहसास था कि बंबई और पूना जैसे ब्राह्मण-वर्चस्व वाले शहरों में उनके लिए अपने पिता के अख़बार का प्रकाशन जारी रखना खासा मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने तारावाड़ी, जहां उन्हें उनके पिता से उत्तराधिकार में करीब 70 एकड़ भूमि मिली थी, में बसना तय किया। उन्होंने अपने ससुर रानोजी रावजी आरू, जो बंबई स्थित निर्णय सागर प्रेस के चेयरमैन थे, की मदद से एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी।
‘दीनमित्र’ को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करवाने के लिए पाटील को तारावाड़ी से करीब 60 किलोमीटर दूर अहमदनगर की अनेक कठिन यात्राएं पैदल करनी पड़ीं। उस समय इस दूरी को तय करने का एकमात्र तरीका बैलगाड़ी से सफ़र करना था, जिससे यह यात्रा लगभग दो दिन में पूरी हो पाती होती थी। लेकिन पाटील ने इस यात्रा को पैदल चलकर पूरा करना तय किया। वे भोर में घर से निकल जाते थे ताकि कार्यालयीन समय में अहमदनगर पहुंच कर कलेक्टर से मिल सकें।

उनके पुत्र माधवराव पाटील ने बाद में लिखा कि ब्राह्मण नौकरशाही ने न केवल मुकुंदराव के अख़बार को पंजीकृत करने में आनाकानी की, बल्कि उनकी राह में रोड़े भी अटकाए। पाटील ‘दीनमित्र’ के पीर-बावर्ची-भिश्ती-खर सब थे। वे उसमें लिखते थे, स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों से विज्ञापन हासिल करते थे, अख़बार छापते थे और उसकी प्रतियों को डाकघर भी ले जाते थे। उनका अखबार ग्रामीण, गैर-ब्राह्मण लोगों तक पहुंचने वाला देश का पहला प्रकाशन था। ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीण भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। और यह सब उन्होंने केवल 25 साल की उम्र में किया।
महत्वाकांक्षी
सत्यशोधक अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाशा जैसे परंपरागत दृश्य-श्रव्य माध्यमों और गोंधल, जागरण और दशावतार जैसे क्षेत्रीय लोकसंगीत माध्यमों का प्रयोग कर सकते थे। इनके श्रोताओं और दर्शकों की संख्या अच्छी-खासी हुआ करती थी और इनके ज़रिए निरक्षर लोगों तक भी अपना संदेश पहुंचाया जा सकता था। लेकिन मुद्रित प्रकाशनों की क्रांतिकारी संभावनाओं के मद्देनजर उन्होंने सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद समाचार पत्र निकाले।
जहां तिलक के ‘केसरी’ और ‘मराठा’ का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को लोगों तक पहुंचाना था, वहीं भालेकर के ‘दीनबंधु’ और मुकुंदराव के ‘दीनमित्र’ का फोकस एक क्षेत्र विशेष पर था। दोनों प्रकाशनों के संस्थापकों को ब्राह्मणों और सत्यशोधकों के बीच के रोजमर्रा के सामाजिक-सांस्कृतिक तनावों और टकरावों की गहरी समझ थी और यह उनके प्रकाशनों में भी प्रतिबिंबित होती थी। भालेकर और पाटील के लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग करना नहीं था। वे मुद्रित प्रकाशनों का उपयोग वैकल्पिक विचारों और दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करने के लिए करते थे।
पाटील को लेखन और पठन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। ‘दीनमित्र’ की पुनः शुरूआत करने के बाद उन्होंने मुद्रित प्रकाशनों की दुनिया को समझना शुरू किया। उन्होंने स्वाध्याय से अंग्रेजी सीखी और रेवरेन्ड आर.एन. तिलक नामक सज्जन की मदद से संस्कृत का ज्ञान हासिल किया। अपने नवअर्जित ज्ञान की दम पर पाटील न केवल संपादकीय लिखने लगे वरन् उन्होंने उपन्यास, खंडकाव्य, लेख, लघुकथाएं और व्यंग्य भी लिखना शुरू कर दिया। सन् 1910 में ‘दीनमित्र’ के पहले अंक के प्रकाशन के समय से ही पाटील ने शेठजी-भट्टजी-लाटजी (जमींदार, पुरोहित और औपनिवेशिक सरकार के कर्मचारी) की ब्राह्मणवादी त्रिमूर्ति पर निशाना साधने के लिए लेखन की विभिन्न विधाओं का उपयोग किया।
इसके चलते ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र दोनों क्षेत्रों के पाठक इस प्रकाशन की ओर आकर्षित हुए। ‘दीनमित्र’ के पहले वर्ष के अंकों की तीन-चार हजार प्रतियों को करीब 600 पाठकों ने पढ़ा। अखबार का वार्षिक चंदा केवल तीन रुपए था और छःह महीने तक अखबार खरीदने के लिए मात्र दो रुपए देने होते थे। कई अन्य अखबारों का मूल्य भी इसके आसपास था लेकिन साल-दर-साल ‘दीनमित्र’ के पाठकों की संख्या इसलिए बढ़ती रही, क्योंकि वह उस दौर में सत्यशोधक आंदोलन के सिद्धांतों की वकालत करने वाले चंद अखबारों में से एक था।
अखबार के वितरण के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार की गई, जिससे वह पूना, बंबई, औरंगाबाद, अमरावती, खानदेश, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, बड़ौदा, परभनी, नांदेड़, जबलपुर, बेलगाम और नागपुर में पाठकों तक पहुंचने लगा। आंदोलन का कोई समर्थक जब पश्चिमी भारत से अन्यत्र रहने चला जाता था तब उसे अखबार डाक के जरिए भेजा जाता था। इस तरह ‘दीनमित्र’ लाहौर, अंडमान द्वीप समूह, सिंगापुर और श्रीलंका तक पहुंचा।
तारावाड़ी से प्रकाशित इस छोटे से समाचार पत्र की इतनी जबरदस्त उन्नति अनापेक्षित थी। बहुत कम लोगों को यह उम्मीद थी कि एक ब्राह्मण-विरोधी अखबार, जिसमें खबरों की जगह केवल राय व्यक्त करने वाले लेख होते थे और जो केवल स्थानीय पाठकों को संबोधित करता था, इतना सफल हो सकता है। ब्राह्मणों ने बिना देर किए इस अखबार पर हल्ला बोल दिया।
‘दीनमित्र’ एक टीन की छत वाले एक अस्थाई मकान से प्रकाशित होता था, जो पाटील को उत्तराधिकार में प्राप्त शुष्क कृषि भूमि पर बना हुआ था। स्थानीय ब्राह्मणों ने पाटील के खिलाफ इस आरोप में मुकदमा दायर कर दिया कि वे कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग कर रहे हैं। ‘दीनमित्र’ को इस तरह के अनेक मुकदमों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसकी विज्ञापन से आमदनी प्रभावित हुई (अखबार के प्रथम पृष्ठ पर होटलों, दवाईयों, किताबों, साईकिल की दुकानों और कृषि उपकरणों के विज्ञापन प्रकाशित होते थे)।
लेकिन सारी मुसीबतों के बाद भी पाटील ने हार नहीं मानी। उनके लिए यह अखबार ही उनका अस्तित्व, उनकी जिंदगी थी। संपादकीय लेखों के अतिरिक्त पाटील ‘दीनमित्र’ में लघुकथाएं, कविताएं और व्यंग्य भी प्रकाशित करते थे। सन् 1910 से 1930 के बीच उन्होंने चार उपन्यास लिखे, जो पहले ‘दीनमित्र’ में किश्तों में प्रकाशित हुए। ये सारे उपन्यास ब्राह्मण पुरोहितों की लोभी प्रवृत्ति पर केंद्रित थे और उनके पितृसत्तात्मक नजरिए का पर्दाफाश करते थे।
उदाहरण के लिए ‘हिंदू अणि ब्राह्मण’ में पाटील ने हिंदू धर्म से ब्राह्मणवाद को निकाल बाहर करने के पक्ष में तर्क दिये। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों ने किस तरह स्थानीय राजाओं और व्यापारियों को मूर्ख बनाया और धर्मग्रंथों को अपनी सोच से प्रदूषित करने के लिए उनमें बाद में सामग्री जोड़ी। इस उपन्यास का कुछ हिस्सा ‘दीनमित्र’ के शुरुआती अंकों में किश्तों में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अन्य उपन्यासों जैसे ‘होली ची पोली’ और ‘धा धा शास्त्री पराणे’ को भी ‘दीनमित्र’ में किश्तों में प्रकाशित किया गया।[6]
यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो विचार प्रतिपादित किए जा रहे हैं, वे पाठकों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं, उन्हें कुछ समयांतर से अलग-अलग मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित किया जाता था। जैसे जो सामग्री पहले ‘दीनमित्र’ में प्रकाशित होती थी, उसे बाद में पुस्तकों, पर्चों और छोटी पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किया जाता था। उत्तमराव पाटील आज भी इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। वे मुकुंदराव की लघुकथाओं, उपन्यासों और भाषणों पर आधारित कई छोटी पुस्तिकाएं संपादित कर रहे हैं। इसके साथ ही वे कुछ शोधार्थियों के साथ मिलकर ‘दीनमित्र’ के सभी संपादकीय लेखों को प्रकाशित करने का उपक्रम किया हैं।[7]
मुकुंदराव की काव्य रचनाएं भी उतनी ही प्रभावी थीं। ‘कृष्ण लीलामृत’ और ‘शेठजी प्रधान’ में यह बताया गया है कि किस तरह औपनिवेशिक शासकों द्वारा लगाए गए कमरतोड़ टैक्सों और स्थानीय ब्राह्मणों की कारगुजारियों के चलते किसान दमन और शोषण का शिकार हो रहे हैं। इन दोनों किताबों में यह दिखाया गया है कि किस तरह गांवों के पारंपरिक लेखाधिकारी कुलकर्णी गरीब और अनपढ़ किसानों की जमीनों को जब्त कर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। इनमें से कुछ पुस्तकों के प्रकाशन में बीसवीं सदी की शुरुआत में कोल्हापुर के राजा रहे शाहू जी का सहयोग भी था। वे सत्यशोधक आंदोलन के एक प्रभावशाली प्रशंसक थे, लेकिन खुलकर सामने आना नहीं चाहते थे।[8]
पाटील के अनवरत प्रयासों के चलते कुलकर्णी के पद पर नियुक्ति का आधार पैतृकता के स्थान पर योग्यता को बनाने के पक्ष में जनमत तैयार हुआ। सन् 1915 में पाटील ने बांबे प्रेसिडेंसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भास्करराव जाधव के साथ मिलकर यह मांग करते हुए एक याचिका तैयार की।
ऐसा बताया जाता है कि पाटील ने अपने खर्च पर इस याचिका की दस हजार प्रतियां छपवाईं और उनके ऊपर इस परिवर्तन के समर्थकों के हस्ताक्षर करवाकर पूरे बंडल को गवर्नर के पास भिजवाया।[9]
उनके प्रयासों का तुरंत कोई नतीजा तो नहीं निकला, परंतु स्वतंत्रता के बाद बनाए गए बंबई परगना एवं कुलकर्णी वतन (उन्मूलन) अधिनियम, 1950 जैसे कानूनों की नींव में उनका अभियान ही था।
चुनौती
सन् 1906 में पाटील ने पहली बार किसी बड़े सार्वजनिक आयोजन में हिस्सा लिया। कुछ ब्राह्मण वकील और सामाजिक नेता इस बात पर अफसोस जाहिर कर रहे थे कि धन की कमी के कारण वे अछूत किसानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सभा के बीच में केवल 21 साल के मुकुंदराव ने खड़े होकर जोर से यह पूछा कि फिर उनके पास भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए पैसा कहां से आ रहा है?
ब्राह्मणों को तब बहुत धक्का लगा जब पाटील ने उन सत्यशोधकों का समर्थन किया, जो किसी दूसरे धर्म को अपनाने के पक्ष में थे। पाटील ने ‘दीनमित्र’ में लिखा “अगर कोई नया धर्म अपनाने से आप लोगों को मूलभूत मानवाधिकार हासिल हो सकते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए।
“आखिर कितने दिन तक आप कीड़े-मकोड़ों और चींटियों जैसी जिंदगी जीते रहेंगे? अगर कोई कुत्ता खाने के लालच में किसी ब्राह्मण के घर में घुस जाता है तो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे लोगों को वे कुत्ते से भी निम्न मानते हैं। आप वहीं जाइए और वहीं रहिए, जहां आपके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाता है। वह हिंदू धर्म हो सकता है या ईसाई धर्म। हिंदू धर्म के असली दुश्मन ब्राह्मण पुरोहित हैं। हिंदुओं के दूसरे धर्मों को अपनाने के लिए ब्राह्मण समुदाय जिम्मेदार है।”[10]
पाटील राजनैतिक श्रेष्ठि वर्ग, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर रहा था, की सोच की खिलाफत करते थे। उन्हें पता था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का सत्यशोधकों के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें शिक्षा तक पहुंच अंग्रेजों ने ही दिलवाई है। पाटील का कहना था कि ब्रिटिश शासन ने गैर-ब्राह्मणों को गरिमा से जीने का और अपना व्यवसाय चुनने का हक दिलवाया है और उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलवाई है।
शायद यही कारण है कि पाटील ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज और उनकी पत्नी मैरी, जिनका बंबई में 1911 में अत्यंत शानोशौकत से स्वागत किया गया था, की तारीफ़ करते हुए लेख लिखा था।
उन्होंने दिसंबर, 1911 में लिखा, “जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ धोखा किया, वे खुश नहीं होंगे।। लेकिन जिन लोगों ने इस सरकार में मानवीय गरिमा का स्वाद लिया है, जो उन्हें रामराज में भी हासिल नहीं थी, वे इस समारोह से बहुत प्रसन्न होंगे।”
बल्कि पाटील को तो इस बात पर अफ़सोस था कि ब्रिटिश भारत में देर से आए। उनके अनुसार अंग्रेजों द्वारा भारत को आधुनिक सुविधाएं जैसे सड़कें, रेलवे, कारखाने और जहाज़ उपलब्ध करवाने से गैर-ब्राह्मणों को सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ने के मौके मिले। इसके अलावा, उन्होंने अपने पाठकों को यह भी ध्यान दिलाया कि सम्राट जॉर्ज की दादी विक्टोरिया ने सन् 1835 में गुलामों का व्यापार ख़त्म करने के लिए अपने खजाने से 22 करोड़ रुपए खर्च किये थे।
पाटील का विदेशी शासकों का समर्थन, तिलक जैसे मराठी राष्ट्रवादियों की प्रत्यक्ष खिलाफत थी। यह एक बंधुत्व की प्रधानता वाले राष्ट्र का विरोध था। पाटील शिव जयंती और गणेश जयंती जैसे राष्ट्रवादी उत्सवों को भी नापसंद करते थे। तिलक के प्रयासों से गणेश उत्सव, राष्ट्रवाद का सार्वजनिक ब्राह्मणवादी स्वरूप बन गया था। पाटील ने मई, 1911 में लिखा, “गणपति उत्सव, शराब पर प्रतिबंध आदि को हानिरहित बताया जाता है। लेकिन इनके ऊपर धर्म का केवल लबादा है और इस लबादे के अंदर राजनीतिक मुद्दों की उछल-कूद और धींगामस्ती है। ढोंग के इतने उदाहरण हम देख रहे हैं। यह उनमें एक नहीं है, ऐसा कौन कह सकता है?”
पाटील की दृष्टि में इन आयोजनों का उद्देश्य ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों के बीच खुले दिल से विचार-विमर्श को संभव बनाना कभी नहीं था। पाटील ने तिलक और ‘केसरी’ को अनेक बार खुली चर्चा करने की चुनौती दी, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया गया। ‘केसरी’ लगातार ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों के बीच की खाई को ढांपने का प्रयास करता रहा। वह गैर-ब्राह्मण आंदोलन को ब्राह्मणों से नफरत करने वालों का आंदोलन बता कर बदनाम करता था। उसका कहना था कि गैर-ब्राह्मण आंदोलन, केवल मराठा समुदाय के भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधि है।
यह सच है कि इस आंदोलन के कई प्रमुख नेता मराठा थे। लेकिन पाटील ने अपने कई संपादकीय लेखों में इस आख्यान को चुनौती दी और अपने पाठकों को याद दिलाया कि इस आंदोलन में महार, मांग, चम्भर, कुम्भर, नाह्वी (नाई), पारित, सली, कोष्टी, शिम्पी, सुनार, लोहार, सुतार, कसार, धनगर, कोली, रामोशी, भिल्ला और मेल जैसे समुदायों के अतिरिक्त, जैन, लिंगायत और प्रभु भी शामिल हैं। अक्तूबर, 1913 में प्रकाशित एक संपादकीय में ‘केसरी’ की आलोचना का जवाब देते हुए पाटील ने लिखा कि “सत्यशोधक समाज का संस्थापक मराठा नहीं था और ना ही ‘कुलकर्णी लीलामृत’ पुस्तक का लेखक मराठा था।[11] और कोल्हापुर में आंदोलन का प्रमुख नेता प्रभु है, उपाध्यक्ष जैन है और सचिव धनगर है।”
पाटील हमेशा तिलक और ‘केसरी’ पर कड़ी नज़र रखते था। इसका एक उदाहरण महत्वपूर्ण है। सन 1916 में तिलक ने अहमदनगर में अपनी प्रसिद्ध उद्घोषणा की, “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पा कर रहूंगा।”
लेकिन इसी सभा में उन्होंने गांवों के कुलकर्णीयों को उनकी अनुवांशिक संपत्ति – वतन – से वंचित किये जाने पर अपनी असहमति भी जाहिर की। यह गांवों में भूमि के स्वामित्व और उसके वितरण पर ऊंची जातियों के नियंत्रण के अधिकार की वकालत थी। पाटील ने चार साल पहले, ‘कुलकर्णी लीलामृत’ में लिखा था, “वतन के समाप्त होने का अर्थ था ब्राह्मणों के प्रभुत्व का अंत। पर इस स्थिति में बढई, नाई और दर्जियों के बारे में कौन बात करेगा।”
तिलक के जातिवादी दृष्टिकोण की आगे और परीक्षा हुई। लगभग उसी समय, महर्षि शिंदे द्वारा अछूत प्रथा के निवारण की मांग करते हुए तैयार की गई एक याचिका चर्चा में थी। तिलक ने इस याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किये। इसके बारे में लिखते हुए पाटील ने कहा कि तिलक स्वराज हासिल करने के तो बहुत इच्छुक हैं, लेकिन वे जाति के प्रश्न पर स्पष्ट बात नहीं करते। सन 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद भी, तिलक के प्रभाव के बने रहने की, वे आलोचना करते रहे। उन्होंने लिखा कि किस प्रकार जिस व्यक्ति को ‘लोकमान्य’ की पदवी दी गई और जिसके लोग प्रशंसक है, उसने कभी विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और अछूत प्रथा के उन्मूलन की बात नहीं कही।
पाटील ने तिलक के राष्ट्रवाद की सबसे तीखी आलोचना, होमरूल आंदोलन पर लिखे अपने संपादकीय लेखों में की। उन्होंने लिखा कि होमरूल आंदोलन के पैरोकारों को राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करते हुए शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित जिन अन्य देशों में औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, वहां के समाजों में धार्मिक एकता है। वे सब ऐसे धर्म में आस्था रखते हैं, जो सभी मनुष्यों को बराबरी का दर्जा देता है। ऐसे राष्ट्र की मांग करना नितांत अनऔचित्यपूर्ण है, जो अछूत प्रथा जैसी बुराइयों से निपटना नहीं चाहता। उन्होंने मांग की कि ऊंची जातियों को पहले गैर-ब्राह्मणों को ‘लघु होमरूल’ देना चाहिए और फिर अंग्रेजों से ‘वृहद् होमरूल’ की मांग करनी चाहिए।
पाटील ने भविष्यवाणी की कि अपने वर्तमान स्वरूप में होमरूल केवल ‘राष्ट्र’ के विद्यमान आख्यान को पोषित करेगा और एक ‘नए राष्ट्र’ को जन्म नहीं देगा। यह महत्वपूर्ण है कि फरवरी 1917 में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख में पाटील ने अविभाजित राष्ट्र की तुलना एक विशाल पेड़ से की। “मैं इस बात से सहमत हूं कि होमरूल, राष्ट्र-वृक्ष के लिए पोषक खाद है, लेकिन ऐसा होने के लिए सबसे पहले राष्ट्र को राष्ट्र-वृक्ष बनना होगा।
“राष्ट्र-वृक्ष के जन्म लेने के लिए यह ज़रूरी है कि वह एक अविभाजित बीज से उत्पन्न हो। इससे एक जाति का राष्ट्र जन्म लेगा और जब उसे होमरूल की खाद मिलेगी तो उसके (राष्ट्र) सभी हिस्से मज़बूत बनेंगे और उसमें मीठे फल लगेंगे। मगर क्या हिंदुस्तान में हमारे पास एक जाति का राष्ट्र-वृक्ष है? हिंदुस्तान में कई जातियों के वृक्ष हैं। फिर यह एक प्रकार की खाद, किस तरह विभिन्न जातियों के लोगों के लिए फलप्रद होगी।”
पाटील ने होमरूल लीग की संस्थापक एनी बेसेंट को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा कि एनी बेसेंट का कहना है कि “अछूत बच्चों को पहले शिष्टाचार सिखाया जाना चाहिए ताकि जब वे ऊंची जातियों के संपर्क में आएं तो ऊंची जातियों के लोगों को शारीरिक क्षति न पहुंचे।” जनवरी, 1915 में प्रकाशित एक संपादकीय में पाटील ने बिना किसी लाग-लपेट के एनी बेसेंट के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित किया– “बेसेंट एक महार और एक ब्राह्मण के बीच अंतर कैसे करेंगीं? क्या वे उनकी आत्माओं में भेद कर सकती हैं?”
सन् 1967 में पाटील की 82 साल की उम्र में मृत्यु के बाद, ‘दीनमित्र’ का प्रकाशन बंद हो गया। नई पीढ़ी के पाठकों से ‘दीनमित्र’ का परिचय हाल में हुआ है। वर्ष 2022 में उत्तमराव पाटील ने अपने दादा के सभी संपादकीय लेखों का संग्रह दस खंडों में प्रकाशित किया है।
मुकुंदराव पाटील उन चंद सत्यशोधकों में से थे, जिनका मिशन औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ और औपनिवेशिक काल के बाद भी जारी रहा, जिन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने अपने समाचार पत्र को प्रतिरोध का उपकरण बनाया। वे एक अनूठे पत्रकार थे, जिनमें साहित्यिक प्रतिभा भी थी और एक तरह की चतुरता भी, जो उनकी दार्शनिक अभिरुचि से उपजी थी।
बीसवीं सदी के दूसरे दशक से देश में राजनीतिक जागृति बढ़ती गई। इसी के साथ राष्ट्र और राष्ट्रवाद के संबंध में पाटील के विचारों में राजनीति और समाज को जोड़ने वाले कड़ी की परिकल्पना और स्पष्ट होती गई। भारत के स्वाधीनता संघर्ष के राष्ट्रवादी जनांदोलन बनने के दौर से पहले पाटील ने लिखा था कि देशभक्ति भी हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है।
“अपने देश पर गर्व करना, स्वार्थपरता से होने वाले हानि को समझना और होमरूल जैसी आधुनिक संस्थाओं के निर्माण का विचार – देशभक्ति की इस कला से हमारा परिचय अंग्रेजों के साथ रहने से ही हुआ है। कई लोग मेरे इस कथन से नाराज़ होंगें और पूछेंगे कि क्या अंग्रेजों के आने से पहले हममें देशाभिमान, देशभक्ति और देशउन्नति के भाव नहीं थे? उन्हें मैं साफ़-साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि हां! अंग्रेजों के पहले आप नहीं जानते थे कि अपने देश पर गर्व करना क्या होता है।”
इस तरह के लेखन से यह साफ़ है कि पाटील जैसे अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों द्वारा प्रतिपादित विचार, व्यापक रूप से स्वीकार्य आख्यानों की पुनर्व्याख्या कर सकते हैं। एक ऐसे दौर में जब भारत के अतीत की सभ्यागत महानता और गौरव का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, पाटील जैसे व्यक्तियों की सोच देश को एकसार बताने और बनाने के प्रयासों के प्रतिरोध में भूमिका अदा कर सकती है।
संदर्भ :
[1] यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ‘सत्यशोधक आंदोलन’ और ‘गैर-ब्राह्मण आंदोलन’ एक नहीं थे। ‘गैर ब्राह्मण आंदोलन’ शब्द सन् 1916 में मद्रास प्रेसीडेंसी में जस्टिस पार्टी की स्थापना के बाद आम बोलचाल में आया। मुकुंदराव पाटील ने कभी औपचारिक रूप से राजनीति में भाग नहीं लिया। इसके अलावा मैंने ‘गैर-ब्राह्मण आंदोलन’ की जगह ‘सत्यशोधक आंदोलन’ शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, क्योंकि इस लेख का फोकस 1920 के पूर्व के काल पर है। मैंने ‘गैर-ब्राह्मण’ शब्द का प्रयोग केवल व्यक्तियों और समुदायों के लिए किया है, आंदोलन के लिए नहीं – लेखक
[2] समाजशास्त्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता गेल ऑम्वेट ने लिखा है कि यद्यपि पाटील “धनी किसानों के प्रवक्ता थे” तथापि यह तर्क दिया जा सकता है कि “कम-से-कम इस दौर में, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके हित, आमजनों के हितों और काफी हद तक अछूतों और मुसलमानों जैसे विशिष्ट अल्पसंख्यक समूहों की ज़रूरतों से जुड़े हुए थे।” (‘कल्चरल रिवोल्ट इन ए कोलोनियल सोसाइटी: द नॉन-ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया’, 2019, मनोहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स)
[3] वाय.डी, फड़के, ‘वी. के. चिपलूणकर’, नेशनल बुक ट्रस्ट, 1982, पृ. 44
[4] आर.के. लेले, ‘मराठी वृत्त पत्रांचा इतिहास’, कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, तृतीय संस्करण, पुणे, 2009, पृ. 199
[5] अरुण शिंदे, ‘सत्यशोधक नियतकालिके’, कृष्ण संशिधान व विकास अकादमी, सोलापुर (2019), पृष्ठ 107
[6] यह दिलचस्प है कि अपने पिता भालेकर के बाद, पाटील ऐसे दूसरे सत्यशोधक थे जिसने साहित्यिक एवं सामाजिक समालोचना के लिए उपन्यास की विधा का इस्तेमाल किया। जोतीराव फुले के वाङ्गमय में उपन्यास नहीं हैं। इसके पीछे के कारण क्या था यह कहना कठिन है। फुले का अध्ययन काफी व्यापक था और निश्चित रूप से उनका साबका औपन्यासिक लेखन से पड़ा होगा। इसी तरह, पाटील के बाद, सत्यशोधकों के लेखन से उपन्यास गायब हो गए।
[7] इस्कीयोंन पब्लिकेशंस पुणे, द्वारा ‘विचार किरण : दीनमित्रकार मुकुंदराव पाटील समग्र वाङ्गमय’ शीर्षक से प्रकाशित यह विशाल संकलन 10 खं में उपलब्ध है, जिसमें लगभग 2,000 संपादकीय लेख संगृहीत हैं।
[8] छत्रपति शाहूजी महाराज कभी सत्यशोधक समाज के सदस्य नहीं रहे। वे स्वयं को आर्यसमाजी बताते थे। परंतु बीसवीं सदी की शुरुआत में सत्याशोधक समाज के उभरते हुए सदस्यों के वे सबसे बड़े सहयोगी थे। शाहू ने गैर-ब्राह्मणों को मुद्रित प्रकाशनों के ज़रिए उनके विचारों के प्रसार के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए।
[9] श्रीराम गुंडेकर, ‘सत्याशोधाकि साहित्यचा इतिहास’, प्रथम खंड, सत्याशोधाकि साहित्य प्रकाशन, लातूर (2010), पृ. 462
[10] माधवराव पाटील, ‘आठवणीं सत्यशोधक दादांच्या’, दीनमित्रकार मुकुंदराव पाटील स्मारक समिति, तारावाड़ी, 2018
[11] फुले की तरह, पाटील भी माली जाति से थे।
(यह आलेख पूर्व में अंग्रेजी में ऑनलाइन पत्रिका ‘फिफ्टीटू’ में प्रकाशित है। यहां लेखक व प्रकाशक की अनुमति से हिंदी में प्रकाशित)
(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in