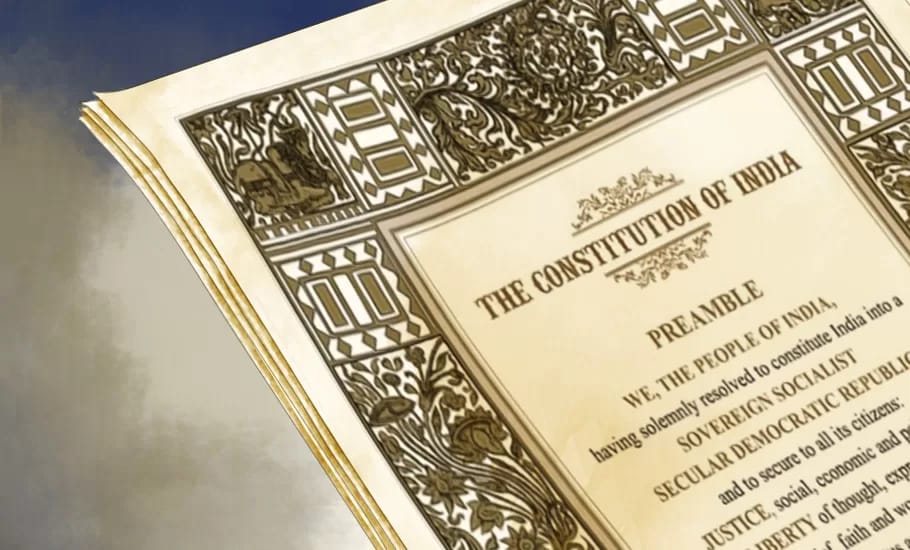क्या मध्य प्रदेश में वे राजनीतिक दल, जो दलित और आदिवासी समाज की राजनीति करते रहे हैं, उनकी कोई निर्णायक भूमिका है या फिर उनकी भूमिका के दूसरे निहितार्थ हैं? या उनसे किसी दूसरे परंपरावादी दल को लाभ मिल रहा है, यदि हां तो वह लाभ किसे मिल रहा है? यह वे सवाल हैं जो चुनावी रंग में सरोबार हो चुकी प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बार-बार उठ रहे हैं।
हाल ही में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) के मध्य हुए चुनावी गठबंधन और कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना करवाए जाने के वादे के मध्य इन सवालों का जवाब तलाशा जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर पर तब जब प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, जिसकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश और विभिन्न जातीय समूहों में रही हो। साथ ही इनमें से अधिकांश – वर्ष 2008 में विधान सभा आम चुनाव के बाद खास तौर से – कांग्रेस और भाजपा के उन बागियों पर निर्भर करते आए हैं, जो टिकट न मिलने से नाराज होकर इनका झंडा उठाकर चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। इन प्रमुख दलों में समाजवादी पार्टी (सपा), बसपा और गोंगपा शामिल हैं।
हालांकि वर्ष 2003 में जब गोंगपा ने तीन विधान सभा क्षेत्रों में जीत का परचम लहराया था, तो उनमें से दो का वजूद पार्टी के वजूद से ज्यादा था। इनमें सर्वप्रथम नाम आता है बालाघाट जिले के अनारक्षित परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से विजयी दरबू सिंह उईके और दूसरा अमरवाड़ा आरक्षित क्षेत्र से जीते दिवंगत मनमोहन शाह बट्टी का। वहीं यह जानना भी दिलचस्प रहेगा कि वर्ष 2018 में हुए विधान सभा आम चुनाव में मध्य प्रदेश में 114 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल भी मैदान में थे, जिन्होंने सामूहिक तौर पर 13,27,994 मत हासिल किए थे। जबकि बसपा, सपा और गोंगपा ने संयुक्त तौर पर 30,83,315 मत प्राप्त किए थे। जबकि इस चुनाव में 18 विधान सभा क्षेत्रों में हार-जीत का फैसला दो हजार से कम मतों से हुआ था। इनमें भी दस सीटों में यह अंतर एक हजार मतों से भी कम का था, जिसमें सात पर कांग्रेस और तीन पर भाजपा प्रत्याशी जीते थे। मगर शेष आठ मे से पांच सीटों पर भाजपा को सफलता हाथ लगी थी।
2003 के बाद बसपा, सपा और गोंगपा का प्रदर्शन
| वर्ष | बसपा (मत प्रतिशत और सीटों की संख्या) | सपा (मत प्रतिशत और सीटों की संख्या) | गोंगपा (मत प्रतिशत और सीटों की संख्या) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 7.76 प्रतिशत, 2 सीटें | 3.71 प्रतिशत, 8 सीटें | 0.23 प्रतिशत, 3 सीटें |
| 2008 | 8.72 प्रतिशत, 7 सीटें | 1.89 प्रतिशत, 1 सीट | 1.8 प्रतिशत, कोई सीट नहीं |
| 2013 | 6.29 प्रतिशत, 4 सीटें | 0.3 प्रतिशत, कोई सीट नहीं | 1 प्रतिशत, कोई सीट नहीं |
| 2018 | 5.01 प्रतिशत, 2 सीटें | 1.30 प्रतिशत, 1 सीट | 1.77 प्रतिशत, कोई सीट नहीं |
स्रोत : केंद्रीय निर्वाचन आयोग
जबकि जातीय समीकरणों के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश में करीब 22 फीसदी आदिवासी मतदाता हैं। वहीं 17 फीसदी दलित मतदाता हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 35 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं। इस तरह 82 सीटें एससी-एसटी के लिए आरक्षित हैं। जबकि 148 सीटें अनारक्षित हैं। वहीं राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा पिछले साल मई में करवाए गए सर्वेक्षण में ओबीसी की आबादी 48 प्रतिशत पाई गई थी, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे 61 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे तौर पर प्रभाव रखते हैं। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में एससी के साथ ही मालवा, भोपाल और होशंगाबाद का इलाका इनका गढ़ माना जाता है। इस प्रकार कुल 230 में से 143 पर एससी, एसटी और ओबीसी ही हार-जीत की दिशा तय करते हैं। इसके अलावा कुछ सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत भी ठीकठाक है। यह अलहदा है कि प्रदेश की राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व और प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा है।

सूबे में ओबीसी जातियों की निर्णायक भूमिका है। हालांकि इसके बावजूद आज कांग्रेस में कमलनाथ का दबदबा है, जिनकी जाति को लेकर स्पष्टता नहीं है। स्वयं कमलनाथ ने अपनी जाति को कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस जाति अथवा किस समुदाय के हैं। इसलिए उन्हें किसी खांचे में नहीं डाला जा सकता है। वहीं भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को लगातार तीन बार मुुख्यमंत्री बनाया है, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं।
वहीं कई और राजनीतिक संगठन भी जातीय समीकरणों को साधते हुए विधान सभा चुनाव में दलित-बहुजन समुदायों का झंडा लेकर उतरने को कुछ इस तरह लालायित हैं कि तीसरे, चौथे और पांचवें मोर्चे भी नजर आने लगे हैं। इसकी शुरुआत बसपा और गोंगपा गठबंधन से हुई है, जो क्रमश: 178 और 52 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कह रहे हैं।
बताते चलें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जौरा, देवताल, ग्वालियर ग्रामीण, पौहारी, रामपुर बघेलान और सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में बसपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि 36 क्षेत्र ऐसे थे, जहां बसपा को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें तो 2003 के बाद उसका कभी खाता भी नहीं खुला। जबकि उसके मत प्रतिशत चुनाव-दर-चुनाव बढ़े हैं।
एक अन्य मोर्चे के तौर पर ओबीसी महासभा, आजाद समाज पार्टी (भीम आर्मी) आदि भी इन प्रस्तावित चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के संस्थापक रहे मनमोहन शाह बट्टी की पुत्री मोनिका के भाजपा का झंडा थाम लेने से इस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। कांग्रेस जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फिर मनावर से कांग्रेस विधायक डा. हिरालाल अलावा पर यकीन कर रही है। वही डा. अलावा भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मोर्चा बनाने की बात कर चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में राजधानी भोपाल में जयस के नेतृत्व में आयोजित सर्व समाज सम्मेलन में 10 से अधिक राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों के साथ ही विभिन्न समाजों के कई संगठनों के प्रमुख और प्रदेश के कई पूर्व विधायक एवं सांसद भी शामिल हुए थे। लेकिन यह भी सत्य है कि जयस आज दो गुटों में बंट चुका है। इसके एक गुट का नेतृत्व डा. अलावा कर रहे हैं और दूसरे गुट की कमान डा. आनंद राय के हाथ में है, जिन्होंने इसी साल 7 जून को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की सदस्यता ले ली।
हालांकि, आज भी मध्य प्रदेश उन कुछ गिने-चुने राज्यों में शुमार है, जहां का मतदाता मुख्यतः दो ही राजनीतिक दलों तक सीमित रहा है। यहां कोई भी तीसरा दल न तो अपना समूचा वजूद खड़ा कर पाया है और न ही मतदाताओं ने ऐसा करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में प्रयोग नहीं हुए। मामा बालेश्वर दयाल, पुरुषोत्तम कौशिक, यमुना प्रसाद शास्त्री और एच.वी. कामथ जैसे समाजवादियों और होमी दाजी, शाकिर अली तथा रामलखन शर्मा जैसे वामपंथियों को यहां के मतदाताओं ने खूब सराहा है। बसपा और सपा के प्रत्याशियों को भी पहले पहले खूब जिताया। लोकसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में बसपा का सर्वप्रथम सांसद रीवा संसदीय क्षेत्र से चुना गया था। मगर सत्ता के साथ फेरे लेने की उनके विधायकों की आदतों ने इन दलों को भी मतदाताओं ने अपने से दूर कर दिया। राजनीतिक दलों के प्रति अरुचि व्यक्त करते हुए यहीं के मतदाताओं ने थर्ड जेंडर का प्रतिनिधित्व करने वाली शबनम मौसी को राज्य विधान सभा में भेजा था। इसी समय कटनी और सागर के महापौर भी थर्ड जेंडर के ही थे। इसके बाद वर्ष 2003 में अनारक्षित परसवाड़ा विधानासभा क्षेत्र से आदिवासी दरबू सिंह उईके को जिताकर मतदाताओं ने एक ऐसा प्रयोग किया था, जिसकी कोई कल्पना भी नही कर सकता था। सत्ताधारी भाजपा से गोंगपा के विधायकों की नजदीकियों की राजनीतिक चर्चाओं ने अगली बार गोंगपा को भी मौका नहीं दिया।
ऐसे में यह कहा जा सकता है कि हो रहे चुनाव में ये सभी मोर्चे और राजनीतिक दल भले ही जातीय समीकरणों का सहारा लेकर चुनावी समर में उतर जाएं। लेकिन कुछ अप्रत्याशित के आसार सामने नहीं दिख रहे और इसकी वजह यह कि ये दलित, आदिवासी और पिछड़ों की राजनीति करनेवाली पार्टियां स्वयं कई खेमों में बंटी हैं।
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in