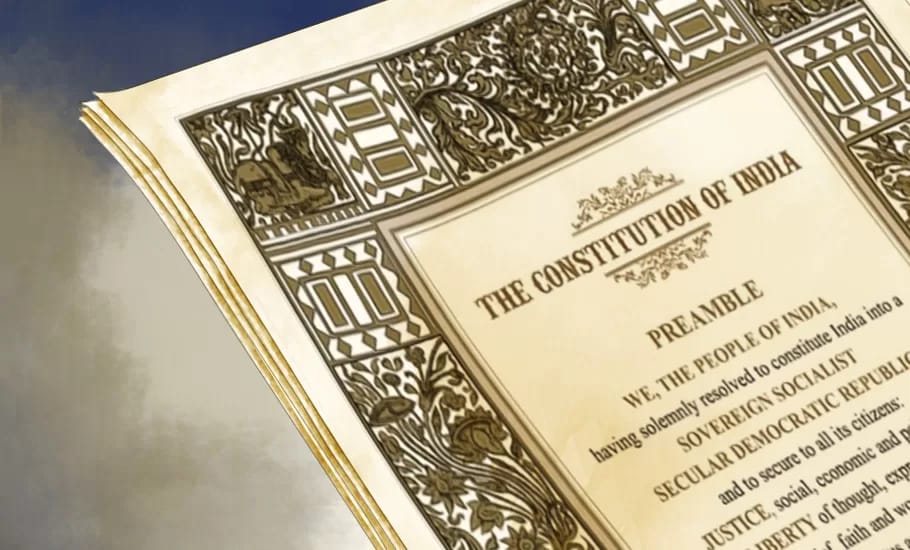विमुक्त जनजातियों, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्कीम फॉर इकोनोमिक एम्पावरमेंट ऑफ़ डीएनटीज़ (सीड) नामक योजना 16 फरवरी, 2022 से शुरू की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, भूमि व आवास जैसे सुविधाएं जुटाना था।
मगर सीड योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम शुरू किये जाने हैं, वे केवल डीएनटी के लिए नहीं बनाए गए थे। इस योजना के अंतर्गत, संस्थागत कोचिंग की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी विद्यार्थियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए है। स्वास्थ्य बीमा योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के जरिए लागू किया जाना है। आजीविका संबंधी घटक को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) की मदद से लागू किया जाना है। भूमि एवं आवास संबंधी घटक को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) एवं इंदिरा आवास योजना (आईएवाय) के अंतर्गत लागू किया जाना है। सीड योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा धन के आवंटन पर निर्भर है। विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) इन सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय के लिए ज़िम्मेदार है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा डीडब्ल्यूबीडीएनसी के लिए पांच वर्ष की अवधि हेतु 200 करोड़ रुपए अर्थात 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मंज़ूर किये गए। इसमें से प्रशासनिक व्यय के लिए कुल परियोजना लागत का एक प्रतिशत अर्थात दो करोड़ रुपए निर्धारित है। यह धनराशि करीब 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष होती है। वर्षवार जारी की गई धनराशि की जानकारी न तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और ना ही डीडब्ल्यूबीडीएनसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
डीडब्ल्यूबीडीएनसी के अध्यक्ष और सदस्य राज्यों के दौरों पर गए, अधिकारियों से मुलाकातें की और बैठकें आयोजित कीं। मगर डीएनटी के कल्याण के लिए कोई नए या बेहतर कदम उठाए गए हों, ऐसा बोर्ड के पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिला-स्तर पर आयोजित बैठकों में अधिकारियों को डीएनटी के लिए योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए जाते हैं, मगर जिला-स्तर के अधिकारीगण न तो यह जानते हैं कि डीएनटी कौन हैं और न ही यह पता है कि उनके विकास और कल्याण के लिए कौन-कौन योजनाएं उपलब्ध हैं और ना ही यह कि इन योजनाओं तक डीएनटी समुदायों के लोगों की पहुंच को कैसे संभव बनाया जाय? शासकीय कर्मियों को योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए डीडब्ल्यूबीडीएनसी ने कोई ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया। इसका कारण यह है कि बोर्ड के सदस्य स्वयं डीएनटी समुदायों के बारे में बहुत नहीं जानते।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव रेड्डी सुब्रमण्यम द्वारा 18 अगस्त, 2020 को जारी एक पत्र में कहा गया– “यदि आप अपने प्रदेश/संघ शासित प्रदेश में डीएनटी समुदायों (सूची संलग्न) का सर्वेक्षण करने की ज़िम्मेदारी किसी विभाग या संस्था को दे सकें, ताकि 31 दिसंबर, 2020 के पहले इसका डाटाबेस तैयार हो सके, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आंकड़ों के संकलन पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा सकेगा।” मगर किसी भी राज्य ने सर्वेक्षण करने की जहमत नहीं उठाई। न तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और न ही डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा राज्यों को सर्वेक्षण करने के लिए प्रेरित करने हेतु कोई कदम उठाए गए।
राज्य सरकारों की इस उदासीनता की जड़ में एक समुदाय के रूप में डीएनटी को कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त न होना है। सरकारी अभिलेखों में उन्हें विमुक्त समुदाय (डीएनसी) कहा जाता है। डीएनटी के कल्याण हेतु कार्यक्रमों का “दिल्ली से गली” तक कार्यान्वयन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि उनके कल्याण की ज़िम्मेदारी किसी विशिष्ट विभाग, मंत्रालय या सरकारी संगठन की नहीं है। सभी विभागों के कर्मियों के पास अपने काम होते हैं और डीएनटी के कल्याण संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व संभालना उनके लिए संभव नहीं होता। अतः डीएनटी के कल्याणार्थ कार्यक्रमों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रशासन और प्रबंधन में रचनात्मकता और उचित दृष्टिकोण होनी चाहिए। इसकी अपेक्षा हम फिलहाल किसी सरकारी तंत्र से नहीं कर सकते।

वजह यह कि बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति का आधार यह नहीं होता कि उन्हें कितना अनुभव हासिल है, वे कितने योग्य हैं और डीएनटी के बारे में कितना जानते हैं, बल्कि यह होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या उसकी समर्थक विचारधाराओं से उनकी कितनी नजदीकी है और भाजपा का हाथ उनकी पीठ पर है या नहीं। जाहिर है कि डीएनटी के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती।
भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण को डीएनटी व घुमंतू जनजातियों का मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। मगर इस कवायद से कोई मानववैज्ञानिक जानकारियां सामने नहीं आईं। सर्वेक्षण के लिए जो प्रश्नावली तैयार की गई थी उसके कोई नृवंशवैज्ञानिक सूचनाएं हासिल नहीं हो सकीं। कोई बाहरी एजेंसी या शोधार्थी, वांछित जानकारी तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो डीएनटी की संस्कृति और उनके जीवन से वाकिफ न हो। घुमंतू जनजातियों और डीएनटी के बारे में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कहीं कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। सर्वेक्षण के लिए उत्तर व दक्षिण भारत की घुमंतू जनजातियों व डीएनटी समुदायों के शोधार्थियों के समूह और इन समुदायों के नेताओं की ज़रूरत होगी, जो बुजुर्गों का भरोसा जीत कर प्रासंगिक प्रश्न तैयार कर सकें।
हम्पी विश्वविद्यालय में आदिवासी अध्ययन विभाग के डीन डॉ. के.एम. मेत्री की घुमंतू जनजातियों पर अनेक पुस्तकें कर्नाटक पुस्तक प्राधिकार की आर्थिक मदद से प्रकाशित हैं। उन्होंने मैदानी स्तर पर जानकारियां इकट्ठा करने के लिए हर समुदाय से ऐसे व्यक्तियों को चुना जो पढ़ना-लिखना जानते थे। प्रोफेसर मेत्री स्वयं एक अनुसूचित जनजाति में शामिल घुमंतू समुदाय से आते हैं। प्रोफेसर मेत्री का कर्नाटक के घुमंतू समुदायों के बारे में वाकिफ होने और हर घुमंतू समुदाय के सदस्य को ही उसके समुदाय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी देने के उनके निर्णय के चलते ही कर्नाटक के घुमंतू समुदायों पर उत्कृष्ट साहित्य का सृजन हो सका, जिसमें हर समुदाय के बारे में अलग-अलग खंड हैं।
डीडब्ल्यूबीडीएनसी के काम करने का तरीका एकदम उलट है। उसके कर्मी अति-आत्मविश्वास से पीड़ित हैं और डीएनटी समुदायों के सदस्यों को सर्वेक्षणों में शामिल करने के इच्छुक नहीं हैं। इसी कारण भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण का नृवंशवैज्ञानिक अध्ययन असफल रहा।
वर्ष 2023 के अंत तक डीडब्ल्यूबीडीएनसी ने डीएनटी के लिए कुछ नहीं किया था। हालात और ख़राब इसलिए हो गए क्योंकि भीकू रामजी इदाते, जिनकी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अच्छी पैठ थी, को अध्यक्ष पद पर सेवावृद्धि नहीं दी गई और उन्हें बोर्ड छोड़ना पड़ा। इससे बोर्ड की नैया पूरी तरह डगमगा गई और वहां अराजकता फैल गई।
इसी वर्ष 18 जनवरी, 2024 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने तीन निगमों को सीड के आजीविका संबंधी घटक के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मान्यता दी। मगर इन निगमों का डीएनटी से कोई लेना-देना नहीं है। यह निर्णय (नेतृत्व विहीन) बोर्ड की सहमति या अनुमोदन के बगैर लिया गया। इन निगमों ने दो स्वयंसेवी संस्थाओं और एक सरकारी संस्था को डीएनटी स्वयं-सहायता समूह बनवाने की ज़िम्मेदारी सौंप दी। ये संस्थाएं इस काम को बहुत बेतरतीब ढंग से कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डीएनटी की कोई समझ ही नहीं है। इस काम के लिए एनजीओ का चुनाव भी एकतरफा ढंग से किया गया। चयन प्रक्रिया में हितधारक संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया और ना ही आवेदन मंगवाए गए।
वकील गौतम राजभर ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं डीडब्ल्यूबीडीएनसी के खिलाफ सीड के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अदालत की अवमानना का प्रकरण दायर किया। डीडब्ल्यूबीडीएनसी ने इस मामले में 10 अक्टूबर, 2024 को एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया था कि बोर्ड ने चार राज्यों – गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा – में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 994 स्वयं सहायता समूह बनवाए हैं, जिनके लाभार्थियों की संख्या 7,878 है। इन स्वयं सहायता समूहों का गठन स्वयंसेवी संस्थाओं (गुजरात और हरियाणा में ‘प्रयत्न’ और महाराष्ट्र में ‘निर्माण’ नामक संस्था) तथा आंध्र प्रदेश में ‘नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज’ के माध्यम से करवाया गया है। इन संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफ़डीसी) द्वारा किया गया है। बोर्ड ने यह दावा भी किया कि आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने के लिए वह कई अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रहा है। बोर्ड के अनुसार, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए संचालित मुफ्त कोचिंग कक्षाओं में क्रमशः 12 और 43 डीएनटी विद्यार्थियों को भर्ती करवाया गया है। ये कोर्स सितंबर, 2024 में शुरू हुए। इसी तरह, जिन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम पात्रता 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना है, उनकी कोचिंग के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी थी, जिसकी अंतिम तिथि 4 नवंबर, 2024 थी। बोर्ड ने यह भी कहा कि अब तक गुजरात में 5,653 और महाराष्ट्र में 248 आयुष्मान कार्ड डीएनटी समुदायों के लाभार्थियों को जारी किये जा चुके हैं। डीएनटी के संगठनों ने इन दावों की सच्चाई जानने की कोशिश की, मगर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे स्वयंसेवी संस्थाओं में पारदर्शिता के अभाव के कारण वे इसमें सफल न हो सके। अब केवल सूचना के अधिकार के तहत आवेदन से ही ज़मीनी सच्चाई का पता चल सकता है।
सन् 2022 में सीड की घोषणा के बाद से, अकेले आंध्र प्रदेश से घुमंतू जनजातियों और डीएनटी के कम से कम 8,060 लोगों ने आजीविका घटक के अंतर्गत अपेक्षित सुविधाएं हासिल करने के लिए आवेदन किया था। मगर उन्हें आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। स्व-नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन लोगों से ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करने के नाम पर और कर्ज दिलवाने का वायदा करके हजारों रुपए वसूल कर लिए हैं।
आवेदन करने की प्रक्रिया काफी उबाऊ और कठिन है, विशेषकर उन लोगों के लिए, जो निरक्षर और आवासहीन हैं। इसके लिए पहचान के दस्तावेज और डीएनटी प्रमाणपत्र ज़रूरी हैं। बाबुओं को डीएनटी के बारे में बहुत सीमित जानकारी है और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं। इससे इन लोगों की मुसीबतों में इज़ाफा ही हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सीड के कार्यान्वयन को एक जादू की छड़ी बताया था, जो उन्हें गरीबी के चंगुल से मुक्त करवा देगी।
वहीं आंध्र प्रदेश का पिछड़ा वर्ग वित्त निगम कुछ जिलों में पंचायत सचिवों और नगर निगमों के माध्यम से घुमंतू लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है। राज्य सरकार के प्रमुख सचिव ने सीड से धन आवंटित न होने की स्थिति के लिए प्लान ‘बी’ तैयार कर रखा है। वह है तेलुगुदेशम पार्टी की तत्कालीन सरकार द्वारा 2018-19 में कार्यान्वित योजना को फिर से लागू करना। इसके अंतर्गत सूचीबद्ध डीएनटी और घुमंतू जनजातियों के सदस्यों को 30,000 रुपए का कर्ज दिया जाता है, जिस पर 90 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होता है। इस प्रकार, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रजातांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के अभाव में चारों ओर भ्रम और अनिश्चितता का बोलबाला है।
समस्याओं के हल हेतु सुझाव
सीड का कार्यान्वयन, डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा सीधे किया जाना ज़रूरी है और इसके लिए तीन अतिरिक्त एजेंसियों, जिनका डीएनटी और घुमंतू जनजातियों से कोई लेना-देना नहीं है, को प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए। बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक वफ़ादारी पात्रता नहीं होनी चाहिए। नया अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसे घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जातियों सहित डीएनटी के वर्तमान हालात और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हो। स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन पारदर्शी ढंग से होना चाहिए। अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ किये गए समझौतों को रद्द किया जाना चाहिए। वर्तमान में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे काम पर रोक लगाकर, ऐसी स्थानीय संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाने चाहिए जो डीएनटी एवं घुमंतू जनजातियों के लोगों के बारे में समझ रखती हों। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा जारी किये गए आवंटन और उसके खर्च का विवरण इन दोनों की वेबसाइटों पर वर्षवार प्रकाशित किया जाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों एवं हितधारकों के लिए विभिन्न स्तरों पर ओरिएंटेशन कैंप आयोजित किये जाने चाहिए, जिसमें उन्हें इन समुदायों के समक्ष उपस्थित समस्याओं और उनके समाधान के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। डीडब्ल्यूबीडीएनसी को सीड के कार्यान्वयन से संबद्ध मंत्रालयों से संपर्क रखना चाहिए ताकि योजनाओं को लागू करने के लिए धन और कर्मी उपलब्ध करवाए जा सकें। आजीविका से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के चुनाव हेतु मार्गनिर्देशों एवं मानकों का निर्धारण करने के लिए डीएनटी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जानी चाहिए। राज्य-स्तरीय डीएनटी कल्याण बोर्डों के कर्मियों का इस्तेमाल डीएनटी से संबंधित जो डाटा एकत्रित किया गया है, उसे ऑनलाइन उपलब्ध करवाने एवं योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य-स्तरीय डीएनटी कल्याण बोर्डों के पर्यवेक्षण में गठित डीएनटी, घुमंतू व अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के सदस्यों के स्वयं सहायता समूहों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कम से कम 100 करोड़ रुपए का लघु ऋण बैंक स्थापित किया जाना चाहिए।
(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in