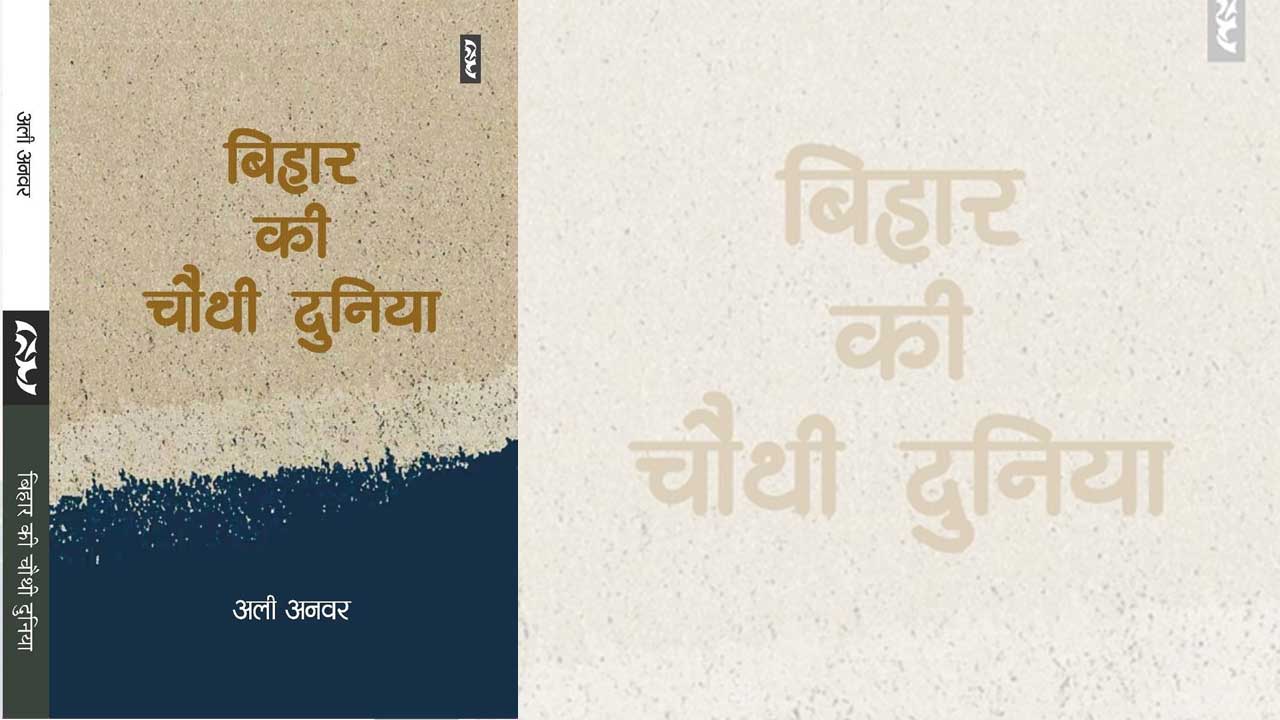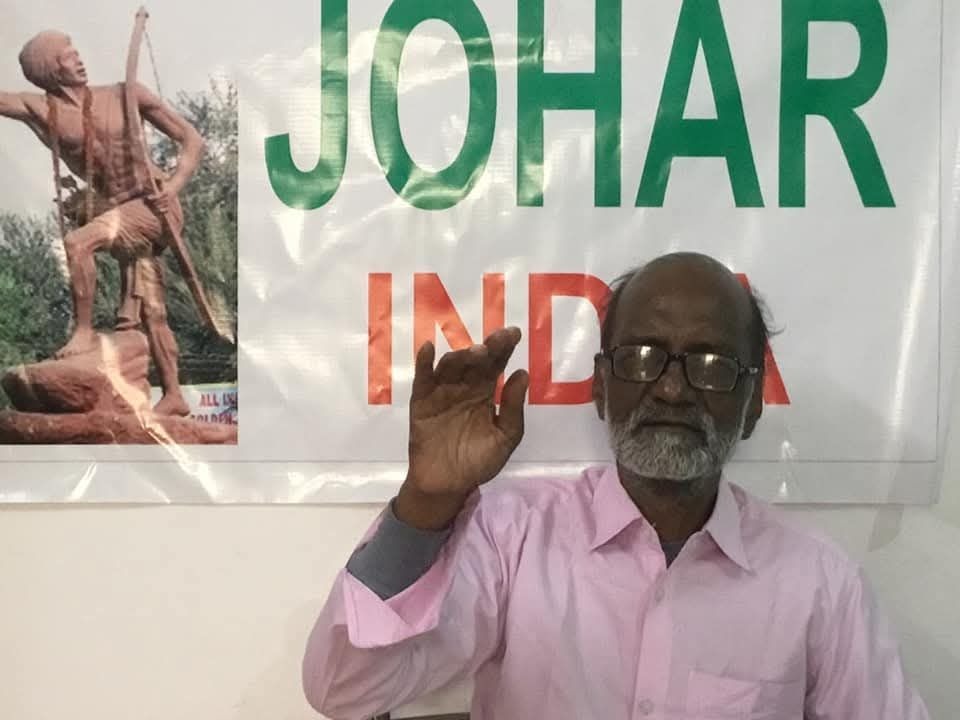मैं मानव-मात्र की समानता में विश्वास करता हूं। मेरे हिसाब से धर्म का अभिप्राय ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करना है, जिनसे न्याय की स्थापना हो। दिलों में एक-दूसरे के प्रति दया, ममता, करुणा तथा प्रेम का उजियारा हो, ऐसे कर्तव्य करना जिनसे हमारे आसपास के प्राणी अधिकाधिक सुखी रह सके। – थॉमस पेन
‘संस्कृति’ समाजशास्त्र के सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके अलग-अलग संदर्भ होते हैं। कई बार परंपरा को ही संस्कृति समझ लिया जाता है। जबकि अनेक बार लोग संस्कृति और सामान्य व्यवहार के बीच अंतर नहीं कर पाते। जनसामान्य ‘संस्कृति’ को सलीके से परिभाषित भले ही न कर पाए, लेकिन यदि किसी व्यक्ति से उसके सामान्य व्यवहार, कार्यकलापों, सामाजिक-पारिवारिक जीवन की प्रेरणाओं के बारे में प्रश्न किया जाए तो बिना झिझके उसका एक ही उत्तर होगा– ‘यही मेरी संस्कृति है।’ संस्कृति मनुष्य और समाज के संबंधों को न केवल व्याख्यायित करती है, अपितु उन्हें सफल एवं सार्थक भी बनाती है। संस्कृति के स्वरूप, उसकी अवधारणा, परिभाषा आदि को लेकर समाजविज्ञानियों के बीच मतभेद रहे हैं। कई बार लोग संस्कृति को मनुष्य के सामान्य व्यवहार से जोड़ने लगते हैं तो कई बार उसे सभ्यता के साथ गड्मड कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति अथवा समाज के संदर्भ में संस्कृति उसके समग्र ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, कला, रोजमर्रा के व्यवहारों, संबंधों, रीति-रिवाजों, परंपराओं आदि का समुच्चय होती है।
संस्कृति का कोई एक स्रोत नहीं होता। मनुष्य संस्कृति के तत्व माता-पिता, गांव-पड़ोस, रीति-रिवाज, किस्से-कहानियों, साहित्य-कला, ज्ञान-विज्ञान आदि विविध स्रोतों से ग्रहण करता है तथा उन्हें अपनी अस्मिता और पहचान के रूप में सहेजकर रखता है। इस तरह कि वे उसके रोजमर्रा के व्यवहार, ज्ञान, सामाजिक संबंधों और मर्यादाओं का आधार बन जाते हैं।
दूसरे शब्दों में संस्कृति उत्तराधिकार का विषय है। व्यक्ति अथवा समाज जिन आदतों को यत्नपूर्वक अपनी विरासत के तौर पर संभाले रहता है, जिनसे उसकी विशिष्ट पहचान बनती है, उनका समन्वित, समावेशी और लोकोपकारी रूप संस्कृति कहा जा सकता है। उनमें कला, साहित्य, अर्जित ज्ञान, रीति-रिवाज, परंपराएं, सामूहिक प्रवृत्तियां, खान-पान, आचार-व्यवहार आदि सब सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा उसमें वे आदर्श और नियम भी समाहित होते हैं, जिन्हें कोई समाज खुद को दूसरों से अलग और बेहतर दिखाने तथा स्थायित्व की भावना के साथ अपनाता है। मनुष्य की भौगोलिक और परिस्थितिकीय विशेषताएं भी उसकी संस्कृति को प्रभावित करती हैं।
‘संस्कृति’ शब्द ‘सम्’ और ‘कृति’ की संधि से बना है। उसका आशय ऐसी अमूर्त्त सामाजिक संरचना से है, जो सभी का साझा हो। संस्कृति और सभ्यता को प्रायः एक-दूसरे के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। तथापि दोनों में अंतर है। सभ्यता की कसौटी भौतिक जगत की उपलब्धियां तथा उनके फलस्वरूप जीवन में आए परिवर्तनों को माना जाता है। सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होती है, एक तरह से उसका हिस्सा भी है, लेकिन वह स्वयं संस्कृति नहीं होती। ऐसे ही जैसे भाषा ज्ञान की वाहक होती है, स्वयं ज्ञान नहीं होती। हां, भाषा का ज्ञान हो सकता है, जो मनुष्य की संपूर्ण ज्ञान-संपदा का मामूली हिस्सा है। इसी तरह मनुष्य अथवा समाज की भौतिक उपलब्धियां भी संस्कृति नहीं होतीं। सभ्यता को आमतौर पर संस्कृति का उत्पाद माना जाता है। लेकिन यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। सभ्यता और संस्कृति का संबंध अन्योन्याश्रित होता है, जिनमें संस्कृति का स्थान अपेक्षाकृत ऊपर माना जाता है। अपनी प्रत्येक उपलब्धि के लिए सभ्यता संस्कृति की ऋणी रहती है। उसे हम संस्कृति का आवरण भी कह सकते हैं। परोक्षतः दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। किसी समूह अथवा समाज की सभ्यता को उसकी संस्कृति अथवा संस्कृतियों का समुत्पाद भी कहा जा सकता है।
संस्कृति और व्यवहार में भी अंतर है। लोग संस्कृति को रोजमर्रा के आचरण के रूप में देखने की भूल कर बैठते हैं। यह गलत है। मनुष्य का नैमत्तिक व्यवहार कानून, समाज, बाजार आदि से प्रभावित हो सकता है। उसका अध्ययन मानव-व्यवहार के अंतर्गत आता है। इस तरह वह मनोविज्ञान की विषय-वस्तु है। संस्कृति व्यवहार भी नहीं होती। उसे व्यवहार की नियंत्रक शक्ति अवश्य कहा जा सकता है। कोई भी सामाजिक अथवा व्यक्तिगत व्यवहार संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, उसे संस्कृति नहीं माना जा सकता। कारण यह कि व्यवहार मूर्त्त होता है, संस्कृति अमूर्त्त। होली के पर्व पर एक-दूसरे पर रंग डालना अथवा रक्षाबंधन के अवसर पर बहन द्वारा भाई को राखी बांधना, सहज सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहार का हिस्सा हैं, स्वयं संस्कृति नहीं है। संस्कृति उनमें अंतर्निहित प्रेरणा है। ऐसी अंतश्चेतना जो मानव मन में अधिकाधिक सभ्य तथा प्राणीमात्र के प्रति अधिकतम उपयोगी होने का उत्साह जगाती है। मनुष्य ऐसी प्रेरणाओं को अपनी-अपनी तरह से परिभाषित कर सकता है। उनके स्वरूप में थोड़ा-बहुत परिवर्तन ला सकता है, किंतु सामाजिक पहचान से जुड़े होने के कारण उन्हें पूर्णतः नकार नहीं सकता। कुल मिलाकर समाज अथवा व्यक्ति-विशेष के संदर्भ में संस्कृति को हम उसकी सामूहिक आदतों, स्वभाव, ज्ञान-विज्ञान, कला, साहित्य आदि के समुच्चय के रूप में देख सकते हैं।
संस्कृति के प्रायः दो रूप दृष्टिगत होते है–
- अभिजन संस्कृति
- बहुजन संस्कृति
अभिजन संस्कृति के लाभार्थी राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक प्रस्थिति के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त लोग होते हैं। भारत के संबंध में इनमें जाति भी जुड़ जाता है। ये अधिकार प्राप्त लोग अपने-अपने क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों पर आसीन रहकर उनका प्रयोग अपनी समाजार्थिक प्रस्थिति को मजबूत करने में लगे रहते है। शेष समाज के हितों की चिंता न कर वे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। विकास के नाम पर ये लोग स्पर्धा को अपरिहार्य मानते हैं। चूंकि इनकी स्पर्धा का उद्देश्य ही अधिकतम लाभार्जन होता है, इस कारण ये उसमें अपने लाभानुपात को शामिल नहीं करते। न उसमें उच्चतम तकनीक के स्थान पर श्रेष्ठतम मानवीय श्रम और कौशल को वरीयता दी जाती है। आमतौर पर श्रम और उत्पादन लागत में कमी, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को ही स्पर्धा का विषय बनाया जाता है। प्रकारांतर में वह इनकी सामाजिक प्रस्थिति को मजबूत करता है। जिससे अभिजन संस्कृति कुछ और ‘अभिजन’ हो जाती है, जबकि बहुजनों का दैन्य बढ़ता चला जाता है।
अपने मूल विषय ‘बहुजन संस्कृति’ पर लौटने से पहले आवश्यक है कि ‘बहुजन’ की अवधारणा तय कर ली जाए। इससे फुले की पुस्तक ‘गुलामगिरी’ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी आसानी से समझा जा सकेगा। इस पुस्तक में वर्चस्वकारी संस्कृति अपने सबसे घातक स्वरूप में – जब कोई संस्कृति मिथों के जरिए बहुजन समाज के सामाजिक मूल्यों पर छा जाती है – प्रकट हुई है। ‘बहुजन’ का अभिधार्थ ‘बहुसंख्यक जन’ अवश्य है, लेकिन इसका आधार मात्र संख्याबल नहीं है। संख्या के माध्यम से बहुजन को परिभाषित करने के अनेक खतरे हैं। इससे ‘बहुजन’ को संख्याबल समझ लिए जाने की संभावना बराबर बनी रहेगी। वह भीड़ को समाज का दर्जा देने के बराबर होगा और प्रकारांतर में अनेक भ्रांतियों को जन्म देगा। पुनश्चः ‘बहुजन’ और ‘बहुसंख्यक जन’ दोनों को एक मान लिया गया तो अल्पसंख्यक मुस्लिमों के मुकाबले हिंदू बहुजन होंगे तथा दलितों के सापेक्ष पिछड़ी जातियों के लोग। इस कसौटी पर आदिवासियों के मुकाबले गैर आदिवासी ‘बहुजन’ माने जाएंगे। यह विभाजन आगे भी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब बहुजन की संकल्पना का आधार और उद्देश्य दोनों समाप्त हो जाएं। जैसे ‘बहुजन’ को ‘बहुसंख्यकजन’ नहीं कहा सकता, ऐसे ही ‘बहुजन’ के आधार पर ‘बहुजनवाद’ जैसी संकल्पना भी अनुचित कही जाएगी। उससे उसके ‘बहुसंख्यकवाद’ में बदलने की संभावना बनी रहेगी। अतएव ‘बहुजन’ की अवधारणा तय करने के लिए संख्या-तत्व को नजरंदाज करना ही उचित होगा।
फिर ‘बहुजन’ किसे माना जाए? इस शब्द का प्रथम उपयोग बौद्ध दर्शन में प्राप्त होता है। बुद्ध इसे परिभाषित नहीं करते, किंतु जिस संदर्भ में वे इसका प्रयोग करते हैं, उससे ‘बहुजन’ की अवधारणा साफ होने लगती है। भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए वे कहते हैं– ‘चरथ भिक्खवे चारिकम् – बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।’ ‘हे भिक्षु! बहुजन कल्याण और बहुजन-हित के लिए निरंतर प्रयाण करते रहो।’ इसके साथ-साथ जैन ग्रंथ ‘विआहपण्णत्ती’ में भी बहुजन उल्लेख राजन्यों, गाथापति तथा श्रेष्ठिजनों से इतर वर्गों के लिए हुआ है। महावीर और बुद्ध राज-परिवार में जन्मे थे। समकालीन राजाओं, विशेषकर श्रेष्ठिवर्ग पर उनका प्रभाव था। बुद्ध भिक्षुसंघ से ‘बहुजन’ के कल्याण हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहने की कामना करते हैं। जबकि महावीर बहुजनों के बीच अपनी चर्चा, संवाद को अपनी साधना का स्वीकार्यता के रूप में देखते थे। तत्कालीन बहुजन समाज की सकल उत्पादकता का दायित्व संभालने वाला वर्ग था। आने वाली शताब्दियों में उसका स्तर लगातार गिरता गया। बहुजन समुदाय के बीच अधिकतम पैठ बनाने को तो बुद्ध और महावीर दोनों ही उत्सुक थे; लेकिन उनके हितों की चिंता, चौतरफा हमलों से उसका संरक्षण दोनों में से किसी के लिए भी प्राथमिकता का मामला नहीं था।
तत्कालीन सामाजिक स्थितियों को देखते हुए इसे समझ पाना कठिन नहीं है। उस समय तक वर्ण-व्यवस्था कट्टर रूप ले चुकी थी। कर्मकांड शिखर पर था। लोग जाति देखकर व्यवहार करते थे। इस मामले में सर्वाधिक मुखर ब्राह्मण थे। उनका दावा था कि उन पर सृष्टि-रचयिता ब्रह्मा की विशेष कृपा है। जिसने उन्हें अपने मुख से पैदा किया है। निहित स्वार्थ के लिए उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी आदि का देवताकरण किया था और लगातार यह प्रचारित करते रहते कि वे यज्ञों के माध्यम से देवताओं के संपर्क में रहते हैं। दूसरा वर्ग क्षत्रियों का था, जिसे समाज की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देवताओं की दुहाई देते-देते ब्राह्मण खुद देवता होने का गुमान करने लगे थे, जबकि क्षत्रिय राज्य के रखवाले से उसका स्वामी बन बैठे थे। स्वार्थ के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय का महिमामंडन करता था और बदले में क्षत्रिय ब्राह्मण के पांव पखारता था।
तीसरा व्यापारी वर्ग था। पहले दो वर्गों की तरह अनुत्पादक वर्ग। उसका कार्य दूसरों के उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाना था। मुनाफे का एक हिस्सा ब्राह्मण और क्षत्रिय को भेंट कर वह मस्त रहता था। शेष जनसमाज यानी चौथे उत्पादक वर्ग में किसान, मजदूर, शिल्पकार आदि सभी आते थे। उनपर समाज के विकास की जिम्मेदारी थी, परंतु थे सब दूसरों की मर्जी के दास। किसी को अपनी रुचि और हितों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता न थी। किसान खेत में पसीना बहाता था, मगर फसल पर उसका अधिकार न था। वह राजा और सामंत की मान ली जाती थी। शिल्पकार अपनी कला से संस्कृति और सभ्यता को संवारने का काम करते थे, किंतु अपने ही श्रम-कौशल पर उनका अधिकार न था। उनके श्रमोत्पाद के मूल्यांकन का अधिकार शासक और व्यापारी वर्ग के पास था। देश में प्राचीन स्थापत्यकला की उन्नति को दर्शाने वाली अनेकानेक इमारतें हैं। परंतु हम केवल उन्हें बनवाने वालों के नाम से जानते हैं। उन कारीगरों के नाम जिन्होंने उन्हें बनाने के लिए अपनी बेमिसाल कारीगारी और श्रम का योगदान दिया था, हमारे ग्रंथों से नदारद हैं। यह दर्शाता है कि उस समाज में वास्तविक उत्पादक जिसे ब्राह्मण शूद्र लिखते आ रहे थे– श्रेय या प्रेय किसी के भी अधिकारी न थे। उनका कर्तव्य था राज्य के लिए कर और ब्राह्मण के लिए दान देना। वफादार रहना तथा उनके प्रत्येक आदेश को कृपा-भाव के साथ ग्रहण करते हुए अपने वर्गीय धर्म का निर्वाह करना। इसी में उसकी मुक्ति है– यह कहकर उन्हें बरगलाया जाता था।

संख्याबल में ऊपर के तीनों वर्ग शेष जनसमाज के सापेक्ष बहुत कम थे। कुल जनसंख्या का बमुश्किल पांचवा हिस्सा। लेकिन समाज के कुल संसाधनों पर उनका अधिकार था। इसलिए संख्या-बहुल होने के बावजूद निचले वर्ण के लोग ऊपर के तीन वर्गों की मनमानी सहने के लिए विवश थे। कार्य-विभाजन के नाम पर ब्राह्मणों ने समाज के बहुसंख्यक हिस्से को छोटी-छोटी जातियों और वर्गों में बांट दिया था। बहुजन के पास बुद्धि थी, हस्तकौशल था, अनथक परिश्रम करने का हौसला तथा ईमानदारी भी थी। नहीं था तो आत्मविश्वास और सपने जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये सब सेवा-भाव की भेंट चढ़ चुके थे। निरंतर बढ़ते सामाजिक दबावों तथा यह भ्रम कि ईश्वर एकमात्र और सच्चा न्यायकर्ता है, कि इस जीवन में उन्हें जो खोना पड़ रहा है वह मृत्योपंरात जीवन में सहज प्राप्त होगा– के चलते वे पूर्णतः नियतिवादी हो चुके थे। अपने सामान्य हितों के बारे में निर्णय लेने के लिए भी वे समाज के शीर्षस्थ वर्गों पर निर्भर थे; तथा उन्हें अपना स्वामी, सर्वेसर्वा एवं मुक्तिदाता मानते थे। हालात ऐसे थे कि अपने प्रत्येक कार्य में स्वार्थ को आगे रखने वाले तीनों शीर्षस्थ वर्गों के बीच अभूतपूर्व एकता थी, जबकि चौथा और बहु-संख्यक वर्ग सामान्य हितों के लिए एक-दूसरे के साथ स्पर्धा करता हुआ, अपनी प्रभावी ताकत खो चुका था। ‘दिमाग’ और ‘हाथों’ की उस अघोषित-अवांछित स्पर्धा में लाखों हाथ, कुछ सौ या हजार दिमागों की मनमानी के समक्ष बेबस थे। ‘बहुजन’ से बुद्ध का आशय ऐसे ही लोगों से था, जो समाज के प्रमुख कर्ता और उत्पादक वर्ग का हिस्सा होने के बावजूद उपेक्षित, तिरष्कृत, उत्पीड़ित और इस कारण विपन्नता का जीवन जीने को विवश थे। अपने जीवन-संबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिए वे ऐसे लोगों पर निर्भर थे जो उन्हीं के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन से शक्तिशाली होकर बहुजन-हितों के विपरीत कार्य करते थे।
कदाचित अब हम ‘बहुजन’ की अवधारणा तय करने की स्थिति में आ चुके हैं। अभी तक के विवरण से जो छवि बनती है, उसके अनुसार ‘बहुजन’ समाज का प्रमुख उत्पादक वर्ग है, जो जाति-धर्म के नाम पर आरंभ से ही अन्याय, असमानता और शोषण का शिकार रहा है। मानव सभ्यता उसके द्वारा बहाए गए पसीने की ऋणी है, फिर भी उसे किसी न किसी रूप में, उसके श्रम-लाभों से वंचित रखा गया है। वह श्रमजीवी वर्ग खेतों में काम करने वाला मजदूर हो सकता है; और गली-नुक्कड़ पर जूते गांठने वाला मोची भी। स्त्री और पुरुष के बीच भी कोई भेद नहीं। आजीविका इस उत्पादक वर्ग का धर्म है और उसका भरोसा भी। इसी कारण बुद्ध पूर्व भारत में वह आजीवक कहलाता था। उन दिनों प्रकृति पर उसे भरोसा था। वही उसकी श्रद्धा का पात्र भी थी। प्रकृति के प्रति सम्मान-भाव के साथ जिस दर्शन की रचना उसने की थी, ब्राह्मणों ने उसे लोकायत नाम दिया। खुद श्रेष्ठजन होने का दावा करते हुए वे लोकायत को सर्वसाधारण का दर्शन कहकर उपहास करते रहे। इसके बावजूद मेहनतकशों का यह दर्शन शताब्दियों तक आंडबर और याज्ञिक कर्मकांडों पर टिके परजीवियों के वैदिक धर्म-दर्शन को चुनौती देता रहा। इस तरह बहुजन की अवधारणा हमें सामाजिक न्याय की भावना से जोड़ती है। अपने साथ-साथ दूसरों के कल्याण के लिए जिम्मेदार बनाती है। यही उसका उद्देश्य है और यही अभीष्ट भी है। हालांकि सामाजिक न्याय की अवधारणा को लेकर मत-वैभिन्न्य हो सकते हैं।
मार्क्स ने पूंजीवादी तंत्र में उत्पीड़ित वर्ग को ‘सर्वहारा’ का नाम दिया था। ‘सर्वहारा’ और ‘बहुजन’ की आर्थिक अवस्था में अधिक अंतर नहीं होता। दोनों ही शोषण का शिकार होते हैं। उनमें से किसी को भी अपने श्रम के मूल्यांकन का अधिकार नहीं होता। फिर भी दोनों की सामाजिक स्थिति में अंतर है। मार्क्स का जन्म ऐसे समाज में हुआ था जिसमें केवल दो वर्ग थे– सामंती पूंजीपति और मजदूर (जिनमें किसान भी शामिल थे)। सामंती पूंजीपति अपनी स्थिति का लाभ उठाकर क्रमश: मजदूर और किसान का शोषण करते थे। मार्क्स की सर्वहारा की परिकल्पना ठेठ पूंजीवादी समाज में आर्थिक विपन्नता के शिकार श्रमिक-वर्ग के शोषण तथा उसके सामाजिक-सांस्कृतिक दुष्परिणामों तक सीमित थी। बहुजन की समस्याओं का मूल सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव तथा उनसे जन्मी आर्थिक विपन्नता है। प्रकारांतर में वही उसकी समाजार्थिक दुरावस्था का कारण बनते हैं।
मुख्यधारा से जुड़ने के लिए सर्वहारा को केवल आर्थिक बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। दूसरी ओर मुख्यधारा से जुड़ने के लिए बहुजन को, आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। चूंकि सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव की गति अत्यंत मंथर होती है, इसलिए बहुजन-कल्याण की राह सदैव अनेकानेक चुनौतियों से भरी होती है। लोकतांत्रिक परिवेश का लाभ उठाकर सर्वहारा अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है। पश्चिमी देशों में ऐसा हुआ भी है। जातीय वैषम्य से निपटने में लोकतांत्रिक सरकारें भी अपेक्षानुरूप सफल नहीं हो पातीं। जाति को व्यक्ति का निजी मामला बताकर प्रतिगामी शक्तियां सामाजिक परिवर्तन को टालती रहती हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव तथा अवसरों की कमी के कारण बहुजन के लिए आर्थिक विषमताओं के चक्रव्यूह को भेद पाना आसान नहीं होता। जटिल जाति-व्यवस्था तथा उसके साथ धर्म का चिरस्थायी गठजोड़, बहुजन के संघर्ष को कई गुना बढ़ा देते हैं।
‘बहुजन’ का प्रथम उल्लेख भले ही बौद्ध दर्शन में हुआ हो, इसकी भूमिका वैदिक संस्कृति की स्थापना के साथ ही बन चुकी थी। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया से भारत पहुंचे पशुचारी कबीलों ने खुद को ‘आर्य’ कहा था। इसका अर्थ बताया जाता है– ‘श्रेष्ठ’ अथवा ‘श्रेष्ठजन’। इस संबोधन का आशय था– मूल भारतवासी अथवा उनसे हजारों वर्ष पहले से इस देश में बस चुके जनसमूहों की संस्कृति को हेय मान लेना। भारत के मूल निवासी कौन थे? विद्वान दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में अग्रणी सिंधु सभ्यता को अनार्य सभ्यता मानते हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी से प्राप्त कंकालों के डीएनए रिपोर्ट से इसकी पुष्टि भी हो चुकी। उसके अनुसार सिंधुघाटी के निवासी ब्राह्मणों की अपेक्षा दक्षिण भारतीयों के बहुत ज्यादा करीब हैं। ‘हिंदू सभ्यता’ में डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों के आधार पर सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को चार नस्लों में बांटते हैं– आद्य-निषाद, भूमध्य सागर से संबंधित जन, अल्पाइन तथा मंगोल, किरात। आगे वे लिखते हैं कि आद्य-निषाद भारत महाद्वीप के निवासी थे। भूमध्यसागरीय लोग दक्षिण एशिया से आए थे। अल्पाइन पश्चिमी एशिया तथा मंगोल, किरात वर्ण के लोग पूर्वी एशिया से पलायन कर लंबी यात्रा के उपरांत भारत पहुंचे थे। इनके अलावा अलग-अलग नस्ल के संसर्ग से जन्मीं संकर नस्लें भी थीं। ऋग्वेदादि ग्रंथों में आर्यजनों ने इन्हीं नस्लों के सापेक्ष जो उनसे सहस्राब्दियों पहले इस प्रायद्वीप पर आकर बस चुकी थीं; तथा अपने श्रम-कौशल के बल पर समृद्ध सभ्यता की स्वामिनी थीं– अपनी वर्ण-श्रेष्ठता का दावा किया है। यदि उनके श्रेष्ठता संबंधी दावे को स्वीकार कर लिया जाए तो समकालीन बाकी नस्लें जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, तुलनात्मक रूप से अश्रेष्ठ अथवा निकृष्ट सिद्ध होती हैं।(डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी, ‘हिंदू सभ्यता’, पांचवा संस्करण [1975 : 46])
पुरातात्विक साक्ष्य इसे वैदिक ब्राह्मणों की आत्ममुग्धता से अधिक मानने को तैयार नहीं है। आज यह प्रमाणित है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता की अपेक्षा 1500-2000 पुरानी तथा उससे कहीं अधिक समृद्ध और सुव्यवस्थित थी। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की शुरुआत 3200 ईस्वी पूर्व से मानते हैं। 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक वह सभ्यता अपने वैभव के शिखर पर थी। उसके बाद उसके पराभव का दौर शुरू हुआ। 1500 ईस्वी पूर्व में आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया, उस समय वह सभ्यता करीब-करीब मिट चुकी थी। उसके अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, मेहरगढ़, राखीगढ़ी जैसे दर्जनों स्थानों पर आज भी सुरक्षित हैं। आधुनिक सिंधुवासियों को दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध नागरिक सभ्यता की नींव रखने वाला बताया जाता है। पुरातत्ववेत्ता इस बात पर सहमत हैं कि सिंधुघाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्रफल से भी अधिक था।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1500 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक के समय को विद्वान ‘अंधकार युग’ मानते हैं। इसलिए कि उस कालखंड के बारे में हमें प्रामाणिक तौर पर कुछ भी ज्ञात नहीं है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेदादि श्रुति ग्रंथों का रचनाकाल भी यही कालखंड है। हालांकि उन दिनों ये आश्रमों में गाए जाने वाले साधारण गीत रहे होंगे, जिनका महत्त्व मंदिरों में सुबह-शाम गाई जाने वाली आरतियों या सामान्य लोकगीतों से शायद ही अधिक रहा होगा। लेकिन ये ग्रंथ 600 ईस्वी पूर्व भी लिखित रूप में मौजूद थे, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। बुद्ध के जीवनकाल तक उपदेशों-गाथाओं को लिखकर रखने की परंपरा ही नहीं थी। आत्ममुग्ध ब्राह्मण तो वैसे भी अपने ‘गीतों’ को छिपाकर रखने के अभ्यासी थे। दूसरी ओर यह प्रमाणित तथ्य है कि सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को न केवल लिपि बल्कि संख्याओं, वास्तविक और प्रतीक मुद्रा तथा उनके अनुप्रयोगों की भी पर्याप्त जानकारी थी। उनके खेती के तरीके विकसित थे। इतने विकसित कि भारत में बीसवीं शताब्दी के आरंभ तक भी उनमें खास परिवर्तन नहीं हो पाया था। उनके पास सुनियोजित व्यापार-तंत्र और ऐसी भाषा थी, जिसके माध्यम से वे समकालीन सभ्यताओं से संवाद करने में सक्षम थे। जबकि आर्यजन महज घुमंतू पशुचारी कबीले थे। सभ्यता की दृष्टि से सिंधुवासियों से लगभग हजार-बारह सौ साल पिछड़े हुए थे। इसके बावजूद यदि उन्होंने स्वयं को ‘आर्य’ यानी ‘श्रेष्ठजन’ कहा, तो इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला या तो वे सिंधु घाटी की सभ्यता के प्राचीन वैभव तथा उसके महत्त्व से अपरिचित थे। अथवा यह संबोधन उन्होंने बहुत बाद में अनार्यजनों पर अपनी सांस्कृतिक विजय, वैदिक संस्कृति की स्थापना के समय चुना था। वे जानते थे कि अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताए बिना जीत को स्थायी बनाना और मूल-भारतवासियों पर ‘आर्यत्व’ को थोप पाना असंभव है। ईसा पूर्व चौथी-पांचवी शताब्दी तक यह लक्ष्य ही बना रहा। यह भी संभव है कि ‘आर्य’ संबोधन मध्य एशिया से प्रयाण से पहले ही उनके साथ जुड़ा हो और उसका अभिप्राय ‘श्रेष्ठजन’ न होकर कुछ और हो। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद, हिंदुओं का पवित्रतम ग्रंथ, जिसकी रचना ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए की गई है– माना जाता है। जबकि उसके आरंभिक उद्गाता ऋषियों में सभी वर्णों के रचनाकार सम्मिलित थे।
वेदादि ग्रंथों को ‘ब्राह्मण-ग्रंथ’ कहने की प्रवृत्ति बहुत बाद में, कदाचित यजुर्वेद की रचना के समय हुई। उस समय तक ‘पुरोहित’, ‘राजा’, सम्राट जैसे पदों का संस्थानीकरण हो चुका था। धर्म और राजनीति दोनों ही व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन चुके थे। वैदिक कर्मकांड जो उससे पहले तक मुख्यतः आश्रमों तक सीमित थे, वे राजा-महाराजाओं तथा धनी व्यापारियों के घर-आंगन तक पहुंचकर वैभव-प्रदर्शन के काम आने लगे थे। ब्राह्मणों की पूरी मेधा यज्ञादि कर्मकांडों को विस्तार देने में जुटी थी। चतुर्भुजी ब्रह्मा के हाथ में ‘ऋग्वेद’ के बजाय ‘यजुर्वेद’ की प्रति का होना, वैदिक धर्म-दर्शन की परपंरा में कर्मकांडों के बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है। ऐसे में ज्ञान की परंपरा का अवरुद्ध होना स्वाभाविक था। वही हुआ भी। उसके तुरंत बाद पौराणिक लेखन की बाढ़-सी आ गई, जिसने उस समय तक उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान और ऐतिहासिक तत्वों का मिथकीकरण करने का काम किया। स्वतंत्र मानस से सोचने के अनभ्यस्त, हताश-निराश बहुजन उन मिथकों को ही इतिहास मानकर– अपने वैभवशाली अतीत को बिसराते चले गए।
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in