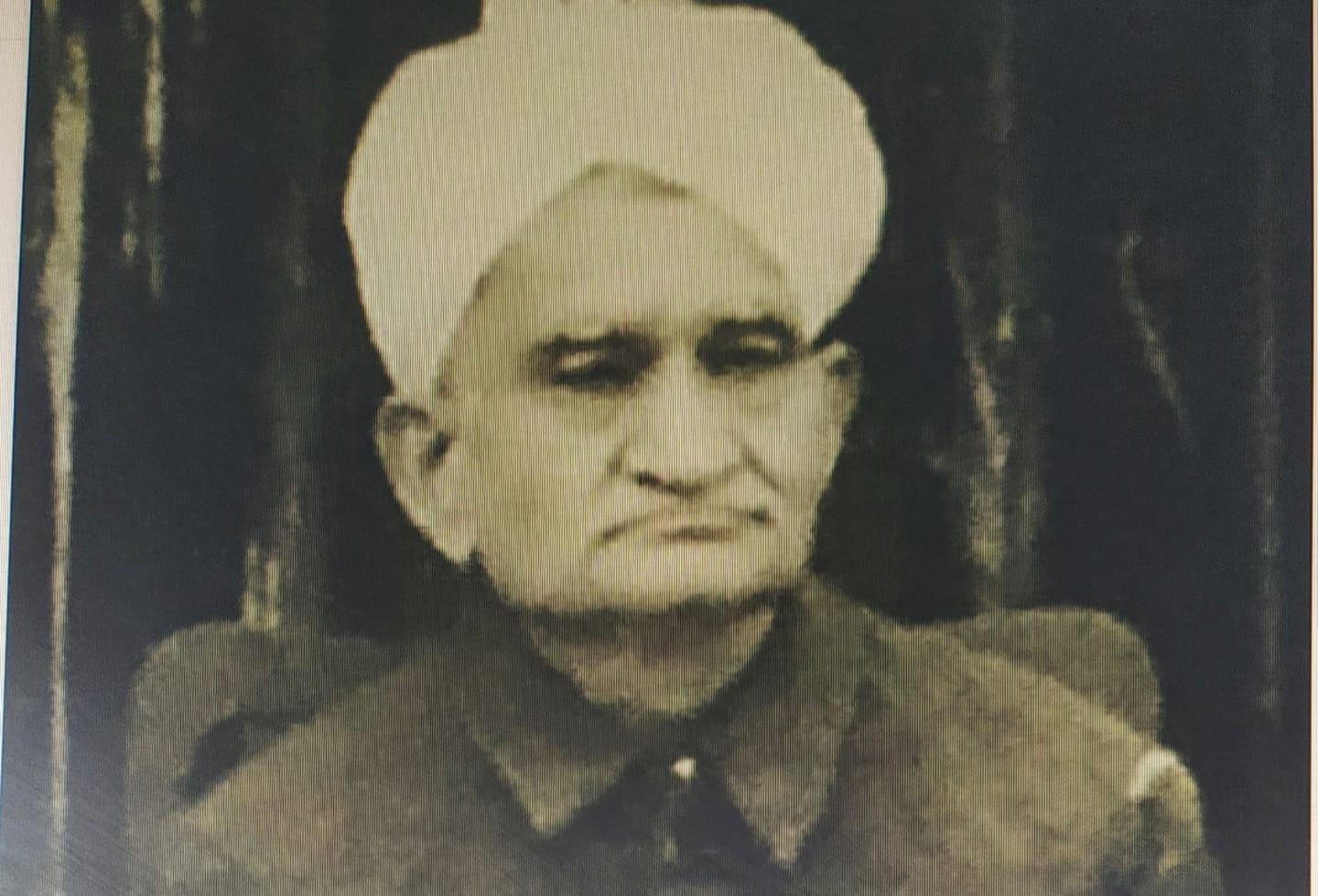जब कोई महापुरुष अज्ञानता में डूबे समाज के लिए अपना सब कुछ बलिदान करता है, तो प्रायः उसका अपना जीवन अनचीन्हा रह जाता है। कारण है कि जिस समाज के लिए वह संघर्ष करता है, वह समाज उसके कार्यों का समय रहते मूल्यांकन नहीं कर पाता। जागरूकता के अभाव में उसके अपने ही समाज के लोग उससे जुड़ी यादों को समय रहते सहेज नहीं पाते। जबकि विरोधी शक्तियां जो दूसरों से ज्यादा साधन संपन्न तथा पहुंच वाली होती हैं, वे उन समाजों तथा उनके मार्गदर्शकों को नेपथ्य में ढकेलने में पूरी ताकत लगा देती हैं। जब तक लोगों को उनके महत्त्व का पता चलता है, तब तक उसके जीवन की अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएं विस्मृत हो चुकी होती हैं। तुकाराम पडवळ (पडवल) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
पडवळ गैर-ब्राह्मण समुदाय के उन चंद बुद्धिजीवियों में से एक थे, जिन्होंने समाज सुधार का रास्ता अपनाया था। धनंजय कीर बताते हैं कि उनका जन्म भंडारी जाति में हुआ था। यह जाति मुख्यतः कोंकण तथा मुंबई के तटवर्ती क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके अधिकांश सदस्य ताड़ी उतारने का काम करते थे। वे अच्छे-खासे योद्धा भी थे। शिवाजी की सेना के प्रसिद्ध हेतकारी योद्धाओं का संबंध भंडारी जाति से ही था। इसी जाति के मायनाक भंडारी छत्रपति शिवाजी की नौसेना में एडमिरल थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवाजी की सेना के एक अन्य एडमिरल, दरिया सारंग के साथ मिलकर मय नाक ने 200 जहाजों के विशाल नौसैनिक बेड़े का नेतृत्व किया था।
पडवळ का जन्मस्थान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का वडावरे नामक गांव था। उनके जन्म-वर्ष को लेकर मतभेद हैं। कीर तथा रोसलिंड ओ’हेनलॉन ने उनका जन्म 1838 ईस्वी बताया है; जबकि अन्यत्र उनका जन्म-वर्ष 1831 (1836 भी) ईस्वी लिखा मिलता है। उनके परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। बस इतना पता चलता है उनके पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो चुकी थी। उस समय वे केवल दस वर्ष के थे। ऐसे में उनके चचेरे भाई की पत्नी उनकी मददगार बनकर आईं। उन्होंने तुकाराम को गोद ले लिया और अपने साथ उन्हें भी मुंबई ले आईं, जहां वे छोटी-मोटी नौकरी से अपना गुजारा करती थीं। जाहिर है कि तुकाराम का बचपन संघर्ष में बीता था। उनकी पढ़ाई की शुरुआत मिशनरी स्कूल से हुई थी। हाई स्कूल तक की पढ़ाई उन्होंने राबर्ट मनी स्कूल से की थी। स्कूली दिनों में ही वे आधुनिक विचारों के संपर्क में आए। फलस्वरूप समाज और राजनीति को लेकर आलोचकीय दृष्टि पनपने लगी थी।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी पडवळ बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में तेज थे। मराठी के अलावा अंग्रेजी का भी ठीक-ठाक ज्ञान था। उम्र के साथ-साथ साहित्यिक तथा वैचारिक पुस्तकें पढ़ने का शौक लगातार बढ़ता गया। अध्ययन पूरा करने के बाद वे रेलवे में काम करने लगे। कुछ समय के लिए उन्होंने वॉलकोट कंपनी में भी काम किया। इस बीच उन्होंने होमियोपैथी का ज्ञान अर्जित किया और प्रैक्टिस करने लगे। उनके पास आने वाले लोगों में आमजनों की संख्या अधिक थी। पडवळ उनके साथ बड़े प्यार और सम्मान के साथ पेश आते। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण उन्होंने कई अभावों को झेला था। जीवन की कटुताओं ने उन्हें सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाया था। उन्होंने युवावस्था में ही समाज सेवा को अपना लक्ष्य मान लिया था। समय के साथ वे समकालीन सुधारवादी नेताओं के संपर्क में आए तथा कुछ ही समय में अपने समय के सभी प्रमुख आंदोलनों का हिस्सा बन गए। धीरे-धीरे समाज में उनका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। पडवळ के समाज सेवा का दायरा बड़ा था। उन्होंने गरीब जनों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, औषधालय चलाए। यहां तक कि अनपढ़ मजदूरों की शिक्षा के लिए भी काम किया।
थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हेलना ब्लॉवत्स्की तथा हेनरी ऑलकोट ने 1875 में न्यूयार्क में की थी। 2 मई, 1880 को पडवळ भी उससे जुड़ गए। थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष तथा संस्थापक हेनरी एस. ऑलकॉट से उनके गहरे संबंध थे। एक तरह से वे उनके भरोसेमंद दोस्त और मददगार थे। आगे चलकर जब सोसाइटी के शीर्ष पदाधिकारी मद्रास प्रांत के अडयार कार्यालय में चले गये तब तुकाराम पडवळ उसके मुंबई दफ्तर का कामकाज देखने लगे। उन्होंने सोसाइटी का पतंजलि योगशास्त्र, सांख्य कारिका, राजयोग, गीता आदि प्रकाशनों में सहयोग दिया। भारतीय समाज के लिए वह परिवर्तनकारी का दौर था। तरह-तरह के अस्मितावादी आंदोलन उभर रहे थे। पडवळ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रगतिशील आंदोलनों का हिस्सा बने थे। माना जाता है कि वे थियोसोफिकल सोसाइटी की भारतीय शाखा के गठन के साथ ही उससे जुड़ चुके थे। सन् 1889 में जब उन्होंने सोसाइटी से अलग होने का फैसला किया, वे उसकी दक्षिणी शाखा के महासचिव पद पर थे। सोसाइटी से अलग होने का कारण उन्होंने अत्यधिक जिम्मेदारियां तथा अंग्रेजी पर अपनी कमजोर पकड़ को बताया था। उन दिनों वे मराठी के भक्तिसाहित्य की खोज और प्रकाशन के काम में जुटे थे, जो थियोसोफिकल संस्था के काम जितना ही महत्त्वपूर्ण था।
उत्साही प्रकाशक
उन दिनों प्रकाशन संस्थान या तो सरकार के अधीन थे, या फिर मिशनरियों का। भारतीय भाषाओं के लिए बस गिने-चुने प्रकाशक काम करते थे। यह देखते हुए पडवळ ने स्थानीय भाषाओं में प्रकाशन के लिये तत्वविवेचक नाम से प्रकाशन संस्थान की शुरुआत की। वह भारत के आरंभिक प्रकाशन संस्थानों में एक था। इस संस्थान के माध्यम से जो बड़ा काम उन्होंने किया वह था, 1889 में सतरहवीं शताब्दी के संतकवि तुकाराम के अभंगों ‘तुकारामबावा आणि त्यांचे शिष्य यांच्या अभंगांची गाथा’ (तुकारामबाबा और उनके शिष्यों की अभंग गाथा) का प्रकाशन। अभंगों को खोजने-संकलित करने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। संत साहित्य पर उनके द्वारा प्रकाशित दूसरी पुस्तक थी– ‘एकनाथ महाराजांच्या अभंगांची गाथा’ (एकनाथ महाराज के भक्ति काव्य का कथा)। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1903 में आया था।
संत तुकाराम, नामदेव आदि महाराष्ट्र के लोकजीवन की आत्मा थे। पेशवाई के दौरान ब्राह्मणों ने उसपर कब्जा कर लिया था। इससे पडवळ की छवि धुन के पक्के, सुधारवादी साहित्यकर्मी की बनी। थियोसोफिकल संस्था की संस्थापकों में से एक हेलेना ब्लवॉत्स्की ने उन्हें ऐसा असाधारण सुधारवादी बताया था, जो एक सनक के लिए हजारों रुपए खर्च करने को तैयार रहता है।[1] संत तुकाराम के अंभंगों को एकत्र करने में उन्होंने अपना बहुत-सा श्रम और संसाधन खर्च किए थे। जैसे ही उन्हें पता चलता कि अमुक व्यक्ति या संस्था के पास संत तुकाराम के अभंगों के मिलने की उम्मीद है, वे तुरंत वहां पहुंच जाते थे। वस्तुतः एक प्रकाशक, सुधारवादी, समर्पित थियोसोफिस्ट, आम आदमी के डॉक्टर के रूप में उनकी पहचान इतनी प्रगाढ़ थी कि लेखक के रूप में किया गया उनका योगदान दब-सा गया था।
उदार डॉक्टर
अपने अनुभव तथा ज्ञान से जनसाधारण को लाभान्वित करने के लिए होमियोपैथिक चैरिटेबिल औषधालय की स्थापना की थी। फलस्वरूप लोगों की समस्याओं तथा उनके दुख-दर्दों को करीब से जानने अवसर मिला। दुकानों, छोटी-छोटी फर्मों पर अनेक ऐसे लोग थे जो चपरासी, कुली, मजदूर जैसे काम करते थे। उनमें से अधिकांश अनपढ़ थे। उन्हें शिक्षित करने के लिए पडवळ ने मुंबई में वयस्क कक्षाओं की शुरुआत की। वे जोतीराव फुले द्वारा शूद्रातिशूद्रों की शिक्षा के लिए चलाए गए अभियान से प्रभावित थे। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने मजदूरों, शिल्पकारों तथा अस्पृश्य कहे जाने वाले बच्चों के लिए स्कूलों की स्थापना की थी। ऐसे सुधारवादी कदमों से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी।[2] होमियोपैथी की प्रैक्टिस के अलावा वे व्यापार भी करते थे। इसके लिए एक यूरोपियन कंपनी के साथ समझौता था। सरकार ने आम जरूरत की वस्तुओं के व्यापार में अप्रत्यक्ष् कर की घोषणा की तो उसका चौतरफा विरोध होने लगा। उनके साथ मिलकर पडवळ भी आंदोलन में कूद पड़े तथा बढ़-चढ़कर सरकार का विरोध करने लगे।
साहसी लेखक
पडवळ ने धर्म तथा जाति-आधारित शोषण को करीब से देखा था। धर्म के नाम पर पुजारी अनपढ़ लोगों को किस तरह से लूटते हैं, इसका उन्हें करीबी अनुभव था; और इस संबंध में उनके विचार जोतीराव फुले से मेल खाते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जाति-व्यवस्था ही निचले तबके के सभी दुखों की जड़ है। इसलिए उन्हें जागरूक करने तथा उनमें अधिकार-चेतना जगाने से महत्त्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। इसके लिए उन्होंने मराठी साहित्य और संस्कृति के अलावा भारतीय धर्मों तथा धर्मशास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था। ‘गुलामी’ (अध्याय 10) में जोतीराव ने लिखा था कि शंकराचार्य के उदय के साथ, ब्राह्मणों की ज्यादतियों को, जिनपर बौद्ध धर्म ने अंकुश लगाया हुआ था, पुनर्जीवन मिल गया गया। शंकराचार्य के उकसावे पर उसके लोगों ने अनेक बौद्धों को तेली के कोल्हू में पिलवा दिया तथा उनके अनेक ग्रंथों को आग के हवाले कर दिया। ठीक यही विचार पडवळ के भी थे। उनका मानना था कि जाति-व्यवस्था ब्राह्मण धर्म की ज्यादतियों की सबसे बड़ी संरक्षक है। उसके रहते बहुसंख्यक गैर-ब्राह्मणों की मुक्ति संभव ही नहीं है। यह ब्राह्मणों के दोहरे मापदंडों पर टिकी है।
लोग इस सच को जानें, इस उद्देश्य से पडवळ ने ‘जातिभेद विवेकसार : जातीय विभाजन पर विमर्श’ शीर्षक पुस्तक की रचना की थी। इसके माध्यम से उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों तथा उनमें निर्धारित शूद्रों के कर्तव्यों एवं अधिकारों को चुनौती दी थी। इन ग्रंथों की मूल स्थापना थी कि कलियुग में, जो सबसे पतित कालखंड है, चतुर्यामी वर्णव्यवस्था के केवल दो वर्ण शेष हैं – पहला ब्राह्मण जिन्होंने अपनी (तथाकथित) वर्णशुद्धता को बनाए रखा है; दूसरा शूद्र जिसमें अंतर-जातीय मिश्रण से पैदा हुई वर्णसंकर जातियां शामिल हैं।[3] पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि हिमालय से कन्याकुमारी तक सभी अनेकानेक उपजातियों और गोत्रों में बंटे होने के बावजूद ब्राह्मण खुद को एक-दूसरे का भाई समझते हैं। दूसरी ओर बहुसंख्यक शूद्र हैं, जो पेशों के आधार पर अनेक जातियों और उपजातियों में बंटे हैं। उनके बीच गहरे मतभेद तथा ऊंच-नीच की भावना है।

दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में अनेक ऐसे हैं जो गुजराती ब्राह्मण का छुआ नहीं खाते; जबकि कुछ ब्राह्मण दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के साथ अन्न-व्यवहार करते हैं। हिंदुस्तान के ब्राह्मण बाहर के ब्राह्मणों का भोजन नहीं करते। वे अपना भोजन खुद पकाते हैं। मानते हैं कि यदि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया तो अन्न महाराज कुपित हो जाएंगे।[4] इसके बावजूद वे सभी एक-दूसरे को ब्राह्मण मानकर भाईचारा निभाते हैं। यह भावना शूद्रों में नदारद है। पुस्तक के उपोद्घात में उन्होंने मनुस्मृति से अनेक श्लोक दिए थे, उनमें कुछ के अर्थ हैं–
जिनके भरोसे ये लोक टिके हैं, वेद जिनके ऊपर आश्रित हैं। ऐसे ब्राह्मणों को जीने की इच्छा रखने वाला भला कौन व्यक्ति दुख पहुंचाने का साहस करेगा। अग्निदेव चाहे वेदमंत्रों द्वारा प्रकट हो या अन्य तरीकों से, वे सभी जगह महान होते हैं। उनकी ज्वाला श्मशान में भी अपवित्र नहीं होती और यज्ञों में आहुतियां डालने पर फिर से तेजवंत हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मण भी सर्वथा पूज्य और महान देवता है। वह चाहे जितने निंदित कर्म करें, सदैव वंदनीय होता है।[5]
‘जातिभेद विवेकसार’ के पहले संस्करण के प्रकाशक थे– वासुदेव नवरंगे। ये वही नवरंगे थे जिनका लोहे का व्यवसाय था तथा जिनकी साझेदारी में जोतीराव ने लोहे के उपकरण बेचने की दुकान खोली थी। गैर-ब्राह्मण समाज में जन्मे नवरंगे खुद अपने समय के बड़े समाज सुधारक थे। वे प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्यों में से थे। सुधार की शुरुआत अपने ही घर और जीवन से होनी चाहिए, इस सिद्धांत का अनुकरण करते हुए, 1870 ईस्वी में उन्होंने एक विधवा को अपनी जीवनसंगिनी बनाया था। उन दिनों यह बड़े साहस का काम था।[6] सन् 1863 में जब वे व्यापार के सिलसिले में लंदन में थे, तब एक अन्य सुधारवादी मामा परमानंद के माध्यम से उन्हें जोतीराव फुले के बारे में जानकारी मिली थी। तब तक जोतीराव शिक्षण संस्थाओं से औपचारिक रूप से अलग हो चुके थे और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। कुछ अवधि के लिए लंदन में रह रहे वासुदेव नवरंगे ने जोतीराव फुले को अपना कारोबार संभालने का जिम्मा दिया। चूंकि दोनों का लक्ष्य एक ही था, इस कारण उस समय जो उन सबके बीच मैत्री हुई और वह अंत तक बनी रही। तुकाराम तात्या पडवळ इस मित्रमंडली का महत्त्वपूर्ण हिस्सा थे।
पेशवाई शासनकाल में शूद्रातिशूद्रों पर इतने अत्याचार किए गए थे कि कोई भी स्वाभिमानी उनके बारे में सुनकर आक्रोश से भर जाता था। पडवळ भी उससे बचे न थे। वे मानते थे कि जाति-व्यवस्था जनसाधारण के शोषण तथा उत्पीड़न का बड़ा कारण है। जाति को लेकर ब्राह्मणों के दोहरे मापदंड हैं। जिन तर्कों के आधार पर वे ब्राह्मणेतर जातियों को हेय कहकर उनका दमन करते हैं, उन्हीं तर्कों के आधार पर वे खुद को शिखर पर रखते हैं। एक ओर संसार को माया बताकर भौतिक सुखों को तुच्छ बताते हैं, दूसरी ओर विभिन्न अवसरों में अनेकानेक कर्मकांडों के नाम पर छत्तीस प्रकार से व्यंजनों से भोग लगाकर ईश्वर को प्रसन्न करने का नाटक करते रहते हैं। उनके लिए धर्म आस्था से ज्यादा आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा, समृद्धि तथा विशेषाधिकार का संबल है। इस काम में धर्म उनके लिए भरोसेमंद मददगार का काम करता है।
ब्राह्मण श्रेष्ठता के दावे मिथ्या, सभी वर्ण रक्त-संकरता के शिकार
पडवळ को विश्वास था कि लोगों के आत्मविश्वास को जगाकर उन्हें दयनीय अवस्था से उबरने के लिए तैयार करने से पुनीत कार्य कोई और हो ही नहीं सकता। इसके लिए धर्म और जाति की आड़ में छिपे ब्राह्मणवादी प्रपंचों को उजागर करना जरूरी था। ब्राह्मणों का दावा था कि शूद्र रक्त-संकरता से जन्मे हैं। यही उनके हिसाब से विभिन्न जातियों के उदय का कारण था। अमुक वर्ण जाति का पुरुष यदि अमुक जाति-वर्ण की स्त्री के साथ संसर्ग करेगा तो उत्पन्न संतान अमुक जाति-वर्ण की होगी, इस तरह के तर्कहीन समीकरण पुराणों, स्मृतियों आदि धर्मशास्त्रों में आए हैं। पडवळ का तर्क था कि रक्तशुद्धता के ऐसे दावे शूद्र तथा ब्राह्मण के स्तरीकरण, उनके बीच ऊंच-नीच के निर्धारण का आधार नहीं हो सकते। उन्होंने तर्क देकर बताया था कि कथित रक्त-संकरता शूद्र तथा ब्राह्मण के बीच अंतर का कारण तो नहीं, समानता का कारण जरूर बन सकती है।
दरअसल ब्राह्मण जिसे रक्त-संकरता कहते हैं, उसके लिखित उदाहरण शूद्रों से कहीं अधिक ब्राह्मणों के बारे में उपलब्ध हैं। अपने तर्क के समर्थन में पडवळ ने उन ऋषियों के बारे में बताया था जो तथाकथित शूद्र के रूप में जन्मे थे, लेकिन अपने अध्यवसाय, ज्ञान, तर्क, विद्वता, सदाचरण के बल पर उन्होंने पूरे लोक को प्रभावित किया था। उनके उच्चकोटि के ज्ञान तथा तत्कालीन समाज में प्रतिष्ठा के कारण ब्राह्मण भी उन्हें उच्च कुलीन मानने को विवश हुए थे। उन्होंने जिन ऋषियों के नाम गिनाए थे, उनमें वाल्मीकि (कोली, मछुआरे), सांख्य, कपिल और पराशर (अति-शूद्र), टंक (चमार), कौंडिन्य और दीर्घतमस (कुंवारी मां), अगस्त्य (घट), वशिष्ट (रंभा), व्यास (मछुआरा) आदि शामिल थे।[7] पुस्तक में सुदास, विश्वामित्र, वेन, मंधाता, पुरुरवा आदि ऐसे लोगों की सूची भी दी थी जो क्षत्रियकुल में जन्म लेने के बावजूद ब्राह्मण मान लिए गए थे। साथ ही ऐसे लोगों का भी उल्लेख था जिन्हें मर्यादाहीनता के कारण ब्राह्मण वर्ण से पदावनत किया गया था।
‘जातिभेद विवेकसार’ का अंग्रेजी शीर्षक उन्होंने ‘जातिभेद विवेकसार : रिफ्लेक्शन ऑन दी इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट’ रखा था। जातीय विमर्श पर किसी भी गैर-ब्राह्मण की यह पहली रचना थी, अभी तक ब्राह्मण शूद्रों को रक्त-संकरता का शिकार बताकर जातियों में बांटते आये थे। अब शूद्र उन्हें वर्णसंकरता का शिकार बताकर उनके श्रेष्ठता दंभ को निशाना बना रहे थे। इससे ब्राह्मण खेमे का तिलमिला उठना स्वाभाविक था। एक ओर प्रगतिशील गैर-ब्राह्मण बुद्धिजीवी पुस्तक की प्रशंसा कर रहे थे, वहीं ब्राह्मण (तथाकथित) प्रगतिशील और परंपरावादी दोनों पडवळ से बुरी तरह चिढ़े हुए थे। मराठी द्विभाषिक पत्रिका ‘ज्ञानप्रकाश’ के संपादकगण प्रगतिशील होने का दावा करते थे। ‘जातिभेद विवेकसार’ ने उन्हें अपना मुखौटा उतारने को विवश कर दिया था। पडवळ की आलोचना करते हुए 1862 में ‘ज्ञानप्रकाश’ के एक संपादकीय में लिखा था कि यह पुस्तक, ‘उन (ब्राह्मणों) के पूर्वजों का अपमान करती है’। दरअसल जिन धर्मशास्त्रों के बल पर ब्राह्मण अभी तक रक्तशुद्धता का दावा करते आए थे, पडवळ ने उन्हीं धर्मशास्त्रों को आधार बनाकर उनके रक्तशुद्धता संबंधी दावे को मिथ ठहरा दिया था।
एक हिंदू कौन है?
‘जातिभेद विवेकसार’ के लेखक के रूप में नाम गया था– एक हिंदू। ‘एक हिंदू’ कौन है, अधिकांश के लिए यह लंबे समय तक रहस्य ही बना रहा। काफी बाद में धनंजय कीर ने इस रहस्य से पर्दा हटाते हुए लिखा कि ‘जातिभेद विवेकसार’ के रचियता, ‘एक हिंदू’ कोई और नहीं, तुकाराम तात्या पडवळ थे।[8] इसके स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें लगा कि नाम का खुलासा करने से पुस्तक की प्रतिष्ठा में जरा भी वृद्धि होगी तो वे नाम का खुलासा अवश्य कर देंगे। पुस्तक उन्होंने देशवासियों को समर्पित की थी–
“मेरे देशवासियो!
यह निबंध मैंने आपको समर्पित किया है। इस उम्मीद में कि यह आपके काम आएगा। यदि यह हिंदू समाज में व्याप्त जातिवाद तथा उसके दुष्परिणामों के बारे में आपकी जानकारी में वृद्धि कर सका तो मैं समझूंगा कि इसे लिखने में मैंने जो श्रम किया है, वह व्यर्थ नहीं गया है।
आपका हमेशा भरोसेमंद
आपका विनम्र शुभाकांक्षी
एक हिंदू”[9]
‘जातिभेद विवेकसार’ का प्रथम संस्करण (1861), अपेक्षाकृत लघ्वाकार, मात्र 59 पृष्ठों का था। स्वयं पडवळ को उससे संतोष न था। धर्म-प्राण जनता उसे स्वीकारेगी, या नकार देगी यह ऊहापोह पुस्तक लिखते समय ही उनके मन में था। लेखकीय असंतोष तथा स्वीकार्यता की चिंता, पुस्तक की भूमिका में साफ झलकती थी–
“मैं इस ग्रंथ को विस्तार में लिखना चाहता था, परंतु इस संदेह के चलते कि इस पुस्तक को पाठकों का समर्थन मिलेगा या नहीं, मैंने इसे संक्षिप्त रखा है। यदि पुस्तक के प्रति पाठकों की रुचि दिखी तो दूसरे संस्करण में श्रुति-स्मृति आदि से व्यापक संदर्भ जोड़े जाएंगे।”[10]
प्रथम संस्करण पर ‘पुणे आब्जर्वर’, ‘ज्ञानोदय’, ‘बांबे गार्जियन’ आदि में अनुकूल प्रतिक्रियायें छपी थीं। ‘जातिभेद विवेकसार’ जोतीराव फुले के आंदोलन के फलस्वरूप सक्रिय हुई शूद्र-प्रतिभा का सार्थक हस्तक्षेप ऐसा माना गया था। रोसलिंड ओ’हेनलॉन लिखती हैं– “जहां तक मुझे पता है ‘ए क्रिटिक ऑफ कास्ट डिवीजंस’ धर्म के विरोध में लिखी गई और मराठी में प्रकाशित पहली पुस्तक थी। हिंदू धर्म में जातीय स्तरीकरण की आलोचना में लिखी गई पुस्तकों में ‘जातिभेद विवेकसार’ स्पष्ट रूप से ऐसा प्रयास था, जिसे निचले जातीय समूहों के दृष्टिकोण से लिखा गया था। इकतरफा दृष्टिकोण के बावजूद पुस्तक में मराठा-कुनबी जाति में व्याप्त वर्णभेद से संबंधित बेशकीमती सामग्री संजोयी गई थी … ”[11]
प्रथम संस्करण पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रियाओं से उत्साहित लेखक ने अपने आश्वासन के अनुरूप, नए संस्करण में पुराणों, उपनिषदों आदि से संदर्भ देकर पुस्तक को और अधिक उपयोगी बना दिया था। 1865 में निकले परिवर्धित संस्करण में 170 पृष्ठ थे। इसकी कीमत रखी गई थी चौदह आना। इस बार इसके प्रकाशक थे– जोती गोविंदराव फुले। फुले ने पुस्तक को अपने खर्च पर प्रकाशित किया। ‘जातिभेद विवेकसार’ की जो सामग्री थी, और प्रथम संस्करण के बाद से ही ब्राह्मण हलके में जैसा प्रतिरोध जारी था, उसे देखते हुए व्यावसायिक प्रकाशक उसके परिवर्धित संस्करण के छापने में रुचि दिखाता, इसकी कम ही संभावना थी। जोतीराव शुरू से ही कहते आए थे कि जाति-व्यवस्था से सबसे ज्यादा लाभ ब्राह्मणों को है, वही इसके मजबूत होने और बने रहने के लिए जिम्मेदार हैं। अतएव बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को है। ‘जातिभेद विवेकसार’ के परिवर्धित संस्करण के प्रकाशक के रूप में जोतीराव फुले का नाम जुड़ना, उसके प्रचार की दृष्टि से भी लाभदायक था। जैसी उम्मीद थी, पाठकों ने नए संस्करण को भी हाथों-हाथ लिया था। पुस्तक की एक हजार प्रतियां देखते-देखते बिक गईं। उन दिनों यह बहुत बड़ी संख्या थी। पुस्तक का तीसरा संस्करण कतिपय विलंब से सन् 1885 में प्रकाशित हुआ था।
ध्यातव्य है कि 1848 के आसपास जब जोतीराव फुले ने समाजसेवा के क्षेत्र में कदम रखा था, तब ब्राह्मण बुद्धिजीवियों का एक वर्ग सामाजिक सुधार के पक्ष में खड़ा था, उसी के एक हिस्से का जोतीराव को स्कूल संचालन के लिए पूरा समर्थन मिला था। उनमें कई जोतीराव फुले के स्कूली जीवन के मित्र थे। उस समय सरकार भी जातीय उत्पीड़न के शिकार रहे वर्गों की मदद करना चाहती थी। जोतीराव फुले ने शूद्रातिशूद्रों के लिए पाठशालाओं की शुरुआत की तो, ब्राह्मणों की नाराजगी की परवाह न करते हुए स्थानीय प्रशासन ने उनका भरपूर समर्थन किया था। उदारवादी दिखने की उम्मीद में, यथास्थिति के पोषक ब्राह्मण भी, सुधारवादियों से आ मिले थे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया द्वारा 1 नवंबर, 1858 को जारी प्रोक्लेमेशन (घोषणा) के बाद सरकार ने ब्राह्मणों को नाराज न करने की नीति के चलते, सीधे हस्तक्षेप से बचना शुरू कर दिया था। बदलते परिवेश में ब्राह्मणों की नई पीढ़ी अपने परंपरागत विशेषाधिकारों को लेकर सजग थी। सन् 1857 के बाद उमड़ी जनभावनाओं को राष्ट्रवाद का नाम देकर वह सुधारवाद के विरोध में आ डटी थी। इसकी समानांतर प्रतिक्रिया कथित शूद्रातिशूद्र वर्गों में हुई थी। ‘जातिभेद विवेकसार’ जैसी पुस्तकों को मिल रही सफलता उसी चेतना का सुफल था।
दूसरे संस्करण की प्रस्तावना में पडवळ ने लिखा था कि भारतीय समाज में व्याप्त विकृत जातिवाद ने भारतीय मनीषा को जकड़ा हुआ है। भारतीय समाज को उससे मुक्ति दिलाने से महत्त्वपूर्ण दूसरा कोई काम नहीं है। उन्होंने लिखा था कि सिर्फ जन्मना जाति के बल पर ब्राह्मणों ने समाज में सर्वोच्च जगह बनाई है। इसके लिए उनमें कोई विशिष्ट योग्यता नही है। जातिभेद का असल उद्देश्य लोगों के दिमाग में यह बिठाना है कि शूद्र, चाहे जितना नेक, उदार और संयमी क्यों न हो, वह कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता।
दूसरे संस्करण ने बाजार में आते ही हलचल मचा दी थी। उसके विरोध में पूना के एक ब्राह्मण ने लिखा था कि पुस्तक का लेखक हिंदुत्व के साये में रहकर भी उसका दुश्मन बना हुआ है। एक ब्राह्मण ने मराठी पत्रिका ‘ज्ञानप्रकाश’ में छपे एक पत्र के जरिए अपना गुस्सा जताया था। वह देवरुख ब्राह्मण था जो पुस्तक में चितपावन ब्राह्मणों के, पद्म पुराण के सह्याद्रिखंड से दिये गए एक श्लोक से कुपित था। पुस्तक के पहले संस्करण में, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशात्रों में की गई मनमानी हेराफेरी तथा हिंदू नैतिकता पर अनावश्यक दबदबे के लिए ब्राह्मणों की आलोचना थी। जबकि दूसरे संस्करण में ब्राह्मणों के दोहरे चरित्र की निंदा की गई थी। उसकी शैली आक्रोशयुक्त एवं प्रहारात्मक थी। पुस्तक के पहले संस्करण में जातिभेद पर अपने क्षोभ को दर्शाते हुए पडवळ ने लिखा था–
“जातिभेद न केवल अनावश्यक है, बल्कि यह मानव सभ्यता का अनर्थ करने वाला है। इससे सामाजिक बुराई और झगड़े पैदा हुए। ऊंची जातियों को गरीबों से कुछ इज़्ज़त मिलती है, लेकिन इसके अलावा जातिभेद का कोई फ़ायदा नहीं है। यवन, म्लेच्छ वगैरह अजनबी हैं, बाहर से आए हैं। लेकिन ऊंची जातियां (वरकाड जाति के लोग) छोटी जातियों को भी अजनबी मानकर उनके साथ भेदभाव करती हैं। इस अन्याय की कोई सीमा नहीं है।”[12]
पुस्तक में पडवळ ने बौद्ध धर्म के उदारवादी दृष्टिकोण की प्रशंसा की थी। उन्होंने लिखा था कि बौद्ध लोग जाति-भेद नहीं रखते थे। उसे मिले समर्थन के कारण समाज पर ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में कमी आई थी। इस कारण वे दक्षिण की ओर पलायन को विवश हो गए थे। आगे चलकर उन्हीं में से एक, शंकराचार्य नामक ब्राह्मण ने हिंदू धर्म में सुधार करते हुए उन अनेक विचारों (जैसे वैदिक हिंसा) को छोड़ दिया, जिनके कारण बौद्ध तथा दूसरे श्रमण धर्म उसकी आलोचना करते आए थे।
पडवळ ने शंकराचार्य को हिंदू धर्म के सुधारवादी का श्रेय दिया था; जबकि सच तो यह है कि शंकराचार्य का सुधार कार्य बिखरी हुई ब्राह्मणवादी ताकतों को एकजुट करने तथा उनके अधिकारों की संरक्षा तक सीमित था। अपने भाष्यों के जरिये उन्होंने प्राचीन स्मृतियों, पुराणों तथा महाकाव्यों में पसरी विभेदकारी वर्णव्यवस्था को नए सिरे से स्थापित किया; जिसके कारण हिंदू धर्म शताब्दियों तक निरंतर पतनशील बना रहा। यही कारण है कि आने वाले बुद्धिजीवियों, समाजसुधारकों यथा पेरियार, डॉ. आंबेडकर आदि को, वास्तविक जाति-उन्मूलन के लिये, ब्राह्मण धर्म के उन्मूलन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ा।
संदर्भ :
[1] केतकी जयवंत, सेकुलराइजिंग कास्ट [2021 : 86-87]
[2] धनञ्जय कीर, महात्मा जोतिबा फुले [1960 : 94]
[3] केतकी जयवंत, सेकुलराइजिंग कास्टमैपिंग: नाइंटिंथ सेन्चुरी एन्टी-कास्ट पॉलिटिक्स [2021 : 13]
[4] जातिभेद विवेकसार, उपोद्घात [1865 : 1-2]
[5] मनुस्मृति 9।317-319
[6] धनञ्जय कीर, महात्मा जोतिबा फुले [1960 : 93]
[7] जातिभेद विवेकसार [1865 : 17 ]
[8] क्या पुस्तक पर लेखक के रूप में अपना नाम न देने का कारण ब्राह्मणों का डर था? इस संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। उससे कुछ ही वर्ष पहले, 1856 में ब्राह्मण जोतीराव फुले पर जानलेवा हमला करा चुके थे। जोतिबा के साहस तथा हत्या के लिए भेजे गये व्यक्तियों के हृदय परिवर्तन के कारण बहुत नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन यह संदेश लोगों में गया था कि अपने विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिए ब्राह्मण किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। फिर अपनी पहचान के छिपाने वाले पडवळ अकेले नहीं थे। परमहंस मंडली के सदस्य भी अपनी पहचान गुप्त रखते थे। उसके वरिष्ठतम सदस्यों में एक दादोबा पांडुरंग तो मंडली की (गोपनीय) बैठकों नियमित रूप से बैठक-स्थल पर जाते थे। लेकिन बैठक में सीधे शामिल होने के बजाय बराबर के कमरे में बैठकर चुपचाप उसकी कार्यवाही को जानने की कोशिश करते थे।
[9] प्रिय स्वदेशबंधूनो!
हा लहानसा निबंध मी तुम्हांस उपयोगी पडेल या आशेनें सादर करितों। याच्या योगानें तुम्हांतून एकाची तरी, आपल्या लोकांमध्यें जो सामंत जातिभेद चालत आहे न्याच्या वास्तविक स्वरूपाविषयीं आणि तज्जनित परिणामाविषयीं खात्री झाली असतां, माझी मेहनत व्यर्थ गेली नाहीं, असे समजायास भला कारण होईल।
मुक्काम मुंबई,
तारीख 1 आगष्ट सन 1861
आपका नम्र अभिष्टचिंतक
एक हिंदु
[10] जातिभेद विवेकसार [1865], जोति गोविंदराव फुले, पुणे
[11] रोसलिंड ओ’हेनलॉन, कास्ट, कन्फलिक्ट, एंड आइडियोलॉजी [1985 : 42]
[12] केतकी जयवंत, रिशेपिंग दि फिगर ऑफ शूद्र : तुकाराम पडवळ, जातिभेद विवेकसार [2023 : 388)
(संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in