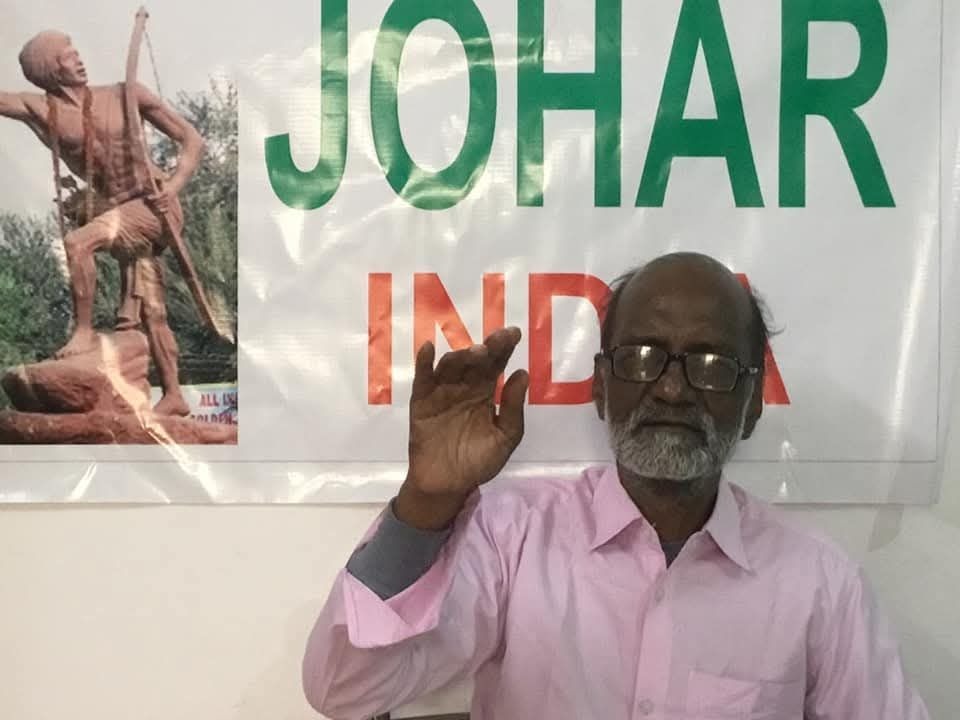बच्चों के लालन-पालन के संदर्भ में भारत के समक्ष दो प्रमुख चुनौतियां उपस्थित हैं। पहली यह कि लड़कियों और लड़कों का लालन-पालन किस तरह एक जैसा हो अर्थात उनके बीच कोई भेदभाव न किया जाए। और दूसरा हम बच्चों को यह कैसे समझाएं कि श्रम की अपनी एक गरिमा है। दूसरी चुनौती हमारे जैसे समाज में और बड़ी है क्योंकि हम मानते है कि शारीरिक श्रम गंवारों का काम है।
शुरुआत पहली चुनौती से। ज़रा सोचें कि अगर किसी एकल परिवार में एक लड़की और एक लड़का है तो मां उन दोनों को भोजन और खेल के बारे में सिखाना कैसे शुरू करती है। सामान्य तौर पर पिताओं की तुलना में माताएं दिन भर में बच्चों से अधिक बार मिलती हैं और उनके साथ ज्यादा समय गुजारती हैं। अगर उस परिवार में विविध प्रकार का भोजन खाया जाता है तो मां बच्चों को यह बताती है कि हर व्यक्ति को मांस और सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि वे स्वादिष्ट होती हैं। इस तरह खाद्य संस्कृति पर अपनी मां से सीखे गए पाठ के आधार पर ही बच्चा मांस, मछली या सब्जियों का आनंद लेने की मानसिक स्थिति में आता है।
हमारे जाति पीड़ित समाज में कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो केवल शाकाहार करते हैं। ऐसे परिवारों में मां बच्चों को सिखाती है कि वे केवल सब्जियां खाएं। वह उन्हें बताती है कि सब्जियां खाने में स्वादिष्ट होती हैं और सेहत के लिए अच्छी भी। ऐसे परिवार का कोई बच्चा यदि विविध भोजन करने वाले किसी परिवार के बच्चे के संपर्क में आता है और मांस या मछली से बने खाद्य पदार्थ खाने की कोशिश करता है तो मां उसे डांटती है। वह कहती है कि मांस-मछली ‘गंदी चीजें’ हैं।
इन बातों का संबंध बच्चे के लड़की या लड़का होने से नहीं है। इसका संबंध परिवार की जाति और उसकी खाद्य संस्कृति से है। बच्चों के पिता भी ठीक यही बातें उन्हें बताते हैं। बच्चों को शुरू से जाति और खाद्य संस्कृति के बारे में बताया जाता है। उन्हें यह बताया जाता है कि सारे परिवार एक-से और एक बराबर नहीं होते और न ही सब बच्चे एक समान होते हैं। धीरे-धीरे यह बात उनके मन में पैठ जाती है और इस प्रकार धर्म, संस्कृति और रीति-रिवाजों के अंतर पैदा होते हैं। भारत में बच्चों को जाति-आधारित खाद्य संस्कृति में प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय मुसलमानों या ईसाईयों में इस तरह का प्रशिक्षण नहीं होता क्योंकि इन समुदायों के सदस्यों की खाद्य संस्कृति में ऐसी खाई नहीं है।
श्रम का मसला
जहां तक श्रम या काम का संबंध है एक ही परिवार और एक ही जाति में भी लड़कियों और लड़कों में भेद किया जाता है। यह बहुत गंभीर है। यह अंतर बचपन में उन्हें मिलने वाले खिलौनों से शुरू हो जाता है। लड़कियों को ‘लड़कियों वाले’ खिलौने दिए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए और अपने बाल कैसे रखना चाहिए। लड़कों को ‘लड़कों वाले’ खिलौने दिए जाते हैं और उन्हें भी यह बताया जाता है कि उन्हें कैसे कपड़े पहनना चाहिए और अपने बाल कैसे रखना चाहिए। बच्चे के लिंग के आधार पर उसके लिए अलग-अलग खिलौने खरीदने का काम माता और पिता दोनों करते हैं।
अगर किसी गरीब परिवार की खिलौने खरीदने की हैसियत न भी हो तब भी बच्चों को मां, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का उदाहरण देकर यह समझाया जाता है कि किस तरह लड़कियां और लड़के अलग-अलग हैं। लड़के और लड़कियां अपने बीच के लैंगिक और जैविक अंतरों को समझने के बहुत पहले अपने परिवारवालों से यह जान जाते हैं कि वे अलग-अलग हैं।

काम के मामले में लैंगिक अंतर और गंभीर होता है। बच्चों की शिक्षा स्कूल में शुरू नहीं होती। वह तभी शुरू हो जाती है जब वे घर में बड़े हो रहे होते हैं और गृहस्थी के कामों में सहयोग करते हैं। घर कार्य संस्कृति के प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। बच्चे देखते हैं कि केवल उनकी मां या घर की अन्य महिला सदस्य झाड़ू लगाती हैं, बर्तन मांजती हैं और कपड़े धोती हैं। वे देखते हैं कि केवल उनकी मांए या अन्य महिलाएं ही रसोईघर में काम करती हैं। वे यह भी देखते हैं कि परिवार के पुरुष सदस्य कभी खाना पकाने से संबंधित किसी गतिविधि में भाग नहीं लेते। वे यह भी देखते हैं कि माताएं या अन्य महिलाएं, पुरुषों और बच्चों को खाना परासेती हैं। वे कभी पुरुषों को यह काम करते नहीं देखते। अधिकांश पुरुष तो वह थाली भी नहीं धोते जिसमें वे खाना खाते हैं।
गावों में बच्चे देखते हैं कि पुरुष मवेशियों की देखभाल करते हैं और घर के बाहर काम पर जाते हैं। वे देखते हैं कि पुरुष खेत जोतते हैं और महिलाएं बीज बोती हैं व खरपतवार साफ करती हैं। इसका उल्टा कभी नहीं होता।
शहरी क्षेत्रों में बच्चे देखते हैं कि कुछ काम माताओं या परिवार के अन्य महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं। पुरुष यदि घर पर भी होता है तब भी वह कभी झाड़ू नहीं लगाता, बर्तन नहीं मांजता, कपड़े नहीं धोता और खाना नहीं पकाता। वह स्कूटर या कार चलाता है और घर के बाहर काम पर जाता है।

जातिगत श्रम विभाजन
भारत में बच्चों को सिखाया जाता है कि श्रम विभाजन जातिगत होता है। दलित, आदिवासी और शूद्र परिवारों में पैदा होने वाले बच्चों को बताया जाता है कि उनके पूर्वज हमेशा से वे काम करते आये हैं जिनमें हाथ गंदे होते हैं। जैसे कि खेती के लिए ज़मीन तैयार करना या शिल्पकारी। उन्हें बताया जाता है कि सार्वजनिक स्थानों की सफाई और चमड़े के उत्पाद बनाना दलितों का काम है। ऐसे कामों के बारे में बात करते समय जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उससे ही यह साफ़ हो जाता है कि इन कामों को नीची निगाहों से देखा जाता है।
ऊंची जातियों – विशेषकर ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय – के परिवारों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि खेतों में अनाज उगाने का काम प्रदूषित करने वाला है और जो लोग मिट्टी में हाथ गंदे करने वाले इस काम को नहीं करते वे अन्यों से श्रेष्ठ हैं। जो लोग ये काम करते हैं वे निम्न हैं। शिक्षित वर्गों द्वारा उत्पादक कार्यों को ‘प्रदूषणकारी’ मानने से उन बच्चों पर भी असर पड़ता है जिनके माता-पिता ऐसे काम करते हैं। उन्हें अपने माता-पिता पर शर्म आने लगती है।
यह भी पढ़ें : चुप्पी से प्रतिरोध तक का मेरा सफ़र
बच्चों को जब यह बताया जाता है कि इस तरह के काम गरिमापूर्ण नहीं हैं तो वे शारीरिक श्रम को निम्न दर्जे का काम मानने लगते हैं। जो जातिगत सांस्कृतिक मूल्य उन्हें सिखाये जाते हैं उनके चलते बड़े होने पर वे बच्चे मानने लगते हैं कि जो लोग खेतों में काम करते हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या लोहे, पीतल, सोने या चमड़े के उत्पाद गढ़ते हैं, वे सम्मान के पात्र नहीं हैं।
जब पीढ़ी-दर-पीढ़ी बच्चों के दिमाग में इस तरह के विचार भरे जाते हैं तो वे राष्ट्रीय संस्कृति बन जाते हैं। बच्चे और युवा शिल्पकारी और कृषि व पशु अर्थव्यवस्था से जुड़े कामों से नफरत करने लगते हैं। भारत के बाहर दुनिया में कहीं भी संस्कार और धर्म यह नहीं सिखाते कि कृषि या चमड़े से जुड़े काम प्रदूषणकारी होते हैं। ऐसा केवल भारत में होता है और वह भी हिंदू धर्म में।
पवित्रता और प्रदूषण की अवधारणाओं का एक और पहलू है, जो विशुद्ध लैंगिक है। करीब 11-12 साल की आयु में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है। इसे भी प्रदूषणकारी और अपवित्र माना जाता है। यही प्रसूति के समय भी होता है, जब प्रसूता के शरीर से रक्तस्नाव होता है।
कॉलेज में पढ़ने वाली एक युवा लड़की सूर्या श्री लिखती है– “फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। वे उसे रजस्वला होना कहते थे।
“शुरुआत में तो मुझे वह बहुत अच्छा लगा। मुझे करीब दो हफ़्तों तक स्कूल से मुक्ति मिल गई। मैं केवल टीवी देखती और अपने चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के साथ खेलती। खाना, सोना, गप्पें मारना और हंसना-हंसाना – बस यही मेरा काम था। सात दिन बाद फिर वही होता था। मेरी ख़ुशी का पारावार न था।
“मगर मुझे यह समझ में नहीं आया कि दरअसल वह मुझे कैदी बनाने का उत्सव था। एक बच्चे को सोने के पिंजरे में बंद करने का उपक्रम। उसके बाद लोगों – विशेषकर मर्दों – का मुझे देखने का नजरिया बदल गया। चाहे बारिश हो या तूफ़ान; या फिर सर्दी – पूरे पांच दिन तक मुझे घर से बाहर रहना पड़ता था। मैं ज़मीन पर सोती थी, जहां कीड़े-मकोड़े मेरे साथी होते थे। मुझे लगातार दर्द होता रहता था – एक नए किस्म का दर्द जिसे मैंने इसके पहले अनुभव नहीं किया था। मेरे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। मैं अब घर के नजदीक की दुकानों पर भी नहीं जा सकती थी। मुझसे कहा गया कि मुझे लड़कों से बात नहीं करनी हैं – अपने चचेरे-ममेरे भाईयों से भी नहीं। मुझसे अपेक्षा यह थी कि मैं हमेशा अपनी माता-पिता की नज़रों के सामने रहूं।”
वह आगे लिखती है– “धीरे-धीरे समाज ने मुझे समझाया कि एक ‘अच्छी लड़की’ कैसी होती है। उसके बाद से मेरे अंदर की बच्ची ने एक मुखौटा पहन लिया – ऐसा मुखौटा जो दुनिया को भला लगे। मैं वही करने लगी जो लोग मुझे करते देखना चाहते थे। वही बोलने लगी जो लोग मुझसे सुनना चाहते थे। मैं अपने परिवार की सबसे आज्ञाकारी लड़की बन गई।” [लर्निंग इंग्लिश नेशनलिज्म में अनलर्निंग ए चाइल्डहुड ऑफ़ साइलेंस एंड एम्ब्रेसिंग ए फ्यूचर ऑफ़ रेजिस्टेंस से। प्रकाशक : फुले-आंबेडकर सेंटर फॉर फिलोसफी एंड इंग्लिश ट्रेनिंग (पैकपेट), तेल्लापुर, हैदराबाद, 2026]
क्या किया जा सकता है
भारत में बचपन में ही बच्चों का परिचय सख्ती से लागू की जाने वाली जातिगत और लैंगिक असमानताओं से हो जाता है। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि शारीरिक श्रम केवल विशिष्ट जातियों के लोगों का काम है और उसमें कोई गरिमा नहीं है; जब तक हम यह मानते रहेंगे कि मासिक धर्म के दौरान और प्रसूति के बाद महिलाओं का शरीर अपवित्र हो जाता है; जब तक हम यह मानते रहेंगे कि कुछ काम महिलाओं के करने के लिए होते हैं और कुछ पुरुषों के लिए तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकेगा। यह पिछड़ी सोच हमें विज्ञान क्षेत्र में बहुत पीछे छोड़ रही है। हम पश्चिमी देशों – जहां का जीवन चक्र अलग है – पर निर्भर हो रहे हैं।
ग्रामीण समाजों पर लेखन के दौरान मेरा साबका दो ऐसी गहन निहितार्थ वाली कहावतों से पड़ा जो इस चक्र को तोड़ सकती हैं। तेलुगू में कहावत है कि ‘बरूडा लेनिड़े बुव्वा लेदु’ (मिट्टी के बिना खाना नहीं) और ‘रजस्वला कनिड़े पिन्देम लेदु’ (मासिक धर्म के बिना बच्चा नहीं)। अगर सभी जातियों के महिला और पुरुष इन दो कहावतों का अर्थ समझ लें और उसके प्रकाश में अपने जीवन में बदलाव ले आएं तो भारत एक शक्तिशाली देश बन सकता है।
(यह आलेख मूल अंग्रेजी में न्यूजक्लिक द्वारा प्रकाशित है तथा यहां इसका हिंदी अनुवाद लेखक की सहमति से प्रकाशित है। अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in