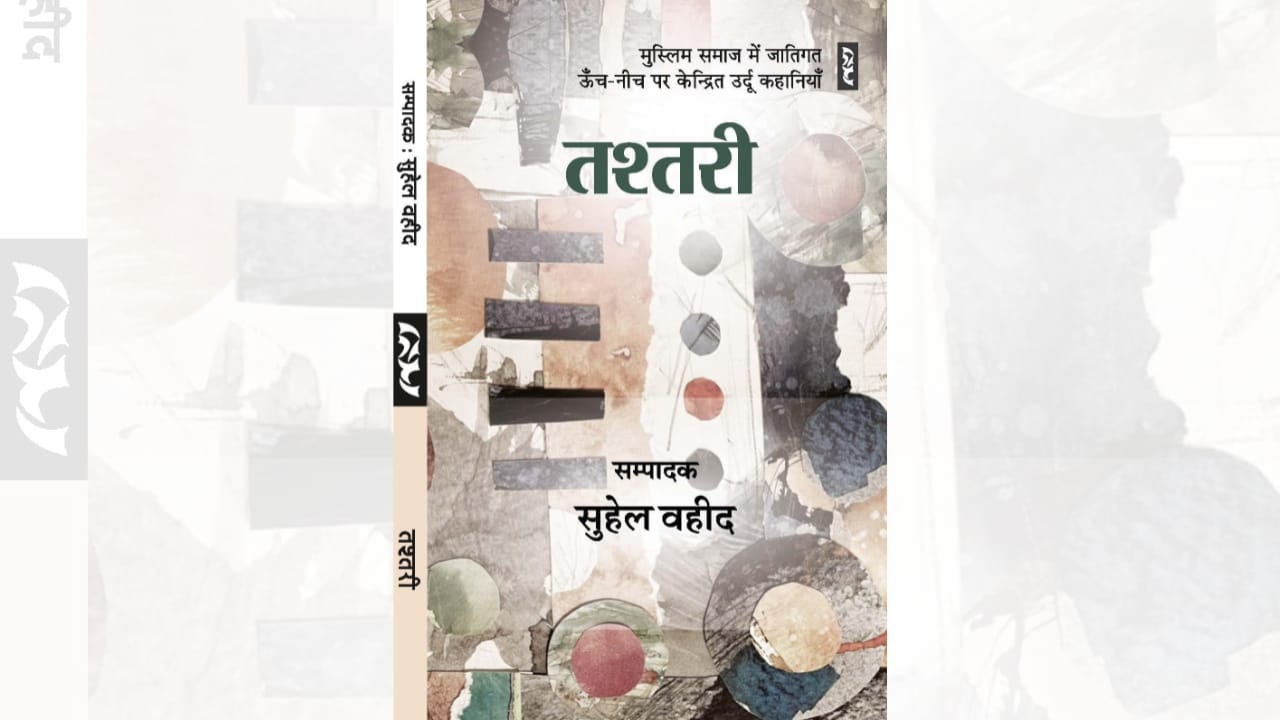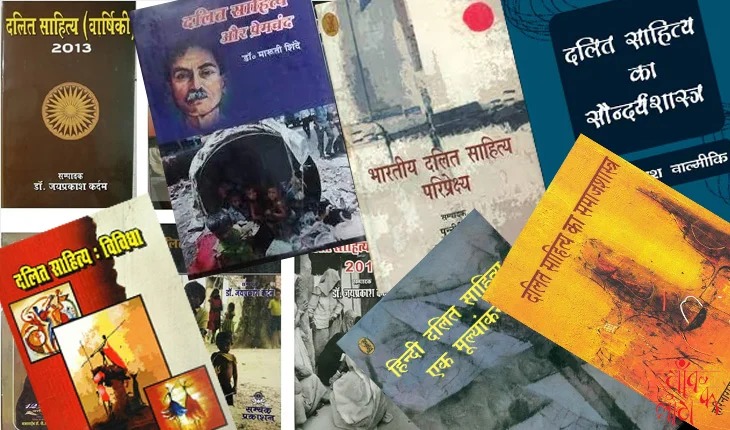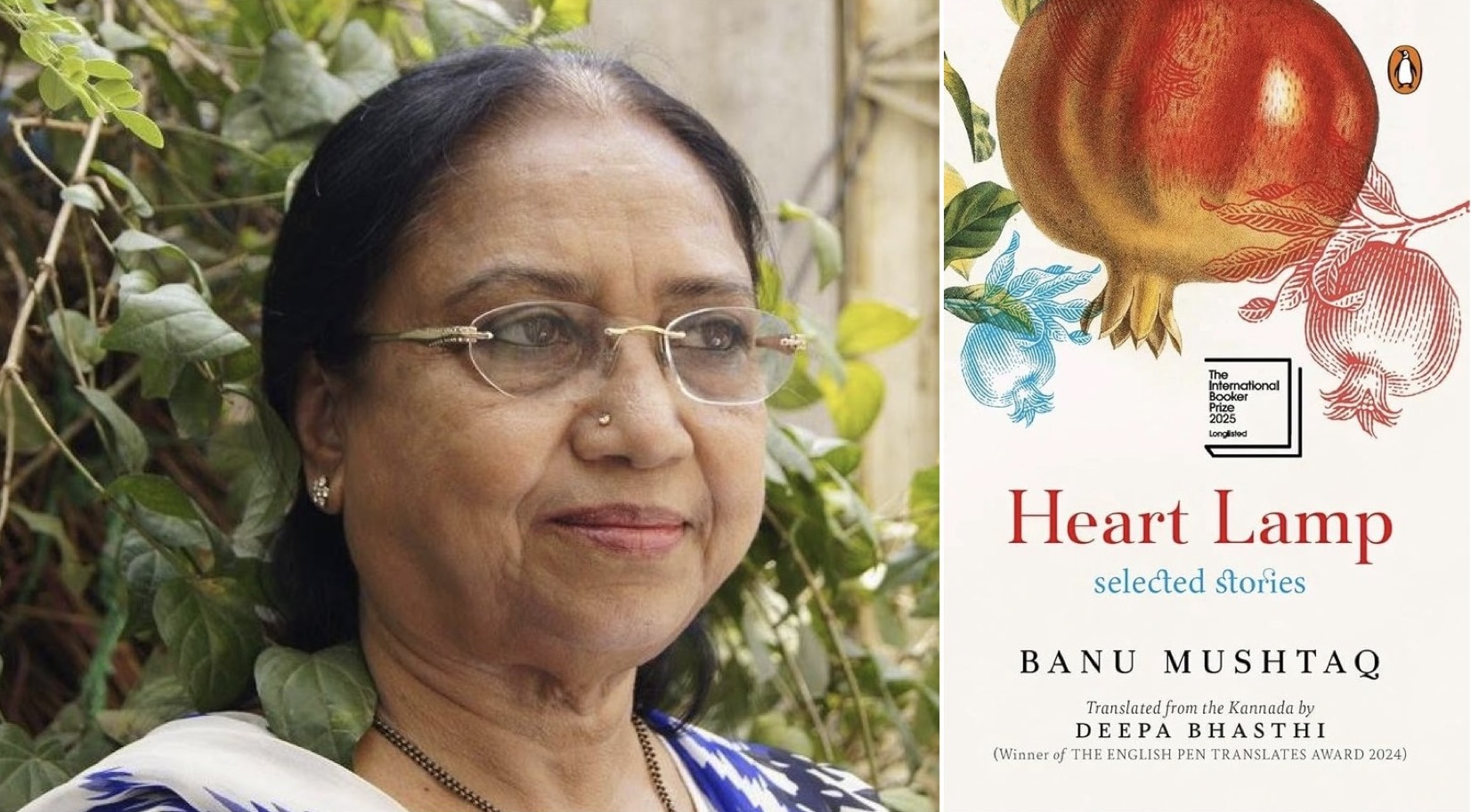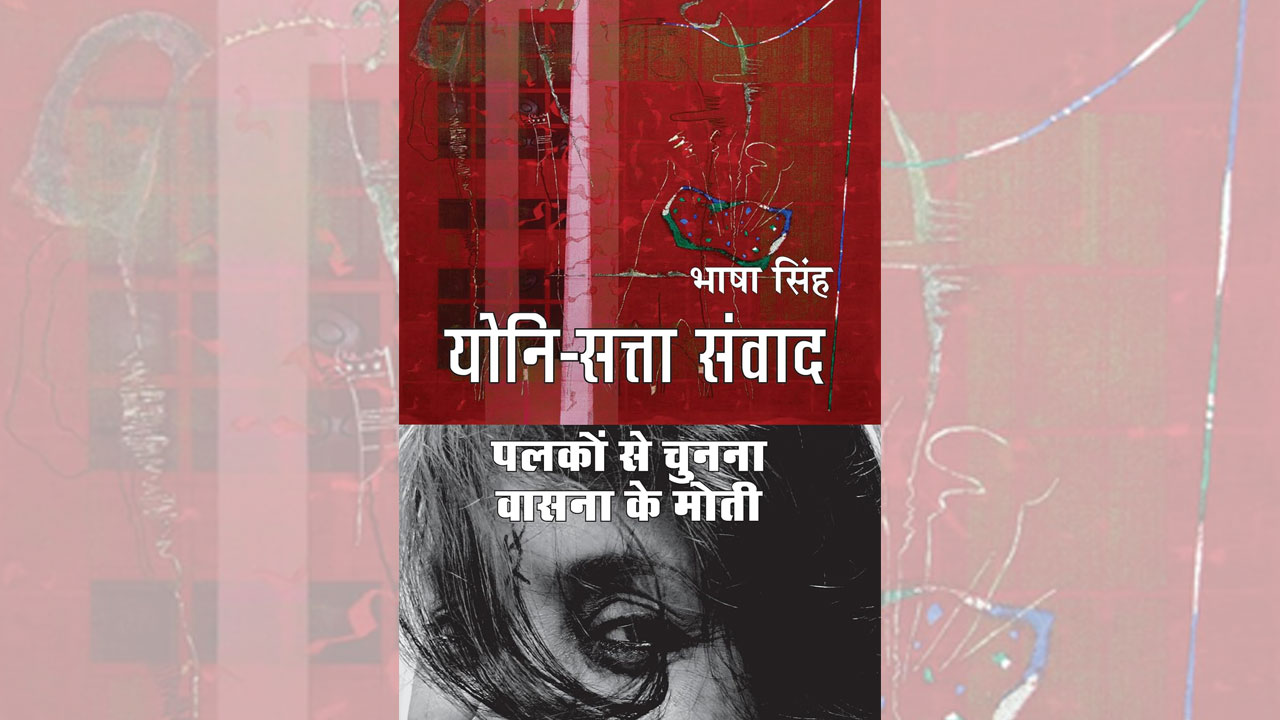इसमे कोई दो राय नहीं है कि दलित आत्मकथाओं ने हिंदी की साहित्यिक चौहद्दी का विस्तार किया और वहीं अपने धधकते अनुभवों से भारतीय समझ को झकझोर कर रख दिया। आधुनिक भारत में प्रकाशित ‘जूठन’, ‘अपने-अपने पिंजरे’, ‘तिरकृष्त’, ‘मेरा बचपन मेरे कंधों पर’, ‘मुर्दहिया’, और ‘शिकंजे का दर्द’ सरीखी दलित आत्मकथाओं के भीतर दर्ज खौलता हुआ सामाजिक यथार्थ और जातिगत अत्याचार इस बात की तसदीक़ करता है कि आधुनिक नागरिक समाज अभी भी जातिवाद के बखेड़े से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका है। देखा जाए तो दलित आत्मकथाएं सिर्फ भारतीय साहित्य की धरोहर ही नहीं, बल्कि इतिहासकारों और सामाजिक विज्ञानियों के लिए दलित समाज और उसके इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन चुकी हैं। दलित आत्मकथाओं के प्रकाशन के क्रम में अभी पिछले वर्ष ही प्रकाशित रामचंद्र राम की आत्मकथा ‘चमरटोली से डी.एस.पी. टोला तक’ सामाजिक और पुलिस प्रशानिक गलियारों की भीतरी और बाहरी दुनिया के यथार्थ से रू-ब-रू कराती हुई दलित जीवन की दुश्वारियों और उसके संघर्ष को भारतीय समाज के सामने प्रस्तुत करती है।
वास्तव में यह आत्मकथा बिहार में जातिवाद और सामंतवाद की बजबजाती हुई नदियों के खौफनाक मंज़र से परिचित करा कर दलित अस्मिता की दावेदरियों को पेश करती है। लेखक रामचंद्र राम मूलत: बिहार के समस्तीपुर जिला से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई समस्तीपुर से ही हुई। अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह सन् 1974 में बिहार लोक सेवा आयोग से सब-इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गए थे। लेखक का पारिवारिक तानाबाना सामाजिक और आर्थिक हैसियत से निचले पायदान पर था। लेखक के पिता कलकता में किसी चमड़ा कारखाना में मजदूरी किया करते थे। लेखक बताते हैं कि उनके गांव के सभी दलित परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय थी। प्राय: अधिकतर दलित अपने जीवन-यापन के लिए चमड़े की फैक्ट्रियों में काम किया करते थे।
जाति-प्रथा एक देशव्यापी समस्या है। इस जाति-प्रथा ने दलित समुदाय को सार्वजनिक संसाधनों से सिर्फ वंचित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें शैक्षिक अवसरों से वंचित कर उनकी बौद्धिकता को भी निखरने नहीं दिया। जाति-प्रथा का एक खौफनाक पहलू यह भी है कि इसके जरिए दलित समुदाय को परिधि से भी बाहर कर उनको हाशिए पर धकेल दिया गया। यहां तक कि उच्च श्रेणी के हिंदुओं ने जाति श्रेष्ठता की ठसक में दलित बस्तियों को कभी सम्मान से नहीं देखा। उनको जाति/कैटेगरी से संबोधित किया गया। आत्मकथाकार रामचंद्र राम खुलासा करते हैं कि उनके मोहल्ले को उच्च श्रेणी के हिंदू चमरटोली कहकर संबोधित किया करते थे। यहां तक कि सरकारी गज़ट में भी उनके टोले को चमरटोली के नाम से ही दर्ज किया गया था।
रामचंद्र राम बताते हैं कि “हमारे टोले को लोग चमरटोली कहकर पुकारते थे। सरकारी गज़ट में भी यही नाम था। वैसे टोला-टोली नाम जाति अधारित होता था। जैसे-चमरटोली, मल्लाहटोली, दुसाध टोली, डोम टोली, कोइरी टोला, गोआर(ग्वाला) टोला, बाभन टोली, मुसहर टोली या मुसहरी आदि-आदि नाम से गांव बंटा हुआ था।” इस आत्मकथा में रामचंद्र राम ने अपने यथार्थपरक अनुभव से यह भी दर्ज किया कि उनके गांव का पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाला नागरिक समूह भी जाति के घाट के पार नहीं जा सका था। वह भी अपने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में जाति-प्रथा से संचलित हुआ करता था। सवर्णों की तरह शूद्र भी दलितों से जातिगत भेद और अस्पृश्यता का बर्ताव किया करते थे।

लेखक बताते हैं कि उन दिनों छुआछूत अपने चरम पर थी। गर्मी में प्राय: दलित टोले का कुआं सुख जाया करता था। दलित महिलाएं कोइरी टोले के कुएं से पानी भरने के लिए जाती थीं। दलित महिलाएं तब तक कुआं के जगत पर कदम नहीं रख सकती थीं, जब तक कि कोइरी समाज की स्त्रियां पानी नहीं भर लेती थीं। लेखक अपनी आत्मकथा में आगे इस बात का भी जिक्र करते हैं कि पिछड़ी जातियों के लोग दलितों से भयंकर अस्पृश्यता का बर्ताव किया करते थे। गांव में शूद्रों की घनी आबादी थी। कोइरी और ग्वाला, बहुसंख्यक संपन्न किसान रेलवे में नौकरी करने वाले थे। वहीं मल्लाह, हजाम, बढ़ई, तेली, तमोली, माली, कानू, लोहार, ततमा आदि जाति के लोग भी तो शूद्र की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन ये लोग अपने को सवर्ण समझने का भ्रम पाले बैठे हैं। चमार, दुसाध, पासी, धोबी, मुसहर – जो गांव के किनारे बसे हैं, जिन्हें अछूत या अस्पृश्य कहा गया है। पिछड़ी, अतिपिछड़ी जाति के लोग भ्रष्ट हो जाने के डर से इनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते, न ही पानी पीते थे। देखा जाए तो मूलत: इस जातिगत भेदभाव की मूल जड़ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसने प्राय: सभी सामाजिक हलक़ों में जातिवाद का रसायन घोल दिया और उसकी जद में पिछड़ी जातियां भी आ गईं। वह भी सवर्णों की देखा-देखी में दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव का बर्ताव करने लगी थीं।
वास्तव में देखा जाए तो जातिवाद का दायरा असीमित है। यह सोचनीय बात है कि शासन-प्रशासन की चौखट भी जातिवाद की बेड़ियों से अब तक मुक्त नहीं हो पाई है। रामचंद्र राम अपनी आत्मकथा में पुलिस प्रशासन के भीतर मौजूद जातिवादी चेहरे को बड़ी शिद्दत के साथ बेनकाब करते हैं। आत्मकथा लेखक रामचंद्र राम को ख़ाकी महकमे के भीतर उच्च वर्ण के अफसरों ने जातिवाद का अहसास करवाया था। उनके सामने जातिगत भेद का घृणित रूप तब सामने आया, जब उनके ही मातहत कनीय पद पर कार्यरत सर्किल इंस्पेक्टर ने जातीय भेदभाव के तहत उन्हें अपमानित किया। हुआ यह था कि एक उच्च वर्ण के सर्किल इस्पेक्टर ने अपनी उच्च वर्ण वाली मानसिकता के ठसक में उनकी रसोई का बना हुआ खाना खाने से इंकार कर दिया। लेखक का कहना है कि दलितों पर सवर्ण अत्याचार के मामले में खुले तौर पर उच्च श्रेणी के अफ़सरों द्वारा सवर्णों और धनवानों का पक्ष लिया जाता था। इस तरह सवर्णों का पक्ष लेकर दलितों को न्याय से वंचित कर दिया जाता था।
लेकिन रामचंद्र राम ने इस जातिवादी इंस्पेक्टर को सबक सिखाने के लिए उस पर कानूनी तौर कार्यवाही को अंजाम दिया। इस आत्मकथा में सामंती शोषण और उपद्रव की जो इबारतें दर्ज हैं, वह किसी भी सभ्य समाज और संवेदनशील नागरिक समूह को झकझोर कर रख देती हैं। सामंती ठसक के निशाने पर अधिकतर दलित-पिछड़ी जातियों की अस्मिता और उसकी दावेदारी रही है। इस आत्मकथा के लेखक जब बतौर थाना प्रभारी पकरीबरावां में तैनात थे तो उसी समय सामंतों ने एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। इस घटना में सामंतों ने न सिर्फ एक पिछड़ी जाति की स्त्री की अस्मिता को लूटने का प्रयास किया बल्कि बचाने आए उसके भाई मनोहर महतो को बड़ी बहरमी से मारपीट कर घायल कर डाला। ये सामंती सिर्फ इतने ही अत्याचार से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने शिल्पकार जातियों के घर और खलिहानों को आग के हवाले कर दिया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना को रामचंद्र राम ने बतौर थाना प्रभारी अपनी बौद्धिकता और सूझ-बूझ से न सिर्फ सामंती मानसिकता को सबक सिखाया, बल्कि पीड़ित वर्ग के लिए न्याय की पहलकदमियों को अंजाम दिया।
वास्तव में यह आत्मकथा सिर्फ रामचंद्र राम के इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने तक जीवन संघर्ष की गाथा नहीं बल्कि यह दलित समुदाय के उस प्रत्येक व्यक्ति की गाथा है जो जातिवादियों के अखाड़े में अपने अधिकारों के लिया लड़ता हुआ, अपनी बौद्धिकता से कुछ हासिल करने के लिए संघर्षरत है। यह आत्मकथा इसलिए भी खास और जरूरी लगती है कि सामाजिक शोषण के साथ ही प्रशासन के भीतर मौजूद जातिवादी चेहरे को बेनकाब करती है। इस आत्मकथा के भीतर मौजूद दलित चेतना शोषण और अन्याय का प्रतिकार कर दलित बौद्धिकता का एक लोकतांत्रिक चेहरा भी प्रस्तुत करती है। इस आत्मकथा में दर्ज कुछ मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग दलित समाज के भीतर पनप रही सामाजिक और शैक्षिक चेतना का नज़ारा भी पेश करते हैं। यदि भारत के बौद्धिक, साहित्यिक अध्येता, समाज विज्ञानी, समाजशास्त्री और इतिहासकार दलित समाज के संघर्ष एवं उसके इतिहास को करीब से समझना चाहते हैं तो यह आत्मकथा उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ साबित हो सकती है।
समीक्षित पुस्तक : ‘चमरटोली से डी.एस.पी. टोला तक’
लेखक : रामचंद्र राम
प्रकाशक : स्वराज प्रकाशक, दिल्ली
मूल्य : 400 रुपए
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in