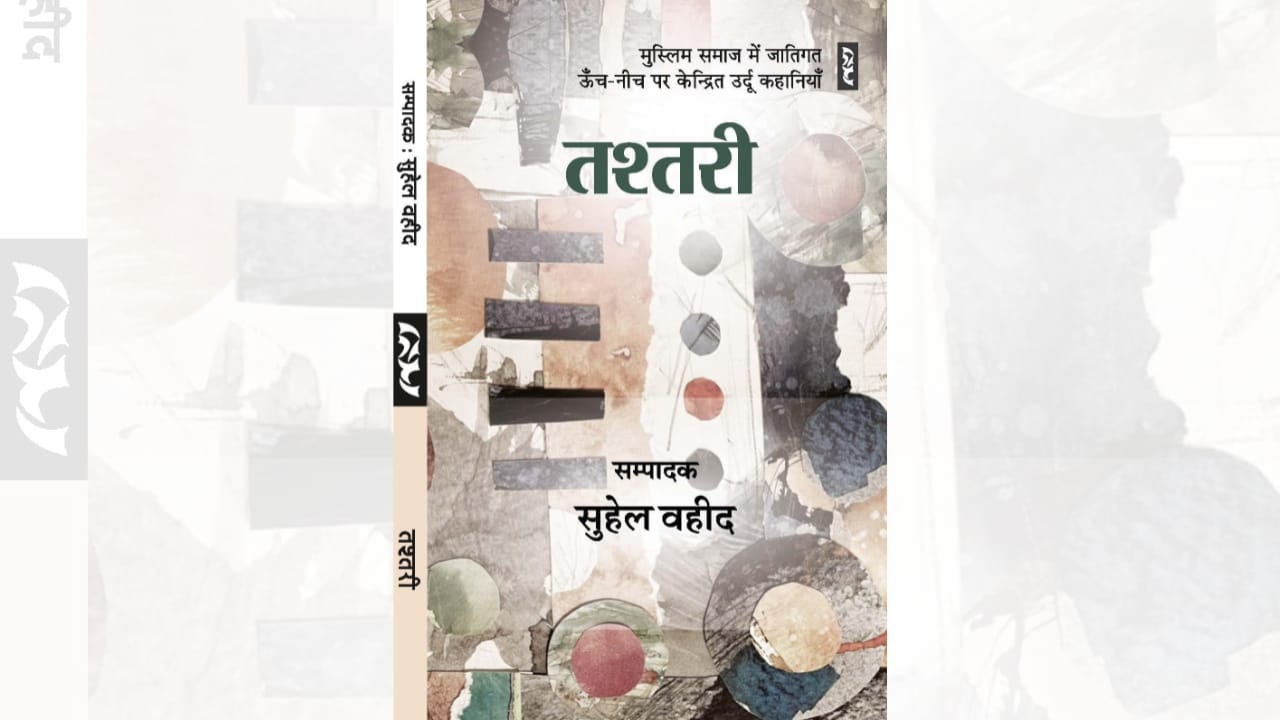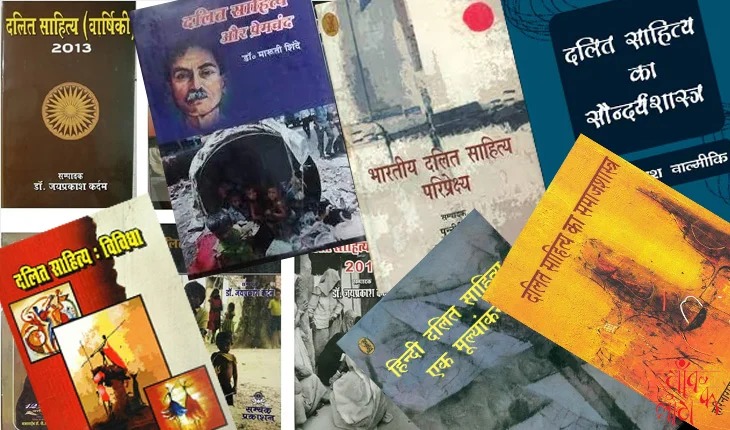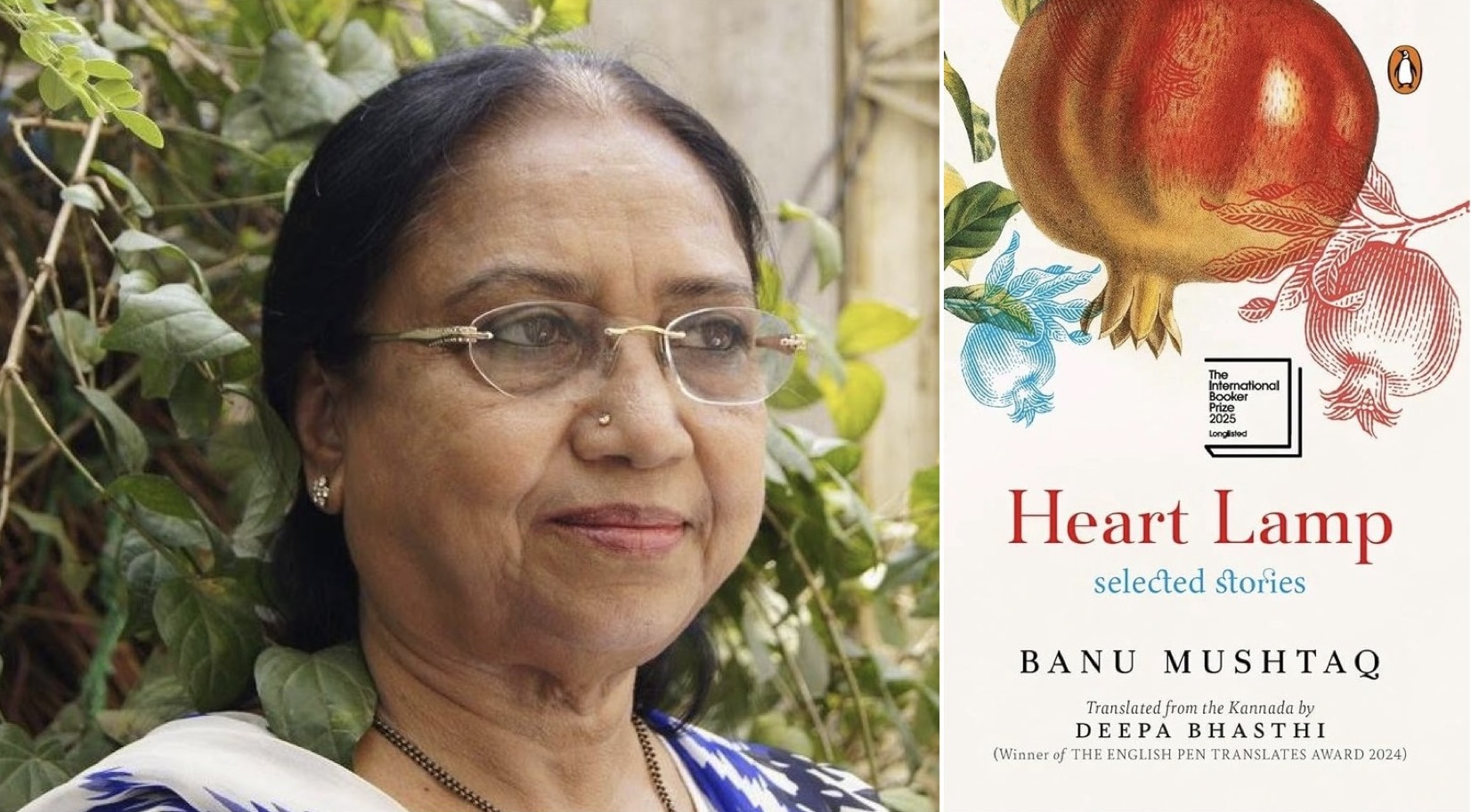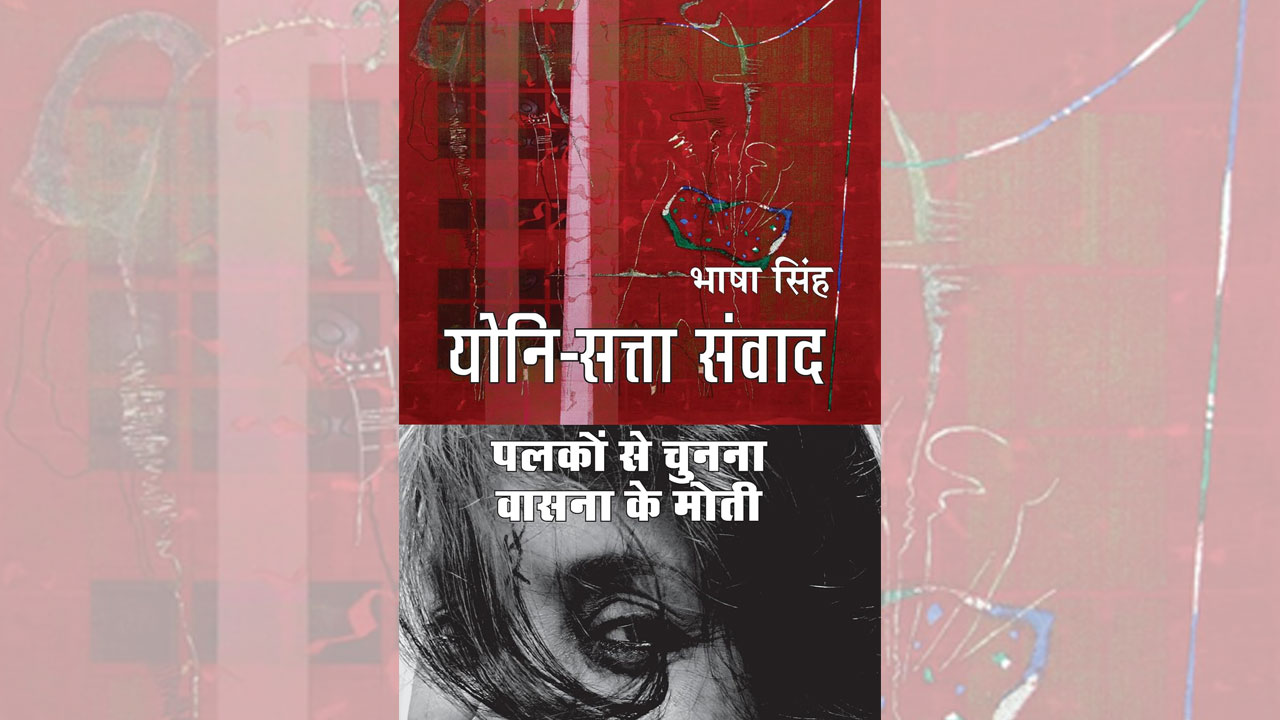कंवल भारती हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक, पत्रकार, कवि एवं दलित चिंतक हैं। उनकी आलोचना का मूल केंद्र आंबेडकरवाद है। वे बुद्ध से बौद्धिकता, कबीर व रैदास से साहस तथा बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर से तार्किकता ग्रहण करते हैं। यही दलित चिंतन की परंपरा रही है। उनकी आलोचनाएं चार्वाकों की भांति लौकिक तथा भौतिक होती हैं। संभवतः उनका आंतरिक पत्रकार रूप ही उन्हें तथ्यों की अभिधात्मक, लौकिक, भौतिक और वैज्ञानिक व्याख्या के लिए प्रेरित करता है।
उनकी सद्य प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक ‘भक्ति आंदोलन और निर्गुण क्रांति’ (2025) नवीन दृष्टिकोण से भक्ति आंदोलन व साहित्य की व्याख्या करती है। साथ ही, अब तक भक्ति आंदोलन पर वर्णाश्रमधर्मी दृष्टिकोणों से हुई व्याख्याओं की पड़ताल करती है। उनकी यह पुस्तक भक्ति आंदोलन की एक वैकल्पिक (सही मायनों में वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करती है।
इस पुस्तक में कुल बीस आलेख हैं, जिसमें से पांच भक्ति आंदोलन पर, तीन कबीर पर, छह रैदास पर (एक आलेख में मीरा पर कुछ पृष्ठ लिखे गए हैं), एक अक्क महादेवी पर तथा पांच अन्य विषयों पर। इस पुस्तक का प्रथम आलेख ‘भक्ति-आंदोलन : एक पुनर्पाठ’ (2024) में आलोचक कंवल भारती तथ्यों तथा अपनी परिकल्पना के आधार पर भक्ति आंदोलन की तार्किक वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे भक्ति के उत्स के संबंध में मत रखते हैं। वे भक्ति काल को स्त्री-शूद्र संतों के उभार काल के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री संतों ने भक्ति काल में मनु के सिद्धांतों को चुनौती दी। वे भक्ति आंदोलन को एक क्रांतिकारी विचारधारा मानते हैं। वे भक्ति आंदोलन की उपलब्धियां बताते हैं – संस्कृत के विरुद्ध लोक भाषा को अपनाना, ब्राह्मणों की विशिष्टता को चुनौती, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति, मंदिर की अनिवार्यता खत्म, पशुओं के प्रति अहिंसा भाव, पोथी-पत्री में विश्वास खत्म और परलोक का खंडन।[1]
‘निर्गुणवाद का अर्थ’ (2022) शीर्षक आलेख में उन्होंने भक्ति के निर्गुण स्वरूप को स्पष्ट किया है। उन्होंने कबीर और रैदास के माध्यम से निर्गुण आंदोलन के अर्थ एवं उद्देश्य को स्पष्ट कर उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि को रेखांकित किया है। वे कहते हैं, “निर्गुणवाद और सगुणवाद असल में, भारतीय मध्यकाल का क्रमशः वामपंथ और दक्षिणपंथ है। जिस तरह वामपंथ को दलितों, पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों, और शोषितों का दर्शन माना जाता है, उसी तरह निर्गुणवाद भी दलितों, पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों और शोषितों का दर्शन था, और जिस तरह दक्षिणपंथ आज ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का प्रपंची पंथ है, उसी तरह सगुणवाद को भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित ब्राह्मणों और शोषक सेठों का दर्शन समझना चाहिए।”[2]
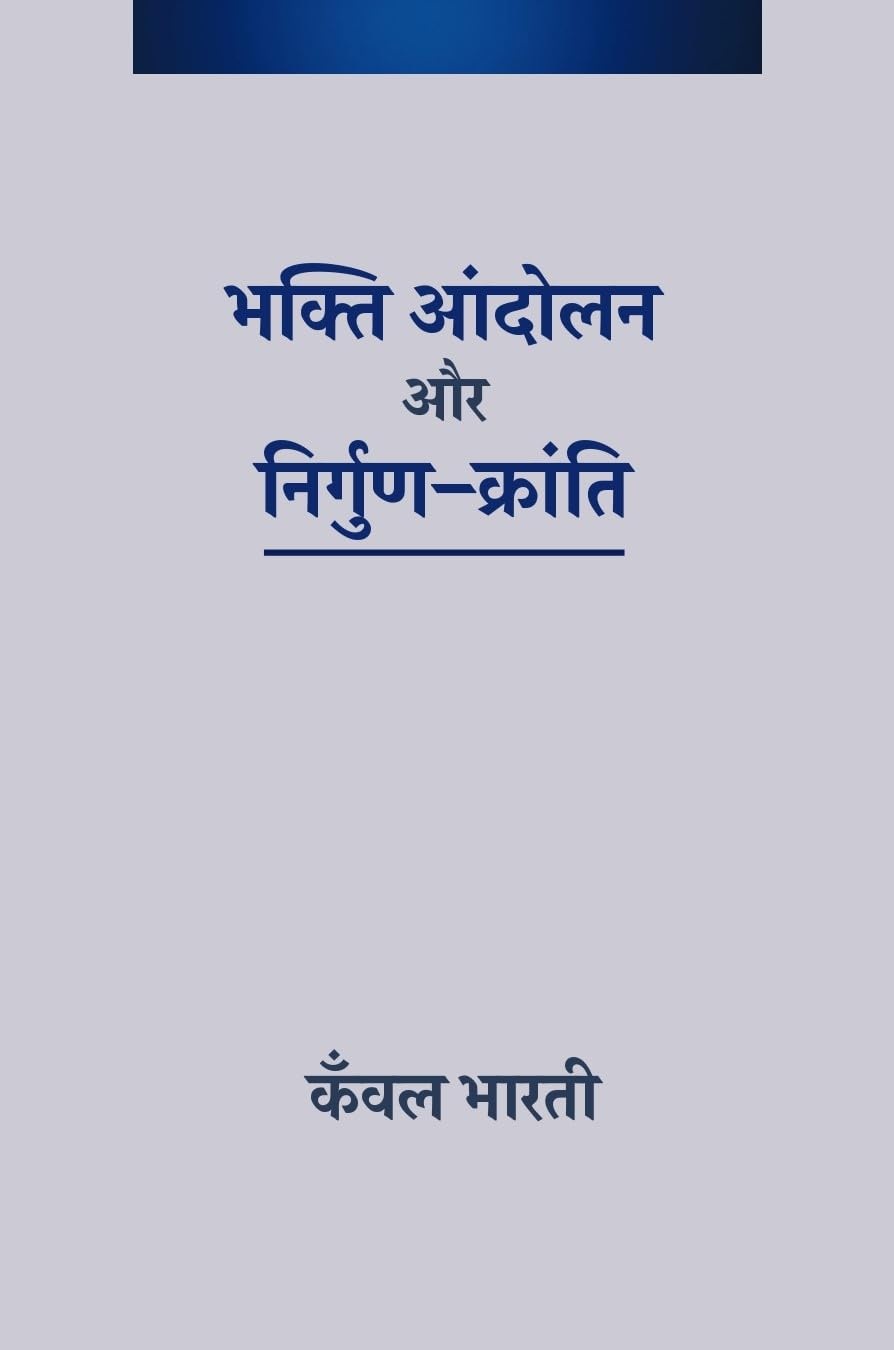
‘भारतीय चिंतन की वैकल्पिक धारा’ (2024) आलेख में कंवल भारती वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति आदि की चिंतन-धारा को वैकल्पिक धारा कह रहे हैं। उनके अनुसार भारत का मौलिक दर्शन है– लौकिक और भौतिक चार्वाकों तथा आजीविकों का दर्शन। इस आलेख में वे बताते हैं कि आर्यों ने किस प्रकार इस चिंतन-धारा को पतन की ओर धकेला। किस प्रकार बौद्धों, जैनियों, चार्वाकों और आजीविकों पर अत्याचार किए गए। किस प्रकार राजसत्ता हिंदुत्ववादियों के नियंत्रण में गई। वे कहते हैं, “मैं इस धारा (भौतिकवादी) को वैकल्पिक नहीं कह सकता, क्योंकि वैकल्पिक धारा प्रतिक्रांति की धारा है। बहुजन-कल्याण की जो भौतिकवादी दर्शन धारा यहां आजीवकों, चार्वाकों, बुद्ध से शुरू होकर सिद्धों, नाथों, कबीर, रैदास, फुले, आंबेडकर, पेरियार से होती हुई संविधान तक आई है, आज उसे नष्ट करने का काम हो रहा है और उसके स्थान पर सनातन दर्शन के रूप में हिंदुत्व का विकल्प दिया जा रहा है।”[3]
इसी तरह ‘भारतीय चिंतन परंपरा में निर्गुणवाद की क्रांति’ (2024) आलेख में वे निर्गुणवाद को भारत की प्राचीन अवैदिक परंपरा से जोड़ते हैं। उसे भक्ति से अलग बताते हैं। किन परिस्थितियों में निर्गुणवाद का जन्म हुआ इसकी पड़ताल करते हैं। निर्गुणवाद ने किस प्रकार सामान्य जनता को गहरे तक प्रभावित किया और वैदिक धारा के सामाजिक नियमों को तोड़ने का काम किया, इन सबकी जांच करते हैं। निर्गुणवाद और भक्तिवाद में अंतर बताते हुए वे कहते हैं, “भक्तिवाद एक ऐसा विचार है, जो संसार से पलायन सिखाता है और संसार की भौतिक सच्चाइयों से आंखें मूंदे रहता है। लेकिन निर्गुणवाद ने संसार से पलायन नहीं किया। सभी निर्गुण चिंतक कवि संसार की कठोर वास्तविकताओं के साथ जीते थे। वे अपनी बस्तियों में अपनी बीवी-बच्चों के साथ रहते थे। वे सुख-दुख, गरीबी, अभाव को अनुभव करते थे और गहरी सामाजिक विषमता, पराधीनता और शोषण के चक्र में पिस रही जनता के बीच रहकर चिंतन करते थे। वह मार्क्स और लेनिन के समाजवाद का दौर नहीं था, लेकिन एक काल्पनिक समाजवाद या समतावाद उनके चिंतन में था, जिसे उन्होंने बेगमपुर, अमरदेसवा, अमृत देश, निर्वानी देश कहा है।”[4]
‘जगतगुरु का मिथक’ (2015) शीर्षक आलेख में वे यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में कुछ लोग किस प्रकार अंधराष्ट्रवाद का शिकार होकर भारत को विश्वगुरु बनाने का भ्रम पाले हुए हैं। वे इस बात का विश्लेषण करते हैं कि भारत ने विश्व के अन्य देशों को क्या दिया और उनसे क्या-क्या लिया? वे भारत की ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर तंज कसते हैं जो यह मानता है कि ब्राह्मण ही केवल गुरु होने का अधिकारी है। वे कबीर को याद करते हैं कि ‘ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाहिं।’[5]
यह भी पढ़ें – शूद्र परंपरा के भक्ति मूल्य
‘सतनामी विद्रोह’ (2013) शीर्षक आलेख को ‘गुरु घासीदास’ (2018) आलेख की पृष्ठभूमि के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि दोनों का प्रकाशन अलग-अलग समय में हुआ है। ‘सतनामी विद्रोह’ में सतनामी पंथ की उत्पत्ति और औरंगजेब के विरुद्ध उनका सशस्त्र विद्रोह का वर्णन है। साथ ही इतिहासकारों द्वारा इस विद्रोह की इतिहास में उपेक्षा किए जाने के कारणों की भी पड़ताल की गई है।
‘गुरु घासीदास’ (2018) आलेख में उन्हीं के बारे में थोड़ी जानकारी तथा उनके विचारों का वर्णन है। वे इसका भी वर्णन करते हैं कि ब्राह्मणवादी आलोचकों ने जिस प्रकार कबीर और रैदास का ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया है, उसी प्रकार का षड्यंत्र गुरु घासीदास के लिए भी रचा गया। इसकी वे ऐतिहासिक जांच करते हैं और ब्राह्मणवादी जाल को काटने का प्रयास करते हैं।
नाथ पंथ पर आधारित ‘नाथ पंथ और मछंदरनाथ’ (2021) आलेख में कंवल भारती ने नाथ पंथ की उत्पत्ति तथा एक प्रमुख नाथ मछंदरनाथ, जो कि गोरखनाथ के गुरु थे, उनके बारे में वर्णन किया है। मछंदरनाथ का नाम 84 सिद्धों में क्यों नहीं है और वे कौन हैं, इसपर प्रकाश डाला गया है। नाथों ने बौद्ध परंपरा और बुद्ध को त्यागकर शैव परंपरा और शिव को क्यों अपनाया, इसपर भी अनुमानित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। ‘जाग मछंदर गोरख आया’ इस लोकोक्ति की भी जांच की गई है।
‘ईश्वर की परिकल्पनाएं अथवा परिहास’ (2011) शीर्षक आलेख में लेखक ने ईश्वर की उत्पत्ति के संदर्भ के मिथकों और कथाओं की ऐतिहासिक पड़ताल की है। वे यह प्रश्न उठाते हैं कि वेद, पुराण, स्मृति आदि में ब्राह्मणों ने अपने ईश्वर को पूज्य सिद्ध करना चाहा है या परिहास किया है? वे शंकर के अद्वैतवाद को भी ईश्वर का परिहास बताते हैं। वे इस्लाम में ईश्वर की व्याख्या को भी परिहास सिद्ध करते हैं। वे ईश्वर की उत्पत्ति का कारण अज्ञान को बताते हैं। राहुल सांकृत्यायन भी अज्ञानता का दूसरा नाम ईश्वर कहते हैं।
‘कबीर का स्त्री-चिंतन’ शीर्षक आलेख में वे कबीर के स्त्री संबंधी पदों की पड़ताल करते हैं। वे यह व्यंग्य करते हैं कि ब्राह्मणवादी आलोचकों के लिए कबीर के स्त्री संबंधी पद ‘अंधे के हाथ में बटेर’ जैसा है। वे इसका इस्तेमाल केवल अपने वर्णवादी तुलसीदास को बचाने के लिए करते हैं। थोड़ा-सा भी किसी ब्राह्मणवादी आलोचक को कह दो कि तुलसी वर्णवादी और स्त्री विरोधी थे, वह तुरंत तुनक कर कहेगा कि कबीर भी तो स्त्री विरोधी थे, यह उस समय की सीमा थी। वह यह कभी नहीं कहेगा कि कबीर वर्णवाद के विरोधी थे, तो तुलसी को भी वर्णवाद का विरोधी होना चाहिए था। कबीर के स्त्री चिंतन संबंधी पदों की व्याख्या में लेखक का मूल स्रोत ‘हंस’ फरवरी 2008 में छपा अनुराधा जी का ‘सती प्रथा और हिंदी मानसिकता’[6] आलेख है। साथ ही उनकी कुछ मौलिक उद्भावनाएं हैं। जैसे– कबीर स्वयं गृहस्थ थे तो वह पूर्णतः स्त्री विरोधी कैसे हो सकते हैं? कबीर की एक पुत्री भी थी; कबीर उपासना के क्षेत्र में स्वयं को स्त्री रूप में प्रकट करते हैं, भक्ति के इस स्तर पर तो तुलसी भी नहीं पहुंच पाते; कबीर अपने समय के सती प्रथा की त्रासदी को अपने शब्दों में इतिहास की तरह दर्ज करते हैं; इत्यादि।
‘कबीर के मूल्यांकन का ब्राह्मणी मापदंड’ (2018) आलेख में वे बात करते हैं कि वर्णाश्रमधर्मी आलोचकों ने किस प्रकार से कबीर की विकृत व्याख्या प्रस्तुत की है। वे कुछ आलोचकों के नाम लेते हैं जिन्होंने कबीर का ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया है तथा उनकी क्रांतिकारिता को कुंद करने का प्रयास किया है। जैसे– रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पारसनाथ तिवारी, परशुराम चतुर्वेदी, बलदेव वंशी, रामकिशोर शर्मा, योगेश्वर, शुकदेव सिंह, वासुदेव सिंह, और पुरुषोत्तम अग्रवाल।[7] वे सवर्ण आलोचकों के कबीर पर किए गए कार्यों को प्रश्नांकित करते हैं। वे प्रश्न करते हैं कि कबीर ने इन आलोचकों को इतना प्रभावित क्यों किया है और यदि वे लोग सच में कबीर से प्रभावित हैं तो अपनी रचनाओं में उन प्रभाव के कारणों का उल्लेख क्यों नहीं करते? वे सवर्ण आलोचकों द्वारा कबीर के गलत पदों के संकलन व अनुचित व्याख्याओं का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे यह सिद्ध करते हैं कि सवर्ण आलोचक कबीर में इसलिए रुचि दिखाते हैं ताकि मनगढ़ंत व्याख्याओं द्वारा उनकी क्रांतिकारिता को कुंद किया जा सके तथा उन्हें सांप्रदायिक सिद्ध किया जा सके।
‘कबीर पर गीता का प्रभाव’ (2023) शीर्षक आलेख में वे कबीर को वैष्णवी रंग में रंगने के उद्देश्य से उनपर गीता का प्रभाव दिखाने का जो ब्राह्मणवादी षड्यंत्र चल रहा है, उसका तार्किक रूप से भंडाफोड़ करते हैं। इस लेख में किसी जयपाल सिंह[8] द्वारा कबीर पर एक संपादित पुस्तक का विश्लेषण किया गया हैं जिसमें संपादक जबरन कबीर पर गीता का प्रभाव दिखाना चाहते हैं तथा अपने मंतव्य पर पैनलिस्ट विद्वानों की मुहर चाहते हैं। ‘कबीर का युगपथ’ पुस्तक के संपादक जयपाल सिंह ने इस पुस्तक में एक परिचर्चा की है जिसमें राजेश जोशी, लीलाधर मंडलोई, कर्मेंदु शिशिर और अजय तिवारी प्रतिभागी विद्वान हैं। गीता प्रभाव वाले संपादक के प्रश्नों पर राजेश जोशी और कर्मेंदु शिशिर, लीलाधर मंडलोई तो लगभग असहमति दिखाते हैं, पर अजय तिवारी सहमति जताते हैं। अजय तिवारी तो हद पार करते हुए कबीर को वेदांती सिद्ध करने लगते हैं।[9] लेखक [कंवल भारती] को अजय तिवारी से इसी तरह की आशा थी। लेकिन वे कहते हैं कि राजेश जोशी, लीलाधर मंडलोई और कर्मेंदु शिशिर का तुलसी के पक्ष में खड़ा होना, उनके प्रगतिशील नजरिए पर पैबंद लगाता है।
‘इतिहास के रैदास’ (2022) शीर्षक आलेख में कंवल भारती रैदास के संबंध में जो किंवदंतियां व अफवाहें फैली हुई हैं, उनकी ऐतिहासिक दृष्टि से पड़ताल करते हुए सत्य घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। वे दिखाते हैं कि जिस प्रकार से कबीर के पदों से छेड़छाड़ की गई, उनके संबंध में अनैतिहासिक और चमत्कारिक बातें फैलाई गई; उसी प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल रैदास के नाम को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। जिस प्रकार कबीर की क्रांतिकारिता को कुंद करने के लिए कबीर पंथ चलाया गया, उसी प्रकार रैदास को भक्त बनाने के लिए रविदासिया पंथ। हमें रैदास को कथाओं में न खोजकर इतिहास में खोजना चाहिए।
जबकि ‘क्या संत रैदास रामराज्य चाहते थे?’ (2023) शीर्षक आलेख में वे डॉ. प्रज्ञा पांडेय द्वारा ‘अमर उजाला’ में 5 फरवरी, 2023 को प्रकाशित ‘जनमानस की आस संत रविदास’ लेख का प्रतिवाद करते हैं। प्रज्ञा पांडेय के लेखन के हिडेन एजेंडे पर वे प्रकाश डालते हैं। लेखक के अनुसार प्रज्ञा पांडेय आरएसएस से जुड़ी मालूम पड़ती हैं और उन्होंने इतिहास की शिक्षा किताबों की जगह आरएसएस मुख्यालय से प्राप्त की हुई लगती हैं। प्रज्ञा पांडेय अपने लेख में रैदास को सगुण-निर्गुण से परे (परोक्ष रूप से सगुण भक्त) सिद्ध करती हैं। वे उन्हें सामाजिक समरसता का प्रतीक और ब्रह्मानंद की प्राप्ति का लक्ष्य रखने वाला भक्त सिद्ध करने का प्रयास करती हैं। रैदास के पाठकों को भ्रम से बचाने के लिए आलोचक कंवल भारती प्रज्ञा पांडेय के लेख का तार्किक विश्लेषण करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सगुण भक्ति एक ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जिसके मूल में वेद, पुराण, उपनिषद, वर्ण-व्यवस्था, स्वर्ग-नर्क, पूजा-कर्मकांडों में विश्वास है और रैदास इन सबके विरोधी थे।[10]
‘संत रैदास के राज्य की अवधारणा’ (2021) और ‘संत रैदास का बेगमपुरा’ (2019)’, इन दोनों आलेखों में कंवल भारती रैदास द्वारा परिकल्पित आदर्श राज्य का विश्लेषण करते हैं। रैदास पराधीनता के दर्द को भलीभांति समझते थे, उनका पद है– “पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन / रैदास पराधीन को, सभ ही समझें हीन।”[11] इसलिए रैदास बेगमपुर या अमृतदेश के रूप में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हैं, जहां कोई गम या दुख-द्वंद्व न हो और सभी समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के भाव के साथ गुजर बसर करें। किसी प्रकार का अभाव न हो। इसे लेखक मार्क्स और लेनिन से पहले का समाजवाद कहते हैं।
‘संत रैदास और नारी’ (2016) आलेख में उन्होंने रैदास की स्त्री दृष्टि पर विचार किया है। वे संत कवियों की स्त्री दृष्टि को उछालना सवर्ण आलोचकों का निजी षड्यंत्र मानते हैं, जिससे वे सगुण कवियों के पितृसत्तात्मक सोच को कवर कर सकें। अंत में सारा ठीकरा मध्यकाल पर फोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कबीर, रैदास आदि संतों को अपने तर्कों द्वारा स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर सिद्ध करते हैं। वे अपने इस आलेख में दिखाते हैं कि जो स्वयं भेदभाव का शिकार हो वह किसी अन्य के प्रति भेदभाव की दृष्टि कैसे रख सकता है? हम स्त्री पराधीनता पर तुलसी का एक पद याद रखते हैं ‘पराधीन सपनेहुं सुख नाहिं’[12], पर हम रैदास के पद को विस्मृत कर देते हैं– “पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत / रविदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत”[13]। जो किसी भी प्रकार के पराधीनता का शत्रु हो वह स्त्री को पराधीन कैसे समझ सकता है। जो वर्णव्यवस्था जैसे मानवीयता के विशाल शत्रु का विरोधी हो वह पितृसत्तात्मक सोच का समर्थन कैसे कर सकता है। वे मीरा और झाली बाई को रैदास की शिष्या मानते हैं। वे सवर्ण आलोचकों से प्रश्न करते हैं कि जब रैदास रामानंद के शिष्य हो सकते हैं, तो मीरा रैदास की शिष्या क्यों नहीं?
‘मीरा और संत रैदास का पुनर्पाठ (2023)’ आलेख दो भागों में बंटा है; पहले भाग में रैदास और मीरा के गुरु-शिष्या संबंध के बारे में तथ्यों की जांच की गई है तथा मीरा के वैधव्य की त्रासद स्थिति का वर्णन, राजस्थान की विधवा स्त्रियों के त्रासदियों का वर्णन है; दूसरे भाग में मीरा के प्रेम की अब तक जो अलौकिक व्याख्या की जाती रही है, उसकी लौकिक और भौतिक व्याख्या की गई है। मीरा के ‘गिरधर नागर’ को एक गुजराती ब्राह्मण[14] बताया गया है। यह आलोचक की अपनी परिकल्पना है। इस आलेख का आकर्षण मीरा का पक्ष ही है जो पुस्तक में आने से पहले से ही चर्चा में रहा है।
‘अक्क महादेवी और शिव’ (2024) आलेख में वे सुभाष राय की पुस्तक ‘दिगम्बर विद्रोहिणी : अक्क महादेवी’ का लौकिक पाठ प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार से सवर्ण आलोचक मीरा के पदों की अलौकिक व्याख्या करते रहे हैं, उसी प्रकार अक्क महादेवी के पदों का भी। कंवल भारती अक्क महादेवी के जीवन की घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पर लौकिक व्याख्या करते हैं। उनका प्रेमी एक मल्लिकार्जुन नामक व्यक्ति को बताते हैं। अक्क महादेवी पर हुए अब तक के शोध कार्यों के संबंध में लेखक कहते हैं, “अक्क महादेवी के वचनों को मूल रूप में पढ़े बिना उनको ठीक से नहीं समझा जा सकता। असल में अध्यात्म के घटाटोप में वास्तविक महादेवी को खोजने का काम शायद अभी होना शेष है। पर कौन करेगा? इस काम की अपेक्षा उन लोगों से नहीं की जा सकती, जो साहित्य और दर्शन में भी वर्ण-व्यवस्था के रक्षक हैं। ये वही लोग हैं, जिन्होंने बुद्ध को ठिकाने लगाया, कबीर से लेकर मीराबाई तक सबको आध्यात्मिक बनाने का ही काम किया।”[15]
‘क्या भक्ति आंदोलन विफल हुआ?’ (2020) आलेख को कंवल भारती ने मैनेजर पांडेय के एक प्रसिद्ध आलेख ‘भक्ति काव्य और हिंदी आलोचना’ के प्रतिपक्ष में लिखा है। उन्होंने मैनेजर पांडेय के उन सभी तर्कों का खंडन किया हैं जो निर्गुण क्रांति को कमजोर करती हैं और सगुण क्रांति को ताकतवर। कंवल भारती के तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि मैनेजर पांडेय सतही मार्क्सवादी थे, अंदर से उनका ब्राह्मणवाद सदैव उनपर हावी रहा। कंवल भारती के लिए भक्ति आंदोलन से तात्पर्य केवल निर्गुण क्रांति से है और वे निर्गुण क्रांति के विफल होने के कारणों को बताते हैं। इस ओर मुक्तिबोध भी अपने एक आलेख में इशारा कर चुके हैं। कंवल भारती कहते हैं, “निर्गुणधारा अपने समय में जिस ब्राह्मण और मुल्ला के खिलाफ युद्धरत थी, वे उस काल के शासक वर्ग थे। शासक वर्ग केवल समाज की सत्ताधारी भौतिक शक्ति ही नहीं होता, बल्कि बौद्धिक शक्ति भी होता है। इस दृष्टि से दोनों तत्कालीन सत्ता के केंद्र बने हुए थे। तब क्या कोई सोच सकता है कि सत्ता के इस बौद्धिक केंद्र को निर्गुणधारा की वैचारिक क्रांति से कितना बड़ा खतरा रहा होगा? और इससे निम्न-जातीय शूद्र कवियों की जान कितने खतरे में पड़ी होगी? तब किसने किसको खत्म किया होगा, इसे समझना मुश्किल नहीं है। कमजोर व्यक्ति शब्दों से लड़ता है और ताकतवर अपने सारे साधनों से लड़ता है। इसलिए पूरा भक्ति आंदोलन नहीं, सिर्फ निर्गुण आंदोलन सामंती और ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा हुआ था। और उसी ने ‘अभिव्यक्ति के सारे खतरे’ उठाए थे। उस अभिव्यक्ति में आग थी, जिसने ब्राह्मणवाद के मार्ग में अंगार बिखेर दिए थे। इसलिए निर्गुण को विफल होना ही था, क्योंकि वह शासित जातियों का आंदोलन था और वह जिसके विरुद्ध खड़ा था, वह ताकतवर शासक वर्ग था। … अगर निर्गुण काव्य ने निम्न वर्गों पर गहरा प्रभाव न डाला होता, तो क्या वह ब्राह्मणवाद के लिए खतरा बनता? क्या तुलसीदास और सूरदास उसका खंडन करते? लेकिन तथ्य यह भी है कि जिस पौधे को खाद-पानी नहीं मिलता, वह मर जाता है। इसी तरह विचार भी मर जाते हैं, जिनका प्रचार नहीं किया जाता है। विचार वही अमर होते हैं, जिनको अमर बनाने के लिए पाला-पोसा जाता है। निर्गुण को वह खाद-पानी नहीं मिला, जो सगुण को मिला। सगुण दर्शन शासक वर्ग के हित में था, इसलिए शासक वर्ग ने उसे सारे साधनों से पाला-पोसा।”[16]
वस्तुतः हम देखते हैं कि आलोचक कंवल भारती भक्ति आंदोलन की एक नई लौकिक और भौतिक संदर्भों में व्याख्या करते हैं। इनका अभिधात्मक व्याख्या स्वरूप इनके पत्रकार व्यक्तित्व का ही परिणाम लगता है। अब तक भक्ति आंदोलन की जो व्याख्याएं हुई हैं वह वर्णाश्रमवादी वैचारिकी की ही उपज हैं। कथित प्रगतिशील धारा के सवर्ण आलोचक भी अपने जन्मजात संस्कारों से मुक्त नज़र नहीं आते। वरिष्ठ आलोचक डॉ. सेवा सिंह कहते हैं कि वर्गीय अवधारणा (समाज) ब्राह्मणीय विचारधारा का ही उपजीव्य है।[17] वास्तव में कंवल भारती, जो चार्वाक, आजीवक, बौद्ध, जैन, कबीर, रैदास, फुले, बिरसा, पेरियार, आंबेडकर की परंपरा से आते हैं तथा इस परंपरा से आने वाले कोई भी प्रतिबद्ध आलोचक द्वारा भारत और भारतीय समाज की जो व्याख्या होगी वही मूल व्याख्या मानी जानी चाहिए, शेष जो वैदिक परंपरा की व्याख्या है उसे प्रतिक्रांति धारा की वैकल्पिक (काल्पनिक) व्याख्या समझ कर बगल में खिसका देना चाहिए।
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक की ओर से जो चूक नज़र आती है उसपर भी एकबारगी विचार करना चाहिए। मसलन, मीरा और अक्क महादेवी के संबंध में लेखक की जो मौलिक स्थापनाएं हैं, उनका स्रोत देना चाहिए। एक शोधार्थी अपने कार्यों को उन्हीं संदर्भों के सहारे आगे बढ़ाता है। हालांकि यह नई उद्भवनाएं हैं इसलिए हम इसे आलोचना की नई दृष्टि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। देखा जाए तो सवर्ण आलोचकों की कितनी ही पुस्तकें बिना संदर्भों की हैं और हमने उन्हें आंख बंद करके स्वीकार कर लिया है, जैसे – रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी आदि। कबीर के पद सांप्रदायिकता से मुक्त हैं, उनके यहां उदाहरण मिलते हैं। लेकिन रैदास को यदि सांप्रदायिकता से मुक्त दिखाना है तो उनकी उस तरह के पदों के उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे, जिनका इस पुस्तक में अभाव है।
अंततः कंवल भारती भी भक्ति के अंतर्गत ही क्रांतिकारिता खोजने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्ति (सगुण भक्ति) स्वयं में सत्ता सापेक्ष है और सत्ता का एक साधन है। इस पुस्तक में निर्गुण आंदोलन को भक्ति से अलगाने वाले पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव दिखता है। हालांकि लेखक के पास अपनी मौलिक संकल्पना है जो सही दिशा में चिंतन की ओर है, किंतु यदि उन्होंने सेवा सिंह और विनोद शाही की पुस्तकों को एक बार देखा होता तो उन्हें अपनी परिकल्पना के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिल जाते। अथवा इस पुस्तक के लेख पुराने होने के कारण लेखक के नए विचार पूर्णतः समाहित नहीं हो पाए हैं। इस पुस्तक के अध्ययन से इतना ज्ञान तो अवश्य हो जाता है कि दक्षिणपंथी सह वर्णाश्रमवादी चिंतकों एवं इतिहासकारों ने मध्यकाल के लगभग सभी प्रतिरोध के नायकों को भक्त बना कर ठिकाने लगा दिया है।
समीक्षित पुस्तक : भक्ति आंदोलन और निर्गुण-क्रांति
लेखक : कंवल भारती
प्रकाशक : स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 350 रुपए
संदर्भ सूची :
[1] भारती, कंवल, (2025), भक्ति आंदोलन और निर्गुण-क्रांति, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 18
[2] वही, पृष्ठ 21
[3] वही, पृष्ठ 27
[4] वही, पृष्ठ 46
[5] वही, पृष्ठ 52
[6] http://raigarsamaj.blogspot.com/2016/10/blog-post_62.html , 26.07.2025 , 22:28
[7] भारती, कंवल, (2025), भक्ति आंदोलन और निर्गुण-क्रांति, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 109
[8] वही, पृष्ठ 112
[9] वही, पृष्ठ 116
[10] वही, पृष्ठ 127
[11] वही, पृष्ठ 133
[12] पोद्दार, हनुमान प्रसाद (सं.), (2014), रामचरितमानस, बालकाण्ड, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ 116
[13] भारती, कंवल, (2025), भक्ति आंदोलन और निर्गुण-क्रांति, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 147
[14] वही, पृष्ठ 165
[15] वही, पृष्ठ 185
[16] वही, पृष्ठ 195
[17] सिंह, सेवा, (2022), भक्ति का लोकवृत : एक इतिहासहंता मीमांसा, आधार प्रकाशन, हरियाणा, पृष्ठ 34
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in