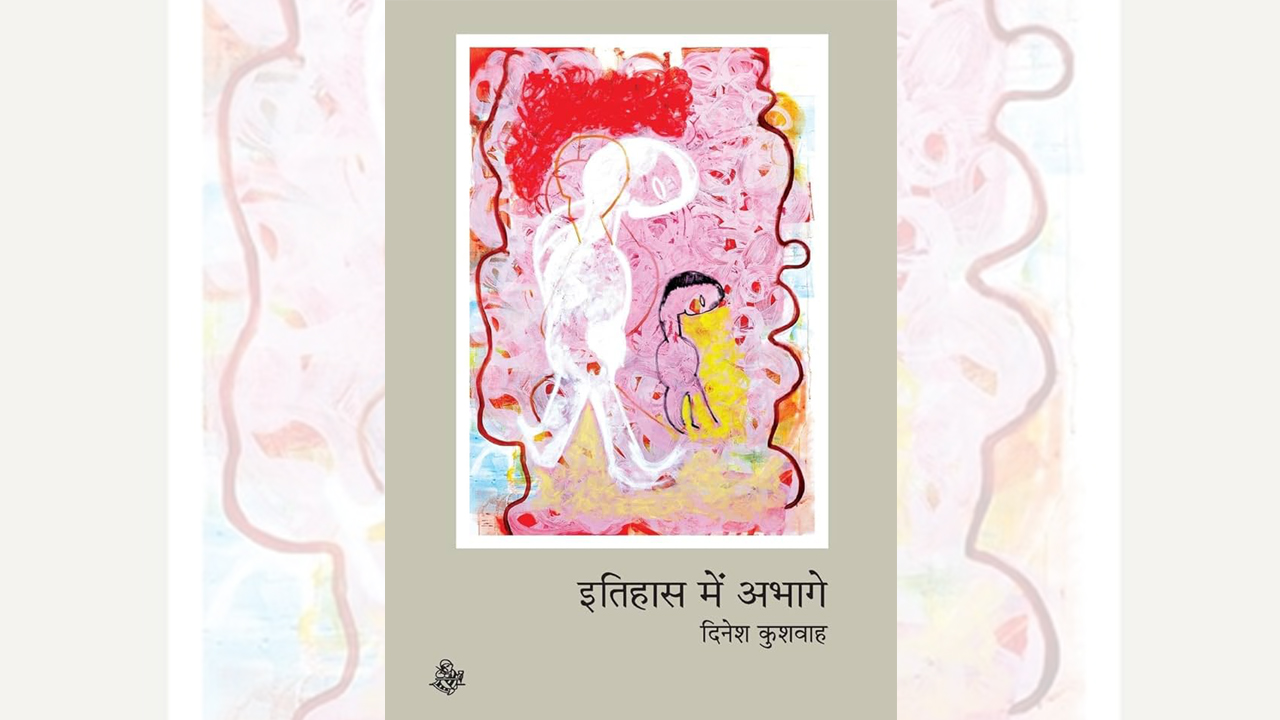राजेन्द्र यादव कथाकार थे, आलोचक थे और संपादक थे। वे भाषाविज्ञानी नहीं थे। बावजूद इसके उन्होंने ‘हंस’ में अग्रलेख लिखते वक्त जगह-जगह भाषा विषयक अत्यंत तल्ख टिप्पणियां की थीं। उन्होंने लिखा है कि भाषाएं न बिगड़ती हैं, न मरती हैं, वे मानवसमाज की तरह सिर्फ विकसित होती हैं। वे घरों-परिवारों, बाजारों या दूसरे कामकाजी क्षेत्रों, खेतों-खलिहानों और कारखानों में अपना रूप ग्रहण करती हैं। उन्हें सबसे ज्यादा बदलती हैं औरतें और श्रम से जुड़े लोग। इस सबकी जानकारी किताबी भाषा विशेषज्ञों को नहीं होती। भाषाएं शुद्धता और उत्कृष्टता के आग्रहों में गतिहीन होकर घुटती और अंतत: मर जाती हैं (हंस, नवंबर, 2003)।
 राजेन्द्र यादव मानते थे कि भाषा का विकास सबसे अधिक औरतें और श्रम से जुड़े लोग किया करते हैं। आचार्यगण उन्हें भले ही भाषा को भ्रष्ट करने वालों की श्रेणी में रखें, पर भाषा के विकास का सत्य यही है। राजेन्द्र यादव की नजर में किताबी भाषा विशेषज्ञों के लिए जो अशुद्ध और निकृष्ट कोटि की भाषा है, बाद में चलकर वही शुद्ध और उत्कृष्ट कोटि की भाषा हो जाती है। विवाह, बारात के बहुतेरे शब्दों का प्रचलन महिलाओं ने किया है।
राजेन्द्र यादव मानते थे कि भाषा का विकास सबसे अधिक औरतें और श्रम से जुड़े लोग किया करते हैं। आचार्यगण उन्हें भले ही भाषा को भ्रष्ट करने वालों की श्रेणी में रखें, पर भाषा के विकास का सत्य यही है। राजेन्द्र यादव की नजर में किताबी भाषा विशेषज्ञों के लिए जो अशुद्ध और निकृष्ट कोटि की भाषा है, बाद में चलकर वही शुद्ध और उत्कृष्ट कोटि की भाषा हो जाती है। विवाह, बारात के बहुतेरे शब्दों का प्रचलन महिलाओं ने किया है।
आचार्यगणों ने कभी उन्हें भ्रष्ट शब्द बताया होगा, पर आज वे हिंदी शब्दकोश में मानक हो गए हैं। मिसाल के तौर पर समधी, सिन्होरा, कोहबर जैसे शब्दों को लिया जा सकता है। आचार्यगण मानते हैं कि ‘समधी’ का शुद्ध रूप ‘संबंधी’ है, पर हिंदी शब्दकोश, महिलाओं द्वारा दिए गए ‘समधी’ शब्द को मानक मान चुका है। व्याकरण की नजर में भाषा की जो अशुद्धियां हैं, वही भाषाविज्ञान की नजर में भाषा का विकास है। समय आने पर व्याकरण भी उसे मानक और शुद्ध मान लेगा।
राजेन्द्र यादव की यह भी स्थापना है कि भाषा का सर्वाधिक विकास खेतों-खलिहानों में, कारखानों में और दूसरे श्रमशील क्षेत्रों में हुआ करता है। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि भाषा के विकास में किसानों, मजदूरों एवं श्रम से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसानों से जुड़े हजारों शब्दों को कोशकारों ने ग्रामीण अर्थात् अशुद्ध मानकर खारिज कर दिया है, पर वास्तव में वे अशुद्ध होते नहीं हैं।
भारत छुआछूत का देश है। छुआछूत की बीमारी यहां की भाषा में भी लगी हुई है। शुद्धतावादी आचार्य किसान-मजदूरों के शब्दों को भ्रष्ट (अछूत) मानकर भाषा में प्रयोग से वंचित कर देते हैं, जबकि उन्हें अपना लेने से भाषा समृद्ध होगी। कारखानों में कई भाषाएं बोलने वाले लोग एक-साथ काम करते हैं। फ लस्वरूप उनकी भाषाओं के बीच शब्दों का आदान-प्रदान होता है। व्याकरण के जानकार लाख कहें कि कारखानों में भाषा प्रदूषित हो रही है, पर राजेेन्द्र यादव उसे भाषा का विकास मानते हैं। आज भी पेशे अथवा श्रम से जुड़े लोगों के शब्दों से लोकमानस भरा पड़ा है पर हिंदी के आचार्यगण मानकीकरण की कसौटी पर उसे खारिज किए जा रहे हैं। उन्हें श्रम-संस्कृति की अपेक्षा यज्ञ-संस्कृति के शब्दों पर आस्था है। वे देवी-देवताओं के पर्यायों में विश्वास करते हैं। आज भी देवी-देवताओं के पर्यायों से हिंदी के शब्दकोश लदे हुए हैं।
राजेन्द्र यादव इसी अंक में आगे लिखते हैं कि हिंदी के साथ सुविधा यह भी है कि समृद्ध करने वाली अनेक बोलियां उसे शक्ति और ऊर्जा देती हैं: ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी जैसी बड़ी बोलियों के भंडार हिंदी के लिए खुले हैं। दरअसल कभी भोजपुरी साहित्य भी हिंदी साहित्य का एक अंग हुआ करता था। कबीर इसके प्रमाण हैं। कबीर की कविताओं में भोजपुरी के शब्द भरे पड़े हैं। आज ऐसा नहीं है। आधुनिक भोजपुरी साहित्य को हिंदी साहित्य से बाहर कर दिया गया है। ब्रज, अवधी, राजस्थानी-सभी हिंदी की बोलियों के साहित्य का यही हाल है। कौरवी, जिसकी बुनियाद पर हिंदी भाषा खड़ी है, उसके शब्द हिंदी शब्दकोश से बाहर हैं। उन्हें लोकभाषा के शब्द का दर्जा प्राप्त है। ऐसे शब्दों के साथ आचार्यगण दोयम दर्जे का व्यवहार किया करते हैं।
राजेन्द्र यादव ने शब्दविज्ञान के मुंह में भी हाथ डाला है। प्रसंग, विभूति नारायण राय का ‘छिनाल’ शब्द है। राय ने स्थापित किया कि ‘छिनाल’ भोजपुरी भाषा का शब्द है और स्त्री-पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने बताया कि ‘छिनाल’ शब्द छिन्न+नाल से बना है, यानी अपनी जड़ों, परिवेश, परंपराओं और पतिव्रत से भटकी हुई औरत के लिए। राजेन्द्र यादव ने लिखा कि ‘छिनाल’ तद्भव शब्द है, तत्सम् नहीं। इस तरह के संधि-विच्छेद सिर्फ तत्सम् शब्दों में ही किए जाते हैं। तद्भव तो अपने रूढ़ और प्रचलित अर्थों में ही स्वीकृत किए जाते हैं (हंस, सितंबर, 2010)। जाहिर है कि राजेन्द्र यादव की यह टिप्पणी अत्यंत बारीक है। वे एक झटके में ही ‘छिनाल’ शब्द की व्युत्पत्ति खारिज कर देते हैं और संधि-जुगाड़ की भत्र्सना करते हैं।
राजेन्द्र यादव व्युत्पत्तिशास्त्र के ज्ञाता नहीं हैं पर उनके द्वारा स्थापित व्युत्पत्तियां आज भी बहस की मांग करती हैं। वे एकमात्र ऐसे व्युत्पत्तिशास्त्री हैं जो भगवान, भाग्य और भगवा जैसे शब्दों को सीधे ‘भग’ (योनि) से जोड़ देने की हिम्मत रखते हैं।
भाषा और लिपि के संबंधों पर विचार करते हुए राजेन्द्र यादव ने लिखा है कि लिपि कभी भाषा नहीं बनाती। वे एक-दूसरे के लिए अनिवार्य भी नहीं हैं। उनका मानना है कि हिंदी रोमन अथवा फारसी किसी भी लिपि में जा सकती है। मिसाल के तौर पर, मलिक मोहम्मद जायसी के ‘पद्मावत’ की मूल पांडुलिपि फारसी में है पर यह महाकाव्य हिंदी की धरोहर है। देवनागरी भी केवल हिंदी की बपौती नहीं है। उसमें संस्कृत, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, गुजराती, नेपाली, पंजाबी जैसी अलग-अलग भाषाएं लिखी जाती हैं। सच यह है कि भाषा का कोई सीधा संबंध लिपि से नहीं है। विकासशील भाषाएं हमेशा लिपि की कैद से छूटने के लिए छटपटाती रहती हैं (हंस, नवंबर, 2013)।
हिंदी प्रदेशों में दलित-पिछड़ों के नामवाची शब्दों को लेकर राजेन्द्र यादव ने लिखा है कि भारत में श्रम और उत्पादन से जुड़ी जातियों को अशिक्षित, कूढ़मगज बनाए रखने के साथ ही तरह-तरह से अपमानित-प्रताडि़त किया जाता था। उनके नाम घृणास्पद, मजाकिया या उन्हें बेवकूफ सिद्ध करनेवाले होते थे। कोई घुरहू, घसीटा होता था, तो कोई खचेड़ू, बुद्धू और जंगालिया (हंस, अक्टूबर, 2010)। कहना न होगा कि राजेन्द्र यादव की यह टिप्पणी वर्तमान में भी पिछड़े-दलित समाज के नामवाची शब्दों में दिखाई पड़ेगी। फेकू, घुरफेंकू, बेचन, बेचू, मुअनी जैसे नामों से आज भी समाज के हाशिए के लोग पुकारे जाते हैं। जातिसूचक शब्दों को किस तरह से गाली के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, किसी से छिपा नहीं है। ‘भठियारा’ का अर्थ ‘सराय का मालिक’ है पर इसका इस्तेमाल गाली के अर्थ में किया जाता है। ‘चोरी-चमारी’ युग्म शब्द बन गया है, मानो चोरी का काम सिर्फ चमार जाति के लोग ही किया करते हैं।
मंडल आयोग की सिफारिशों में ‘कुचरा’ तथा ‘बुड़बक’ दो जातियां भी शुमार हैं पर हिंदी में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किसी को अपमानित करने के लिए किया जाता है। आदिवासियों का एक तबका ‘असुर’ है, जो झारखंड में निवास करता है और जिसका प्रमुख पेशा लोहा गलाने का है। ‘असुर’ का अर्थ-प्रयोग तो हिंदी शब्दकोश में जगजाहिर है, पर हिंदी की आदिवासी विरोधी मानसिकता ने अन्य कई आदिवासी तबकों के नामों को घृणास्पद अर्थों से भरकर स्खलित किया है। जैसे ‘असुर’ आदिवासियों का तबका है, वैसे चुहाड़, चाईं और चुतिया भी आदिवासियों के तबके हैं। इनका प्रयोग भी हिंदी में किसी को अपमानित करने के लिए ही किया जाता है। लाख की चूडिय़ां बनाने वाले कारीगर के लिए ‘लखेरा’ शब्द प्रचलित है पर भोजपुरी में ‘लखेरा’ का अर्थ ‘आवारा’ होता है। ऐसे ही न जाने कितने जातिसूचक शब्दों को शुद्धतावाची आचार्यों ने दूसरे अर्थों से भरकर गंदा और घृणास्पद बनाने का काम किया है।
शायद इसीलिए राजेन्द्र यादव ने लिखा है कि सौ साल पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ‘सरस्वती’ के माध्यम से हिंदी भाषा, व्याकरण व वर्तनी का जो मानकीकरण किया था, ‘हंस’ ने उन सब पर प्रश्नचिन्ह लगाने का दुस्साहस किया (हंस, अगस्त, 2010)।
(फारवर्ड प्रेस के फरवरी, 2014 अंक में प्रकाशित )
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in