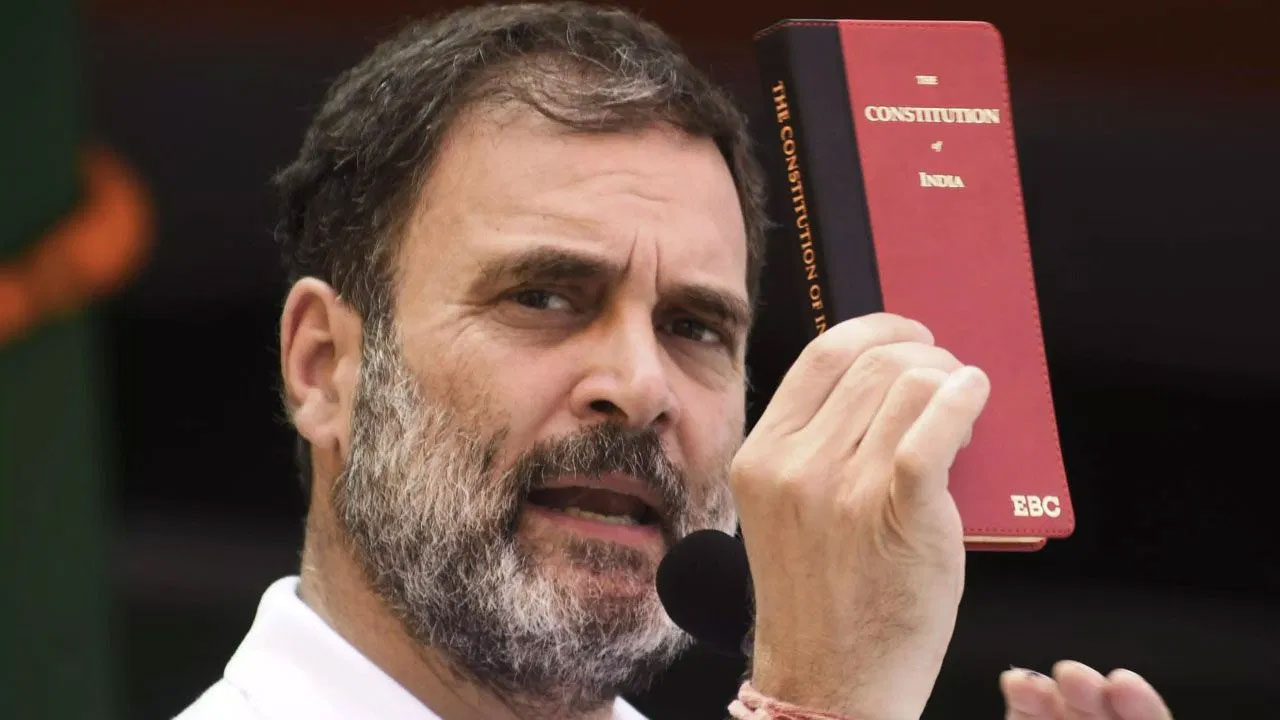कांशीराम : 15 मार्च, 1934 – 9 अक्टूबर, 2006
बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम को, उनकी 81वीं जयंती के अवसर पर, श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा कि हम भारत के जातिवाद से ग्रस्त समाज में परिवर्तन लाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्मरण करें।
कांशीराम के राजनैतिक परिदृश्य पर उभरने से बहुत पहले, फुले, आंबेडकर व पेरियार ने सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे पर गहराई से विचार किया था। उदाहरण के लिए, आंबेडकर ने जोर देकर कहा था कि सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनैतिक परिवर्तन अर्थहीन हैं। अपने अत्यंत विद्वतापूर्ण लेख ‘रानाडे, गाँधी एंड जिन्ना’ (1943) में बाबासाहेब ने तथ्यपरक व तार्किक तरीके से यह साबित किया था कि सामाजिक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ‘अधिकांश लोगों को यह अंदाज़ा नहीं है कि समाज, किसी व्यक्ति का, सरकार की तुलना में कहीं अधिक दमन व उत्पीडऩ कर सकता है’, उन्होंने लिखा था।

आंबेडकर के विचारों से गहरे तक प्रभावित कांशीराम ने भी इस मुद्दे पर जोर दिया। आंबेडकर की तरह, कांशीराम ने भी ‘सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन’ के प्रति गंभीर न होने के लिए गाँधी व जिन्ना की आलोचना की। वे कहते थे कि परतंत्र भारत में जहाँ ऊंची जातियां अंग्रेजों की गुलाम थीं, वहीं दमित वर्ग, ‘गुलामों के गुलाम’ थे। जहाँ ऊंची जातियों के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आन्दोलनों का प्रयास था कि अंग्रेज जल्दी से जल्दी उन्हें सत्ता सौपें (स्वराज) वहीं नीची जातियों के नेता, ‘आत्मसम्मान’ व ‘सदियों पुरानी गुलामी व संत्रास से मुक्ति के लिए संघर्षरत थे ‘उस गुलामी से, जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ पता ही नहीं था’। उन्होंने इस मुद्दे पर अपने पर्चे (‘द चमचा एज’, 1982) में विस्तृत प्रकाश डाला। यह पर्चा पूना समझौते के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिखा गया था।
तत्पश्चात, सन 1997 में, जब स्वाधीनता की पचासवीं वर्षगाँठ के अवसर पर, ब्राह्मणवादी व पूंजीवादी शासक वर्ग स्वतंत्र भारत की ‘उपलब्धियों’ का जश्न मना रहा था, कांशीराम ने उनका ध्यान सडांध मारते भारतीय समाज की ओर आकर्षित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ‘स्वाधीन भारत में बहुजन पराधीनता’ विषय पर भाषण देते उन्होंने आम्बेडकर की इस चिंता को रेखांकित किया कि सामाजिक दास्यमुक्ति के बगैर, केवल राजनैतिक स्वतंत्रता से लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। ‘भारत ने बाहरी साम्राज्यवादी ताकतों को उखाड़ फेंका था परन्तु देश के अन्दर कुछ वर्ग अब भी जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये जंजीरें थीं खून पीने वाले साहूकार, सामाजिक उंचनीच, जाति व्यवस्था, धार्मिक भेदभाव आदि’ (अनुज कुमार द्वारा सम्पादित, ‘बहुजन नायक कांशीराम के अविस्मरणीय भाषण’, 2000, पृष्ठ 23)
आरपीई से लेकर बसपा तक, राजनेता व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने पचास वर्ष की जीवनयात्रा में, कांशीराम, न्याय की राह की हर बाधा ‘चाहे वह अछूत प्रथा हो, असमानता हो, जातिवाद हो या पुरातनपंथी विचार या सोच’ को दूर कर समाज में बदलाव लाने के प्रति प्रतिबद्ध रहे. उन्हें महसूस हुआ कि अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें ‘मनुवादी व्यवस्था की शिकार’ 6000 जातियों को एक करना होगा। वे यह जानते थे कि जाति ‘दुधारी तलवार’ है, जो बहुजनों के लिए लाभकारी हो सकती है, बशर्ते वे अपने दमनकतार्ओं के विरुद्ध लामबंद हो जाएँ. उन्हें पता था कि अगर बहुजनों को उनके साथ हो रहे भेदभाव और उनके शोषण के प्रति जागृत कर दिया जाये तो वे राजनैतिक सत्ता हासिल कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने समाजसुधार आन्दोलन की ज़मीन पर बसपा को खड़ा किया, ताकि ‘सत्ता’ की ‘गुरकिल्ली’ हासिल की जा सके।
जहाँ वे जीवनभर जातिगत भेदभाव के खिलाफ खुल कर बोलते रहे और नीची जातियों की एकता स्थापित करने में जुटे रहे, वहीं उनके आलोचकों ने यह कहकर उनपर हल्ला बोला कि वे ‘जातिवाद’ फैला रहे हैं। कुछ उदारवादी व वामपंथी अध्येताओं ने तो यह आरोप भी लगाया कि वे आम्बेडकर की राह से भटक गए हैं। उनका कहना था कि जहाँ आम्बेडकर जाति के उन्मूलन की बात कहते थे वहीं कांशीराम, जातियों की बीच की खाई को और गहरा कर रहे हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं था। कांशीराम जातिविहीन समाज के निर्माण के पैरोकार थे और वे यह नहीं मानते थे कि जातिगत दमन की बात करने से जातिवाद बढेगा। उलटे, उनका तर्क यह था कि जातिगत दमन के अस्तित्व को स्वीकार करना, उसका उन्मूलन करने की आवश्यक शर्त है। ‘हम जाति के उन्मूलन की बात करते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए, सबसे पहले, हमें जाति का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। हम जाति से अनभिज्ञ रहकर या उसे नजऱंदाज़ कर, जाति को नष्ट नहीं कर सकते।’ (कुमार, 2000, पृष्ठ 68)
कुछ समय पहले, जाति जनगणना को लेकर भी इसी प्रकार की बहस छिड़ी थी। उच्च जातियों के इस तर्क का जवाब देते हुए कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, दलितबहुजन अध्येताओं ने कांशीराम के तर्क को दोहराते हुए कहा कि जाति जनगणना से नीची जातियों की सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, जिससे नीति-निर्माताओं और सरकार को जातिवाद से लडऩे के लिए उपयुक्त कदम उठाने में मदद मिलेगी।
जैसा कि द्रविड़ इतिहास, जाति संबंधों व जनसंस्कृति के जानेमाने विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर एमएसएस पांडियन ने लिखा था -ऊंची जातियों के उदारवादी व वामपंथी विद्वान अक्सर सार्वजनिक मंचों से जाति के प्रश्न पर चर्चा का विरोध करते हैं, परन्तु वे स्वयं ‘जाति व जातिगत संबंधों का दूसरे रूपों में इस्तेमाल करते हैं’ (‘वन स्टेप आउट ऑफ़ मोडरनिटी’, इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 4 मई, 2002)। ऊंची जातियों के लोग जाति-आधारित राजनैतिक एकता और आरक्षण की पुरजोर खिलाफत करते हैं, परन्तु अपने हितों की पूर्ति के लिए अपनी जाति के तंत्र का इस्तेमाल करने में उन्हें कोई गुरेज़ नहीं होता। समाजशास्त्री विवेक कुमार ठीक ही पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि व्यापार-व्यवसाय, मीडिया, शिक्षण संस्थानों व न्यायपालिका में ऊंची जातियों का कब्ज़ा है?
यह विडम्बना ही है कि ऊंची जातियों के लोग जाति व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ उठाते हैं और नीची जातियों पर जातिवाद को बढ़ावा देने का दोषी ठहराते हैं। कांशीराम ने ऊंची जातियों के इस दोगले चरित्र को उजागार करते हुए कहा था, ‘जाति व्यवस्था से केवल मुट्ठी भर ऊंची जातियों को लाभ मिला है। इसके विपरीत, 85 प्रतिशत बहुजनों को इससे नुकसान हुआ है और वे हजारों सालों से अपमान और शोषण का शिकार हो रहे हैं। जब ऊंची जातियों को जाति व्यवस्था से लाभ ही लाभ है तो वे भला क्यों इसके उन्मूलन के लिए पहल करेंगीं।’ (कुमार, 2002, पृष्ठ 68)
समाज के रूढ़िवादी तबके को तो छोडिये, मुख्यधारा के वामपंथी और समाजवादी भी जाति के प्रश्न पर चर्चा से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि जातिगत एकता से ‘वर्गीय एकता’ टूट जाएगी। वामपंथियों और समाजवादियों का मखौल बनाते हुए कांशीराम ने कहा था, ‘हमारे बुद्धिजीवी सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद, समाजवाद और साम्यवाद में है। जिस देश में मनुवाद है, वहां कोई और वाद सफल ही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई वाद, ‘जाति’ के यथार्थ को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। इसलिए, बुद्धिजीवियों का यह कत्र्तव्य है और मेरा भी यह कत्र्तव्य है कि हम एक ऐसे वाद का विकास करें, जो मनुवाद और जाति के अस्तित्व को नकारे नहीं’ (कुमार, 2000, पृष्ठ 78)।
इस दौर में, जब सहचर पूँजीवाद और ब्राह्मणवाद का हमला तेज हो रहा है, समय आ गया है कि हम सब कांशीराम के क्रांतिकारी विचारों को अपनाएं और प्रजातान्त्रिक शक्तियों का वृहद् गठबंधन बनाने की ओर अग्रसर हों।
(फारवर्ड प्रेस के मार्च, 2015 अंक में प्रकाशित )
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in