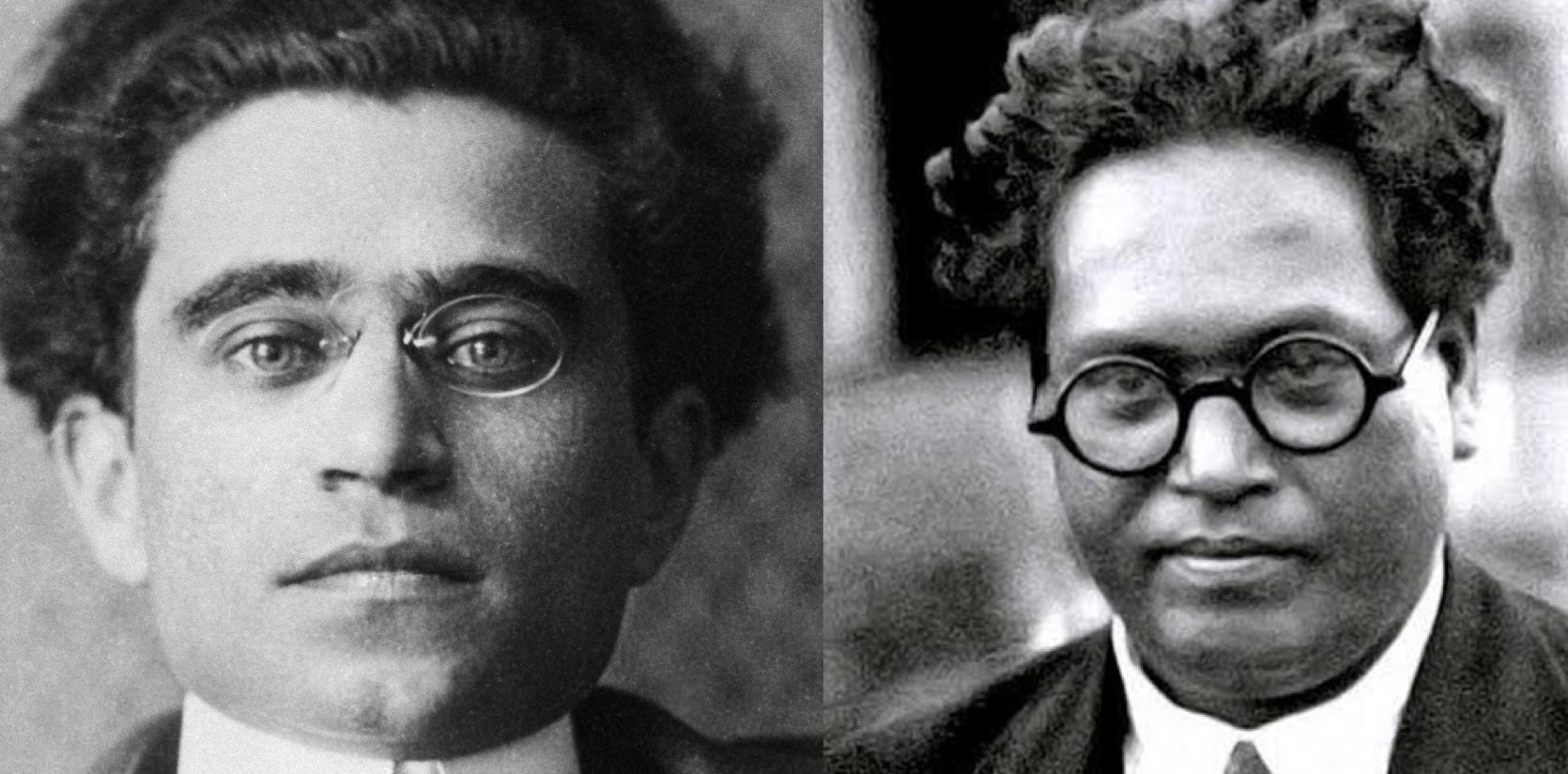वैश्वीकरण में मुक्त व्यापार और मुक्त संचार ने जहां विश्व को आर्थिक उदारता दी है वहीं उसने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र को भी अधिक उदार और व्यापक बनाया है। वैश्वीकरण की और चाहे जो भी सीमाएं हों, पर इसकी मुक्ति चेतना में हाशिए की चीजों को भी महत्व के केन्द्र में स्थापित करने की प्रवृत्ति है। संचार-क्रांति इसे और व्यापक बना रही है। इसके पैरोकारों का कहना है कि जिस प्रकार बांध टूट जाने से पानी समुद्र की सतह पकड़ लेता है, उसी प्रकार मुक्त व्यापार और बाजार से धनी देशों की पूंजी और पैसे गरीब और विकासशील देशों में जाएंगे, वहां की गरीबी में कमी आएगी और समानता बढ़ेगी। भावों और विचारों का भी वही हाल है। कोई माने-न-माने, जिस प्रकार ‘ब्लैक लिटरेचर’का प्रभाव मराठी के ‘दलित साहित्य’पर पड़ा, उसी प्रभाव में हिन्दी का ‘दलित साहित्य’भी उदित हुआ। भारत जैसे दुनिया के सर्वाधिक बहुलतावाले देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निजी सत्ता प्रतिष्ठानों को भी अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा अन्य यूरोपीय देशों की तरह डायवर्सिटी के तहत वंचित और पिछड़े समाजों को अवसर देने ही पड़ेंगे। भारतीय लोकतंत्र अभी केवल राजनीति तक सीमित है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र कायम होना अभी बाकी है।
इसलिए अस्मिताओं और अस्तित्व की टकराहटें हैं। अस्मिताओं की इस उथल-पुथल और टकराहटों ने अनेक नए सांस्कृतिक और साहित्यिक विमर्शों को जन्म दिया है। दलित, स्त्री, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रवासी और अन्य नए विमर्श तेजी से उभर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी या शूद्र साहित्य विमर्श भी एक नया विमर्श है, जिसका दायरा अन्य विमर्शों से बड़ा है।
अस्मितामूलक साहित्य
दलित साहित्य वह है, जिसमें दलितों को नायकत्व प्राप्त हो, स्त्री साहित्य वह है, जिसमें स्त्रियों का नेतृत्व हो, आदिवासी, अल्पसंख्यक, प्रवासी आदि तमाम विमर्शों को लेकर लगभग यही सच्चाई सामने आती है। भोगे हुए यथार्थ के नाम पर ऐसे तमाम हक तो उन्हें मिल ही जाते हैं। तो क्या शूद्र अथवा ओबीसी साहित्य का मामला भी यही सच नहीं है ? स्मरण रहे फुले ने पिछड़ों को शूद्र और अछूतों को अतिशूद्र कहा था। वह रचना जिसमें तमाम विघ्न-बाधाओं को तोड़ता हुआ पिछड़े वर्ग का नायक एक प्रतिमान खड़ा करता है, ओबीसी या शूद्र साहित्य है।
इस दृष्टि से देखें, तो साहित्य, संस्कृति, समाज और राजनीति में ओबीसी नायकों की कमी नहीं है। उनके नायकत्व को साहित्य में कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं गया, जिस दृष्टि से हाशिए के अन्य विमर्शों ने अपने नायकों को देखा है। किन्तु क्या जैसे-तैसे केवल नायकत्व और जीत दिला देना ही ओबीसी साहित्य की अस्मिता और पहचान हो सकती है ? इसके पीछे कोई सिद्धांत या विचारधारा नहीं हो सकती ?
ओबीसी साहित्य का समाजशास्त्र और राजनीति
ओबीसी या पिछड़ा कोई जाति नहीं एक संवैधानिक वर्ग है, जिसमें हिन्दू, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सैकड़ों जातियां शामिल हैं, जिन्हें ‘मंडल कमीशन’के तहत देश में और स्थानीय सामाजिक-शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के अनुरूप कुछ प्रांतों में सरकारी नौकरियों मे आरक्षण प्राप्त है। इनमें से नाई, कहार, कुम्हार, कानू, कुंजरा, कबारी, मल्लाह, तांती, नट, बंजारा, जुलाहा, धुनिया, धोबी; मुस्लिम, धनकार,  लोहार आदि ऐसी सैकड़ों कामगार जातियां हैं, जिनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। यह सच है कि दलित अछूत समझे जाते थे और सवर्ण समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता था। सदियों तक वे अपमान और वर्ण-व्यवस्था जनित अमानवीय शोषण और यातनाओं के शिकार हुए। पर पिछड़े समाज के लोग सवर्ण समाज के सीधे सम्पर्क में रहे। उनके दास-दासी और मजदूर बनकर दलितों से भी अधिक सामंती जुल्म सहे। बेकारियां कीं, परिवार सहित दिन-रात उनकी सेवा की, बदले में तिरस्कार, अपमान और पशुवत् व्यवहार के शिकार हुए। वस्तु की तरह उनका क्रय-विक्रय होता रहा। दहेज के रूप में इनकी बहू-बेटियां मालिकों की बेटियों की दासी बनकर उनके ससुराल जाती रहीं और रखैल का जीवन जीती रहीं। इन शूद्रों से व्यक्तिगत सम्पति का अधिकार भी छीन लिया गया। इन्हें सदियों तक गुलामों की जिन्दगी जीनी पड़ी। गांवों में हाल-हाल तक वे बंधुआ मजदूरों की जिंदगी जीते रहे हैं। खोजने पर छिटपुट उदाहरण आज भी मिल जाएंगे। जीविका का कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वे दुख-अपमान सहकर भी मालिकों की सेवा में लगे रहे।
लोहार आदि ऐसी सैकड़ों कामगार जातियां हैं, जिनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। यह सच है कि दलित अछूत समझे जाते थे और सवर्ण समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता था। सदियों तक वे अपमान और वर्ण-व्यवस्था जनित अमानवीय शोषण और यातनाओं के शिकार हुए। पर पिछड़े समाज के लोग सवर्ण समाज के सीधे सम्पर्क में रहे। उनके दास-दासी और मजदूर बनकर दलितों से भी अधिक सामंती जुल्म सहे। बेकारियां कीं, परिवार सहित दिन-रात उनकी सेवा की, बदले में तिरस्कार, अपमान और पशुवत् व्यवहार के शिकार हुए। वस्तु की तरह उनका क्रय-विक्रय होता रहा। दहेज के रूप में इनकी बहू-बेटियां मालिकों की बेटियों की दासी बनकर उनके ससुराल जाती रहीं और रखैल का जीवन जीती रहीं। इन शूद्रों से व्यक्तिगत सम्पति का अधिकार भी छीन लिया गया। इन्हें सदियों तक गुलामों की जिन्दगी जीनी पड़ी। गांवों में हाल-हाल तक वे बंधुआ मजदूरों की जिंदगी जीते रहे हैं। खोजने पर छिटपुट उदाहरण आज भी मिल जाएंगे। जीविका का कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वे दुख-अपमान सहकर भी मालिकों की सेवा में लगे रहे।
चूंकि इनके सामाजिक और आर्थिक सरोकार सीधे तौर से सामंती जातियों से जुड़ते थे, अत: उनकी शद्धता और श्रेष्ठता एवं अपनी जीविका की रक्षा के लिए उन्हें भी दिखावे के तौर पर दलितों के साथ अछूतपन का ही व्यवहार रखना पड़ा। यह ब्राह्मणवाद की श्रेणीगत असमानता थी, जो ऊपर से नीचे तक हर जाति में व्याप्त थी। किन्तु पिछड़ी जातियों के मन में दलितों के प्रति सहानुभूति और उदारता बनी रहीं। दलितों की तो बस्तियां अलग थीं, अत: फुर्सत के समय उन्हें अपने समाज के साथ दुख मनाने और क्षोभ व्यक्त करने का भी अवसर और अवकाश था। पर शूद्र या ओबीसी कामगार जातियों के पास तो वह भी सहूलियत नहीं थी, क्योंकि उन्हें सवर्ण समाज के बीच ही घर बसाकर रहना पड़ता था। इसलिए वे मार खाकर भी रो नहीं सकते थे। यशपाल जी की एक कहानी है-‘दुख का अधिकार’, जिसमें तरबुज बेचनेवाली एक औरत बाजार में बैठी तरबुज भी बेच रही है और रो भी रही है। कल ही सांप काटने से उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। वह तरबुज काटने खेत में गया था। वहीं एक विषैला सांप तरबुज के लतर में छिपा था। घर में दो-चार दिन बैठकर उसे बेटे की मौत का गम मनाने की भी फूर्सत नहीं है। पेट की मार उसे बाजार तक ले आई है। रह-रहकर उसके आंसू फूट पड़ते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में भी उनकी लगभग यही स्थिति रही। स्त्रियों की भी स्थिति लगभग यही थी, पर उसका स्वरूप अलग था। इसलिए मक्खली गोशाल, कबीर से लेकर महात्मा फुले तक-जो आंदोलन चले, उनमें दलित-पिछड़ों को लेकर वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध हर काल में कॉमन रहा। पर कालक्रम से उनमें मुस्लिम अल्पसंख्यक और स्त्रियों की समस्या और स्थिति भी जुड़ती चली गई। कबीर ने जाति और वर्ण-व्यवस्था के साथ-साथ हिन्दू-मुस्लिम सवालों और संकीर्णता को उठाया। जाहिर है, बुद्ध के समय मुसलमान नहीं थे। पर फुले तक आते-आते इसमें स्त्रियों के सवाल भी शामिल हो गए। राजाराम मोहन राय ने सती-प्रथा के खिलाफ आंदोलन अवश्य छेड़ा, पर स्त्रियों की अन्य समस्याओं की ओर उनका ध्यान नहीं गया। फु ले ने पहली बार स्त्री को भी दलित कहा और स्त्री-शिक्षा, बाल-विवाह, विधवा-जीवन, कन्या भू्रण-हत्या आदि सवालों को उठाया और उसके लिए आंदोलन चलाए। फुले ने शूद्रातिशूद्र आंदोलन चलाकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ सीधे विद्रोह कर दिया। गांधी के दलितोद्धार केवल छुआछूत तक सीमित थे पर डॉ. आम्बेडकर ने तो तमाम आंदोलनों का निचोड़ रख दिया। बाबासाहेब के आंदोलन में दलित, ओबीसी, मुस्लिम और स्त्री की तमाम समस्याएं शिद्दत से आई हैं। किन्तु 1932 में ‘पूना-पैक्ट’से जब दलितों को आरक्षण मिल गया, तो पिछड़े वर्गों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई और इस वर्ग के नेता, लेखक और बुद्धिजीवी संघ-संगठन बनाकर अपने हक की मांग करने लगे। वे बाबासाहेब के आंदोलन के पूरक बने, समानांतर नहीं। परिणामस्वरूप बाबासाहेब ने संविधान में ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’नामक अध्याय धारा, 340 जोड़ा।
पिछड़े वर्ग के तत्कालीन समाजसेवी, नेता और लेखक
आरम्भ में आर्यसमाजी जोश में पिछड़ों में जो जातीय संगठन बने, उनमें ‘कृण्वन्तु विश्वमार्यं’के आधार पर जनेऊ धारण करने एवं अपने आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण या क्षत्रियों के वंशज कहलाने की होड़ मची। पर जब सवर्णों ने ऐसे प्रयासों का विरोध किया, तो पिछड़ों का आंदोलन ‘त्रिवेणी संघ’के रूप में और फिर ‘पिछड़ा वर्ग संघ, ‘अर्जक समाज’आदि आंदोलनों के रूप में आधुनिक विकल्प बनकर आगे बढ़ा। इनके नेता और  समाजसेवियों में प्रमुख नाम हैं : बिहार से ‘त्रिवेणी संघ’के संस्थापक बाबू दासू सिंह, नवदीप चन्द्र घोष, गुरुसहाय लाल, गणपति मंडल, आरएल चंदापुरी, चुल्हाई साहू, संत प्रसाद गुप्त, जगदेव प्रसाद, राम लखन सिंह यादव, देवशरण सिंह, राम अवधेेश सिंह आदि। उत्तर प्रदेश से डॉ. बदलू राम ‘रसिक’, रामस्वरूप वर्मा, चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु, द्वारका प्रसाद मौर्य, दुर्गादत्त सिंह कुशन, शिवदयाल सिंह चौरसिया, दुर्गादीन साहू, छेदी लाल साथी, बाबूलाल प्रजापति, कुंवर उदय वीर सिंह आदि। दिल्ली से रामप्रसाद सैनी, प्यारे लाल सोनकर, पृथ्वीपाल सिंह, ज्ञानेन्द्र नाथ, भैरव प्रसाद चन्द्र, रामप्रसाद धनगर, सरदार मोहन सिंह, भगवान दास सेठ, बिहारी लाल, जीडी चौरसिया, जीपी यादव, बदन सिंह पाल आदि। मध्य प्रदेश से डॉ. इन्द्रजीत सिंह, खूबचंद पटेल, चिंतामणि साह, गोखुल प्रसाद सैनी, कन्हैया लाल जी आदि। पंजाब से डॉ. हजारी लाल, संतराम बीए, अमीर सिंह, चौधरी चानन सिंह, सीताराम सैनी आदि। पश्चिम बंगाल से आशुतोष दास, एसके सरकार, उपेन्द्र नाथ बर्मन, गौरसुंदर नाथ, खलीलुर्रहमान अंसारी, विवेकानंद विश्वास आदि। ओडिशा से यदुमण मंगराज, डॉ. पी पारीजा, लक्ष्मी नारायण साहू आदि। राजस्थान से महंथ लक्षानंद, घीसाराम जाट, कालू राम राठौर, स्वामी परमानंद जी भारती, संतोष सिंह कछवाहा, छोटेलाल सुखाजी, राम स्वरूपचंद लाल आदि। मुम्बई से केएस डोंडकर, डब्लू सिंह वाग, जीसी बोबाड़े, केपी साह, एसआर लोण्ढे, आरबी राउत, डीआर गाढ आदि, आंध्र प्रदेश से जी. लच्छना, डॉ. एन चेन्ना रेड्डी, जीआर वर्मा, के कामराजू, ए हुसैनप्पा, टीएन विश्वनाथ रेड्डी। मैसूर कर्नाटक से बी गोपाल रेड्डी, एनसी देशप्पा, पी मरियप्पा, केजी देशप्पा, केपी बोडियर, एम बीरप्पा, एनबी कृनप्पा आदि। मद्रास तमिलनाडु से वीएम घटिकाचलम, एनई मनोरम, एस रामानाथन, एमए नायर आदि। केरल में क्रिश्चियन पिछड़ा वर्ग संगठन से पीएम अब्राहम, पी नीलकंठ, बीडी जॉन, ईपी वर्गीज आदि। असम से जीतेन्द्र नाथ चौधरी, हीरालाल गुप्ता, गौरमोहन दास, चारू बर्मन, सोनाराम फूकम, गिरधारी दास, ज्ञान मोहन दास, एमएन सैकिया, नीलाम्बर दास आदि।
समाजसेवियों में प्रमुख नाम हैं : बिहार से ‘त्रिवेणी संघ’के संस्थापक बाबू दासू सिंह, नवदीप चन्द्र घोष, गुरुसहाय लाल, गणपति मंडल, आरएल चंदापुरी, चुल्हाई साहू, संत प्रसाद गुप्त, जगदेव प्रसाद, राम लखन सिंह यादव, देवशरण सिंह, राम अवधेेश सिंह आदि। उत्तर प्रदेश से डॉ. बदलू राम ‘रसिक’, रामस्वरूप वर्मा, चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु, द्वारका प्रसाद मौर्य, दुर्गादत्त सिंह कुशन, शिवदयाल सिंह चौरसिया, दुर्गादीन साहू, छेदी लाल साथी, बाबूलाल प्रजापति, कुंवर उदय वीर सिंह आदि। दिल्ली से रामप्रसाद सैनी, प्यारे लाल सोनकर, पृथ्वीपाल सिंह, ज्ञानेन्द्र नाथ, भैरव प्रसाद चन्द्र, रामप्रसाद धनगर, सरदार मोहन सिंह, भगवान दास सेठ, बिहारी लाल, जीडी चौरसिया, जीपी यादव, बदन सिंह पाल आदि। मध्य प्रदेश से डॉ. इन्द्रजीत सिंह, खूबचंद पटेल, चिंतामणि साह, गोखुल प्रसाद सैनी, कन्हैया लाल जी आदि। पंजाब से डॉ. हजारी लाल, संतराम बीए, अमीर सिंह, चौधरी चानन सिंह, सीताराम सैनी आदि। पश्चिम बंगाल से आशुतोष दास, एसके सरकार, उपेन्द्र नाथ बर्मन, गौरसुंदर नाथ, खलीलुर्रहमान अंसारी, विवेकानंद विश्वास आदि। ओडिशा से यदुमण मंगराज, डॉ. पी पारीजा, लक्ष्मी नारायण साहू आदि। राजस्थान से महंथ लक्षानंद, घीसाराम जाट, कालू राम राठौर, स्वामी परमानंद जी भारती, संतोष सिंह कछवाहा, छोटेलाल सुखाजी, राम स्वरूपचंद लाल आदि। मुम्बई से केएस डोंडकर, डब्लू सिंह वाग, जीसी बोबाड़े, केपी साह, एसआर लोण्ढे, आरबी राउत, डीआर गाढ आदि, आंध्र प्रदेश से जी. लच्छना, डॉ. एन चेन्ना रेड्डी, जीआर वर्मा, के कामराजू, ए हुसैनप्पा, टीएन विश्वनाथ रेड्डी। मैसूर कर्नाटक से बी गोपाल रेड्डी, एनसी देशप्पा, पी मरियप्पा, केजी देशप्पा, केपी बोडियर, एम बीरप्पा, एनबी कृनप्पा आदि। मद्रास तमिलनाडु से वीएम घटिकाचलम, एनई मनोरम, एस रामानाथन, एमए नायर आदि। केरल में क्रिश्चियन पिछड़ा वर्ग संगठन से पीएम अब्राहम, पी नीलकंठ, बीडी जॉन, ईपी वर्गीज आदि। असम से जीतेन्द्र नाथ चौधरी, हीरालाल गुप्ता, गौरमोहन दास, चारू बर्मन, सोनाराम फूकम, गिरधारी दास, ज्ञान मोहन दास, एमएन सैकिया, नीलाम्बर दास आदि।
आजादी की लड़ाई के दौरान शुरू हुए इन आंदोलनों के कारण ही पिछड़ों में राजनीतिक चेतना आई और समाजवादी आंदोलनों के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों में पिछड़ों का नेतृत्व और शासन हो गया। आजाद भारत में यह चेतना सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर में आई। फिर कांशीराम ने इसे धार दी। लालू यादव ने सम्पूर्णता के साथ दलित-पिछड़े और अल्पसंख्यक एजेंडे को राजनीति में शामिल किया और सफल हुए। बिहार में कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, यूपी में चौधरी चरण सिंह, कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, मायावती, हरियाणा में देवीलाल, तमिलनाडु में करुणानिधि, कर्नाटक में देवेगौड़ा आदि इसी चेतना के प्रतीक और उपज हैं। आज की राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र भी पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि और प्रतीकों पर टिका है। इसी चेतना को भुनाने के लिए भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी आज नरेन्द्र मोदी के रूप में पिछड़ा चेहरा आगे करना पड़ा है। किन्तु चाहे पिछड़ी राजनीति हो या दलित राजनीति आज फुले और बाबासाहेब के मार्ग से भटकती हुई दिखाई दे रही है, जिसका लाभ मनुवादी ताकतों को मिल रहा है।
ओबीसी साहित्य का स्वरूप और संभावनाएं
ओबीसी साहित्य पर काम नहीं हुए हैं। अन्यथा वैश्य समाज सहित पिछड़े वर्ग के जो हिन्दी कवि, साहित्यकार थे या हैं, उनमें दलित-पिछड़ी चेतना के अनुरूप संवेदना, कथ्य, पात्र और परिस्थितियों का चित्रण अवश्य मिलता है। आजादी के पूर्व फुले, पेरियार, नारायण गुरु, भारतेन्दु, संतराम बीए, रामस्वरूप वर्मा, चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु आदि सक्रिय रूप से इन्हीें दलित-पिछड़ी चेतना के अनुरूप लिख रहे थे। इनमें से कुछ लोग आजादी के बाद भी सक्रिय रहे। भारतेन्दु की चेतना में ‘वैदिक हिंसा’पर व्यंग्य, ‘भारत दुर्दशा’में ब्राह्मण-श्रमण विवाद पर प्रहार आदि ऐसे अनेक स्थल हैं, जहां से ओबीसी विमर्श की खोज की जा सकती है। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद भले ही ब्राह्मणवादी चेतना के साहित्यकार हों, किन्तु उनका अंतिम चिंतन ‘कंकाल’उपन्यास में आया है, जहां उन्होंने धर्म के पाखंड और संस्कृति की धज्जियां उड़ाई हैं। भिखारी ठाकुर के भोजपुरी नाटकों में ओबीसी साहित्य की आत्मा बसती है। उनके नाटकों के प्राय: सभी नायक-नायिका और पात्र इसी पिछड़े वर्ग के हैं। वातावरण और परिस्थिति भी पिछड़े समाज के ही हैं। रेणु की रचनाओं की बनावट-बुनावट तो वैसी है ही, उनकी संवेदना और कथ्य भी पिछड़े समाज के हैं। चाहे संवदिया, ठेस, तीसरी कसम, लालपान की बेगम, पंचलाइट, रसप्रिया, रसूल मिसतिरी जैसी कहानियां हों या ‘मैला आंचल’, ‘परती परिकथा’जैसे उपन्यास-सभी के नायक और परिवेश यही पिछड़ा और उनका पिछड़ा समाज है। उसी प्रकार संजीव के उपन्यास और कहानियों में नाई, कहार, लोहार, कुम्हार नायकों को देखा जा सकता है। चन्द्रकिशोर जायसवाल, रामधारी सिंह दिवाकर, सुरेन्द्र स्निग्ध, दिनेश कुशवाहा आदि की रचनाएं भी ऐसे ही कथ्य, शिल्प, पात्र और पिछड़े जीवन की संवेदनाओं से भरी पड़ी हैं। ऐसी रचनाएं और लिखी जा रही हैं। यह प्रवृत्ति और बढ़ेगी।
ओबीसी साहित्य के सिद्धांत और सीमाएं
आज के वैज्ञानिक जीवन का जैविक सच यह है कि मानवेतर प्राणि और वनस्पतियों में क्रॉस ब्लीड से उत्तम नस्लें तैयार की जाती हैं। यही सच मानव प्राणी का भी है। किन्तु वर्ण और जाति-व्यवस्था द्वारा बड़ी होशियारी से इसे दलित और पिछड़ों के हक में निषेध कर दिया गया। विवाह को जाति और वर्णों में तो सीमित कर दिया गया, पर शूद्रों के लिए सगोत्राीय और द्विजवर्णी जातियों के लिए विगोत्रीय विवाह की व्यवस्था की  गई, जिससे द्विजवर्णी जातियों में नस्ल सुधार तो हुए पर दलित और पिछड़ों में ऐसा नहीं हुआ। स्मरण रहे यह प्रथा भारतीय समाज में आजतक प्रचलित है। उसकी देखा-देखी मुस्लिम समाज में भी यह प्रथा समा गई और तो और कायस्थों में भी शूद्रों की तरह शादियां सगोत्रीय ही होती हैं क्योंकि कायस्थ भी शास्त्र से शूद्र ही हैं। उनमें भी नस्ल सुधार की वही समस्या है, जो शूद्रों में है। इसलिए जाति-प्रथा के उन्मूलन और नस्ल सुधार के लिए फुले, बाबासाहेब आम्बेडकर, पेरियार, डॉ. राममनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर आदि सभी ने ‘अन्तर्जातीय विवाह’पर बल दिया था। तो क्या अस्मिता विमर्श से अंतर्जातीय शादियां रुक जाएंगी और समाज सीमित हो जाएगा ? ऐसा बिलकुल भी नहीं है।
गई, जिससे द्विजवर्णी जातियों में नस्ल सुधार तो हुए पर दलित और पिछड़ों में ऐसा नहीं हुआ। स्मरण रहे यह प्रथा भारतीय समाज में आजतक प्रचलित है। उसकी देखा-देखी मुस्लिम समाज में भी यह प्रथा समा गई और तो और कायस्थों में भी शूद्रों की तरह शादियां सगोत्रीय ही होती हैं क्योंकि कायस्थ भी शास्त्र से शूद्र ही हैं। उनमें भी नस्ल सुधार की वही समस्या है, जो शूद्रों में है। इसलिए जाति-प्रथा के उन्मूलन और नस्ल सुधार के लिए फुले, बाबासाहेब आम्बेडकर, पेरियार, डॉ. राममनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर आदि सभी ने ‘अन्तर्जातीय विवाह’पर बल दिया था। तो क्या अस्मिता विमर्श से अंतर्जातीय शादियां रुक जाएंगी और समाज सीमित हो जाएगा ? ऐसा बिलकुल भी नहीं है।
यह कटु सत्य है कि अंतर्जातीय शादियां पहले उसी समाज से शुरू हुईं, जिस समाज या उसके सुधारवादी नेताओं ने इसका विरोध किया था। तमाम विरोधों के बावजूद गांधी के पुत्र देवदास गांधी ने ब्राह्मण लड़की से शादी की। इन्दिरा जी सहित तमाम अंतर्जातीय विवाह उच्च वर्ग के ऊंची नस्ल और जातियों में हुई। आज भी मुस्लिम समाज के शेख-सैयद-पठानों की शादियां यदि ब्राह्मण समाज में होती हैं, तो इसमें जाति नहीं नस्लगत समानता पाई जाती है। अधिकांश मुस्लिम नेताओं की शादियां ऐसी ही हैं। कुछ अपवाद सम्पन्न दलित या पिछड़ों में देखे जा सकते हैं। पर यह सामान्य प्रवृत्ति नहीं है। फिर अंतर्जातीय विवाह से जातियां टूटती कहां है ? जातियां पितृसमाज में पिता की और मातृसमाज में माता की जातियों के रूप में बदल जाती हैं। इसलिए ऐसे विमर्शों से कोई फर्क पडऩेवाला नहीं है, उल्टे उनकी सम्मानजनक स्थिति देखकर दूसरे समाज के लोग प्रभावित होंगे और शादियां होती हैं, तो इसमें मनाही कहां है ?
ओबीसी साहित्य के संबंध में दूसरी आशंका यह जताई जा सकती है कि यह वर्ग विमर्श से अलग जाति विमर्श में बंट जाएगा। ऐसी आशंका ‘साहित्य में आरक्षण’ वाले प्रसंग पर नामवर सिंह सहित कई विद्वानों ने जताई थी। इस प्रसंग में जब मैंने नामवर जी से पूछा, तो उन्होंने प्रतिप्रश्न किया था-‘तो क्या जितनी जातियां हैं, उतने साहित्य हों ? साहित्य खंड-खंड हो जाएगा।’प्रथम दृष्टि में यह आशंका जायज लगती है पर साहित्य अखंड कब रहा है ? इसकी अखंडता का आभास तभी तक होता रहा, जब तक इस पर किसी खास जाति या वर्ग का आधिपत्य रहा। अन्यथा यह हर काल में बंटता रहा है। आज भी अघोषित रूप से इसके जातिगत खेमे बने हुए हैं, चाहे वह मुख्यधारा का अभिजन साहित्य हो, चाहे अस्मिता विमर्श वाला बहुजन साहित्य। महत्व भले ही प्रतिभा का हो, पर धीरे-धीरे उसमें जातियां घुस आती हैं। भारत में चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, दर्शन हो, समाज हो, राजनीति हो-हर क्षेत्र में जातियां घुसी हुई हैं। ओबीसी साहित्य की सैद्धांतिकी में भी मनुवादी प्रवृत्तियों का विरोध और पिछड़े समाज के मान-सम्मान, अस्मिता, अस्तित्व और मानवीय गरिमा की स्थापना ही है। इनकी चिंता में हाशिए की तमाम धाराएं और नया सांस्कृतिक विमर्श है। इसकी विचारधारा में लोहिया, गांधी, आम्बेडकर आदि सभी हैं। अपने ऐतिहासिक प्रतीकों और दबे हुए इतिहास की खोज भी इसकी चिंता में है। इसलिए ओबीसी विमर्श की धार तेज होगी।
(फारवर्ड प्रेस, बहुजन साहित्य वार्षिक, मई, 2014 अंक में प्रकाशित )
(बहुजन साहित्य से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें ‘फॉरवर्ड प्रेस बुक्स’ की किताब ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ (हिंदी संस्करण) अमेजन से घर बैठे मंगवाएं . http://www.amazon.in/dp/