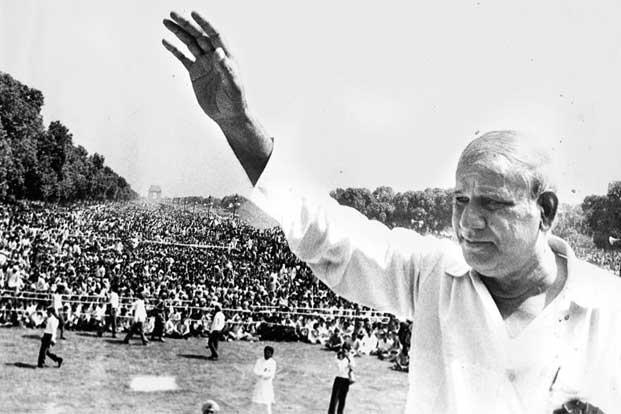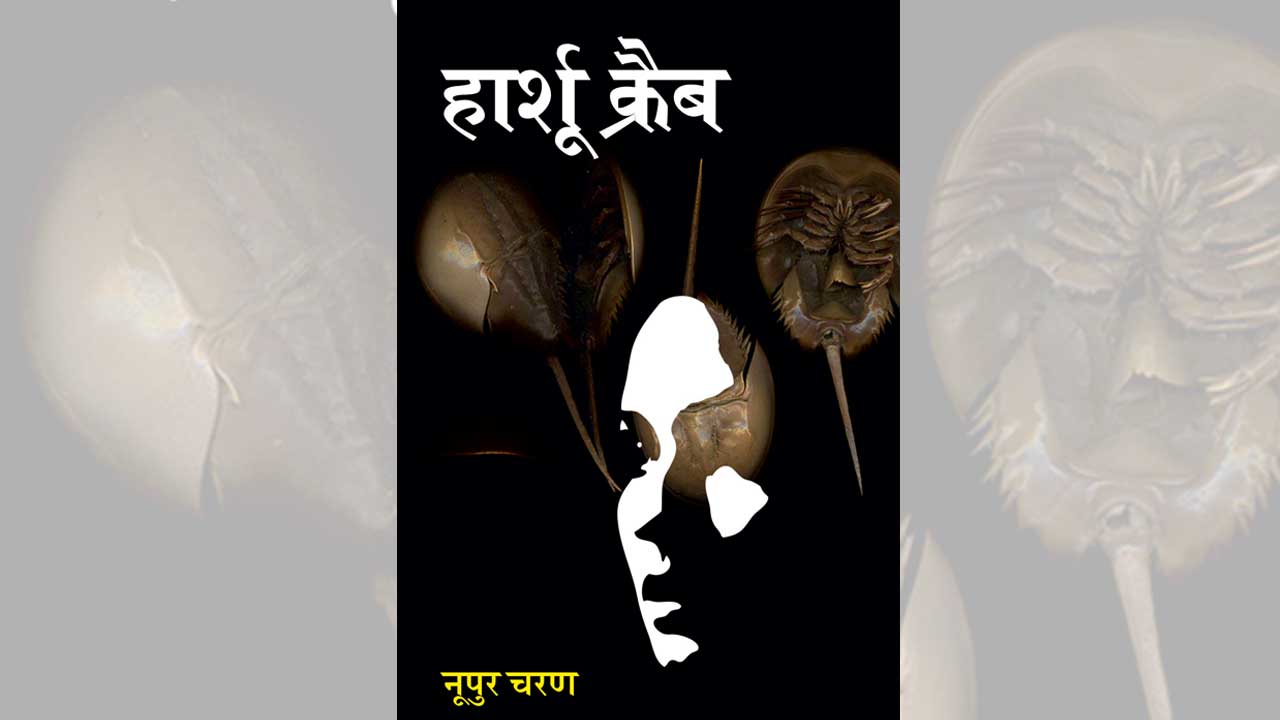दलित संगठनों और व्यक्तिगत रूप से निकलने वाली कोई दो दर्जन पत्र-पत्रिकाएं मुझे डाक से लगभग हर महीने मिलती हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा सीधे रद्दी में जाती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं, जिन्हें मैं खोलकर देखना भी पसंद नहीं करता और रद्दी में डाल देता हूं। कुछ को खोलकर देखता हूं, तो बकवास लगती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों निकल रही हैं, क्यों वे लोग अपना धन और समय इस बकवास के काम पर खर्च कर रहे हैं? इनमें कुछ पत्र-पत्रिकाएं 25-30 सालों से, और कुछ तो 50 से भी ज्यादा सालों से निकल रही हैं। पर, उनके संपादक सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के सिवा आज तक कोई झण्डा नहीं गाड़ सके।
इसके सिवा, कुछ अच्छी पत्रिकाएं भी निकलीं, जिन्होंने पत्रकारिता में अपना कीर्तिमान बनाया। उनका इंतजार रहता था। जैसे ही वे आतीं, एक नया कुतूहल जगाती थीं, लेकिन उनकी आयु ज्यादा नहीं रही। वे साल-डेढ़ साल तक निकलने के बाद बंद हो गईं। पर अपनी अल्पायु में भी उन्होंने विचार और विमर्श के क्षेत्र में जो काम किया, उसका नशा आज भी उनके पाठक वर्ग पर है। उनका जब भी जिक्र चलता है, तो हरेक के मुंह से यही निकलता है कि काश वे बंद न हुई होतीं।
जब फारवर्ड प्रेस निकलनी शुरु हुई, तो पहले अंक से ही उसने अपना विशिष्ट प्रभाव डाला। एक अच्छी वैचारिक खुराक के रूप में उसने मेरे दिमाग में जबरदस्त दस्तक दी। इसने ‘अश्वघोष’ और ‘माझी जनता’ के बंद होने के दुख को बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कम किया। फारवर्ड प्रेस की बहुजन अवधारणा उसकी मुख्य चेतना है। राजनीति में बहुजन की अवधारणा के जनक कांशीराम थे। पर इसकी वैचारिक और साहित्यिक अवधारणा के जनक साठ और सत्तर के दशकों में चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, जिन्होंने बहुजन विचार माला के अन्तर्गत दलितों और पिछड़े वर्गों के नायकों तथा उनकी विचारधारा को हिन्दी जगत में प्रतिष्ठित किया था। वह बोधानंद जी के नौरत्नों में थे, जिनमें उनके अतिरिक्त स्वामी अछूतानन्द (चमार), रायसाहब रामसहाय (पासी), रायसाहब रामचरण (मल्लाह), शिवदयाल सिंह चैरसिया (बरई तमोली), महादेव प्रसाद (धानुक), बदलूराम रसिक (तेली) और गौरी शंकर पाल (गड़रिया) थे। ये सभी उस समय के सुप्रसिद्ध लोग थे। उनका बहुजन चेतना का नवजागरण आंदोलन अस्सी के दशक तक चला। इसी आन्दोलन ने ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, मंगलदेव विशारद, और डा. अंगने लाल जैसे बहुजन विचारकों को पैदा किया। बाद के वर्षों में यह अवधारणा संकीर्ण चेतना की शिकार हो गई, और यह दलितों और डा. आंबेडकर के इर्द-गिर्द सिमटती चली गई।
दो दशक बाद फारवर्ड प्रेस ने बहुजन अवधारणा को साहित्य और राजनीति दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। अपने पहले ही अंक में वह यह दस्तक देने में सफल रहा। इसने न केवल विचार के स्तर पर बहुजन अवधारणा पर व्यापक बहस चलाई, जिसने काफी हद तक विमर्श को बदला बल्कि देश भर के प्रतिष्ठित बहुजन साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों को भी, उनके साक्षात्कार के माध्यम से, जोड़ा। यह कहा जा सकता है कि इसने अपने तईं एक नई राजनीतिक भूमिका भी तय की है, जिसने जाति के घटाटोप में विचारोत्तेजक सवाल उभारे हैं। हालांकि उन सवालों से सहमत नहीं भी हुआ जा सकता है, पर यथास्थितिवाद के विरुद्ध, वे सोचने को विवश तो करते ही हैं।
फारवर्ड प्रेस की दूसरी सबसे बड़ी वैचारिक भूमिका मिथकों के पुनर्पाठ की है। उसमें प्रकाशित महिषासुर की कथा के बहुजन-पाठ ने, देश भर के बहुजनों में ही हलचल नहीं पैदा की, वरन् उसकी आवाज, ब्राह्मणवादी हिन्दू संस्कृति के रक्षकों के कानों में भी गूंजी। वह गूंज संसद तक पहुंची, और उससे ब्राह्मणवादी सत्ताधारी वर्ग तिलमिला गया। हिंदू धर्म के सारे तीज-त्यौहार अनार्य जातियों के नरसंहार के लोकोत्सव हैं, जो बहुजनों को अपमानित करने वाले हैं। अत: इसमें संदेह नहीं कि फारवर्ड प्रेस की इस क्रांतिकारी पहल ने बहुजन समाज के उस इतिहास को सामने लाने का काम किया है, जिसे ब्राह्मणों ने अपने मिथकीय उपक्रमों से दबा दिया था। यह इतिहास गौरवशाली था और एक पृथक समतावादी धर्म-दर्शन पर आधारित था। आज उसे पूरी संजीदगी से सामने लाने की जरूरत है।
फारवर्ड प्रेस बंद होने जा रहा है, यह खबर उसके लाखों पाठकों के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी टीम के लिए भी दुख का विषय है। हालांकि उसकी क्षणिक चमक एक बड़ा उजाला तो दे ही गई है, पर उसने यह भी साफ कर दिया है कि यथास्थितिवादी शक्तियों की सत्ता किस तरह क्रान्ति को कुचलती है।
(फॉरवर्ड प्रेस के अंतिम प्रिंट संस्करण, जून, 2016 में प्रकाशित)