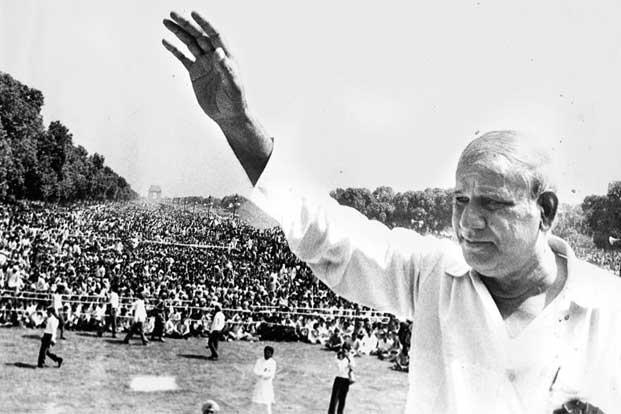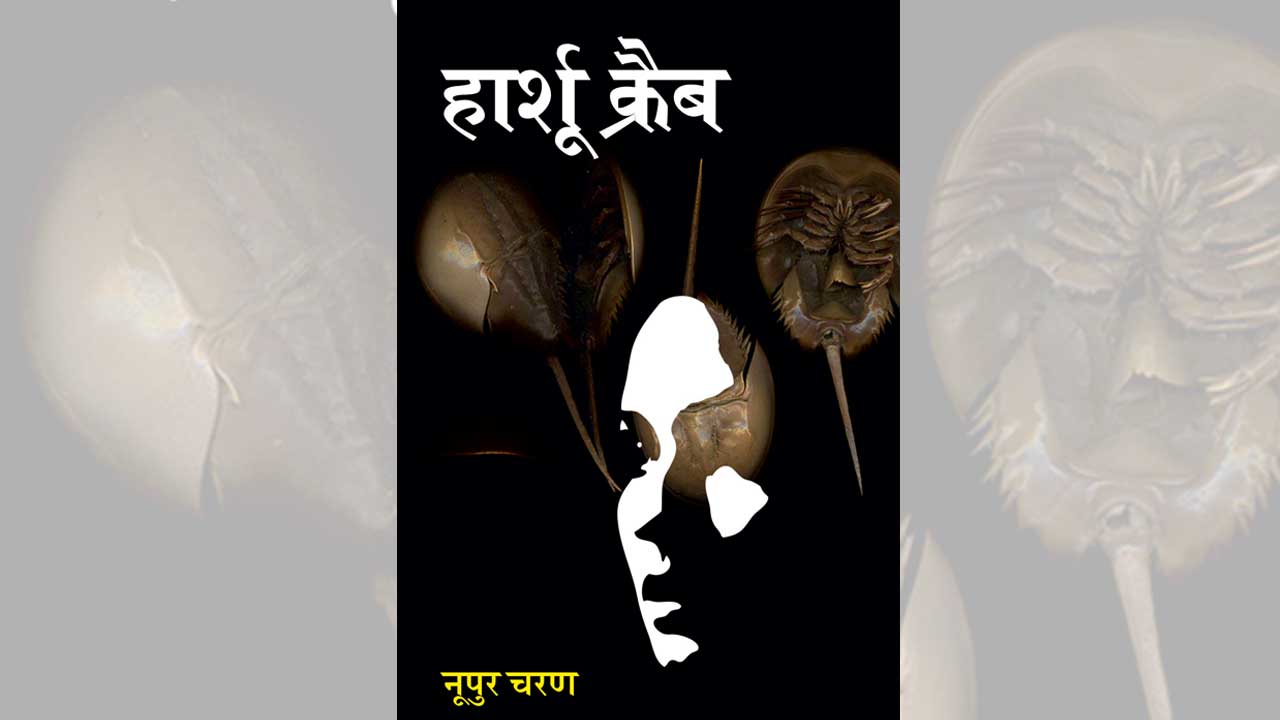जेम्स आगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में निकाला गया ‘हिक्कीज् बंगाल गजट’ भारत में पहला मुद्रित समाचारपत्र था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ‘उदन्त मार्तंड’ के साथ मानी जाती है, लेकिन इसके पहले ईसाई मिशनरियों ने ‘दिग्दर्शन’ पत्र के जरिए समाज में चेतना फैलाने का कार्य पूर्ण समर्पण से किया। सामाजिक नवजागरण में पत्र-पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्णव्यवस्था में दलित-बहुजन समाज की छटपटाहट देखने के बाद उन्हें गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने लेखन को हथियार बनाया। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि मौखिक की अपेक्षा लिखित साहित्य सामाजिक परिवर्तन के लिए कहीं अधिक आवश्यक और अनिवार्य होता है। फुले ने ‘दीनबंधु’, ‘सुधारक’, ‘दीनमित्र’ व ‘शेतकयाचा कैवारी’ में लेखन कर दलित लेखन की नीव रखी। इसी परंपरा ने समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। मैं फॉरवर्ड प्रेस को इसी कड़ी में बहुजन समाज के लिए एक सामाजिक परिवर्तनकारी पत्रिका के रूप में देखता हूं।
 मेरे लिए फॉरवर्ड प्रेस को पढ़ने के कई कारण रहे हैं। शुरुआत में मैं जब अपने घर में इसकी सदस्यता लेने के बारे में सोच रहा था तो सबसे बड़ी समस्या मेरे विद्रोही तेवर थे। मैं हिन्दू धर्म के ब्राह्मणवादी कर्मकांडों को तर्क के आधार पर काटता था। लंबे समय, (लगभग 2012) से पीएचडी के लिए घर से बाहर भी था, इसलिए मैंने घरवालों से कहा कि एक ऐसी पत्रिका है जो अंग्रेजी सीखने में उनकी मदद करेगी। मैंने जब कहा कि यह एक सामाजिक पत्रिका है तो घर-वालों को लगा कि इस तरह की पत्रिका से उनका अपना सामाजिक वजूद ही न डगमगा जाए। लेकिन मैं जब भी घर जाता फॉरवर्ड प्रेस के सारे पिछले अंक घर में रखकर आ जाता। समय के साथ परिवार में कर्मकांडों पर बहसें भी होती रहीं। पहले परिवारजनों को लगता था कि इस तरह के विचार मेरे अकेले के दिमाग की उपज हैं। इसका कारण सामाजिक बहुजन साहित्य का आभाव था। मेरी इच्छा परिवार को आधुनिक ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के दलदल से बाहर निकालने की थी और यह काम सिर्फ बहुजन साहित्य के माध्यम से हो सकता है। इस क्रम में फॉरवर्ड प्रेस का मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ा योगदान है। फॉरवर्ड प्रेस अन्य पाठकों के लिए भले ही एक पत्रिका हो लेकिन मेरे लिए सामाजिक क्रांति का दूत है। इस पत्रिका ने अनेक सामाजिक आंदोलनों को एक नई दृष्टि देने के साथ-साथ जागरूक करने का कार्य भी किया है। भारत में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों की एकता के लिए किसी पत्रिका ने सोचा भले ही होगा, कार्य करने का मन फॉरवर्ड प्रेस ने ही बनाया।
मेरे लिए फॉरवर्ड प्रेस को पढ़ने के कई कारण रहे हैं। शुरुआत में मैं जब अपने घर में इसकी सदस्यता लेने के बारे में सोच रहा था तो सबसे बड़ी समस्या मेरे विद्रोही तेवर थे। मैं हिन्दू धर्म के ब्राह्मणवादी कर्मकांडों को तर्क के आधार पर काटता था। लंबे समय, (लगभग 2012) से पीएचडी के लिए घर से बाहर भी था, इसलिए मैंने घरवालों से कहा कि एक ऐसी पत्रिका है जो अंग्रेजी सीखने में उनकी मदद करेगी। मैंने जब कहा कि यह एक सामाजिक पत्रिका है तो घर-वालों को लगा कि इस तरह की पत्रिका से उनका अपना सामाजिक वजूद ही न डगमगा जाए। लेकिन मैं जब भी घर जाता फॉरवर्ड प्रेस के सारे पिछले अंक घर में रखकर आ जाता। समय के साथ परिवार में कर्मकांडों पर बहसें भी होती रहीं। पहले परिवारजनों को लगता था कि इस तरह के विचार मेरे अकेले के दिमाग की उपज हैं। इसका कारण सामाजिक बहुजन साहित्य का आभाव था। मेरी इच्छा परिवार को आधुनिक ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के दलदल से बाहर निकालने की थी और यह काम सिर्फ बहुजन साहित्य के माध्यम से हो सकता है। इस क्रम में फॉरवर्ड प्रेस का मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ा योगदान है। फॉरवर्ड प्रेस अन्य पाठकों के लिए भले ही एक पत्रिका हो लेकिन मेरे लिए सामाजिक क्रांति का दूत है। इस पत्रिका ने अनेक सामाजिक आंदोलनों को एक नई दृष्टि देने के साथ-साथ जागरूक करने का कार्य भी किया है। भारत में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों की एकता के लिए किसी पत्रिका ने सोचा भले ही होगा, कार्य करने का मन फॉरवर्ड प्रेस ने ही बनाया।
देश के बहुजन विचारधारा के समर्थक अनेक बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने का कार्य फॉरवर्ड प्रेस ने किया। अंतर अनुशासनिक विषयों के विद्वानों ने अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित किया। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस पत्रिका का बहुत सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। चार्वाक, रैदास, कबीर के साथ भक्ति आंदोलन के नायकों और आधुनिक युग के नायक महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले से लेकर शाहूजी महाराज, व डॉ आंबेडकर के विचारों को इस पत्रिका ने स्थान दिया। समसामयिक घटनाओं को इनकी वैचारिकी से जोड़कर सटीक विश्लेषण के जरिए ओबीसी समाज में बौद्धिक चेतना जागृत करने का प्रयास भी किया। मेरी समझ विकसित करने में, मुझे डॉ आंबेडकर के वैचारिक आंदोलन से जोडऩे में इस पत्रिका का बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं फॉरवर्ड प्रेस के प्रिंट संस्करण का सदैव आभारी रहूंगा, खासकर प्रमोद रंजन और उनकी टीम से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। पत्रिका जिस रूप में है, संपादकीय टीम भी उसी स्वरुप में रही है। मैंने प्रमोद रंजन के मन में एक नई वैचारिक बहस छेडऩे की जिद देखी है। उनसे हर मुलाकात बहुजन समाज के लिए एक नए दृष्टिकोण से कार्य करने की प्रेरणा देती है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस सामाजिक आंदोलन में उनकी भूमिका रहेगी।
दरअसल, आयवन कोस्का ने एक ऐसी पत्रिका की नींव रखी है, जो कांचा आयलैया के शब्दों में कहे तो दलितीकरण है। वर्धा विवि में दलित एवं जनजाति अध्यन केंद्र के निदेशक प्रो. कारुण्यकारा, नए छात्रों एवं शोधार्थियों को फॉरवर्ड प्रेस पढ़ने की सलाह देते थे। उनका मत है कि भारत के इतिहास को देखें तो दलितीकरण के लिए, साहित्यों का अध्ययन और प्रचार महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही द्विभाषी के साथ ही सामाजिक पत्रिका होने के कारण आप सभी को उसे पढ़ते रहना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से कहते थे कि हिंदी भाषा कभी-कभी ज्ञान को संकुचित कर देती है। हिंदी उत्तर भारत में संचार और वातार्लाप की भाषा है, लेकिन मौलिक लेखन करने के लिए जिस अध्ययन की आवश्यकता होती है, उसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। हमारे विश्वाविद्यालय के शिक्षकों प्रो. कारुण्यकारा, डॉ. सुनील सुमन और डॉ. सुरजीत सिंह ने छात्रों को बहुजन आंदोलन से जुड़ने के लिए सदैव प्रेरित किया तथा शोधार्थियों को सामाजिक बौद्धिक प्रशिक्षण देने के लिए बहुजन पत्रिकाओं का इस्तेमाल किया। डॉ. सुनील सुमन शोधार्थियों को फारवर्ड प्रेस की में बरशिप लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसके लिए हम लोगों को गर्व भी होता कि किसी पत्रिका का सदस्य बनकर हम भी इसी वैचारिक आंदोलन के साक्षी बन रहे हैं। फॉरवर्ड प्रेस का विद्यार्थियों के लिए सालाना शुल्क मात्र 100 रूपए था, जिसे बड़ी आसानी से छात्र चुका सकते थे। एम.फिल के छात्र दो वर्ष और पीएचडी के छात्र 5 वर्षों के लिए सदस्यता लेते थे। लगभग सभी मित्रों ने अपने गृह जिले के मित्रों और अपने घरों में भी सदस्यता दिलाई थी। एक प्रकार से प्रिंट संस्करण ने सामाजिक क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन अल्प समय में ही हमारे बहुजन अभियान का साथ छोड़ने की खबर ने बहुजन आंदोलन को थोड़ा कमजोर किया है। इंटरनेट की सेवा हर जगह मौजूद नहीं होती है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इंटरनेट संस्करण पढ़ना मुश्किल होगा। प्रिंट संस्करण बड़ी आसानी से गाँव कस्बों में पहुंच जाता था। एक नई ऊँचाई की ओर यह पत्रिका हमें लेकर चलती, लेकिन इसका प्रिंट संस्करण बंद होना पारिवारिक बौद्धिक क्षति है, जिसकी भरपाई असंभव है। ऐसा लगता है कि परिवार का एक सदस्य अलग होकर अपना जीवन जीने जा रहा है या किसी दूसरे क्षेत्र का चुनाव अपने जीवनयापन के लिए कर रहा है और वह भी परिवार के सदस्यों से बिना पूछे!
(फॉरवर्ड प्रेस के अंतिम प्रिंट संस्करण, जून, 2016 में प्रकाशित)