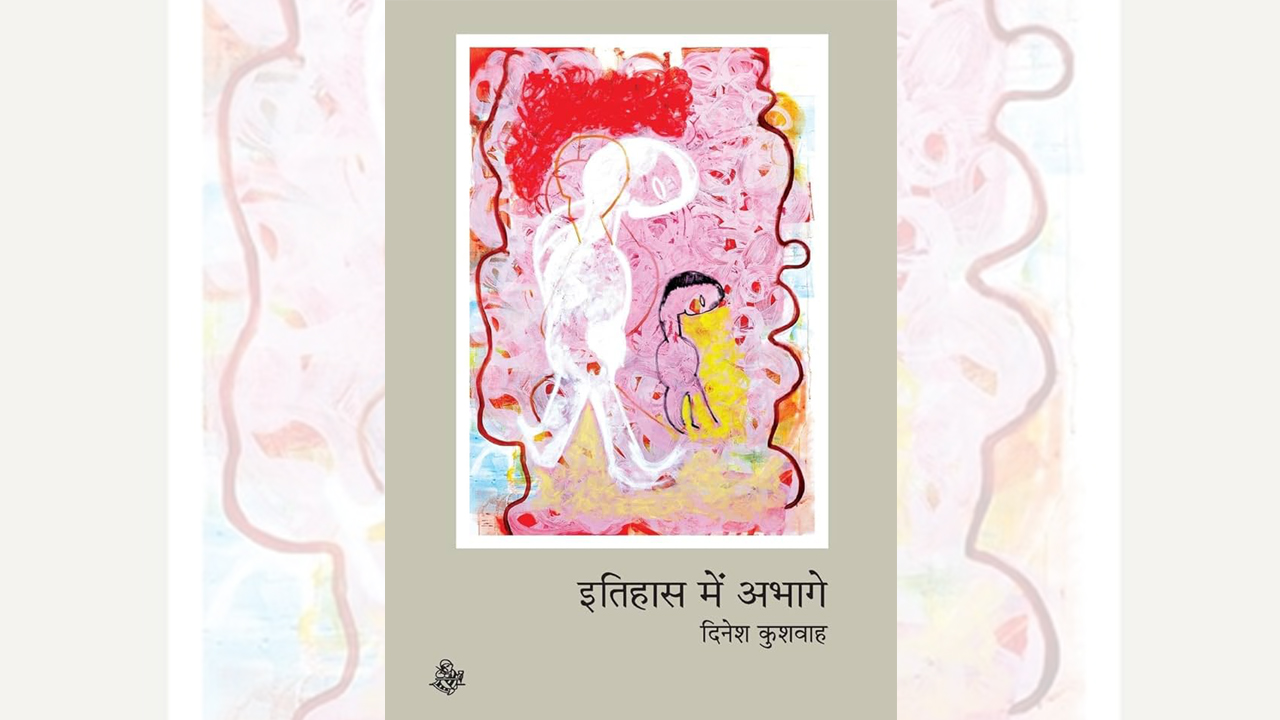बहुजन समाज को वह साहित्य तो पढ़ना ही चाहिए, जो विशेष तौर पर उसके जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उदाहरण के लिए महात्मा फुले, घासीराम, डॉ. अांबेडकर, पेरियार, नारायण स्वामी, कांशीराम, ओमप्रकाश वाल्मीकि, कँवल भारती, डॉ. धर्मवीर, तुलसीराम आदि के द्वारा लिखा साहित्य यानि बहुजन साहित्य। क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का मंथन कर ऐसे सूत्र और सिद्धांत निकाले हैं, जो उसके छद्म, दुहरेपन, कहनी और करनी का विरोध, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्विरोध, अन्यायपरस्ती, शोषणपरस्ती आदि का उद्घाटन करते हैं। प्राचीन साहित्य में भी ऐसे लेखक और कवि रहे हैं, जिन्होंने हिंदू चित्त में भरे हुए विषों को अपनी रचना का विषय बनाया है, जैसे हिंदी में कबीर, रैदास, दादू, मीरा आदि। इन्हें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम समझ सकें कि जो विद्रोह हम आज कर रहे हैं, उसकी परंपरा बहुत पुरानी है। हमें बौद्ध साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि किन तर्कों के आधार पर वैदिक धारा से असंतोष प्रगट कर एक नयी, समतावादी सांस्कृतिक धारा फूटी थी और कैसे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी के मेयार एकदम बदल दिये थे। यह सारा प्राचीन विद्रोही साहित्य बहुत ही सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। हाँ, इसका वितरण अभी तक इस तरह नहीं हो पाया है और सहित्यिक संस्कार का प्रसार इतनी शिद्दत से नहीं किया गया है कि हर बहुजन के घर में कबीर, रैदास, अांबेडकर या लोहिया की कोई न कोई किताब जरूर हो।

हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में दलित विद्रोह की धारा दलित साहित्य से ही फूटी थी। बेशक इसकी पृष्ठभूमि में महात्मा फुले और डॉ. अांबेडकर का साहित्य और कर्तृत्व था, लेकिन विचार की अपेक्षा साहित्य समाज में जल्दी फैलता है। इस लिहाज से दलित या बहुजन साहित्य की जितनी रचना अभी तक हो जानी चाहिए थी, हुई नहीं है। बहुजन समाज ज्यादातर विचारों के संघर्ष में ही लगा रहा है, जब कि इस संघर्ष को जन-जन के घर-परिवार तक पहुँचाने के लिए संवेदना अर्थात राग की रचनाओं का सामने आना जरूरी है। आज भी दलित और बहुजन साहित्यकार अपने समाज के लिए कम लिखते हैं, उस समाज में सम्मान पाने के लिए ज्यादा लिखते हैं, जिसमें उनके प्रति पूर्वाग्रह अभी भी कम नहीं हुआ है। वे चाहे तो प्रतिष्ठित साहित्यिक मंचों के लिए भी लिख सकते हैं, पर उन्हें अपनी बोली-बानी और शैली तथा मुहावरों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
शोषण और अन्याय का विरोध मनुष्य के मन में दोनों स्तरों पर फूटता है – विचार के स्तर पर भी और संवेदना के स्तर पर भी। लेकिन विचार के लिए जैसी मानसिक तैयारी या परिपक्वता चाहिए, वह युगों से पढ़ाई-लिखाई और ज्ञान के अन्य स्रोतों से वंचित रखे जाने के कारण इस वर्ग के कम लोगों में पायी जाती है, यही कारण है कि पूरी दुनिया में साधारण मनुष्य का दुख-सुख तथाकथित मुख्य धारा की बनिस्बत लोक साहित्य में ज्यादा फूटा है। लोक साहित्य वे रचनाएँ हैं जिनके लेखक का नाम नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में लोक साहित्य है, जिसे कई-कई पीढ़ियों के स्त्री-पुरुषों ने लिखा, गाया, माँजा और चमकाया है। भारत के लोक साहित्य में स्त्री की वेदना सब से सशक्त ढंग से व्यक्त हुई है। लेकिन इसके साथ ही किसानों, धोबियों, सूदखोरी के शिकार परिवारों, नीची मानी वाली जातियों की पीड़ा भी बहुत ही मार्मिक रूप से मुखरित हुई है। दुर्भाग्य की बात है कि लोक पीड़ा की यह अभिव्यक्ति धरोहर अभी भी या तो लोक स्मृति में कैद है या मोटी-मोटी किताबों में सुरक्षित है।

दलित और बहुजन समाज को यदि अपनी पीड़ा से निस्तार पाने की आकुलता होती, तो वह अपने दर्द को कलात्मक ढंग से प्रगट करने के विविधरंगी प्रयास करता। इसी में उसकी मुक्ति भी है। गालिब का मशहूर शेर है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अब हमें अपने दर्द को सिर्फ सहलाना नहीं है, उसे टोपी की तरह सिर पर प्रतिष्ठित करना है, आभूषण की तरह पहनना है। दर्द को कला रूप में सामने रख देने पर उसका परिताप आँखों के रास्ते से बह निकलता है और समाज को शुद्ध और प्रांजल करता है। इसलिए देश भर में हर महीने सैकड़ों ऐसे कार्यक्रम – गीत, संगीत, नाटक, प्रहसन आदि – होने चाहिए जो हमारे लोक साहित्य में दबी पड़ी व्यथा, पीड़ा, प्रवंचना बोध और अन्याय चेतना को बहुत ही कलात्मक ढंग से पेश करते हों। सिर्फ आरक्षण के लिए लड़ना ही बहुजन का संघर्ष नहीं है – उन परिस्थितियों को उभारना भी इस संघर्ष का हिस्सा भी जिनके परिणामस्वरूप आरक्षण जैसी सतह पर अतार्किक जान पड़ने वाली तरकीब में उच्चतम किस्म की तार्किकता दिखाई पड़ने लगे।
फिर कला का भी सवाल है। बेशक संघर्ष से भी कला का विकास होता है और फुरसत से भी। लेकिन कोई समाज हमेशा संघर्षरत नहीं रहता। फुरसत के समय वह गाता, बजाता और नाचता भी है। इसलिए हमें अपनी अभिव्यक्ति को माँजने के लिए अपने से भिन्न वर्गों और समाजों का बेहतर साहित्य भी जरूर पढ़ना चाहिए। जहाँ उचित लगे, उसमें रस लेना चाहिए, जहाँ अनुचित लगे, उसका तिरस्कार करना चाहिए और सीखना तो हर रचना से चाहिए। निश्चय ही मानव जाति में द्वंद्व हैं, पर क्या मानवता नाम की कोई साझी विरासत नहीं है?
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें :