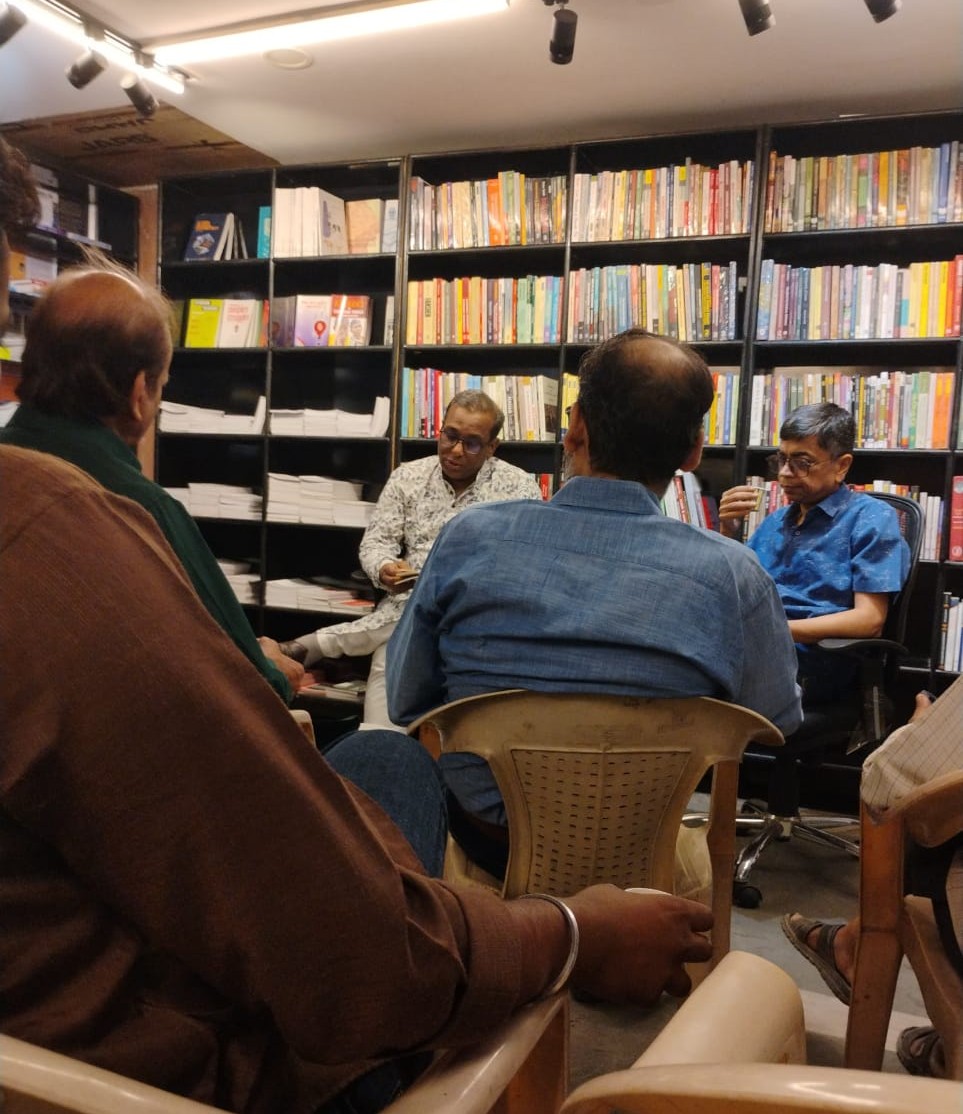लेख श्रृंखला :जाति का दंश और मुक्ति की परियोजना
एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में भारत में जाति सिर्फ अपना रूप बदल रही है। निर्जात (बिना जाति का) होने की कोई प्रकिया कहीं से चलती नहीं दिखती। आप किसी के बारे में कह सकते हैं कि वह आधुनिक है, उत्तर आधुनिक है- लेकिन यह नहीं कह सकते कि उसकी कोई जाति नहीं है! यह एक भयावह त्रासदी है। क्या हो जाति से मुक्ति की परियोजना? एक लेखक, एक समाजकर्मी कैसे करे जाति से संघर्ष? इन्हीं सवालों पर केन्द्रित हैं फॉरवर्ड प्रेस की लेख श्रृंखला “जाति का दंश और मुक्ति की परियोजना”। इसमें आज पढें कमलेश वर्मा – संपादक।
जातिवादी भेदभाव के सभी रूपों का खात्मा हो बहुजनों का लक्ष्य
मेरे ख्याल से जाति से मुक्ति का प्रश्न रोमानियत से भरा हुआ है। इस प्रश्न को प्रायः भारतीय समाज के सन्दर्भ में देखा जाता है और कहा जाता है कि विश्व में ऐसी सामाजिक प्रणाली कहीं और नहीं है। जाति जन्म-आधारित एक पहचान है। जन्म के आधार पर कोई न कोई पहचान प्रायः सभी समाजों में देखी जाती है और उस पहचान के आधार पर कुछ न कुछ भेदभाव भी देखे गये हैं। भारत की जाति-व्यवस्था से लेकर विश्व की जन्म-आधारित पहचान में क्रमशः परिवर्तन देखे गए हैं, मगर इन्हें समाप्त होते हुए नहीं देखा गया है। जाति,नस्ल और क्षेत्र के आधार पर मनुष्य की जो पहचान बनती है उसे मिटाना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है।

अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाने के बावजूद ओबामा की नस्लीय पहचान मिटायी नहीं जा सकती। जाति से मुक्ति का सवाल मेरे विचार से बेमानी है। जन्म-आधारित पहचान के कारण होनेवाले भेद-भाव के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है। मिथक और आख्यान से लेकर इतिहास तक में इस भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष दिखाई पड़ता है।
वाल्मीकि और विश्वामित्र की लड़ाई का एक पक्ष यह भी है कि ‘ब्रह्मर्षि’ के रूप में क्षत्रिय को भी मान्यता मिले(जैसे माँग उठाई जा रही है कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर ओबीसी की नियुक्ति हो)। कृष्ण और शिशुपाल के बीच हुए विवाद में यह बात भी आती है कि ‘यादव’ की अग्रपूजा भला कैसे हो सकती है। यही सवाल 1954 में प्रकाशित उपन्यास ‘मैला आँचल’ में हरगौरी सिंह उठाता है कि ‘ग्वाला होकर लीडरी?’ शिवाजी काछी जाति में पैदा होकर ‘छत्रपति’ कैसे हो सकते हैं? आख्यान,इतिहास और उपन्यास के ये प्रसंग उस भेदभाव तथा उसके खिलाफ हुए संघर्ष को दिखलाते हैं। न तो विश्वामित्र और कृष्ण जातिमुक्त हुए और न ही शिवाजी। ‘मैला आँचल’ के बालदेव और कालीचरण यादव सवर्णों की जातिवादी राजनीति का जाति-आधारित जवाब हैं। आज का कोई ‘हरगौरी सिंह’ यह कह सकने की स्थिति में नहीं है कि ‘ग्वाला होकर लीडरी?’ कई ‘यादवों’ और दूसरी पिछड़ी जातियों ने दिखा दिया कि वे ‘लीडरी’ कर ही नहीं सकते बल्कि सिखा भी सकते हैं।
सवर्णों की जातिवादी राजनीति को मंडल की राजनीति ने ध्वस्त कर दिया है, वहीं इस राजनीति पर ‘जातिवाद’ के सर्वाधिक आरोप लगे हैं। पिछड़ों के ‘जातिवाद’ से मुक्ति के लिए ‘विकास’ की राजनीति खड़ी की जाती रही है जो अवान्तर से सवर्णों के वर्चस्व की पुनर्स्थापना की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। इसी के साथ पूँजीवादी संरचना भी अपना खेल खेलती है जो ऊपर से चमक-दमक से भरी हुई कार्यकुशल तो नज़र आती है, मगर अपनी बनावट में कुछ घरानों के आधिपत्य में होती है। परिवार और घराने मूलतः जाति के आधार पर बने होते हैं। जिन क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं हुआ, वहाँ सवर्णों का व्यावहारिक आरक्षण आज भी लागू है। कुल मिलाकर यह कि धर्म ,समाज, राजनीति, व्यवसाय, नौकरी, सेना, न्यायालय, मीडिया आदि किसी भी क्षेत्र में जातिविहीन व्यवस्था को खोज पाना असंभव है। जातिवाद के खिलाफ खड़े हुए आन्दोलनों की भी परिणति यही हुई कि एक जाति का वर्चस्व टूटा और दूसरी जाति का वर्चस्व कायम हुआ। आप बुद्ध से लेकर आंबेडकर तक के क्रम को देख सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके प्रयासों का महत्त्व कम हो जाता है, मगर इनकी कोशिशों की व्याख्या करते समय सावधान रहने की जरूरत है। जातिवाद के खिलाफ हुए आन्दोलन वस्तुतः भेदभाव के खिलाफ प्रभावी रहे। इनका उपयोग वंचित वर्गों (जाति-आधारित) को साधन-संपन्न बनाने में तथा उन्हें एक राजनीतिक वर्ग के रूप में संगठित करने में हुआ।
जातिविहीन समाज के ढाँचे के बारे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई समाज बन सकता है जहाँ जन्म-आधारित कोई पहचान न हो! मनुष्य को प्रकृति ने कुछ भिन्नताएँ दी हैं, जैसे- नस्ल। वर्ण और श्रम ने भिन्नता बनाई है, जैसे- जाति। इसी तरह भूगोल ने मनुष्य को कई रंग और रूप दिये हैं। ये सभी भिन्नताएँ माता-पिता से संतान के क्रम में प्रवहमान हैं। क्या इन्हें नाम दिये बगैर हमारी भाषा चल सकती है? इन भिन्नताओं के कुछ नाम तो जरूर होंगे, आप चाहें तो संशोधित नाम रख सकते हैं। गांधीजी ने ‘अछूत’ की जगह ‘हरिजन’ का प्रयोग किया और अँग्रेज सरकार ने ‘अनुसूचित जाति’ का तो मराठी भाषा ने ‘दलित’ शब्द का। मगर, इन सभी नामों का संबंध जन्म-आधारित पहचान से है। जातिविहीन समाज कैसा हो सकता है? इसका एक रूप महानगरीय आबादी में देखा जा सकता है। टू और थ्री बी एच के में बसी यह आबादी जाति-आधारित बसावट को तोड़ती है, मगर ‘समाज’ कहला सकने की योग्यता नहीं रखती है। साथ ही यह सवाल बना रहता है कि क्या ये लोग जाति के प्रश्न से मुक्त हैं? हम पाते हैं कि यह आबादी भी अपनी-अपनी इकाई में निर्जात नहीं है। जाति-आधारित सामाजिक बसावट से ये अलग तो हो गये हैं मगर ‘संरचना’ से अलग नहीं हुए हैं। यह प्रयास केवल आवासीय रूप तक सीमित है, इससे ‘जाति’ के विभिन्न पक्षों का कोई सम्बन्ध नहीं बनता है।
राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया के माध्यम से जातिवादी शोषण को कम करने में सफलता मिली है। आरक्षण ने अब तक के सभी उपायों में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका निभायी है, क्योंकि इसने आर्थिक और शैक्षणिक प्रक्रिया को तेज गति दी है। दलित और मंडल की राजनीति ने बहुजन समाज को जातिवादी भेदभाव से लड़ने में मदद पहुँचाई है। अनेक परिवर्तनों के साथ बहुजन-विरोधी जातिवादी भाषा में भी कमी आयी है। मंडल के पहले के समाज की भाषा में खुलेआम जातिवादी गलियाँ दी जाती थीं, जिनका प्रतिकार आसान नहीं होता था। आज कानून और राजनीति के डर से ही सही, भाषा में हुए परिवर्तन को लक्षित किया जा सकता है।

दलित और मंडल राजनीति का मूलाधार है — जातिवादी शोषण से मुक्ति के संघर्ष की अटूट परंपरा। इन दोनों की सशक्त मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि समाज के इतिहास में जातिवादी भेदभाव की नींव कितनी गहरी रही है। इन दोनों में ‘जाति’ के सवाल पर कुछ अंतर हैं। दलित राजनीति अस्पृश्य जातियों को एक वर्ग के रूप में लेकर चलती है। वहाँ लम्बे समय तक यह ‘वर्ग’ महत्त्वपूर्ण बना रहा। मंडल की राजनीति की शुरुआत तो वर्ग से हुई, मगर ‘शुद्ध’ जाति-आधारित राजनीति के प्रश्नों को खुलकर सामने आने का रास्ता इसी ने बनाया। तथाकथित मुख्यधारा की राजनीति जाति के प्रश्न पर ‘हिडेन एजेंडा’ से प्रायः संचालित होती रही है। सारांश यह कि भारतीय राजनीति का कोई भी रूप जाति के सवाल से परे नहीं रहा है।
भारत की कृषि-उत्पादन-प्रणाली एक सुगठित और अविचल जाति-आधारित व्यवस्था से बँधी थी और व्यापार-प्रणाली पर भी कुछ जातियों का एकच्छत्र राज था। तब से लेकर आज तक, उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली जन्म-आधारित पहचानवाले लोगों से बँधी रही है। इसलिए यह ‘मासूम’ सवाल कि ‘जाति से मुक्ति’ कैसे हो? — आकर्षित तो जरूर करता है, मगर मूल समस्या से ध्यान हटानेवाला बन कर रह जाता है। जाति-आधारित शोषण से मुक्ति का संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है कि हम अपने समाज को ‘जाति’ के दंश से आज़ाद कर सकें। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि पूँजीवाद का जाति-विरोधी जो रूप दिखाई पड़ता है, उसके धोखे में पड़ने की जरूरत नहीं। पूँजीवाद मनुष्य को ग्राहक के रूप में देखता है, इसलिए ग्राहक बनने के रास्ते में ‘जाति’ जहाँ तक बाधक बनती है उसका विरोध वहीं तक होगा। यदि ‘जाति’ के उपयोग से पूँजी का विस्तार हो तो वह उसका उपयोग धड़ल्ले से करेगा।
असहमति की संभावनाओं के बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय मनुष्य की सबसे बड़ी सामाजिक पहचान उसकी ‘जाति’ है। ‘निर्जात’ हो जाना एक यूटोपिया है, जैसे कबीर का ‘अमर देसवा’। सुनना अच्छा तो लगता है कि काश हम केवल ‘मनुष्य’ होते! मगर, सावधान रहना चाहिए कि केवल मनुष्य होने से ज्यादा अच्छा है ‘सामाजिक-राजनीतिक मनुष्य’ होना और यह बनने में ‘जाति’ की अविचल भूमिका से भला कौन इंकार कर सकता है!
( कॉपी संपादन : सिद्धार्थ )
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें