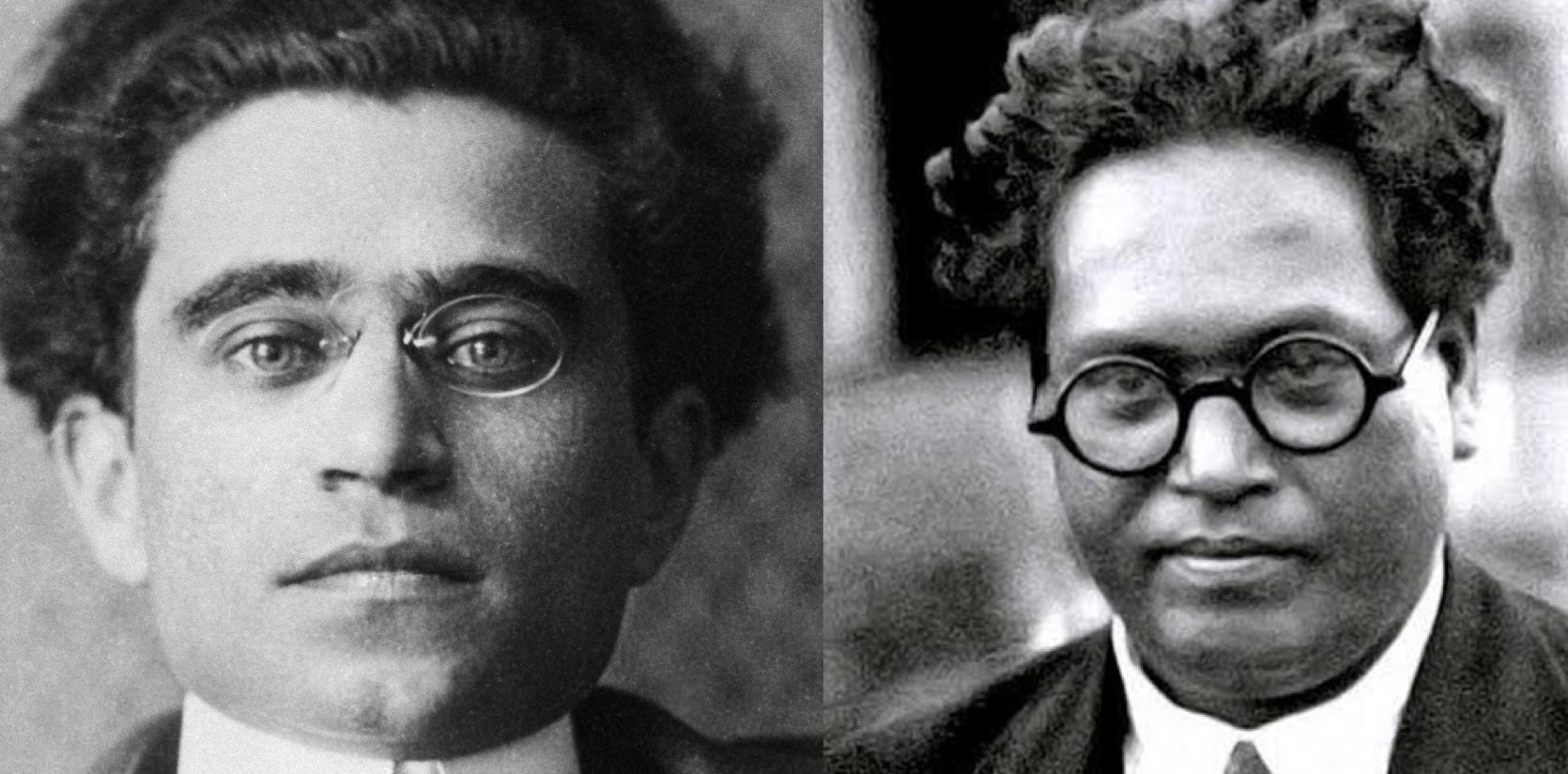विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी संघर्ष के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए मैं कुछ बातें, रिपोर्टें, कथानक और भावार्थ रखना चाहता हूं, जो यह समझने में हमारी मदद कर सकते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया के आदिवासी क्या कर रहे हैं। किस हाल में हैं? उनकी वास्तविक समस्याएं क्या हैं, जिनसे वे जूझ रहे हैं? दुनिया और समाज के दीगर लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं?
इस क्रम में सबसे पहले मैं प्रखर पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव की किताब ‘देसगांव’ (2020) में संकलित एक रिपोर्ट ‘पत्थरगड़ी : एक संवैधानिक विरासत का आँखों देखा इतिहास’ का ज़िक्र करना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ‘ऑर्गेनाइजर’ के 17 मई सन 2018 के अंक में पत्थरगड़ी को लेकर एक भ्रामक रपट छापी गई, जिसमें कहा गया कि पत्थरगड़ी, ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन है। इससे एक महीने बाद जब सरसंघचालक मोहन भागवत छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे, उसी समय यानी 21 जून, 2018 को झारखंड के खूंटी में पांच एनजीओ कर्मियों के बलात्कार की खबर सामने आई और तेजी से चारों ओर फैली। इसके साथ ही पत्थरगड़ी की भी खबर राष्ट्रीय स्तर पर छा गई। फिर तो “समूची सरकारी मशीनरी और मीडिया ने मिलकर पत्थरगड़ी को माओवादियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के साथ जोड़कर बदनाम कर दिया। पुलिस ने खूंटी के गांवों पर पत्थरगड़ी के मास्टरमाइंड की खोज में हमला किया, जिसमें एक आदिवासी मारा गया।” (देसगाँव, पृष्ठ 211-212)
अभिषेक ने अपनी रिपोर्ट में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भील आदिवासियों की ऐतिहासिक विडंबनाओं और उनके साथ हुये दीगर विश्वासघातों की ओर संकेत किया है। पत्थरगड़ी पेसा कानून की पहली व्यावहारिक और क्रांतिकारी पहलकदमी तथा अभिव्यक्ति है। यह डूंगरपुर के आदिवासियों के अधिकारों की मुनादी है। इतिहास का यह पत्थर डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा ने गाड़ा था। पत्रकार अभिषेक ने इसके निशानों को ढूंढते हुये डूंगरपुर के सुदूर देहातों तक यात्रा की, जिसमें उन्हें आदिवासियों के राजा के साथ छल व सरकार द्वारा उनके साथ छल और आदिवासियों के प्रतिरोध के अत्यंत मार्मिक विवरण मिले। शहर लौटते हुए गहरी उदासी के साथ उन्होंने इस इतिहास को याद किया “यहां के आदिवासी अपने राजा डूंगर बरंडा का ‘बलिदान दिवस’ हर 15 नवंबर को मनाते हैं। इस साल राजा को मरे 726 वर्ष पूरे हो जाएंगे। डूंगरपुर राज ‘भील प्रदेश’ को डूंगर नू घेर या डूंगर नू पाल के नाम से जाना जाता था। यहां आदिवासियों की तमाम पालों (गांवों का समूह) के गमेती (प्रधान) ने राजा डूंगर को अपना राजा नियुक्त किया था। कहते हैं कि उस समय एक बनिया व्यापार करने के लिए शालासाह-थाना गांव आया। उसकी एक खूबसूरत कन्या थी। राजा ने उसे विवाह का प्रस्ताव भेजा। बनिया मान गया, लेकिन उसने पीठ पीछे राजा को मारने का षड्यंत्र रचा।

यह साजिश डूंगर राज की राजधानी आसपुर के पास बड़ौदा के एक राजपूत सामंत के साथ मिलकर रची गई। शादी 1336 संवत की शुक्ल दशमी को तय थी। राजा बारात लेकर पहुंचा। घरातियों ने मनुहार करके बारातियों को जहरीली शराब पिला दी और राजपूतों ने अचानक हमला कर दिया। राजा ने शराब नहीं पी थी इसलिए वह बच गया, बाकी बाराती मारे गए। राजा उनसे लड़ते हुए डूंगरपुर पहुंचे। राजा की दो रानियां थीं – कालिका और धनु। वे भी राजपूतों से लड़ते हुए मारी गईं। पहाड़ की चोटी से कुछ दूर पहले राजा पर पीछे से राजपूतों ने वार किया। राजा भी वीरगति को प्राप्त हुए। राजा डूंगर जहां मारे गए, वहां आज भी उनकी याद में एक छतरी बनी हुई है और डूंगरपुर में ही दोनों रानियों धनु माता और कालिका माता के मंदिर हैं। इसके बाद राजपूतों ने अगले दिन भील प्रदेश का नामकरण मारे गए राजा के नाम पर किया और खुद उस पर राज किया। आदिवासियों के राज का कोई दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। उनका इतिहास ही मिटा दिया गया। राजा के मारे जाने के अगले दिन से डूंगरपुर की स्थापना का दिवस मनाया जाने लगा जो आज तक जारी है। अजीब बात यह है कि डूंगरपुर के स्थापना दिवस से एक दिन पहले यहां के अपने आदिवासी राजा का शहादत दिवस यहां के मूलनिवासी मनाते हैं। (वही , पृष्ठ 220) अगले दिन राजपूत उसी राजा की मौत का जश्न मनाते हैं। एक बनिए के सहारे बिना किसी पूर्व दुश्मनी के राजा के खिलाफ षड्यंत्र करके उसे मार डालने वाले ठीक अगले दिन स्थापना दिवस का जश्न मनाते हैं। वह राज्य उसी के नाम पर है, लेकिन उस पर राज करने वाले हैं राजा के हत्यारे राजपूत। कैसा लगता होगा भीलों को यह देखकर कि आज वे जिसकी शहादत की स्मृति को ताज़ा करने बैठे हैं, कल उसी की हार का उत्सव होगा? क्या वे कोई तकलीफ महसूस करते होंगे? क्या वे कभी अपनी पीड़ा का आख्यान रचेंगे?
आप याद कीजिये महिषासुर नामक एक व्यक्ति की हत्या के जश्न में डूबनेवाले उन समाजों का जो भीलों की तरह महिषासुर की शहादत नहीं दुर्गा की विजय में मस्त हैं। आप कल्पना कीजिये छल से बलि का राज्य हड़पने और उनको मारकर जमीन में गाड़ देनेवाले लोगों को पालते-पोसते बलि के वंशजों को कि वे आज क्या कर रहे हैं? धोखे और छल से बलि का सब कुछ छीन लेने वाले वामन ने बलि को एक धागा बांधा था कि अब आप अपने वचन से मुकरेंगे नहीं और इस प्रकार उनसे उनका सब ले लिया और उन्हें मार डाला। वही धागा इतिहासक्रम से चलता हुआ आज रक्षाबंधन बन चुका है। बलि के वंशज आज अपने पूर्वज को धोखे देने के लिए बांधे गए इस बंधन को अपना त्योहार बना चुके हैं। हर शुभ काम में वे नारियल फोड़ते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पुष्यमित्र शुंग पत्थर पर उनके पूर्वजों का मस्तक पटककर तोड़ता था। इतिहास की घुमावदार वीथियों में चलते हुए थककर उन्होंने अपना अपराधबोध खो दिया। उनके सामने उनके राज्य पर कोई और बैठा है और वे उसकी खुशी के गीत गा रहे हैं। आदिवासियों और मूलनिवासियों की यही त्रासदी है।
ऐसा नहीं है उनका सब कुछ छीनने की घटना एक बार गई। इतिहास बताता है कि छल और धोखे की घटनाएं बार-बार होती रहीं। कहा जा सकता है कि भारत में आदिवासियों का इतिहास केवल धोखा खाने और बदहाली के गर्त में गिरते रहने का इतिहास है। उदाहरण के लिए इसी किताब में दो और घटनाएँ हैं। “साठ के दशक में डूंगरपूर के शाही परिवार के महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर ने घोषणा की कि वे अपने राज्य की ज़मीनें बेचने जा रहे हैं। भीलों ने अपने नाते-रिश्तेदारों से उधार लेकर उन लोगों से संपर्क किया जो राजा को जानते थे। उन्हें राजा ने दयालुता में कुछ ज़मीनें 50 रुपया बीघा की दर पर दे दीं। कुछ लोगों को ज़मीनों का पट्टा भी मिला। यह पट्टा कागज पर नहीं था बल्कि कपड़े के एक टुकड़े पर स्याही से बिक्री का सबूत बनाया गया था। कइयों को यह भी नहीं मिला। इसी शाही जमीन को चक राजधानी के नाम से जाना गया। इन ज़मीनों पर जो 21 गांव बसे, उनके नाम के आगे चक लगा हुआ है।” (वही, पृष्ठ 220-221)
लेकिन यह पट्टा केवल धोखा था और राजा ने इस प्रकार गरीब भीलों के लाखों रुपए डकार लिए। “अगले कुछ सालों तक यहाँ यथास्थिति बनी रही। जिन्हें जमीन मिली उन आदिवासियों ने उसे साफ करके खेती लायक बना लिए और उपज लेने लगे। अचानक 1977 में राजस्थान सरकार ने जमीनों का सर्वे शुरू किया और भीलों से कहा गया कि यह जमीन उनकी नहीं है। राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी एस्टेट अधिग्रहण कानून, 1963 के मुताबिक पुराने राजाओं की सारी जमीन अब सरकार की थी। राजा ने यह बात भीलों को जमीन देते वक्त उनसे छिपा ली थी। अधिकतर जमीन 1963 के बाद ही भीलों को बेची गई थी। सर्वे के बाद भी पांच-छह साल तक आदिवासी खेती करते रहे लेकिन 1982 से उनके पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी नोटिस आने शुरू हो गए। इन भीलों से अतिक्रमण के दंडस्वरूप 500 से 5000 रुपए के बीच राशि सरकार ने मांग ली। … एक बार फिर से भीलों को कर्ज लेना पड़ा, अपने गहने बेचने पड़े ताकि दंड चुकाया जा सके। किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। सबको यह लग रहा था कि दंड देने के बाद जमीन फिर से उनकी हो जाएगी। बाद के वर्षों में दंड की राशि तो कम होती गई लेकिन 30 से ज्यादा वर्षों से लगातार वसूली की जा रही है। भीलों ने अपनी जमीन के एवज में तीन दशक के दौरान जितना दंड चुकाया है, वह उनकी जमीन की मूल कीमत से भी कहीं ज्यादा है।” (वही , पृष्ठ 221)
आखिर यह कहानी क्या बताती है? यही कि स्वतंत्र भारत के सदियों पहले धोखे से भीलों का राज्य छीन लिया गया और स्वतंत्र भारत के बरसों बाद उन्हें धोखे से सरकारी जमीन बेच दी गई। यह तब हुआ जब उनके देश का एक संविधान है और उसमें उनके लिए भी वैसे ही अधिकार हैं जैसे बाकी देशवासियों के। लेकिन इस संविधान के बावजूद उन्हें दंडित किया गया जबकि असली अपराधी महारावल लक्ष्मण सिंह थे, जिन्होंने बड़ी चालाकी से सरकारी जमीन को अपनी कहकर भीलों को पट्टा दे दिया था। क्या ऐसा कोई सबूत कि उन्हें कोई सजा दी गई? इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बाद में राजपरिवार ने 1963 में ली गई जमीन के लिए सरकार द्वारा तय मुआवजे पर असंतोष जाहिर किया और इसके खिलाफ अजमेर की उच्च अदालत में अपील की। 2006 में यह मामला उदयपुर रेवेन्यू कोर्ट में गया जिस पर कोई फैसला नहीं हुआ और उसी के साथ आदिवासियों की जमीन का मामला भी अटका है। अब इस बात पर गौर कीजिये कि सरकार ने राजा को मिलने वाला मुआवजा तय किया यानी जमीन को अधिग्रहित किया। राजा ने फिर भी वह जमीन अपनी बताकर भीलों को बेची। इसका मतलब राजा ने केवल भीलों को ही नहीं, बल्कि सरकार को भी धोखा दिया। फिर क्या होना चाहिए? परन्तु हुआ कुछ नहीं।
और तो और, राज्य सरकार ने भी कमोबेश वही किया जो राजा ने किया था। सामाजिक न्याय की अवधारणा बनने वाले चिंतकों को इस पर गहराई से सोचना चाहिए कि बहुजन की परिभाषा के तहत एससी, एसटी, ओबीसी और माइनारिटी बी बात करना आदिवासियों के साथ हुए धोखे और बहिष्कार को बड़ा सवाल नहीं बना सकता। उनके जीवन और इतिहास को और भी शिद्दत से देखे जाने की जरूरत है। और केवल अस्मितावादी दृष्टिकोण से ही उन्हें देखना आधा-अधूरा निष्कर्ष देगा। उन्हें संपूर्णता में देखना और अपने साथ जोड़ना होगा। वे हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। उनका अतीत जितना दर्दनाक है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ़ों से भरा उनका वर्तमान है। डूंगरपुर के मामले को ही एक मॉडल मान लिया जाय तो पता चलेगा भारत के एक बहुत बड़े भू-भाग में रहने वाले आदिवासी सरकार और राजा की दोहरी मार के शिकार हैं। 1987-98 में 15 गांवों के 450 आदिवासी किसानों को गैर खातेदारी के तहत जमीन दी गई लेकिन इसकी शर्त यह थी कि राजा के लिए जो मुआवजा तय होगा उसका भुगतान किसान करेंगे। लेकिन सच यह है जिस जमीन पर वे पचास साल से खेती कर रहे हैं वह उनकी नहीं है। राजा ने मुआवजे की राशि पर अधिग्रहण के समय से ही 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की है। आप इस बात की कल्पना कीजिये कि दृश्य कितना भयावह है? लेकिन वास्तविकता यही है। वे जितना अपने अतीत से लड़ रहे हैं उससे कहीं अधिक आज के दौर से लड़ रहे हैं। एक मुफ्तखोर, मुआवजाखोर, षड्यंत्रकारी और जनविरोधी दुनिया उनके चारों ओर है, जिसमें सरकार-सामंत-बनिया-कॉर्पोरेट-न्यायालय-सैन्यबल सब कुछ है। इसी में उनके विरोध में खबरें छापकर उनके जीवन को विकृत करके पेश करनेवाली मीडिया है, जिसमें तरह-तरह के फाहश और फूहड़ लेखक-कवि-कलाकार और समाजशास्त्री हैं।
यह भी पढ़ें : हूल से उलगुलान तक : आदिवासी विद्रोहों की जड़ में रहे हैं वन कानून
सरकारी खातों और व्यवहार में आदिवासी जीवन एक विडम्बना और मज़ाक बनकर रह गया है। बरसों पहले प्रसिद्ध पत्रकार पालागुमि साइनाथ ने एक रिपोर्ट लिखी थी – ‘धुरवा मुंडा सड़क जो कहीं नहीं जाती’। दो दशक पहले उन्हें पता चला कि एक आदिवासी परिवार के दो सगे भाइयों में से एक को सरकारी कर्मचारियों ने आदिवासी तथा दूसरे को गैर-आदिवासी दर्ज कर दिया है, जिससे एक को मिलने वाली सहूलियतें बंद हो गईं। यह मामला स्पेलिंग मिस्टेक का था। जो कर्मचारी उनके नामांकन के लिए आया था उसने एक भाई का टाइटल धुरवा और दूसरे का धरुवा लिख दिया। यह बात विभाग में ऊंचे दर्जे तक पहुंची और एक भाई को आदिवासी नहीं माना गया। पी. साइनाथ के लिए यह बहुत दिलचस्प मामला था। यात्रा के दौरान जब वे मुख्य सड़क से उतर कर कच्ची सड़क पर चले तो छह किलोमीटर दूर उन्होने देखा कि फिर से पक्की सड़क शुरू हो गयी। आठ किलोमीटर बाद वह खत्म हुई और फिर कच्ची सड़क से उन्होंने दस किलोमीटर की यात्रा की तब उस गांव में पहुंचे। पक्की सड़क धुरवा मुंडा नाम के एक आदिवासी के नाम पर थी जो उसी गांव में रहता था। वे उससे मिलने गए तब देखा कि वह एक गरीब अधेड़ आदिवासी है, जिसकी माथे की लकीरें चिंताओं से बनी हैं । उन्होने पूछा कि तुमको पता है कि इस जिले में तुम्हारे नाम पर एक पक्की सड़क है। धुरवा मुंडा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए इंकार किया। उसने साइनाथ से प्रार्थना की कि साहब आप यहां के पटवारी के चंगुल से मेरी जमीनें निकलवा दीजिये। वह अपने साले को आगे करके हमारे गांव के कई लोगों की जमीनें हड़प चुका है। वह सरकारी आदमी है, लेकिन हमारी तो कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है।
हम साफ-साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जंगलों में आग लगी है और दूसरी ओर शांति के गीत गाये जा रहे हैं। आग और संगीत को लेकर लोक में एक व्यंग्य है – ‘आग लगी हमरी झोपड़िया में हम गायें मल्हार’। लेकिन देखा लगातार यही जा रहा है। पिछले तीन दशकों में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के जंगलों में प्रतिदिन आदिवासियों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन जो बातें बाहर आनी चाहिए, वे नहीं आईं। आईं तो ढोल-ढमाकों की आवाजें आईं। जिस मुख्यधारा की चिंताएं वसुधा भर में अपनी कुटिया बनाना था, वह इस बात को लेकर कतई चुप थी कि आदिवासियों से लड़ने के लिए आदिवासियों को ही तैयार किया गया है। जंगलों में रहनेवाले साम्राज्यवादी टुकड़खोरों और शहरी विकासवादियों बीच एक गहरा समझौता हो गया कि हमको किस बात पर ताली बजाना है और किस चीख पर कानों में रुई ठूंस लेना है। यह आज का सबसे भयावह सत्य है और इसकी आड़ में आदिवासियों के हक की बातें और उनकी हत्याएं बड़ी आसानी से छिप जाती हैं। यह बात क्या छिपी हुई है कि देशी-विदेशी पूंजी और सरकारी बूटों के तले दम तोड़ता आदिवासी अपने अस्तित्व और अधिकार की लड़ाई लगातार हार रहा है ।
मुझे मारियो वर्गास ल्योसा के उपन्यास ‘किस्सागो’ (स्टोरीटेलर) की याद आती है जिसमें एक विशाल पहाड़ी पर रहनेवाले आदिवासियों के उजाड़ने का सवाल उठाया गया है और इसे एक द्वंद्व के रूप में रखा गया है कि क्या खनिज संपदाओं के अकूत भंडार के लिए आदिवासियों को उजाड़ दिया जाय या तिजारती व्यवस्था की लार टपकाती लालच को रोका जाय? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ नत्थी है अपने प्राचीन रहवासों में निवास करते भोले-भाले और मुनाफे तथा लालच से दूर आदिवासियों और उनकी जीवन-संस्कृतियों को न छेड़े जाने का सवाल। इस सवाल को बहुत गहरे विषाद के साथ देखा जा सकता है और वहां दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ पर्यावरण, मनुष्यता और उसकी अस्मिता के सारे रूपों को बचाने के लिए उठे हाथ हैं तो दूसरी ओर खलील जिब्रान के शब्दों में ऐसे जीव हैं जिनका धड़ मनुष्य का और सिर जानवर का है और जो बहुत तेजी से जंगलों और पहाड़ों को खा रहे हैं और नदियों और समुंदरों को पी रहे हैं। यह पूछने पर कि आप इतनी तेजी से यह सब क्यों खा-पी रहे हैं वह जवाब देता है कि इसलिए कि कल पता नहीं यह रहे न रहे।
भारत के आदिवासियों के अपने अनवरत संघर्ष हैं, लेकिन उनकी कहानियां कब बाहर आती हैं? अव्वल तो जीवन की कड़ी चुनौतियों ने उन्हें शब्दों की दुनिया से काफी दूर कर दिया है। उनके बच्चों के स्कूल पैरामिलिटरी के कैंप बने हुए। वे खनन मशीनों और उनकी सुरक्षा में लगी बख्तरबंद गाड़ियों के शोर में जी रहे हैं। उन पर लगातार शक किया जा रहा है। उनकी एक-एक गतिविधि को दर्ज किया जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ों में कब वे या उनके परिवार के लोग न रहें इसका कोई ठिकाना नहीं। थानों में उनकी बहन-बेटियों के साथ कब सामूहिक बलात्कार हो इसका कोई हिसाब नहीं। चारों तरफ हंटिंग चल रही है, लेकिन खबरें विकास की आ रही हैं। खबरें खलील जिब्रान के द्वारा देखे गए उन जीवों की आ रही हैं जो उनके जंगलों और पहाड़ों को एक ही दिन में चर जाना चाहते हैं। सच यह है कि भारत केवल पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि यहाँ के प्रभुवर्ग की पूरी तरह बेईमानी पर आधारित राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी है जिसकी मूल प्रवृत्ति अपने ही लोगों के खून की आखिरी बूंद निचोड़ लेने की है। शहरी और औद्योगिक सर्वहारा तो इसके खिलाफ एकजुट हो भी सकता है लेकिन आदिवासी इस कदर बिखरे हुए और असहाय हैं कि उनकी आवाजें बहुत दूर तक नहीं जा पातीं।
मेरे सामने जब भारत के बहुजन का यह हिस्सा आता है तो लगता है कि कहने को भले ही हम उनको अपना मानने का दावा करें लेकिन हम उनके जीवन से पूरी तरह परिचित ही नहीं हैं। हमारे पास उनका सही सही डाटा ही नहीं है और वे हमारे सरोकारों में बहुत हद तक आंकड़े से ज्यादा नहीं हैं। इस संबंध में कथाकार-इतिहासकार सुभाष चन्द्र कुशवाहा ने एक बार एक दिलचस्प तथ्य साझा किया। वे जब मध्य भारत में भील विद्रोह पर काम कर रहे थे तब सामान्य संदर्भ किताबों में उनके लिए सामग्री थी ही नहीं। उन्होंने सामग्री की तलाश में लंदन से लेकर आस्ट्रेलिया के अखबारों तक की खाक छानी और जो तथ्य मिले वे लोमहर्षक थे। भीलों को काबू करने, जो काबू में न आए उनको धोखा देने और उनका सामूहिक संहार करने की दिल दहलाने वाली कहानियां सामने आईं। भीलों का अप्रतिम नायक तांतिया मामा भारत के इतिहास का बेमिसाल चरित्र है। बहुत पहले से संघ ने उसके हिंदुकरण की कोशिशें कर दी थी। संघ के हिन्दी मुखपत्र ‘पांचजन्य’ ने 1980 के दशक में एक भारी-भरकम अंक निकाला था – ‘वीर वनवासी अंक’। पूरे अंक में भारत के सैकड़ों आदिवासी नायकों को उन लोगों के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाया गया, जिनका सफाया संघ का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उन दिनों भारत के बुद्धिजीवी प्रायः ऐसे लोगों के बारे में सोचने से गुरेज रखते थे। उनको न इसमें दिलचस्पी थी न कोई सरोकार। इसका परिणाम हुआ कि संघ ने भारत के जंगलों के हर कोने में राम के चरणों की निशानदेही की और कहीं शबरी तो कहीं सुग्रीव, कहीं जामवंत कहीं जटायु तो कहीं संपाती को राम की सेवा करते दिखाते हुए कहानियां गढ़ीं। आज हालात यह है कि संघी आदिवासियों का बहुत बड़ा समूह अस्तित्व में है, जो कहीं सलवा जूड़ुम में हिस्सेदार है तो कहीं रामकथा कहते हुए। बाजी हाथ से निकली हुई है। सामाजिक न्याय की ताक़तें भी महज़ सरकारी नौकरियों में उनके आरक्षण के सवालों तक ही उन्हें जोड़ पाई हैं। उनके जंगलों की कॉर्पोरेट द्वारा लूट, उनके प्रतिरोध को खत्म करने के लिए चलाये जा रहे अनवरत दमन, पेसा कानून और वनाधिकार के उनके संघर्ष को समर्थन, उनके शिक्षा के अधिकार को समर्थन और उनकी हत्याओं और बलात्कार के खिलाफ व्यापक बहुजन गोलबंदी आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है ।
मेरे मन में लगातार यह सवाल उठता है कि आदिवासियों की आत्माभिव्यक्ति के जितने भी रूपों से हम परिचित हैं क्या वे हमारे भीतर कोई गहरी भावना जगाते हैं? हमारे मानवीय सरोकारों में उनका जीवन और उनके सुख-दुख कोई जगह बना पाते हैं? उनका जीवन, उनके संघर्ष, उनके किस्से, उनकी चुनौतियां, पूरे देश के समाजों के साथ उनकी तुलनाएं, उनकी अपनी स्वतःस्फूर्त अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था में उनकी जगह, उनका हिस्सा और उनकी वास्तविक भागीदारी, उनका असंतोष, उनका गुस्सा, उनका संघर्ष और उसकी परिणतियां, उनके संसाधनों की लूट और उनकी हत्याएं हमें कितना संवेदनशील बनाती और विचलित करती हैं?
महाश्वेता देवी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है ‘चोट्टि मुंडा और उसका तीर’। चोट्टि मुंडा को अपने पूर्वज बिरसा भगवान के संघर्षों की गाथा याद है। वह जानता है कि बिरसा भगवान का संघर्ष और बलिदान कितना महान है। वह तीर चलना चाहता है। उसमें इसकी प्रतिभा है। लगन है। वह एक विलक्षण युवा है। आखिर वह अपने गुरु की शिक्षा से तीर चलाने में प्रवीणता हासिल कर लेता है। सबसे पहले वह मेलों में प्रतियोगिता जीतता है और धीरे-धीरे उसका नाम चारों ओर फैल जाता है। लेकिन उसके चारों ओर अपार दुख हैं – शोषण, गरीबी, अन्याय और आदिवासियों को सरेआम ठगने का सिलसिला है। बोलने पर पुलिसिया दमन और उत्पीड़न। मैदानी लोगों, बनियों और पुलिस का गठजोड़ और आतंक। चोट्टि को लगता है इस तीर का अर्थ ही क्या जब वह अन्याय के खिलाफ न चले।
लेकिन गजब यह है कि उसे तीर चलाने की मनाही है। सरकार और समाज द्वारा यह इजाजत नहीं है। एक दिन चोट्टि का बाप अपमानित होकर आत्महत्या कर लेता है। एक दिन तमाम मुंडा अपना गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और चोट्टि कुछ नहीं कर पाता। यह प्रतीक कथा बहुत कुछ कहती है।
बहरहाल, चोट्टि मुंडा के पास तीर तो है लेकिन उसे चलाने की आज़ादी नहीं है। उसका हथियार खेल का माध्यम भर रह गया है। मुक्ति का माध्यम नहीं बन पा रहा है। पता नहीं चोट्टि मुंडा को तीर चलाने की आज़ादी कब मिलेगी? वह दिन निश्चित रूप से आदिवासी जीवन और साहित्य का नया अध्याय बनेगा!
(संपादन : नवल/अनिल/अमरीश)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in
फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें
मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया