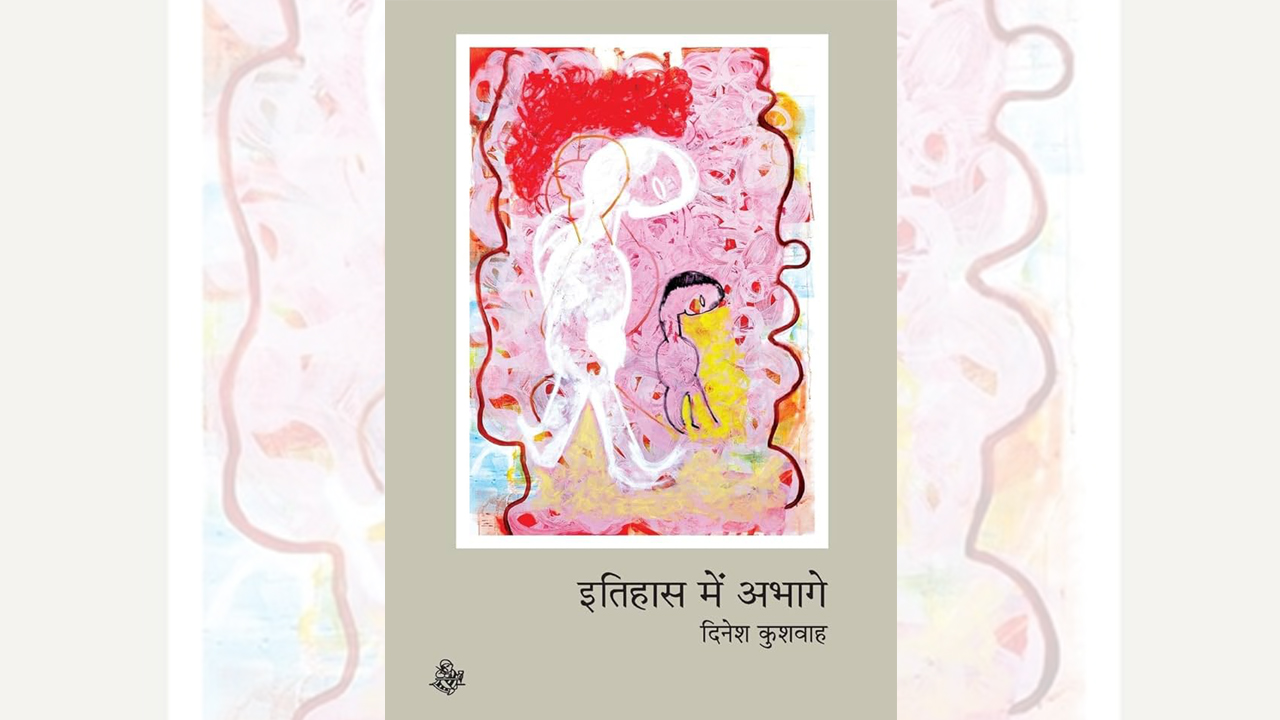[दलित साहित्य अब अनेक स्तरों पर मुख्यधारा के साहित्य के साथ मुठभेड़ कर रहा है। समालोचना के क्षेत्र में भी अनेक आवाजें इसके भीतर से भी उठी हैं और विमर्श का विस्तार हुआ है। यहां तक कि दलित साहित्य के नामकरण पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही, देश में मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में दलित साहित्य की दिशा कैसी हो, इन बातों को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजेश पासवान से फारवर्ड प्रेस ने खास बातचीत की। प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग]
पहले भाग के आगे
साहित्य की अन्य विधायें जैसे कि हम कहानियों, उपन्यासों, कविताओं व नाटकों की बात करें तो उत्तर भारत के दलित साहित्य में एक खालीपन सा दिखता है। ऐसा क्यों?
खालीपन नहीं है। इन विधाओं में भी लोग लिख रहे हैं। अच्छी कविताएं, अच्छी कहानियां, उपन्यास, नाटक भी लिखे जा रहे हैं। इतिहास की दृष्टि से भी काम हुआ है। लेकिन चूंकि कहने के लिए ‘मैं’ वाली भावना आ जाती है और यह इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि कविता, कहानी, नाटकों में भी इसकी अभिव्यक्ति मिल जाती है। वास्तव में अगर कोई दलित कहानीकार भी लिख रहा है तो वह भी अपनी जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को ही अपने कहानी का आधार बनाता है। उसमें थोड़ा बहुत वह रुपांतरण करते हैं। आप देखिए कि ओमप्रकाश वाल्मीकि की कई कहानियों में उनकी आत्मकथाओं के प्रसंग मिल जाते हैं जो उनके अपने जीवन से जुड़े हुए हैं। जितने भी दलित साहित्यकार हैं वो निबंध, कहानी और उपन्यास जो कुछ भी लिख रहे हैं, कहीं न कहीं उनमें दलित जीवन की घटनाएं और उनके अपने अनुभव शामिल हैं। आप कह सकते हैं कि उनकी आत्मकथाओं का विस्तार कहानियों में, कविताओं में, उपन्यास आदि सारी चीजों में हैं। और वह दलित संवेदना का भी विस्तार है। जैसे कि बहुत प्रसिद्ध कविता है ओमप्रकाश वाल्मीकि की “ठाकुर का कुआं, खेत ठाकुर का…” – इसमें वह कहते हैं कि भाई, मेरा क्या है जब सब कुछ ठाकुर का है। तो यह सही है कि जमीनों पर कब्जा कुछ लोगों का है। बाकी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा भी उन्हीं लोगों का है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस तरह की दलित समाज की विडंबनाओं की व्याप्ति लगभग दलित साहित्य के सभी विधाओं में हैं।
एक और आप कमी के रूप में मान लें या जो भी कहें कि शुरूआती दौर के जितने भी प्रमुख दलित साहित्यकार रहे हैं वे पूर्णकालिक अकादमिशियन नहीं रहे हैं। उनके पास दूसरी नौकरियां थीं। ओमप्रकाश वाल्मीकि डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्टरी में काम करते थे। कंवल भारती जी भी सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। डॉ. श्यौराज सिंह बेचैन अकादमिक जगत में हैं। जयप्रकाश कर्दम भी सरकारी अधिकारी रह चुके हैं। बाकी माता प्रसाद जी जैसे लोगों ने अन्य सरकारी नौकरियों में रहते हुए साहित्यक कार्य को अंजाम दिया है। और अकादमिक क्षेत्र में जो लोग हैं, उनका काम पढ़ना-पढ़ाना और रिसर्च करना आदि रहा है। अब जो दूसरी पीढ़ी आ रही है, जो अकादमिक जगत में है, लिख-पढ़ रही है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि धीरे-धीरे उनमें अकादमिक उत्कृष्टता भी आ रही है। हालांकि पहले वालों में भी कम नहीं है। पहले वालों का जो है, वह सबकुछ स्वाध्यायजनित है। लेकिन अकादमी में आने के बाद उसको एक और अकादमिक आकार मिल रहा है। मैं कभी-कभी मजाक में कहता हूं कि परती जमीन में जब हम खेती करते हैं तो जो पहली फसल होती है, थोड़ी सी कमजोर होती है। लेकिन जैसे-जैसे हम उस पर लगातार खेती करते जाते हैं, लगातार सिंचाई-निराई आदि होने लगती है, वैसे-वैसे दाने पुष्ट होने लगते हैं। इसी तरह से दलित साहित्य भी है। दलित साहित्य जो इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है क्योंकि पहली और दूसरी पीढ़ी के लोग अभी लिख रहे हैं और धीरे-धीरे उनमें परिपक्वता आएगी।
जब हम हिंदी के मुख्य धारा के साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो वह भी 20-25 वर्षों के साहित्य का इतिहास नहीं है। यह है तो कई सौ वर्षों का। उनकी परंपरा चली आ रही है। उनके लिखने वालों की भी साहित्यिक अभिरुचि की परंपरा कई पीढ़ियों से रही है। दलित साहित्य के संदर्भ में कहें तो धीरे-धीरे यह मुकाम भी हासिल होगा और आने वाले समय में चीजें और बेहतर होंगीं। और यह एक शुभ संकेत है कि भारतीय गणतंत्र के बाद जब लोकतांत्रित चीजें मजबूत हुईं तो दलित समाज में भी एक मध्यवर्ग विकसित हुआ है। 1950 के बाद आरक्षण के लागू होने के कारण मध्यवर्ग जब विकसित हुआ तो उसी अनुपात में दलित साहित्य में भी वृद्धि हुई है। इससे पहले का जो साहित्य अनगढ़ा साहित्य है। हालांकि आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र और कमजोर होने वाला है क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां कुछ ही पार्टियों में या व्यक्तियों में और विचारधाराओं में केंद्रित हो रही हैं। आने वाला समय बहुत कठिन होने जा रहा है।

दलित साहित्य में समालोचना के क्षेत्र में जिस तरीके का काम होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हो पा रहा है। इक्के-दुक्के लोग ही कर पा रहे हैं। क्या आपको यह बात चिंतित नहीं करती?
यह आप सही कह रहे हैं। समालोचना के क्षेत्र में कम काम हुआ है और इसकी कुछ वजहें भी मैं मानता हूं। जब साहित्य की कोई रचना छपकर आ जाती है, तो उस पर चर्चा करने का अधिकार सबको है। जो भी पाठक है, किताब उसी की हो जाती है। पाठक उसे अच्छा या बुरा कह सकता है। उसको कूड़ा कह सकता है या उसको श्रेष्ठ साबित कर सकता है। यह पाठक का अधिकार है। लेकिन ऐसा मैं देखता हूं कि कुछ अपवादों को छोड़कर हमारे जो दलित बुद्धिजीवी हैं, दलित साहित्यकार हैं, यदि उनकी कोई आलोचना होती है तो उस आलोचना को वे साहित्यिक भाव से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फिर वे यह जानने में लग जाते हैं कि आलोचक की जाति क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका सरनेम क्या है। इस आधार पर वे आलोचना का मूल्यांकन करने लगते हैं। मुझे लगता है कि बौद्धिक बहस के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं। चर्चा साहित्य की होनी चाहिए न कि साहित्यकार की होनी चाहिए। रचना अगर जनता के बीच में आ गई तो सबको खुली आलोचना करने का अधिकार है। और उस रचनाकार को भी आलोचना को सुनने का, समझने का और अगर परिवर्तन जरूरी है तो परिवर्तन करने का अधिकार है। दलित साहित्यकारों में यह भाव अभी कम है। इस कारण कई बार लोग दलित साहित्य की मुखर आलोचनाएं नहीं कर पाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार आलोचनाएं होती हैं तो आलोचनाओं में जो तथ्य दिए जाते हैं, उन तथ्यों पर बात न करके हम आलोचक की जाति, धर्म और उसकी विचारधारा पर बात करने लगते हैं। ऐसे में अगली बार आलोचक सोचते हैं कि अब मुझे आलोचना करनी ही नहीं है। दूसरी एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा कि दलित साहित्यकार हिंदी साहित्य व हिंदू सामाजिक व्यवस्था के मुखर आलोचक रहे हैं। इस दृष्टि से दलित आलोचना को अगर हम देखे तो इसका विमर्श व्यापक रहा है। दलित साहित्यकार इतिहास दृष्टि में नए तरीके से देख रहे हैं। राजनीति की नए सिरे से व्याख्या कर रहे हैं। साहित्य में भी नए सिरे से व्याख्या कर रहे हैं। साहित्य में भी आप देखिए कि ज्यादातर जो दलित साहित्य के निबंध हैं, वह हिंदी साहित्य की आलोचना से ही उभरे हैं। डॉ.धर्मवीर की जो कबीर विषयक दृष्टि है या प्रेमचंद विषयक दृष्टि है; कंवल भारती द्वारा अनूदित जो कबीर के ऊपर ‘कबीर और कबीरपंथ’ जो बहुत अच्छी पुस्तक आई है; संत रैदास पर बहुत अच्छी पुस्तकें डॉ.धर्मवीर की भी हैं और सौंदर्य शास्त्र को लेकर जो भी किताबें आई हैं— इन सभी के आधार पर कहा जा सकता है कि आलोचना दृष्टि विकसित हुई है। लेकिन दलित साहित्य में दलित साहित्य के प्रति आलोचना दृष्टि कम विकसित हुई है। इसे आप मोह कह सकते हैं या फिर आत्मप्रशंसा का भाव। मुझे लगता है कि यह जितना कम हो दलित साहित्य के लिए उतना ही ठीक है।
एक लोक मान्यता रही है कि साहित्य राजनीति को दिशा प्रदान करता है। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है साहित्य कहीं न कहीं सत्ता के लिए उपकरण के जैसा है। दलित साहित्य के मामले में इसे आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, दलित राजनीति को सिर्फ दलित साहित्य ही नहीं, बल्कि दलित समाज की सारी गतिविधियां दलित राजनीति को सपोर्ट करती हैं। दलित राजनीति को सपोर्ट करने में दलित संबंधी सारे विमर्श बहुत सहायक हुए हैं। लेकिन उसी अनुपात में दलित राजनीति ने दलित साहित्य को, दलित सामाजिक व्यवस्था को, दलित विमर्श को या दलित जो आध्यात्म है, उसी अनुपात में सपोर्ट नहीं किया है। मैं एक उदाहरण देकर कहूं कि जो भी सजग दलित समाज है, वह सामाजिक राजनीति में अपनी बात बेबाकी से रखता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि दलित राजनीति कर रहा है। मुझे ध्यान है 1997 में मैंने एम.ए किया और दलित साहित्य में एम.फिल तथा बाद में दलित साहित्य पर ही पीएचडी किया। पर जहां भी मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाता था, दलित साहित्य पर बात होती थी, लेकिन उसके बाद फिर दलित राजनीति पर बात होने लगती थी। तो जो भी सतर्क दलित है, उसको लोग मानते हैं कि वह सतर्क है। जाहिर तौर पर यदि कोई दलित है तो दलित राजनीति का भी एक हिस्सा है। लेकिन दलित राजनीति और खासकर बसपा को हम कहें कि ये दलित राजनीति के एक प्रतीक के रूप में देखें तो बसपा जैसे राजनीतिक दलों में दलित साहित्य के साथ दलित साहित्यकारों के साथ, दलित समाज के अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ या दलित समाज की अन्य जो संवेदनाएं हैं, जो दलित युवाओं की संवेदनाएं हैं या जो अन्य मुद्दे हैं, उनको कम एड्रेस किया है। दलितों को बसपा की मौजूदा राजनीति ने नहीं, बल्कि मान्यवर कांशीराम की राजनीति रही, उसने बहुत समृद्ध किया है। मान्यवर की राजनीति ने निकस बनाए, जिसे लेकर दलित साहित्य का विस्तार हुआ। उन्होंने सामाजिक संगठनों को जोड़ा। महापुरुषों पर चर्चाएं की। इन्हीं सब पर चर्चाओं को विस्तार देने का काम दलित साहित्य ने किया। उन महापुरुषों की जीवनियां लिखीं। उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया। उसमें पत्र पत्रिकाएं निकलीं। यह सब दलित समाज को राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न करने का काम किया गया। लेकिन दलित राजनीति जब शीर्ष पर थी तब उस समय अनुपात में उन्होंने दलित साहित्य को और मजबूत करने का काम नहीं किया। इसे दलित राजनीति की एक कमी कह सकते हैं। लेकिन दलित राजनीति को आप कह सकते हैं कि आज भले पराभव के दौर से गुजर रही है, लेकिन दलित साहित्य अभी भी उत्कर्ष पर है। दलित उद्यमिता अपने विकास से गुजर रही है। दलित अध्यात्म भी अपने …
दलित अध्यात्म से आपका क्या तात्पर्य है?
हर आदमी की अपनी आध्यात्मिक अभिरुचि होती है। जैसे बाबासाहब आंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो बहुत सारे लोगों को लगा और आज भी लगता है कि बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। अगर धर्मांतरण कर लेते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस वजह से आप देखिए बहुत सारे ऐसे धर्मांतरण के आंदोलन भी चल रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट करने की कोशिशें भी चल रही हैं। ऐसा करनेवालों को लगता है कि ऐसा करने से दलित समाज की आध्यात्मिक जरूरतों की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही दलित अध्यात्म का टर्म मैंने इजाद किया। लोग इससे असहमत हो सकते हैं कि आज जो कि एक धर्म है या फिर उसके आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि एक बिजनेस यूनिट के रूप में भी काम कर रहे हैं। आप उसे कंपनी मान सकते हैं। इसमें पूंजी का निवेश होता है। उसकी अपनी संरचना होती है। मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूं कि दलित समाज में बहुत अधिक बेरोजगारी है और बेरोजगारी को एक तरीके से कम किया जा सकता है कि इस समय जितने भी बाबासाहब के नाम पर, दलित महापुरुषों के नाम पर बहुत सारे बौद्ध विहार बने हुए हैं, अन्य जो भी पार्क, प्रतिष्ठान आदि बने हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी दलित युवाओं को दी जाय। अगर हम हिंदू मंदिरों के संदर्भ में कहें तो हर मंदिर से आय भी पैदा होती है। वहां पर लोग पूजा-पाठ करते हैं। चढ़ावा आदि चढ़ता है। उस चढ़ावे से कुछ परिवारों का भरण-पोषण होता है। कुछ लोग कहते हैं इन चढ़ावों से अंधविश्वास, पाखंड में कहीं न कहीं बढ़ोत्तरी होती है। लेकिन दलित उसे एक अवसर के रूप में ले सकते हैं। जितने भी बाबा साहब से संबंधित संस्थान हैं, उन्हें नॉलेज लर्निंग सेंटर के रूप में डेवलप किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि इन संस्थानों में लोग बाबासाहब की जयंती या परिनिर्वाण के मौके पर ही जाते हैं। बाबाासाहब की प्रतिमा के पास कोई दलित युवा जाकर वहां रहे। वहां लाइब्रेरी शुरू करें या कोचिंग सेंटर के रूप में विकसित करे, वहां पर पढ़ने-पढ़ाने का काम करे। वह एक अच्छा रिसोर्स सेंटर हो सकता है। और आसपास के लोग वहां जाएं, बैठें तथा काम करें। क्योंकि भले धर्म की अपनी लाख बुराईयां हों, लेकिन धर्म एक-दूसरे की सामाजिकता के निर्वहन के भी काम आता है। जैसे लोग मस्जिद में हर शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज़ पढ़ना एक बहाना है। उसी बहाने एक-दूसरे से लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। चर्च में भी लोग रविवार को जाते हैं, आपस में मिलते-जुलते हैं। लेकिन इस तरह से लगातार मिलने-जुलने का आयोजन दलित समाज में कम ही होता है। जैसे एक बार मैं नागपुर गया था तो मैंने देखा कि हर रविवार को वहां भीम महिला मंडल नामक संगठन की महिलाएं किसी न किसी के घर में मिलती थीं और आपस में बातचीत करती थीं।
तो जहां-जहां डॉ आंबेडकर के नामपर पार्क, बौद्ध विहार है, वहां-वहां कोई आदमी इस काम को शुरू कर सकता है। इस तरह से लाखों दलित युवक इंगेज हो सकते हैं। और वो धर्म का बाबासाहब के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के बजाय जागरुकता, तार्किकता, ज्ञान और एक इनोवेटिव, आइडिया फैलाने का काम कर सकते हैं। चूंकि अगर वहां पे इस तरीके की चीजें विकसित हो जाएंगी तो लोग आना-जाना, उठना-बैठना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि यह नए दौर की जरूरतें हैं और इसको करना चाहिए। (हंसते हुए) भविष्य में सेवानिवृत्ति के बाद मै भी इस तरह का प्रयास कर सकता हूं।
(संपादन : समीक्षा/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in