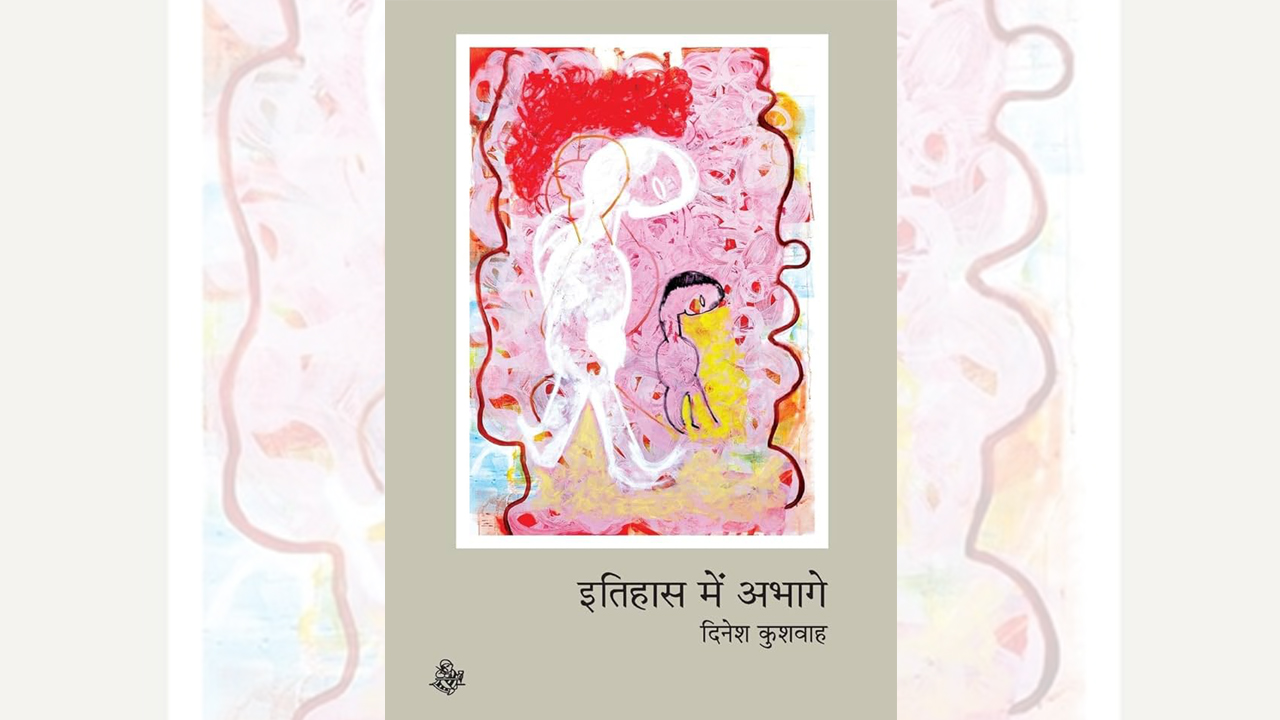‘स्त्री अस्मिता’, यानी पर्यायक्रम से अपने अस्तित्व को लेकर गर्व, अपने अस्तित्व पर थोपे गए पाखंडपूर्ण परिचय का विरोध और अपने अस्तित्व को सही मायने में प्रतिष्ठित करने की लड़ाई है। उदाहरणस्वरूप– हां, मैं हूं नारी या फिर मुझे अपने नारी होने पर गर्व है। नारी रूप में जन्म लेने के कारण न तो कोई नारी पुरुषों से कमतर है और न ही उसे पुरूषों के अधीन रहकर जीना है। लेकिन भारतीय समाज यही विमर्श थोपता आया है।
अलग-अलग कालखंडों में भारत की कितनी ही नारियों में स्त्री अस्मिता की यह आग कभी पूर्णांश में तो कभी भग्नांश में कौंधती आई हैं। आज तो अकादमिक और व्यवहारिक जगत में ‘स्त्री अस्मिता’ एक ज्वलंत मुद्दा है। कुछेक नई चूनौतियों के बाद भी स्वीकारना होगा कि स्थान, परिवेश और परिचय के अनुरूप आज स्त्रियों के हालात में काफी साकारात्मक परिवर्तन आया है। पहले एक-दो महिलाएं ही जहां साहस कर पाती थीं। लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसकी भागीदार बनती जा रही हैं।
हालांकि यह भी सत्य है कि पुरुष प्रधान हर क्षेत्र, अब चाहे वह अकादमिक और साहित्यिक जगत ही क्यों न हो, उनमें स्त्रियों की अपनी पैठ बनाना एक लंबा संघर्ष रहा है। यह संघर्ष जनजातीय साहित्यकारों के लिए और अधिक बढ़ जाता है। इन तमाम संघर्षों को पार कर आज जनजातीय कवयित्रियों की ‘मानक भाषागत’ रचनाएं पर्याप्त सुर्खियां बटोरने में सक्षम हो रही हैं। सुशीला समद, रोज केरकेट्टा, ग्रेस कुजूर, दमयंती बेसरा, जसिंता केरकेट्टा, निर्मला पुतुल, वंदना टेटे, उज्ज्वला ज्योति तिग्गा, उषाकिरण आत्राम आदि जैसी आदिवासी कवयित्रियों के काव्यजगत में हम केवल आदिवासियों और उनकी समस्याओं से ही रू-ब-रू नहीं होते, बल्कि कहीं न कहीं मनुष्य जाति और उससे जुड़ी पहलुओं से भी जुड़ते हैं।
उषाकिरण आत्राम एक ऐसा ही नाम है। वह अपनी मातृभाषा गोंडी के साथ ही मराठी और हिंदी में सृजन करती हैं। उनका एक महत्वपूर्ण काव्यसंग्रह है– ‘मोट्यारिन’। मोट्यारिन का तात्पर्य ‘घोटूल’ की शिक्षिका से है। उनका दायित्व युवतियों के चरित्र और व्यक्तित्व को सजाना-संवारना, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना होता है। यह इस काव्यसंग्रह का सशक्त पक्ष है। मसलन, ‘मोट्यारिन’ शीर्षक कविता में घोटूल की शिक्षिका मोट्यारिन युवतियों से कहती है–
“सखियो! सहेलियों! हो जाओ सावधान मेरी बेटियों!
मैं हूं मोट्यारिन तुम्हारी!
फेंक दो फटे फूटे वस्त्र अपने तन से
तोड़ दो मणि की माला अपने गले से
हो जाओ मुक्त इस बन्धन से”[1]
होना हो तो, पलाश की लाल अंगार हो!’ शीर्षक कविता में हम देखते हैं कि पति अपनी पत्नी को कोमल शृंगार कर पराए व्यक्ति के गलत नजरों में पड़ने के स्थान पर पलाश की तरह लाल अंगार बनने को कहता है–
“मत बनो रातरानी
बनना हो तो, बन जाओ पलाश की लाल अंगार
लाल धधकती अंगार ही है तुम्हारा शृंगार”[2]
इस क्रम में निर्मला पुतुल की निम्न पंक्तियां जहन में आती हैं–
“तन के भूगोल से परे
एक स्त्री के
मन की गांठे खोल कर
कभी पढ़ा है तुमने
उसके भीतर का खौलता इतिहास”[3]

युग-युगांतर से केवल दैहिक स्तर पर मापित-तुलित स्त्रियों के पतियों द्वारा ऐसा आग्रह सच में विलक्षण है। यह उषाकिरण आत्राम के काव्यसंसार में बराबर मिलता है। ठीक उसी प्रकार ‘शृंगार’ शीर्षक कविता में भी एक आदिवासी मां अपनी बेटी को क्रांतिमय ओजस्वी शृंगार करने को कहती है–
“गजरा मत बांधना बालों में तुम
सारी नजरें रूकेंगी उसपर
तुम मत बांधना गजरा
…
हो सूरज की भांति तेजस्वी
हो नागिन जैसी
हो जाओ सूरजफूल
हो जाओ लाल लाल पलाश की अंगार
तभी दिखेगा
इन बाजारू लोगों को तुम्हारा तेजस्वी शृंगार।”[4]
कई आदिवासी लोककथाओं, मिथकों में स्त्रियों को ‘सूरज’ के रूप में स्वीकारा गया है। कवयित्री आत्राम द्वारा स्त्रियों को ‘सूरज’ की भांति तेजस्वी होने का संदेश रमणिका गुप्ता के शब्दों की ओर ले जाती है– “प्रकृति के सूर्य जैसे शक्तिशाली प्रतिमान को स्त्री मानना एक मुकम्मल सोच को प्रतिपादित करता है। इसमें पुरुष की हेजेमनी नहीं है।”[5]
दरअसल उषाकिरण आत्राम की कविताओं में हम स्त्रियों के प्रति ‘केवल भोग की वस्तु’, ‘कोमल-सुंदर निहारने योग्य वस्तु’ आदि जैसे परिचय से इतर अपना एक ‘सशक्त मानवीय’ परिचय बनाने का संदेश देख पाते हैं। ये कविताएं ‘देह’ से ऊपर उठ कर मन-मस्तिष्कधारी परिचय ग्रहण करने की प्रेरणा देती है। इस तरह के अन्य उदाहरण भी मौजूद हैं, जहां प्रकृति और नारी का सुंदर समन्वय करते हुए नारी को ऊर्जामय उड़ान भरने को कहा गया है। ‘अब ऊंचे उड़ जा रे रानपक्षी’ कविता की कुछ पंक्तियां देखिए–
“रानपक्षी ऊंचे उड़ जाओ! रानपक्षी-सूर्यपक्षी
अब एक दिशा के जोड़ीदार बनो
क्योंकि दोनों के खून और सूर्यअग्नि एक रंग के हैं।”[6]
समय-समय पर विविध तरीके से शारीरिक व मानसिक तौर पर शोषित आदिवासी युवतियों को ‘जंगल की केतकी! अब बुद्धिमान बनो’ शीर्षक कविता में अपनी शक्ति को पहचानते हुए ऊर्जावान बनने की प्रेरणा देते हुए कवयित्री कहती हैं–
“अब यहां आओ महानगर के गुलाब, मोगरा के बगीयन में
सांपो का जहर पीकर आना
अपने असली रूप गुण
अस्तित्व का दर्शन देना”[7]
दरअसल ये पंक्तियां ‘इकोफेमिनिज्म’ की झांकी भी प्रस्तुत करती हैं। अपनी कोमल रूपरेखा हो या अपेक्षित तेजमयता, स्त्रियां हर रूप में प्रकृति के स्वरूप के अनुकूल ठहरती हैं। इसका प्रमाण कवयित्री ने भी अपनी कविताओं में दिया है। लेकिन इन प्रेरणा भरे भावनाओं के विरोधाभासी दृश्यों का भी आदिवासी समाज और इनकी कविताओं में अभाव नहीं है। स्त्री को आगे बढ़ाने की, उसको सशक्त करने की कितनी ही बड़ी-बड़ी बातें भला हम क्यों न कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर स्त्री शोषण की वीभत्सता की कतई कमी नहीं है। आदिवासी समाज में फैले नशाबाजी, नशाबाज पुरुषों द्वारा अपनी स्त्रियों का शोषण जैसे अत्यंत जरूरी मुद्दों को भी कवयित्री ने उठाया है। ‘वह और मैं’ शीर्षक कविता इसका उदाहरण है–
“मेरे आदमी ने बजाया मुझे ढोल की तरह
राण निकाल रूपया
तुमने बेचा गुंजा, बेलवा, और मैंने लकड़ी
सब पैसे कहां गए
…
उसने दहाड़ा सुअर की तरह
देती क्यों नहीं रूपया?
मैं क्यों नहीं करूं नशा”[8]
इसके अलावा समय-समय पर दिकुओं (बाहरी लोगों) की ललचायी नजर और शोषण के दृश्य भी इनकी कविताओं में शामिल हैं–
“मजदूरी के लिए सावरकर जमींदार रेंजर के पास जाती
तब वे भी सूंघते फिरते अड़ोस-पड़ोस में
कोई भी आओ टिकली मारकर जाओ
हल्दी पाउडर समझते हैं मुझे”[9]
कवयित्री की ये पंक्तियां दरअसल केवल आदिवासी नारियों की जीवनदशा को नहीं उभारती, मेहनत-मजदूरी से घर चलाने की कोशिश करने वाली हर गरीब स्त्री की दशा पर प्रकाश डालती है। वंदना टेटे कहती हैं– “विस्थापन, पलायन, औद्योगिकीकरण की सबसे ज्यादा मार आदिवासी महिलाओं को ही भोगनी पड़ी। इन जगहों पर चाहे वह आदिवासी समाज की महिला हो या गैर-आदिवासी समाज की दिहाड़ी मजदूर ‘रेजा’ हो या फिर किसी गैर सरकारी विभाग में कार्यरत मध्यमवर्गीय महिला, दोनों ही समान रूप से उत्पीड़ित हैं।”[10] आदिवासियों की आर्थिक विपदापन्न दशा उस समाज की स्त्रियों पर कितना कठोर आघात करती है, इसे हम निम्न पंक्तियों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जहां अपने भूखे बच्चे के पेट में चार दाने डालने की कोशिश में मटका खरोंचती मां पर जब पति चिढ़ जाता है तब वह कहती हैं–
“क्या करूं?
बच्चा भूख के कारण रो रहा है
मटके की पेंदी से एक भी बूंद तो निकल जाए
सोचकर यह खारंखोरं खारंखोरं
मटके का पेंदी खरोंच रही।”[11]
इस प्रकार घर-परिवार, समाज-जाति के बंधनों में कितनी ही महिलाएं अपने वजूद से वंचित कर दी जाती हैं। ऐसी ही एक आदिवासी स्त्री पूछती है–
बता मां, मैं किसकी हूं
…
मेरा अधिकार क्या है
मां तुम ही बताओ मैं किसकी हूं
जहां जाती हूं वही देखती हूं
सबको लगता है मैं उनकी हूं।[12]
लेकिन दैन्यता का अहसास होना और सवाल पूछना भी तो स्त्री की सजगता का ही प्रारंभिक पर्याय है। इसका एक और प्रमाण उषाकिरण आत्राम की कविता ‘गूंगे यातनाओं का जाहिरनामा’ में मिलता है, जो कि स्त्री अस्मिता की अनन्य पहचान है–
दिमाग को तकलीफ़ न देते हुए
बैलों जैसे बोझ ढोते आए
घूमते रहे मेदी के बैल जैसे
पति को परमेश्वर मानकर पूजा व्रत करते रहे
…
ए बाई! अत्याचार का यह वृक्ष अब
जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे
यहां सूर्य शक्ति के बेल लगाएंगे
…
हम सावित्री की बेटियां बनेंगे
रणांगना दुर्गावती ललकारी बनेंगे।[13]
ग्रेस कुजूर भी अपनी एक कविता में कहती हैं–
“हे संगी
संभालो अपना तरकस…
बिरसा आबा का तीर…
मैं बनूंगी एक बार और
सिनगी दई”[14]
हालांकि उषाकिरण आत्राम ने रणांगना दुर्गावती बनने की बात कही है, लेकिन यह कविता केवल आदिवासी स्त्री की ही नहीं समस्त स्त्री जाति की परंपरागत छवि को उभारती है और उनमें अपेक्षित परिवर्तनकामी चाह की ओर भी दृष्टि आकर्षित करती है। उनकी ‘सलाह’ शीर्षक कविता भी अपने-आप में बहुत मर्मस्पर्शी है–
“बेटी तुम रोना नहीं,
रोना सुखी औरतों का काम है
हमें जन्म से ही रोने की आदत नहीं”[15]
कहते हुए कवयित्री ने आदिवासी स्त्रियों के संघर्षशील और भावनात्मक विलासिता रहित जीवन को उभारा है। तमाम दुःख-दर्द, वेदना, पीड़ाओं को सहकर चलने वाले इन स्त्रियों के पास मानो विलाप करने, रूठने, शिकायत करने की भी फुर्सत नहीं। समस्याओं का दोषारोपण भगवान पर कर जी हल्का करने की भी विलासिता नहीं। यहां ये स्त्रियां सामान्य स्त्री जाति से तनिक अलग दिखाई देती हैं। उनकी जीवन-दृष्टि एक अनन्य ऊष्मा लिये नजर आती है। तमाम दुःख-पीड़ाओं में भी बिना थके-हारे चलते जाने का यह जज्बा इन्हें सशक्त, दृढ़ रूप में प्रतिष्ठित करती है। पारंपरिक मानक भाषा जनित साहित्य और कलाओं में आदिवासी स्त्रियों की स्थिति पर बात करते हुए वंदना टेटे ने कहा है– “अस्मिता, स्वशासन, और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष करती हुई आदिवासी स्त्रियां साहित्य और फिल्मों में एक सिरे से गायब हैं।”[16] और उनका यह कथन काफी हद तक सही है।
दरअसल मानक भाषा के साहित्य में युग-युगांतर से आदिवासियों की सकारात्मक अनुपस्थिति, तथा आदिवासी स्त्रियों के वर्णित स्वरूप की ही प्रतिक्रिया है आज के आदिवासी साहित्य और उसमें वर्णित स्त्री में।
संदर्भ –
[1] आत्राम, उषाकिरण (2013). मोट्यारिन, मुक्तरंग प्रकाशन, लातूर, पृ. 29
[2] वही, पृ. 40
[3] पुतुल, निर्मला (2005). नगाड़े की तरह बजते शब्द, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ. 8
[4] आत्राम, उषाकिरण (2013). मोट्यारिन, मुक्तरंग प्रकाशन, लातूर, पृ. 81
[5] गुप्ता, रमणिका (2018). आदिवासी लेखन : एक उभरती चेतना, सेप्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 12
[6] आत्राम, उषाकिरण (2013). मोट्यारिन, मुक्तरंग प्रकाशन, लातूर,पृ. 49
[7] वही, पृ. 66
[8] वही, पृ. 116
[9] वही, पृ. 18
[10] टेटे, वंदना, आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, पृ. 75
[11] आत्राम, उषाकिरण (2013). मोट्यारिन, मुक्तरंग प्रकाशन, लातूर, पृ. 63
[12] वही, पृ. 18
[13] आत्राम, उषाकिरण (2013). मोट्यारिन, मुक्तरंग प्रकाशन, लातूर, पृ. 74
[14] आदिवासी स्वर और नई शताब्दी- सं. रमणिका गुप्ता, वाणी प्रकाशन,संस्करण : 2008, पृ. 23
[15] आत्राम, उषाकिरण (2013). मोट्यारिन, मुक्तरंग प्रकाशन, लातूर, पृ. 102
[16] टेटे, वंदना (2013). आदिवासी साहित्य : परंपरा और प्रयोजन, प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन, रांची,पृ. 72
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in