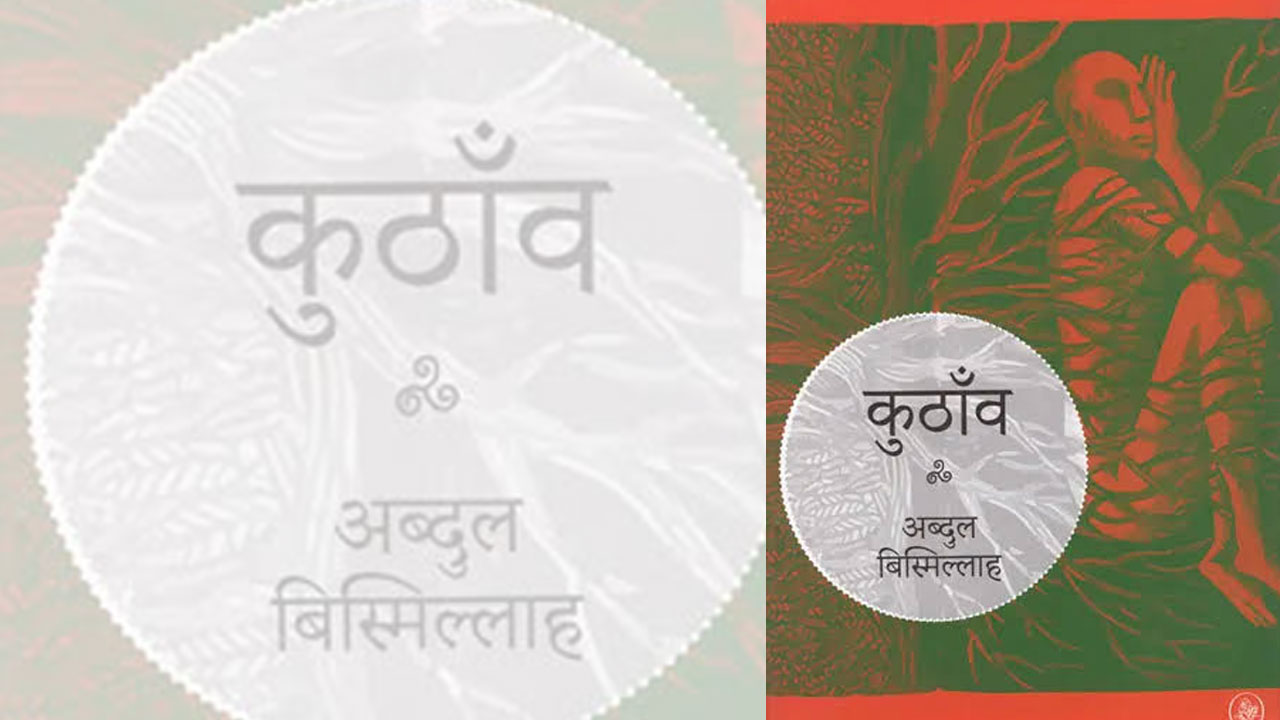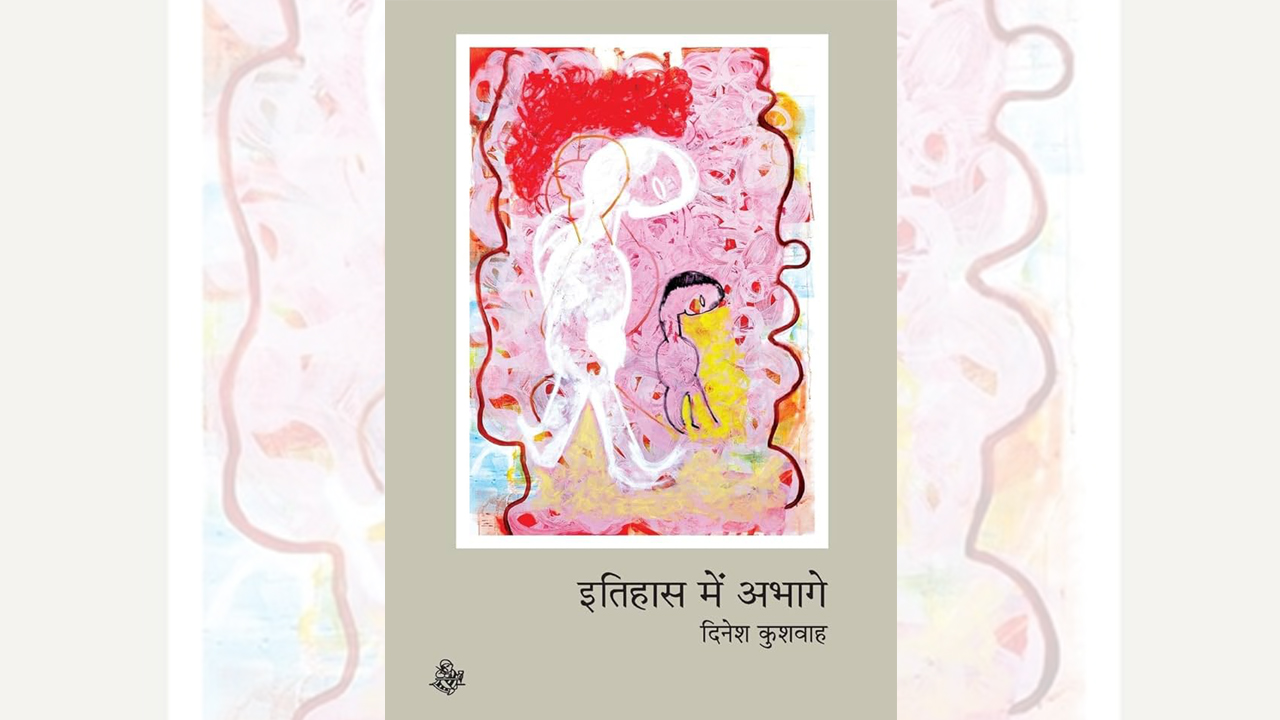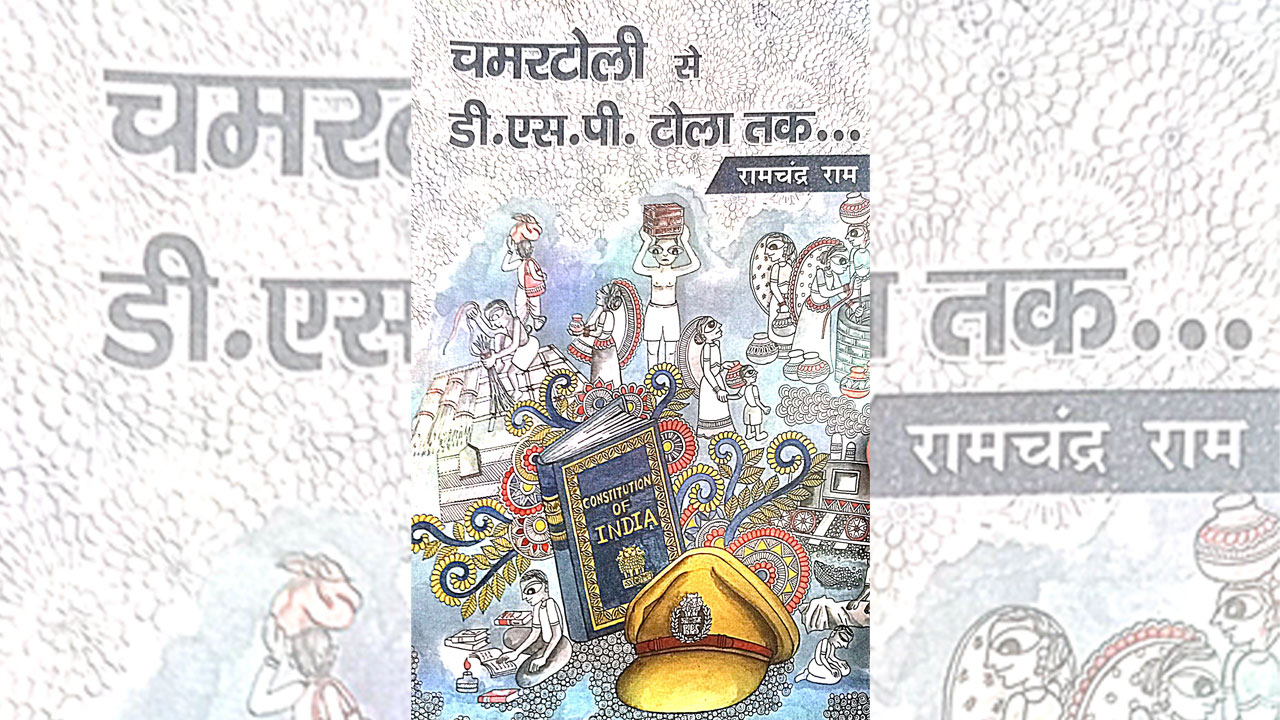महाश्वेता देवी (14 जनवरी, 1926 – 28 जुलाई, 2016) पर विशेष
सन् 1981 – नलिनी सिंह के कार्यक्रम ‘सच की परछाइयां’ के लिए पलामू के बंधुआ मज़दूरों के बारे में महाश्वेता दी से एक साक्षात्कार लेना था। कोलकाता दूरदर्शन की टीम बालीगंज स्थित उनके घर पर पहुंची। किताबों और फ़ाइलों से अंटे पड़े उनके बहुत छोटे-से कमरे में लाइट और कैमरा फिट किया गया। दीदी शायद रसोई से निकल कर आईं, एक काले पाड़ वाली मुसी-तुसी (सिलवटों वाली) सूती साड़ी पहने। मेरी ओर देख कर बोलीं– “शूधा, हमको हिंदी अच्छा नहीं आता है। चोलेगा तो?” मैंने बांग्ला में कहा– “दीदी, जैसा भी बोलेंगी, हमारी समझ में आ जाएगा।”
उन्होंने अपनी फाइलों के ढेर को एक ओर सरकाया और कुर्सी पर बैठ गईं– चलो शुरू करो। निर्देशक ने कैमरामैन को देखा, कैमरामैन ने मेरी ओर। साड़ी की ओर इशारा करते हुए मेरे कान में कुछ फुसफुसा कर कहा। मैंने दीदी से पूछा– “दीदी, साड़ी बदलेंगी?”
क्यों? उन्होंने अपनी साड़ी को देखा, पल्ला घुमा कर सामने कस लिया। फिर बोलीं– ठीक है न! कैमरामैन ने बेमन से हामी भर दी– ठीक है, चलेगा। एक दो ट्रायल शॉट हुए। पंखे की हवा से बाल कुछ उड़े हुए थे। निर्देशक ने दीदी को इशारे से कहा– “ज़रा बालों में कंघी फिरा लें।” अब तो महाश्वेता दी हत्थे से उखड़ गईं– “हमारा बात सुनेगा कि साड़ी देखेगा, हमारा चूल (बाल) देखेगा? शुरू करो।”

दस मिनट की बाइट भेजनी थी ‘सच की परछाइयां’ के लिए। साक्षात्कार 45 मिनट का हुआ। दीदी अपनी बांग्ला मिश्रित हिंदी में बेझिझक धाराप्रवाह बोलती रहीं। कोलकाता दूरदर्शन पर पूरा कार्यक्रम अलग से प्रसारित किया गया।
रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने हमारे लिए एक ख़ास कमरा खोला। बालीगंज के उनके पहले तल्ले के घर में बरामदे को फलांग कर दूसरे कमरे में जाना पड़ता था, जहां आदिवासियों के हाथों से बनाई गई टोकरी, आसन और कई हस्तशिल्प रखे थे। हमारे सामान खरीदने पर वे बेहद खुश हुईं। मना करने के बावजूद बाकायदा उन्होंने रसीद काटी और ज़बरदस्ती थमायीं।
महाश्वेता दी के घर पर ही चुन्नी कोटल से मिलना हुआ। वह मिदनापुर की लोधा जाति की पहली ग्रेजुएट लड़की, जिसने एम.एस.सी में दाखिला लिया और जिसे अंततः मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी। बूधन शवर की मौत, जिसे आत्महत्या का नाम दिया गया था, का मुकदमा भी महाश्वेता दी ने ही दायर किया। उनकी पूरी मेज़ आदिवासियों के मामले और कोर्ट-कचहरी की फाइलों से भरी पड़ी थी।

एक वाकया उन्होंने सुनाया था कि एक बार सिंहभूम के आदिवासियों के साथ वे खाने बैठीं। पत्तल पर भात के साथ नमक-मिर्च रखा था। दीदी ने पूछा– भात किस चीज़ से सानेंगे? एक आदिवासी ने जवाब दिया– “दीदी, भूख से सान लीजिये।” यह घटना महाश्वेता दी ने मेरी किताब “औरत की कहानी” के वक्तव्य के लिए बताई और कहा– “भूख से बढ़कर कोई पढ़ाई नहीं होती!” इसी शीर्षक से उनका वक्तव्य मैंने लिया। उनकी कहानी ‘रूपसी मन्ना’ के साथ, जो एक गरीब औरत के गलत के खिलाफ उठ खड़े होने और प्रतिकार की कहानी थी।
सन् 2009। कोलकाता के सॉल्ट लेक में महिलाओं का एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, जिसमें मुंबई से मेरे साथ मित्र उर्मिला पवार और अरुणा बुरटे गई थीं। मुंबई की डॉ. मंजुला जगतरामका भी उन दिनों वहीं थीं। हम चारों रोज़ सुबह एक साथ जाते और रात को लौटते। महाश्वेता दी भी कई सेशंस में वक़्ता थीं। वहां एक साथ चार-पांच जगह अलग विषयों पर चर्चा के सेशंस चल रहे थे। एक बार वे किसी और सेशन में थीं और हम दूसरे में बैठे थे। चर्चा के बीच में देखा, महाश्वेता दी पीछे से चली आ रही हैं। उनको आते देख कुछ हलचल हुई। उन्होंने उंगली मुंह पर रख इशारा किया– “चुप! चुप! चालू रखो…” और पीछे पड़े एक मूढ़े पर मेरे पास ही बैठ गईं। उन दिनों घुटने की तक़लीफ़ के कारण मैं भी ज़मीन पर नहीं बैठ सकती थी। मंच जैसा तो कुछ था नहीं, पर बोलने वाले आगे की पंक्ति में बैठे थे। अरुणा बुरटे ने इशारा किया– “दीदी को यहां भेज दो।” मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे ज़ोर से डांट दिया– “तूई चुप कोरे बोश तो!” पूरे सेशन में वे कुछ नहीं बोलीं, सिर्फ सुनती रहीं। लगभग एक घंटा बैठने के बाद चुपचाप उठीं और चली गईं। कार्यक्रम चलता रहा। ऐसी सरल और सहज थीं महाश्वेता दी।
सन् 2009 में जब कथादेश के लिए मन्नू दी पर मैंने एक अंक संपादित किया तो उन्होंने मन्नूजी पर एक संस्मरण लिख कर दिया जो अंक में भी था और फिर किताब में भी। अपनी कहानियों की एक किताब उन्होंने अपनी ‘प्रिय बांधवी मन्नू भंडारी को’ समर्पित की।
बहुत से लोग उनकी कहानियों पर बनी फिल्मों से ही उन्हें जानते हैं– जैसे कि हरनाम सिंह रवेल द्वारा निर्देशित व दिलीप कुमार व संजीव कुमार द्वारा अभिनीत ‘संघर्ष’, गोविंद निहलानी की ‘हज़ार चौरासी की मां’, कल्पना लाज़मी की (गुलज़ार लिखित) ‘रुदाली’, गौतम घोष की ‘गुड़िया’ और चित्रा पालेकर की ‘माटी माय’। उन्हें इन फिल्मों में चित्रा पालेकर द्वारा निर्देशित और नंदिता दास अभिनीत ‘माटी माय’ सबसे ज्यादा पसंद थी, जो उनकी चर्चित कहानी ‘डायन’ पर बनी थी।
महाश्वेता दी हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा, एक ताकत रहेंगीं।
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in