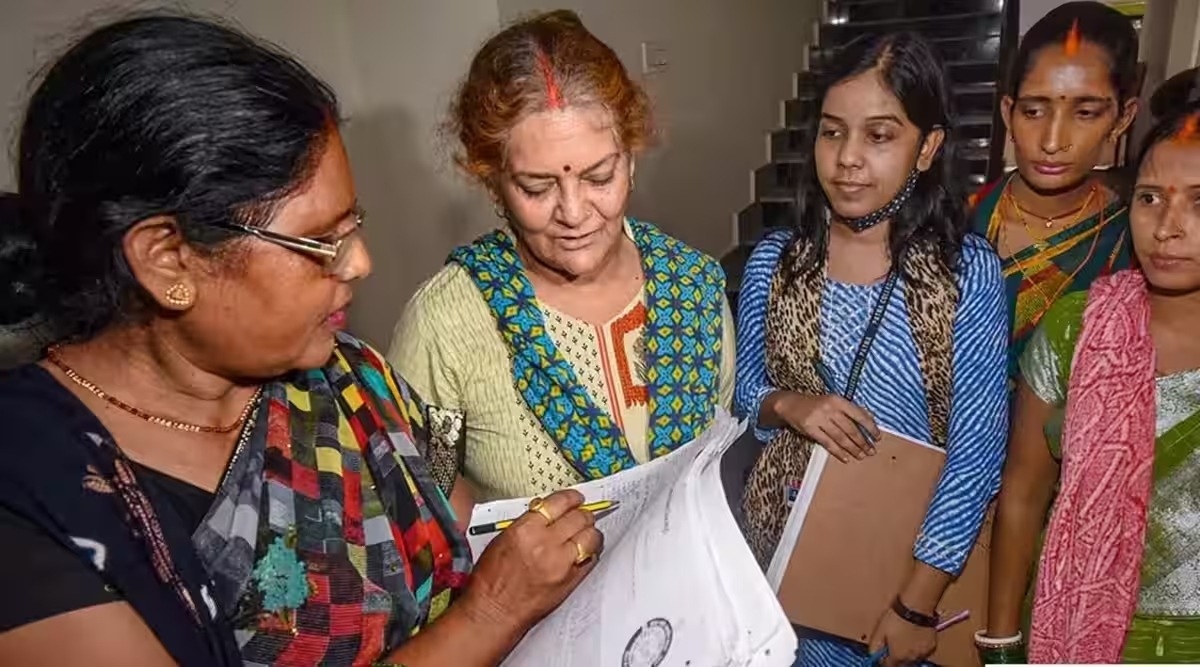विगत 3 जुलाई, 2025 को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) भवन का उद्घाटन किया। वहां बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने में पीडीए की एकता अहम् होगी। एक वाजिब सवाल यह है कि पीडीए में शामिल असंख्य हाशियाकृत समुदायों को एक करना भला कैसे संभव होगा?
दरअसल, समाजवादी पार्टी (सपा) पीडीए के फार्मूले का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के मतदाताओं में अपनी पैठ बनने के लिए कर रही है। विभिन्न पार्टियों की राजनीतिक गोलबंदी की रणनीतियों को समझने और यह जानने के लिए कि सबाल्टर्न समूह उन्हें कैसे देखते हैं, मैंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की यात्रा की। हर पार्टी अपने-अपने तरीकों से सबाल्टर्न सामाजिक समूहों को अपने झंडे तले लाने का प्रयास कर रही है। मतदाताओं, और विशेषकर दलितों और पिछड़ी जातियों, को रिझाने के लिए सपा के कार्यकर्ता उन्हें बता रहे हैं कि बसपा के प्रमुख नेता सपा में शामिल हो गए हैं। यह प्रचार उन अनेक कारणों में से एक था जिनके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को उम्मीद से ज्यादा कामयाबी हासिल हुई। मगर कुछ ऐतिहासिक कारणों के चलते यह कहा जा सकता है कि ‘पीडीए’ सपा के लिए उस तरह का कमाल नहीं कर पाएगा जैसा कि ‘बहुजन’ ने बसपा के लिए किया था।
पीडीए आज भी केवल एक चुनावी नारा बना हुआ है। सन् 2024 के आमचुनाव के दौरान पहली बार पीडीए शब्द को उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता हासिल हुई। कई बसपा नेताओं ने सपा की सदस्यता ले ली। ये नेता लंबे समय से बसपा में थे और दशकों लंबे राजनीतिक अनुभव से लैस थे। इनमें शामिल थे रामाचल राजभर, लालजी वर्मा, मिथिलेश कटियार, के.के. सचान, दद्दू प्रसाद और शाह आलम (जिन्हें गुड्डू जमाली के नाम से भी जाना जाता है)। मगर क्या केवल इससे सपा वह कर सकेगी, जो बसपा ने कर दिखाया था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें अतीत पर नज़र डालनी होगी। हमें यह देखना होगा कि सत्ता में रहने के दौरान इन दोनों पार्टियों ने समाज के वंचित वर्गों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या किया। इन दोनों पार्टियों का राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र से किस तरह का नाता है?
डॉ. आंबेडकर का जोर ‘हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाने’ और ‘विरोधाभासों से भरा जीवन जीना बंद करने’ पर था। विरोधाभासों से भरे जीवन से उनका मतलब था राजनीतिक समानता के बाद भी सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का बरक़रार रहना। उनका कहना था कि राजनीतिक लोकतंत्र का लक्ष्य, सामाजिक लोकतंत्र के उद्देश्यों को हासिल करना होना चाहिए। बसपा की स्थापना ने उत्तर भारत में एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। पार्टी का मुख्य लक्ष्य सदियों से दमित बहुजनों – एससी, एसटी, ओबीसी और धर्मांतरित अल्पसंख्यकों – को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलवाकर भारतीय समाज में समानता स्थापित करना।

बसपा के संस्थापक कांशीराम का दर्शन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक सिद्धातों पर आधारित था। बसपा से पहले उन्होंने कई सामाजिक संगठनों की स्थापना की थी। सन् 1971 में उन्होंने ऑल इंडिया एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी एम्प्लाइज एसोसिएशन का गठन किया। 1978 में इस संस्था का नाम बदलकर ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन (बामसेफ) कर दिया गया। उन्होंने 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति (डीएस-4) स्थापित की। अंततः 1984 में उन्होंने बसपा नाम से एक राजनीतिक दल स्थापित किया। इस प्रकार कांशीराम का जोर संवैधानिक सिद्धांतों को धरती पर उतारने पर था और बसपा मूलतः सामाजिक लोकतंत्रवादी रही।
दूसरी ओर, यह बहस का विषय है कि पीडीए ने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में किस हद तक योगदान दिया है। पीडीए शब्द का प्रयोग पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया और तब से यह लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। मगर यह शब्द सपा की मूलभूत प्रकृति को अभिव्यक्त नहीं करता। बेशक 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले ने काम किया। उत्तर प्रदेश में सपा को 37 सीटें मिलीं और भाजपा को 33। सन् 2019 के चुनाव में सपा केवल पांच सीटें हासिल कर सकी थी, वहीं भाजपा ने 62 सीटें जीती थीं। सपा उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है।
2024 के लोकसभा चुनाव में बहुसंख्य दलितों और पिछड़ों ने सपा को वोट दिया था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बसपा के अनेक असंतुष्ट नेता चुनाव के ठीक पहले सपा में शामिल हो गए थे। इसका एक कारण यह था कि मायावती के नेतृत्व में बसपा अत्यंत कमज़ोर दिखलाई दे रही थी। दूसरे, भाजपा नेताओं ने यह घोषित कर दिया था कि अगर उनके गठबंधन को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत मिला तो वे संविधान में बदलाव करेंगे। इस कारण दलित और पिछड़ी जातियों के मतदाताओं, जिन्हें बसपा ने संविधान के महत्व से अवगत करवा दिया था, ने इस खतरे को देखते हुए सपा को वोट दिया।
इन मतदाताओं ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए सपा की सामाजिक न्याय-विरोधी नीतियों को नज़रंदाज़ किया। ये नीतियां 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में सपा के शासनकाल में सबके सामने आ गईं थीं। सपा सरकार ने अति-निर्धन बेघर शहरवासियों के लिए बनाई गई कांशीराम शहरी आवास योजना और लड़कियों के लिए बनाई गई सावित्रीबाई फुले बालिका मदद योजना की नाम बदल दिए। उसने सरकारी सेवाओं में एससी-एसटी समुदायों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का विरोध किया। अलग-अलग मंचों से पीडीए का नारा बार-बार बुलंद करने के बावजूद, अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल की सामाजिक न्याय-विरोधी अपनी नीतियों के लिए कभी भी सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगी।
डॉ. आंबेडकर के अनुसार प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय एक क्रांति था और उसके बाद हिंदू धर्म का पुनरोदय एक प्रतिक्रांति। अगर हम इसे उत्तर प्रदेश पर लागू करें तो बसपा का 2007-12 का शासनकाल क्रांति था और सपा का 2012-17 का शासनकाल, प्रतिक्रांति। सपा के शासनकाल के विपरीत, बसपा अपने शासनकाल में बहुजन के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसके बरक्स सपा के अधिकांश नेता और कार्यकर्ता जाति-व्यवस्था का पालन करते हैं, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के समर्थक हैं और ऊंची जातियों के अपने मतदाताओं को नाराज़ करने से परहेज़ रखते हैं। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में भूस्वामी ओबीसी और भूमिहीन या छोटी जोतों के मालिक अति-पिछड़ी जातियों/दलितों के बीच टकराव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। सपा के अधिकांश बड़े नेता और कार्यकर्ता भूस्वामी ओबीसी जातियों से हैं और उन्होंने इस खाई को पाटने के लिए कुछ नहीं किया है। इस तरह पीडीए सिर्फ एक खोखला नारा भर बन कर रह गया है। आज की स्थिति में सपा ज़मीनी स्तर पर इस तरह का गठजोड़ बनाने में सक्षम नहीं है।
नतीजा यह कि आने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें संविधान मुद्दा नहीं रहने वाला है, में समाजवादी पार्टी के दलितों व अति-पिछड़ी जातियों का समर्थन खो बैठने की संभावना है। पीडीए की अवधारणा बहुजन की अवधारणा का स्थान नहीं ले सकती जब तक कि वह सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित न हो।
(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया)
फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in