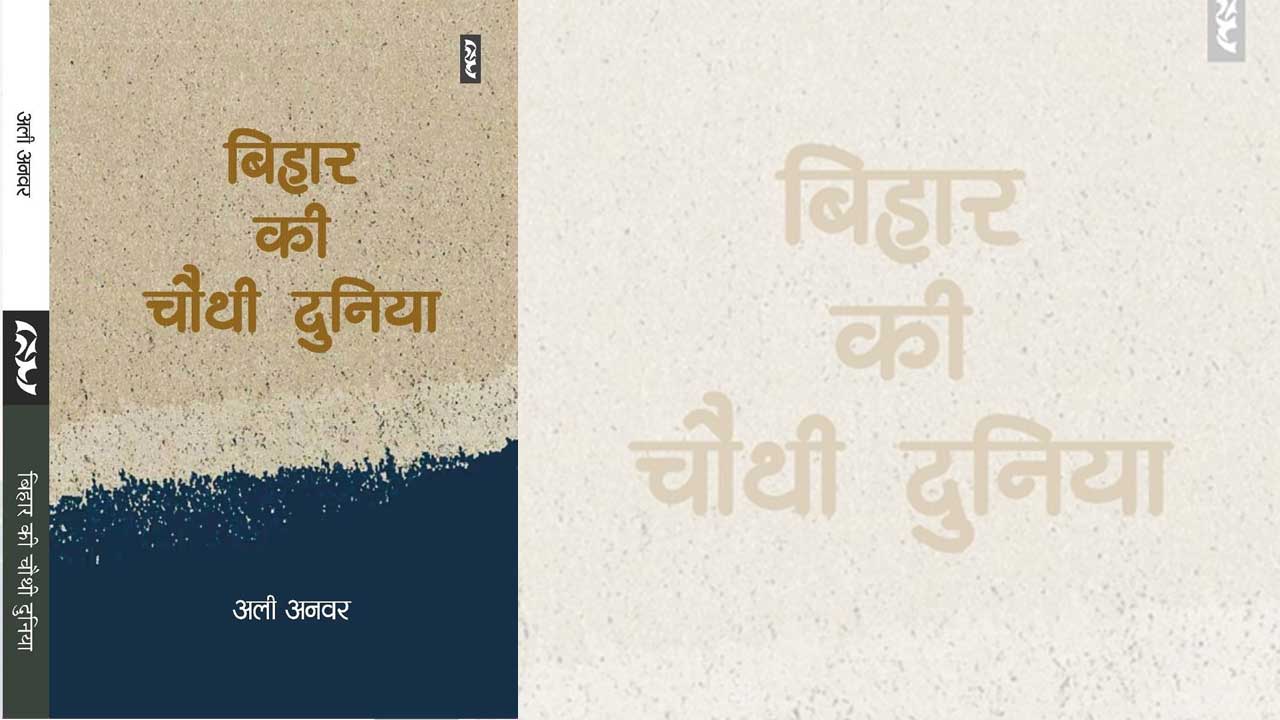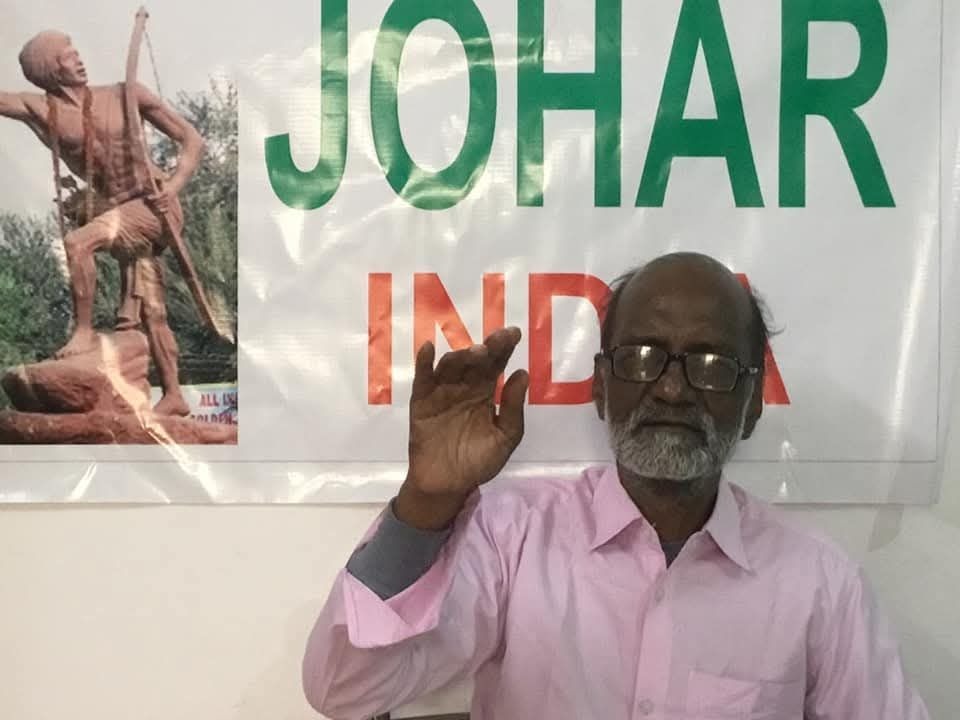वर्तमान समय यह प्रश्न पूछ रहा है कि “जाति-व्यवस्था का अंत हो अथवा जाति-व्यवस्था फिर से अपने स्वर्ण युग की तरफ लौटे?” उत्तर देने की जिम्मेदारी इस देश के वामपंथी, समाजवादी, प्रगतिशील व फुलेवादी-आंबेडकरवादी आदि लोगों की है। वामपंथी पार्टियों व संगठनों ने जाति-व्यवस्था की चुनौती को कभी स्वीकार ही नहीं किया। वे हमेशा जातिअंतक खेमे से सुरक्षित दूरी ही रखते आए हैं, इसलिए उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी वे कभी पूरी कर ही नहीं पाएंगे।
समाजवादियों में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने जातिअंतक खेमे में बड़ी भूमिका निभाई। नेहरू ने 1955 में कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल कर ओबीसी के नेतृत्व में संभावित जातिअंतक लड़ाई को दबा देने का प्रयास किया। डॉ. लोहिया ने तत्कालीन दिग्गज ओबीसी नेता आर.एल. चंदापुरी के साथ गठबंधन करके वर्ग संघर्ष व जातिअंतक संघर्ष की एकजुटता का सैद्धांतिक पक्ष सफलतापूर्वक सामने रखा। ‘पिछड़ा पावे सौ में साठ’ यह नारा जातिअंतक लड़ाई का बिगुल ही था। इस संघर्ष से ही 1967 में पहली राजनीतिक लड़ाई सफल हो सकी। उत्तर प्रदेश में पहले ओबीसी मुख्यमंत्री राम नरेश यादव बने। ऐसे ही बिहार में 1960 और 1970 में सतीश प्रसाद सिंह, बी.पी. मंडल, दारोगा प्रसाद राय और कर्पूरी ठाकुर ओबीसी मुख्यमंत्री हुए। कहना अतिरेक नहीं कि इसी लड़ाई से आगे चलकर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेता उभरे, जिन्होंने मंडल युग को एक वास्तविकता बनाकर देश की राजनीति को ‘ओबीसी केंद्रित’ किया।
हालांकि, इस देश के वामपंथी, समाजवादी और फुले-आंबेडकरवादी यह नहीं जानते कि आरएसएस-भाजपा के हाथों में सबसे बड़ा हथियार ‘सांस्कृतिक संघर्ष’ है। जब इस हथियार का उपयोग किया जाता है तब बड़े-बड़े सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ही मंडल आयोग का युग सामने आया, ब्राह्मणवादी प्रति-क्रांतिकारी खेमे ने इसका विरोध किया और राम मंदिर के नाम पर एक सांस्कृतिक संघर्ष पैदा किया। समाजवादी ओबीसी नेता इस सांस्कृतिक संघर्ष का सामना नहीं कर सके, क्योंकि ये ओबीसी नेता फुले-आंबेडकरवादी नही थे, लोहियावादी थे और लोहिया स्वयं राम-कृष्ण के भक्त थे।
यह अतिश्योक्ति नहीं कि केवल सामाजिक व राजनीतिक संघर्षों से अवतरित मंडल युग, बिना सांस्कृतिक संघर्ष के कारण कमजोर पिलर पर खड़ा था, जिसका भरपूर फायदा ब्राह्मणी खेमे ने उठाया और 2014 में उनकी प्रतिक्रांति कामयाब हो गई। दरअसल हुआ यह कि मंडल आयोग के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के कारण, देश भर में ओबीसी सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागृत हो गए थे। ओबीसी समुदाय स्वतंत्र रूप से एक वोट बैंक बन चुका था। संघ-भाजपा ने प्रधानमंत्री के पद के लिए मोदी नामक ‘ओबीसी मुखौटा’ लगाकर इस वोट बैंक को लूट लिया, और 2024 में पेशवा की अखिल भारतीय ब्राह्मणी प्रतिक्रांति सफल हो गई। ब्राह्मणी खेमे ने राम मंदिर के नाम पर सांस्कृतिक हथियार चलाया और मंडल युग के सामाजिक-राजकीय आंदोलन की नींव कमजोर कर दी।
यह याद रखा जाना चाहिए कि सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष जितनी जल्दी सफल होते हैं, उतनी ही जल्दी वे असफल भी हो जाते हैं। जबकि सांस्कृतिक संघर्ष लंबा होता है, अपने खेमे को मजबूत बनाता है एवं सामाजिक-राजनीतिक लड़ाई का मार्ग सुगम बनाता है।
उत्तर भारत में इस प्रकार का सांस्कृतिक संघर्ष खड़ा करने की कोशिश पहले अर्जक संघ बनाकर महामना रामस्वरूप वर्मा ने की और बाद में 1980 के दशक में मान्यवर कांशीराम ने की। ये दोनों खुद को फुले-आंबेडकरवादी मानते थे। ब्राह्मणवादी प्रतीकों के खिलाफ लड़ने के लिए तात्यासाहब महात्मा फुले ने अपनी किताबों – ‘गुलामगिरी’ और ‘किसानों का कोड़ा’ – में बलीराजा, शंबुक और एकलव्य जैसे महान प्रतीक दिए। तात्यासाहेब के इसी अब्राह्मणी सिद्धांत को विकसित करते हुए बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर ने ‘हिंदू धर्म की पहेलियां’ नामक एक किताब की रचना की और अब्राह्मणी सांस्कृतिक संघर्ष को चरम पर पहुंचाया।

हालांकि कांशीराम चाहते तो लालकृष्ण आडवाणी की राममंदिर शिलान्यास यात्रा (1989) और रामरथ यात्रा (1990) के विरोध में ऐसे अब्राह्मणी प्रतीकों का जुलूस निकाल सकते थे, जिससे राम के नाम पर बहुजनों के एकतरफा होने को कुछ हद तक रोका जा सकता था। उस वक्त कांशीराम की पार्टी (बसपा) उत्तर भारत में मजबूत स्थिति में थी।
कांशीराम स्वयं देशभर में काडर कैंप संचालित करते थे। मैं स्वयं इसका हिस्सा रहा हूं। इन्हीं काडर कैंपों के जरिए बहुजन समाज पार्टी बन रही थी। संघ-भाजपा ने राममंदिर के लिए आंदोलन 1984 से ही जोर-शोर से शुरू कर दिया था। उसी वक्त कांशीराम के काडर कैंप भी जोर-शोर से चल रहे थे। लेकीन कांशीराम द्वारा संचालित काडर कैंपों में सिर्फ 15 बनाम 85, आरक्षण, वर्ण-जाति की रचना और ब्राह्मणविरोध इन्ही मुद्दों पर विचार रखे जाते थे। जबकि संघ-भाजपा के राममंदिर के मुद्दे को लेकर कांशीराम के काडर कैंपों में शंबुक, एकलव्य, कर्ण आदि अब्राह्मणी प्रतीकों पर बात की जानी चाहिए थी, जो कभी नहीं हुआ। अगर कांशीराम सच्चे फुले-आंबेडकरवादी होते, तो वे राम के खिलाफ शंबुक का क्रांतिकारी संघर्ष जरूर रखते और आडवाणी की रामनामी यात्राओं के खिलाफ शंबुक, एकलव्य की यात्राएं व जुलूस जरूर निकालते। सिर्फ दो-तीन जातियों का गठजोड़ तैयार करके राजनीतिक सत्ता हासिल करना ही उनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणवादी भाजपा से एकतरफा दोस्ती1 भी की, जिसका परिणाम आज हम बसपा को खत्म होने के रूप में देख सकते हैं।
उस समय (1989 में) महाराष्ट्र के धुले-नंदुरबार जिले में इस तरह के ‘ब्राह्मणवाद विरोधी सांस्कृतिक संघर्ष’ को खड़ा करने की पूरी कोशिश की गई थी। इसमें मैं भी शामिल था। तब सुप्रसिद्ध भारतविद रहे कॉमरेड शरद पाटील2 की सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सीता, शंबुक, ताड़का, शूर्पणखा और एकलव्य के प्रतीकों का एक जुलूस धुले शहर में निकाला गया था। इस जुलूस में, हमने राम, कृष्ण, द्रोणाचार्य आदि जैसे ब्राह्मणवादी नायकों के खिलाफ मुर्दाबाद और बहुजन नायकों के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसी जुलूस का अनुकरण करते हुए अगर उस दौरान कांशीराम, आठवले, प्रकाश आंबेडकर, लालू-मुलायम, छगन भुजबल जैसे राष्ट्रीय दलित-ओबीसी नेताओं ने देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया होता, तो वर्ष 2014 में आरएसएस-भाजपा की ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति सफल नहीं होती और इन नेताओं पर संघ-भाजपा का गुलाम बनने की नौबत नहीं आती।
सांस्कृतिक संघर्ष के बिना की गई कोई भी राजनीति आपको ‘किसी की पूंछ या गुलाम’ बना ही देती है। कांशीराम की बसपा, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा की ‘दलित प्रकोष्ठ’ या ‘बी’ टीम बनकर रह गई है। महादेव जनकर की तथाकथित ओबीसी पार्टी (राष्ट्रीय समाज पक्ष) को हमेशा भाजपा की पूंछ के रूप में देखा गया है। छगन भुजबल, जिन्हें कभी ‘ओबीसी का पैंथर’ के रूप में जाना जाता था, आज देवेंद्र फड़णवीस-अजित पवार के गोठे (दालान) की ‘बकरी’ बनकर रह गए हैं। और यह सब केवल ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक संघर्ष का विरोध नहीं करने की वजह से हो रहा है।
जाति-व्यवस्था को खत्म करने के लिए सांस्कृतिक संघर्ष का सिद्धांत सबसे पहले रखा जोतीराव फुले ने। वे इसे अमल में भी लाए। ‘बलीराजा के पतन के बाद का इस देश का इतिहास ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संघर्ष का इतिहास है’3, यह उन्होंने द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का विवरण देकर सिद्ध भी किया। उसके लिए उन्होंने दशावतारों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। आर्य-ब्राह्मणों के सेनापति वामन के खिलाफ बलीराजा के क्रांतिकारी युद्ध का इतिहास उन्होंने लिखा है। राम के विरोध में शंबूक-रावण के अलावा द्रोणाचार्य, परशुराम, कृष्ण के विरोध में कर्ण-एकलव्य के क्रांतिकारी संघर्ष को उजागर किया। भविष्य में कोई ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज को ‘गाय-ब्राह्मणों का राजा’ बताकर उनका ब्राह्मणीकरण कर सकता है, यह सोचकर तात्यासाहब ने शिवाजी राजा को ‘शूद्रातिशूद्रों का राजा’ बनाया और उसके लिए 35 पन्नों का ऐतिहासिक पोवाड़ा (गीत) लिखा। भविष्य में कोई ब्राह्मण भाद्रपद महीने में मनाए जानेवाले बली महोत्सव पितृपक्ष का महत्व कम करने के लिए दस दिनों का गणपती महोत्सव शुरू कर सकता है, यह जानते हुए तात्यासाहेब ने पहले ही भाद्रपद महीने में पंद्रह दिवसीय पितृपक्ष-श्राद्धपक्ष का क्रांतिकारी इतिहास लिखकर बहुजनों के सामने रखा है।4 यह सब तात्यासाहब ने इसलिए किया ताकि ब्राह्मण उसे भी बदलकर ‘बहुजनों का शर्मनाक इतिहास’ न बना दें। इस तरह से तात्यासाहब ने इस सांस्कृतिक संघर्ष की नींव रखी।
तात्यासाहब की अपेक्षा इतनी ही थी कि बहुजन जनता इन त्यौहार-महोत्सव और रूढ़ि-परंपराओं के संबंध में वर्ण-जाति विरोधी इतिहास से प्रेरणा ले और ब्राह्मणवाद के खिलाफ उसके खात्मे तक लड़ाई जारी रखे। लेकिन फुले-आंबेडकर के अनुयायी उनके आरक्षण सिद्धांत से परे कुछ भी नहीं देखते हैं। आमजनों में भी यही मान्यता है कि आरक्षण से अच्छी नौकरी और उसके उपरांत सुंदर पत्नी मिलती है। नौकरी, सुंदर पत्नी, कार और बंगला से परे तात्यासाहेब और बाबासाहेब ने बहुत कुछ कहा है। बेशक, आमजनों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके दलित-ओबीसी नेताओं ने फुले-आंबेडकरवाद को ब्राह्मणों और मराठों के यहां गिरवी रख दिया है। ब्राह्मणी खेमा इस तरह के एकतरफा सांस्कृतिक अभियान की वजह से लगातार विजयी हो रही है और दलित-बहुजन जनता सांस्कृतिक संघर्ष के अभाव में हार का शर्मनाक जीवन जी रही है।
तमिलनाडु इसका अपवाद है, जहां रामासामी पेरियार के नेतृत्व में 1925 में शुरू हुआ गैर-ब्राह्मणी सांस्कृतिक आंदोलन 1967 में राजनीतिक क्रांति के रूप में परिवर्तित हुआ। लेकिन पहले यह एक सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। वर्ष 1916 में डॉ. सी. नतेशा मुदलियार, पी. थेगाराया चेट्टी व टी.एम. नायर ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। ये तीनों संस्थापक ब्राह्मणेतर (ओबीसी) जाति से थे। पार्टी का मुख्य एजेंडा था– सभी गैर-ब्राह्मण जाति-धर्मों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण प्राप्त करना। आदिवासी, अछूत, गैर-ब्राह्मण जातियां (यानी आज की ओबीसी जातियां), मुस्लिम, ईसाई, लिंगायत, आदि-द्रविड़ – यह सभी गैर-ब्राह्मण जाति के और गैर-ब्राह्मण धर्म के हैं। वर्ष 1919 में मांटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार प्रांतीय विधानसभा की स्थापना के लिए 1920 में चुनाव हुए। जस्टिस पार्टी ने पहला आम चुनाव जीता और मद्रास प्रांत में पहली सरकार बनाई। देश के आधुनिक इतिहास में पहली ओबीसी-बहुजन सरकार सत्ता में आई। अकाराम सुब्बारायलू रेड्डी पहले ओबीसी मुख्यमंत्री (मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री) बने। जैसे ही सरकार बनी, जस्टिस पार्टी ने 16 सितंबर, 1921 को आरक्षण अधिनियम पारित किया। अधिनियम के अनुसार, गैर-ब्राह्मण जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में सभी उच्च पदों को सभी जातियों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। हालांकि, वहां की अदालत ने इस कानून पर तुरंत स्थगन आदेश दे दिया। अमल में लाए जाने के पहले ही ब्राह्मणों ने इस कानून को रद्द कराने में सफलता हासिल कर ली। इस आदेश के पीछे कांग्रेस के ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, यह मालूम होते ही रामासामी पेरियार गुस्सा हो गए। उस समय वे कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे। उन्हें दक्षिण का महात्मा गांधी माना जाता था। पेरियार कांग्रेस के हर सम्मेलन में आरक्षण प्रस्ताव पेश करते थे। लेकिन हर सम्मेलन में उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता था। हालांकि, 1925 में जब वे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गए, तब आरक्षण संबंधी प्रस्ताव के साथ अपना इस्तीफा भी ले गए। उन्होंने कहा कि या तो आरक्षण प्रस्ताव स्वीकार करें वरना मै इस्तीफा दें रहा हूं। कांग्रेस सम्मेलन में हमेशा की तरह पेरियार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। रामासामी पेरियार ने मंच पर ही अपना इस्तीफा दे दिया।
उस वक्त ओबीसी-बहुजनों की जस्टिस पार्टी सत्ता में थी। फिर भी ब्राह्मण आरक्षण अधिनियम पर रोक लगवाने में सफल हो गये थे। पेरियार जान गए कि सिर्फ राजनीतिक सत्ता हासिल करने से कुछ नहीं होगा। अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व पूर्ण रूप से उखाड़कर हमेशा के लिए नष्ट करना है तो उनके खिलाफ सांस्कृतिक युद्ध लड़ना पड़ेगा। और 1925 में ही उन्होंने आत्म-सम्मान आंदोलन शुरू किया। यह उनके द्वारा सांस्कृतिक युद्ध की घोषणा थी। पेरियार ने आरक्षण अधिनियम के समर्थन में पूरे मद्रास प्रांत में सामूहिक रैलियों का आयोजन किया। इन रैलियों में पेरियार ने ब्राह्मणवादी धर्म, ब्राह्मणवादी संस्कृति और ब्राह्मण देवी-देवताओं के खिलाफ विचार रखे। बाद में ब्राह्मणों के आदर्श राम के खिलाफ तमिल में ‘रामायण पारदींगल’ नामक किताब लिखकर रावण को नायक बताया और लोगों को ब्राह्मणों के षड्यंत्र से दूर रहने के लिए कहा। 1959 में उनकी यह किताब ‘दी रामायणा : अ ट्रू रीडिंग’ नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, जिसे वर्ष 1968 में उत्तर भारत में पेरियार ललई सिंह ने हिंदी में ‘सच्ची रामायण’ शीर्षक से प्रकाशित किया।
खैर, रैलियों का परिणाम यह हुआ कि पेरियार को भारी जन समर्थन मिला और 1927 में आरक्षण अधिनियम का अमल शुरू हो गया। इस कानून की वजह से सभी जाति-धर्म के लोगों को आरक्षण मिलने लगा। यह कानून स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने (1950) तक अमल में रहा।
सनद रहे कि जस्टिस पार्टी केवल एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था। धर्म, संस्कृति, जाति-व्यवस्था आदि के सवाल पर उसकी कोई नीति नहीं थी। अगर आप सामाजिक आंदोलन करेंगे तो आरक्षण आदि अधिकार ही मिलेंगे। यदि आप राजनीतिक आंदोलन करेंगे तो राजनीतिक सत्ता मिलेगी। अर्थात आपको केवल मंत्रियों-मुख्यमंत्रियों के पद मिलेंगे। मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में लिए गए आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय ब्राह्मणों द्वारा तुरंत स्थगित कर दिए जाते हैं और सत्ता में बैठे दलित-ओबीसी हाथ मलते रह जाते हैं।
लेकिन अगर आप सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के साथ-साथ सांस्कृतिक आंदोलन को भी करते हैं, तो पूर्ण सत्ता आपके हाथ में आती है। जब जस्टिस पार्टी सत्ता में आई, तो 1921 में आरक्षण अधिनियम लागू किया गया, लेकिन ब्राह्मणों ने आरक्षण अधिनियम को उसी क्षण से निरस्त कर दिया। मतलब कानून अमल में आया ही नहीं। यह अमल में तब आया जब पेरियार ने 1925 में ब्राह्मणवादी कांग्रेस को लात मारते हुए, ब्राह्मणवादी संस्कृति के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। केवल दो साल के भीतर ही आरक्षण कानून लागू हो गया और सबको आरक्षण मिलने लगा। हालांकि, इसके बावजूद जस्टिस पार्टी सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर ही बनी रही। परिणामस्वरूप, 1937 में जस्टिस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और ब्राह्मणवादी कांग्रेस सत्ता में आई। पेरियार के ब्राह्मण विरोधी आत्म-सम्मान आंदोलन ने कांग्रेस को मद्रास प्रांत में ओबीसी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। के. कामराज उनमें से एक थे। के. कामराज, करुणानिधि-स्टालिन की तरह, नाई-सेन, धोबी-परिट, लोहार, बढ़ई आदि पेशा वाली जाति अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते थे।
मौजूदा संविधान 26 जनवरी, 1950 को अमल में आया। इसके साथ ही नया आरक्षण कानून भी अमल में आ गया। तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने फिर से आरक्षण कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने हमेशा की तरह इस आरक्षण कानून को तुरंत खारिज कर दिया। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए आरक्षण को तुरंत स्थगित करने का आदेश दिया। अदालत के इस आदेश के कारण पूरे देश के दलितों व आदिवासियों को मिलनेवाला आरक्षण बंद हो गया और तमिलनाडु में विशेष प्रावधान के तहत ओबीसी को मिलनेवाला आरक्षण भी। उस वक्त सिर्फ तमिलनाडु की ओबीसी जनता ने पेरियार के नेतृत्व में आक्रमक आंदोलन शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ गैर-ब्राह्मण (ओबीसी) जातियों का आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि केंद्र में सत्तासीन नेहरू की सरकार को इस ओबीसी आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। पेरियार ने केंद्र सरकार से संसद का सत्र बुलाकर संविधान संशोधन करने को कहा। तदुपरांत पहला संविधान संशोधन किया गया और आरक्षण को लागू किया गया। दुनिया के इतिहास में काले लोगों के आंदोलन ‘ब्लैक लाइव्स मैटर्स’ ने 2020 में जिस तरह से अमेरिका जैसी महाशक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को घुटने टेककर माफी मांगने को मजबूर कर दिया था, उसी तरह 1950 के दशक में तमिलनाडु के ओबीसी का आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को घुटनों पर ला दिया था।
पेरियार के विचारों पर आधारित द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) पार्टी की स्थापना 1948 में हुई थी। बीस साल के बाद यह पार्टी 1967 में सत्ता में आई। आजाद भारत के तमिलनाडु में कांग्रेस के के. कामराज के बाद दूसरे ओबीसी मुख्यमंत्री अन्नादुरई हुए। तब से वहां आरक्षण की सीमा बढ़ती गई और 69 प्रतिशत तक पहुंच गई। आरक्षण टिकाए रखने के लिए 1951 में पहला संविधान संशोधन करवाना व मिले हुए आरक्षण को जयललिता के मुख्यमंत्रित्व काल में केंद्र में सत्तासीन नरसिम्हा राव सरकार पर दबाव डालर नौंवी अनुसूची में डलवाना, ब्राह्मण पुजारियों को कानून बनाकर हिंदू मंदिरों से निष्कासित करना आदि ऐसी कई क्रांतिकारी घटनाएं केवल तमिलनाडु में ही संभव हो सकती है। वजह यह कि वहां की जनता ओबीसी के नेतृत्व में लंबे समय से अब्राह्मणी सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रही थी और आज भी लड़ रही है। उनके इसी संघर्ष की वजह से तमिलनाडु ‘अब्राह्मणी राष्ट्र’ के रूप में सिद्ध हुआ है।
पेरियार ने तात्यासाहब महात्मा जोतीराव फुले के ‘फुलेवाद’ को निरीश्वरवाद की झालर लगाकर ब्राह्मणी-अब्राह्मणीवाद को विकसित रूप में प्रस्तुत किया।
महाराष्ट्र को ‘अब्राह्मणी राष्ट्र’ बनाने में फुले के अनुयायी सफल नहीं हो सके, क्योंकि वे ऐन लड़ाई के वक्त गांधीवाद के झांसे में आकर कांग्रेसी ब्राह्मणवाद के शरण में चले गए। लेकिन उसी कालखंड में पेरियार ब्राह्मणवादी कांग्रेस को लात मारकर बाहर आते हैं और ब्राह्मणी संस्कृति के विरोध में युद्ध छेड़ देते हैं। परिणामस्वरूप तमिलनाडु (मद्रास) ‘अब्राह्मणी राष्ट्र’ बनता है।
ब्राह्मणों का पहला व अंतिम अड्डा मंदिर होता है। इस अड्डे से ब्राह्मणों को निष्कासित करनेवाला तमिलनाडु एकमात्र राज्य है, इसी एक सबूत के आधार पर ही यह सिद्ध होता है कि तमिलनाडु ‘अब्राह्मणी राष्ट्र’ है।
लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं कि तमिलनाडु में जाति-व्यवस्था नष्ट हो चुकी है। भारत में जाति व्यवस्था को कायम रखकर अकेले तमिलनाडु से जाति-व्यवस्था नष्ट करना संभव ही नहीं है। उसके लिए तमिलनाडु के ओबीसी नेतृत्व को देश स्तर पर जातिअंतक लड़ाई का नेतृत्व करना होगा। तमिलनाडु के ओबीसी नेतृत्व को देशव्यापी कृति कार्यक्रम ताबड़तोड़ हाथ में लेना होगा। यथा–
- उत्तर भारत में ब्राह्मणवाद ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। दक्षिण के राज्यों में अभी भी ‘अब्राह्मणवाद’ थोड़ा कम ज्यादा मात्रा में जीवित है। उसे फिर से पूरी ताकत से खड़ा करने के लिए तमिलनाडु के ओबीसी नेतृत्व में सीता, शंबूक, रावण व बलीराजा, एकलव्य गौरव यात्रा निकलनी चाहिए।
- तमिलनाडु में पेरियार के विचारों-कार्यों पर आधारित पुस्तकों का देश की सभी भाषाओं में अनुवाद करके सभी राज्यों में भेजना चाहिए।
- हम लोग 27 वर्षों से ‘फुले-अंबेडकर विद्यापीठ’ स्थापित करके महाराष्ट्र में प्रगतिशील पुस्तकों पर परीक्षा का आयोजन करते हैं। उसी तरह ‘पेरियार फुले अंबेडकर विद्यापीठ’ की स्थापना करके देश भर में विभिन्न भाषाओं में राज्यस्तरीय परीक्षा आयोजित हो, तो युवा पीढ़ी को पेरियार के विचारों व कार्यों की जानकारी होगी।
- प्रत्येक राज्य में कुछ ओबीसी कार्यकर्ता प्रामाणिक रूप से कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु सरकार प्रोत्साहित करे।
- प्रत्येक राज्य के ऐसे प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर देश स्तर पर ओबीसी के नेतृत्व में नई ‘अब्राह्मणी पार्टी’ बनाई जा सकती है।
- हिंदी भाषा के अभाव में तमिलनाडु देश से कटा हुआ है, अब हिंदी भाषा का सदुपयोग करते हुए तमिलनाडु देश से खुद को जोड़े और जातिअंतक अब्राह्मणी क्रांति करे।
(यह आलेख प्रो. श्रावण देवरे द्वारा 1 मई, 2022 को चेन्नई में दिए गए संबोधन का विस्तृत रूप है, जिसे उन्होंने विषय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर विस्तार दिया है।)
(संपादन : राजन/नवल/अनिल)