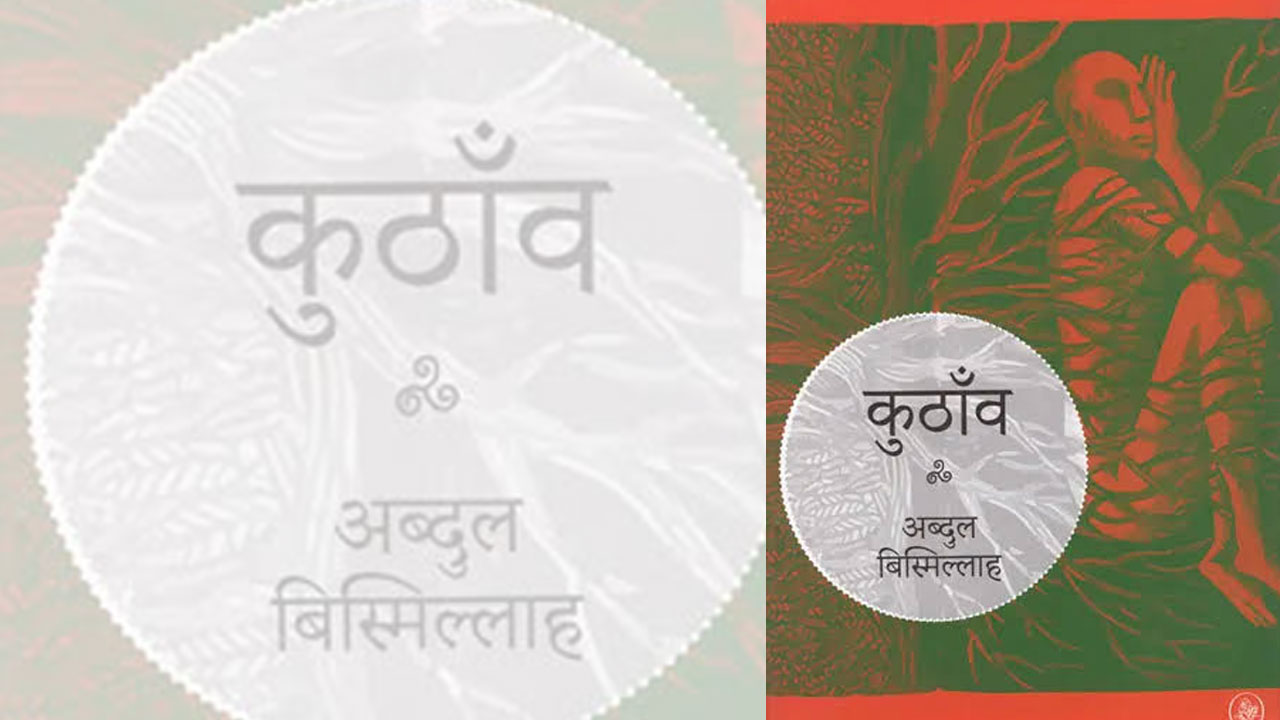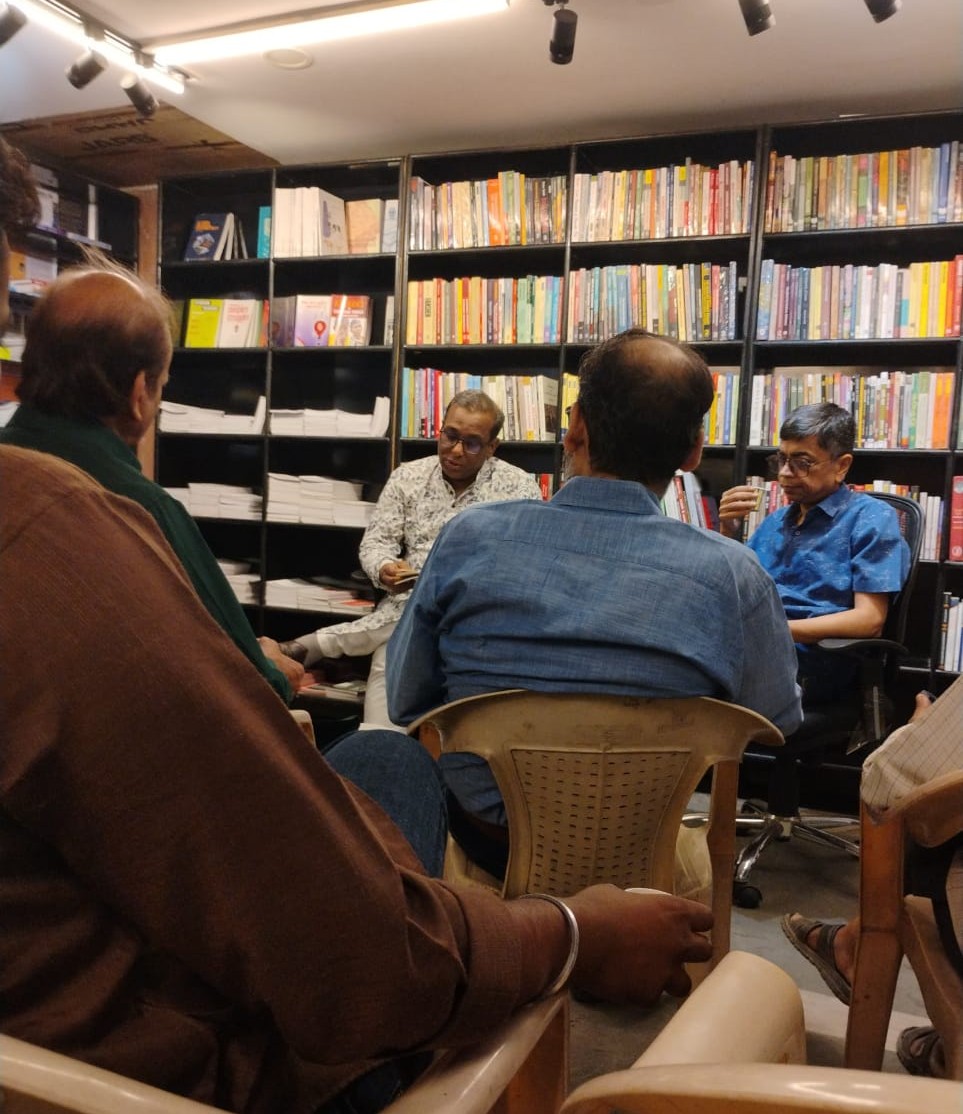पिछले दिनों मैं एक विचित्र स्थापना से गुजरा। एक दलित साहित्यकार का तर्क था कि सावित्रीबाई फुले दलित साहित्य की प्रतीक नहीं हो सकती बल्कि अछूतानंद हरिहर की पत्नी को यह सम्मान मिलना चाहिए। इस हास्यास्पद तर्क के बरक्स हमारे सामने डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर द्वारा बुद्ध, कबीर और जोतिबा फुले को अपना आदर्श बताए जाने का सत्य है जबकि इनमें से कोई भी दलित नहीं था। इस पृष्ठभूमि में सवाल यह बनता है कि हिन्दी का दलित साहित्य आन्दोलन कहां पहुंचा है और क्या यह महात्मा फुले के शब्दों में ‘अतिशूद्रों’का सहित्य भर रह गया है ? सवाल यह भी है कि जिस वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ दलित साहित्य का अभ्युदय हुआ, उसके शिकार शूद्रों की पीड़ा या उनके संघर्ष और अभिव्यक्ति को शामिल किए बिना क्या दलित साहित्य ब्राहमणवाद के खिलाफ साहित्यिक-सांस्कृतिक विकल्प दे सकेगा? और इसी कारण शूद्रों-अतिशूद्रों व आदिवासियों के साझे संघर्ष के साहित्य की अवधारणा की जरूरत है। इसको ‘बहुजन साहित्य’कहा जा सकता है, कहा जा रहा है या फुले-आम्बेडकरी साहित्य कहा जा सकता है।
यदि बहुजन साहित्य की अवधारणा है तो अवश्य ही द्विज साहित्य का भी अस्तित्व है। यद्यपि द्विज साहित्य नाम की कोई घोषित श्रेणी नहीं है परंतु साहित्य में प्रतीकों, बिम्बों, भाषा, परिवेश और उद्देश्य, जिसके तहत चातुर्वर्ण और वर्णाश्रम धर्म का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन होता है, के आधार पर द्विज साहित्य की पहचान की जा सकती है। वहीं बहुजन साहित्य के प्रतीक, बिम्ब, भाषा और परिवेश बहुजन समाज के होंगे और उद्देश्य, चातुर्वर्ण और वर्णाश्रम धर्म के विरोध के साथ-साथ बहुजन संघर्षों व स्वप्नों की अभिव्यक्ति होगा। यह तो बहुजन साहित्य की मूल प्रवृत्ति होगी परंतु यदि बहुजन साहित्य की अवधारणा आकार ले रही है तो उसका सौन्दर्यशास्त्र भी विकसित किया जाना चाहिए।
बहुजन सौन्दर्यशास्त्र की कसौटी पर ही बहुजन साहित्य को कसा जाना चाहिए अन्यथा कोई भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के साथ बहुजन साहित्य में ही योगदान कर रहा होगा।
पिछड़ी जाति के मौजूदा परिवेश को भी देखा जाना चाहिए। दिखता तो यह है कि पिछड़ी जातियों में ब्राह्मणवाद ने खूब पैठ बना रखी है।  पिछड़ी जातियां, दलितों की तुलना में सांस्कृतिक वर्चस्व और नियतिवाद से ज्यादा ग्रस्त हैं। यदि पिछड़ी जाति के किसी साहित्यकार में नियतिवाद या सांस्कृतिक वर्चस्व या चातुर्वर्ण के प्रति समर्पण दिखता है, तो क्या उसे ‘बहुजन साहित्य’कहा जा सकेगा ? दूसरी ओर, ‘बहुजन साहित्य’के लिए फुले-आम्बेडकरी चेतना का होना भी जरूरी है और ऐसा है तो फिर सवाल खड़ा होगा कि अगर जन्मना द्विज साहित्यकार में फुले-आम्बेडकरी चेतना है और ब्राहमणवाद तथा वर्णाश्रम के प्रति निषेध है, तो क्या उसका साहित्य बहुजन साहित्य के दायरे में आएगा ? इन सारे सवालों का जवाब बहुजन साहित्य की अवधारणा के प्रणेताओं को अवश्य देना चाहिए।
पिछड़ी जातियां, दलितों की तुलना में सांस्कृतिक वर्चस्व और नियतिवाद से ज्यादा ग्रस्त हैं। यदि पिछड़ी जाति के किसी साहित्यकार में नियतिवाद या सांस्कृतिक वर्चस्व या चातुर्वर्ण के प्रति समर्पण दिखता है, तो क्या उसे ‘बहुजन साहित्य’कहा जा सकेगा ? दूसरी ओर, ‘बहुजन साहित्य’के लिए फुले-आम्बेडकरी चेतना का होना भी जरूरी है और ऐसा है तो फिर सवाल खड़ा होगा कि अगर जन्मना द्विज साहित्यकार में फुले-आम्बेडकरी चेतना है और ब्राहमणवाद तथा वर्णाश्रम के प्रति निषेध है, तो क्या उसका साहित्य बहुजन साहित्य के दायरे में आएगा ? इन सारे सवालों का जवाब बहुजन साहित्य की अवधारणा के प्रणेताओं को अवश्य देना चाहिए।
दरअसल, हमारे बीच किसी भी नई पहल को सिरे से नकारने की प्रवृत्ति होती है। हिन्दू मिथकों के विरुद्ध प्रतिमिथक गढने के प्रयास हो रहे हैं। यह एक सामाजिक यथार्थ है जिसे नकारा नहीं जा सकता। महिषासुर की पूजा हो या होलिका का पुनर्पाठ या महाराष्ट्र में महान बहुजन विभूतियों से संबंधित दिवसों को समर्पित दशहरा हो, या ‘बली राजा,’का त्योहार-ये सब वैकल्पिक सांस्कृतिक प्रयास हैं। यह सांस्कृतिक चेतना या ब्राहमणवाद से टकराने वाले ऐसे दूसरे सांस्कृतिक प्रयास जिस साहित्य में दर्ज होंगे, वह बहुजन साहित्य ही तो होगा। बहुजन साहित्य को दलित साहित्य के साथ और उसके विस्तार के रूप में विकसित होना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है कि यह दलित साहित्य आन्दोलन के खिलाफ न खड़ा हो जाए। इस अवधारणा के सूत्रधारों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। यह ‘फारवर्ड प्रेस’का बहुजन साहित्य अंक है पिछड़ी जातियों में ब्राह्मणवाद ने खूब पैठ बना रखा है। पिछड़ी जातियां, दलितों की तुलना में सांस्कृतिक वर्चस्व और नियतिवाद से ज्यादा ग्रस्त हैं। क्यों न अगले वर्ष बहुजन साहित्य के कुछ मानक और बहुजन साहित्य सौन्दर्यशास्त्र की नींव के साथ-साथ कुछ प्रचलित साहित्यिक कृतियों की आलोचना प्रकाशित की जाए। एक मुक्कमल सौन्दर्यशास्त्र के लिए यह भी तो जरूरी है।
(फारवर्ड प्रेस, बहुजन साहित्य वार्षिक, मई, 2014 अंक में प्रकाशित )
(बहुजन साहित्य से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें ‘फॉरवर्ड प्रेस बुक्स’ की किताब ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ (हिंदी संस्करण) अमेजन से घर बैठे मंगवाएं . http://www.amazon.in/dp/