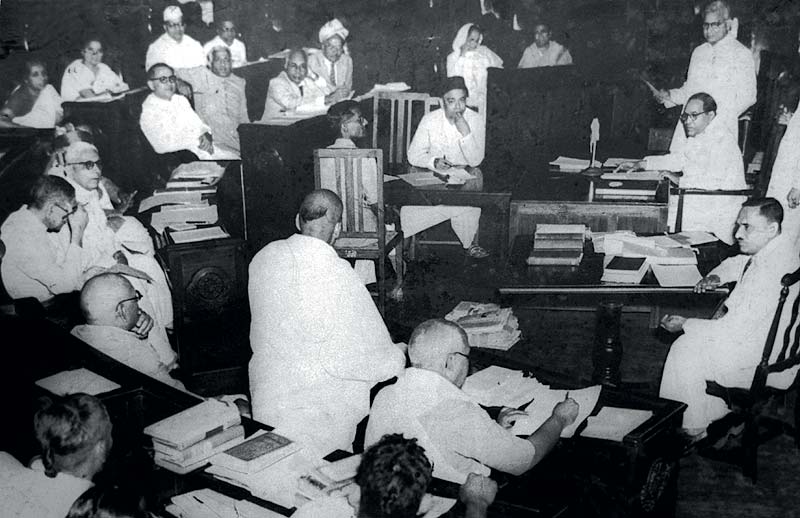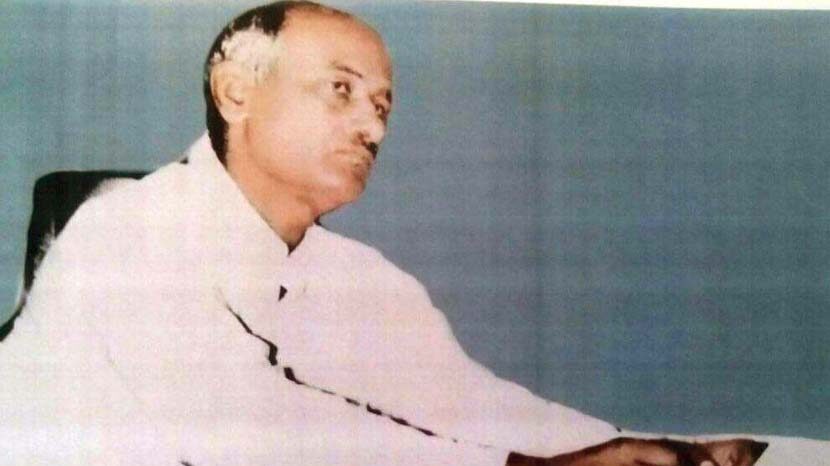मुद्राराक्षस की पुस्तक ‘धर्मग्रंथों का पुनर्पाठ’ का अवलोकन
मुद्राराक्षस की बहुत बेहतरीन, विवेक पर लगातार रन्दा चलाने वाली, सदैव ज़रूरी और प्रासंगिक किताब है, ‘धर्मग्रन्थों का पुनर्पाठ’; जिसके अब तक कई संस्करण आ चुके हैं। यह किताब प्रमाणित करती है कि मुद्राजी का अध्ययन-चिन्तन कितना व्यापक, गहरा और अग्रगामी दृष्टि से सम्पन्न था।
इस पुस्तक की पहली और लगभग सर्वोपरि विषेशता यह है कि यह आद्यंत बहुत ही सावधानी, प्रमाणिकता और निर्भीकता के साथ लिखी गई है। हवा में कुछ नहीं है, बल्कि कहना यह चाहिए कि हज़ारों सालों की ब्राह्मणवादी हवाबाज़ी को बहुत गहरे और विस्तार में जाकर निर्मूल किया गया है। मुद्राजी इसमें रामविलास शर्मा से टकराते हैं और उनके वेद, महाभारत सम्बन्धी अध्ययन की चिन्दियाँ बिखेर देते हैं। रामविलासजी से टकराने का साहस और विषद अध्ययन हिन्दी में इक्का-दुक्का लोगों के पास ही रहा है। मुद्राजी के विवेचन में प्रामाणिकता, तुर्षी और अकाट्यता इसलिए आई क्योंकि उन्होंने सन्दर्भित समस्त ग्रन्थों की सीधे मूल प्रतियाँ, मूल किताबें देखी थीं और तब उस मूल पाठ का पुनर्पाठ-दरअसल असल पाठ-प्रस्तुत किया। (धर्मग्रंथों का पुनर्पाठ, साहित्य उपक्रम, संस्करण 2009; पृ. 221)।

इस पुस्तक की दूसरी बड़ी विषेशता यह है कि यह संदर्भित धर्मग्रन्थों का पाठ करते हुए उनके रचनाकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि स्थितियों, परिस्थितियों का अनिवार्यत: ध्यान रखकर चली है। तत्कालीन स्थितियों परिस्थितियों के मद्देनज़र उन्हें समझा-समझाया गया है। मुद्राजी ने इस पुस्तक में एक जगह लिखा है-‘‘वेद पढ़ते या उसके अनुवाद उद्धृत करते समय उस काल की सम्पूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति देखनी चाहिए जो वेदेतर तमाम साहित्यों में मिलती है।’’ (वही, पृ.190)। इसका एक परिणाम तो यह हुआ है कि समय-सापेक्ष इतिहास-दृष्टि निर्मित हो सकी और दूसरा और बड़ा अग्रगामी परिणाम यह हुआ कि परम्परा में अंतर्व्याप्त ब्राह्मणतन्त्रीय सर्वसत्तवाद, चालाकियों, दुरभिसन्धियों, धूर्तताओं, लम्पटताओं, अहमन्यताओं इत्यादि के लगभग अबूझ-से चेहरे एकदम साफ़ और खरे उभरते दिखाई दिए, कि पाठक की आँखे जैसे भड़भड़ाकर खुल जाएँ! जैसे इतिहास का और अतीत का कच्चा नंगा चिट्ठा पटपटाकर हमारे सामने खुलने लगे और हम गश खाते-खाते यक़ायक़ स्तम्भित हो लें! यह किताब एक निर्मम आरी की तरह हमारी अब तक की सारी पूर्वावधारणओं को बेतरह काटती चलती है। हमें इसका अन्देशा तो था और इससे पहले भी इस तरह की बातें देखने सुनने में आई थीं, लेकिन हिन्दी के एक रचनात्मक लेखक की ओर से यह पहली और शायद एकमात्र किताब है, जो हमारे यहाँ के कथित धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, महाख्यानात्मक ग्रन्थों का ऐसा खुलकर असल रहस्योद्घाटन करती हो! आचार्य नामवर सिंह और इनके सम्प्रदाय के लोग देखें कि ‘दूसरी परम्परा’ की खोज कैसे की जाती है!
मुझे नहीं पता कि हिन्दी के किसी अन्य लेखक, चिन्तक ने हिन्दी भाषा के विषय में इस तरह की कोई आत्मनिरीक्षणात्मक और इतिहासपुष्ट टिप्पणी की हो; अब तक तो हमें यही सिखाया-पढ़ाया गया है कि हिन्दी आमजन की, संघर्षचेतना की भाषा रही है, पर यह एक बिल्कुल ही नई बात है, जो मुद्राराक्षस कहते हैं-‘‘हिन्दी भाषा का जन्म भी ब्राह्मण साम्प्रदायिकता और पूर्वग्रह से ही हुआ था।’’(वही, पृ0 221) इस एक निष्कर्ष से अन्य निष्कर्ष प्रभावित हों, यह स्वाभाविक ही है।
मुद्राजी ने इस पुस्तक में हमारे यहाँ के धर्मग्रन्थों के पुनर्पाठ के माध्यम से हमारे यहाँ की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि लगभग समस्त परम्पराओं का पुनर्पाठ प्रस्तुत किया है और हमें चुनौती दी है कि हम देखें कि हमारे यहाँ किस तरह का वैचारिक, भावमूलक, अकादमिक घालमेल मूल रचना और उसके निर्वचन में किए जाते रहने की शैतान की आँत जैसी लम्बी दुराग्रही और दुष्टतापूर्ण और हिंसक परम्परा रही है। मुद्राजी ऐसा दरअसल इसलिए कर पाए कि उनका प्रस्थान-बिन्दु ही यह रहा है कि किसी रचना के पीछे का मक़सद क्या रहा हो सकता है? वह किन लोगों, किस वर्ग-समूह को सम्बोधित है? वह इन लोगों की आकांक्षाओं, मंशाओं के हित में क्या शिल्प-प्रविधि अपनाती है; इत्यादि। मुद्राजी बात यहाँ प्राचीन साहित्य के रचनाकाल के निर्धारण की कर रहे हैं लेकिन प्रकारान्तर से वे इन रचनाओं की समकालीनता की पड़ताल का सिलसिला ही जारी रखे हुए हैं: ‘‘हमारी नजर से भारत की प्राचीन किताबों के लेखनकाल का सबसे निर्णायक तत्व होना चाहिए रचना की सामाजिक सांस्कृतिक जरूरत। रचना अपने समय के किन लोगों की कौन-सी उम्मीदें पूरी करती है और इस काम में वह रचना किन तत्वों को इस्तेमाल में लाती है।’’ (वही, पृ. 212)।
मुद्राजी का भारत की पुरानी किताबों की समकालीनता की पड़ताल का यह सिलसिला अनवरत और ताल ठोंकू अन्दाज़ में इस किताब में चलता है। समकालीनता के साथ-साथ आने वाले समय में किस पर इनका कैसा क्या प्रभाव था, किसको इनसे क्या-क्या फ़ायदा-नुकसान हुआ, इसका भी हिसाब वे लेते चले हैं। वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रन्थों तक लगातार एक ही लक्ष्य इन लोगों का रहा; ब्राह्मण तन्त्र की स्थापना और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्चस्व का निर्माण। इस सम्बन्ध में इस पुस्तक के कुछ सूत्र वाक्य निम्नानुसार लिए जा सकते हैं-
1. ईसापूर्व, विशेषकर बुद्ध और उनसे पहले का समय भारतीय विचार परम्परा में दो हिस्सों में स्पष्ट रूप से बँटा देखा जा सकता है। एक पक्ष वह है जो तर्क, जिज्ञासा और शंका पर आधारित है और दूसरा वह, जो आस्था और उपासना पर केन्द्रित रहा है। उपासना और आस्था केन्द्रित साहित्य मुख्यतः ब्राह्मण साहित्य है। उपनिषद इसी परम्परा के दस्तावेज हैं। (वही, पृ. 88-89)। उपनिषदों का बयान बड़े बौद्धिक उत्साह के बावजूद ब्राह्मण पूजा या ब्राह्मण श्रेष्ठता पर ही समाप्त होता रहा है। (वही, पृ. 136)। उपनिषदों में उस समय तक विकसित समृद्ध विचार परम्परा से न सीधा टकराव है, न उसका खण्डन बल्कि अक्सर उपनिषदकार अच्छे चिन्तन के संकेत देने के बाद ब्राह्मण कर्मकाण्ड की अहमियत सिद्ध करने लग जाता है। (वही, पृ. 155)।
ब्राह्मण साहित्य को लेकर कोई भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण साहित्य का सीधा-सा मतलब है ब्राह्मण या ब्राह्मण तन्त्र के अनुयायियों, प्रवाचकों, प्रवक्ताओं द्वारा लिखा गया साहित्य। जिन्हें हम कथित तौर पर हिन्दू धर्म से जुड़ी रचनाएँ मानते-कहते आए हैं, वे लगभग सारी ही ऐसी ही हैं।
2. ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जहाँ सिर्फ ब्राह्मणों के घरेलू ग्रन्थ हैं, वहीं अथर्ववेद ब्राह्मणों द्वारा बाकी समाज को कैसे प्रभावित किया जाए, इसके उपयोग में आने वाली किताब है और वही हुआ भी। (वही, पृ. 100)। ईरान के उत्तर-पश्चिम के प्राचीन मीडियन लोगों की धर्म-पुस्तक जेन्दावेस्त और अथर्ववेद में गहरी समानताएँ है। दोनों ही कबीलाई ओझा चरित्र के ग्रन्थ हैं। (वही, पृ. 99)
3. मनुस्मृति में ऊपरी तौर पर व्यक्ति, परिवार और समाज के करने, न करने लायक काम गिनाए गए हैं। राजसत्ता और ब्राह्मण श्रेष्ठता पर सबसे ज्यादा विस्तार से लिखा गया है, पर इस किताब का मुख्य कथ्य समाज में जाति-व्यवस्था को मजबूत करना, स्त्री जातिमात्र को हीन सिद्ध करना है। संस्कारों पर विस्तार से लिखा जरूर दिखता है, पर वह भी ब्राह्मण तन्त्र को स्थापित करने की नीयत से किया गया है। (वही, पृ. 102)।
4. कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनुस्मृति नामक धर्मशास्त्र, दोनों की भूमिका एक ही है और दोनो ही किताबें उस समाज और राजव्यवस्था का विवरण देती हैं, जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि रहे और सारी राजनीतिक, सामाजिक प्रक्रिया वैसे चले जैसा ब्राह्मण आदेश दे। (वही, पृ. 175)
5. सामान्यतः महाभारत सत्य-असत्य, न्याय-अन्याय जैसे मूल्य निर्धारणों की गाथा है, पर पूरी पुस्तक पर नजर डालने पर एक दूसरी ही बात सामने आती है।स्पष्टता दिख जाता है कि ब्राह्मण को सांस्कृतिक, सामाजिक इतिहास के शिखर पर होना, सिद्ध करना इस किताब का पहला बड़ा मक़सद है। भारत आने के बाद भारतीय समाज के जिस स्वरूप और इतिहास का सामना ब्राह्मण ने किया, उसकी वास्तविक छवि को मिटाना भी ब्राह्मण का दूसरा बड़ा उद्देश्य था। महाभारत द्वारा यही दोनो काम ब्राह्मण शिद्दत से करता है। (वही, पृ. 201)
6. गीता एक तरह से वेदान्त और भागवत का समन्वित रूप है। वेदान्त ही बड़ी आसानी से उन वल्लभाचार्य तक पहुँच जाता है जो भक्ति-आन्दोलन के सबसे बड़े और प्रखर प्रतिष्ठता थे। गीता और भागवत दोनों ग्रन्थ या तो एक-दूसरे के पूरक हैं या आपस में समन्वित होने पर भक्ति-दर्श्न बन जाते हैं। यह एक बड़ी वैचारिक भ्रान्ति है कि गीता एक सुव्यवस्थित दार्शनिक चिन्तन है। वस्तुतः यह कृष्ण-भक्ति को ही महिमामण्डित करने वाली एक रचना है। (वही, पृ.194-95)।
7. जिस तरह गीता का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण तन्त्र के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति है, ठीक उसी तरह महाभारत का मुख्य कथ्य ब्राह्मण तन्त्र की प्रतिष्ठा ही है। (वही, पृ. 206)।
इस पुस्तक के ‘गीता का पुनर्पाठ’ अध्याय पर अलग से विस्तार के साथ विचार की ज़रूरत है, जो पाँच उपबिन्दुओं में विभाजित है। इस अध्याय से गीता के बारे में हमारे कई भ्रम दूर हो सकते हैं। इनमें ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ इत्यादि प्रसिद्ध श्लोक की व्याख्या अद्भुत और ऐतिहासिक महत्व की है। (द्रष्टव्य, वही, पृ. 197)।

संस्कृत के रचनात्मक साहित्य के बारे में मुद्राजी जो टिप्पणियाँ करते हैं, वे भी अच्छी-ख़ासी खराद पर चढ़ी हुई-सी लगती हैं। मसलन यह कि ‘‘संस्कृत साहित्य, जो भास से शुरू होता है, मृच्छकटिकम् जैसे बिरले अपवाद को छोड़कर प्राचीन ब्राह्मणग्रन्थों, पुराणों और महाकाव्यों के कथानकों को लेकर ब्राह्मण संस्कृति और कर्मकाण्ड की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए लिखा गया।’’ (वही, पृ. 174)। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्योद्घाटन इस साहित्य में स्त्री के उपस्थापन को लेकर किया गया है। जिसे कथित रूप से हम प्रेम कहते आए हैं, अपने वास्तविक प्ररूप में वह कुछ और ही है। मुद्राजी लिखते हैं-‘‘इस समूचे साहित्य का प्रमुख लक्ष्य शायद वात्स्यायन के कामसूत्र के प्रभाव में स्त्री-भोग को सबसे ज्यादा जगह देना रहा है। अगर देवियों का जिक्र भी है तो अभूतपूर्व यौन आनन्द के लिए, जैसे कुमार सम्भवम् या गीत गोविन्दम्।’’ (वही)। इस क्रम में सबसे दिलचस्प यह तथ्यानुसन्धान है, जो साहित्य की परिस्थिति-सापेक्षता की अवधारणा के तहत है-‘‘सम्भव है स्त्री को ब्राह्मण संस्कृति जैसे अत्यन्त नीचे के दर्जे पर रखती रही है, उसी तरह उसके नग्नतम भोग की भी समर्थक रही हो। आखिर अश्वमेध जैसे अनुष्ठानों में रानी के स्तर की स्त्री को लेकर भी ब्राह्मण जैसी नग्नता का आचरण करता रहा है, उसके चलते कविता में स्त्री के साथ यही सुलूक असामान्य नहीं कहा जा सकता। शायद ब्राह्मण की यही कामलिप्सा संस्कृत भाषा के साहित्य में अश्लीलता की हद तक पहुँचकर व्यक्त होती है।’’ (वही)।
धर्मग्रन्थों के मार्फ़त प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति पर विचार इस पुस्तक का एक प्रमुख एजेण्डा रहा है। न केवल स्त्री, बल्कि ब्राह्मण तन्त्र द्वारा ज़बर्दस्ती हाशिये पर धकेले गए भारतीय समाज के अन्य वर्गों-जिनमें शूद्र कही गई जातियाँ प्रमुख हैं-की नियति का भी पुनरवलोकन इस पुस्तक की केन्द्रीय चिन्ताओं में सर्वप्रमुख रहा है। इस सम्बन्ध में मुद्राजी के इन दो अभिमतों का उल्लेख लगभग अनिवार्य है। इनमें एक तो स्त्री और गैर-सवर्ण मूलवासी समाज के प्रति धर्मग्रन्थों के रवैये पर है और दूसरा शूद्र-समस्या के प्रति हमारे यहाँ के वामपन्थियों के रवैये और स्टैण्ड पर है-
- ईसा से कोई छह-सात सदी पहले से लेकर उन्नीसवीं सदी के शुरू तक ब्राह्मण समुदाय लगातार इस दिशा में काम करता रहा। इन सभी धर्मग्रन्थों का मूल उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करना बताया गया है। पर समाज को व्यवस्थित करने के तथाकथित उद्देश्य से लिखे गए इन धर्मग्रन्थों का मकसद रहा है स्त्री और गैर-सवर्ण मूलवासी समाज का खून चूसना और उनका बेजा लाभ उठाते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को समृद्धि शिखर पर बनाए रखना। (वही, पृ. 118)।
- वामपंथ ने भारतीय इतिहास के इस पहलू का सही भाष्य कभी नहीं किया। वामपन्थ शूद्र-समस्या को 90 फीसदी भारतीयों की नहीं, एक चौथाई समाज की समस्या मानकर चलता है। शूद्र की समस्या वामपन्थ सिर्फ अस्पृश्यता मानता है या एक धार्मिक सांस्कृतिक विकार। वामपन्थ नहीं देखता कि दस करोड़ लोगों के धर्मग्रन्थ बाकी सारे 90 करोड़ को शूद्र मानते हैं। वामपन्थ यह भी नहीं समझना चाहता कि शूद्र ही मजदूर हैं, यह हिन्दू धर्मग्रन्थ भी मानते हैं। शूद्र आदोलन ही वास्तविक मजदूर आन्दोलन है, यह न समझना वामपन्थ की सबसे बड़ी राजनीतिक असफलता है। (वही, पृ. 130)।
इस पुस्तक में मुद्राजी प्रास्थानिक तौर पर इतिहासवेत्ताओं की इस बहुप्रचलित मान्यता का खण्डन करते हैं कि आर्य कहीं बाहर से आए थे। बल्कि इसके स्थान पर वे एक बिल्कुल नई और पर्याप्त तर्कसंगत स्थापना देते हैं कि दरअसल ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग ही बाहर से आए थे। मुद्राजी की स्थापना यह भी है कि आर्य यहीं का कुलीन या लेजर क्लास था, जिस पर हिंसा और धार्मिक अन्धविश्वास और कर्मकाण्ड के ज़रिए बाहर से आए ब्राह्मणों ने अपना प्रभुत्व और वर्चस्व स्थापित किया। मुद्राजी की एक और मौलिक स्थापना यह है कि भारतीय भूभाग में शूद्र कोई नहीं था; ब्राह्मणों ने अपने प्रभुत्व में आए राजनीतिक, आर्थिक सत्ताधारियों के मार्फ़त उस समय के विशाल श्रमशील कामगार, किसान, दस्तकार वर्ग को शूद्र घोषित करते हुए उनके समस्त राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और यहाँ तक कि न्यूनतम मानवाधिकार भी छीन लिए और उन्हें बेतरह जन्मजन्मान्तर तक भयावह हाशिए पर धकेल दिया। यह आकस्मिक नहीं है कि इस पुस्तक में बाहर से आकर यहाँ अपनी सर्वसत्ता स्थापित करने वाले ब्राह्मणों की तुलना बार-बार अँग्रेज़ों से की गई है। जैसे अँग्रेज़ों ने यहाँ प्रभुत्व स्थापित करते हुए संस्कृति को हथियार बनाया था, ठीक वही काम यहाँ आकर ब्राह्मणों ने किया। मुद्राजी लिखते हैं-‘‘भारत में शासन पर अधिकार हो जाने के बाद बर्तानिया स्थित अंग्रेज जाति ने अपनी सत्ता को मज़बूत करने के लिए संस्कृति को बड़ा साधन बनाया था। उसने धीरे-धीरे नाटक, साहित्य, शिक्षातन्त्र, राजतन्त्र, अर्थतन्त्र में सीधे हस्तक्षेप किया था। ठीक यही काम ब्राह्मण ने भारत में ईसवी सन् के आसपास शुरू किया। (वही, पृ.175)।
इस समीक्षा का समापन मुद्राजी द्वारा प्रयुक्त दो महत्वपूर्ण प्रत्ययों के उल्लेख के साथ किया जाना उपयुक्त होगा। इसमें एक है-‘सोशल डार्विनिज्म’ (वही, पृ. 150) तथा दूसरा है-‘समाज को नाबालिग बनाना’ (वही, पृ. 151)। ये दोनों ही प्रत्यय ‘उपनिषद् पुनरीक्षण’ शीर्षक अध्याय में प्रयुक्त हुए हैं और लगभग साथ-साथ आए हैं। ये दोनों काम ब्राह्मण ने किए। बीसवीं शताब्दी के मध्य में वामपन्थ-विरोधी अभियान के तहत पूँजीवादी व्यवस्था के पक्षकारों-सोशल डार्विनिस्ट विचारकों-द्वारा सामाजिक, आर्थिक समानता के विरुद्ध जो कुछ किया गया, बुद्ध पूर्व और बुद्ध युग के ब्राह्मण विचारकों ने भी ठीक यही किया। (वही, पृ. 150-51)। इसी विवेचन के क्रम में मुद्राजी ने नाबालिग शब्द का कुछ इस तरह इस्तेमाल किया-‘‘वेदोत्तर काल का ब्राह्मण समाज को इसी तरह नाबालिग रखना चाहता है। धर्मतन्त्र इस काम में उसकी सबसे बड़ी मदद करता है। गगग धर्मतन्त्र समाज को नाबालिग बनाने की सबसे बड़ी मशीन होता है।’’ (वही, पृ. 151)। नाबालिग कितना दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है, हम समझ सकते हैं।
मुद्रराक्षस की यह किताब समय की निरन्तरता और समय-सापेक्षता की कसौटियों पर इतिहास के विज्ञ पुनरीक्षण और पुनर्लेखन का बेहतरीन उदाहरण है।
बहुजन साहित्य से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए फॉरवर्ड प्रेस की किताब बहुजन साहित्य की प्रस्तावना, देखें। यह हिंदी के अतरिक्त अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। प्रकाशक, द मार्जिनलाइज्ड, दिल्ली, फ़ोन : +919968527911
ऑनलाइन आर्डर करने के लिए यहाँ जाएँ: अमेजन, और फ्लिपकार्ट। इस किताब के अंग्रेजी संस्करण भी Amazon और Flipkart पर उपलब्ध हैं।